मुझे यक़ीन है कि अब वह कभी लौटकर नहीं आएँगे
 हिन्दवी डेस्क
06 अगस्त 2024
हिन्दवी डेस्क
06 अगस्त 2024
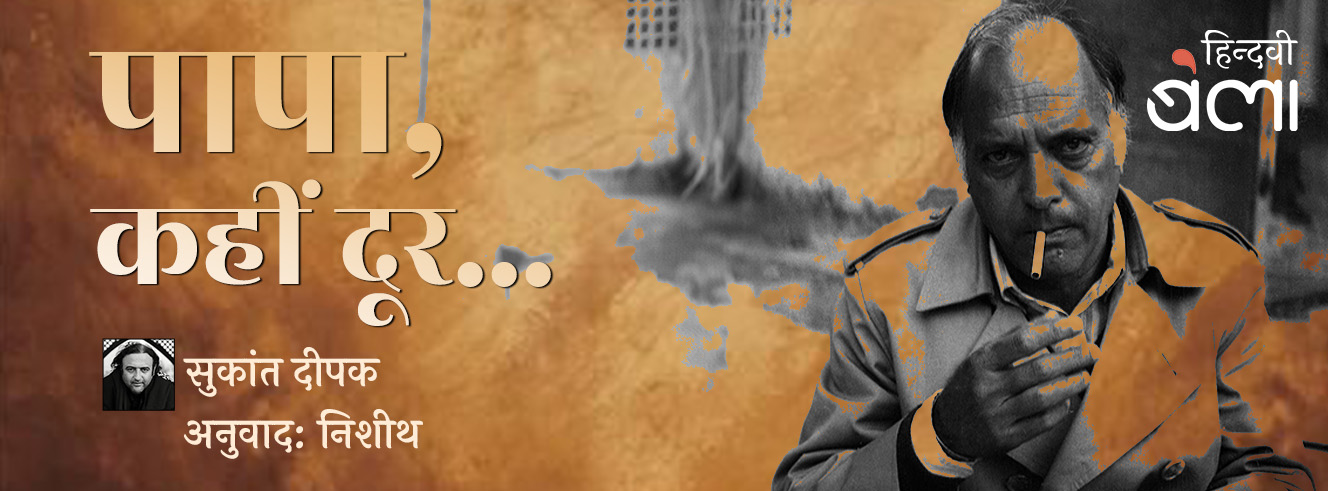
तड़के तीन से साढ़े तीन बजे के बीच वह मेरे कमरे पर दस्तक देते, जिसमें भीतर से सिटकनी लगी होती थी। वह मेरा नाम पुकारते, बल्कि फुसफुसाते। कुछ देर तक मैं ऐसे दिखावा करता, मानो मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा हो। फिर वह बेधड़क दरवाज़ा पीटने लगते। मैं बिस्तर से उठकर दरवाज़े के क़रीब जाता, मगर खोलता नहीं। वह गिड़गिड़ाते, “मेरा सिर उस सरिये से फोड़ दो। मुझे मालूम है तुम अपने पलंग के नीचे सरिया रखते हो। मारो मुझे।” और हर बार की तरह मैं उनसे कहता, ‘‘दफ़ा हो जाइए यहाँ से।’’ कहना न होगा कि मैंने उनके साथ ऐसा बर्ताव किया, जैसा लोग-बाग अपने पालतू कुत्ते के साथ भी नहीं करते।
एक रोज़ 7 जून 2006 की सुबह, वह सैर पर निकले और फिर कभी नहीं लौटे। जब हम―मेरी माँ, बहन और मैं―आश्वस्त हो गए कि अब वह वापस नहीं आने वाले, तो हमने एक साथ राहत की साँस ली। कहना चाहिए कि लगभग जश्न का माहौल था, मानो कोई बला टल गई हो।
“मुझे उम्मीद है कि हम उनकी शक्ल अब दुबारा नहीं देखेंगे”—मेरी बहन ने कहा। मैं और माँ भी यही चाहते थे। यूँ तो आजीविका के लिए माँ केमिस्ट्री पढ़ाती थीं, मगर वह कला-सृजन की घोर प्रशंसक थीं।
(यहाँ तक कि वह हुसैन की चित्रकारी की हूबहू नक़ल कर सकती थीं।)
स्वदेश दीपक के बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षणों को 1990 के दशक में पहचाना गया। इस समय तक वह अपने परिवार, यार-दोस्तों और सगे-संबंधियों द्वारा एक घृणित और तिरस्कृत व्यक्ति के तौर पर देखे जाने लगे थे। यह लोकप्रिय लेखक, जिसे वर्ष 2004 में संगीत नाटक अकादेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अपने कमरे में क्वीन-साइज़ बिस्तर पर लेटे-लेटे घंटों छत को घूरता रहता था। मैं उनके कमरे के भीतर झाँकता, न डरने का नाटक करता और वापस अपने कमरे में चला जाता। उनके लिए प्रार्थना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। उन दिनों मेरे कमरे की दीवारें मार्क्स और लेनिन के पोस्टरों से भरी रहती थीं, जिसमें एक छोटी-सी जगह बिकिनी पहने सिंडी क्रॉफ़र्ड ने भी घेर रखी थी।
उन्होंने आत्महत्या का पहला प्रयास साल 1999 में किया था। एक रात ग़ुस्लख़ाने में भयानक शोर मचा हुआ था। माँ और बहन भागकर वहाँ पहुँचीं। जगा तो मैं भी था, मगर अपनी जगह से हिला तक नहीं। रात हो चुकी थी, इस समय मुझे ऐसी चीज़ों से बेख़बर होकर, गहरी नींद में होना चाहिए था। मेरी चचेरी बहन—जो पेशे से एक डॉक्टर थी—को बुलाया गया। वह अपने पति के साथ आई, वह भी पेशे से डॉक्टर ही थे। दोनों अभी भी नींद में थे, मगर उस नाज़ुक समय में उन्होंने वही किया, जिसकी उनसे उम्मीद की गयी थी। उन्होंने मिलकर उनके आत्महत्या करने के प्रयास को नाकाम कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम क़रीब दो घंटे तक चला और इस दौरान मैं अपनी जगह से इंच भर भी नहीं हिला।
मेरी डॉक्टर बहन ने तय किया कि अब बिना किसी देरी के इन्हें मनोचिकित्सक के पास ले जाने का समय आ गया है। उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जो अंबाला से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर था। अंबाला―जहाँ हम रहते थे (जिस घर में मैं अब भी रहता हूँ)। वहाँ उन्हें कुछ गोलियाँ दी गईं। गोलियाँ लेकर वह दिन भर बेसुध होकर सोते रहे। कुछ ही दिनों बाद, उन्होंने गोलियाँ लेना बंद कर दिया। एक बार फिर कष्ट सहने की घड़ी आ गई थी―और इस बार उन्हें यह अकेले नहीं झेलना था।
वर्ष 1991 में उन्होंने बहुचर्चित हिंदी नाटक ‘कोर्ट मार्शल’ लिखा था। कलकत्ता में नाटक के पहले शो के दौरान उनकी मुलाक़ात एक महिला से हुई, जिसे उन्होंने ‘मायाविनी’ कहा। वह उसे आजीवन भूल नहीं पाए। मुझे याद है कि एक बार मैंने उनसे इस शब्द (मायाविनी) का अँग्रेज़ी अनुवाद पूछा था। उन्होंने मेरी आँखों में देखते हुए कहा था—“क्या वाक़ई तुम्हें लगता है कि अँग्रेज़ी इतनी समृद्ध भाषा है कि मायाविनी की जादुई-शक्ति को अपने भीतर समायोजित कर सके?” यह बात उस शख़्स ने कही थी, जिसने अंबाला के एक कॉलेज में छब्बीस वर्षों तक एम.ए. इंग्लिश की कक्षाएँ ली थीं।
(हालाँकि, मुझे ‘मायाविनी’ के लिए अपने अनगढ़ और अधूरे अनुवाद से ही संतोष करना पड़ा : The seductress of illusion.)
मुझे यह भी याद आता है कि मैंने उनसे पूछा था कि आप अस्वस्थ क्यों हैं? आख़िर, उनको किस बात की तकलीफ़ है? जब डॉक्टरों ने कहा है कि इस बीमारी का इलाज किया जा सकता है, तो वह दवाएँ क्यों नहीं लेते? उन्होंने कहा—“वैसे, तुम्हारा सवाल अच्छा है। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि काले जादू का इलाज किया जा सकता है? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इसका इलाज किया जाना चाहिए, वह भी कमबख़्त कुछ गोलियों से? मैं बीमार हूँ क्योंकि मैंने उसका अपमान किया, क्योंकि मैं उसके प्रेम के प्रति समान भाव रखने में चूक गया।”
“तो क्या मुझे कभी किसी स्त्री का प्रेम-प्रस्ताव ठुकराना नहीं चाहिए?”
“देखो, ऐसी स्थिति केवल तभी बनती है, जब स्त्रियाँ तुम्हारा प्रेम पाने की इच्छुक हों और तुममें दिलचस्पी दिखाएँ। तुम्हारे लक्षण बहुत अच्छे हैं। तुम एकदम निर्मल हो—अपनी माँ की तरह। तुम्हारे अंदर मेरा भदेसपन, बदज़ुबानी, अनगढ़ता और वह आकर्षण नहीं है; जिससे लोग सम्मोहित हो उठते हैं। केवल वही स्त्रियाँ तुम्हारे प्रति आसक्त होंगी, जिन्हें काला जादू न आता हो। एक तरह से देखा जाए तो तुम लकी हो। लेकिन मज़ाक़ से इतर, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो―अगर किसी स्त्री को तुमसे लगाव हो जाए, उसे तुम्हारा प्रेम चाहिए हो, तो तुम भी उसे उतना ही प्यार देना।”
इतना कहकर उन्होंने ठहाका लगाया। मैं भी हँस पड़ा। उनकी यही निठुराई मुझे बेहद भाती थी, जबकि मेरी माँ और बहन को इससे चिढ़ होती।
इस समय तक उन्होंने कॉलेज जाना बंद कर दिया था, उनका कहना था कि वह अब बहुत थक चुके हैं। शुरुआती वर्षों में, यह बाइपोलर डिसऑर्डर से अधिक अवसाद जैसा लगता था। वह आदमी जिसे अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाना जाता था, जो हमें आघात पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ता था, वह अब बिना किसी चूँ-चपड़ अपनी बेइज़्ज़ती बर्दाश्त कर लेता। माँ स्कूल से वापस आकर उन्हें यह बताना नहीं भूलतीं कि हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन वह उन पर बरस पड़ीं―“मज़ा तो ख़ूब आ रहा होगा न तुम्हें जो घर बैठे-बैठे बीवी की कमाई खाने को मिल जा रही है? ग़ज़ब बेशर्म आदमी हो तुम!” वह स्तब्ध रह गए। उनके मुँह से एक शब्द भी नहीं फूटा। वह धीमी चाल से अपने कमरे में चले गए। कमरा तो क्या, एक अँधेरी खोह थी जो उनकी अनफ़िल्टर्ड सिगरेटों के कसैले धुएँ से अटी हुई थी।
ज़ाहिर है कि मैं माँ का ही साथ देता। उनकी मौजूदगी मेरे लिए विषाक्त हो गई थी। एक आदमी जो शारीरिक रूप से तंदुरुस्त था, वह कैसे यह बहाना कर सकता था कि उसके साथ किसी ने जादू-टोना किया है?
मैं अब कॉलेज में आ गया था, यह वही कॉलेज था, जहाँ वह पढ़ाया करते थे। मैंने कभी नहीं चाहा था कि इस कॉलेज में मेरा दाख़िला हो। मुझे यही एक डर सताता रहता था कि अगर कोई टीचर मुझसे उनके बारे में पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूँगा? एक कारण और था। वह यह कि यह एकदम देसी क़िस्म का कॉलेज था। मेरे अधिकांश यार-दोस्त बड़े शहरों में चले गए थे। मैं कॉलेज में अधिकतर लोगों से बात ही नहीं करता था, यहाँ तक कि टीचरों से भी नहीं। उनमें से अधिकांश तो ऐसे ही थे, जो मेरी क्लास के लड़कों से बहुत अलग नहीं थे―उन्हीं की तरह जाहिल। सिवाय उस एक आदमी के, जिससे पढ़ने का अवसर कभी मेरे हाथ नहीं आया।
एक दिन मैं सिगरेट ख़रीदने के इरादे से बहुत दूर तक पैदल चला गया। लौटकर घर आने पर एक पड़ोसी ने कहा कि फ़ौरन मोंगा अस्पताल चले जाओ। स्वदेश ने ख़ुद को जलाने का प्रयास किया था। मैं वैसा ही शांत बना रहा, मानो मुझे कोई असर ही नहीं हुआ। मैंने बस अपने आपसे कहा―एक और मुसीबत गले पड़ गई।
मैंने अपनी एनफ़ील्ड निकाली और अपेक्षाकृत एक लंबा रूट लेकर सीधे अस्पताल के गेट पर पहुँच गया। मुझे याद नहीं आता कि इस दौरान मैंने कोई जल्दबाज़ी दिखाई हो। आज सोचता हूँ तो यही लगता है कि मेरा इरादा केवल वहाँ बैठे लोगों को डराना था।
माँ उनके साथ ही बैठी थी। डॉक्टर दंपति भी वहाँ पहुँचे हुए थे। वह होश में ही थे। मैंने सीधे उन्हीं से पूछा, “क्या हुआ?”
“मैं ऐसे फ़ालतू सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। जाओ अपना काम करो।”
इस बात पर वहाँ मौजूद महिला डॉक्टर हँस पड़ी और फिर झेंप गई।
मेरा मन हुआ कि अभी के अभी उनको जान से मार डालूँ।
कुछ ही दिनों बाद वह वापस घर आ गए थे।
एक साल बाद उन्होंने मुझे वह घटना याद दिलाई। उन्होंने पूछा कि क्या उस दिन मुझे उनका जवाब इसलिए पसंद नहीं आया, क्योंकि दूसरे अस्पताल से आयी वह ख़ूबसूरत बर्न स्पेशलिस्ट हँस पड़ी थी।
मैंने हामी भरी।
वह मेरे उत्तर से संतुष्ट हुए।
कुछ ही दिनों बाद मैंने इस बात का बदला ले लिया। दरअसल, अँग्रेज़ों के ज़माने का हमारा एक बहुत बड़ा बंगला है, जिसकी काफ़ी समय से मरम्मत नहीं हुई थी। वह कुछ-कुछ वैसा ही दिखता था, जैसा भूतिया फ़िल्मों में देखने को मिलता है। आमतौर पर हम एक छोटे से स्टोर-रूम में कुछेक अतिरिक्त गैस सिलेंडर रखते हैं। (अब भी, जब मैं अकेला रहता हूँ, वे वहीं पड़े हैं।) एक दिन वह उसी स्टोर-रूम में चले गए। जब काफ़ी देर तक वह बाहर नहीं आए तो माँ दबे पाँव―किसी घिसीपिटी हिंदी फ़िल्म के बेढंगे जासूस की तरह―उनके पीछे गईं। तभी एकदम से उनकी चीख़ सुनाई दी। इस बार मैंने फ़ुर्ती दिखाई। वह एक पुरानी माचिस से सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। हालाँकि वह माचिस को ठीक से पकड़ तक नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका दाहिना हाथ अभी भी गलपट्टी में था।
‘‘जाइए अपना काम कीजिए’’―आख़िर मैंने कह ही दिया।
उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से मुझे घूरा।
मैंने उनके हाथ से माचिस छीन ली और डॉक्टर दंपति को फ़ोन करने चला गया। वर्षों तक उनकी संगति में रहते-रहते माँ ने भी हिंदी की एक से बढ़कर एक चुनिंदा गालियाँ सीख ली थीं। उस आदमी को सँभालते हुए, गाहे-बगाहे वह काफ़ी प्रभावी ढंग से उन गालियों का इस्तेमाल करती थीं, जो कभी-कभी अचानक ही एक अजीब-सी ऊर्जा से भर उठता था।
डॉक्टर दंपति ने हाज़िर होने में देर नहीं लगाई। चचेरी बहन के पति हमेशा की तरह शांत और संयमित थे। वह स्वदेश को उनकी स्टडी में लेकर गए और उनसे बिना कोई तारीख़ डाले सुसाइड नोट लिखने के लिए कहा।
मेरे पिता मुस्कुराए और धीमी आवाज़ में कहा, “तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। मगर तुम मेरा लिखा सच होने दोगे न?”
डॉक्टर साहब ने कोई जवाब न देकर सिर्फ़ लिखते रहने का इशारा किया। जैसे ही उन्होंने बोल-बोलकर लिखवाना शुरू किया, स्वदेश भड़क गए और कहा, “मुझे बख़्श दो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे डिक्टेशन की ज़रूरत है, वह भी तुमसे?”
उस वक़्त डॉक्टर की शक्ल देखने लायक़ रही होगी, मगर मुझे अफ़सोस है कि मैं देखने से चूक गया।
माँ ने मेरी बहन को फ़ोन किया, जो तब तक ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ में काम करने लगी थी। बिना कुछ बोले वह चुपचाप सारी बातें सुनती रही। पीजीआई के वरिष्ठ लोगों से संपर्क किया गया। मनोविकार चिकित्सा वार्ड में कोई बेड ख़ाली नहीं था। तब शायद मेरी बहन ने मदद के लिए अपने कलीग्स से गुहार लगाई थी। उच्च पद पर आसीन एक संपादक ने पीजीआई के निदेशक को फ़ोन घुमाया और बर्न वार्ड में स्वदेश के लिए एक बेड और मनोचिकित्सकों के साथ परामर्श की व्यवस्था करने के लिए कहा। सब कुछ इतने क़ायदे और साफ़गोई से हुआ था कि असामान्य लग रहा था।
मैंने तय किया कि अस्पताल में उनसे बहुत ज़्यादा नहीं मिलूँगा। स्कूल से लौटकर माँ सीधे अस्पताल के लिए रवाना हो जातीं, बल्कि एक तरह से वह लगभग वहीं रहने लगी थीं। हमारे परिवार के एक क़रीबी सीनियर पुलिस अफ़सर ने माँ की अनुपस्थिति में, उनके चंडीगढ़ पहुँचने तक वार्ड में एक नियमित गार्ड के रहने की व्यवस्था कर दी थी।
वह चार महीने तक बर्न वार्ड में रहे। उनके घावों के निशान अब तक पूरी तरह नहीं भरे थे, इसलिए उसका इलाज भी साथ-साथ चल रहा था। मगर इस बार किसी ख़ूबसूरत महिला डॉक्टर से नहीं, बल्कि जाने-माने डॉ. चारी से। उनके बारे में अफ़वाह थी कि वे वही डॉक्टर थे, जिन्होंने राजीव गांधी को बम से उड़ाए जाने के बाद उनके चेहरे को देखने लायक़ बना दिया था।
(वैसे बताता चलूँ कि श्रीलंका के आंतरिक मामलों में भारतीय हस्तक्षेप के बाद जो नतीजे सामने आए, उससे स्वदेश बड़े प्रसन्न हुए थे।)
स्वदेश की एक बहन, जिनसे हमारा कोई विशेष लगाव नहीं था (उस डॉक्टर दंपति को छोड़कर, स्वदेश की तरफ़ के किसी भी रिश्तेदार से हमारा उतना मेलजोल नहीं था) ख़ामोशी से प्रार्थना करतीं, अस्पताल में मेरी माँ के साथ रहने लगीं। वह उस पीढ़ी की महिला थीं, जो प्रार्थनाओं में विश्वास करती थी। स्वदेश का मानना था कि उनकी बहन के हाथों में जादुई-स्पर्श था, जो रोगी को भी चंगा-भला कर सकता था। वह इसी ताक में रहते थे कि कब वह उनके माथे पर अपना हाथ फिराती हैं। उनके ऐसा करते ही वह खिल उठते।
स्वदेश का केस वाक़ई दिलचस्प था, जिसपर चर्चा करने के लिए मनोरोग वार्ड में एक विशेष बैठक बुलाई गई। बिरले ही ऐसा होता था, जब डॉक्टरों को हिंदी के एक ऐसे लेखक का इलाज करने का मौक़ा मिले, जिसे अँग्रेज़ी में बात करना पसंद हो और इस गुमान में रहता हो कि लोग उसपर मुग्ध रहते हैं। हर कोई यह केस हथियाना चाहता था या फिर इसी जुगत में था कि कुछ नहीं तो उस टीम का हिस्सा ही बन जाए, जो उन पर हुए काले-जादू का उपचार करने वाली थी।
अंततः दुबले-पतले और छोटे कद के ऐनकधारी डॉ. प्रताप शरण को यह केस सौंपा गया। “कृपा करके कल उनकी सभी कहानियाँ, उपन्यास और नाटक मुझे उपलब्ध कराए जाएँ।”― उन्होंने माँ से कहा। एक ठहराव के साथ उन्होंने अपनी बात को विस्तार दिया, “मुझे यह जानकारी होनी ही चाहिए कि आख़िर मुझे किन चीज़ों से निपटना है।” माँ का कहना था कि वह बता सकती हैं कि उन किताबों में क्या-क्या लिखा है। यह सुनते ही उन्होंने कहा, “मैं भी एक पढ़ा-लिखा आदमी हूँ।” फिर कुछ ठहरकर उन्होंने आगे कहा, “मैं उन्हें पढ़ सकता हूँ। कृपा करके वे किताबें मेरे लिए मँगवा दें।” और फिर उनकी प्रतिक्रिया जाने बग़ैर वह बाहर चले गए।
किताबें मिलने के हफ़्ते भर बाद डॉ. शरण ने स्वदेश से मिलने का निर्णय लिया।
“यहाँ सभी मेरे ख़िलाफ़ हैं। यहाँ कोई मेरी नहीं सुनता। यहाँ किसी को भरोसा नहीं होता कि ये सब मायाविनी का किया-धरा है, मगर उसे कोई सज़ा नहीं मिलनी चाहिए”―स्वदेश ने डॉ. शरण से कहा।
डॉक्टर ने संक्षिप्त वाक्यों में अपनी बात कही। उन्हें अपना ठहराव रास आता था। “मेरा नाम डॉ. प्रताप शरण है। मैं आपका डिफ़ेंस लॉयर हूँ। मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है कि मायाविनी ही आपकी इस हालत की ज़िम्मेदार है। मैं यह भी समझता हूँ कि इसके लिए उसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए।”
यह सुनकर स्वदेश सन्न रह गए। उसी क्षण वे डॉक्टर के मुरीद हो गए।
अंबाला से चंडीगढ़ तक प्रतिदिन चालीस किलोमीटर की थकाऊ यात्रा की साँसत माँ चुपचाप सहती रहीं और बदले में उफ़् तक नहीं किया। एक बार भी नहीं। वह स्वदेश को हर दिन नहलातीं और उनके लिए दवाइयाँ लेने एक अलग इमारत-स्थित केमिस्ट की दुकान पर जाती थीं।
मगर एक दिन स्वदेश ने कहा कि उनके दाँतों में तेज़ दर्द उठ रहा है और वह फट पड़ीं, “तेरा सत्यानाश हो कमीने, देख तूने मेरा क्या हाल करके रख दिया। मैं कभी कितनी ख़ूबसूरत हुआ करती थी और अब मेरी शक्ल किसी भिखारिन से भी गई-गुज़री लगती है। तू कहीं जाकर मर क्यों नहीं जाता!”
एक मरीज़ को देख रहे एक युवा डॉक्टर ने अपने हाथ रोक दिए और वार्ड से बाहर चला गया। अचानक से सन्नाटा पसर गया। किसी मरीज़ के साथ आई, गाँव-देहात की एक बूढ़ी औरत, माँ के पास जाकर बैठ गई और स्नेहपूर्वक उनकी बाँह सहलाती रही। इस दौरान उन्होंने आपस में कोई बात नहीं की।
डॉक्टरों ने अपनी तरफ़ से कोई कसर नहीं छोड़ी और हर चीज़ आज़माकर देख ली, जिसमें इलेक्ट्रो-कन्वल्सिव या कहें कि ‘शॉक थेरेपी’ भी शामिल थी। चार महीने बाद हमसे उन्हें घर ले जाने को कहा गया ताकि वे यह न समझ बैठें कि अस्पताल ही उनकी दुनिया है।
“अब उन्हें यहाँ थोड़ी देर के लिए भी रखना ख़तरे से ख़ाली नहीं होगा।”―डॉ. शरण ने बेहद शांत भाव से कहा।
अक्टूबर में स्वदेश को घर ले आया गया। वह देर तक अपने बग़ीचे को देखते रहे। शरद ऋतु के आगमन से पूरा लॉन पीपल के पत्तों से भर गया था। “घास को घुटन हो रही होगी, तुम्हें बग़ीचे की सफ़ाई करा लेनी चाहिए”―वह कहते रहे―“ऐसा लगता है कि घर पहले से बहुत छोटा हो गया है। और जहाँ मैंने गुलाब के पौधे लगाए थे, वह बग़ीचा कहाँ चला गया?”
कोई भी उन्हें यह बताने के मूड में नहीं था कि उनके लगाए अधिकांश पौधे सूख गए हैं, क्योंकि बाग़ का माली उत्तर प्रदेश स्थित अपने पैतृक गाँव चला गया था। और वैसे भी हमारे पास उस बड़े-से बग़ीचे—जिसने अनावश्यक रूप से जगह घेरी रखी थी—की देखभाल करने से बेहतर काम पड़े थे। मगर किसी ने ज़रूर उन्हें ये सब बताया होगा, क्योंकि मुझे याद है कि उन्होंने अपने में ही बड़बड़ाते हुए कहा था―“मगर कम से कम गुलाबों को तो पानी दिया ही जा सकता था। इतने से काम में किसी का कितना ही समय ख़राब हो जाता।”
एक महीने में ही स्वदेश की हालत में सुधार आने लगा। उन्होंने फिर से सुबह सैर पर जाने की शुरुआत कर दी। वह अपनी पसंदीदा चाय की टपरी पर जाने लगे, जहाँ शाम को दिहाड़ी मज़दूरों का जमावड़ा लगता था। उन्होंने कभी ख़ुद को किसी से अलग या विशिष्ट नहीं समझा। वहाँ आने वाले लोगों में से अधिकांश उनसे भली-भाँति परिचित थे। वह अक्सर उनके लिए सिगरेट का एक एक्स्ट्रा पैकेट ले जाते थे। उनके भीतर का कम्युनिस्ट शायद चाय की उन बैठकों में ही सबसे अधिक जाग उठता था।
घर में रहते हुए, कभी-कभी उन्हें हमारा भी ख़याल आ जाता था। मैं तब तक पक्का शराबी हो चुका था। ज़ाहिर है कि हर कोई इससे चिंतित था। स्वदेश ने मुझे कई बार समझाने की कोशिश की कि समझदारी इसी में है कि पीने की शुरुआत दिन में नहीं, बल्कि शाम को की जाए। मैंने उनके सुझाव पर शायद ही कान धरा और अगले तीन साल तक मैंने अपनी ज़िंदगी को नरक बना लिया।
उनका अनोखा सेंस ऑफ़ ह्यूमर लौट आया था। एक शाम जब मैंने उन्हें बाज़ार में टहलते देखा तो अपनी मोटरसाइकिल रोककर उनसे कहा कि चलिए आपको घर तक छोड़ देता हूँ। क़रीब दस मिनट बाद ही उन्होंने कहा, ‘‘रुक जाओ।’’
“मैंने तुम्हारे लिए 55000/- रुपए फँसाकर यह मोटरसाइकिल इसलिए नहीं ख़रीदी कि तुम इसे रिक्शे की तरह चलाओ। इससे तो अच्छा है कि मैं पैदल ही चला जाऊँ।”
लेकिन सबसे अधिक आश्वस्त करने वाली बात यह थी कि उन्होंने अपना आख़िरी काम, जो कि एक निराली रचना साबित हुई—‘मैंने मांडू नहीं देखा’―लिखना शुरू कर दिया था। इसमें उन्होंने एक मनोरोगी के रूप में अपने वर्षों के अनुभव का विवरण दिया था। मैं उस पुस्तक के अध्यायों को सुनने वाला पहला व्यक्ति था। उनकी समस्त कथाओं में एकछत्र राज करने वाले सर्वव्यापी एकाकी नायक की जगह अब एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली थी, जो अपने मस्तिष्क के भीतर के प्रेतों से संघर्ष कर रहा था। वहाँ किसी के लिए कोई दुर्भावना नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनिया के प्रति एक भयावह नीरवता थी। अपनी स्टडी में घंटों बिताते हुए वह जिस रफ़्तार से किताब पर काम करने लगे थे, वह हमने पहले कभी नहीं देखी थी। शायद उन्हें आभास हो गया था कि उनकी तबीयत फिर से बिगड़ने वाली है। दिन बीतने के साथ-साथ हमने ग़ौर किया कि उन्होंने खाना-पीना कम कर दिया है और घर से बाहर भी कम ही निकलते हैं।
अमेरिका में बसे परिवार के एक क़रीबी सदस्य ने कहा कि वह उन्हें इलाज के लिए अमेरिका ले जाना चाहते हैं। और वे इस बात को लेकर बहुत संजीदा भी थे। मगर स्वदेश ने उनकी तरफ़ देखते हुए कहा―“मैं मर भी जाऊँ तब भी उस घटिया मुल्क में क़दम नहीं रखूँगा।” सच कहूँ तो उन्हें हवाई यात्राओं से चिढ़ थी, क्योंकि उस दौरान उन्हें धूम्रपान करने की मनाही होती थी। निकोटीन युक्त च्युइंग-गम का सेवन वह कभी नहीं करते थे। एक बार तो एक एयर-हॉस्टेस से उन्होंने यहाँ तक कह दिया, “मैं च्युइंग-गम चबाने के बजाय थोड़ा कष्ट ही झेल लूँगा। कोई भी प्रतिष्ठित आदमी ऐसी दयनीय स्थिति में नहीं होना चाहिए।”
यह संस्मरण रिकॉर्ड समय में लिखा और प्रकाशित किया गया था। उनके जैकेट पर उनके पसंदीदा चित्रकार मरहूम जहाँगीर सबावाला की पेंटिंग उकेरी गई थी। इन सबके होते उन्हें प्रसन्नचित्त होना चाहिए था, मगर हमने ग़ौर किया कि जब वह अपनी आख़िरी किताब की पहली प्रतियों वाला पुलिंदा खोल रहे थे तो उनके भीतर कोई उत्साह नहीं था।
हम समझ गए कि वह अपनी पहली वाली स्थिति में लौट आए हैं और उनके साथ-साथ हम सभी।
मैंने माँ को, पापा की बीमारी और उनकी अपनी ही कड़वाहट से निपटने के लिए अकेला छोड़ दिया और हिंदुस्तान टाइम्स में काम करने के लिए चंडीगढ़ आ गया, बल्कि माँ ने ही मुझे जाने के लिए प्रोत्साहित किया था और ज़ोर देकर कहती रहीं कि तुम्हारा खुली हवा में साँस लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैंने भी वही किया। शराब, शबाब और कला-सृजन में डुबकी लगाते हुए मैंने चंडीगढ़ में एक शानदार समय जिया।
मैं हर वीकेंड पर घर जाता था। पापा को मेरे आने का बेसब्री से इंतज़ार रहता था, यह दीगर बात है कि उन्होंने खुलकर यह कभी नहीं कहा। सिवाय एक बार, जब उन्होंने इशारों-इशारों में ही कहा था, “शनिवार के दिन मैं बार-बार अपने कमरे से बाहर देखता रहता हूँ। मुझे बरामदे में खड़ी मोटरसाइकिल को देखकर बड़ा अच्छा लगता है।”
हम किताबों के बारे में बातें करते थे। आजकल मैं क्या पढ़ रहा हूँ, किस तरह के लेख लिख रहा हूँ, किस तरह की लड़कियों को डेट कर रहा हूँ, वग़ैरा-वग़ैरा।
एक बार उन्होंने बातें-बातों में ही कहा―“मुझे इस बात की बेहद ख़ुशी है कि तुम्हारी सभी प्रेमिकाएँ उम्र में तुमसे काफ़ी बड़ी हैं। मुझे यक़ीन है कि एकाध तजुर्बेकार महिलाओं से संभोग के बाद तुम्हें ढेर सारा मातृवत् स्नेह मिलेगा।”
माँ को बाप-बेटे के बीच के इन ‘अश्लील’ वार्तालापों से सख़्त चिढ़ होती थी।
कई वर्षों बाद, माँ ने मुझे बताया कि चंडीगढ़ के मेरे मकान मालिक ने स्वदेश को फ़ोन करके शिकायत की थी कि मेरी बरसाती में आए दिन महिलाएँ आती रहती हैं, और वह इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा ने उनसे विनम्रतापूर्वक कहा था, “आपको यह सब ख़ुद ही उससे कहना चाहिए। मैं लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दख़ल नहीं देता...” और फ़ोन रख दिया।
जून 2006 में एक दिन मेरे पास माँ का फ़ोन आया, “स्वदेश कल बाहर गए थे और तब से अभी तक वापस नहीं आए।” मैं फौरन भाँप गया कि वह अब कभी वापस नहीं आएँगे। मैंने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाया, अपने पसंदीदा बार में रुककर मज़े से दो बीयर का आनंद लिया और अंबाला के लिए निकल पड़ा। हमने एक दिन और इंतज़ार किया, मगर वह नहीं लौटे। वह कोई नोट या चिट्ठी भी नहीं छोड़ गए। उनकी कलाई घड़ी, बटुआ और दो टॉर्च―जिन्हें वह हमेशा अपने पास ही रखते थे―उनके कमरे में ही रखे थे।
अगले दिन हम पुलिस स्टेशन गए। मैंने अपनी प्रेस आईडी दिखाई और सारा काम ‘बिजली की तेज़ी’ से होने लगा। उन्होंने मुझे चाय-समोसे भी ऑफ़र किए। इंस्पेक्टर ने कहा कि उसे इस बाबत अपने सीनियर्स की तरफ़ से भी फ़ोन आए थे―मेरी बहन ने फिर से अपने ‘प्रभुत्व’ का इस्तेमाल किया था―और आश्वासन दिया कि शाम तक हमें ख़बर कर दी जाएगी।
“ख़बर? किस बात की?” मैंने पूछा।
पुलिसवाला कुछ क्षण तक मेरी शक्ल देखता रहा गया। और फिर वहाँ से चलता बना।
आज इतने सालों बाद भी मैं उसका चेहरा नहीं भूला हूँ। पतला चेहरा और बला का ख़ूबसूरत युवक।
शायद स्वदेश दीपक का इतिहास जानकर, उन्हें अंदाज़ा हो गया था कि उनके जैसे लोग एक बार खो जाने के बाद दुबारा कभी नहीं मिलते।
हमने भी उनकी तलाश में कोई बहुत बड़ा ‘सर्च ऑपरेशन’ नहीं चलाया। न ही हम हरिद्वार गए, जैसा कि कुछ रिश्तेदारों ने सुझाया था। हाँ, मगर एक बार मैं उनके मनोचिकित्सक से ज़रूर मिला था। उनका कहना था, “बस ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह जीवित न हों। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा कि लिथियम के बग़ैर उन पर क्या बीत रही होगी।”
मुझे यक़ीन है कि अब वह कभी लौटकर नहीं आएँगे। बावजूद इसके, आज भी मैं अपने पलंग के नीचे लोहे का एक सरिया ज़रूर रखता हूँ।
अनुवाद : निशीथ
~~~
प्रस्तुत संस्मरण—Papa, Elsewhere, जेरी पिंटो द्वारा संपादित पुस्तक The Book of Light: When a Loved One Has a Different Mind, संस्करण : 2016, प्रकाशक : Speaking Tiger से लिया गया है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
