देश-प्रेम और पहले प्रेम के दरमियान
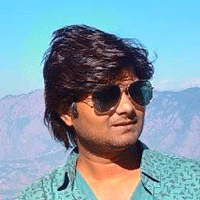 गोविंद निषाद
15 अगस्त 2025
गोविंद निषाद
15 अगस्त 2025
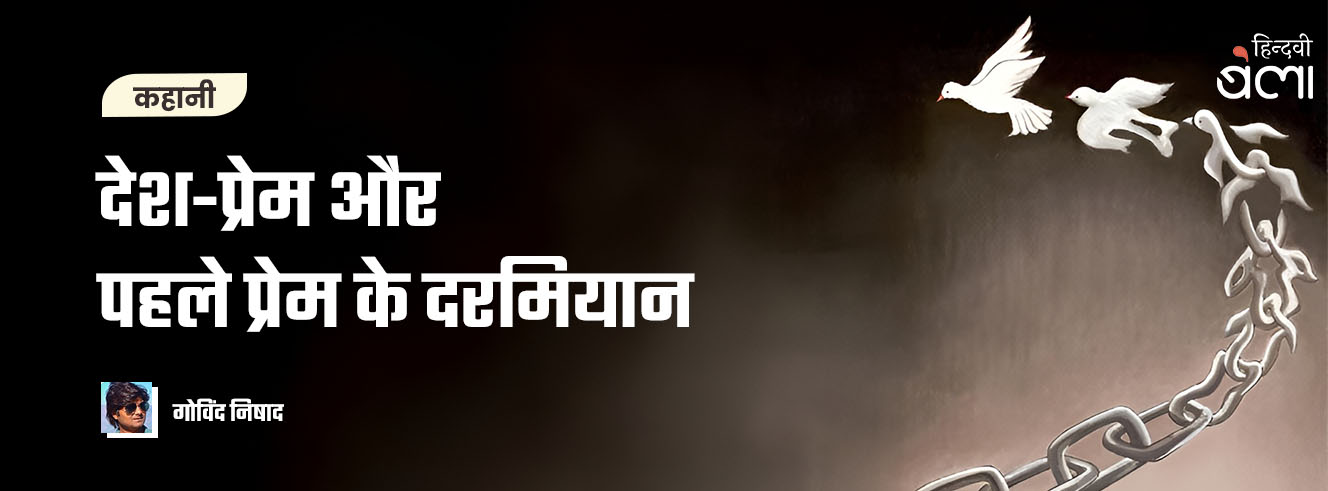
मैं एक कहानी कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कथा-कहन के पैमानों पर यह सही बैठती नहीं है। फिर यह कहानी कैसे हुई—जब यह मानकों पर खरा नहीं उतरती तो। जो भी हो मैं कोशिश भरपूर करूँगा। मुझे पता है कि ‘मैं’ सूत्रधार को आप मुझ ही पर आरोपित करके इसे संस्मरण कह देंगे। अरे! मैं भी न क्या कह रहा हूँ—मेरा काम है लिखना, फिर कोई उसे कहानी मानकर पढ़े या संस्मरण। क्या फ़र्क़ पड़ता है। सबसे ज़रूरी है, लिखा जाना तो लिखते हैं :
जीवन में आशा की एक किरण भी दिखाई देती है, तो उसके पीछे भागता हूँ। भागते-भागते जब थक जाता हूँ, तब लौट आता हूँ—उसी निराशा भरे जीवन शून्य में। इस शून्य को भेदना बहुत मुश्किल लगता है। कोशिश करता हूँ इसे भेदने की, लेकिन बार-बार असफल हो जाता हूँ। जीवन की राह पहले जितनी आसान लगती थी, अब उतनी ही मुश्किल लगती है। लगता है कि अभी जहाँ हूँ—यहाँ नहीं आना था। यह राह मेरे लिए तो नहीं बनी है। कितनी मुश्किल और कितनी निराशाएँ हैं इस रास्ते में। रोज़ एक निराशा घेर लेती है। यहाँ से कैसे आगे बढ़ें? इसका कोई उत्तर नहीं सूझता है।
“तुम तो यही करना चाहते थे ना?”
“हाँ, लेकिन तब पता नहीं था कि यह बस कुछ दिन का भ्रम है—जो समय बीतने पर टूट जाएगा।” मैंने निराशा भरे स्वर में कहा।
“तुम तो बड़े निराशावादी निकले?” उसने कहा।
“अरे नहीं, मैं पहले बहुत आशावादी था। सब कुछ अच्छा लगता था, लेकिन ज़्यादा बरसात बाढ़ ला देती है।”
“तुम सोचते बहुत हो”
“क्या कहा?”
“अरे यही कि तुम सोचते बहुत हो”, मैं ख़यालों की दुनिया में डूब गया था। उसने हाथ खींचा और कहा, “सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो?”
“सुन रहा हूँ”—मैंने ऐसे कहा जैसे गहरी नींद से जगा होऊँ।
“तो बताओ कि इतना दिमाग़ क्यों लगाते हो?”
“दिमाग़ कहाँ लगाता हूँ, बस सोचता हूँ कि दुनिया को इस तरह सुंदर बनाया जा सकता है—तो लोग जानते हुए भी बनाते क्यों नहीं?”—मैंने उसकी तरफ़ देखकर उसका जबाब जानना चाहा।
“देखो, मैं कोई फ़िलॉसफ़र नहीं हूँ जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दे पाऊँ। मैं बस चाहती हूँ कि तुम जो चाहते थे, वह सब तो तुम्हें मिल ही गया न; फिर किस बात के लिए निराश रहते हो। तुमने तो उम्मीद से कहीं ज़्यादा पाया है।” उसने ग़ुस्सा करते हुए कहा।
“अच्छा-अच्छा ठीक है। ज़्यादा न चिल्लाओ। तुम नहीं समझोगी।”
मेरी इस बात में बेरुख़ी थी। वह उदास हो गई। उसने भुनभुनाते हुए कहा कि, “अब कुछ नहीं हो सकता है। जो आदमी जीवन में कुछ नहीं कर रहा है, उसे तो तुम्हारे मुताबिक़ इस दुनिया में रहना ही नहीं चाहिए। ज़बरदस्ती निराश होने का नाटक करता है। मैं जा रही हूँ, जब तुम आशावादी हो जाना तो बताना, नहीं तो भाड़ में जाओ। तुम्हारे साथ रहकर मुझे पागल नहीं होना।”
उसके जाने के बाद लगा कि क्या मैं सचमुच का नाटक करता हूँ। सही तो कहा उसने कि मैंने अपने जीवन में ज़्यादा ही पाया है। क्या था मैं? कोयला फोड़ता-बीनता एक लड़का और कुछ भी नहीं। कितना कुछ पा गया हूँ! अगर उसी रास्ते चलता तो किसी झुग्गी-झोपड़ी में गुम हो गया होता। मैंने उसे रोका नहीं जाने दिया।
वापस लौटकर जब उसे कॉल लगाया तो लग ही नहीं रहा था। बार-बार कोशिश करने के बाद भी मैं नाकाम रहा। मुझे पता चल गया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तभी मेरे मोबाइल पर ईमेल आया। देखा तो कल स्वतंत्रता दिवस के लिए संस्थान से नोटिस आया था कि नौ बजे सभी छात्र उपस्थित हों।
मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था—न तो उसके चले जाने का, न कल के स्वतंत्रता दिवस का। सब उबाऊ लग रहा था। मैं बिस्तर पर लेटते हुए सपनों की दुनिया में खो गया, जहाँ प्रेम भी था और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का आह्लाद भी।
तब 15 अगस्त और 26 जनवरी का दिन हमारे लिए पर्व था, जैसे पूरे देश के लिए। इसकी तैयारियाँ हम एक अगस्त या एक जनवरी से ही शुरू कर देते थे। मैं इस पर्व पर बात करूँ—उससे पहले मैं स्कूल और उनके अध्यापकों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ।
मेरी पढ़ाई एक ऐसे स्कूल में शुरू हुई थी, जहाँ एक पंडित जी छप्पर डालकर पढ़ाते थे। तब यह स्कूल उस क्षेत्र का एक माना-जाना स्कूल था। दूर-दूर से बच्चे यहाँ पढ़ने आते। सिर्फ़ गाँव की दक्षिण पट्टी के बच्चों को छोड़कर। वह दूर किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते—जहाँ वज़ीफ़ा मिलता था। उस पट्टी से बहुत कम बच्चे यहाँ पढ़ने आते। वैसे अक्सर कक्षाएँ बाहर मैदान में ही लगती।
एक विशाल आम का पेड़ पूरे स्कूल को अपनी छत्रछाया से आच्छादित करता था। वह इतना विशाल था कि लड़के जब पत्थर मारते तो अंतिम ऊँचाई तक कभी नहीं पहुँचता था। इस पेड़ की शाखाएँ अलग-अलग कक्षाओं के लिए जगह दे देतीं। जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया था, तब कापी पर लिखने का ज़माना नहीं था। तब हम लकड़ी के पटरे पर कक्षा एक में लिखते। कक्षा एक का विभाजन दो भागों में किया गया था—गदहिया गोल और बड़ी गोल।
बड़ी गोल के विद्यार्थी कक्षा दो में प्रवेश पाते। यहाँ से पटरी का काम ख़त्म हो जाता। अब हम स्याही से लिखते। क़लम नरकट की डंडी से बनाई जाती। पूरे कक्षा पाँच तक यही करना था। यहाँ की फ़ीस प्रति माह दस रूपये हुआ करती थी। यहाँ पढ़ाने वाले शिक्षकों में केवल दो शिक्षक थे। पंडित जी और बाले मुंशी। पंडित जी का पूरा नाम रामानंद तिवारी और बाले मुंशी का नाम बालचंद निषाद था। उनकी कक्षाओं की कोई नियमित समय सारणी नहीं थी।
पंडित जी का जब तक मन करता एक ही विषय पढ़ाते रहते। वह विकलांग थे। उनके शरीर पर कूबड़ निकला हुआ था। वह बहुत शख्त शिक्षक माने जाते थे। ऐसा कोई दिन नहीं गुज़रता, जब कोई बच्चा बिना उनकी मार खाए घर आता। जो बच जाता वह अपने आपको भाग्यशाली समझता। वह सुबह सबसे पहले गणित पढ़ाते। बच्चों को पंक्ति में बैठा दिया जाता। फिर वह जोड़-घटाव-गुणा-भाग आदि गणितीय पहेलियों को बच्चों से क्रमवार पूछ-पूछकर हल करवाते। मैं डरा रहता, लेकिन मेरा आत्मविश्वास हमेशा ऊँचा होता। इस दौरान सभी बच्चे मार खाते लेकिन मैं बच जाता। डर तो मुझे भी लगा रहता लेकिन मैं गणितीय पहेलियों को सुलझा देता। मैं अक्सर सोचता कि जब मेरा नंबर आए तो सवालों की पहेलियाँ थोड़ी सीधी और सरल हों।
पंडित जी एक छड़ी लेकर चलते थे। उसी छड़ी से बच्चों की पिटाई भी करते थे। जो लड़का मार खाने के लिए हथेलियाँ आगे नहीं करता, वह उसी छड़ी के मुड़े हुए भाग से गले में फँसाकर उसे खींच लेते। फिर कान उमेठते हुए उसकी पीठ पर घूसों की बरसात कर देते। इस कक्षा के बाद भी किसी को छुट्टी नहीं मिलती। वह हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान और नैतिक विज्ञान पढ़ाते। सिर्फ़ अँग्रेज़ी एक ऐसा विषय था, जो उनकी ज़द के बाहर था।
वह बाले मुंशी के हवाले था। वह भी बेरहम दिल थे। पढ़ाते हुए, थोड़ी-सी ग़लती होने पर बहुत पीटते। यह बच्चों के लिए स्कूल न होकर मार खाने की जगह थी। जो दिन भर मार खाने से बच जाता, समझो कि कोई पुण्य करके आया होता। मैं इस पुण्य के कुंड में डुबकी मारकर आता था। अंतिम समय शाम को सभी पाँच कक्षाओं के विद्यार्थी इकट्ठा होते और ज़ोर-ज़ोर से पहाड़ा पढ़ते। इतना तेज़ कि उसकी आवाज़ दूर गाँव के अंतिम छोर तक जाती। फिर पंडित जी एक कथा सुनाते जो किसी प्रवचन कि शैली में होती। अंत में उसमे कोई-न-कोई सीख होती।
पंडित जी विद्वान आदमी थे। वह हर विषय पर नाटक लिख देते और उसके डायलॉग बहुत अच्छे होते। 14 अगस्त और 25 जनवरी को आधे बेला की कक्षाएँ होतीं, मतलब कि एक बजे के बाद छुट्टी। यह आधे बेला की छुट्टी ऐसी होती थी कि जैसे कोई भुआ उड़ा चला जा रहा हो और हम उसे अपनी हथेलियों पर गिरने दे और जब वह थम जाए तो फूक मारकर उड़ा दें। आधे बेला की छुट्टी इसलिए होती कि छात्र अपनी पूरी तैयारी से अगले दिन आएँ। इसमें सबसे ख़ास बात होती कि सबके कपड़े धुले हुए हों।
यहाँ पढ़ने वाले ज़्यादातर छात्र ग़रीब घरों से आते थे, जिनके लिए दो कपड़े सिलवाना बाप के सिर का बोझ बढ़ा देना था। इसलिए ज़रूरी था कि बच्चे कपड़े धुले हुए पहनकर आएँ। उस दिन हम हाथों से पन्नों पर तिरंगा ऐसे बनाते रहे, जैसे आसमान में बादल अटखेलियाँ कर रहे हों और हर बार कुछ बादल उड़ कर इधर से उधर हो जाते थे। बहुत कोशिश के बाद मैं सफल हो पाया था, रंगों को क़रीने से सजाने में। फिर उसको बाँस की शाखा जिसे कइन कहते हैं—उसके शीर्ष पर लगाया और झंडा फहराने लगा। कल इसी को लेकर स्कूल जाना था।
ऐसा करना सभी छात्रों को अनिवार्य होता। माँ ने मुझे बाँस पर चढ़कर कइन काटते देख कहा, “अरे उ पंडित जी कइन से मडई छवइहै। एही माले लड़िकन के कइन लावय के कहै न।” सुबह-सुबह फेरई ने अपना लाउडस्पीकर लगा दिया, जिस पर महेंद्र कुमार का गाना बजता रहा— “मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे-मोती, मेरे देश की धरती।” इसे सुनकर मेरे रोम-रोम पुलकित हो गए। उस दिन नियत समय पर सभी छात्र स्कूल में इकट्ठा हुए और प्रभात फेरी निकाली गई। इसमें लड़कियाँ सबसे आगे थीं और लड़के पीछे।
आगे साइकिल में बंधे हुए लाउडस्पीकर लगे हुए थे। माइक पर सबसे अच्छा गाने वाली लड़कियाँ थीं—जो पहले गाती— “विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा।” फिर उसी को सभी बच्चे दोहराते। बीच-बीच में लड़कियाँ नारें लगाती—भारत माता की... सभी बच्चे मुट्ठियाँ तानकर कहते—जय। फिर वह कहतीं महात्मा गांधी…बच्चे मुट्ठी तानकर ज़ोर से चिल्लाते—अमर रहें। जवाहरलाल नेहरू अमर रहें...अमर रहें। सुभाषचंद्र बोस अमर रहें। सरदार पटेल अमर रहें। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। भगत सिंह ज़िंदाबाद...। चंद्रशेखर आज़ाद ज़िंदाबाद...। पीछे के बच्चों को कुछ साफ़-साफ़ सुनाई नहीं दे रहा रहा था, तो वह अपनी अलग नारेबाज़ी कर रहे थे।
ऐसे ही यह प्रभात फेरी पूरे गाँव का चक्कर लगाती रही और पूरा गाँव इसे देखने के लिए सड़कों के किनारे खड़ा था। सभी हम पर स्नेह की वर्षा कर रहे थे। जैसे ही किसी छात्र का घर आता तो वह चाहता कि उसकी माँ-पिता उसे पंक्ति में देखें। उनके दिखने पर बिखरने वाली मुस्कान से धरती महकने लगती। गाँव का चक्कर लगाकर हम स्कूल में इकट्ठा हुए। साथ में इकट्ठा हुआ पूरा गाँव। बुज़ुर्ग से लेकर नौजवान, महिलाएँ और नवयुवतियाँ; सैकड़ों की संख्या में स्कूल प्रांगढ में जमा हो गए। इन दर्शकों के सामने किसी ने कोई गीत गाया तो कोई भाषण देने आगे आया। भाषण देने वाले अक्सर रट्टा मारकर सुनाते और बीच में ही भूल जाने पर शर्माते हुए मंच से उतर जाते। दर्शकों को सबसे ज़्यादा मज़ा नाटक देखने में आता।
मुझको भी कक्षा पाँच में नाटक करने का अवसर मिला। पहला नाटक था लक्ष्मण और परशुराम संवाद का। इसमें मुझे राम का किरदार मिला था। दूसरा नाटक क्रांतिकारियों का था—जिसमें भगत सिंह से लेकर गांधी सबको पंडित जी ने एक ही नाटक में सभी पात्रों को शामिल कर दिया था, तीसरा नाटक था रानी कर्णावती द्वारा हुमायूँ को रक्षाबंधन भेजकर गुजरात के सुल्तान से राज्य की रक्षा करने का वचन लेने का।
हमने नाटक की तैयारियाँ एक अगस्त से शुरू कर दी थी। प्रशिक्षण का ज़िम्मा होता पंडित जी पर और निर्देशक उस समय मैं बना था। हम रोज़ शाम को एक घंटे पढ़ाई छोड़कर रिहर्सल करते। इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल डायलॉग याद करने की होती। अभिनय तो बाद की बात थी। इस दौरान पूजा भी वहीं रहती।
अब मैं प्रेम पर आता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सिर्फ़ संस्मरण सुनाकर आपका समय बर्बाद कर रहा हूँ। उसे रानी कर्णावती की भूमिका निभानी थी। इसके लिए वह रोज़ाना आती रिहर्सल करने। मैं निर्देशन कर रहा था तो मुझे सबको बताना होता कि किसको किस तरह अभिनय करना है और कौन-सा डायलॉग कैसे बोलना है।
मैं सिखाते हुए पूजा को ख़ूब देखता। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराती तो लगता कि जीवन को वही रुक जाना चाहिए। हमारी प्रेम कहानी पहले से शुरू हो चुकी थी—जिस पर मैं आपको बाद में ले चलूँगा। हाँ तो नाटक की सारी तैयारियाँ हो गईं। अंतिम दिन से दो दिन पहले हमें पंडित जी के सामने डेमो देना था। हम इसमें पास हो गए। लेकिन नाटक करने के लिए जब मैं पहली बार इतने लोगों के सामने खड़ा हुआ तो मुझे काटो तो ख़ून नहीं। मेरे हाथ काँपने लगे, लेकिन जैसे ही मैंने अपना पहला डायलॉग माइक पर बोला और आवाज़ गूँजीं तो मेरा आत्मविश्वास बढ़ गया। अब मैं बेधड़क होकर अपने डायलॉग बोल रहा था। महीने भर के रिहर्सल के बाद भी बहुत से छात्र आत्मविश्वास की कमी के कारण नाटक के दौरान अपना डायलॉग भूल जाते। ऐसे छात्रों की बाद में बहुत किरकिरी होती।
दूसरे नाटक में मुझे खलनायक का किरदार मिला, जिसमें मुझे गुजरात के शासक का किरदार निभाना था; जो मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला है—तभी रानी कर्णावती हुमायूँ को राखी भेजती है और अनुरोध करती है कि वह अपना भाई का फ़र्ज़ अदा करें। हुमायूँ गुजरात के शासक को हराकर अपना वचन पूरा करता है। फिर भगत सिंह और नेहरू की भूमिका मैंने बख़ूबी निभाई। उस दिन जिस तरह का मैंने अभिनय किया, उसकी तारीफ़ बहुत दिनों तक हुई, लेकिन बाद में मुझे सभी चिढ़ाते कि धनुषवा त टूट गयल सीता कहां गइनि? फिर वह खिलखिलाते हुए कहते कि सीता त ओकर पूजा हई न। अरे नाही ऊ त रानी कर्णावती बा। एकर दुश्मन। फिर हम सब हँसने लगते। यह सब महीनों चलता रहा।
कक्षा पाँच के विद्यार्थियों को ही नाटक मंचन का मौक़ा मिलता। उस बार एक लड़के ने अपना नाम गाना गाने में लिखवाया। उसे मंच पर बुलाया गया और उसने गाया- “तोहके चाही जीयते गिरई, अब का मुरई लेबू ना’ चारों ओर ठहाके गूँजने लगे। पंडित जी ने तुरत उसे रूकवाकर अपने पास बुलाया और लगे थप्पड़ पर थप्पड़ जड़ने लेकिन दर्शकों और बच्चों को ख़ूब मज़ा आया। एक गाना लड़कियाँ हमेशा गातीं—
“देसवा के हमरे सम्मान दा
माता सरस्वती वरदान दा।”
दूसरा गाना होता—
“गांधी बाबा जात रहने बिरला भवनवा
रहिया में ढूकल रहनै नाथू दुशमनवा
पहली गोली फायर कइनै दूसरा निशनवा
तीसरे में मार दिहनै गांधी जी क जनवा।”
रसूल मियाँ का लिखा यह गीत कई सालों तक आम जनमानस की स्मृतियों में अलग-अलग तरह से ज़िंदा रहा। अब इनाम देने का समय आया। मुख्य अतिथि के रूप में उस इलाक़े के मशहूर पुस्तक विक्रेता मुंशी जी को बुलाया गया था। लाउडस्पीकर पर नाम पुकारे जाने लगे। फिर ईनाम पाने वाला लड़का जाता, उसे कॉपी और पेन दिया जाता। वह सभी के पैर छूकर वापस आ जाता। अगर दर्शकों में से किसी को ईनाम देना होता तो वह भी देता। मेरे शानदार अभिनय से प्रेरित होकर मुझे एक दर्शक की तरफ़ से सौ रूपए का ईनाम मिला था। मैं ख़ुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था।
बाद में सबको लड्डू बाँटा गया। सब इसे प्रसाद की तरह ग्रहण करते। मुझे याद है वह पूरा दिन हर्षौल्लास से भर गया था। अब आप कहेंगे कि इसमें कहानी कहाँ है तो भई वो क्या न कि मैं कहानी कहना तो चाहता हूँ लेकिन बन नहीं पा रही है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ—तो पीछे की तरफ़ चलते हैं।
मेरी लिखावट और पढ़ने-लिखने की ललक ने मुझे अध्यापकों के बीच लोकप्रियता दिला दी थी। मैं कक्षा का मानीटर घोषित था। लंच के बाद सुलेख लिखाया जाता। ऐसा होता कि कक्षा चार-पाँच के बच्चों को एक हाथ की दूरी पर बैठा दिया जाता। फिर मैं आगे की तरफ़ बैठता अन्य छात्रों के बिल्कुल सामने। मैं तेज़ी से बोलता अंतरराष्ट्रीय, संस्कृति, परिष्कृत...। मैं जितने ही कठिन से कठिन शब्द चुन सकता था—उतने कठिन शब्द चुनकर बोलता।
उसे छात्रों को बिना देखे सही-सही लिखना होता। फिर कापियाँ जमा की जातीं और मैं उसका परीक्षण करता। एक-एक अक्षर का बारीक़ परीक्षण। अगर ज़रा-सी भी लिखने में ग़लती हुई तो मैं उस पर क्रास का चिह्न बना देता। मतलब कि अब किसी छात्र की कॉपी में जितने कट लगे हैं—उसे उतनी छड़ी की मार पड़नी तय होती। मैं ठहरा मानीटर तो आराम से बच जाता। कुल मिलाकर मेरी धाक जम गई थी। इलाहाबादी में कहें तो भौकाल था गुरु अपना उस स्कूल में।
एक दिन जब मैं कॉपियों का परीक्षण कर रहा था। एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे प्रार्थना की कि क्या मैं उसे कॉपी दे सकता हूँ ताकि वह ग़लत शब्द को सही कर सके। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन जब उसने मासूम-सा चेहरा बनाते हुए फिर कहा तो इस बार मैं पिघलने से ख़ुद को रोक नहीं पाया। मैंने कॉपी उसे दे दी। वह मुस्कुराते हुए चली गई। वह पतली-सी लेकिन गोरी लड़की थी। दूर एक गाँव से आती थी।
अब मैं उसे देखता और बोलता कुछ नहीं। दोनों एक-दूसरे को बस निहारते रहते। एक दिन उसने ऑफ़र दिया कि वह चाहे तो आकर उसके साथ खेल सकता है। फिर क्या। मेरी तो लॉटरी निकल आई। अब मैं अक्सर ही उसके साथ ही खेलता। यह मेरे दिल में प्रेम का फूटा पहला अंकुरण था। वह अक्सर मेरे लिए घर से कुछ खाने के लिए लाती। बदले में मैं उसकी कॉपियों का परीक्षण करते हुए उसके ग़लत अक्षर को सही कर देता—जिससे वह मार खाने से बच जाती। उसके गृहकार्य को कर देता। उसको पढ़ाता और समझाता।
एक दिन मैंने कहा कि मैं एक चीज़ लाया हूँ तुम देखोगी? उसने कहा कि दिखाओ तो मैंने अपना हाथ आगे कर दिया, जिस पर लिखा हुआ था—‘पूजा’। अरे तुमने तो मेरा नाम लिखा है। वह किसी चिड़िया की तरह किलकिलाने लगी। फिर उसने अपने हाथ को मेरे हाथ में लेकर कहा कि फिर तुम अपना नाम मेरे हाथ पर भी लिख दो। मैंने वैसा ही किया। अब यह हमारी दिनचर्या का एक हिस्सा हो गया।
मैं बस उसे गणित के सवालों से नहीं बचा पाता—जब पंडित जी उससे पूछते। फिर हाथ आगे करके उसे दो-तीन छड़ी लगाते तो वह आँखें बंद कर लेती और मुझे लगता कि वह छड़ियाँ मेरे पीठ पर पड़ रही हैं। वह रोने लगती। कक्षा की समाप्ति के बाद मैं उसे सांत्वना देते हुए गणित पढ़ाता लेकिन उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फिर वह मेरे साथ खेलते हुए मार खाना भूल जाती। हम दोनों एक दूसरे की हथेलियों पर एक-दूसरे का नाम लिखते और उसे निहारते रहते जैसे उस समय हम रिश्तेदारों द्वारा लाई गई मिठाइयों की तरफ़ निहारते थे।
एक दिन किसी लड़के ने उसके हाथ पर लिखा हुआ नाम देख लिया और पंडित जी से शिकायत कर दी। मुझे बुलाकर जब उन्होंने हाथ खोलने को कहा तो मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। जैसे ही मैंने हाथ खोला, उस पर ‘पूजा’ लिखा हुआ उन्हें दिख गया। फिर क्या पंडित जी की नज़रों में यह सबसे बड़ा गुनाह था—जो अक्षम्य था। आज मानीटर को पीटा जाता देख सभी ख़ुश थे, पूजा को छोड़कर।
बाद में वह मेरे हाथों को अपने हाथ में लेकर सहलाने लगी, लेकिन पंडित जी ने मुझे इतना हड़काया था कि आज के बाद उसके पास दिखना भी मत। उस बात को याद करते ही मैं भाग खड़ा होता। थोड़े दिन मैं उससे भागता रहा, लेकिन जब मामला ठंडा हो गया तो फिर से हमारी प्रेम कहानी शुरू हो गई।
उन दिनों रजनी मेरा जिगरी यार था। हम दोनों पढ़ाई-लिखाई में ठीक उलट थे। मैं जितना पढ़ने वाला, रजनी उतना ही पढ़ाई के नाम से दूर भागने वाला। फिर भी दोनों में ख़ूब पटती। रजनी उस समय के बड़े पुस्तक विक्रेता मुंशी जी का ही भतीजा था। तब उनकी दुकान पर भीड़ ही लगी रहती। जुलाई का महीना किताबों से निकलने वाली ख़ूशबूओं से भर जाता।
वह रोज़ पैसे चुराकर लाता और दोनों बाज़ार जाकर मस्त समोसा, चाट, लौंगलता खाते। एक दिन उसकी चोरी पकड़ी गई। उसके चाचा ने उसे कुएँ में लटका दिया—यह कहते हुए कि बोल आज के बाद चोरी न करबे ना। वह गिड़गिड़ाकर माफ़ी माँगने लगा और रोता रहा। फिर उसे बाहर निकाला गया।
अब मिठाई पर ताले लग गए। अब दोनों बाहर चोरी करते। अब हमने एक किराने की दुकान से खटाई चुराना शुरू कर दिया। एक दिन दुकानदार ने मुझे पकड़ लिया और मुझे उठाकर पटकने जा ही रहा था कि मेरे पिता आ गए वर्ना मैं फटकर कद्दू हो जाता। कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि आपका लड़का चोरी करता है। फिर क्या पिता ने वहीं मुझ पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। मुझे क़सम दिलाई कि आज के बाद वह फिर कभी भी चोरी नहीं करेगा लेकिन खटाई छोड़ अन्य जगहों पर हम चोरी करते रहे।
दरअस्ल सवाल चोरी का नहीं—प्रेम का था। जब तक रजनी पैसे चुराकर लाता रहा, तब तक तो पूजा के लिए मैं सबकुछ उपलब्ध करा देता; लेकिन जैसे ही चोरी पर ताले लगे, वैसे ही हमारे लिए मिठाई खाना और पूजा को खिलाना मुश्किल हो गया। हम दर-दर भटकते कि कहीं से कुछ तो जुगाड़ हो जाय, इसलिए हमारी चोरियाँ जारी रहीं। बस तरीक़ा हमने बदल दिया था। रजनी दुकान से किताब चुरा लाता और सस्ते दाम में छात्रों को बेच देता। पूजा भी ख़ुश—हम भी ख़ुश।
एक दिन दुपहर की छुट्टी के बाद हम दोनों खेल रहे थे। पूजा ने देखा कि एक लड़का अमरूद खा रहा है। उसे भी लालच आ गई। वह माँगने गई। उसने पूजा को सुना दिया, “खेले के रहि त गोभिया बा—अउर अमरूद चाही त आ गइनि हमरे लगे।”
वह रूआँसा-सा मुँह लेकर बैठी हुई थी। मैंने जब उससे पूछा तो उसने सारा किस्सा सुना डाला। मैंने कहा कि—रोवत काहे बाटू। हम बेहने लावत हई—तोहरे खातिन अमरूद। दूसरे दिन दुपहर में खाने की छुट्टी हुई। मैंने रजनी को साथ लिया और चल दिए दोनों भुतहिया बाग। उस बाग़ में कोई नहीं जाता था। वह एक बंद पड़े भट्टे के पास था। वह भी खंडहर में तब्दील होकर एक डर पैदा करता था।
उस बाग़ के बारे में प्रसिद्ध था कि उसमें भूत और चुड़ैल रहते हैं। उसमें कोई भी जल्दी जाने की हिम्मत नहीं करता। उस बाग़ में दो अमरूद के पेड़ थे। उस पर ख़ूब फल लगते थे। उस दिन दोनों ने मिलकर तय किया कि हम दुपहर की छुट्टी में अमरूद तोड़ने चलेंगे। वह किसी तरह हिम्मत बाँधकर अमरूद के पेड़ के पास पहुँच गए। दोनों पेड़ पर चढ़े और अमरूद तोड़ने लगे।
रजनी को एक बड़ा-सा पका अमरूद ऊपर डाली पर दिखा। उसे सीधे हाथ से तोड़ना मुश्किल था, लेकिन रजनी नहीं माना—वह उसे तोड़ने के लिए चढ़ता ही गया। डाल उसके भार को सहन नहीं कर पाई और वह धम्म से नीचे गिर गया। नीचे खपरैल के टुकड़े और ईटे थीं। उसका एक हाथ ईंट पर ही गिर गया। जब तक वह सँभलता रजनी दर्द के मारे चिल्लाने लगा। मैंने देखा कि रजनी का हाथ टूटकर लटक गया है।
मेरे तो होशोहवास उड़ गए। मैं चिल्लाते हुए सरपट भागा जैसे खरगोश जिसके पीछे शिकारी पड़े हो। मुझे लगा कि मेरे पीछे भूत लगे हुए हैं। मैंने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा कि रजनी किस हाल में है। टोले में आकर चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ हकलाने लगी। मैं बता ही नहीं पा रहा था कि क्या हुआ है? मेरा शरीर पसीने से भीग गया था। पानी पीने के बाद मैंने पूरे हालात बयाँ किए। लोग बाग़ की तरफ़ दौड़े। देखा तो टूटा हाथ लेकर रजनी चला आ रहा है। सब कहने लगे कि उसी भूत का काम है। कौन-सी ज़रूरत थी वहाँ जाने की। अब भुगतो। सब लोग मेरे ऊपर बिफर पड़े।
मैं रोता रहा। मुझे भी लगा कि किसी भूत ने रजनी को धक्का दे दिया। शाम तक मुझे भी बुखार आ गया। माँ ने दवाई के साथ ओझाई भी कराई। मैं कुछ दिन में ठीक हो गया। दवा से ठीक हुआ या ओझाई से किसी को नहीं पता था। दोनों के अपने-अपने दावें थे। मैं कई दिन स्कूल नहीं गया। पंडित जी ने मेरे घर लड़कों की एक टोली भेजी। घर आने पर उन्हें पता चला कि मैं बीमार हूँ तो वह चले गए।
एक हफ़्ते बाद मैं स्कूल गया। पूजा पूछने लगी कि स्कूल क्यों नहीं आ रहे थे। मैं दूसरे दिन तुम्हारे लिए अमरूद लेकर आई थी। अब मैं क्या बताऊँ कि उसे अमरूद खिलाने के चक्कर में मैंने अपने दोस्त का भूतों से हाथ तुड़वा दिया। बाद में जब उसने रजनी के हाथ में प्लास्टर देखा तो उससे पूछने लगी कि यह कैसे हुआ। उसने कहा कि हम तुम्हारे लिए भुतहिया बाग में अमरूद तोड़ने गए थे। वहीं पेड़ से गिरकर उसका हाथ टूट गया।
हम तीनों ठहरे छोटे बच्चे। डर गए। पूजा ने मुझको हिदायत दी कि आज के बाद वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा। उसने कहा कि अब कभी वहाँ मत जाना। मैंने हाँ में सिर हिलाया। खेलते-खेलते दोनों कब पाँच पास कर गए पता ही नहीं चला। वह स्कूल पाँचवीं तक ही था। पूजा यहाँ से छूट गई। इस तरह मेरा पहला प्रेम समाप्त हो गया, लेकिन पूजा मेरी स्मृतियों में आज भी ज़िंदा है—यह बताने के लिए कि प्रेम कभी मरता नहीं है।
मैंने सोये-सोये कई बार उसे कॉल किया, लेकिन नंबर नहीं लग रहा था। मैं सोचने लगा कि सही में मैं बहुत सोचता हूँ। देखो न मैं पहली प्रेमिका के बारे में सोचने लगा जबकि वह ठीक से कहें तो प्रेम नहीं था। हाँ यह ज़रूर है कि यहाँ दैहिक प्रेम में ब्लॉक प्रमुख आप कभी भी बन सकते हैं। अरे वो वाला नहीं, मोबाइल वाला ‘ब्लॉक’ प्रमुख।
हाँ तो मुझे कल स्वतंत्रता दिवस समारोह में जाना तो है, लेकिन मन में न कहीं कोई आह्लाद है, न उत्साह। है तो चारों ओर फैली उदासी, जिसका मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। चलो इसे अब ‘मैं’ की जगह ‘वह’ करके पढ़ते हैं—तब शायद कुछ कहानी जैसा लगे। नहीं तो इसमें कहानी कहाँ है? हूँ तो सिर्फ़ ‘मैं’।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
