काम को खेल में बदलने का रहस्य
 हिन्दवी डेस्क
02 जुलाई 2024
हिन्दवी डेस्क
02 जुलाई 2024
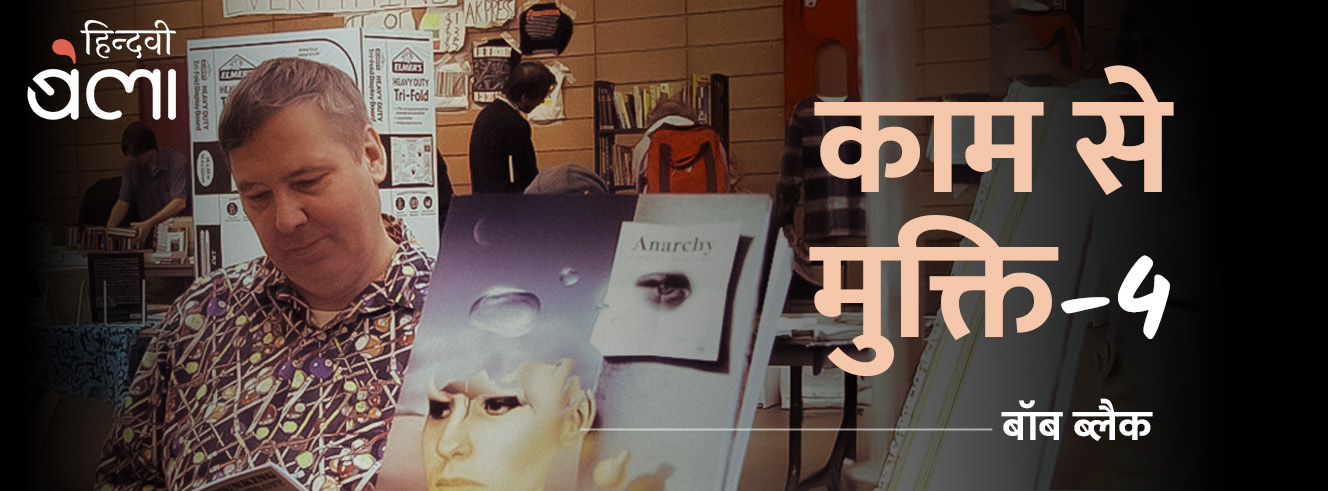
...मैं इससे सहमत नहीं। यह संभव है कि काम का ख़ात्मा किया जा सकता है। काम की जगह ढेर सारी नई तरह की गतिविधियाँ ले सकती हैं, अगर वे उपयोगी हों तो।
काम के ख़ात्मे के लिए हमें दो तरफ़ से क़दम बढ़ाने होंगे—काम की मात्रा तथा गुणात्मकता दोनों को बदलना होगा।
एक तरफ़, काम के बोझ को कम करने के लिए अभी किए जा रहे काम में बड़े पैमाने पर कटौती करनी होगी। अभी ज्यादातर काम बिना मतलब के और ग़ैर-ज़रूरी हैं, हमें इनसे मुक्ति पा ही लेनी चाहिए।
दूसरी तरफ़, मुझे लगता है कि यह सबसे ज़रूरी मामला है और इससे एक नई क्रांतिकारी शुरुआत होगी। हमें बचे हुए ज़रूरी और फ़ायदेमंद काम को कई तरह के आनंदमय खेल और कला जैसी गतिविधियों (मौज-मस्ती वाले क्षणों) में बदल देना चाहिए। यह दूसरे मौज-मस्ती वाले क्षणों से अलग नहीं होगा, सिवाए इसके कि इससे हमें कुछ उपयोगी उत्पाद भी मिल जाया करेंगे।
निश्चित तौर पर इससे इस गतिविधि का आकर्षण कम नहीं होगा। तब संपत्ति तथा सत्ता के जितने नक़ली बखेड़े हैं, ध्वस्त हो जाएँगे। उत्पादन तथा रचना मस्ती बन जाएँगे। तब हमें एक-दूसरे से डर लगना ख़त्म हो जाएगा।
मैं यह नहीं मानता कि ज़्यादातर काम मौज-मस्ती की गतिविधि में बदले जा सकते हैं। सच कहें तो ज़्यादातर काम को बचाया जाना भी नहीं चाहिए, वो इस लायक़ हैं ही नहीं। काम-व्यवस्था, इसके राजनीतिक व क़ानूनी हथियार, इन सब की सुरक्षा, इन सब का फैलते जाना, ये सारी चीज़ें तो हम पर बोझ ही हैं। अगर इन सब को ध्वस्त कर दें तो काम का छोटा हिस्सा ही बचता है, जो हमारे लिए उपयोगी है। धीरे-धीरे ये काम भी ख़त्म हो जाएँगे।
बीस साल पहले पॉल एवं पर्सीवल गुडमैन ने यह अनुमान लगाया था कि उस समय किए जा रहे सारे काम का मात्र पाँच प्रतिशत—अब यह प्रतिशत और भी कम होगा—भोजन, कपड़े और मकान की हमारी न्यूनतम ज़रूरतों को पूरा कर देता है। यह उनका सोचा-समझा अनुमान मात्र ही है, पर मुख्य मुद्दा तो साफ़ है—प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज़्यादातर काम सामाजिक और व्यापार नियंत्रण के बेकार से हितों के लिए ही होते हैं।
झटके में ही हम करोड़ों सामान बेचने वालों, सैनिकों, पुलिस, प्रबंधकों, स्टॉक-ब्रोकर्स, पुजारी, बैंक-कर्मी, वकील, शिक्षक, ज़मींदार, सुरक्षाकर्मी, मीडिया वाले तथा इन सब के लिए काम करने वालों को आज़ाद कर सकते हैं। हर बार जब हम किसी बड़े क़द के मालिक या संस्था को ध्वस्त करते हैं तो इसका असर दूर तक होता है, क्योंकि हम उसके चाटुकारों, चाकरों और मातहतों को भी आज़ाद करते हैं। इस तरह अर्थव्यवस्था अंदर से ही धाराशायी होती जाती है।
कुल मज़दूरों में चालीस प्रतिशत सफेदपोश कर्मचारी हैं। इनमें से ज़्यादातर अब तक के गढ़े गए कामों में सबसे ज़्यादा उबाऊ, थकाऊ और मूर्खता वाला काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर, पूरा का पूरा उद्योग-जगत, बीमा एवं बैंकिंग और ज़मीन-जायदाद के कारोबार की बेकार-सी काग़ज़ी कार्यवाहियों को इधर से उधर करते रहते हैं। यह मात्र संयोग की बात नहीं है कि अन्य क्षेत्र (सेवा क्षेत्र) फैलता जा रहा है, जबकि उद्योग क्षेत्र स्थिर पड़ा है और खेती क्षेत्र सिकुड़ता ही जा रहा है।
चूँकि काम ग़ैर-ज़रूरी है—सिवाय उनके, जिनकी सत्ता की यह रक्षा करता है, इसलिए मज़दूरों को तुलनात्मक रूप से उपयोगी कामों से अनुपयोगी कामों में बदला जाता है। यह सिर्फ़ व्यवस्था का हौवा बनाए रखने के लिए होता है। कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर है। इसलिए अगर हमने काम ख़त्म कर लिया है तो भी जल्दी घर नहीं जा सकते। वे हमारा समय छीनते हैं, इतना समय कि हम उनके होकर रह जाएँ, हालाँकि इतने ज़्यादा समय की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं तो पिछले 50 सालों में औसत प्रति सप्ताह काम का समय क्या कुछ मिनट भी कम नहीं होता?
हमारा अगला क़दम होगा उत्पादन के काम को तहस-नहस करने का। युद्ध संबंधी सामानों का उत्पादन, न्यूक्लियर ऊर्जा, जंक भोजन, महिलाओं के साफ़-सफ़ाई वाले सामान, दुर्गंध-नाशक इत्र, इन सब को ख़त्म करना होगा। इसमें सबसे ज़रूरी होगा गाड़ी-घोड़ों के उद्योग को उखाड़ फेंकना।
कभी-कभार स्टॅनले स्टीमर या मॉडल-टी चल सकता है, पर गाड़ी-घोड़ों के प्रति कामुक प्यार, जिससे डेट्रॉयट और लॉस एंजल्स जैसे गंदे शहर पलते हैं, का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर तो समझिए कि हमने ऊर्जा का संकट, आबो-हवा का संकट, कई अनसुलझे सामाजिक संकट इन सारे समस्याओं का परोक्ष समाधान अपने-आप कर लिया।
अंत में, हमें सबसे बड़े व्यवसाय (जो सबसे ज़्यादा समय खाता है, जहाँ भत्ता भी सबसे कम या नहीं मिलता, और जो सबसे उबाऊ काम है) को भी ख़त्म कर देना चाहिए। मेरा मतलब है, औरतों को घर के काम और बच्चे पालने के काम से। भत्ता-मज़दूरी ख़त्म होने से तथा पूर्ण बेरोज़गारी हासिल होते ही लिंग के आधार पर श्रम विभाजन का मतलब ही ख़त्म हो जाता है।
आज का एकाकी परिवार आधुनिक भत्ता-मज़दूरी द्वारा थोपे गए श्रम-विभाजन की ज़रूरत के हिसाब से उसकी सहूलियत के लिए ही बना है। अच्छा या बुरा, पिछले सौ-दो सौ सालों में जो स्थितियाँ रही हैं, उनमें यह क़तई आर्थिक दृष्टि से तर्कसंगत रहा है कि पुरुष कमा कर लाए, औरत घर में खटे और हृदयहीन दुनिया में पुरुष को संबल दे और बच्चे विद्यालय नामक जवानी के यातना-शिविर (कंसनट्रेशन कैंप) में जाएँ ताकि माँ के आँचल से दूर तो रहें पर फिर भी नियत्रंण में रहें। साथ ही जी-हुज़ूरी और समय की पाबंदी सीखें, जो मज़दूरों के लिए बहुत ज़रूरी है।
ईवान ईलिच का मानना है कि अगर पितृसत्ता से छुटकारा मिल जाए तो एकाकी परिवार से भी छुटकारा पा लेना चाहिए। एकाकी परिवार का ‘छाया काम’ काम की व्यवस्था को संभव बनाता है, जिसके लिए ऐसे परिवार का होना ज़रूरी है। इस ग़ैर-एकाकी परिवार की सीमा की रणनीति का अर्थ बचपन से मुक्ति तथा स्कूलों को बंद करना होगा। (Bound up with this no-nukes strategy is the abolition of childhood and the closing of the schools.)
इस देश (अमेरिका) में पूर्ण रूप से छात्रों की संख्या पूर्ण रूप से मज़दूरों की संख्या से ज़्यादा है। बच्चों को छात्र नहीं शिक्षक होना चाहिए। मौज-मस्ती वाली क्रांति उनके सहयोग के बिना संभव नहीं क्योंकि खेलना-कूदना वे बड़ों से बेहतर जानते हैं। बड़े और बच्चे एकदम एक समान नहीं हैं, पर आपसी सहयोग से एक जैसे हो जाएँगे। उम्र की खाई को सिर्फ़ खेल-कूद ही पाट सकता है।
मशीनीकरण, कंप्यूटर और इंटरनेट ने भी हमारी ज़िंदगी में काम के बोझ को बहुत बढ़ाया है। अभी तक मैंने इस बोझ को कम से कम करने की संभावना पर बात ही नहीं की है। सारे वैज्ञानिक, इंजीनियर, तकनीकी विशेषज्ञ युद्ध से जुड़ी खोज तथा जल्द ही पुरानी पड़ जाने वाली तरह-तरह की अन्य खोजों में फँसे रहते हैं।
इन झंझटों से मुक्त होते ही ये सभी थकावट और ऊब दूर करने के मज़ेदार तरीके, साथ ही खदान जैसी ख़तरनाक कामों को ख़त्म करने के तरीके खोजने जैसी दिलचस्प गतिविधि में अपना समय लगाएँगे। निश्चित तौर पर कई मज़ेदार गतिविधियाँ इनके सामने होंगी। हो सकता है वे सबके लिए विश्वव्यापी मल्टी-मीडिया संचार तंत्र खड़ा कर पाएँ या फिर अंतरिक्ष कॉलोनी ही बनाएँ।
मैं कोई उपकरण (gadget) उत्साही इंसान नहीं हूँ। मैं बटन दबाने से चीज़ें हासिल हो जाने वाले स्वर्ग में रहना पसंद नहीं करूँगा। हर काम करने के लिए मुझे रोबोट जैसे ग़ुलाम नहीं चाहिए, मैं ख़ुद से अपनी चीज़ें करना चाहूँगा। मुझे लगता है श्रम बचाने वाली तकनीक के लिए एक जगह है, लेकिन बस थोड़ी-सी ही।
इस मामले में इतिहास और इतिहास से पहले के दस्तावेज हमारा उत्साह नहीं बढ़ाते। जब उत्पादन-तकनीक शिकार और भोजन इकट्ठा करने से खेती की तरफ़ और फिर उद्योग की तरफ़ बढ़ी, तो काम बढ़ता गया और हमारी क्षमता और आत्मविश्वास घटता गया। जैसा कि हैरी ब्रेव्हरमैन का मानना है—उद्योगों के फलने-फूलने से काम और हमारे जीवन की गंदगी बढ़ती गई। सचेत और विवेकशील लोगों ने हमेशा इस चीज़ को महसूस किया और समझा है।
जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है, अब तक श्रम बचाने की जितनी भी तकनीकें ईजाद की गई हैं, उनमें से कोई भी एक क्षण का भी श्रम बचाने में कामयाब नहीं हुई।
कार्ल मार्क्स ने लिखा है—“1830 ई. से मज़दूर वर्ग के विद्रोह के ख़िलाफ़ पूँजी को हथियार मुहैय्या कराने के गरज से जितनी भी खोजें हुईं और चीज़ें ईजाद हुई हैं, उन पर एक मुकम्मल इतिहास लिखा जा सकता है।”
उत्साही तकनीकी प्रेमी—जैसे संत साइमन, कॉंम्त, लेनिन, बी एफ स्कीनर हमेशा बेशर्म तानाशाह भी रहे हैं, जिसे हम तकनीकशाही भी कह सकते हैं। कंप्यूटर विद्वान (रहस्यवादियों) के वादों को लेकर हमें पूरी तरह सावधान रहना चाहिए। वे कुत्तों की तरह काम करते हैं, संभव है, अगर उनकी चले तो हम सबको भी वैसा ही करना पड़े। लेकिन, अगर उनके पास उच्च तकनीकी दौड़ के अलावा मानव हित में एक भी कोई खास योगदान है, तो हमें उन्हें एक मौक़ा अवश्य देना चाहिए।
मैं वाक़ई में यह चाहता हूँ कि काम खेल में बदल दिए जाए। पहला क़दम यह होगा कि हम ‘तय काम (नौकरी)’ और ‘व्यवसाय (धंधा)’ जैसी सोच से छुटकारा पा लें। मज़ेदार गतिविधियाँ भी जैसे ही कुछ खास लोगों द्वारा (जिसे वही तय लोग कर सकते हैं कोई और नहीं) किए जाने वाले तयशुदा काम यानी नौकरी में बदल दी जाती हैं, वे अपना मज़े वाला अंश खो बैठती हैं। क्या यह शर्मनाक नहीं कि खेतिहर मज़दूर खेतों में शरीर तोड़ते रहें और वातानुकुलित कमरों में बैठने वाले उनके मालिक हर हफ़्ते घर जाएँ और मज़े से बागीचों में टहला करें?
स्थायी (लगातार चलते रहने वाला) मौज-मस्ती के जीवन में हमें शौक़ीनों और प्रेमियों का स्वर्ण-काल देखने को मिलेगा, जिसके सामने नवजागरण (रिनेसाँ) भी शर्म से पानी भरे। कोई काम या नौकरी नहीं होगी, बस कुछ गतिविधियाँ करने को होंगी और मज़े में उन्हें करने वाले लोग।
चार्ल्स फूरियर ने काम को खेल में बदलने का रहस्य सुझाया है, हमें उपयोगी गतिविधियों को अपने जीवन-समाज में इस तरह से सजाना चाहिए कि अलग-अलग समय में अलग-अलग लोग इसे करें और आनंद उठाएँ। अगर हम ऐसा संभव कर पाएँ कि लोग वही चीज़ें करें जिसे करने में उन्हें मज़ा आता है, तो इतना काफ़ी होगा उन चीजों से विवेकहीनता और विकृति हटाने में जो इन गतिविधियों के काम में बदलते ही पैदा हो जाती है।
उदाहरण के तौर पर मुझे थोड़ा-बहुत (ज़्यादा नहीं) पढ़ाने के काम में मज़ा आएगा, पर मुझे मजबूर और बेमन के छात्र नहीं चाहिए और न ही मैं दयनीय किताबी पंडित बनना चाहूँगा।
दूसरे, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जिन्हें लोग कभी-कभी थोड़ी देर के लिए करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं और हमेशा तो बिल्कुल ही नहीं। बच्चों के साथ के लिए आप कुछ घंटे किसी बच्चे के साथ बिता सकते हैं, पर उतना बिल्कुल नहीं, जितना उनके माँ-बाप। किसी भी माँ-बाप को यह अच्छा लगेगा अगर आप उनके बच्चे के साथ थोड़ा समय बिताएँ, उन्हें कुछ ख़ाली समय भी मिल जाता है पर अगर लंबे समय तक वे अपने बच्चे से अलग रहें तो उन्हें घबराहट होने लगेगी।
लोगों के बीच इन विभिन्नताओं से ही स्वतंत्र-खेल-पूर्ण-जीवन संभव है। यही सिद्धांत अन्य कई दूसरे तरह के गतिविधियों में भी लागू होता है, खासकर आदिम क़िस्म की। बहुत लोगों को ख़ाली समय में खाना बनाने मे आनंद मिलता है, पर तब नहीं, जब काम के लिए शरीर को भोजन देने की आवश्यकता हो।
तीसरे, कुछ चीज़ें अगर आप ख़ुद करें, ख़राब माहौल में करें या किसी की आज्ञा पर करें तो अच्छी नहीं लगती पर अगर दूसरी चीज़ें वैसी ही रहें और स्थितियाँ बदल जाएँ तो हो सकता है, कुछ ही देर के लिए सही, आपको मजा आए। शायद कुछ हद तक, यह सारे कामों के लिए सच है। कई बार लोग अपनी (बर्बाद हो रही) कल्पना-शक्ति से बेकार वस्तुओं का इस्तेमाल कर नवाचार से काम को भी खेल में बदल देते हैं।
गतिविधियाँ जो कुछ लोगों को अच्छी लगती हैं, वो हमेशा दूसरों को भी अच्छी लगें ज़रूरी नहीं, लेकिन हर किसी में कई क़िस्म की रुचियाँ होती हैं और क़िस्मों में रुचियाँ भी। जैसा कि कहावत है— ‘एक बार कुछ भी’।
फूरियर यह अंदाजा लगाने में माहिर था कि कैसे बुरी से बुरी भ्रष्ट तथा विकृत रुचियों को भी उत्तर-सभ्य जीवन में उपयोगी बनाया जा सकता है, जिसे वह मधुर-संगत-जीवन कहता है। उसका मानना है कि सम्राट नीरो का बदलाव संभव था, अगर उसने बचपन में ही किसी कसाईखाने में ख़ून बहाने की अपनी प्यास बुझा ली होती।
छोटे नटखट बच्चे जो गंदगी में लोटना पसंद करते हैं, उन्हें भी सुधारा जा सकता है। छोटे समूहों में बाँट दीजिए, शौचालय साफ़ करवाइए, कूड़ा फेंकवाइए और सबसे अव्वल को इनाम दीजिए। मैं ठीक इन्हीं उदाहरणों की पैरवी नहीं कर रहा, बल्कि इनमें छिपे सिद्धांत की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि पूरी तरह क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए एक आयाम के रूप में बहुत सही है।
ध्यान रहे, ऐसा नहीं है कि हमें आज का काम जस का तस उठाना है और उसमें उन जैसे लोगों को शामिल करना है, अगर ऐसा करें तो कुछ लोगों को वाक़ई विकृत होना होगा। अगर इन सब में तकनीक की कहीं भूमिका है तो वह काम को मशीनीकरण द्वारा ख़त्म करने से ज़्यादा मनोरंजन के नए क्षेत्र खोलने में है।
कुछ हद तक हम हस्तकला या हस्तशिल्प की तरफ़ वापस जाना चाहेंगे, विलियम मॉरिस के अनुसार साम्यवादी क्रांति का यह संभावित और इच्छित फल होगा। कला घमंडियों और संग्रहकर्ताओं से छीन ली जाएगी, एक कुलीन दर्शक-वर्ग की विशिष्ट दुकान के रूप में इसे नष्ट कर दिया जाएगा, और इसकी सुंदरता तथा रचना के गुण को सहज जीवन से जोड़ दिया जाएगा, जिसे काम ने हमसे चुरा लिया है।
यह एक संयत कर देने वाली वास्तविकता है कि यूनानी कलश, जिसके बारे में प्रशंसा गीत गाए जाते हैं तथा जो अजायबघर में प्रदर्शित किए जाते हैं, अपने समय में जैतून का तेल रखने के काम आते थे। मुझे संदेह है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाने वाले सामानों, शिल्पों का भविष्य इतना सुंदर होगा। सच तो यह है कि काम की दुनिया में विकास जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, अगर कुछ है तो ठीक इसका उल्टा। हमें बीते जमाने से कुछ भी उठा लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, उन्हें कोई हानि भी नहीं होती और हम अमीर भी हो जाते हैं।
रोज़ाना की ज़िंदगी को फिर से रचने का मतलब है, आज के नक़्शे-क़दम के किनारों से कूच कर देना। यह सच है कि इस बारे में हम जितना सोचते हैं, मदद करने वाले आकलन उससे ज़्यादा हैं। फूरियर, मॉरिस तथा मार्क्स में कहीं-कहीं बाए संकेतों के अलावा भी कई लोगों ने लिखा है, जिनमें क्रॉपोटकीन, सिंडिकेटवादी पटौद तथा पुगेट पूजे, पुराने अराज्यवादी-साम्यवादी बर्कमैन तथा नए बुकचीन शामिल हैं। गुडमैन भाइयों की कम्यूनीतास इस मामले में अनुकरणीय है कि यह ये सिखाता है कि दिए गए कार्यों (उदेद्श्यों) से क्या कुछ नया गढ़ा जा सकता है।
साथ ही यह भी कि एक बार नज़र भरमाने वाले तंत्र को नष्ट कर देने के बाद वैकल्पिक, सटीक, मध्यवर्ती तथा ख़ुशनुमा तकनीकों के अग्रदूतों, जैसे सुमाकर और खासकर ईलिच, के धुधंले संदेशों से क्या कुछ समेटा-बटोरा जा सकता है। परिस्थितिवादी– जैसा कि वैनिजेम के ‘रिवॉल्यूशन इन डेली लाइफ़’ तथा ‘सिचुएसनिष्ट इंटरनेशनल एंथोलोजी’ में दर्शाया गया है—बेरहमी से मौज-मस्ती और आनंद वाले हैं, भले ही उन्होंने कभी मज़दूर-परिषद् के क़ानून के समर्थन को काम के नाश के बराबर नहीं आँका।
इनकी असंगति वामपंथ के मौजूदा सारी व्याख्याओं से ज़्यादा बेहतर है। वामपंथ के भक्त काम के अंतिम समर्थक दिखते हैं, क्योंकि अगर काम न हो तो मज़दूर नहीं होंगे, और बिना मज़दूरों के वामपंथ संगठित किसे करेगा?
ज़ाहिर है काम को ख़त्म करने वाले ज़्यादातर अपने ही बल-बूते होंगे। काम द्वारा मूढ़ बना दी गई रचनात्मक शक्तियों के मुक्त होते ही क्या कुछ नया सामने आएगा, कहा नहीं जा सकता। कुछ भी हो सकता है। एक बार उपयोग-मूल्यों का उत्पादन आनंददायक खेल-गतिविधि के साथ तालमेल बैठा ले तो अपनी धर्मविज्ञानी व्यंजना के साथ नीरस वक्ता की ‘स्वतंत्रता बनाम आवश्यकता’ की समस्या का व्यावहारिक रूप से समाधान हो जाएगा।
जीवन एक खेल बन जाएगा, एक नहीं बल्कि कई तरह का खेल। लेकिन शून्य-योग जैसा खेल नहीं, जिसमें एक की जीत दूसरे की हार हो बल्कि एक ऐसा खेल, जिसमें हर कोई जीतेगा। एक बढ़िया यौन मुठभेड़ क्रीड़ा इस उत्पादक-खेल का उदाहरण मापदंड हो सकती है, खेलने वाले एक दूसरे के आनंद को तीव्र करते हैं, कोई अंक नहीं गिनता लेकिन दोनों जीतते हैं।
जितना ज़्यादा आप देते हैं, उतना ही ज़्यादा आप पाते हैं। मौज-मस्ती भरी ज़िंदगी में यौन सुख का बेहतरीन मज़ा रोज़ाना ज़िंदगी के अच्छे-खासे हिस्से में शामिल हो जाएगा।
अगर खेल आम हो तो ज़िंदगी के हर क्षण में कामुक आनंद की प्राप्ति होती है। यौन क्रिया की चाहत ज़रूरत और हताशा के रूप में कम, खेल के रूप में ज़्यादा होगी। अगर हम सही-सही खेलें, paradigm तो जिंदगी को जितना हम देते हैं, उससे ज़्यादा पा सकते हैं लेकिन तब, जब हम सिर्फ़ खेलने के लिए खेलें।
किसी को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए।
दुनिया के मजदूरो! आराम करो।
अनुवाद : मनोज कुमार झा, विनय रंजन और रूपम कुमारी
~~~
समाप्त
पहली, दूसरी और तीसरी कड़ी यहाँ पढ़िए : दुनिया के मजदूरो! आराम करो | अगर कोई कहता है कि वह ‘आज़ाद’ है... | काम से बचना सिर्फ़ अनिच्छा का मामला नहीं है
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

