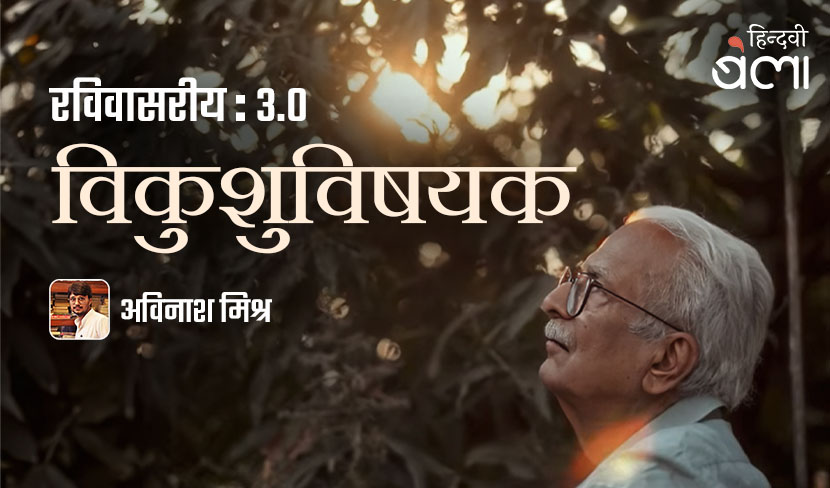अगर कोई कहता है कि वह ‘आज़ाद’ है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या मूर्ख है।
 हिन्दवी डेस्क
30 जून 2024
हिन्दवी डेस्क
30 जून 2024

...काम आज़ादी का मज़ाक़ उड़ाता है। समझाया तो यह जाता है कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और हमें सारे अधिकार प्राप्त हैं। दूसरे; जो दुर्भाग्यशाली हैं, वे हमारी तरह स्वतंत्र नहीं हैं और उन्हें पुलिसिया राज्य में रहना पड़ता है। ऐसे पीड़ित लोगों को हमेशा जी-हुज़ूरी करनी पड़ती है। अब चाहे कैसी भी मनमानी हो, नहीं तो मालिक लोग हमेशा कड़ी नजर रखते हैं।
राज्य के अफ़सरान रोज़ाना ज़िंदगी की छोटी-छोटी बातों पर भी शिकंजा कसे रहते हैं। डंडा घुमाने वाले अधिकारी वे सिर्फ अपने हुज़ूर (घोषित या अघोषित) के लिए जवाबदेह होते हैं। विरोध और नाफ़रमानी की सज़ा किसी न किसी रूप में भुगतनी ही पड़ती है। जासूस मालिक को ख़बर पहुँचाते रहते हैं। हम सभी जानते हैं कि ये सारी चीज़ें कितनी बुरी और ग़लत हैं।
तो रहें, यही है आधुनिक काम की जगह और उसकी शैली। कट्टरवादी, उदारवादी, स्वतंत्रतावादी जो भी तानाशाही को गाली देते हैं, वे नक़ली और दोमुँहें हैं। अगर हम तुलना ही करें तो किसी भी अमेरिकन काम की जगह से एक ग़ैर-स्तालिन तानाशाही में ज़्यादा आज़ादी दिखती है। दफ़्तरों-कारखानों में वैसा ही अनुशासन और अफ़सरशाही है जैसा कि जेलों, मठों में। सच कहें तो, जैसा कि फ़ुको तथा दूसरों ने भी कहा है, जेल और कारखाने लगभग एक ही समय हमारे जीवन में आए। इनके मालिकों ने मिलजुल कर जंजीरें तथा लग़ाम के तरीके ईज़ाद किए।
काम करने वाला इंसान समय की किश्तों में ग़ुलाम है। हुज़ूर तय करते हैं—कब आना है, कब जाना है और इस बीच क्या करना है। वह यह भी बताते हैं कि काम कितना करना है और कितनी तेज़ी से। वह लगामों को अपमानजनक हद तक कसने के लिए तैयार बैठा होता है, अगर उसे लगे तो वह यह भी तय करेगा कि आप क्या और कैसे पहनें और कितनी बार शौचालय जाएँ।
कुछ मजबूरियों को अगर छोड़ दें, तो वह किसी को, कभी भी, किसी भी, या बिना किसी कारण के काम से हटा सकता है। चुग़लखोरों तथा काम-निरीक्षकों द्वारा सब पर जासूसी करवाई जाती है। हर मज़दूर पर मोटी-मोटी फ़ाइल तैयार की जाती है। किसी भी बात का जवाब देना मालिक के ख़िलाफ़ विद्रोह माना जाता है। फिर न सिर्फ़ काम से हाथ धोना पड़ता है बल्कि बेरोज़गारी भत्ता भी गँवाना पड़ सकता है।
ध्यान देने की बात है, विद्यालयों तथा घरों में बच्चों के साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाता है। कहा जाता है, वे नासमझ हैं, तो उन्हें समझदार तो बनाना ही पड़ेगा न। तो क्या ये सारी बातें बच्चों के माता-पिता और शिक्षकों पर भी लागू नहीं होतीं जो काम करते हैं?
काम के हावी होने तथा हमें तुच्छ बनाने के तौर-तरीके ताउम्र हमारी ज़िंदगी में नकेल कसे रहते हैं। ज़्यादातर महिलाएँ और ज़्यादातर पुरुष अपने काम के ज़्यादातर समय में यह ज़िल्लत झेलते हैं। अगर हम अपने जीवन-समाज की व्यवस्था को लोकतंत्र या पूँजीवाद या इससे भी बेहतर उद्योगवाद कह दें तो कुछ खास ग़लत नहीं होगा, पर असल में यह कारखानों का फ़ासीवाद या गिने-चुनों की दफ़्तरशाही ही है।
अगर कोई कहता है कि वह ‘आज़ाद’ है, तो वह या तो झूठ बोल रहा है या मूर्ख है। असल में तो आप वही हैं, जो आप करते हैं। अगर आप लगातार उबाऊ, बेकार सा नीरस काम करते रहते हैं तो निश्चय ही आप भी उबाऊ, नीरस और मूर्ख बन जाएँगे। दिमाग़ का नाश तो टेलीविज़न और शिक्षा भी करती है, पर हमारे चारों तरफ़ पसरती जा रही कम-दीमाग़ी की मुख्य वजह काम ही है।
अगर कोई ताउम्र कड़े शिकंजे में कसा रहे, पढ़ाई ख़त्म होते ही काम उस पर सवार हो जाए, ज़िंदगी की शुरुआत घर और परिवार में क़ैद हो तथा जीवन का अंत अस्पतालों में हो तो इंसान ऊँच-नीच के वर्गीकरण का अभ्यस्त तो हो ही जाता है। साथ ही मानसिक रूप से ग़ुलाम भी हो जाता है। मुक्त (स्वायत्त) होने की हमारी भूख इस कदर कुचली गई होती है कि हमें आज़ादी से डर लगने लगता है, और यह डर (फोबिया) विवेकहीन या तर्कहीन नहीं होता।
जी-हुज़ूरी की दीक्षा काम की जगह से पसर कर घर-परिवार में घुस जाती है और कई रूपों में सामने आती रहती है। फिर राजनीति हो या संस्कृति या कुछ और, हर जगह इसका विस्तार होता जाता है। एक बार काम हमारी जीवन-शक्ति चूस ले तो हम हर जगह ऊँच-नीच के वर्गीकरण और दक्षता के सामने नतमस्तक होते रहते हैं। हम इसके अभ्यस्त हो जाते हैं।
हम इस कदर काम की दुनिया में फँस गए हैं कि हम नहीं देख पाते, वह हमारे साथ क्या-क्या कर रहा है। हमें इतर समय और समाज के लोग चाहिए जो देख पाएँ और हमारे बीमार वर्तमान की गंभीरता को समझ पाएँ। हमारे ही सामाजिक जीवन में एक समय था, जब ‘काम-नीति’ हमारे समझ से बाहर होती थी। शायद वेबर का कुछ मतलब था, जब उसने इसकी शुरुआत को एक धर्म, कॉल्विनवाद, से जोड़ा; जो अगर चार सदी पहले की बजाय आज उभरी होती तो तुरंत (शायद सही भी) एक सनक (कल्ट) के रूप में हम पर चस्पा हो जाती।
मामला कुछ भी हो, हम पुराने समय के विवेक और समझदारी से ही काम को सही तरीके से देख और समझ पाएँगे। पुराने लोगों ने काम को काम के रूप में ही देखा और उनकी समझ, कुछ कॉल्विनवादी सनकियों के बावजूद, तब तक क़ायम रही, जब तक उद्योगवाद ने उसे उखाड़ न फेंका, पर उनके मसीहाओं के समर्थन के बिना शायद यह संभव न होता।
चलिए एक क्षण को मान लेते हैं कि काम इंसान को बेवक़ूफ़, दब्बू या आज्ञाकारी नहीं बनाता। यह भी मान लेते हैं, हालाँकि यह मनोविज्ञान तथा एक खास तरह की विचारधारा के विद्वानों की नाफ़रमानी होगी कि हमारे स्वभाव व चरित्र के बनने में काम का कोई असर नहीं पड़ता। और यह भी मान लें कि काम उबाऊ, थकाने वाला तथा अपमानित करने वाला नहीं होता, जैसा कि यह होता है। तब भी, काम हमारी मानव-सुलभ तथा लोकतांत्रिक इच्छाओं का फिर भी मखौल ही उड़ाता है, क्योंकि यह हमारा बहुमूल्य समय खा जाता है।
सुकरात ने कहा है कि अकुशल मज़दूर अच्छे दोस्त या नागरिक नहीं बन सकते, क्योंकि दोस्ती या नागरिकता की ज़िम्मेदारी निभाने के लिए इनके पास समय ही नहीं होता। वह सही था। काम का दबाव ही ऐसा होता है कि चाहे हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं, बार-बार घड़ी की तरफ़ देखना मज़बूरी होती है। ख़ाली समय की एकमात्र विशेषता यह होती है कि मालिक को इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते।
ख़ाली समय का ज़्यादातर हिस्सा काम के लिए तैयार होने, काम पर जाने, काम से वापस लौटने तथा काम से हुई थकान मिटाने में जाता है। अगर कड़वे सच को हल्के ढंग से कहें तो ख़ाली समय वह समय है, जब उत्पादन के एक साधन के रूप में मज़दूर न सिर्फ़ अपने-आप को अपने ही ख़र्चे पर काम की जगह से ले जाता और ले आता है, बल्कि अपने-आप को काम के लायक़ बनाए रखने की अहम ज़िम्मेदारी भी निभाता है।
कोयला या लोहा ऐसा नहीं करते। लेथ मशीन या टाइपिंग मशीन ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मज़दूर ऐसा करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि एडवर्ड जी रॉबिंसन ने अपनी अपराधियों वाली एक फ़िल्म में कहा है—काम मूर्खों या दुर्बलों के लिए होता है।
प्लूटो तथा ज़ेनोफोन, दोनों सुकरात को इस समझ की अगुआई का श्रेय देते हैं। साथ ही समझ को साझा भी करते हैं कि इंसान तथा नागरिक के रूप में मज़दूर पर काम का बेहद नुक़सानदेह असर पड़ता है। हेरोडोटस के अनुसार काम के प्रति नफ़रत प्राचीन ग्रीस में, जब वहाँ संस्कृति-समाज अपने चरम पर था, तभी पैदा हो गई थी। अगर हम रोम से ही एक उदाहरण लें तो सिसरो ने साफ़ कहा है, “जो कोई भी पैसे के बदले अपना श्रम देता है, वह ख़ुद को बेचता है और अपने को ग़ुलामों की क़तार में शामिल कर लेता है।”
ऐसी साफ़गोई आम तो नहीं है, लेकिन आज भी मौजूद आदिम समाजों में, जिन्हें हम प्रायः नीची नज़रों से देखते हैं, ऐसी समझ साझा करने वाले लोग हैं। जिन्होंने पश्चिमी मानव-शास्त्रियों को राह दिखाई है। पॉस्पोजिल के अनुसार पश्चिमी ईरियन के कपॉऊकूओं के जीवन में संतुलन की एक समझ है, वे रोज़ काम नहीं करते, वे हर दूसरे दिन काम करते हैं। आराम का दिन “खोई हुई ताक़त और स्वास्थ्य को वापस पाने के लिए” होता है। यहाँ तक कि अठारहवीं सदी में भी हमारे पुरखे, जो आज के जीवन की राह पर काफ़ी आगे निकल चुके थे, कम से कम इस बात को समझ पा रहे थे कि वे क्या-क्या भूल और खो चुके हैं, उद्योग-जीवन का काला रूप उनकी नज़रों से छुपा नहीं रहा था।
‘संत मंडे’ के प्रति लोगों की श्रद्धा तब के कारखाना के मालिकों के लिए हताशा और परेशानी का कारण था, क्योंकि इससे वस्तुतः हफ़्ते में काम के दिन कुल पाँच ही बचते थे। 150-200 वर्ष पहले पाँच दिन काम के सप्ताह का क़ानून बनने से पहले तक लोगों की नाफ़रमानी जारी रही। लोगों को काम की घंटी के सामने झुकाने में लंबा समय लगा। घड़ी ईज़ाद होने से पहले घंटी का ही इस्तेमाल होता था। यह सच है कि एक-दो पीढ़ी तक वयस्क पुरुषों की जगह औरतों तथा बच्चों को काम पर लगाना पड़ा, जो जी-हुज़ूरी के आदी होते हैं और जिन्हें कारखानों की ज़रूरत के हिसाब से ढाला जा सकता है।
यहाँ तक कि प्राचीन शासन व्यवस्था में शोषित किसान भी ज़मींदारों से अच्छा-खासा समय छीन लिया करते थे। लाफार्ज के अनुसार फ़्रांस में किसानों के कैलेंडर का चौथाई हिस्सा रविवार तथा अन्य छुट्टियों से भरा पड़ा था। ज़ार के रूस के गाँवों (जो शायद ही प्रगतिशील समाज था) के संदर्भ में चायनोव का आँकड़ा भी कैलेंडर का चौथाई या पाँचवा हिस्सा किसानों के आराम को समर्पित दिखाता है।
जाहिर है, हम इन ‘पिछड़े’ समाजों से काफी पीछे हैं। शोषित ‘मुज़िक’ लोगों को आश्चर्य होगा कि हम काम करते ही क्यों हैं। यह अचरज हमें भी होना चाहिए। फिर भी, हमें अपनी दुर्दशा को पूरी तरह समझने के लिए मनुष्य के सबसे पुराने हालात की तरफ़ देखना चाहिए। तब, जब न कोई सरकार थी न ही कोई संपत्ति का बखेड़ा, जब हम शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले समूह के रूप में मौज से घूमते रहते थे।
हॉब्स का मानना है कि तब ज़िंदगी छोटी, गंदी तथा क्रूर थी। दूसरे मानते हैं कि तब ज़िंदगी जीवन बचाए रखने के लिए एक हताश और बेकार-सा संघर्ष थी, यह कठोर प्रकृति के ख़िलाफ़ एक लड़ाई थी, जहाँ मौत और आपदा कमज़ोर और दुर्भाग्यशाली लोगों की ताक़ में रहती थी। दरअसल यह अपने डर का एक बयान है कि अगर सरकार न हो तो हम क्या करेंगे? कैसे जिएँगे। हम शासन वाली जिंदगी के इतने आदी हो चुके हैं कि उसके इतर कुछ देख ही नहीं पाते, जैसा घरेलू लड़ाइयों के दौरान हॉब्स के इंग्लैंड ने महसूस किया था।
हॉब्स के कई हमवतन दूसरी तरह के समाज—खासकर उत्तरी अमेरिका में—वालों से मिल चुके थे, जो जीवन की दूसरी शैलियों को जीते थे; लेकिन वे अपनी वर्तमान राह पर इतना आगे बढ़ चुके थे कि दूसरी शैलियों को समझ पाना मुश्किल था। राह में अपने से पीछे चलने वाले समाजों (भारत के हालात जैसे समाज) को उन्होंने ज़्यादा बेहतर समझा और ज़्यादातर लुभावना भी पाया।
सत्रहवीं सदी के दौरान भारत में बसने वाले अँग्रेज़ों में से कई आदिवासियों में घुल-मिल गए, तो कइयों ने, जो युद्ध में बंदी बनाए गए थे, वापस जाने से इनकार कर दिया। जैसे पश्चिमी जर्मनी वाले कभी बर्लिन-दीवार लाँघकर पूर्वी जर्मनी जाने को लालायित नहीं हुए, उसी तरह शायद भारत के लोगों ने भी कभी गोरों के इलाकों में बसने की कोशिश नहीं की।
“योग्य की उत्तरजीविता (योग्य के बच पाने की क्षमता)”, थॉमस हक्सले का यह कथन डॉर्विनवाद का नया संस्करण है। यह विक्टोरियन इंग्लैंड के आर्थिक हालातों में जीवन को डॉर्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत की तुलना में बेहतर समझता है। अराज्यवादी क्रॉपोट्किन ने अपनी किताब “म्युचुअल एंड, अ फ़ैक्टर ऑफ़ इवाल्यूशन” में इस बात को साफ-साफ दिखाया है।
क्रॉपोट्किन एक वैज्ञानिक, भूगोल का विद्वान था, जिसे साइबेरिया में देश-निकाला दिए जाने के कारण अनचाहे ही घूम-घूम कर खोज करने का भरपूर मौक़ा मिला। उसे पता था कि वह क्या कह रहा है। ज़्यादातर सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों की तरह, हॉब्स और उनके अनुयायियों ने जो बातें कहीं, वे वास्तव में उनकी जीवनी ही थी।
मानव-वैज्ञानिक मार्शल साहलिन ने अपने समय के शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले समूहों का अध्ययन किया और आँकड़ा इकट्ठा किया। उसने अपने एक लेख ‘द ऑरिजिनल एफ्ल्यूएंट सोसायटी’ में हॉब्स के मिथकों की धज्जियाँ उड़ा दीं। वे हमारी तुलना में बहुत कम काम करते हैं और उनके काम को खेल से अलग कर पाना बहुत मुश्किल है।
साहलिन का निष्कर्ष था, “शिकारी तथा भोजन इकट्ठा करने वाले हमसे कम काम करते हैं, वे लगातार मेहनत नहीं करते, भोजन ढूँढ़ने का काम अंतरालों में होता है, उनके पास ख़ाली समय भरपूर होता है, साथ ही अन्य समाजों की तुलना में प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति दिन में सोने का समय ज़्यादा होता है”।
वे औसतन दिन में चार घंटे काम करते हैं, तब, जब हम यह मान लें कि वे जो कर रहे हैं, वह काम ही है। उनका ‘श्रम’, जैसा कि हमें लगता है, कुशल और दक्ष श्रम होता था, जिसमें शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का इस्तेमाल होता था। साहलिन के अनुसार बड़े पैमाने पर अकुशल श्रम औद्योगिक समाज से इतर लगभग असंभव है। अगर यह सच है तो यह फ़्रेडरिक शिलर की खेल की परिभाषा पर खरा उतरता है; एकमात्र अवसर, जब मानव अपनी पूरी मानवीयता को सँजो पाता है। तब, जब वह अपने सोचने और महसूस करने, दोनों को पूरी तरह खेल में डुबो पाता है।
शिलर कहता है, “जानवर तब काम करता है, जब भूखमरी सामने हो, खेलता तब है जब शरीर शक्ति से भरपूर हो, जब भरपूर-से-भरपूर जीवन ही गतिविधियों का कारण बन जाए।” इसके उलट अब्राहम मास्लोव का एक आधुनिक संस्करण भी है, जिससे विकास के ज़िद की बू आती है—मानवीय गतिविधि किसी चीज़ की ‘कमी’ और या किसी चीज़ की ‘बढ़ोतरी’ से प्रेरित होती है।
जहाँ तक उत्पादन संदर्भ की बात है, खेलकूद और आज़ादी एक साथ शुरू होती है और एक साथ ही ख़त्म होती है। यहाँ तक कि मार्क्स भी (जो अपने सारे अच्छे इरादों के बावजूद आख़िरकार उत्पादन-वाद के देवताओं में से एक है) मानता है, “आज़ादी का क्षण तबतक शुरू नहीं हो सकता, जबतक मज़दूर ज़रूरत और बाहरी उपयोगिता के लिए काम करने को बाध्य है।”
मज़दूर के पक्ष या ख़िलाफ़ में खड़े होना अजीब-सी असंगत बात है। मार्क्स शायद कभी भी इस समझ को समझ नहीं पाया कि काम ही हर दुख की जड़ है और इसका नाश ही हमारे जीवन में ख़ुशियाँ बिखेर सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं।
औद्योगिक यूरोप से पहले हर गंभीर सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास में काम से मुक्त जीवन, आगे या पीछे जा कर जैसे भी हो, में जाने की चाह साफ़-साफ़ दिखती है। इनमें से कुछ प्रमुख इतिहास वर्णन हैं—एम डॉरोथी जॉर्ज की ‘इंग्लैंड इन ट्रांजिशन’, तथा पीटर बुर्क की ‘पॉपुलर कल्चर इन अर्ली मॉडर्न यूरोप’। डैनियल बेल का लेख, ‘वर्क एंड इट्स डिस्कॉटेंट्स’ भी खासा महत्त्व का है। यह एक संपादित पुस्तक ‘द एंड ऑफ़ आइडियोलॉजी’ का पहला लेख है।
यह लेख साफ़तौर पर विस्तार से ‘काम के ख़िलाफ़ विद्रोह’ को आवाज़ देता है। यदि इसे समझा गया होता तो यह किताब की आत्मसंतोष से भरी चुप्पी को तोड़ पाता। न तो समीक्षा करने वाले, न ही विचारों के अंत की ख़ुशियाँ मनाने वाले पकड़ पाए कि बेल का ‘एंड ऑफ़ आइडियोलॉजी’ शोध-पत्र समाज के असंतोष के अंत की तरफ़ इशारा नहीं कर रहा बल्कि एक नई राह की शुरुआत की बात कर रहा है, जो किसी भी विचारधारा से बँधी या प्रभावित नहीं है।
ठीक इसी समय ‘पॉलिटिकल मैन’ में सेमूर लिप्से ने घोषणा की, “औद्योगिक क्रांति की मूल समस्याएँ हल कर ली गई हैं”। अफ़सोस कि कुछ ही वर्षों बाद कॉलेज के छात्रों के उत्तर-औद्योगिक या महा-औद्योगिक असंतोष ने लिप्से को यू सी बर्कले छोड़कर थोड़ी ज़्यादा (पर अस्थायी) शांति वाली जगह हॉवर्ड जाना पड़ा।
जैसा कि बेल ने देखा, ‘द वेल्थ ऑफ़ नेशंस’ में एडम स्मिथ बाज़ार और श्रम-विभाजन के लिए पूरे उत्साह के बावजूद एन रैंड, शिकागो अर्थशास्त्रियों, या अपने किसी भी आधुनिक दोयम दर्जे के अनुयायी की अपेक्षा काम के जघन्य पहलू की ओर अधिक सावधान और ईमानदार था।
एडम स्मिथ ने साफ़ कहा, “लोगों की ज़्यादातर समझदारी ज़रूरी तौरपर उनके सामान्य रोज़गार से ही बनती-बिगड़ती है। इंसान जिसकी ज़िंदगी कुछ सरल से कामों को करने में ही बीत जाती है। उसे अपनी समझ का इस्तेमाल करने या बढ़ाने का मौक़ा ही नहीं मिल पाता, वह उतना ही मूर्ख या अज्ञानी बन जाता है, जितना एक इंसान के लिए बनना संभव है।”
साफ़ और गाढ़े शब्दों में यह एडम स्मिथ द्वारा काम की समीक्षा है।
1950 के दशक में आइजनहॉवर के राष्ट्रपति शासन काल के समय अमेरिका नई दुनिया, नए भविष्य की तरफ़ क़दम बढ़ा रहा था, तकनीकी विकास नई करवटें ले रहा था। शांति भी थी, अमेरिका के लोग आत्ममुग्ध थे। यह समय आइजनहॉवर-पागलपन और अमेरीकन आत्मसंतुष्टि का स्वर्णकाल माना जाता है। उसी दौरान 1956 में बेल ने 1970 के दशक में उभरने वाली एक ऐसी बीमारी की तरफ़ इशारा किया, जो किसी की पकड़ और समझ से बाहर थी। कोई भी राजनीतिक समझ न इसे नियंत्रित कर पा रही थी न संभाल पा रही थी।
एच ई डब्ल्यू की एक रिपोर्ट में इसे ‘अमेरिका में काम’ के रूप में चिह्नित किया गया। इस समस्या को न तो समझा जा सकता है, न ही इसका कोई फ़ायदेमंद इस्तेमाल संभव है, इसलिए इसे सीधे-सीधे नज़रअंदाज कर दिया गया। यह समस्या है ‘काम के ख़िलाफ़ विद्रोह’।
मुक्त बाज़ार के पैरोकार अर्थशास्त्री, जैसे—मिल्टन फ़्रेडमैन, मुरे रोठबार्ड, रिचर्ड पोज़्नर इत्यादि, किसी के किसी भी लेख में इस समस्या का ज़िक्र नहीं आता क्योंकि उनकी भाषा में, जैसा कि वे स्टार ट्रैक में कहते हैं, इसका जोड़-घटाव नहीं किया जा सकता इसलिए इसका कोई मतलब नहीं निकलता।
आज़ादी के प्रेमियों का काम के ख़िलाफ़ विरोध या ऐतराज, पैतृकवादी या उपयोगितावादी धारा के मानववादियों को अगर नहीं लुभा पाया तो और कई कारण हैं, जिन्हें वे अनदेखा नहीं कर सकते। अगर एक किताब के नाम के जरिए ही बात कहें तो कह सकते हैं—काम हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। सच कहें तो काम सामूहिक हत्या या नरसंहार है। जो भी इन पंक्तियों को पढ़ रहा है, उनमें से ज़्यादातर, सीधे या किसी और तरह से, काम की मौत का शिकार होंगे।
अनुवाद : मनोज कुमार झा, विनय रंजन और रूपम कुमारी
~~~
अगली बेला में जारी...
पहली कड़ी यहाँ पढ़िए : दुनिया के मजदूरो! आराम करो।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
24 मार्च 2025
“असली पुरस्कार तो आप लोग हैं”
समादृत कवि-कथाकार विनोद कुमार शुक्ल 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। वर्ष 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना ह
09 मार्च 2025
रविवासरीय : 3.0 : ‘चारों ओर अब फूल ही फूल हैं, क्या गिनते हो दाग़ों को...’
• इधर एक वक़्त बाद विनोद कुमार शुक्ल [विकुशु] की तरफ़ लौटना हुआ। उनकी कविताओं के नवीनतम संग्रह ‘केवल जड़ें हैं’ और उन पर एकाग्र वृत्तचित्र ‘चार फूल हैं और दुनिया है’ से गुज़रना हुआ। गुज़रकर फिर लौटना हुआ।
26 मार्च 2025
प्रेम, लेखन, परिवार, मोह की 'एक कहानी यह भी'
साल 2006 में प्रकाशित ‘एक कहानी यह भी’ मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध आत्मकथा है, लेकिन मन्नू भंडारी इसे आत्मकथा नहीं मानती थीं। वह अपनी आत्मकथा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट तौर पर लिखती हैं—‘‘यह मेरी आत्मकथा
19 मार्च 2025
व्यंग्य : अश्लील है समय! समय है अश्लील!
कुछ रोज़ पूर्व एक सज्जन व्यक्ति को मैंने कहते सुना, “रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना अश्लील हैं, क्योंकि वे दोनों अगम्यगमन (इन्सेस्ट) अथवा कौटुंबिक व्यभिचार पर मज़ाक़ करते हैं।” यह कहने वाले व्यक्ति का
10 मार्च 2025
‘गुनाहों का देवता’ से ‘रेत की मछली’ तक
हुए कुछ रोज़ किसी मित्र ने एक फ़ेसबुक लिंक भेजा। किसने भेजा यह तक याद नहीं। लिंक खोलने पर एक लंबा आलेख था—‘गुनाहों का देवता’, धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास की धज्जियाँ उड़ाता हुआ, चन्दर और उसके चरित