हथेलियों में बारिश भरती माँ
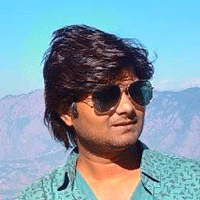 गोविंद निषाद
07 जुलाई 2025
गोविंद निषाद
07 जुलाई 2025

इलाहाबाद उस दिन मेघों से आच्छादित रहा। कुछ देर तक मूसलाधार फिर रुक-रुक कर बारिश होती रही। मैं अपने कमरे में बैठा अमरूद के पेड़ पर गिर रही बूँदों को देख रहा था। देखते हुए स्मृतियों की बूँदें मेरे मन पर भी गिरने लगीं। मन भीगने लगा। याद आया कि उन दिनों बारिश जब भी आती, माँ हाथ में कटोरा या थाली थमा देती। बूँदें छप्पर के हर उस छेद से टपकने लगती जिसे चूहों ने पूरी साल मेहनत से बनाया होता। बारिश जैसे-जैसे बढ़ती जाती बूँदें टपकने की जगहें बढ़ती जातीं। पानी ओरी से कम छेदों से ज़्यादा गिरता। यह समय होता जब खाने के बर्तनों को बूँदें बटोरने के काम पर लगा दिया जाता।
सबसे बड़ा बर्तन जैसे बाल्टी वहाँ लगाई जाती—जहाँ पानी ज़्यादा गिर रहा होता और लोटा उस जगह रखा जाता—जहाँ पानी टप-टप गिर रहा होता। माँ चूल्हे को सबसे पहले बचाती। वह उसके ऊपर एक प्लास्टिक की बोरी रख देती। फिर भी घर में पानी भरने लगता। घर के मुख्य द्वार पर पानी उलीचते-उलीचते गड्ढा बन जाता। छप्पर में जो थोड़ी जगह बच जाती, वहाँ माँ हमारा बिस्तर लगा देती। रात में पता चलता कि गोढ़वारी यानी की पैर की तरफ़ खटिया पानी से भीग गई है।
माँ सारी रात पानी उलीचती हुई, दुखी हो रही होती और यह सोचकर ख़ुश हो रही होती कि खेत में पानी भर जाएगा तो रोज़-ब-रोज़ पानी भरने से मुक्ति मिलेगी। हम सिकुड़े हुए बिस्तर में ख़ुश होते रहते कि कल जब खेतों में पानी भर जाएगा और सिवान से गुज़रने वाली नहर पानी के सैलाब से भर जाएगी—तब हम नहाने चलेंगे। पैर पर पानी गिरता रहता और हम सोते रहते। बरसात जब धीरे-धीरे झीसी में बदल जाती तो माँ भी सो जाती। पानी उलीचते और भीगते हुए हमें पता ही नहीं चलता कि हम दुखी हैं या ख़ुश।
मुझे याद है उस साल का मौसम शापित होकर आया था। सावन के बादल आसमान में ऐसे मँडरा रहे थे जैसे वह दंडित करने आए हो। उनका सफ़ेद रूई जैसा रंग भैस के काले रंग में बदलने लगा। माँ को आभास भी नहीं था कि ये बादल जब एक बार छा जाएँगे, फिर वे महीनों तक छटेंगे नहीं। माँ उस दिन भी शाम को खेतों की तरफ़ धान की निराई करने गई थी।
जब वह लौट रही थी तो उसके पीछे-पीछे काले घने बादल भी चले आ रहे थे। जैसे ही माँ पगडंडी से उतरकर घर की तरफ़ आईं। बूँदें गिरनी शुरू हो गई। घर तक पहुँचते-पहुँचते यह मूसलाधार बारिश में तब्दील हो गई। माँ ने एक लंबी दौड़ लगाई लेकिन वह बच नहीं पाईं। उन्होंने जब झोपड़ी की किवाड़ खोलकर प्रवेश किया तब तक वह भीग चुकी थी। आते ही माँ ने अफसोस किया कि आज वह खाना बनाने के ईंधन यानी गोबर के उपले और सनई की लकड़ी बाहर नहीं निकाल पाई।
जिस घर में वह भूसा रखती वह टीन की छत थी। माँ को सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी भैंस की थी। वह किसी बच्चे की तरह उसे पालती-पोसती। बच्चे की तरह पाले-पोसे क्यों न। उसके बिना हमारी आर्थिक दिनचर्या ठप्प हो जाती। भैंस के दूध और घी के भरोसे ही घर चलता। मैं स्कूल जा पाता। जो थोड़े से कपड़े मेरे पास थे—उसमें थोड़ा दूध ज़रूर मिला होता।
माँ, पिता के रिक्शे से ज़्यादा रूपए अपनी भैंस से कमा लेती। कभी-कभार माँ और पिता आपस में इसी बात को लेकर भिड़ जाते कि दोनों में से कौन ज़्यादा कमाता है। माँ, पिता को सुना देती, “अक्को पैसा तोहार लउकैला कि खाली बोलबै करैला।” पिता ग़ुस्सैल थे। उनका ग़ुस्सा बस नाक पर होता। वह किसी भी तरह माँ को बस हराना चाहते, लेकिन हर बार हार जाते—माँ के के आगे। वह माँ को बस यही कहते—“जा अपने भैंस के भरोसे रहा। हमसे मत कभ्भो पैसा माँगा।” माँ उसी रौब के साथ उन्हें सुना देती—“रख्खे रहा तू आपन पैसा, तोहरे पइसा के कवनो जरूरत ना बा हमके।” पिता का ग़ुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता। वह किसी भी हद तक जाकर माँ को हराना चाहते, इसलिए वह माँ को कुछ भी सुना देते—“जब तोके इतनै दिक्कत बा त तै हमार घर छोड़ के चल जो। जो अपने नइहरै में रह। दिहलै त हवै तोर माई-बाप।” मेरे माँ के कोई भाई नहीं थे।
नाना-नानी के पास मेरे बड़े भाई और बहन रहते थे। मरने से पहले नाना ने अपनी ज़मीन भाई के नाम पर कर दी थी, इसलिए वह बार-बार माँ को ‘नकिहवा’ चले जाने की धमकी देते। माँ बिफर पड़ती और एक साँस में सब सुना देती—“काहे जाई बतावा। ना जाब यहि रहब। कौनो काम-धाम के ना खाली आई के झगड़ा करै के बा।”
जो बादल उस दिन छाए थे, वह महीनों तक छाए ही रहे। ऐसा लगा की वह आसमान में चुंबक की तरह चिपक गए हैं। एक हफ़्ता गुज़रने के बाद आफ़त आनी शुरू हो गई। छप्पर के चारों ओर पानी भर गया जो रिस-रिसकर अंदर आने लगा। माँ चूल्हे को कितना बचाती। वह भी भीख गया। हमारे नए-पुराने-फटे सभी कपड़े भीग गए। भैंस के लिए चारा भी मिलना मुश्किल हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह हमारे लिए प्रलय लेकर आया था।
हम अब सोने के लिए दूसरों के घर जाने लगे। हमारे पैर पानी में लगातार रहने के कारण सड़ गए। अब माँ बारिश को गालियाँ देने लगी, “दहिजरा क नाती कब तक बरसी। लगत ह जीयै ना देई।” उस पर माँ की गालियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वह अपनी धुन में मस्त बरसता रहा। बारिश के हफ़्तों तक होने पर अब छप्पर पर तिरपाल लगाए जाने के सिवा कोई अन्य विकल्प हमारे पास नहीं था। अब हमें इससे थोड़ी राहत मिली थी।
जिस नकिहवा चले जाने की धमकी पिता, माँ को देते—उस गाँव का नाम एक तालाब के नाम पर पड़ा था। तालाब क्या था पूरी झील थी। एक बार गाँव के मूरत निषाद जो मेरे नाना लगते थे—उन्होंने बताया था कि उसका नाम नकिहवा ताल इसलिए पड़ा क्योंकि उस ताल में हमेशा नाक तक पानी रहता है। यह पूरे केवटहिया के लिए आजीविका का मुख्य स्त्रोत था।
यहाँ से कमाने के लिए भी लोग मछली मारते और खाने के लिए भी। शाम को पूरे गाँव में सभी घरों में सिर्फ़ मछली बनती। मैं मछली खाने का बहुत शौकीन नहीं था इसलिए कि अक्सर काँटा मेरे मुँह में फँस जाता। मैं जब भी अपने ननिहाल जाता शाम को खाने की सोचकर सिहर जाता। शाम को थाली में छोटी मछली देखकर ही मेरा पेट भर जाता। पड़ोस के मामा अक्सर मुझे सुना देते—“करे त कैसन केवट हवे, तोसे मछरी ना खवात।” मैं शर्म से लाल हो जाता। वह छोटी-छोटी मछलियों को इस तरह खाते जैसे आलू खा रहे हैं। मैं तली या भूनी मछलियों का भी पोस्टमार्टम कर देता। फिर उसके सभी भागों को अलग-अलग करता। फिर पता चलता कि खाने का कोई अंग बचा ही नहीं। निवाला मुँह में डालकर उसे मिनटों तक चुभलाता। जैसे ही निगलना चाहता कि लगता उल्टी हो जाएगी।
मैंने एक रात किसी तरह मछली खाई और सोने के लिए छत पर चला गया। गर्मियों के दिन थे। वह गाँव रात में एक टापू जैसा लगता। दूर छत से एक रोशनी चलती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने उत्सुकतावश पूछा तो किसी ने कहा कि वह भूत है जो अपना खाना बना रहे हैं। मैं ठहरा बहुत बड़ा डरपोक। मारे डर के मेरी सिट्टी-पिट्टी गुम। मैं सबके बीच में जाकर सो गया। रात में मछलियों ने अपना कमाल दिखाया। वह बाहर निकलकर पानी में जाने को छटपटाने लगीं। मैं मुँह खोलता तो लगता कि अब बाहर आईं कि तब। अचानक से मेरा मुँह खुल गया। मैं दौड़कर छत के एक तरफ़ भागा। मुझे भागता देखकर मामा के लड़के की आँखें खुल गईं। वह दौड़ता हुआ आया। मेरे पास आकर उसने पूछा कि क्या हुआ। मैं इतना लस्त हो चुका था कि मेरे मुँह से ठीक से आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरे मुँह से निकल रहा था—“उलटि गइल।”
वह हँसने लगे। तब तक और लोग भी मेरे पास आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मामा के लड़के ने कहा, “पता नहीं का कहत ह उलटि गइल।” फिर सब हँसने लगे। उन्होंने मुझसे फिर पूछा—“क्या हुआ?” मैंने फिर वही जवाब दिया, “उलटि गइल।” चारों ओर ठहाके गूँजने लगे। फिर किसी ने पूछा, “का उलटि गइल?” मुझे इसके सिवा कोई जवाब ही नहीं सूझ रहा था। सब हँसते-हँसते लोट-पोट हो गए। फिर मेरा मुँह धुलाकर मुझे सुला दिया गया।
माँ के बचपन के दिन इन्हीं मछलियों को खाते और पकड़ते बीते थे। जहाँ और गाँवों के लोगों के पास खाने के लिए राशन कम पड़ने लगता था—वहीं नकिहवा केवटहिया में खाने की कभी कमी नहीं हुई। माँ पैदा भले लड़की हुई थी लेकिन थी पूरी मर्द। ऐसा कोई काम नहीं जो माँ नहीं कर सकती थी। माँ बहुत अच्छी तैराक और शिकारी थी। वह मछलियाँ पकड़ने के कई तरीक़े जानती थी। जाल बुन सकती थी। कटिया फँसा सकती थी। तैरकर पूरा तालाब पार कर सकती थी। ऐसी कोई मछली नहीं थी जिसका नाम वह न जानती रही हो और उसे खाया न हो। माँ पानी के साँप को हाथों से पकड़कर उसकी पूँछ को घुमा सकती थी। वह वो सब कर सकती थी—जिसका संबंध पानी से था।
पानी ने माँ के जीवन को सिरजा था। हाँ कभी-कभी जब पानी बहुत बरसता और तालाब भरकर बाहर आने लगता—तब माँ को वह परेशान करता, लेकिन इसमें भी माँ आपदा में अवसर तलाश लेती। अब मछलियाँ सीधे घर ही आ जातीं। घर पर ही तालाब की मछलियाँ आकर तैरने लगतीं।
जब माँ का पिता से विवाह हुआ, तब माँ का पानी से रिश्ता टूट गया। अब माँ की आजीविका भैंस थी। वह उसे किसी भी प्रकार से परेशान नहीं देख सकती थी। माँ ने हमारे लिए कांस-फूस की झोपड़ी और जहाँ भैंस रहती और उसका भूसा रखा जाता— पर लोहे की टीन डलवा रखी थी।
उसी टीन में माँ ईंधन भी रखती। रात के समय यहाँ जाना ख़तरनाक हो सकता था क्योंकि अक्सर बरसात के दिनों में साँप यहाँ आकर अपना ठिकाना बना लेते। लगातार हो रही बारिश के बीच खाना बनाना माँ के लिए एक चुनौती भरा काम था। माँ हमें भूखा नहीं रख सकती थी। वह गई और ईंधन खीच लाई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। छप्पर से पानी जगह-जगह टपकने लगा।
एक छेद से होकर बारिश की बूँदें चूल्हे पर गिरने लगीं। माँ ने उस पर पॉलीथीन की बोरी रख दी। धीरे-धीरे छप्पर हर उस जगह से टपकने लगा—जहाँ से चूहों ने अपनी सुरंगें बनाई थीं। अब माँ ने सारे बर्तनों को पहले की तरह उसी ढंग से काम पर लगा दिया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाना बनाना मुश्किल था। माँ ने उसका एक समाधान निकाला कि चूल्हे के ऊपर छाता लगातार मैं खड़ा हो जाऊँ।
बर्तन में गिरता पानी एक संगीत की तरह लगता। टप-टप की आवाज़ कानों को सुकून पहुँचाती। सुबह अगर बारिश न थमी हो तो बाहर जाकर नित्य क्रिया करने में बहुत परेशानी होती। माँ बोरी की डोंगी बनाकर दे देती और हम उसे ओड़कर बाहर निकल जाते। फिर बाहर निकलकर देखते कि खेतों में कितना पानी लगा है। पानी भरा देखकर मन भर आता। अगला मुआयना होता नहर का। अगर पानी नहर की सतह से ऊपर निकलकर बहने लगता तो मन ख़ुश होता कि ख़ूब नहाया जाएगा।
वापसी में अक्सर मैं पूरी तरह भीग चुका होता। आते ही माँ की डाँट पड़ती। “कल का कपड़ा अभी सूखा नहीं है और यह दूसरा भी भिगा के आ गया।0” अब मैं क्या पहनूँ इसकी बड़ी चिंता रहती। फिर माँ पुराना कपड़ा गर्म चूल्हे पर रख देती। मिट्टी में मौजूद गरमी से वह हल्का-सा सूख जाता। बरसात में माँ मुझे भैंस चराने के काम से मुक्ति दे देती। नहीं तो आम दिनों में मुझे ही भैंस चरानी होती।
दिन में घर पर कोई रहने लायक़ जगह नहीं बचती। सब तरफ़ कीचड़ ही कीचड़। बिस्तर तक साफ-सुथरा पैर ले जाना संभव नहीं होता। सड़क से घर तक आने-जाने के लिए ईंट बिछाई जाती। ऊपर से फिसलकर गिरने का डर। रोज़ दो-चार लोग फिसलकर गिर जाते। कीचड़ में फिसलकर गिरने वाले को सिर्फ़ चोट ही नहीं लगती—उसके कपड़े भी कीचड़ में लिथड़ा जाते। सबसे बड़ी मुश्किल तब होती जब पता चलता कि यही आख़िरी सूखा हुआ कपड़ा था।
उन दिनों सबसे बड़ी चुनौती माँ के लिए होती—भैंस के लिए हरे चारे की व्यवस्था करना। वह भूसा नहीं खाती। माँ उसे पूरे महीने जब हलवा खिला रही हो तो वह बरसात में भात क्यों खाए। जब हरा चारा मिलना मुश्किल होने लगता, तब माँ भगवान को कोसती कि कितने दिन तक अभी और बरसेंगे। ज़्यादा बारिश से सब कुछ नम होने लगता। ऐसा लगता कि बारिश से कुछ नहीं बचा है—शरीर भी नहीं।
पैरों की उँगलियाँ सड़ने लगतीं। पैरों में कलकलाहट लगातार बढ़ती जाती। रात में पैरों को खटिया के बाध से रगड़ते कि कलकलाहट कुछ कम हो। कोई आराम नहीं होता। आराम तभी होता, जब उँगलियों मे तेल लगाकर उसकी आग में सेकाई की जाती। हाथों की त्वचा सिकुड़ जाती। शरीर का साँवलापन बढ़ने लगता। जैसे-जैसे बारिश होती जाती— नून, तेल और लकड़ी का जुगाड़ करना माँ के लिए मुश्किल होता जाता। बारिश का एक लहरा जाने के बाद दूसरे के आने के बीच में माँ सभी काम कर लेती।
हमारी पढ़ाई इन दिनों बंद हो जाती। जहाँ सोने की जगहें कम होती जा रही हो—वहाँ पढ़ने के लिए जगह बचाना मुश्किल होता। इन दिनों मैं अक्सर रात में ही घर सोने आता। दिन भर बाज़ार में पड़ा रहता। वहीं सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा होकर बरसात की लहरों का आनंद लेते। उनका आधा समय नहर में नहाने में ही बीत जाता। शाम को वापस घर आते। माँ खाना बनाकर इंतिज़ार कर रही होती। खाना खाता। अगर बारिश हो रही होती तब कुछ समय के लिए पानी उलीचने के काम से माँ को फ़ुर्सत देकर मैं पानी उलीचने का काम सँभाल लेता।
इतना होने के वाबजूद माँ और मैं दोनों बारिश का इंतिज़ार बेसब्री से करते। माँ को इसलिए इंतज़ार होता कि बिना बारिश के धान की खेती कैसे होगी। ऊपर से गर्मी से राहत भी इसी बरसात से मिलती थी। धान की रोपनी से पहले ‘जरई’ को तैयार करना ज़रूरी होता। इसे तैयार करने में पानी की बहुत खपत होती थी जो बिना बरसात संभव नहीं होती।
दूसरा उसका इंतिज़ार इसलिए भी हम करते क्योंकि बीज तैयार होने के बाद रोपनी का काम बिना बारिश असंभव था। एक खेत ऐसा था कि बिना बारिश वहाँ रोपनी हो नहीं सकती थी। इसलिए माँ इंतिज़ार करती बारिश का। उमड़ते-घुमड़ते बादलों को देखकर दोनों लोग ख़ुश हो जाते—यह जानते हुए कि बारिश हुई तो छप्पर चूने लगेगी। रूई के फाहे जैसे काले बादलों को उड़ते देखकर रोम-रोम पुलकित हो जाता। जैसे ही काले बादल क्षितिज से उगते और चढ़ना शुरू करते—मन उछलने लगता। काले बादल पूरे सिवान सहित गाँव को ढक लेते। कभी-कभी इतने काले कि दुपहर में ही रात का आभास देकर रोमांस पैदा करते।
दूर से ही बारिश होने की आवाज़ को भाँपकर हम भीगने के लिए तैयार हो जाते। भीगना वैसे भी ज़रूरी होता। कितने काम करने होते जो हो रही बारिश में ही करने हो सकते थे। दुआर पर जमा हो रहे पानी को निकालने के लिए नाली साफ़ करनी होती। अगर छप्पर कहीं बुरी तरह चूं रही हो तो ऊपर चढ़कर वहाँ प्लास्टिक की बोरी रखनी होती। इस तरह बारिश में भीगने का एक अलग सुख मिलता।
यह काम संपन्न हो जाने के बाद मैं निकल जाता सड़क पर भीगने। उसके बाद तो बच्चों की टोली पूरे मुहल्ले में धमाल-चौकड़ी मचा देती। सब लोग डाँटते कि बारिश में मत भीगो लेकिन हम कहा सुनने वाले होते। जब तक बारिश होती भीगते रहते—जब तक गर्मी में ठंडी का एहसास न हो जाए। रात में सोने पर बाहर हो रही बारिश की आवाज़ और अंदर टपकते पानी की आवाज़ नुसरत फ़तेह अली ख़ान, पंडित छन्नूलाल और पंडित कुमार गंधर्व जैसे क्लासिकल गायकों की आवाज़ की तरह मधुर गायन में बदल जाती। जितना सुख इन्हें आज सुनने में मिलता है—तब वही सुख बारिश की बूँदों से मिलता था।
पानी गिरने की आवाज़ में बारिश होने की मात्रा के अनुसार उतार-चढ़ाव होता रहता। खेतों में अचानक उग आए पीले मेंढ़कों की टर्र-टर्र, झींगुरों की चिचियाती आवाज़ें और वन मुर्गियों की आवाजें इसे और मधुर बना देती। इसे सुनते-सुनते कब गहरी नींद में मैं सो जाता—पता ही नहीं चलता। सुबह इसी धुन के साथ आँख खुलती। बाद में छप्पर की जगह टिन आ गया। पानी चूना बंद हो गया। लेकिन बूंदों का संगीत अब दोगुनी-तिगुनी आवाज़ में सुनाई देता। अब बारिश आने का सुख और बढ़ गया। पानी उलीचने और छप्पर टपकने दोनों से मुक्ति मिल गई।
बारिश आने पर मैं कब दुखी हुआ। मुझे याद नहीं। तब पता भी नहीं था कि दुख और सुख क्या होते हैं। अब मैं सोचता हूँ कि क्या इसे मैं दुख या आर्थिक विपन्नता कहूँ या मन की संपन्नता। मैंने बारिश का हमेशा से इंतिज़ार ही किया। आज भी करता हूँ। मैं उन दिनों को संघर्षमय या कष्टमय जीवन कहकर इसका तिरस्कार नहीं करूँगा।
यह जीवन के स्थायी भाव था। हमने बिना यह सोचे कि यह दुख है—उसे जिया। आज जब जीवन सुखमय हो गया है, तब यह कहना कि—“बारिश तो कष्ट देती है या मेरा जीवन संघर्षों से भरा रहा है” ठीक नहीं होगा। बारिश और पानी ने मेरे जीवन को सीचा है। आज जब पक्के मकान में रहता हूँ—तब लगता है कि जीवन उन दिनों की अपेक्षा ज़्यादा आरामदायक है, लेकिन अब मन तमाम तरह के दुखों से भर गया है। बारिश अब भी होती है लेकिन मन प्रफुल्लित नहीं होता। माँ अब कितना ख़ुश रहती है—इसका केवल अनुमान ही लगा सकता हूँ। बारिश इस बार मन पर भी बरस जाना।
~~~
सूचना : हिन्दवी उत्सव-2025 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं : रजिस्टर कीजिए
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

