‘रेख़्ता वो भाषा है जो इस्तेमाल से बनती है’
 निरंजन श्रोत्रिय
18 अगस्त 2025
निरंजन श्रोत्रिय
18 अगस्त 2025
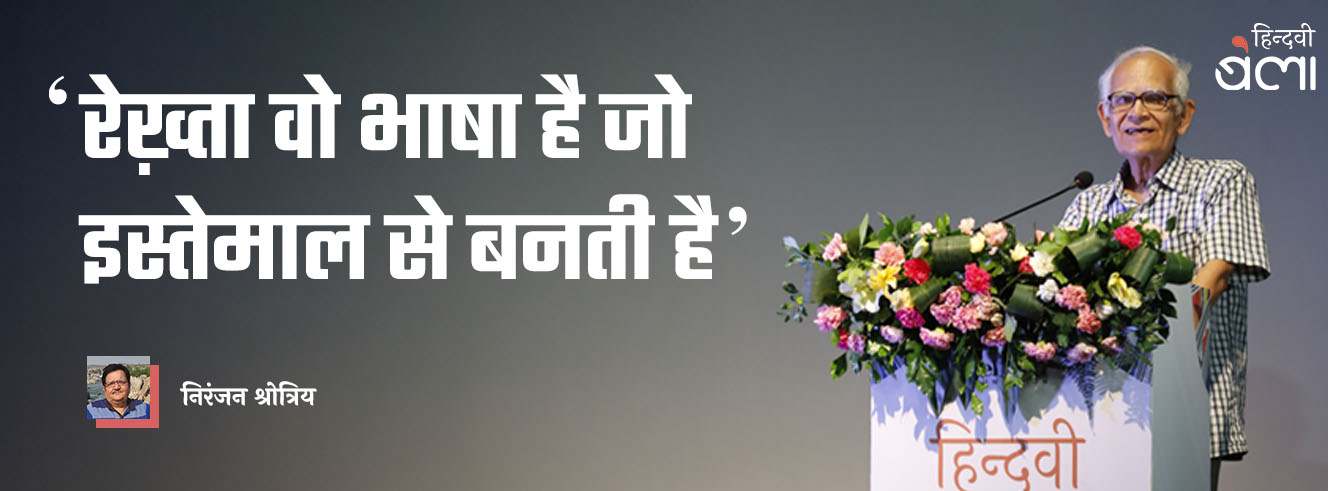
सालों पहले देश के मूर्द्धन्य शिक्षाविद् कृष्ण कुमार की एक पुस्तक पढ़ी थी—‘विचार का डर’। वैचारिक निबंधों की इस पुस्तक में शिक्षा, समाज और बौद्धिक स्वतंत्रता के परस्पर संबंधों पर गंभीर चिंतन है। शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक संरचनाओं में विचार की स्वतंत्रता और इसके दमन के विभिन्न पक्षों पर विचार करते हुए, वह तार्किक रूप से कुछ निष्कर्षों पर पहुँचते हैं। वह उन कारणों को इंगित करते हैं, जो स्वतंत्र चिंतन एवं अभिव्यक्ति को बाधित करते हैं। उनकी कई स्थापनाएँ विश्वप्रसिद्ध शिक्षाविद् पाओलो फ़्रेरे की स्थापनाओं के समांतर भी हैं। वह भी शिक्षक की बहुआयामी भूमिका को रेखांकित करते हुए, उसे संस्कृति का संवाहक निरूपित करते हैं। इस किताब में उन्होंने सालों पहले उन ख़तरों को भी चीन्हा था कि कैसे सत्ता/राजनीति शिक्षा के माध्यम से युवा पीढ़ी को नियंत्रित अथवा अनुकूलित करती है।
कृष्ण कुमार के विचारोत्तेजक निबंधों एवं एनसीईआरटी (NCERT) के निदेशक के रूप में किए गए नवाचारों के कारण उनके प्रति मेरे मन में बेहद आदर था। उनसे प्रत्यक्षतः मिलने का सौभाग्य तब मिला, जब मैं वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की एक कार्यशाला के सिलसिले में एनसीईआरटी के हॉस्टल में ही ठहरा था। किताबों से अटे उनके चैंबर में पौन घंटे की मुलाक़ात में यही भाव जगा कि वह बोलते रहें और हम सुनते रहें। हाल ही में संपन्न हुए ‘हिन्दवी’ के वार्षिक आयोजन ‘हिन्दवी उत्सव’ में जब उनका वक्तव्य सुना, तब भी मनोदशा कुछ ऐसी ही बनी। काश! हमारी शिक्षा ऐसे ही हाथों में महफ़ूज़ रहती, लेकिन इस मुल्क के भाग में कुछ और ही बदा था।
लगभग चालीस मिनट के वक्तव्य में, उन्होंने भाषा की बनक, उसकी सांस्कृतिक भूमिका, सामाजिक पैठ जैसे महत्त्वपूर्ण पक्षों को सोदाहरण प्रस्तुत किया। संवादात्मक भाषा की ऐसी रवानी, व्यंजना का ऐसा सर्जनात्मक उपयोग और अकाट्य तार्किक प्रतिपादन इन दिनों कहाँ सुनने-पढ़ने को मिलता है! कबीर, रहीम, रघुवीर सहाय, प्रेमचंद, भवानी प्रसाद मिश्र, सर्वेश्वरदयाल सक्सेना, शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा, श्रीलाल शुक्ल, विनोद कुमार शुक्ल, फणीश्वरनाथ रेणु, लोठार लुत्से जैसे लेखकों के ज़रिये उन्होंने हिंदी भाषा के संघर्ष को रेखांकित किया। यह भी लगा कि कृष्ण कुमार जैसे विद्वान् सर्जक-चिंतक ही वह कारण है; जिसकी वजह से एनसीईआरटी की हिंदी पुस्तक पढ़ने वाले छात्रों की शैक्षिक, भाषिक बल्कि सांस्कृतिक समझ अलहदा होती है।
कृष्ण कुमार कहते हैं कि ‘हिंदी सेवी’ एक भ्रामक शब्द है। इस भाषा को सेवा की नहीं, बरते जाने की ज़रूरत है। इस भाषा की ग्राह्यता और लोक में इसकी पैठ ही इसे बचा पाई है और आगे भी बचा पाएगी। उन्होंने कटाक्ष किया कि तत्सम, तद्भव तक तो ठीक, लेकिन विदेशी शब्दों में उर्दू को शामिल कर लिया गया है। ज़ाहिर है कि इसके लिए हिंदी के वे ‘विद्वान् शिक्षक’ ही उत्तरदायी हैं, जो अपने कंधों पर देश का भार होने का मुग़ालता पाले कक्षा में घुसते हैं। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ और चेष्टा सक्सेना का ज़िक्र करते हुए उन्होंने भोजपुरी और बुंदेली को भी बोली नहीं भाषा ही बताया। दुर्भाग्य है कि हिंदी ने भारतीय बोलियों से ही दूरी बनाए रखी। इस दुराग्रह को दूर करने में ‘रेख़्ता फ़ाउंडेशन’ जैसी सशक्त संस्था की निर्णायक भूमिका हो सकती है।
कृष्ण कुमार ने कहा कि इसमें बहस की कोई गुंजाइश नहीं कि हिंदी एक समय राष्ट्र के स्वतंत्रता-आंदोलन का बड़ा प्रतीक थी। बाद में यह राष्ट्रीयता और बराबरी का भी प्रतीक बनी रही, लेकिन इसका दुष्प्रभाव यह हुआ कि हिंदी इस तरह सत्ता के निकट आती गई। सत्ता और वाणी के केंद्र एक-दूसरे से जितने दूर रहें, दोनों का उतना ही भला होता है। इस निकटता से वाणी का नुक़सान अधिक होता है।
“कई बार लगता है कि मैं व्यंजना की मरुभूमि में पहुँच गया हूँ।” जैसे महत्त्वपूर्ण वाक्य बोलते हुए कृष्ण कुमार व्यंजना की पारंपरिक कंडीशनिंग पर सवाल उठाते हैं। तो क्या वाक़ई हिंदी केवल अभिधा या संदेश की ही भाषा रह गई है? उनका यह हिंदी ही नहीं हर भाषा के लिए एक अद्यतन और ज्वलंत सवाल है और यह भी कि आपके सिलेबस में जो ‘मॉडल आंसर’ है, उसके बरक्स किसी कविता को पढ़ते हुए छात्र के भीतर उपज आए नए बिंबों की कोई जगह नहीं! कैसे हम हिंदी भाषा की इन गहराइयों को अपनी अगली पीढ़ी तक सौंपेंगे जो हमें लेखकों की एक सुदीर्घ परंपरा से मिली है? आज सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम अपने समय में व्यंजना के दरवाज़े खोलें। यह सबसे बड़ी शब्द शक्ति है जिसके ज़रिये सत्य की रक्षा कितने ही दमघोंटू समय में की जा सकती है। हमारे बच्चे अपनी भाषा में और कुछ भले न सीखें केवल चीख़ना सीख लें। यह चीख़ जिस दिन सुन ली जाएगी; उस दिन हमारी हिंदी केवल प्रतीक नहीं, स्वतंत्रता की संवाहक बन जाएगी।
और साथियो, यह कृष्ण कुमार की समापन टिप्पणी (concluding note) नहीं है। वह कहते हैं कि अब तो तालाब में केवल एक ही फूल को खिलने की इजाज़त है! मैं बॉटनी का प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तालाब में खिलने वाले और भी बेहद ख़ूबसूरत पौधे होते हैं, वह तो है ही जिसका ज़िक्र हुआ।
अंततः व्यंजना में ही इस टिप्पणी का अंत—दुष्यंत कुमार के इस शे’र से :
अब तो इस तालाब का पानी बदल दो यारो
ये कँवल के फूल अब मुरझाने लगे हैं
~~~
कृष्ण कुमार का वक्तव्य यहाँ सुन सकते हैं : कृष्ण कुमार
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
