जन्मशती विशेष : युक्ति, तर्क और अयांत्रिक ऋत्विक
 बेबी शॉ
04 नवम्बर 2025
बेबी शॉ
04 नवम्बर 2025
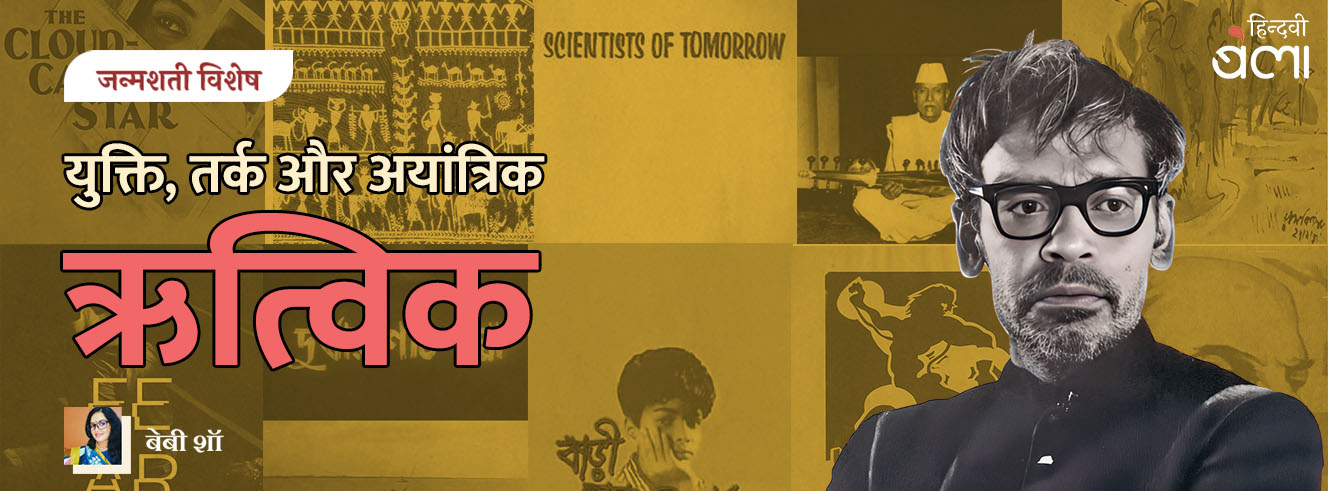
—किराया, साहब...
—मेरे पास सिक्कों की खनक नहीं। एक काम करो, सीधे चल पड़ो 1/1 बिशप लेफ़्राॅय रोड की ओर। वहाँ एक लंबा साया दरवाज़ा खोलेगा। उससे कहना कि ऋत्विक घटक टैक्सी करके रास्तों से लौटा... जेबें खाली, सपने भारी। वह तुम्हें किराया थमा देगा।
वह लंबा पुरुष—कहते हैं कि हर बार, बार-बार किराया चुकाता रहा। ऋत्विक उसे छेड़ते, पर दिल खोलकर कहते, ‘‘भारत की धरती पर कैमरे की आँख को सबसे सटीक बिठाने का जादू उसी लंबे साये को आता है।’’ वह फिर मुस्कुराकर जोड़ते, ‘‘हाँ, और मैं भी थोड़ा-बहुत जानता हूँ।’’ वह लंबा साया जिसके लिए सिनेमा का हर रंग, हर सपना; ऋत्विक की लेखनी में ढल चुका था, वह थे—एक और किंवदंती—सत्यजित रे। ‘अयांत्रिक’ के परदे पर नज़र पड़ते ही सत्यजित ने कहा, ‘‘यदि ऋत्विक बाबू वक़्त की धारा के साथ यह चित्र दिखा पाते, तो वह राह दिखाने वाले सितारे होते।’’
यहाँ हम इस विषय पर अगर और विचार करें तो देखेंगे कि ऋत्विक घटक की सिने-भाषा केवल सिनेमा जैसे कला-माध्यम के प्रति ईमानदार रहने के लिए ही नहीं थी। इसके पीछे उनका गहरा राजनीतिक दर्शन था। यह दर्शन निश्चित रूप से वामपंथी विचारधारा का था; लेकिन यह इस प्रकार वामपंथ था, जो हर पल स्वयं से सवाल उठाने का एक संदर्भ रचता है।
ऋत्विक की फ़िल्म ‘नागरिक’ से ही हम देख सकते हैं कि वह हमें सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। वह हमें झकझोरते हैं। यहाँ हम केवल एक फ़िल्म देखकर, मनोरंजन के लिए समय बिताकर, थोड़ा आराम करके अपने रोज़मर्रा के काम में वापस नहीं लौट सकते। उनकी फ़िल्में हमारे भीतर एक नई चेतना जगाती हैं। ऐसी चेतना जो हमें असहज करती है; जो हमारे जीवन को एक नीरस, जड़ जलाशय जैसे अस्तित्व से मुक्त करती है।
ऋत्विक की फ़िल्में हमें वह पारंपरिक सिनेमा नहीं दिखातीं जो हम आमतौर पर देखते हैं; बल्कि वे हमें उस दुनिया में ले जाती हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। इस भावनात्मक अनुभूति को रचने के लिए वह प्राचीन टोटेम, टैबू और विश्वासों के प्रतीकों का उपयोग करते हैं। इस वजह से ही उनकी फ़िल्मों में देश या बंगाल की मातृप्रतिमा का आर्किटाइप बार-बार लौटता है। चाहे वह ‘तितास एकटी नदीर नाम’ हो, ‘कोमल गंधार’ हो, ‘सुवर्णरेखा’ हो या ‘मेघे ढाका तारा’ हो—हम देख सकते हैं कि ऋत्विक का बनाया एक भी फ़्रेम अराजनीतिक नहीं है। वह हमें उसी तरह असहज करते हैं; जैसे जीवनानंद दास हमें असहज करते हैं, हालाँकि जीवनानंद दास ने जिस तरह ‘नगर की महान् रात्रि को लीबिया के जंगल जैसा’ देखा, ऋत्विक ने उस तरह नहीं; बल्कि उन्होंने एक अनूठे अंदाज़ में अपनी फ़िल्मों में एक तरह का तंत्र रचा। यही कारण है कि ऋत्विक की सिने-भाषा अन्य सभी फ़िल्म-निर्माताओं की भाषा से बेहद अलग है।
ऋत्विक ने स्वयं कहा था, “जिस दिन सिनेमा से भी अधिक शक्तिशाली कोई माध्यम उभरेगा, मैं सिनेमा को ठोकर मारकर उसकी ही राह पकड़ लूँगा—आई डॉन्ट लव फ़िल्म्स...” इस वाक्य से यह स्पष्ट होता है कि उनका मन सिनेमा-मोह में नहीं फँसा था, न ही वह किसी कला-माध्यम की भक्ति या अंधभक्ति से बँधे थे। उनके लिए कला आत्म-उद्देश्य नहीं थी, बल्कि विचारों को उकेरने का हथियार थी।
ऋत्विक एक जगह कहते हैं, ‘‘चलचित्र कला में मैं नहीं, बल्कि वे जो विश्व के सबसे गंभीर कलाकार हैं और मेरे बांग्लादेश में भी जो गंभीर कार्य करते हैं; जिनके नाम-धाम आपने सुने-टुने हैं, वे सभी एक व्यक्ति से प्रेरित हैं और वह व्यक्ति हैं—सर्गेई आइज़ेंस्टाइन। अगर आइज़ेंस्टाइन न होते, तो हम काम-काज का ‘क’ भी नहीं सीख पाते। वह हमारे पिता हैं। हमारे गुरु। उनकी रचनाएँ, उनके सिद्धांत और उनकी फ़िल्में—इन सबने बचपन में हमें दीवाना बना दिया था... और तब ये आसानी से उपलब्ध नहीं होती थीं। बड़ी मुश्किल से, छिपाकर-छिपाकर इन्हें लाया जाता था। ये आइज़ेंस्टाइन... आप सत्यजित रे से भी पूछ सकते हैं, वह स्वीकार करेंगे कि वह हमारे पिता हैं और उनसे ही हमने फ़िल्म काटना सीखा... फ़िल्म-निर्माण में यह एक बड़ी बात है। फिर पुडोवकिन साहब। पुडोवकिन 1949 में आए थे। तब मुझे सौभाग्य मिला था—पार्टी की ओर से... पार्टी ने मुझ पर यह ज़िम्मेदारी डाल दी कि पुडोवकिन के पीछे-पीछे थोड़ा घूमो। उस दिन पुडोवकिन ने मुझे एक बात बताई थी, जो मेरी शिक्षा का आधार बनी। वह यह थी कि फ़िल्म बनाई नहीं जाती। ‘फ़िल्ममेकिंग’ शब्द बकवास है। फ़िल्म बनती है—ईंट से ईंट जोड़कर। एक मकान जिस तरह बनता है, उसी तरह फ़िल्म शॉट-दर-शॉट काटकर बनाई जाती है। यह बनती है। यह बनाई नहीं जाती।’’
ऋत्विक आगे एक और साये का ज़िक्र करते हैं। वह हैं—लुई बुनुएल। वह लिखते हैं, “फ़िल्म का मर्म क्या है, यह मुझे उन चंद सितारों से मिला।”
ऋत्विक कला के जन्मजात राही थे। सिनेमा उनकी रगों में बहता था। यह सच निर्विवाद है कि वह कला के जिन पथों पर चले—कहानी, नाटक और यहाँ तक कि निबंध—उनमें सिनेमा के प्रति उनकी उदारता सागर-सी गहरी थी, जिसमें उन्होंने जीवन भर प्रयोगों के रंग भरे। यही वजह है कि ‘अयांत्रिक’ में वह यंत्र और मानव-सभ्यता का द्वंद्व बुनते हैं, ‘मेघे ढाका तारा’ में नीता की माँ का चित्र रचते हैं, ‘सुवर्णरेखा’ में माधवी मुखोपाध्याय के किरदार में पुराणों की सौंधी छाप उकेरते हैं और फिर ‘तितास एकटी नदीर नाम’ एवं ‘युक्ति, तक्को आर गप्पो’ में मानवता की गहरी छुअन बिखेरते हैं। इन फ़िल्मों के परदे पर काँटेदार तारों की रक्तिम कथा सजती है। प्रेम के गहन दृश्यों में भी वह पल अनमोल हो उठता है, जब उस पार बंगाल की ओर रवाना ट्रेन का स्वर गूँजता है और आगमनी-विजया का ग्रामीण राग हृदय को छू लेता है। प्रेम का ज़िक्र करते हुए ऋत्विक ख़ुद लिखते हैं, “मैं कभी उन घिसे-पिटे, प्यार-मोहब्बत के साधारण क़िस्सों में नहीं उलझता—जहाँ एक लड़का, एक लड़की प्रेम में डूबते हैं; पहले जुदा रहकर दुख भोगते हैं, फिर मिलन की राह पाते हैं या कोई बिछड़कर मिट्टी में मिल जाता है। ऐसी बनावटी और सजीली कहानियाँ लिखकर या परदे पर दिखाकर भोले दर्शकों को हँसी-आँसुओं में डुबो देना, दो पल में उन्हें कहानी से बाँध देना और फिर उनके द्वारा वह सब भूलकर हँसते-खिलखिलाते घर लौटकर खा-पीकर सो जाने में मेरा वजूद नहीं।”
हमने ‘युक्ति, तक्को आर गप्पो’ में देखा कि कैसे तृतीय धारा की क्रांतिकारी राजनीति से जुड़े युवाओं के बीच स्वयं ऋत्विक द्वारा निभाया गया नायक ‘नीलकंठ’ एक गहन राजनीतिक संदर्भ बुनता है। ऐसा तीखा और विचारोत्तेजक संवाद हमें गोदार और मिगुएल लिट्टिन की फ़िल्मों में मिलता-झलकता है। यह फ़िल्म ऋत्विक का लिखा एक काव्यात्मक निबंध ही है। नीलकंठ, इसमें कोई संदेह नहीं, स्वयं ऋत्विक का ही प्रतिबिंब है।
वह कहते हैं, “सोचो, गहराई से सोचो, सोच को साधना बनाओ...” यह वचन हमारी भाषा में एक अमर उक्ति बन गया। ‘युक्ति, तक्को आर गप्पो’ के अंतिम दृश्य में, भोर की पहली किरणों में डूबकर वह पुकारते हैं, “मैं एक बार सत्य का साक्षात्कार करना चाहता हूँ।”
ऋत्विक हमारे हृदय में यूँ ही साँस लेते हैं। वह हमें मनोरंजन की मृदु लहरों में नहीं बहाते, बल्कि एक अनवरत असहजता के भँवर में डुबो देते हैं। वह जिस सत्य का साक्षात्कार अपनी फ़िल्मों में तलाशते हैं, उसी सत्य को वह दर्शकों के हृदय तक ले आते हैं। अविभाजित बंगाल की माटी में उनका बचपन बीता, औपनिवेशिक भारत के छायाचित्र में, पर कोलकाता की उस आधुनिकता से कोसों दूर जो औपनिवेशिक रंग में रँगी थी। वह पूर्वी बंगाल की उस ग्रामीण धरती में पले; जहाँ नदियाँ माँ-सी बाँहें फैलाए प्रकृति के कंठ में बसती थीं, जहाँ साम्राज्य और यंत्र-सभ्यता की जकड़न हमेशा ढीली रही।
“ऋत्विक दा, आपकी हर फ़िल्म में दो बंगालों के बँटवारे को लेकर बहुत कोलाहल है!”
“कोलाहल! बंगाल को टुकड़े-टुकड़े करके चूर-चूर कर दिया, और कोलाहल! इस तूफ़ानी वक़्त में क्या मैं नाचूँ-गाऊँ? यह तो सरासर बदमाशी है! मैं उन नीचों को... स्साले हरामी! मैं दिल से चाहता हूँ, जी-जान से चाहता हूँ कि दोनों बंगालों की संस्कृति को एक फ़्रेम में बाँध लूँ। तुम मुझे मार्क्सवादी कहो या कुछ और, लेकिन विरोध का आलम तो बुनना ही होगा। पर स्साला, कोई समझा ही नहीं!”
ऋत्विक नशे में डूबे हुए हैं! एक-एक कर शराब की बोतलें ख़ाली हो रही हैं! सितारे टूटकर बिखर रहे हैं...
यह जगह कोई ख़लासीटोला नहीं थी, बल्कि यह जगह थी—ऑटोमोबाइल एसोसिएशन क्लब...
‘युक्ति, तक्को आर गप्पो’ के बाद एक क़रीबी पत्रकार ऋत्विक से उनकी नई फ़िल्म की बात छेड़ रहा था। वह बता रहे थे—‘विष्णुप्रिया’ नाम की एक फ़िल्म का सपना। तभी देश-विभाजन का ज़िक्र छिड़ा और बस तूफ़ान उठ खड़ा हुआ!
“इस देश के कम्युनिस्ट...!”
“हरामख़ोर! सारे अनपढ़ों का झुंड! कोई कुछ समझता ही नहीं। छोड़ो ये सब! मेरी फ़िल्म की कहानी सुनो!”
...आग अभी बाक़ी थी। ऋत्विक की उत्तेजना भरी कहानी के बीच, हंगामे का राग छेड़ते हुए मंच पर त्रयी अवतरित हुई—शक्ति चट्टोपाध्याय, सुनील गंगोपाध्याय, संदीपन चट्टोपाध्याय! पास ही बैठे पूर्णेंदु पत्री ने ख़तरे की घंटी सुन ली। कवि तुषार रॉय भी वहाँ थे। उनकी यादें कहती हैं कि शराब के सुरूर में डूबे शक्ति चट्टोपाध्याय अचानक उठ खड़े हुए। वह सबकी पीठ थपथपाते हुए ऋत्विक की फ़िल्म की तारीफ़ों के पुल बाँधने लगे। फिर वह ऋत्विक के पास पहुँचे, उन्हें गले लगाया और झकझोरने लगे। ग़ुस्से में तिलमिलाकर ऋत्विक खड़े हो गए!
एक पल में शराबख़ाने के आलम ने सन्नाटे की चादर ओढ़ ली!
ऋत्विक गरजे, “शराब पीकर हुल्लड़ मचाना मेरे बस की बात नहीं! इससे नशे का रंग फीका पड़ जाता है और सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है!”
अविभाजित बंगाल ऋत्विक के सौंदर्यबोध का प्राण बना, शायद इसलिए कि उनकी स्मृतियों में वह प्राकृतिक विस्तार सदा थिरकता रहा। उनकी रचनात्मकता, कला और अविभाजित बंगाल की साझा स्मृतियों के ताने-बाने में ही उनकी फ़िल्मों में प्रकृति का वैभव जीवंत होता है। पर मुझे लगता है कि प्रकृति के ये दृश्य केवल सौंदर्य नहीं, बल्कि सत्ता को चुनौती देने वाली एक काव्यात्मक भाषा बन गए। आशिष राजाध्यक्ष ने उजागर किया था कि ऋत्विक की फ़िल्में मिथकों को चूर करने के लिए बुनी गई हैं। मिथक यानी वे धारणाएँ जो समय की गलियों में चलते-चलते निर्विवाद सत्य का रूप ले लेती हैं, वे चित्र जो किसी संस्कृति के हृदय में बहुसंख्यकों की स्वीकृति पाते हैं।
बेर्टोल्ट ब्रेष्ट कहते हैं कि जब कला आधिपत्यकारी नज़रिये और सत्ता के बीच की कड़ी को अभिव्यक्त करती है, तभी मिथक सवालों के कठघरे में खड़ा होता है।
ऋत्विक ने प्रकृति के दृश्यों के माध्यम से अपनी फ़िल्मों में उस मिथक पर प्रहार किया, जो औपनिवेशिकता और उसके बाद राष्ट्र-राज्य की नींव में बसता है—राष्ट्रीय प्रगति और प्रकृति से कटे सभ्यता के उत्थान का मिथक। इस प्रहार का निशाना बनी सीमाएँ, यांत्रिक समय की कठोर गति और औपनिवेशिक ढाँचे में गुँथा शोषण का सिलसिला। यह सिलसिला वर्ग, लिंग और अन्य अदृश्य विभाजन-रेखाओं के रूप में राष्ट्र के शरीर में चुपके से साँस लेता है। जैसे 1950 से 1955 के बीच नाइजीरिया के इबादान विश्वविद्यालय में ‘इबादान स्कूल ऑफ़ हिस्ट्री’ की स्थापना हुई। पश्चिमी इतिहास-लेखन की पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए इस स्कूल ने अफ़्रीका, विशेष रूप से नाइजीरिया, के अपने इतिहास को रचने का एक नया तरीक़ा अपनाया। यहाँ मान्यता थी कि यह पद्धति अफ़्रीकी समाज के विकास की आंतरिक गतिशीलता को उजागर कर सकती है। इसका मुख्य आधार मौखिक परंपरा थी जो कहानियों, कहावतों, गीतों, नृत्यों और लोकाचार के माध्यम से स्मृतियों को संरक्षित करती है। इन मौखिक परंपराओं में अफ़्रीका के इतिहास का बहुआयामी, समृद्ध और विविध स्वरूप छिपा हुआ है।
पश्चिमी दावे कि ‘अफ़्रीका का कोई इतिहास नहीं’ या ‘उसका इतिहास केवल औपनिवेशिक प्रभाव का परिणाम है’—इन धारणाओं को ख़ारिज करते हुए इबादान स्कूल ने नाइजीरिया की अपनी ऐतिहासिक पहचान की खोज की। मौखिक परंपराओं को उन्होंने इतिहास के वैध स्रोत के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने विशेष रूप से नाइजर डेल्टा क्षेत्र, नाइजर नदी और उसकी असंख्य शाखाओं व उपनदियों में मौखिक इतिहास का एक विशाल संग्रह तैयार किया।
ऋत्विक तब अपनी माँ और बहनों के साथ बालीगंज प्लेस के घर में सपनों और जद्दोजहद के ठिकाने पर थे, जब सुरमा शिलॉन्ग की पहाड़ियों को अलविदा कहकर कोलकाता में अपने मामा के आँगन में एमए की पढ़ाई के लिए उतरी।
ऋत्विक रोज़ सुरमा को पढ़ाते थे। वह किताबों के पन्नों में लेनिन, मार्क्स, प्लेख़ानोव की रोशनी बिखेरते। वह बातों की माला में तर्क और विश्वास पिरोते। वह ‘विसर्जन’ के रिहर्सल में अपर्णा का किरदार समझाते हुए, गहरी नज़रों से नज़रें मिलाकर कहते, “मैं बैठा हूँ भरे मन से—देना चाहता हूँ, लेने वाला कोई नहीं!”
सुरमा का मन मानो तूफ़ान में उलट-पलट गया। वह भी प्रेम-रंग में डूब गई!
एक दिन ऋत्विक का मन उदास था। वह पढ़ाते-पढ़ाते जेल के दो साल की कहानी सुनाने लगे। वह बचपन में माँ के बिछड़ने की टीस उकेरने लगे। यहीं हुआ—पहले प्रेम का पहला निवेदन!—“लक्ष्मी! तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूँगा, तुम्हें सब कुछ दूँगा!”
इस मुग्धता में दो दिल ठहर गए, नज़रें टिक गईं! रिहर्सल में देर हो गई। इसके बाद कोलकाता की हवाओं में उनकी नज़दीकियों की चर्चाएँ तैरने लगीं। घर की मनाही और गणनाट्य की फुसफुसाहट को ठुकराकर सुरमा ने स्क्वॉड बदल लिया। वह हर दिन ऋत्विक के घर पढ़ने के बहाने चली जाती। ऋत्विक लौटते वक़्त उसे सुनाते—हावड़बिल की जल-कथाएँ, मयमनसिंह और राजशाही की बातें, ‘बेदिनी’ का सुरमयी राग...
एक रोज़ संध्या की गलियों में टहलते हुए बाँसुरी की तान और तानपूरे की झंकार एक जलतरंग बनकर गूँजी।
‘नागरिक’ एक बेरोज़गार युवक का सपना थी—घर बसाने, ज़िंदगी सँवारने का सपना। यह फ़िल्म ऋत्विक ने अपनी जेब की आख़िरी कौड़ी लुटाकर बनाई थी। भूपति नंदी ने घर गिरवी रखा था। किसी ने प्रोविडेंट फ़ंड तोड़ा था। पर अंत में सब बेकार! इस फ़िल्म में रामू नाम का एक युवक था। वह हर दिन कैलेंडर की तस्वीर को निहारता और रात में दूर से भटकती वायलिन की धुन सुनकर सो जाता।
“अख़बारों में ढेर सारे विज्ञापन देखे। यह फ़िल्म रिलीज़ क्यों नहीं हुई?”
“हा हा हा! शायद किसी दिन होगी! सुना, पार्टी ने मेरे ख़िलाफ़ एक आदमी का कमीशन बिठाया है? कॉमरेड प्रमोद दासगुप्ता उसका हिस्सा है!”
“जानती हूँ। ‘नीचे का महल’ के रिहर्सल से लौटते वक़्त मामी ने बताया। पार्टी तुम्हें निकाल बाहर करेगी! उमानाथ दा, काली बनर्जी, ममता अहमद ख़ान—सबने तुम्हारे ख़िलाफ़ चार्ज का समर्थन किया है!”
“फिर भी तुम...!”
“देर हो रही है, चलो।”
“लक्ष्मी!”
“कॉमरेड ज्योति बसु तुम्हारे साथ हैं; लेकिन ये पार्टी, आईपीटीए (इप्टा), तेईस चार्ज—काम नहीं करने देंगे! नया दल बनाओ। ग्रुप थिएटर!”
“लक्ष्मी! क्या तुम आओगी? तुम मिल जाओ तो ज़िंदगी नए सिरे से सजाऊँगा!”
“आऊँगी!”
प्रेम की राह पर ऋत्विक और सुरमा (लक्ष्मी) की शादी हुई, लेकिन वही सुरमा अपनी बेटी को लेकर ऋत्विक की बेतहाशा शराबख़ोरी से तंग आकर मायके लौट गई।
तरुण मजूमदार—एक और फ़िल्मकार—ने अपनी यादों में यह क़िस्सा उकेरा :
रमेश बाबू—यानी रमेश जोशी, नामी एडिटर—फ़िल्म-इंडस्ट्री उन्हें सच्चे, सात्विक, कुँवारे, थोड़े में संतुष्ट, एक दुर्लभ इंसान के रूप में जानती है। ऋत्विक की हर फिल्म के फ़्रेम उन्होंने ही तराशे।
एक दिन किसी वजह से तरुण बाबू एडिटिंग रूम की बालकनी से गुज़र रहे थे। उन्होंने देखा कि कमरा नंबर चार में मूवीओला के सामने रमेश बाबू चुपचाप बैठे हैं—अकेले...
“क्या हुआ? आज काम नहीं?”
“था। ऋत्विक आए और फिर चले गए।”
“कहाँ?”
रमेश बाबू ने हिचकते हुए बताया कि आज ऋत्विक और उनकी पत्नी की शादी की सालगिरह है।
“वह बहुत अफ़सोस कर रहे थे, ‘ऐसे दिन भी बीवी को एक साड़ी नहीं दे पाया। जेब में कुछ नहीं।’ सुनकर मन ख़राब हो गया। मैंने कुछ पैसे उनके हाथ में थमाए और कहा, ‘जाओ, अच्छी-सी साड़ी ख़रीदकर उन्हें दे आओ। देर मत करना।’”
थोड़ी देर बाद रमेश बाबू के पास एक फ़ोन आया।
दूसरी ओर से किसकी आवाज़ थी, समझ में नहीं आया। बस रमेश बाबू की बात सुनाई दी, “वह आए और फिर चले गए। शादी की सालगिरह पर बीवी को साड़ी देने के लिए मुझसे कुछ पैसे लिए।”
दूसरी ओर से क्या जवाब आया; यह भी समझ में नहीं आया, लेकिन रमेश बाबू का चेहरा अचानक असहाय, भोला-सा दिखने लगा।
“क्या हुआ?”
“और क्या! फ़िल्म के प्रोड्यूसर का फ़ोन था। मेरे से पैसे लेने और सालगिरह की साड़ी की बात सुनकर बोले, ‘क्या बात! चार दिन पहले यही कहकर मुझसे भी पैसे ले गए थे—शादी की सालगिरह, बीवी के लिए साड़ी...’”
ये थे—ऋत्विक! नदी जैसे! पानी जैसे! पहाड़ और देशांश जैसे!
ऋत्विक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए लगातार स्मृतियों की गलियों में भटकते रहते हैं। वह जैसे यादों की धूप में जलते जा रहे हों।
“जब ‘ज्वाला’ लिखा था, तब नहीं जानता था कि खाँसी के साथ ख़ून कैसे उठता है... और आज! अब जीना नहीं चाहता। इन सुअरों के बच्चे वाले इस देश में जीने का क्या फ़ायदा?”
वह लगातार बोलते-बोलते थक जाते, हाँफने लगते! कभी-कभी ख़ून की उल्टी... ऐसी भयंकर बीमारी के बावजूद उन्होंने अपनी आख़िरी दो फ़िल्में पूरी कीं—बारिश में भीगते हुए, धूप में जलते हुए—उस पार ‘तितास एकटी नदीर नाम’ और इस पार ‘युक्ति, तक्को आर गप्पो’। पर शरीर अब और साथ नहीं दे पा रहा था।
ढाका से दुखद समाचार आया—ऋत्विक गंभीर रूप से बीमार। कोलकाता चिंतित। सत्यजित रे बेचैन। मृणाल सेन ने स्वयं जाकर उन्हें वापस लाने की ज़िम्मेदारी ली। वह लौटे... और फिर एक रोज़ बांग्लादेश में ‘तितास एकटी नदीर नाम’ रिलीज़ हुई। उस समय ऋत्विक अस्पताल में थे।
औपनिवेशिक और निम्नवर्गीय इतिहास-लेखन के कई मुद्दे ऋत्विक की फ़िल्म ‘तितास एकटी नदीर नाम’ (1973) में प्रतिध्वनित होते हैं। यह फ़िल्म नदी और मछुआरा-समुदायों के महाकाव्यात्मक इतिहास को प्रस्तुत करती है। व्यक्तिगत और सामूहिक अनुभवों के माध्यम से यह एक जीवंत ऐतिहासिक चित्रपट रचती है। 159 मिनट की इस फ़िल्म में ऋत्विक ने वैकल्पिक इतिहास-निर्माण का सशक्त प्रयास किया। इतिहास के तीव्रता से लुप्त होते इस स्वरूप के प्रति ऋत्विक बहुत सजग थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, “वह जीवन, वह स्मृति, वह उदासीनता... मुझे पागल की तरह तितास की तरफ़ खींचती है। यह फ़िल्म उन खोई स्मृतियों को श्रद्धांजलि है। इसमें कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। यह उपन्यास मेरे लिए महाकाव्यात्मक है। मैंने उस महाकाव्य को पकड़ने की कोशिश की है। इस फ़िल्म को बनाते समय मैंने महसूस किया कि उस अतीत का कोई निशान बाक़ी नहीं है, न रह सकता है। इतिहास बहुत क्रूर और निर्मम है; यह रुकता नहीं, यह क्षमा नहीं करता। यह सब कुछ खो देता है।”
इसलिए ही यह उपन्यास और फ़िल्म—दोनों ही—नदी, उसकी घाटी, मछुआरा-समुदाय, उनकी सामूहिक आकांक्षाएँ और मौखिक संस्कृति के माध्यम से एक कालातीत इतिहास की ओर संकेत करते हैं। यह इतिहास पश्चिमी तर्कवाद से नहीं; बल्कि लोगों के जीवन, श्रम और स्मृतियों से निर्मित होता है।
ऋत्विक के इस राजनीतिक चिंतन में हमारे मन के अनुत्तरित प्रश्नों की गूँज बसती है।
‘सुवर्णरेखा’ में बंदरगाह का प्रतीकात्मक चित्र—वह हृदयविदारक दृश्य जहाँ भाई अपनी बहन का वध करता है... और ‘मेघे ढाका तारा’ में नीता की वह करुण पुकार, “दादा, मैं जीना चाहती हूँ”... यह सब हमारे अपने अंतःकरण की चीत्कार बनकर गूँज उठता है। यह चीत्कार ऋत्विक की बाद की फ़िल्मों में तो है, लेकिन हमारे समकालीन फ़िल्म-निर्माताओं में इसका घोर अभाव है। सत्यजित रे की ‘महानगर’, ‘सीमाबद्ध’, ‘जन अरण्य’ और ‘प्रतिद्वंद्वी’ में यह चीत्कार गूँजता है। मृणाल सेन की ‘इंटरव्यू’, ‘भुवन शोम’ और ‘आकालेर संधाने’ में भी यह व्यथा मौजूद है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है कि नब्बे के दशक की शुरुआत से बांग्ला-सिनेमा में धीरे-धीरे यह चीत्कार और यह राजनीतिक जिज्ञासा लुप्त होने लगी। यहाँ तक कि सिनेमा की भाषा में भी बांग्ला-फ़िल्में न तो अंतरराष्ट्रीय सिनेमा की बराबरी कर पाईं, न ही भारत के अन्य राज्यों की श्रेष्ठ फ़िल्मों के समकक्ष खड़ी हो सकीं। पूँजीवाद की जिस वस्तु-संस्कृति के विरुद्ध ऋत्विक ने सिनेमा की भाषा और माध्यम से लड़ाई लड़ी, उसी वस्तु-संस्कृति के आलिंगन में बांग्ला-सिनेमा डूब गया।
आज जब हम ऋत्विक घटक की फ़िल्में देखते हैं तो जो राजनीति, जो राजनीतिक संदर्भ हम महसूस करते हैं; वह समकालीन बांग्ला-सिनेमा में समझ से परे हो जाता है। आज की बंगाली फ़िल्में देखने पर लगता है कि हमारी वास्तविकता या तो बहुत सुखमय है या अत्यंत पराक्रमी। हमारे भीतर जो स्वस्थ तर्क-वितर्क है, जो राजनीतिक द्वंद्व है, सत्य या सत्य के विविध रूपों के लिए जो संघर्ष है, जो मानसिक अस्थिरता है, जीवनानंद दास का वह जो ‘विपन्न विस्मय’ है—यह सब आज की बंगाली फिल्मों में सर्वथा अनुपस्थित है। असहज करने की संस्कृति तो दूर, अब बांग्ला-सिनेमा का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि वह मध्यमवर्गीय मनोरंजन के लिए कितना उपयुक्त है। ऋतुपर्ण घोष की फ़िल्मों में भी ऋत्विक घटक के ये राजनीतिक प्रश्न लुप्त हैं। यहाँ ऋत्विक का कहा याद करने ज़रूरत है, ‘‘वास्तविकता इतनी ‘सुंदर’ नहीं है। सत्य इतना ‘कोमल’ और इतना सजा-सँवरा नहीं है।’’
“मुझे तो टीबी है!”—दो घूँट लेते ही ऋत्विक बोले...
उन्हें ज़्यादा देर बात करने पर खाँसी उठती है। खाँसी में मुँह से ख़ून निकलता है। वह रूमाल से मुँह पोंछ लेते हैं। फिर भी जनता का कैसा अनोखा मोह! संजय लिखते हैं, “वही खाने की होड़ थी। ऋत्विक घटक की शराब थी... प्रसाद।”
“यूनिवर्सिटी में बर्गमैन का एक रेट्रोस्पेक्टिव हो रहा है, ऋत्विक दा। चलेंगे?”
“बर्गमैन सब ढोंग है, सौ फ़ीसदी जालसाज़ी। एंतोनियोनी का स्टाइल ध्रुपद-सा है। छोड़ो, जो समझ नहीं आता, उस पर तुम लोग बकबक मत करो। सुनो, आठ-दस साल बाद लोग मेरी फ़िल्में तलाशेंगे। मेरी फ़िल्मों के लिए पागल हो जाएँगे। तुम देख लेना!”
ऋत्विक की सोच और उनके सिनेमा के माध्यम से हम एक अंतर्घटना का प्रसार देखते हैं—देवेश राय और नवारुण भट्टाचार्य के कथा-संसार में। अगर आज के युग में ऋत्विक होते तो वह डिजिटल माध्यम को भी अपनी राजनीतिक चेतना को जन-जन तक फैलाने के लिए हथियार बनाते। ऋत्विक जानते थे कि उनकी फ़िल्में सोचने के लिए मजबूर करती हैं, वे सोच को साधना बनाती हैं। ऋत्विक बेहद संक्रामक हैं। फिर भी, वह पूजनीय बन गए। उन्हें न कोई गटक सका, न कोई पचा सका।
जीवनानंद दास की कविताओं में ‘विपन्न विस्मय’ मानव-अस्तित्व, समाज और प्रकृति के टकराव की गहरी अनुभूति है। ऋत्विक ने अपनी फ़िल्मों में इस विस्मय को दृश्यमान किया। ‘मेघे ढाका तारा’ में नीता की चीत्कार, ‘सुवर्णरेखा’ में नदी का प्रतीक या ‘तितास एकटी नदीर नाम’ में प्रकृति का विनाश—जीवनानंद की अस्थिरता को प्रतिध्वनित करता है। ‘युक्ति, तक्को आर गप्पो’ में—“सोचो, सोचने का अभ्यास करो”—राजनीतिक जिज्ञासा में बदल जाता है। ऋत्विक प्रकृति, वर्ग और लिंग के शोषण के माध्यम से औपनिवेशिक आधुनिकता पर सवाल उठाते हैं। वह जीवनानंद की विपन्नता को राजनीतिक भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उनकी फ़िल्में हमें सत्य की खोज में सवाल उठाने की प्रेरणा देती हैं।
ऋत्विक के राजनीतिक प्रश्न समाज में गहरे व्याप्त असमानता, शोषण और झूठ के ख़िलाफ़ एक सचेतन लड़ाई थे। उन्होंने सिनेमा को एक ऐसा माध्यम बनाया, जो न केवल मनोरंजन करता है; बल्कि दर्शकों को सोचने, सवाल उठाने और समाज के प्रति ज़िम्मेदार होने के लिए प्रेरित करता है। उनके ये सवाल आज भी हमारे बीच जीवित हैं और उनका सिनेमा हमें उस सत्य की खोज में प्रेरित करता है।
ऋत्विक अकेले थे, अकेले हैं और शायद आज भी अकेले ही लड़ रहे हैं—हमारे भीतर—हमारी चेतना के उस कोने में जहाँ सत्य, तर्क और युक्ति अब भी जीवित हैं। आइए इस क़िस्से से इस असमाप्त स्मरण को फ़िलहाल यहीं रोकते हैं...
एक लड़का—रंजन मजूमदार—‘युगांतर’ नाम के अख़बार में काम करता है। वह सिनेमा-पृष्ठ पर कभी-कभार फ़िल्मों की समीक्षा भी लिखता-टिखता है। इसके साथ ही वह कई निर्देशकों के साथ सहायक का काम भी करता फिरता है। वह थोड़ा मस्तमौला टाइप का लड़का है। एक बार किसी बात पर उसने किसी निर्देशक के काम की इतनी तारीफ़ की कि अख़बार में छपवा दी। फिर जो हुआ, वह कुछ ऐसा था।
ऋत्विक बाबू का चेहरा भले ही थोड़ा ठूँठ-सा हो, लेकिन क़द ख़ासा लंबा है... और उससे भी लंबी उनकी उँगलियाँ हैं। वह तर्जनी हिलाकर पुकारते हैं :
“ए स्साला, सुन!”
“मुझे बुला रहे हैं?”
“हाँ-हाँ, तुझे ही... तेरा नाम क्या है?”
“रंजन! रंजन मजूमदार...”
‘‘‘युगांतर’ में हर तरह की बकवास लिखता है, है ना?”
“वो, थोड़ा-बहुत...”
“इस बार भी लिखा है न, शुक्रवार को।”
“हाँ दादा, उसी दिन तो सिनेमा का पेज निकलता है, इसलिए...”
“सुना, किसी को बहुत तारीफ़ करके आसमान पर चढ़ा दिया तूने...”
“नहीं, मतलब... थोड़ा-सा...”
“चुप!” कहकर उन्होंने अपनी वह अविस्मरणीय चेतावनी दी, “अगर कभी सुना कि मेरे नाम पर भी ऐसा कुछ लिखा तो जूतों से तेरे मुँह को और लंबा कर दूँगा। मेरे नाम पर कोई तारीफ़ नहीं। समझ में आया?”
ऋत्विक अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हैं। उन्नीस दिन हो गए। सब कुछ आँसुओं से धुंधला हो रहा है। धुंधला दृश्य। शहर। कैमरा। लेंस। फ़रवरी का महीना। उम्र पचास—4 नवंबर 1925 से 6 फ़रवरी 1976 तक। एक झोले में ढेर सारे पुरस्कार—पद्मश्री, राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, बाबिसस पुरस्कार और भी बहुत कुछ...
पद्मा का तट, मेघना का चार, भैरव बाज़ार—सब कुछ धुंधला हो गया। कभी उन्होंने लिखा था, “बूढ़ीगंगा, कितने समय से तेरी गोद में सिर नहीं रखा!”
मृणाल सेन ने सुरमा को ख़बर भेजी। कोलकाता की हवा में शोक की लहर फैल गई। पीजी अस्पताल के सामने अनगिनत लोगों का सैलाब। किसी ने रवींद्रनाथ का गीत शुरू किया, “जिस रात मेरे दरवाज़े तूफ़ान से टूट गए...”—ऋत्विक का पसंदीदा गीत!
एक शवयात्रा स्टूडियो पाड़ा से होकर घाट की ओर बढ़ चली... और सौ साल पहले जन्मा एक अद्भुत पुरुष अपनी आश्चर्यजनक मस्ती और उपस्थिति, दृष्टि और दृश्यात्मकता, कविता और कैमरा, कहानी और हास्य, जीवन और मृत्यु के बीच की खींचतान में—हमारे दिलों में एक मिथक बनकर रह गया!
•••
बेबी शॉ को और पढ़िए : विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय : एक अद्वितीय साहित्यकार | काँदनागीत : आँसुओं का गीत | रवींद्रनाथ ने कहा है कि...
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
