आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ : हमरेउ करम क कबहूँ कौनौ हिसाब होई
 शैलेंद्र कुमार शुक्ल
21 अक्तूबर 2024
शैलेंद्र कुमार शुक्ल
21 अक्तूबर 2024
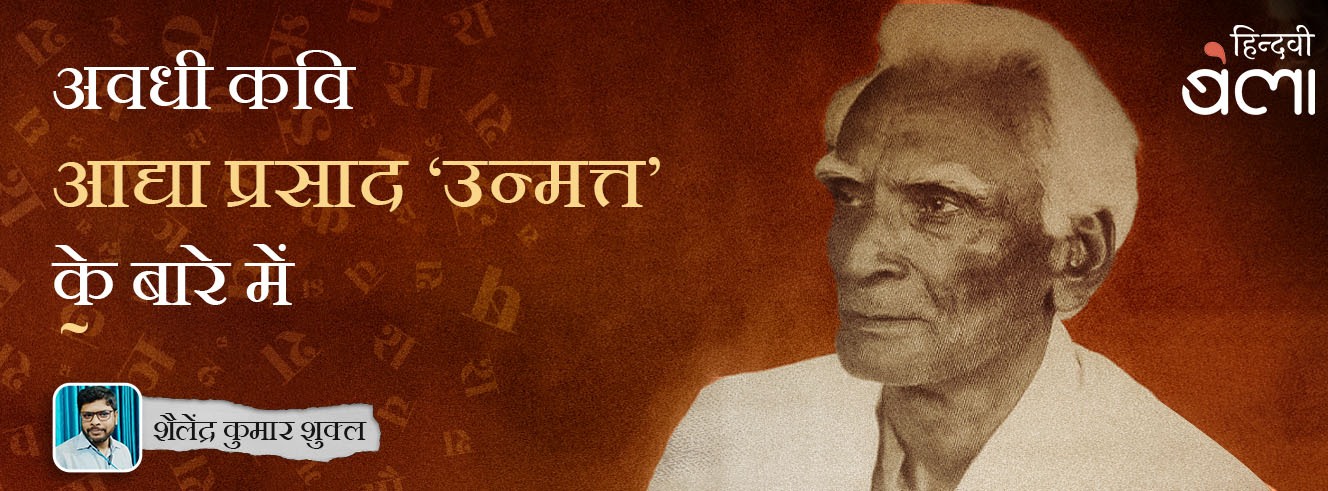
आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ अवधी में बलभद्र प्रसाद दीक्षित ‘पढ़ीस’ की नई लीक पर चलने वाले कवि हैं। वह वंशीधर शुक्ल, रमई काका, मृगेश, लक्ष्मण प्रसाद ‘मित्र’, माता प्रसाद ‘मितई’, विकल गोंडवी, बेकल उत्साही, जुमई ख़ाँ ‘आज़ाद’, विश्वनाथ पाठक, रफ़ीक़ शादानी इत्यादि कवियों की अवधी काव्य-परंपरा के महत्त्वपूर्ण कवि हैं। आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ का जन्म प्रतापगढ़ जनपद की तहसील सदर (वर्तमान में रानीगंज) में स्थित मल्हूपुर गाँव में 13 जुलाई 1935 ई. में हुआ। इनके पिता पंडित उमाशंकर मिश्र सीमांत किसान थे। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई-लिखाई गाँव में ही हुई, और उच्च शिक्षा में यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से विधि स्नातक थे। बाद में इन्होंने प्रतापगढ़ जनपद में काफ़ी समय तक वकालत की और कुछ वर्षों तक ‘युवा शक्ति’ नामक पत्र का संपादन देश की राजधानी दिल्ली से किया, जहाँ उन्हें त्रिलोचन का सानिध्य मिला।
आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ हिंदी और अवधी दोनों में कविताएँ लिखते थे, लेकिन उन्हें अवधी कविताओं से ही पहचान मिली। दरअस्ल उन्होंने अपना श्रेष्ठतम अपनी मातृभाषा में ही दिया। उनकी अवधी कविताओं की एकमात्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण किताब ‘माटी और महतारी’ प्रतापगढ़ की माटी के जुनूनी कवि केशव तिवारी के सद्प्रयासों से हमें मिल सकी—मैं तहे-दिल से उनका आभारी हूँ। उनका अन्य हिंदी और अवधी साहित्य सबका हुआ, यह राग छेड़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधुनिक अवधी ही नहीं हर मातृभाषा के लेखक का 80 से 90 प्रतिशत साहित्य ऐसे ही नष्ट हो चुका है या नष्ट होने के कगार पर है।
आज ऐसे साहित्य का हिंदी में कोई स्थान नहीं। इतिहास की एक शातिर-दर्दनाक घटना में हिंदी-उर्दू के संस्कारिक समर में उत्तर भारत की मातृभाषाओं को राजनीतिक बलिबेदी पर क़ुर्बान कर दिया गया और हिंदी इस तरह विजयी हुई। चंदबरदाई, गोरखनाथ, विद्यापति, ख़ुसरो, मुल्ला दाउद, कुतुबन, मंझन, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, रहीम और रसखान सब हिंदी के कवि हैं; इन्हें विश्वविद्यालयों के हिंदी-विभागों में पढ़ाया जाता है, इनके साहित्य पर हिंदी में शोध होते हैं, इनके साहित्य पर लिख-लिख कर हिंदी के प्रोफ़ेसर महान् आलोचक कहलाए, इनके साहित्य को संपादित करने वाले लोग हिंदी में मूर्धन्य विद्वान माने गए, प्रकाशक इनका साहित्य छाप-छाप कर मलामाल हो गए।
लेकिन यह सवाल आज हिंदी के नीतिनिर्धारकों से पूछना भी बर्दाश्त नहीं किया जाता कि जिस साहित्य पर हिंदी में आप स्वर्ण-युग का ढिंढोरा बजाते नहीं थकते, उसी साहित्य की भाषाओं का इतना घोर अपमान आप कैसे कर लेते हैं। दरअस्ल आपकी भाषिक बनावट ही ऐसी है। ‘आप किसी शर्त के मुहताज़ नहीं’।
अवध के किसान-मज़दूरों की तरह अवधी के कवियों के साथ भी न्याय नहीं हुआ। अवधी के अधिकतर श्रेष्ठ कवि सीमांत किसान या कामगार की जीवन समस्याओं के भुक्तभोगी रहे। उनकी रचनाओं में उनके जीवन की सघनता जिस रूप में गुथी हुई है, वह एक भोगे जा रहे यथार्थ में सौंदर्य और जिजीविषा को भी लोक स्वाभिमान की कसौटी पर कसते चलते हैं। लोक स्वाभिमान उनके स्वभाव का कवच है। वे इससे समझौता कभी नहीं करते। और यह आज के हिंदी-कवियों और मातृभाषाओं के कवियों के बीच महीन अंतर है।
ऐसा भी नहीं है कि मातृभाषा के कवियों में समझौतावादी या मौक़ापरस्त होते ही नहीं, ज़रूर होते हैं लेकिन उनके पास कविता नहीं होती। यह कोई जादुई बात नहीं है, इसका कारण सिर्फ़ भाषिक संरचना है। लोक और मानक में अब इतना तो फ़र्क़ होना ही चाहिए। हमारे समकाल के अद्भुत प्रतिभासंपन्न कवि-चिंतक अविनाश मिश्र अपने चर्चित उपन्यास 'वर्षावास' में लिखते हैं—“कैसे-कैसे दुष्कर्मों में लगे रहकर भी कुछ व्यक्ति कितनी-कितनी सुंदर कविताएँ लिख लेते हैं, यह बात अचरज में डालती है और बताती है कि कविता किसी शर्त की मुहताज नहीं” और यह सौ फ़ीसदी सही है कि आज हिंदी कविता जहाँ पहुँच चुकी है, वहाँ कवि होने और कविता करने की सचमुच कोई शर्त नहीं बची।
समय के साथ-साथ मूल्य बदले हैं और मूल्यों के साथ—कविता। सदैव बदलाव ही मूल्यवान नहीं होते, बदलावओं की प्रासंगिकता महत्त्वपूर्ण होती है, वही मायने रखती है। यहाँ यही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदी-कविता के रास्ते मातृभाषाओं की कविताओं का विकास नहीं हुआ है और ख़ासतौर पर मैं अवधी कवियों के बारे में यह कह सकता हूँ कि वहाँ दुष्कर्मी अपना लोक स्वाभिमान कितना भी प्रयास कर ले बचा नहीं पाएगा और लोक स्वाभिमान से विहीन व्यक्ति सच्ची लोक-कविता की नागरिकता कभी नहीं ले सकता। लोक में चतुराई के संसाधन कम हैं, तकनीकें कम हैं। जहाँ तन ढकने के लिए आज भी कपड़े का अभाव है, वहाँ सभ्यता पर नित-नए ओहार ओढ़ाना किसान-मज़दूर जीवन में संभव नहीं।
सच्चा लोक-जीवन आज भी जैसा दिखता है, वह वैसा ही हर जगह मिल जाएगा। इसका असर विचारधारा या युगदर्शन के बारे हम देख सकते हैं। कहीं-कहीं काइयाँपन यहाँ भी मिल जाता है, लेकिन वह ढके होने पर भी फटे पर्दे से साफ़-साफ़ झलकता रहता है। रेणु के ‘मैला आँचल’ में डॉक्टर प्रशांत का एक कथन यहाँ याद आता है—“गाँव के लोग बड़े सीधे दिखते हैं; सीधे का अर्थ यदि अपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसरिक बुद्धि का सवाल है, वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में पाँच बार ठग लेंगे। और तारीफ़ यह है तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी।”
यह है लोक जीवन की सच्चाई जो इनके भावों के अनुरूप भाषा की संरचना में शामिल है। लोक-कवियों के साथ यह समस्या सदैव रहेगी कि लोक-जीवन में दुष्कर्मी कभी भी अच्छी कविता नहीं रच पाएगा। वह किसी और भाषा में जहाँ अपने अवगुण छिपा सके काव्यगुणयुक्त कविता भले लिख ले। जहाँ चोर को अपनी चतुराई पर गुमान है, डाकू को अपने कारनामों पर अहंकार है, मुनीम को अपनी चंटग़ुलामी पर ग़ुरूर है, पुरोहित को अपनी पोंगापंथी पर अभिमान है; इस तरह सब खुले हुए हैं लगभग। तो ऐसे समाज में कवि कुछ और होकर कुछ और दिखाने की कोशिश करे तो यह आसपास वाला समाज उसे बनार बना कर छोड़ेगा। इसीलिए लोक-कवि का जीवन और रचना बहुत अलग-अलग नहीं हो सकती। शायद इसलिए भी मातृभाषाओं के रचनाकारों के साथ न्याय नहीं हो सका, क्योंकि अकादमिक अदालतों में हिंदी के न्यायाधीश अपने अवगुण बहुत सुथरे आवरणों में ढके न्याय-दंड ठोकने में व्यस्त हैं।
इन वर्चस्वशाली डंडाधीशों की भाषिक राजनीति और छल-छद्मी साहित्यिक ठेकेदारी को मातृभाषाओं के सजग कवि ख़ूब समझते हैं। उनमें ठगे जाने की कसक कविता की भाषिक संरचना में भी अवचेतन स्वरूप विकल नाद के रूप में यत्र-तत्र गूँजती हुई दिखाई दे जाती है। आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ की सीमित लोकप्रिय ग़ज़ल अपने अवधी समाज की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को किस सघनता से कहती है, जिसमें एक भाषा का और उसके साहित्य के अपमान की पीड़ा को कोई भी सजग पाठक महसूस कर सकता है—
पोल खोली, कुछ न बोली डोलि जाई का करी!
ओनकी जफड़ी से कसत इज्जत बचाई का करी!
बूँद भै जानै न हमरी जात कै औकात जे
वही समुंदर की लहर कै गीत गाई का करी!
जिस भाषा ने ढोंगियों, मावलियों, लुटेरों, हत्यारों, बलात्कारियों और जघन्य अहंकारियों के लिए कविता के दरवाज़े खोल दिए हों; उस भाषा के साहित्यिक वर्चस्ववादी शिकारियों के जाल से ‘उन्मत्त’ सरीखे अवधी के कवि अपनी इज़्ज़त कैसे बचाएँ, यह हमारे समय की विकट चुनौती है। कवि कहता है—क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता कि इनकी पोल खोलूँ या चुप्पी साध लूँ या किसी दूसरे निकल जाऊँ! जो जायसी से लेकर पढ़ीस तक खाँड़े की धार पर चलने वाली हमारी बिरादरी की बूँद भर औकात नहीं जानते उस महासमुद्र की पुनीत लहरों के गीत इन्हें सुनाऊँ! और ये सुनेंगे!
अपराधियों की भी भाषा होती है, उनका साहित्य नहीं होता था। लेकिन जब कोई भाषा अपराधियों को कविता रचने की आज्ञा दे तो उसका भविष्य अंधकार की ओर प्रस्थान कर चुका होता है। वह अपनी अस्मिता खो देती है। कविता किसी भी भाषा की सर्वोत्तम विश्वसनीयता है। परिचय से प्रेम के दरवाज़े खुल सकते हैं और प्रेम विश्वासों की स्याही से अपने समय के सत्य और न्याय के साफ़ों पर कविता बन कर भाषा में उतरता है।
परिचय और प्रेम पर बात होते ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ‘लोभ और प्रीति’ निबंध की यह पंक्तियाँ याद आनी लाज़मी है—“इस लोभ के लक्षणों से शून्य देश-प्रेम कोरी बकवास या फ़ैशन के लिए गढ़ा हुआ शब्द है। यदि किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने देश के मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, गुल्म, पेड़, पत्ते, वन, पर्वत, नदी, निर्झर सबसे प्रेम होगा, सबको वह चाह भरी दृष्टि से देखेगा, सबकी सुध करके वह विदेश में आँसू बहाएगा। जो यह भी नहीं जानते कि कोयल किस चिड़िया का नाम है, जो यह भी नहीं सुनते कि चातक कहाँ चिल्लाता है, जो आँख भर यह भी नहीं देखते आम प्रणय-सौरभपूर्ण मंजरियों से कैसे लदे हुए हैं, जो यह भी नहीं झाँकते कि किसानों के झोपड़े के भीतर क्या हो रहा है, वे यदि दस बने-ठने मित्रों के बीच प्रत्येक भारतवासी की औसत आमदनी का परता बताकर देश-प्रेम का दावा करें तो उनसे पूछना चाहिए कि ‘भाइयों! बिना परिचय का यह प्रेम कैसा?”
यहाँ मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि देशप्रेम में भाषा की क्या भूमिका होती है? क्या जिन भाषाओं से पहले हवा, पानी और भोजन लेकर एक महान् भाषा बनी, उस भाषा के सुभट अब उन्हीं भाषाओं का ख़ून चूसकर गला दबाते हुए देश का कौन-सा हित कर रहे हैं?
“सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार”
क्या इस केंद्रीकरण से जनपदीयता का शोषण नहीं हो रहा? आज जनपदीयताएँ मरती जा रही हैं। उन्हें मारा जा रहा है। उनकी भाषाएँ अपमान का विष पीकर आत्महत्याएँ कर रही हैं। उनके कवि ख़त्म हो रहे हैं। उनके साहित्य का इस हिंदी-केंद्रीकृत समय में कोई प्रकाशक नहीं मिल रहा। वे जायसी, तुलसी, रहीम के वारिस अपनी विरासत पर ढोंगियों और अपराधियों द्वारा बेदख़ल कर दिए गए हैं। क्या आज हिंदी एक भाषा, एक नेता, एक देश की विषैली बयार में शिकार नहीं कर रही है?
आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ अपनी जनपदीयता का दुख कहते हैं, यह आज हर जनपदीयता की मातृभाषा और उसके अपमानित साहित्य का दर्द है—
फूस की मड़ई मा बनि बारूद हम पैदा भये
आगि देखी तौ भभकि के बरि न जाई का करी!
छाँव की खातिर पसीना ख़ून से सींचा किहे
झोंझ से माटा झरैं तौ मुह नोचाई का करी!
पूत जो पूछै बमकि के बाप से तू का किह्या
ऊ बेचारा हाथ मलि के रहि न जाई का करी!
हिंदी के विद्वान टाइप लोगों से कभी-कभी कोई पूछ ही लेता है कि साहब अवधी का आधुनिक साहित्य कहाँ हैं? तो वे बड़ा ग़ज़ब का उत्तर देते पाए जाते हैं कि जिस भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जैसा महाकवि पैदा हो गया जिससे कुछ बचा ही नहीं, जिससे कुछ छूटा ही नहीं। तुलसी के बाद अवधी में कोई बड़ा कवि इस स्तर का हुआ ही नहीं कि उसकी नोटिस ली जाए। यह उत्तर तुलसीदास भी यदि सुनते तो यही कहते—“सिर धुनि गिरा लगत पहिचाना”
तब तो यह भी पूछा ही जा सकता है कि जब अवधी में जायसी जैसा बड़ा कवि हो चुका था तो तुलसी जैसे बड़े कवि क्या ज़रूरत थी। अवधी का भट्ठा यही बैठ जाना चाहिए था। मतलब अवधी में और बड़े कवि होने की गुंजाइश सदैव बनी रही है और बनी रहेगी। हिंदी में तुलसी के बाद ताला लग गया, अब उनको अवधी के बड़े कवि की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसे में हिंदी, अवधी से पूछे कि तुमने आधुनिक युग में क्या किया तो अवधी हाथ मलकर न रह जाए तो क्या करे! साजिशें कितनी शातिर हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं हैं।
आज जब हिंदी की आज़ाद नैया में अवधी के खेवैयों को याद करता हूँ, तो अपभ्रंश का एक दोहा याद आता है—
भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि महारा कंतु।
लज्जेजं तु वयंसिअहु जइ भग्गा घरु एंतु।।
हज़ार बरस पुरानी ग्राम्य-गिरा में ग्रामीणा कहती है—भला हुआ प्रिय अपने देश और ईमान के लिए युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, यदि युद्ध क्षेत्र से वह पीठ दिखाकर भाग आता तो मैं अपनी समवयस्कों के बीच अपमानित होती। यह है भाषा का ईमान। क़ुर्बानी के ऐसे ही महान् मनोभावों से बनता है—किसी भाषा का चरित्र, उसका स्वभाव। यह ग्राम्यता है और इसी को हम जनपदीयता कहते हैं। यह है देसप्रेम जिसके पुरषार्थ से संभव होता है देश। जो देसप्रेमी नहीं उसका देशप्रेम सिर्फ़ छलवा है, ढोंग हैं, गद्दारी है।
देशप्रेम के बारे में आचार्य शुक्ल के उपरोक्त उद्धरण के आलोक में अवधी कवि ‘उन्मत्त’ की एक कविता ‘पाती’ ज़रूर देखनी चाहिए जिसमें अवध के एक गाँव की किसान स्त्री अपने पति को चिट्ठी लिख रही है जो देश के लिए सीमा पर छिड़े युद्ध में शामिल है। स्त्री चिट्ठी में जो लिखती है, उसका समाजशास्त्रीय अध्ययन यदि करेंगे तो हमें देशप्रेम की असल समाजिकता और भाषिक वर्गीयता बहुत गझिन रूप में दिखाई देगी। वह जिस वातावरण को चिट्ठी में दर्ज कर रही है वह पहली काव्य-अनुभूति है, जिसे कवि दूसरी अनुभूति के तौर पर कविता में दर्ज करता है। कविता में जो चीज़ें आती हैं, वे ही देशप्रेम के असली लोक तत्व हैं—
गइया नधाय गइ जगतू कै, बड़कई भैंसि तेलियानि अहै
बछिया मरि गइ खुरपका रहा, ओसर भुवरई बियान अहै
कइसे पठई नाहीं तौ नैनू से दुइ मेटी अबकी भरी अहैं
तू कहे रह्या तोहरी खातिर राबिउ एक गगरी धरी अहै
घिउ दूध खूब उतरान अहै, तोहरिन इयादि कै रोई थै
गंजी से दुपहरिया काटी एक जूनी रोटी पोई थै
अपने सेनानी पति को किसान नायिका चिट्ठी में लिख रही है कि गाय नधा गई है, भैंस तेलिया गई है, बछिया खुरपका रोग से मर गई, भूरी ओसर (पहिला भैंस) ने बच्चा दिया है, दूध-घी घर में ख़ूब हो रहा है, तुम्हें तो नैनू (मक्खन) बहुत प्रिय है—लेकिन जब नैनू से दो-दो मेटी (मृदभांड) भरी हुई हैं, तब तुम घर नहीं हो! छुट्टी में गाँव आने पर राब (गीली गुड़) खाने की तुम्हारी इच्छा थी, तो एक गगरी वह भी रखी हुई है। और सुनो! अभी दस दिन पहले रमबरना के कुत्ते ने अइया (दादी) को काट लिया तिस पर ओरहन देने जब मैं गई तो उसकी माँ उलटे मुझे ही डाँटने लगी। ऊसर खेत के मेड़ पर अभी परसों ही छोटकवा लरिका गिर पड़ा, जिससे उसके कापर में कंकड़ गड़ गया है। मकड़ी के जाले से इलाज तो किया लेकिन चोट का दाग़ पड़ ही गया। पिछले मंगल को तो रतन और सुम्मारी दोनों बुज़ुर्ग स्वर्ग सिधार गए। ठीक ही रहा बुढ़ौती का दर्द बहुत पीड़ा देता है। जिस बूढ़े की बूढ़ी न हो, उसका तो बुढ़ापा नर्क़ ही होता है, खटिया पर पड़े-पड़े ख़ाँसने-कराहने से बचे और घर वालों को भी खुरदुरु के झंझट से मुक्ति मिली। जानते हो घर के पिछवारे नाबदान के किनारे जो पपीता का पौधा था, आजकल ख़ूब फला है और घूरे पर वाले कोहड़ा की बेल ख़ूब फल-फूल रही है। इसकी लताओं पर फूले हुए इन पीले फूलों को देखकर मेरा कलेजा जलने लगता है।
कविता की कुछ पंक्तियों का यह सारांश इसलिए यहाँ रख रहा हूँ कि कविता में देशप्रेम की बकैती करने वाले यह जाने की देशप्रेम के तत्त्व कौन से हैं। सच्चा देशप्रेम क्या होता है। देश को आज़ाद कराने की असली लड़ाई किसने लड़ी है। आज़ादी के मूल्य क्या होते हैं। आज़ादी के विरुद्ध ग़ुलामी की कलावादी चाटुकारिता, भोंड़ी नंगई और दंगापरस्त सांप्रदायिकता देशभक्ति पर बोलने का कोई अधिकार नहीं रखती, यह कविता हमें बताती है।
कविता में जिस किसान, स्त्री का चरित्र देशप्रेम की सच्चाई बनकर उभरता है, उसे मैं भारत-बहन ही कह सकता हूँ क्योंकि भारतमाता की शब्द गरिमा आज सांप्रदायिक उन्मादियों ने बर्बाद कर दी है। वे भारत की इस बहन के बलिदान को रत्तीभर भी नहीं जानते। चिट्ठी में ग्रामीणा लिखती है कि अभी एक दिन अइया बाज़ार गई थी—उन्होंने बताया कि देल्हुपुर की हाट में एक बड़ी भारी सभा जुटी थी, जहाँ लोग देश की आज़ादी को बचाने के लिए चंदा इकठ्ठा कर रहे थे। इस तथ्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह चीन-भारत युद्ध के समय का वर्णन है। सभा में युवाओं से ख़ून माँगा जा रहा था, माताओं-बहनों से गहने चंदे में माँगे जा रहे थे।
आइया ने बताया कि वहाँ क्रांतिकारियों के ओजस्वी भाषण हुए, जिनमें यह बताया गया देश की आज़ादी ख़तरे में हैं, देश कि छाती दुश्मन रौंद रहा है, यह सुन कर उनका भी ख़ून गर्म हो गया। उन्हें भी जोश चढ़ गया। उन्होंने भी ज़ोरदार आवाज़ में कुछ शब्द कहे। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि छोटका तो डर ही गया। आगे वह नायिका चिट्ठी में जो लिखती है, उस बलिदान की क़ीमत है यह आज़ादी इसे कभी नहीं भूलना चाहिए—
हमरी आँखी कै माछु आजु तोहका लरिकन कै कसम अहै
अपनी माई के दूध अउर अपने पुरिखन कै कसम अहै
आगे जो गोड़ बढ़ाया तौ पीछे जिन आपन आँख किह्या
हम रांड होब तौ होइ दिह्या एकर कौनौ जिन माख किह्या
हम तोहरइ नउना रटत रटत तोहरे लरिकन का सेइ लेब
कौनौ सूरत बूड़त बाड़त हम आपन नइया खेइ लेब
मुल जौने दिन ताना पउबै हम कुआँ इनरा थाहि लेब
तोहरे नउना कइ गारी सुनि हम गड़ही तारा थाहि लेब
यह है देश के लिए देस का बलिदान। ऐसे ही तमाम देसों के अनवरत बलिदानों से देश बना है, जिसे राष्ट्र कहा गया। आज इसी राष्ट्रीयता के साथ छल हो रहा है, पाखंड हो रहे हैं। जनपदीयताओं को अपमानित कर राष्ट्र का सम्मान बढ़ाया जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। यह बात हमें कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि मातृभाषाओं को अपमानित कर हम हिंदी का सम्मान कभी नहीं बढ़ा पाएँगे।
जनपदीयता ही वह अन्नपूर्णा है, जिससे हिंदी का आज भी पोषण होता है। यह तथ्य उतना ही सत्य है, जितना यह कि किसान-मज़दूरों की मेहनत और बलिदान पर धरती का हर वर्ग ज़िंदा है—
ई अन्नपुरना कै मंदिर सबके दाता कै धाम यहे
केतनौ केउ चढ़े आकसे पर मुल आवै सबके काम इहै
परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ने में हमारी जनपदीय ताक़तों का जो योगदान था, उसे राष्ट्रीयता के छद्म रंगरूटों ने जघन्य साज़िशों के तहत भुला दिया और सांप्रदायिकता का चरस बो कर स्वतंत्रता के मूल्यों को लगातार बर्बाद किया गया। देश में आज़ादी के बाद धर्म और जाति की कट्टरताओं को इस तरह हवा दी गई कि वर्ग-संघर्ष की लड़ाई पीछे छूट गई। पूँजी और सामंतवाद के गठजोड़ ने सांस्कृतिकरण के तहत संकुचित केंद्रीयता को इतनी ताक़त दी कि विकेंद्रीकृत समाजिकता का प्रबल राजनीतिक ह्रास होता चला गया।
जनपदीयताएँ इस क़दर शोषण का शिकार हुईं कि मोटाई हुई केंद्रीयता का बोझ असह हो उठा। इनकी आहात चित्कारें जनपदीय भाषाओं के साहित्य में दर्ज हुईं, जिसे स्वतंत्र भारत में उपेक्षा के प्रतिबंधों से मार दिया गया। उनके आर्त नाद आज भी सिसकते हुए अपनी कहानी कहते हैं—
नेता अफसर मुल्ला पंडित तब्बौ बंटाधार हियाँ
चरैं देस सब चरतै बाटेन के बाटै रखवार हियाँ
आपन चरैं पूत हित जोगवैं नातिउ खातिर धरे रहैं
सेंध काटि जिन आल्हा गावैं एत्ती किरपा करे रहैं
देश के विकास पर लंबी-लंबी फेंकने वाले नेता हैं, ईमानदारी के दारोमदार का ढिंढोरा पीटने वाले अफ़सर हैं, क़ौम के इंसानियत का भोंपू बजाने वाले मुल्ला हैं, सद्कर्मों पर ज्ञान बघारने वाले पंडित हैं, फिर भी यहाँ ग़रीबी, जहालत, भ्रष्टाचार, लूट, असमानता, कट्टरता, हत्या, बलात्कार चहुँ ओर फैले हुए हैं। दरअस्ल आज़ादी के बाद विदेशियों से बढ़कर इन्होंने इस देश के साथ अन्याय किया है। वर्चस्वशाली नाम और काम के बीच दरिंदे ज़िंदा विलोम हैं। इनके लिए जनपदीयताएँ नर्म चारे से भरे खुले चरागाह हैं, जहाँ सब चरने वाले देश के उत्थानवादी साँड हैं, जिन्हें देश की रखवाली का ठेका मिला है। ये इस देश के किसान-मज़दूरों की गाढ़ी कमाई ख़ूब लूटते हैं और इतना लूटते हैं कि अपने बेटों के लिए ही नहीं अपने नाती-पोतों के लिए भी लूट कर रख जाते हैं।
किसान कवि ‘उन्मत्त’ कहते हैं अरे! चोट्टे हरामखोरों तुमको जो करना है, करो लेकिन विकास, ईमानदारी, इंसानियत और सद्कर्मों का आल्हा कृपा करके मत गाइये, यह बर्दाश्त नहीं होता!
विसंगति और विडंबना का अखाड़ा बना हमारा सांस्कृतिकबोध जनपदीय विश्वसनीयता को चकमा देकर आवारा पूँजी की हमदर्द सत्ताओं के सामंती अभिरुचि वाले चरित्र को पहचान नहीं पा रहा है। हमें कहाँ ख़ुश होना है और कहाँ दुखी होना चाहिए, सामान्य हित-अनहित के मनोभावों को ही भ्रमित कर दिया गया है। आज देश की संपूर्ण जनपदीयताएँ अपने हितों के ख़िलाफ़ अनहित का समर्थन कर रही हैं, मतदान कर रही हैं। राष्ट्रीयता के नाम पर आज ऐसा चरस समाजिकता ने पी लिया है कि अन्याय ही धर्म बनता जा रहा है और धर्म असलियत का चिर शत्रु। सारे प्रतीक अपने चिह्नित स्थानों से हट कर वर्चस्वशाली लंपटों के इशारों पर करतब दिखा रहे हैं। ‘उन्मत्त’ इसे अपनी कविता में स्पष्ट करते हैं—
तेले क धार उप्पर बाती क फोंक नीचे
ई दाम कै दुसासन लछमिउ क चीर खींचे
अँधरन क राज बाटइ एनका अँजोर कइसन
अंधेर की नगरी मा के साह चोर कइसन
हरिचन्द भये झुट्ठा औ चोर भे मुरारी।
अब कइसे दिया बारी॥
ऐसे विकट समय में भी अपमान और शोषण की दाहकता से तपी हुई प्रतिभाएँ जनपदीयता की ताक़त बन कर उभरती रही हैं। अवध की माटी में ऐसे विद्रोही रूख सदा से उगते आएँ। और अवधी की सबसे बड़ी ताक़त तो यह मान ही लेनी चाहिए कि जिसने आज के सामंती-पूँजीवादी गठजोड़ के सम्मुख घुटने टेक बाज़ारू बनने से इंकार कर दिया। ‘उन्मत्त’ अपनी माटी की तासीर बताते हैं—
साँच होय तौ आँच न आवै झूठ होय भुँइ लोटी
हियाँ तोप कै मोहड़ा फेरे लाठी अउर लँगोटी
यह बात कविता में सहज तौर पर गांधी के लिए कही गई है, लेकिन यह क़तई नहीं भूलना चाहिए कि गांधी ने लाठी और लँगोटी किसान-मज़दूरों के सम्मान में जनपदीय पक्षधरता को मजबूत करने के लिए अपनाई थी। गांधी इस जाति के स्वाभिमान पर मुग्ध थे। सबूत के तौर पर गांधी के भाषण जो उनके दस्तावेज़ों में मौजूद हैं, काशी नागरी प्रचारणी सभा में, 5 फ़रवरी 1916 और भागलपुर में, 17 अक्तूबर 1917 देखे जा सकते हैं। गांधी अवधी की ताक़त समझते थे। उन्होंने इस भाषा के बारे में बहुत बड़ी बातें कही हैं, कभी इस पर विस्तार से लिखूँगा।
इस भाषा में एक ग़ज़ब का स्वाभिमान है कि इसके कवि यदि इस शर्त पर खरे नहीं उतरते तो वे कविता के नाम पर लंतरानी भले करते रहें कोई कविता कभी नहीं लिख पाएँगे। इस भाषा की एक ख़ासियत तो यह भी कही जा सकती कि कवि गुण भले हेरा जाएँ, लेकिन अवगुण चीख-चीख कर सब कह देते हैं। यही कारण है कि तुलसी जैसे कवि को स्वाभिमान मरने नहीं देता और दोष उन्हें जीने नहीं देते। इस भाषा के इस कवि ने प्रासंगिकता का जो अमर वरदान हासिल किया, विश्व-साहित्य में भले ही किसी को मिला हो। इस भाषा में आज भी आधुनिक युग के सैकड़ों कवि ऐसे हैं जिनका मूल्यांकन नहीं हुआ। जिनके बारे में मैं पूरे होशोहवास में कह सकता हूँ कि वे अपने समय के हिंदी लेखकों से बहुत बड़े हैं। व्यक्ति के रूप में भी और रचनात्मकता के रूप में भी। वे अपने समय का इंतिज़ार कर रहे हैं कि उनका भी कभी मूल्यांकन होगा—
सूरज कै रथ रोंकि सका के सका है अकास क बादर बाँधी
धार समुंदर कै न रुकी ललकारे हैं राम सरासन साधी
आह गरीब क जो निकसी तब टूटी है काल कराल समाधी
के जग मा जेकरे बल पौरुख रोके रुकी बदलाव कै आँधी
‘उन्मत्त’ को भरोसा है एक-न-एक दिन ग़रीब जनता की सहनशीलता का बाँध ज़रूर टूट जाएगा, बदलाव प्रकृति का शाश्वत नियम है। जब सूरज का रथ कोई नहीं रोक सका, आकाश में बादल को कोई नहीं बाँध पाया, राम के शस्त्र संधान कर ललकारने पर भी समुद्र की लहरें नहीं रुकी, तो क्या ग़रीब का शोषण और अपमान सदैव एक ही करवट रहेगा!
कभी-न-कभी सहनशीलता का बाँध ज़रूर टूटेगा क्योकि ग़रीब की चित्कार से कठोर काल की विकराल समाधि भी टूट जाती है। इस संसार में किसी में ऐसा बल और पौरुष नहीं पैदा हुआ कि वह बदलाव की आँधी को रोक सके!
समाजिकता का पुनर्मूल्यांकन करने वाले नायक जिस दिन अपनी सच्ची विरासत पहचान लेंगे, बदलाव की दिशा सुनिश्चित हो जाएगी। आज हम छोटी-छोटी संकुचित इकाइयों में बँटे हुए हैं। हमारी जनपदीय विरासत की असली ताक़त को गुमराह कर सैकड़ों मोर्चों पर उलझा दिया गया है। बिना एकजुटता कभी बड़े बदलाव नहीं हो सकते। वे तभी तक कामयाब हैं, जब तक हम बिखरे हुए हैं।
सच्चे कवियों का काम हमें एकजुट करना है और विरोधी षड्यंत्रों को बेनक़ाब करना है। ‘उन्मत्त’ अपनी परंपरा के कवियों कबीर, तुलसी, रहीम, पढ़ीस, वंशीधर, जुमई ख़ाँ की तरह अपने समय की विखंडकारी ताक़तों की पहचान अपने लोगों को बताते हैं। वह सांप्रदायिक अश्लीलता को इस तरह बेनक़ाब करते हैं—
मुल्ला पंडित गुरू पादरी एक से एक बड़े
घर गरीब कै बरै धधकि के तापैं खड़े खड़े
आगि लगावैं सगर दौड़ि फिर दौड़ैं लै लै पानी
एनकी तिकड़म भरी चाल मा जूझैं अज्ञानी
मजहब के आँधर कोल्हू मा सुधुआ पेरा बा
समझि बुझी के चला सँघाती पाख अँधेरा बा
आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ एक तरफ़ सांप्रदायिक साज़िशों को बेनक़ाब करते हैं तो दूसरी तरफ़ जनपदीय जन को वर्ग-संघर्ष की असली स्थिति से अपने अंदाज में रूबरू कराते हैं। धर्म और जाति में उलझी हमारी समाजिकता अपने असली संघर्ष से बेख़बर है। ‘उन्मत्त’ यह ख़ूब समझते हैं कि हमारी जनपदीयता धर्म और जाति में जितनी उलझती जाएगी आवारा पूँजी का उत्तर साम्राज्यवाद हमें लूट-लूट कर ग़ुलाम बनाता जाएगा। हमारे स्वतंत्रता के मूल्य बाज़ार की आँधी में हेरा जाएँगे। अभी हम अपने दुख-सुख एक-दूसरे से आपस में बाँट लेते हैं। आने वाला वक़्त हमसे यह भी छीन लेगा। वर्ग-संघर्ष का चित्र उनकी कविता में देखिए—
दिल्ली की बड़की कोठी से झुग्गी बोली रोय
तू खजूर हम भुइँका तिनका केहि विधि मिलना होय
हाथे फरुहा मुड़े पलरी सपन भये सब चूर
दिल्ली कै किल्ली हाथे मा तब्बौ दिल्ली दूर।
पीर पराई का जानइ ना जेकरे फाटि बेवाय
अब का होई भाय गोबरधन अब का होई भाय।
जाति और धर्म की कट्टरता की आड़ में पूँजीवादी नव-उदारता हमारा हर मोर्चे पर दोहन करने में कामयाब रही, यह नव-साम्राज्यवाद की कटु सच्चाई है। पूँजीवाद के जो सहयोगी बने उन्हें सभी क्षेत्रों में दलाली करने पर सम्मान और रोज़गार मिले और जो इसका अंध समर्थन न कर सके उन्हें उपेक्षाओं के शांत हथियारों से श्रेणीबद्ध कर निपटाया गया।
जनपदीयताओं ने असफल असहयोग किया, वे टूटती गईं लेकिन झुक नहीं पाईं। अवधी का स्वभाव उत्तर भारत की जनपदीयताओं में सबसे प्रखर रहा है। इसके सांस्कृतिक कारण भी हैं। इसी अवधी जनपदीयता के सशक्त कवि हैं आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’। उनमें एक अवधी-जन का स्वाभिमान परंपरागत कूट-कूट कर भरा है। उनकी रचना और उनका रचनाकार तराजू के समानतर बराबरी के पलड़े हैं। पसंघे की एक रत्ती भर गुंजाइश नहीं। उन्होंने ‘माटी औ महतारी’ किताब का समर्पण बहुत भारी मन से इस टीस के साथ किया है कि “अपने पिता स्व. पंडित उमाशंकर मिश्र के बरे, जेका अउर कुछ न दै पाये।”
इस कृति की कविताओं को समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो बात साफ़ हो जाती है। उनकी गर्वीली ग़रीबी और अपमानित स्वाभिमान के बारे में यदि जानना हो तो किताब की भूमिका पढ़ सकते हैं।
इसी भूमिका में वह कहते हैं—“सब हमारि मददौ हमेसा करइ चाहत रहे, औ चाहा थीं मुला हमरे केहू से कुछु मागै क सहूर नाहीं अहै, ओ काउ करैं। बिना मांगे तौ केउक कुछ मिलत नाहीं औ जो कबौ मागै क मन होथै हमरे अगवा रहीमदास खड़ा होइ जाथीं। जे हमका मदद करै क कभौ गोष्ठी सम्मेलन औ सभा म उवादा करा थीं हम ओनकै दुआरै छोड़ि देई थै। सोचित थै दुआरे जाब तौ सोचिहैं कि उवादा कै दिहे रहें उहै मांगै आइ अहैं।”
यही है अवधी स्वभाव का स्वाभिमान जिसे आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ अपनी जनपदीय भाषा परंपरा के महान् कवि को याद करते हुए बचाने के लिए हर क़ीमत चुकाने की ताक़त रखते हैं। वह जीवन में तमाम उतार-चढ़ाओं के थपेड़े खाकर भी भाषा के स्वाभिमानी ईमान से नहीं डिगते और जिन्होंने भाषा के ईमान को बेचकर स्वाभिमान को बाज़ार में बेच दिया वे अपने समय में तो धन, पद और सम्मान से भले लदे-फदे रहे हों आज उनके पास न कोई कविता है ना वह देह जो धन, पद और झूठे सम्मनों से बेईमान हुई थी।
आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ की कविताएँ पढ़कर लोक मन अपने हृदय से उनका सदैव सम्मान करता रहेगा। वह अवधी के सच्चे सपूत थे। उन्होंने स्वयं लिखा है कि उन्हें निराला, महादेवी वर्मा, दिनकर, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि कवियों का स्नेह और आशीष मिलता रहा है।
इस किताब में उन्होंने कई लोगों को अपनी ओर से धन्यवाद ज्ञापित किया है। लेकिन सबसे रोचक और ज़ोरदार धन्यवाद उन्होंने अवधी के व्यापारी जगदीश पीयूष को दिया है। ‘माटी औ महतारी’ किताब छापने का बड़ा भारी श्रेय उन्हें ही जाता है, क्योंकि उन्होंने वह सब किया जो आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ नहीं कर पाये, उनके आगे रहीम आ जाते थे, लेकिन पीयूष के आगे रहीम नहीं आए कभी। यही कारण था कि आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ के पास कविता थी और कुछ नहीं और पीयूष के पास कविता नहीं थी और सब कुछ।
ख़ैर धन्यवाद ज्ञापन देखिए—“वै बड़े कर्मठ औ जुझारू मनई अहैं। हमार उनकै साथ पिछले 35 बरस से अहै। ओनकै ललकार औ फटकार आखिर हमका इ किताब छपावै बरे तैयार कइ दिहिस। वैसे वै अहिन हमार छोट भाय मुला गुरू गुरै रहिगा चेला सक्कर होइ गवा। अब तौ ओनही हमका रस्ता देखावा थीं।’ आगे गुरु वाले प्रकरण पर एक जगह उन्होंने और लिखा है कि ‘ओनकै नाव न खोलब मुला गुरु की तुमड़ी म मूतइ वाले चेलन क नाहीं भूलि सकित, ओनकै बन्दना करी थै। आखिर तुलसीदासौ केहे रहेन ‘जे बिनु काज दाहिने बाएँ।”
यह है जनपदीयता का दुख। अवधी का इतना स्वाभिमानी और प्रखर कवि आख़िर करे तो क्या करे। “ओनकी जफड़ी से कसत इज्जत बचाई का करी”।
आज आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ को गए 18 साल बीत रहे हैं, लेकिन अवधी के इस कवि का आज तक कोई मूल्यांकन नहीं हुआ। जब अवधी का ही दरवाज़ा बंद है तो इस भाषा के कवि को कौन पूछे। वर्चस्व की ताक़तें कैसे काम करती हैं, यह माया अच्छे-अच्छे विद्वान् नहीं जानते, और जो जानते भी हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनके भी दुख हैं। जिस भाषा ने उन्हें पद और प्रतिष्ठा दी, उस भाषा की साम्राज्यवादी नीति की रक्षा करना वे अपना धर्म समझते हैं। साहित्य के बड़े-बड़े प्रगतिशील भाषा के मामले में कट्टर साम्राज्यवादी हैं और यह सब हिंदी में ही संभव है।
अविनाश मिश्र की बात यहाँ भी अपनी प्रासंगिता स्पष्ट करती है और यह भी हमारे समाज की सच्चाई है कि अपने स्वाभाविक मूल्यों के ख़िलाफ़ हर जगह दलाल होते आए हैं। तो ऐसे दलाल अवधी में भी ख़ूब भरे पड़े हैं और वे ही ख़ुद हो अवधी का सबसे बड़ा उद्धारक सिद्ध कर सत्ता की चाकरी में भाषा का चीर-हरण करते रहते हैं। उनसे बचना बहुत कठिन है। क्योंकि उनके पास वह सब कुछ है जो एक भाषा के सधे हुए बेईमान के पास होना चाहिए— जैसे संस्थान, एकेडमी, पुरस्कार, प्रकाशक, संपादक, गोष्ठियाँ और सेमिनार। इन ताक़तों के आगे स्वाभिमानी जनपदीय साहित्यिक अंततः टूट जाता है।
आद्या प्रसाद ‘उन्मत्त’ भी इनकी ताक़त के सामने आख़िर क्या ही कर सकते थे, सिवाय इस उम्मीद के कि कभी-न-कभी तो बदलाव ज़रूर होगा—
ई दिन बरिस बरिस का घूरेउ क दिन फिरा बा
हमरेउ करम क कबहूँ कौनौ हिसाब होई
ई तेल दिया बाती सब केकरी मसक्कत से
जब ई केहू न समझी तौ इनकलाब होई।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
