तेरह दिन की एक आत्मकथा
 प्रिया वर्मा
29 मार्च 2025
प्रिया वर्मा
29 मार्च 2025
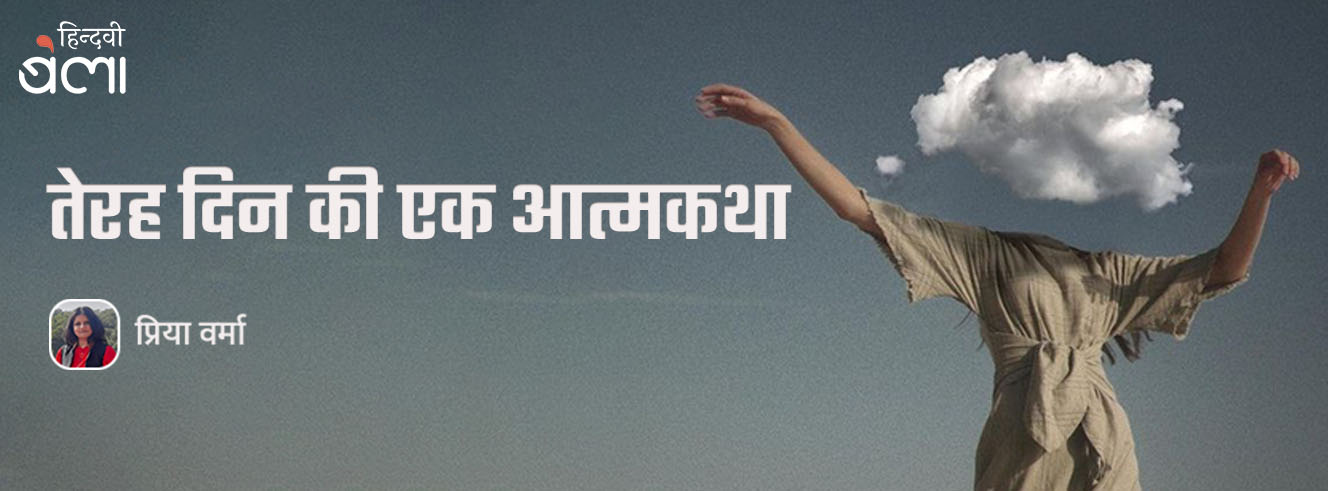
रहना यहीं था—इसी समाज में, घर के भीतर, घर के बाहर।
घर भीतर ढूँढ़ते हुए अब, सब इधर-उधर था। कोई याद अपनी जगह पर नहीं मिल रही है इस जगह। अभी तो रहना है, यह सोचकर यादों को तरतीब देने का मन बना लिया।
बड़े दिन बाद, इस बार वहाँ क़रीब तेरह दिन रही। शायद सवा-पौना दिन बढ़ाकर या घटाकर कुछ कम-कुछ ज़्यादा ही रही वहाँ—उस घर में।
याद में खोई हुई चीज़ें, कभी कैलेंडर के ढेर में मिलतीं तो कभी डायरियों में और कभी दिनों के हिसाब-किताब में। कभी किसी याद में मैं नन्हीं बच्ची होती हूँ, किसी में स्कूल-ड्रेस पहने कोई साधारण-सी दिखती गहरी साँवली छुपी-ढकी चुप्पा लड़की; जो इसलिए अपने सपनों को छिपाकर रखना चाहती थी, क्योंकि बता देने से सपने पूरे नहीं होते। वह बोलना भी चाहती थी, लेकिन इतना जानती नहीं थी कि अपने सपनों के बारे में किससे बोलना है?
मौत के बाद इधर तेरह दिन का रिवाज है—ऐसा पिता ने ही कभी बताया था, बड़े ताऊ के घर से निकलने के बाद। ताऊ की मृत्यु गले के कैंसर से हुई थी। उनका घर मोदीनगर, ग़ाज़ियाबाद में था। मोदीनगर से लौटते हुए रामपुर के पास ढाबे पर चाय पीते हुए, मृत्यु के बाद निभाई जाने वाली रस्मों का लोकाचार जैसे ढपोरशंखई पर पिता से बहस हो रही थी मेरी। अंत में वह विराम चिह्न लगाते हुए बोले—“रहना तो बेटा हमें इसी समाज में है!”
...और रहना ही था इस घर में। न रहती तो कौन रहता उनके पीछे! अधेड़ हो चुकी उनकी पत्नी यानी मेरी माँ; जिसकी कमर अब झुकने लगी थी, इसलिए झुकने लगी थी कि वह रीढ़ को सीधा रखने का अतिरिक्त प्रयास करती रही थीं। वह पैंतीस बरस प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल रही थीं और रिटायर हो चुकी थीं; लेकिन किसी पर बोझ नहीं बन सकतीं थी, इसलिए फिर से नौकरी की तलाश में जुटी रहती थीं। सो कमर जवाब देने लगी। ज़रूरत से अधिक तनाव क्या कोई सह भी सकता है—इलास्टिक भी नहीं, रेशम भी नहीं और जीवन तो बिल्कुल नहीं सहता। रीढ़ तो हड्डियों का ढाँचा ठहरी।
एक ताज़े वैधव्य को जीना, वह भी निपट अँधेरे में, उस जगह जिसे बाल-बच्चों के शोर में उनके साथ रहकर घर कहा हो, उस घर में एकदम अकेला हो जाना मुश्किल होता और संतान के जीवित रहते सूतक के दिनों में माँ का अकेला रह जाना, यह एक क़िस्म की हिंसा होती, अतः मैं संग ठहर गईं। वह भी इसलिए कि मुझे वहाँ ठहरे अरसा हो गया था।
उनके घर में यानी मेरे पिता के घर। बहुत बरस बाद, बहुत सारे खट्टे अनुभवों को सीने में दुपट्टे से छुपाना चाहते हुए रही। मिठास की खोज करते हुए रही। मिठास को यदि सुख कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसे स्मृति के स्वाद तक ही सोच सकती थी, जिसके याद आने भर से मन घुलकर चाशनी-सा हो जाए, ऐसा मीठा
उस घर में जहाँ भोर के तारे को देखते हुए देहरी पर मुट्ठी भर जौं, सिंदूर और फूल रखकर, दीप जलाकर नमस्कार किया था और सूरज उगने के साथ रोती सुबकती चली आई थी।
हाँ जितना याद आ रहा है कि आँखों का पानी नापने का मेरे पास तब कोई पैमाना नहीं था। न किसी ने मेरी घुलती आँखों को धुँधुआते हुए देख ही पाया था।
घर जहाँ अब मैं नहीं रहती थी। जहाँ से जब बाहर आई तब से मैं कहीं नहीं रहती, जिसे अपना घर समझकर इतने बरस रहती थी। अब वहाँ केवल माँ बचने वाली थी और इसी कारण बचने वाला था मायका, जितने दिन रही, अपने मायके में रही।
पिता की निश्चेष्ट देह के साथ, उस पूरी रात भर—मैं और माँ और मायका। साथ आए परिजन—मेरे जीवनसाथी और बच्चों को नींद आ गई—तीनों अंदर कमरे में जाकर सो गए। सुबह होने पर उन्हें जगाया। इधर छोटी बहन अपने पति और बच्ची समेत उसके शहर से चल दी थी, सुबह आती। आस-पड़ोस में से लोग दस मिनट-आधे घंटे को आते, साथ बैठते, अफ़सोस करते, उठते हुए कहते—“शायद दरवाज़ा खुला रह गया है, देखकर अभी लौटते हैं।”
चाय का पूछते, फिर खाने का। मैं उन सब के लिए मेहमान थी—बाहरी। अपने घर में बाहरी, अपने घर में मेहमान। उस घर में जहाँ मैंने बड़ा होना सीखा, खिलंदड़ापन छोड़ना सीखा और ब्याह के बाद घर का छूट जाना भी।
अब याद कर रही हूँ कि उस रात क्या मैंने चाय पी थी? अगर पी थी तो कितनी बार? नहीं पी तो कितनी बार मना किया? कितनी बार झूठ बोला? कितनी बार कहा सब ठीक है? पता नहीं कौन-सी धूपबत्ती जला दी गई थी? किसने जलाई थी? बार-बार कि सुबह तक वह महक मिटी नहीं! अब तक नथुनों से वह गंध नहीं मिटी। जैसे स्मृति के शरीर से लिपट गया है वह धुआँ। उस धुएँ के घेरे में रहना अब रास भी आने लगा। लगने लगा कि यही मोह है। मोह या प्रेम या संबंध या रक्त का बंधन। क्या सही शब्द है इस लगाव के लिए?
उस आँगन में चाँद पहले भी सैकड़ों बार देखा था। अलग-अलग भावों से भरते हुए—चढ़ते, खिलते, मुँह चुराते, इठलाते, लेकिन जैसा चाँद उस रात था, वह पहली बार था। समझ आया कि यह चाँद इस समय कितना अनूठा और याद में कील ठोंकने के निशान की तरह रह जाने वाला चाँद होने जा रहा है।
उस दोपहर मैं रसोई में बस एक रोटी ही बनाती रह गई थी पिता के लिए और पिता थे कि रोटी खाए बग़ैर ही दूसरी दुनिया को चले गए। मिले भी नहीं।
आख़िरी बार कहा भी नहीं कि अच्छा बेटा चलते हैं अब! जब तक मैं टिफ़िन लादे और बोतल में नारियल पानी भरकर पहुँची, वह शांत हो चुके थे। पहली बार देख रही थी कि सबसे गहरी नींद में लीन चेहरा कैसा निष्कलुष होता है! लगता है कि अभी पुकारने पर उनकी नींद टूट जाएगी और जाग जाएँगे, लेकिन नींद से जगाना—अमानवीयता है! एक तरह का अपराध!
उनके चले जाने के बाद जितने बचे थे, वे उस सबको एंबुलेंस के स्प्रिंग लगे स्ट्रेचर पर लिटाए हुए लेकर, मैं कहीं खोई हुई लौट रही थी। रास्ते में उन्हें हवा अपने शोर से न सताए या कि मच्छर न लगे इसलिए अपना ओढ़ा हुआ सफ़ेद छींटदार दुपट्टा उतारा और ओढ़ाया। बार-बार उनकी बाँह को छूते हुए मैंने नरमी को सख़्ती में बदलते महसूस किया। यह सख़्ती एक मृत देह की निठुराई थी। एक संकेत कि अब फ़र्क़ नहीं पड़ रहा; तुम कितना भी मुझे छुओ, सहलाओ, पुचकारो, प्यार करो या आवाज़ें देकर जगाओ।
चेहरा दूसरी ओर, खिड़की की तरफ़ मुड़ गया था। मानो हम माँ बेटी की ओर देखना नहीं चाहते थे या हम से हमारी लापरवाहियों के लिए रूठ गए थे। उनकी हथेली जितनी देर अपनी हथेलियों के बीच थाम रखी थी, लगा नहीं कि उन तक मेरी कंपकंपाती हुई उम्मीद पहुँच नहीं रही!
कभी धोखा नहीं देते, जो अपने होते हैं—ऐसा मानती थी माँ। कहतीं कि कोई तुम्हारा अपना नुक़सान करेगा भी तो कोशिश करेगा कि तुम्हें छाँह में रखे, धूप के वार से दूर। फिर लगा कि देह में तो केवल देह बची रह गई। कोई और चीज़ थी जो मेरी कोमल मुलायम हथेली को थामती और सड़क पार करवाती थी। मुझे बाँह भरकर गोद में उठाती। वह कोई रोशनी थी जो कुछ दो तीन घंटे पहले ही कहीं खो गई थी; जिसकी कमी अब दिन ढलने के साथ पसरते अँधेरे में दिखाई दे रही है। तो हथेली छोड़कर माँ के कंधे पर अपना बोझ डाल दिया। मेरे अपंग स्वार्थ का तो कोई अंत ही नहीं था। या कि यह अंत के आगे की कोई स्थिति थी, जिसे समझने का साहस मुझमें अभी तक नहीं जन्मा था।
यह कैसा चीकट शोक था कि हाथ में पकड़े फ़ोन के ज़रिये लगातार मुझे मालूम होता रहता था कि उन्हीं दिनों कई हज़ार किमी दूर गज़ा पट्टी और इजराइल के बीच एकतरफ़ा घमासान में गज़ा शहर में जाने कितने बच्चों के पिता और कितने पिताओं के बच्चे मारे गए, कुचले गए, रौंदे गए, और भूख-प्यास से मरने छोड़ दिए जा रहे हैं। मैं कितनी अश्लील लग रही थी कि मेरे दुख में मैं किस क़दर लिथड़ी जा रही थी कि किसी फ़ोन को उठाते भी मेरा अहम काँप रहा था। कोई बाहरी तसल्ली नहीं सुनना चाहती थी जैसे।
यह जो सामने लेटे हैं इस वक़्त, इनसे मुझे कितनी शिकायतें रहीं। अभी आज सुबह तक भी क़रीब दो तीन शिकायतें तो थीं ही, जो अब छाछ में मक्खन की तरह बिलो गईं। अपनी याददाश्त में मैं किसी रेतीले ढूह का तिरोहित होना और रेत कणों में अपनी ज़िंदगी का डूबते जाना देख रही थी। डर रही थी कि अब इन शिकायतों की साँसों का इंतज़ाम मैं कैसे करूँगी? कहाँ से लाऊँगी वह ऑक्सीजन सिलिंडर? वह मकान, वे लपटें, वे चीथड़े, जिन्हें मैं अपने विक्षिप्त दिनों में अपनी देह से उतारती और उन्हें दान कर देती। जैसे वह किसी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित देवी प्रतिमा हों जिस पर पुजारी वस्त्र आभूषण चढ़ाने, उतारने, नहलाने और सजाने का काम करता है, मोहल्ले के आस्तिक धड़े को भरमाए रखता है। मैं किसके सामने ख़ुद को रद्दी काग़ज़ से तोलूँगी और उनके फ़ैसलों में उन्हीं को ग़लत ठहराऊँगी। सब एक देह के ठंडे पड़ते जाने से उठते भँवर में अपनी पहचान खोता चला जा रहा था।
अस्पताल से गाड़ी स्टार्ट होने के साथ ही माँ ने आश्वस्ति चाही—मतलब दिया बुझ गया? मैंने कुछ कहा नहीं; लेकिन उन्होंने सुन लिया, क्योंकि चुप मुझसे रहा नहीं गया। कुछ मिनट बाद माँ ने ही गाड़ी के भीतर जम चुका मौन तोड़ा।
“सब को ख़बर कर दो”। “फोन…”
ख़बर करने के लिए कुल पाँच नंबर याद आए। बारी-बारी से मिलाया और ख़बर कर दी।
फिर कुछ और मिनट तक बर्फ़ जमी रही। मुझे कोई आवाज़ आई। देखा वह बोल रही थीं—अब उनका क्या होगा? वह कैसे जिएँगीं—किसके सहारे जिएँगीं? पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा—अभी मैं हूँ। मेरे साथ जी लेना, जैसे मैं जियूँ। आप जीना लेकिन मेरे सहारे नहीं अपने सहारे। अपनी रीढ़ है आपकी—जिसके दम पर आपने मुझे गोद लिया, पाला, बड़ा किया, उस रीढ़ के सहारे जीना। यह जो सामने गिर गया है सहारा, यह भ्रम टूट चुका है अब कि हम इसके सहारे थे।
इतना सब कहा नहीं था। सोचकर रह गई। सोचा था शिकायतों को कंधे पर टिकाए बग़ैर मैं भी कैसे जियूँगी अपनी पीठ पर लादकर। क्या बोझ से मेरी पीठ दोहरा नहीं जाएगी?
अपनी नाकामियाँ, हार, बेइज़्ज़तियाँ किसे सौंपूँगी? कहा नहीं। कहा कुछ भी नहीं था उस वक़्त। एंबुलेंस दौड़े जा रही थी। तेज़ शोर करती, हॉर्न देती, रास्ता बचाती हुई सबसे तेज़ शायद।
तब जाना कि हर एंबुलेंस में गंभीर और मरणासन्न मरीज़ ही नहीं होते। कुछ में गंभीरता से मरी हुई ज़िंदगियाँ भी ज़रूर होती हैं और कुछ में लाशें भी, जैसे उस रोज़ थी। मैं थी, पिता थे; पहली बार एंबुलेंस के अंदर—ज़िंदा और ठीकठाक। ज़िंदा लेकिन ठीकठाक पर मुझे संदेह है।
पिता के चले जाने के बाद कुछ दिनों तक लगा ही नहीं कि पिता नहीं हैं। लगा कि वह कहीं गए हैं। कहीं बाहर। किसी शहर, किसी क़स्बे, किसी नाते-रिश्तेदारी में, किसी ब्याह-शादी में, किसी ज़रूरतमंद को ख़ून देने, बरेली तक। बरेली ही था मेरे क़स्बे के सबसे क़रीब का शहर।
कुछ घंटों, हफ़्तों तक अजीब-सा इंतज़ार रहा। अजीब-सा दर्द था, अजीब-सी चोट लगी थी मुझे। कहाँ लगी थी, मुझे उस जगह का पता नहीं चलता था। टटोलने पर भी नहीं। जैसे अबोले बच्चे को पेट दर्द बताना नहीं आता ऐसा कुछ मेरे साथ दोहराया जा रहा था।
अपनी देह में वह कौन-सी जगह होती है, जिस में ऐसे दर्द रहते हैं जो किसी को समझाए नहीं जाते। ऐसी चोटें जैसे बहुत काले चमड़े पर मारे गए कोड़े से पड़ा नील।
वह रास्ता लंबा था बहुत, जिस पर उन्हें दिन में आना था साँस लेते हुए और लौटने के पहले उनकी साँसों की पोटली का ग़ुम हो जाना था। मेरे जिस्म में इतनी जान नहीं थी कि अपनी साँसों में से कुछ साँसों को उन्हें देकर उनका मुझ पर चढ़ाया साँसों का क़र्ज़ उतार पाती। जान ही नहीं पाई कि रेशम की डोरी से भी धीमी आवाज़ होती है, जब साँस की डोरी टूटती है। वरना थाम न लेती। उनके आगे हठ करती। ज़मीन पर लोट जाती और कहती कि बाद में कभी जाना। अभी नहीं! ऐसा कर पाती तो जानती हूँ, वह मेरी सुन लेते। मैं एकसंग उनकी माँ उनकी बेटी। कैसे टालते! इसलिए जब ग़लती कर दी तो चुपचाप ऐसे लेट गए कि जैसे मृत्यु आ गई हो। और मैं कुछ न कह सकूँ। उन्हें बख्श दूँ। उनसे अब कोई ज़िद न करूँ।
शाम के सवा तीन से रात के साढ़े नौ बज गए थे। उस घर के आँगन से मुझे क्या हटाना, क्या रखना है? माँ ने एंबुलेंस में समझा दिया था।
दुनिया इतनी अड़ियल जगह है कि भूख, प्यास और मौत के आ जाने पर भी अपना नंगापन नहीं छोड़ती। आँगन बहुत छोटा था—संकरा, इसलिए उनकी देह को उत्तर का सिरहाना मैं नहीं दे सकी। छोटे ताऊ ने कहा पूरब-पश्चिम बिछा! आने-जाने वालों का भी सोच!
मैं आने-जाने वालों का सोचने लगी। सोचने लगी कि कहना मानने वाली लड़कियों के पास उनकी अपनी बुद्धि और विवेक नहीं होता। वे बस कहना मानती हैं। वे शरीफ़ घर की लड़कियाँ होती हैं।
पिता के शरीर को लाया गया। लिटाया गया। एकाएक रोने की आवाज़ें आईं। ये परिवार था पिता का। वह परिवार जिसे उसने उनके गिरे हुए समय में लताड़ें दीं। हुक्का पानी बंद करने जैसा माहौल बनाया, जिस चुप से पिता बहुत ख़ौफ़ खाते थे और सबसे अच्छा व्यवहार और थोड़ा सम्मान चाहते थे, आज वह पिता नाउम्मीद होकर ख़ुद चुप थे। अगर इसे नाउम्मीद न कहूँ तो स्थितिप्रज्ञता कह सकती हूँ कि दुख और विछोह को जताती इन आवाज़ों का उनके कानों की झील में एक कंकड़ भी गिरता तो आवाज़ न होती, लहर न उठती। स्पंदन कहीं दूर खो चुके थे। प्राण प्रयाण पर जा चुके थे अकेले।
वे जो मेरे पिता के भाई-बंधु-पड़ोसी थे, बाहर से आए झाँककर वापस चले गए। औरतें कुछ देर बैठतीं। मेरा मुँह देखतीं, माँ का मुँह देखतीं। देखतीं कि हम कब टूट कर फूट पड़ेंगे। पर जाने क्या जम गया था हमारे अंदर कि जैसे हम इस दृश्य के लिए जाने कब से ख़ुद को तैयारी में लगाए हुए थे। हमारे लिए पिता का यह बिछावन अप्रत्याशित, अनपेक्षित बिल्कुल नहीं था जैसे। हमने कभी नहीं सोचा था कि वह अमर हों। हमने उनकी मौत की कल्पना बहुत सालों पहले से ही की हुई थी। केवल उनकी मौत की ही क्यों अपनी मौत की भी और भी अपनों की मौत की कल्पना भी।
दो लोग उस जगह उनके साथ बैठे रहे। मृत देह जहाँ रखी थी, वह स्थान अपनी पूर्व स्मृतियों के साथ अलग फुलझडियाँ छोड़ रहा था। कभी कोई दृश्य जागता रहा कभी कोई अदृश्य। यहीं आँगन में मैंने कितनी अल्पनाएँ सजाई थीं, होली दीवाली के मौक़े पर। अभी पूरी रात काटनी थी जो किसी अज्ञात पहाड़-सी लग रही थी और हम निहत्थे।
अब जब याद कर रही हूँ, वह जगह तो पीछे का कुछ नहीं उभरता, सिवा उस देह के जो इतने वर्षों से हमारी अपनी थी। हम जिसके लौटने का इंतज़ार करते थे। वह ख़ाली हाथ घर नहीं लौटे कभी। कानपुर के किसी कारख़ाने में स्टोर-कीपर की नौकरी करने वाले पिता एक दिन स्टोर में हुई चोरी के बाद पूछताछ की रस्म अदायगी में छंटनी में निकाल दिए गए। कानपुर छूट गया तो फ़र्रुखाबाद चले आए। यहाँ भी ठंडी सड़क के पार किसी फ़र्टिलाइजर कंपनी में काम किया। फिर एक छंटनी का दौर आया और वह ख़ाली होकर बैठे रहे।
उस शहर में एक रिश्तेदारी निकल आई थी। यहाँ तो खाने को दौड़ता दिन, बिताने को उनके दवाखाने की बेंच पर बैठ दिन निकाल लेते। देखते-ही-देखते मरीज़ों को देखना, समझना, समझाना से लेकर जाँचना और दवाई लिखना तक सीख लिया था, एक तरह के कंपाउंडर हो गए मामा के दवाख़ाने में। मामा भी सगे नहीं, सगे से बढ़कर। बीवी उनकी सोशल वर्कर और अँग्रेज़ी मीडियम का स्कूल चलातीं, जिसमें माँ नौकरी करने लगीं और बेसिक पढ़ाई-लिखाई मुफ़्त में मुझे मयस्सर होने लगी। चार पैसे आने लगे तो पिता का हौसला माँ ने बढ़ाया और कहा छोटी जगहों पर इतने लोग कंपाउंडर से डॉक्टर हुए जा रहे हैं तो तुम ही कब तक सिधाई और ईमानदारी की पताका फहराए घूमोगे! भगवान चाहता तो तुम्हारी नौकरी दो-दो बार न छीनता। वह चाहता है कि तुम ख़ुद का कोई काम करो; जिससे ग़रीब-ग़ुरबों की मदद हो और डाक्टरी से बढ़िया और कौन काम है, जो व्याधि हरे और दुआ बटोरे नाम भी कमाए।
जैसे गरम लोहे पर हथौड़े की चोट लग गई और कंपाउंडरी करते-करते एक दिन पास ही के गाँव जाकर मेन बाज़ार में एक आठ-बाई-छह की दुकान तय कर आए किराए पर। मामा का आशीर्वाद लिया। अब मामा रिश्ते में साले कम गुरू ज़्यादा थे। अपना दवाख़ाना खोला। बूंदी के लड्डू बँटे और पूरियाँ छनीं। फिर हम यानी मैं और माँ भी गाँव चले आए। तब से गाँव-गाँव में पिता डॉक्टर साब के नाम से जाने जाते। संपेरे का मुफ़्त इलाज किया तो बदले में साँप काटे के ज़हर उतारने की जड़ी दे गया बतौर मेहनताना। अब यह जो ज़हर इनकी देह पर चढ़ता जा रहा है ज़िंदगी का, इसके लिए मैं कौन-सी जड़ी लाऊँ! बिना डिग्री के डॉक्टर होने वाले एक डॉक्टर की संतान होने के कितने नुक़सान होते हैं, मैं किसी भी तरह गिनवा नहीं सकती लेकिन एक करुणामय पुरुष की संतान होने के बहुत फ़ायदे हैं। मसलन कि एक तो आज्ञाकारी होना ही है।
सुबह होने में वक़्त लगा, लेकिन सुबह हुई। होनी ही थी। ऐसा ही कुछ नियम है। दिन के बाद शाम, शाम से गहराती है रात, रात के बाद आ ही जाती है अपने आप सुबह। अँधेरे का छाता फट गया और रोशनी के छींटे भीतर तक गिरने लगे। लोग आते गए, जाते गए। अपने रिश्ते पिता के साथ कैसे रहे, इस पर बताते, हैरान होते जैसे कि यह उनकी देखी कोई पहली आकस्मिक घटना है, जोकि सरासर एक छद्म है, मैं उनकी सहानुभूति पर हाथ जोड़ती रही और मैं कर भी क्या सकती थी! न चाहते हुए भी मुझे विनम्र और ज़रूरतमंद दिखना पड़ा क्योंकि यही रिवाज है। मृत्यु का लोकाचार यही कहता है कि चुप रहिए और सब सहिए।
नई पीली सूती चद्दर आई, फूल, सुतली, बाँस, बताशे, मखाने, मेवा, नारियल, देसी घी, हवन सामग्री, हंडिया, कंडे, रस्सी आई। बान आए। हर चीज़ कोरी, एकदम नई।
नए बान भी।
अर्थी में कसे गए उनके शरीर को देखकर नहीं उनके चेहरे को देखते ही हर इतवार सुबह में बान की ढीली हुई चारपाई कसते उकडूँ बैठे पिता दिखाई दिए। कभी बान की चारपाइयों पर ही सब सोया करते थे बड़े आँगन में। मैं पिता के साथ सोती रही कक्षा छह तक। पिता की नंगी-नरम पसीने से नम पीठ पर बान वाली चारपाई की छपाई पर हाथ फिराती तो सुख होता था।
पिता के साथ सोती तो उनकी बग़ल से आती गंध मुझे सुहाती। पिता की देह से उठती वह गंध ऐसा परिवेश बनाती कि मैं सुरक्षित हूँ। शायद परिंदों और चौपायों में गंध का रसायन विज्ञान अधिक पाया जाता है, तो इस लिहाज़ से उन दिनों मैं प्रकृति के अधिक क़रीब रही होऊँगी। उसी प्रकृति के क़रीब जिसकी गोद में बैठाने को वह मुझे सुबह पाँच बजे उठाकर रामलीला मैदान के आगे की गुमटी तक ले जाया करते थे, भराभर जाड़ों में। अपनी लड़की को बिगाड़ रहे हो—मोहल्ला कहता है। उन्होंने कभी नहीं सुना। सुना भी तो मुझ तक आने नहीं दिया।
बान की बिनी चारपाइयों पर लगे सफ़ेद खेस के बिछौने और वह बड़ा-सा आँगन। वही आँगन जो बँटते-बनते, इतना बड़ा ही बचा कि उन की पार्थिव देह को उत्तर दक्षिण नहीं मिला पूरब-पश्चिम ने उनकी देह का बचा खुचा लोहा, चुंबक खींच बाहर किया।
अब वे ठंडे पड़ गए थे। कोहरे पाले जैसे। रात एक बजे जब किसी के कहने पर उनके मुँह में गंगाजल और तुलसी दल और माँ के माँग-टीके का एक सितारा तोड़ा और मुँह में डाला। वह पी गए। मुझे लगा शायद वह ज़िंदा होने वाले हैं। अभी रात है, सो रहे हैं। सुबह होने के पहले ही चाचा उनके नथुनों में रूई के फाहे रख गए। मैं डर गई थी कि अगर साँस आई तो वह कैसे लेंगे? दम घुटने लगता, सो मैंने फाहे हटा दिए। उनसे झख करती रही इसलिए भी कि उन्हें अकेलेपन से ऊब थी और बातें करना उनकी हॉबी थी।
उस रात मैं दूसरे मनुष्य में तब्दील हो चुकी थी। उस मनुष्य में जिसे हम सपने में देखते हैं, अपने मुखौटे की तरह देखते हुए सब कुछ निरपेक्ष। कुछ बुरा नहीं हुआ था, जैसे और अभी तो वह बान वाली चारपाई के पायताने के रस्से को कसकर चारपाई सोने लायक़ तनी हुई बना रहे हैं, जिस पर मैं सोऊँगी उनके साथ। उनकी छाती पर कान टिकाए धुकधुकी सुनूँगी और सुनूँगी उनके पेट के हुक्के की गुड़गुड़ाहट। अभी उनके तलवे में गुदगुदी करूँगी और वह दिन भर के अपने देखे सुने क़िस्से सुनाएँगे, आज ये हुआ, आज वो हुआ—लेकिन ऐसा कुछ आज नहीं हो रहा।
चारपाई कसते हुए पिता हूबहू ठीक मेरी आँखों की तरल झिल्ली में तैर आए हैं, जिन्हें किसी और झिल्ली में उन्हीं बानों से, नए ख़रीद कर लाए बानों से कसे गए दिख रहे हैं। बेजान—मुर्दा कहते हैं कठोर शब्द में।
चलते हुए नमस्कार की घड़ी में मुझे बुलाया तो मैं उन्हें नमस्कार कर विदा नहीं कर रही थी, पर जैसे मेरे बचपन का एक दृश्य छिटका और पिता के रूप में मुझे कहने लगा मुझे प्रेम से जाने दो और मैंने उन्हें लिपट कर चूम लिया साथ ही माँ का ख़याल रखने का वादा किया।
...और मुझे नहीं याद कि किन-किन लोगों ने अपने कंधों पर उन्हें उठाया था और लिए चले गए।
पिता के पीछे रह गया उनका अपना परिवार। कुछ घंटों बाद सब लौट आए, बस उन्हें कहीं छोड़ आए। पिता के भाइयों की चहल क़दमी बराबर होती रहती, उसी फाटक के अंदर उनके अपने-अपने रिहायशी हिस्सों में; मगर कुछ था जिसके खो जाने का ग़म बहुत ज़्यादा तैर रहा था हवा में। सब चुप थे। सब अपनी-अपनी याद में थे पिता के साथ, जिन्हें चौराहे पर और आँगन में दीप जलाकर अँधेरे से बचाने की कोशिश करना अभी बाक़ी था।
पर जब सब किया था तो इसे ही क्यों छोड़ना? एक पत्तल, पहली पत्तल परोसकर चौराहे पर। कुत्ते, बिल्लियों, कौवों को खाने के लिए रखना। लौटते हुए के रास्ते में काँटे रखना, कीलें बिखेरना कि वह लौट न सकें। जिस राह गए उस राह से नहीं लौटे कि वह साथ चलें तो रास्ता भटक जाएँ। क्या वाक़ई? यह सब वे लोग अब भी कर रहे थे लगातार, जबकि उनके होते हुए पर भी उन्होंने उनके साथ यही किया था। उन्हें अनबोले का ख़ौफ़ बड़ा था, उन्हें अबोला ही दिया था मिलकर उनके भाइयों ने।
अगले दिन सुबह सब सामान्य लग रहा था। चाय बनी तो मैंने झाड़ू उठाई। सोचा घर का कोना-कोना बरसों बाद बुहार दूँ। सफ़ाई कर के बैठूँ फिर पिता की बातें करूँ। माँ को देखूँ, उन्हें बताऊँ कि जो उन्होंने कहा था आख़िरी ई सी जी के वक़्त कि अब मेरा क्या होगा?—मैं कह दूँ कि मैं हूँ आपके साथ। मुझे देखो न आप। जैसे मेरे लिए आप हो वैसे आपके लिए अब से मैं।
ज्यों ही अलमारी खोली तो जैसे कोई पोटली खुलकर फ़र्श पर बिखर गई। ये गोलियाँ कैसी थीं? माँ ने बताया जब उन्हें नींद नहीं आती थी तो लेते थे। इतनी गोलियाँ कौन रखता है घर पर, वह भी नींद की गोलियों जैसी जोखिम भरी भावुकता। अक्सर खाते थे माँ ने बताया। परसों रात भी ऐसे ही बिखरी पड़ी थीं।
गोलियाँ बिखरी थीं तो माँ ने समेट दी थीं। अब मेरी बारी थी, यह सुनकर बिखरने की। मुझे कैसे समेटतीं वह?
पिता नहीं थे। कहीं भी नहीं। न कहीं गए थे। न कहीं से लौटने वाले थे। न संभव था उनका होना, न संभावना थी कि वह लौट सकते हैं। हमने शरीर जलाकर राख कर दिया था। पता नहीं कितनी गोलियाँ भी साथ ही राख में मिली होंगी
और क्यों?
इतना बड़ा प्रश्नवाचक शब्द होता है—“क्यों”।
इतना वृहद इतना विशालकाय कि इसके सामने मैं बौनी पड़ गई थी। मुझे कोई उठाने नहीं आया। न गले से भींचकर रुलाने, न सँभालने ही। न वजह बताने कि क्यों रखते थे वह इतनी ढेर नींद की गोलियाँ? शायद कोई जानता ही न था कि उनके भीतर क्या चलता रहा? कब के मर चुके थे वह या कि मरने से कितना डरते थे? उन्हें अपने भाई बंधुओं से थोड़ा प्यार और संवाद चाहिए था। कभी न मिला तो शायद गोलियों की गोद में सिर टेककर आ जाती रही थी नींद। उन्हें किसी की कमी अखरती नहीं होगी। क्या जाने किसी मरीज़ के लिए रखी हों या क्या जाने किसी और की हों। मैं डूब रही थी उतरा रही थी। ख़ुद सवाल उठा रही थी और ख़ुद जवाब दे रही थी।
ऊपर से शांत और सहनशील दिखती हुई भीतर से भी अब चुप थी।
यही कर सकती थी। यही नियम है। मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं था जो कहता कि पिता नहीं न सही, अब से तुम्हारे साथ मैं हूँ!
शायद एक माँ से बचा हुआ मायका ही वह ईमानदार सहारा था, जो मुझसे बिना कहे कह रहा था कि तुम्हारे साथ हूँ। तब तक, जब तक तुम्हारे लिए माँ हैं। चाहो तो तुम मुझमें आकर छुप जाना। मेरी छाती से लिपटकर बाक़ी सब भूल जाना और बस इतना याद रखना कि पिता नहीं हैं। न सही। मैं हूँ। मैं तुम्हारा अपना मायका हूँ। कुछ दिन रहना फिर लौट जाना।
ख़ुश रहना।
रह रही हूँ।
याद आ रही है वह बात कि—“रहना तो बेटा हमें इसी समाज में है।”
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

