मृत्यु ही जीवन का सबसे विश्वसनीय वादा है
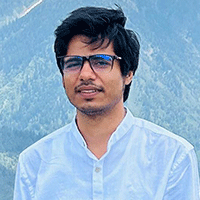 रविंद्र कुमार
20 सितम्बर 2025
रविंद्र कुमार
20 सितम्बर 2025
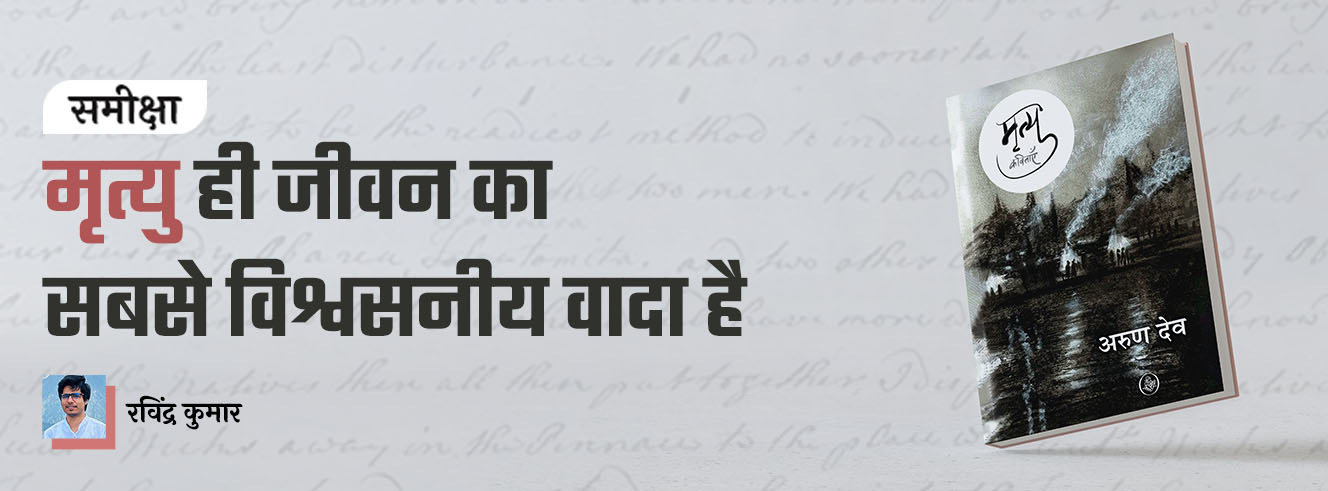
जिस क्षण हम जन्म लेते हैं, उसी क्षण मृत्यु हमारे साथ चल पड़ती है। हमारा हर क़दम अपनी मृत्यु की ओर उसकी छाया की तरह उठता है। हर बीता हुआ कल वर्तमान में समाकर आने वाले कल से मिलने की दिशा में बढ़ता है। अरुण देव का नया संग्रह ‘मृत्यु : कविताएँ’ इसी अवश्यम्भावी सहयात्री का सामना करता है, उसे नकारता नहीं, बल्कि कविताओं के सहारे उसका आलिंगन करता है।
जीवन और मृत्यु सहोदर स्थितियाँ हैं—एक-दूसरे की परछाइयाँ। मृत्यु जगत का शाश्वत सत्य है और जीवन उसी के साये में पलता है। इसके बावजूद आधुनिक हिंदी काव्य में मृत्यु के अनुभवों पर केंद्रित किसी समूचे संग्रह का अभाव रहा है। ऐसी स्थिति में समकालीन कवि, आलोचक और संपादक अरुण देव द्वारा रचित कविता-संग्रह ‘मृत्यु: कविताएँ’ (राजकमल प्रकाशन, 2025) का प्रकाशन एक विशिष्ट साहित्यिक घटना है।
अरुण देव, जन्म 1972; समकालीन हिंदी कविता के चर्चित स्वर हैं और ‘क्या तो समय’, ‘कोई तो जगह हो’ और ‘उत्तर पैग़म्बर’ जैसे सराहे गए संग्रहों के बाद अब चौथे कविता-संग्रह के रूप में उन्होंने मृत्यु जैसे दुरूह विषय पर क़लम उठाई है। उन्होंने सिर्फ़ क़लम नहीं उठाई, बल्कि गगन गिल के शब्दों में यह रचनाएँ “मृत्यु की चेतना से प्रभासित विज़डम” रचती हैं, जो हमारे भीतर जीवन की नई प्यास भर देती हैं।
प्राक्कथन में डॉ. राधावल्लभ त्रिपाठी लिखते हैं कि “जीवन और मृत्यु के बीच कितना कम फ़ासला है... एक बारीक रेखा है, जिसके एक पार जीवन है और दूसरे पार मृत्यु।” यह पंक्ति पूरे संग्रह की केंद्रीय भावना का सूत्रवाक्य बन जाती है। अरुण देव ने मृत्यु के लगभग सभी आयामों और भावों को इन सौ कविताओं में दर्ज किया है। कवि अरुण कमल ठीक ही कहते हैं कि “मृत्यु की कविताएँ अंततः जीवन की कविताएँ होती हैं”—इस संग्रह को पढ़ते हुए सचमुच जीवन का मूल्य नए अर्थों में उजागर होता है।
यहाँ मृत्यु किसी परलोक की कल्पना या ईश्वर के सहारे से नहीं आती। यह मृत्यु यहीं की है, इसी पृथ्वी की, इसी मनुष्य जीवन की। कवि स्पष्ट करता है कि जो कुछ है, इसी लोक में है। यह दृष्टिकोण कवि को किसी भी तरह की सांत्वना-प्रधान काव्यभूमि से अलग करता है और एक ठोस यथार्थ में टिकाता है।
मृत्यु के विविध रूप
संग्रह की कविताओं में मृत्यु कभी गहरी निजी अनुभूतियों के रूप में आती है, तो कभी सामाजिक-राजनीतिक प्रसंगों को छू जाती है।
एक कविता में पिता अंतिम बार घर से विदा होते हुए माँ से बच्चे की तरह अपनी भूलों की माफ़ी माँगते हैं और कहते हैं, “अच्छा, अब मैं चलता हूँ।” फिर वे चुपचाप मृत्यु की उँगली पकड़कर चल देते हैं। यह दृश्य मृत्यु को भयावह नहीं, बल्कि एक स्नेही सहयात्री बना देता है।
दूसरी ओर, एक कविता कहती है : “जो स्त्रियाँ मरती हैं उन्हें मृत्यु नहीं, जीवन मारता है।” यह पंक्ति स्त्री जीवन के दमन और पीड़ा की त्रासदी को एक ही झटके में उद्घाटित कर देती है।
कुछ कविताएँ जीवन से प्रेम करने वाले गहरे दार्शनिक दृष्टिकोण को उद्घाटित करती हैं। जैसे : “मृत्यु के बाद अहम् की राख बचती है, घृणा की जली टहनियाँ।” कवि यह याद दिलाता है कि मनुष्य जिस अंधेपन का जीवन जी रहा है, उसमें यह भूल जाता है कि जीवन, अहंकार, प्रभुता, शत्रुताएँ—ये सब क्षणिक हैं। शाश्वत केवल मृत्यु है।
इसी तरह एक अन्य कविता में कवि लिखता है : “वह नहीं चाहता है उसकी उपलब्धियों से भर दी जाए शोकसभा की यह शाम, विवरणों से ऊब जाएँ परिजन।” यह पंक्ति मृत्यु को दिखावे और औपचारिकता से परे रखकर उसकी सहजता को सामने लाती है।
कुछ कविताएँ हमारे समय की सामूहिक त्रासदियों को दर्ज करती हैं—मलबे के नीचे दबे मासूम बच्चे, हिंसा और विस्थापन से जर्जर जीवन। कवि लिखता है : “कुछ देर पहले यहाँ घर था— मुन्नी और उसकी गुड़िया, माँ पर गिर रही है रात और राख, बाबू को चुप करा रहा है भाई, उसके एक हाथ पर गहरा ज़ख़्म है।”
कवि अपने युग-बोध से पूरी तरह सजग है। उसे पता है कि असहमति की आवाज़ें दबा दी जाती हैं, असहमत इंसानों को सज़ाएँ मिलती हैं। इसको दर्ज करते हुए कवि लिखता है कि यदि उसकी जेब से आत्महत्या का पुर्ज़ा मिले तो इसे आत्महत्या न समझा जाए, बल्कि हत्या समझा जाए। यह स्वर मृत्यु के बहाने वर्तमान राजनीतिक असहिष्णुता पर सीधा प्रहार है। इस तरह मृत्यु यहाँ केवल निजी क्षति नहीं है, बल्कि सामाजिक अनुभव भी है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर हमें झकझोरती है।
सांस्कृतिक और दार्शनिक आयाम
अरुण देव की कविताएँ भारतीय परंपरा और विश्व साहित्य, दोनों से गहन संवाद करती हैं।
महाभारत के यक्ष-प्रश्न, युधिष्ठिर की कथा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण से लेकर कबीर के निर्भीक स्वर तक के संकेत यहाँ मिलते हैं। कवि का जन्मस्थान कुशीनगर (जहाँ बुद्ध ने अंतिम श्वास ली) भी एक प्रतीकात्मक भूमि है, जो संग्रह में कई बार उभरता है। अरुण देव कबीर से लेकर कामू तक को याद करते हैं। एक कविता में स्पष्ट पंक्ति आती है: “जीवन के दलदल में धँसे सिसीफ़स से कहता है अल्बैर कामू।” यह संदर्भ भारतीय अनुभव और यूरोपीय अस्तित्ववाद के बीच एक सेतु बना देता है।
वे कुछ शब्दों में ही गहरी बात कहने का हुनर जानते हैं। संग्रह की पहली कविता है : “अंत है, अनंत है, अंतिम है, आश्वस्ति है।” और वही संग्रह इस आश्वस्ति पर समाप्त होता है : “मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, सृष्टि रहेगी।” यही जीवन का सार है कि जीवन कितना भी क्षणिक और क्षणभंगुर हो, मृत्यु चाहे सहयात्री हो, फिर भी मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रह जाता है।
भाषा और शिल्प सौंदर्य
शिल्प की दृष्टि से अरुण देव की कविताएँ अत्यंत प्रभावशाली हैं। अधिकांश मुक्त छंद में लिखी गई हैं और कई कविताएँ इतनी संक्षिप्त हैं कि वे अंतिम साँस जैसी प्रतीत होती हैं।
भाषा सीधी और पारदर्शी है, पर उसमें बिंबों और रूपकों की ताज़गी है। राख से अस्थियाँ चुनने को कवि “फूल चुनना” कहता है—मृत्यु के कर्म को करुणा और कोमलता से रूपांतरित कर देता है।
जैसा कि यह संग्रह कवि ने अपने पिता को समर्पित किया है, तो स्वाभाविक है कि कविताओं में बार-बार पिता की स्मृति आती है। एक जगह वे लिखते हैं : “पुल से गुज़रता हूँ, नदी को देखता हूँ—जो ले गई थी पिता को।” यहाँ कवि भारतीय सांस्कृतिक जीवनबोध को भी रेखांकित करता है, जहाँ नदियाँ, आकाश, वृक्ष और प्रकृति जीवन और मृत्यु से गहराई से जुड़ी होती हैं। वह कहता है : “प्रणाम करता हूँ पिता को, नदी को, प्रतीक्षारत मृत्यु को।”
यहाँ मृत्यु को कभी भी ईश्वर, परलोक या पुनर्जन्म के सहारे से नहीं देखा गया है। यह भौतिक संसार का सत्य है। यही बात इन कविताओं को आधुनिक भी बनाती है और विशिष्ट भी।
और अंत में
‘मृत्यु: कविताएँ’ पढ़ते हुए मृत्यु का भय नहीं, बल्कि एक निर्भीक दृष्टि और जीवन के प्रति नया सम्मान जागता है। डॉ. त्रिपाठी ने सही कहा है : “कविता मृत्यु का सामना करने के लिए हमें कवच पहनाती है।” यह संग्रह भी पाठक को मृत्यु के भय से मुक्त कर साहस का कवच पहनाता है। कवि गगन गिल उत्तरकथन में लिखती हैं : “हम कितनी बार, किस-किस तरह से रोज़ मरते हैं... इस मरने में भी सांस्कृतिक स्मृति है।” सचमुच, इन कविताओं में मृत्यु केवल अंत नहीं, बल्कि जीवन की निरंतरता का प्रतिबिंब है।
संग्रह की अंतिम पंक्ति—“मैं नहीं रहूँगा, तुम नहीं रहोगे, सृष्टि रहेगी”—मृत्यु की क्षणभंगुरता और सृष्टि की निरंतरता दोनों का गान करती है।
समग्रतः, ‘मृत्यु : कविताएँ’ हिंदी कविता में मृत्यु-चिंतन को नया आयाम देने वाली महत्त्वपूर्ण कृति है। यह संग्रह मृत्यु का उदात्त अभिवादन करता है और जीवन के महत्व को और भी गहरा बना देता है। अरुण देव ने निर्भीक होकर मृत्यु जैसे विषय को अपनाया है और उसे कविता के माध्यम से मानवीय अनुभव का अभिन्न अंग बना दिया है। ये ‘मृत्यु : कविताएँ’ न केवल हिंदी साहित्य के लिए, बल्कि विश्वकविता के परिप्रेक्ष्य में भी महत्त्वपूर्ण है। यह संग्रह मृत्यु और जीवन के सहजीवन की ऐसी गाथा कहता है, जो हमें हमारे अपने भीतर झाँकने और अपनी नश्वरता को पहचानने का साहस देता है। यही किसी भी बड़े कवि का काम है और अरुण देव ने इसे पूरा किया है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
