कथा-कला-कलाकारों के साथ रचनात्मकता के संसार में प्रवेश
 रहमान
18 फरवरी 2025
रहमान
18 फरवरी 2025
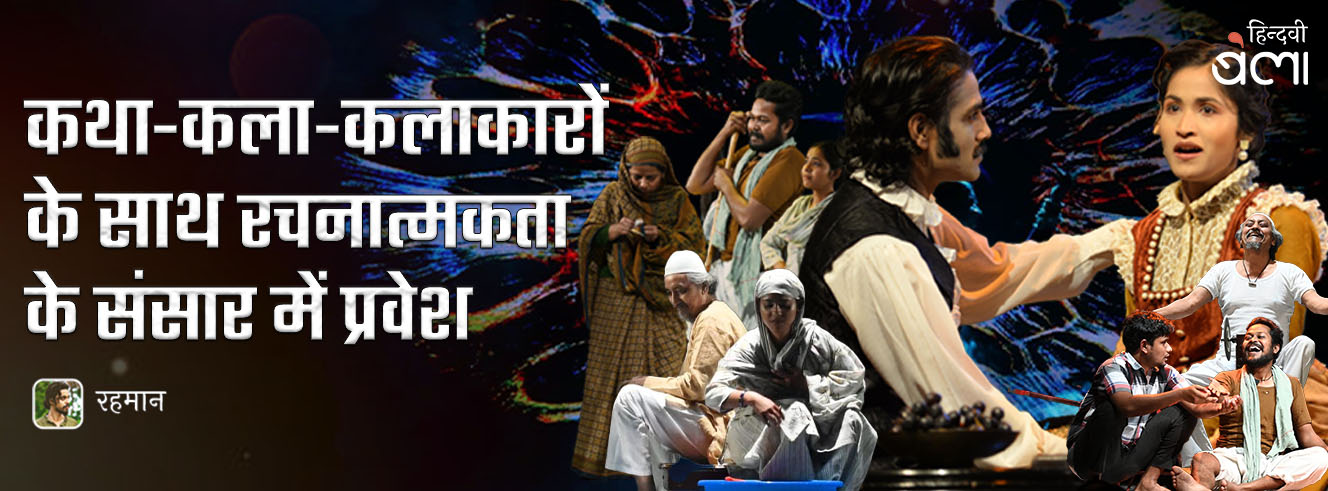
भारत रंग महोत्सव—अभिमंच सभागार में, ऋषिकेश सुलभ के उपन्यास ‘दातापीर’ पर आधारित, कृष्ण समृद्धि द्वारा नाट्यान्तरित और रणधीर कुमार द्वारा निर्देशित नाटक ‘स्मॉल टाउन ज़िंदगी’ रागा पटना के कलाकारों द्वारा खेला गया।
यह नाटक दर्शकों को एक छोटे से शहर में बसे विश्वास, अस्तित्व और मानवीय स्थिति के समृद्ध ताने-बाने में डुबो देता है। ऋषिकेश सुलभ की कथा, कुशलतापूर्वक छोटे शहर के अस्तित्व, विश्वास की ताक़त और कठिनाई का सामना करने वालों की स्थायी भावना का एक विशद चित्रण तैयार करते हुए उन व्यक्तियों के जीवन को आपस में जोड़ती है, जो गूढ़ दाता पीर से सांत्वना चाहते हैं।
नाटक के केंद्र में रशीदन का संघर्ष है जो कथा को समृद्ध करता है, जो उसके काम क़ब्र-खुदाई से जुड़े सामाजिक कलंक के ख़िलाफ़ उसकी अथक लड़ाई को चित्रित करता है। उसकी बेटी, अमीना, इस संघर्ष को प्रतिबिंबित करती है, जो एक ऐसे चक्र में फँस गई है जो निकल भागने के प्रयासों के बावजूद अटूट लगता है। नाटक उसकी आंतरिक दुनिया की एक झलक पाने का अवसर देता है और सांत्वना के क्षणभंगुर क्षण प्रदान करते हुए अमीना के दाता पीर के दृष्टिकोण के माध्यम से एक असली, दार्शनिक तत्व को प्रस्तुत करता है।
फ़ज़लू, जिसका जीवन—जीवन की क्रूर सच्चाइयों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। वह कम उम्र से ही शारीरिक परिश्रम, सामाजिक तिरस्कार और अस्तित्वगत प्रतिबिंब के बोझ से जूझते हुए क़ब्र-खुदाई की पारिवारिक परंपरा में फँसा हुआ है। इसके विपरीत, साबिर का जीवन एक अलग रास्ता पकड़ता है। उसी दरिद्र पृष्ठभूमि में से उभरते हुए, साबिर को संगीत के माध्यम से एक राहत मिलती है, पटना की धूल भरी सड़कों से शास्त्रीय शहनाई की दुनिया तक की उसकी यात्रा फ़ज़लू के उदास अस्तित्व के सापेक्ष एक जीवंत विपरीतता है।
यह जुड़ाव इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे भाग्य, अवसर और व्यक्तिगत पसंद किसी की नियति को गढ़ते हैं।
रशीदन और अमीना के समानांतर जीवन के माध्यम से, नाटक व्यवस्थागत दारिद्रय पर नियंत्रण पाने के पीढ़ीगत संघर्ष और इसके द्वारा लगाई गई जाने वाली सीमाओं की पड़ताल करता है।
निर्देशक रणधीर कुमार का निर्देशकीय कौशल पूरे नाटक में बार–बार उभर कर आता है। नाटक के कथानक के अनुरूप सेट, वस्त्र और प्रकाश का संयोजन नाटक को और सुंदर बनाता है, जिसे देखकर दर्शक नम आँखों से यह सोचते हैं कि एक ज़िंदगी और उसके प्रेम, सुख और दुख का एक रूप यह भी है।
अभिनेताओं ने शुरू से लेकर आख़िर तक कहीं भी नाटक को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया है। रशीदन की भूमिका में अंजलि शर्मा का काम हृदयस्पर्शी था। मंच पर उन्हें देखते हुए, कई बार मुझे मेरी माँ और चाचियों का ख़याल आया। वह अकेली मंच पर उन तमाम औरतों के दुःख को बयान कर रही थी, जो जीवन की तमाम झंझावातों के साथ क़ब्र से भी छोटे कमरे में जीने के लिए अभिशप्त हैं। बेटी अमीना और चुन्नी का किरदार प्रियांशी और रौशनी दास निभा रही थीं। जिन्हें देखते हुए आपको यकीन हो जाता है कि आँखों में सपने लिए बेमन से जीती लड़कियों का चेहरा कैसा फ़क सफ़ेद होता है। बेटे फ़जलु के रूप में सौरभ सागर की भरपूर सराहना होनी चाहिए। उन्होंने किरदार के नब्ज़ को आख़िर तक पकड़े रखा।
समद बने आदिल रशीद एक मंजे हुए अभिनेता हैं। यह उन्होंने नाटक में पुनः साबित किया। साफ़ ज़बान और सुंदर संवाद अदायगी उनसे सीखने योग्य है। साबिर , सत्तार और बबलू बने अभिनेता राहुल रवि, सुनील बिहारी व संदेश भी पीछे नहीं रहे। संदेश का प्रेमी रूप दर्शकों को 'स्मॉल टाऊन ज़िंदगी' के सुंदर प्रेम रूप से रूबरू कराता है।
पार्श्व ध्वनि संयोजक और निर्देशक से मेरी निजी शिकायत है। मात्रानुसार हर चीज़ सुंदर लगती है। इस बात को पार्श्व ध्वनि संयोजक को समझना चाहिए। नाटक के साथ जुड़ाव में ख़लल उनकी तेज ध्वनि से बार-बार होता है। निर्देशक महोदय आधे नाटक में अभिनेताओं से यांत्रिक रूप में संवाद क्यों बुलवा रहे थे? यह मेरे लिए उत्सुकता का विषय है।
~
भारत रंग महोत्सव—एसआरसी ऑडिटोरियम में, सपना और वीरेन बसोया द्वारा लिखा गया, साथ ही वीरेन बसोया द्वारा निर्देशित नाटक '7:40 की लेडीज़ स्पेशल' आवारा थिएटर ग्रुप मुंबई के कलाकारों द्वारा खेला गया।
यह नाटक एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति पूजा शर्मा के जीवन कथा पर आधारित है, जिसे जूनियर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वह अपने अद्भुत नृत्य कौशल के लिए लोकप्रिय है। यह कहानी पूजा के लोकप्रिय होने से पहले की अनकही यात्रा है, जिसमें उनके जीवन की तीन महत्त्वपूर्ण जीवन-परिवर्तक घटनाओं का उल्लेख है।
पहली तब होती है, जब उन्हें पता चलता है कि वह दूसरों से अलग हैं। वह एक ग़लत शरीर में पैदा हो गई है क्योंकि वह औरों से भिन्न महसूस करती है।
दूसरी घटना—जब पलास (बचपन का नाम) शारीरिक हिंसा का शिकार होता है, उस भयावह अनुभव से गुज़रने के बाद परिवार और अपना शहर छोड़ने का फ़ैसला कर ख़ुद की तलाश में बॉम्बे पहुँचता है।
तीसरी घटना जीवन को बदलने वाली घटना है, जब उसे अपने नृत्य कौशल और प्रतिभा के लिए स्वीकृति और सम्मान प्राप्त होता है, न कि लिंग के आधार पर, जिसके लिए वह लड़ रही है।
यह ट्रांसजेंडर लोगों के अज्ञात संघर्षों और स्वयं को स्थापित करने की मजबूत कहानी है। समाज, परिवार और बाक़ी जगहों पर लिंग के आधार पर किए जाने वाले भेदभाव का कटु सत्य उजागर करती हुई, यह चकाचौंध और लोकप्रियता के पीछे की उस काले सच पर प्रकाश डालती है, जो पूजा के जीवन का हिस्सा है।
हमारा समाज बहुत-सी बुनियादी बातों के प्रति उदासीन है। उसके उदारवादी ना होने के मूल में रूढ़िवादी विचारधारा है। जो एक समय में समाज ने व्यवस्था के नाम पर गढ़ी थी, लेकिन समय और काल के अनुरूप उसमें मूलभूत परिवर्तन होने चाहिए थे।
नाटक शुरुआत से लेकर अंत तक आपको हँसाता और रुलाता है। पूजा शर्मा की कहानी के माध्यम से हम अपने समाज और स्वयं के उस विकृत रूप से रूबरू होते हैं। जिसे मंच पर घटित होता हुआ देखकर देह सिहर जाता है। हम सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम जाने-अनजाने अभी भी उन्हें अतिरिक्त में गिनते हैं। जबकि वे अतिरिक्त नहीं हैं।
प्रस्तुति में कई ख़ामियाँ थीं, प्रकाश और पार्श्व ध्वनि संयोजक को थोड़ी अधिक तन्मयता से काम करना चाहिए था। बावजूद इसके पूजा शर्मा की वेदना दर्शकों तक स्पष्ट पहुँची। बिना किसी सेट के नाटक को मजबूती से प्रस्तुत करना एक चुनौती है। जिसे हद तक निर्देशक वीरेन भुनाते हैं।
इस कहानी का उद्देश्य समाज को एलजीबीटीक्यू समुदाय के संघर्षों के बारे में जागरूक करना और रूढ़ी मानसिकता को बदलना है ताकि हम सभी लिंगों के लिए सुरक्षित और उचित स्थान बना सके।
~
भारत रंग महोत्सव—एलटीजी ऑडिटोरियम में, जयंत दहलवी द्वारा लिखा गया और ज्योति सवारीकर द्वारा अनूदित नाटक 'पुरुष' आदर्श शर्मा के निर्देशन में, रंगमोहिनी आर्ट एंड वेलफेयर सोसाइटी, भोपाल के कलाकारों द्वारा खेला गया।
मुंबई की मध्यवर्गीय महाराष्ट्रीयन पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक 'पुरुष', नाटककार जयवंत दलवी की लैंगिक गतिशीलता और पुरुष वर्चस्व के ख़िलाफ़ एक महिला की लड़ाई की सशक्त खोज है।
कहानी अंबिका के इर्द-गिर्द घूमती है, जो समानता की एक निडर वकील और जाति व्यवस्था की आलोचक है। निचली जाति के कार्यकर्ता से उसका विवाह सामाजिक मानदंडों के प्रति उसकी अवज्ञा को दर्शाता है।
एक राजनेता के प्रवेश के साथ कहानी एक अंधकारमय मोड़ लेती है, जिससे अंबिका को दर्दनाक अनुभव और सार्वजनिक अपमान का सामना करना पड़ता है। अपनी माँ को खोना और उसका आत्मविश्वास का कम होना एक निम्न बिंदु को दर्शाता है, जिससे अंबिका को पितृसत्ता की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
'पुरुष' अंततः लचीलेपन की कहानी है। अपने अस्तित्व को पुनः प्राप्त करने की दिशा में अंबिका की परिवर्तनकारी यात्रा प्रणालीगत उत्पीड़न को चुनौती देती है, और गहराई से जड़ जमाए हुए मानदंडों पर चिंतन को जन्म देती है। एक नाटक से कहीं अधिक, 'पुरुष' एक कार्रवाई का आह्वान है, जो दर्शकों को सामाजिक अन्याय पर सवाल उठाने और प्रतिकूल परिस्थितियों पर मानवीय भावना की जीत का जश्न मनाने के लिए प्रेरित करता है।
यह नाटक पुरुषों नहीं अपितु पुरुषत्व की उस रूढ़िवादी सोच पर बार–बार कड़ा प्रहार करता है, जो यह कहता है कि स्त्रियों का जन्म महज़, पति को शारीरिक सुख, बच्चे पैदा करने और घर की देखभाल करने के लिए हुआ। स्त्री और पुरुष की जनन प्रक्रिया एक समान है। जब दो लिंगों की उत्पति समान रूप से हुई है, तो एक लिंग विशिष्ट कैसे और कब हो गया? उन दोनों लिंगों को जन्म देने वाली माँ एक स्त्री है। तो पुरुष स्त्री से अधिक बलवान किस रूप में? नाटक के अंत में अंबिका का प्रतिकार पुरुषत्व और पितृसत्ता पर प्रहार है। और सबके लिए एक चेतावनी भी कि स्त्री यदि अपने सबसे कोमलतम रूप में है तो उससे अधिक कोमल और कुछ नहीं, और उसकी कठोरता के सामने पहाड़ भी नज़रें झुकाए खड़ा हो जाएगा।
नाटक में कई ऐसे दृश्य हैं, जिसमें निर्देशक ने प्रतीकात्मक रूप से चीज़ों का इस्तेमाल कर उसे और प्रभावशाली बनाया। गुलाबराव जब अंबिका की अस्मिता पर हाथ डाल रहा होता है तो उसका मुँह अपने चमचे की खादी टोपी से बंद करता है। जिस खादी टोपी को पहनकर अंबिका के पिता जीवनपर्यंत लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहे। इस एक दृश्य में वर्तमान राजनीति परिलक्षित होता है। जिस खादी से बापू ने देश बनाया, वही खादी आज उसे लूट रही है।
सभी अभिनेताओं ने सशक्त अभिनय से कहानी की डोर को आख़िर तक थाम कर रखा। अंबिका बनी अभिनेत्री और उसके माता पिता सहित पति और राजनेता गुलाबराव अपने–अपने किरदार में फब रहे थे। नाटक शुरुआत में आपको गुदगुदाता है और आख़िर में प्रश्नों के साथ छोड़ जाता है कि आख़िर कब तक पुरुष का पुरुषत्व स्त्रियों का हनन करता रहेगा? क़ानून और न्याय एक ही जन्म में कब संभव होगा? हम पुरुष रूप में जन्म लेने भर से कब तक स्वयं को महान कहेंगे?
~
भारत रंग महोत्सव में—अभिमंच सभागार में, पैट्रिक हैमिल्टन द्वारा लिखा गया और शेखर कामत निर्देशित नाटक 'गैस लाइट' राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक छात्रों द्वारा खेला गया।
नाटक की पृष्ठभूमि 1880 के धुँध भरे लंदन में जैक मैनिंगम और उनकी पत्नी बेला के उच्च मध्यम वर्गीय घर की है। बेला स्पष्ट रूप से तनाव में है और उसके दबंग पति (जो अपनी पत्नी के सामने नौकरानियों के साथ छेड़खानी करता है) की कड़ी फटकार मामले को और भी बदतर बना देती है।
बेला के लिए सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात जैक का घर से बिना किसी कारण के ग़ायब हो जाना है। वहीं जैक, बेला को यह समझाने पर आमादा है कि वह पागल हो रही है, यहाँ तक कि उसे यह भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि वह कल्पना कर रही है कि घर में गैस की रोशनी कम हो रही है।
रफ़ नामक एक पुलिस जासूस की उपस्थिति बेला को एहसास कराती है कि जैक उसके उत्पीड़न के लिए ज़िम्मेदार है। रफ़ बताता है कि ऊपर के अपार्टमेंट में कभी एलिस बार्लो रहती थी, जो एक अमीर महिला थी, जिसकी हत्या उसके गहनों के लिए कर दी गई थी। हत्यारा कभी नहीं मिला।
जैक हर रात गहनों की तलाश में फ़्लैट पर जाता है और अपार्टमेंट की गैस लाइट जलाने से बिल्डिंग के बाक़ी हिस्सों में रोशनी कम हो जाती है। कथित तौर पर ख़ाली अपार्टमेंट में उसके क़दमों की आवाज़ बेला को यकीन दिलाती है कि वह कुछ सुन रही है।
मेरियम-वेबस्टर डिक्शनरी ‘गैसलाइटिंग’ शब्द को सामान्यतः समय के साथ किसी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक बदलाव के रूप में परिभाषित करती है, जो पीड़ित को अपने ही विचारों, वास्तविकता की धारणा या यादों की वैधता पर सवाल उठाने का कारण बनती है और सामान्य तौर पर भ्रम, आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान की हानि, किसी की भावनात्मक या मानसिक स्थिरता की अनिश्चितता की ओर ले जाती है।
वर्तमान समय में तक़रीबन हर क्षेत्र में गैसलाइटिंग करना आम बात हो गई है। विशेष कर मानवीय रिश्तों व स्त्री-पुरुष संबंधों में तो इसका चलन अधिक बढ़ गया है। हम यह भूल चुके हैं कि इसका किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। मानवीय रिश्तों सहित हर क्षेत्र में यह बेझिझक किया जा रहा है। नाटक शुरुआत से लेकर अंत तक गैस लाइटिंग और उसके प्रभावों से उत्पन्न परिणाम से होते हुए, उससे बचकर निकलने की एक झलक है। जिसे देखते हुए, हमें ये ख़याल आता है कि जो हम महज़ आनंद, डार्क ह्यूमर या फिर किसी और तरह से बोल अथवा कर रहे हैं। वह कुछ और नहीं गैसलाइटिंग है।
नाटक में अभिनेता, पार्श्व ध्वनि, प्रकाश और सेट सहित निर्देशक की दृष्टि एक लय में बंधी नज़र आती है। मंच पर हो रहे एक सामान्य हलचल का प्रभाव दर्शक पर पड़ रहा हो तो प्रस्तुति अपने मकसद को प्राप्त करती है। नाटक के कथानक से अधिक बेला बनी पूजा प्रियदर्शिनी व जैक बने मनोज वैरागी सहित सभी अभिनेताओं का अभिनय था। जिससे प्रस्तुति एक ही समय में मनोरंजक और प्रभावशाली ढंग से निकल कर आती है। नाटक की सफलता में प्रकाश परिकल्पक की भूमिका अहम थी।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
