भारतीय विज्ञान संस्थान : एक यात्रा, एक दृष्टि
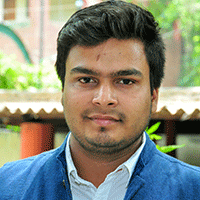 उत्कर्ष पांडेय
12 अप्रैल 2025
उत्कर्ष पांडेय
12 अप्रैल 2025

दिल्ली की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच देश-काल परिवर्तन की तीव्र इच्छा मुझे बेंगलुरु की ओर खींच लाई। राजधानी की ठंडी सुबह में, जब मैंने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा शुरू की, तब मन के एक कोने में यह उद्देश्य था—भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) के उस परिसर को देखना, जिसकी गूँज मैंने वर्षों से किताबों, आलेखों और चर्चाओं में सुनी थी। रास्ते भर मन एक अजीब उत्साह और श्रद्धा से भरा था—जैसे कोई तीर्थयात्री किसी पवित्र स्थान की ओर बढ़ता है। इस यात्रा में समय सीमित था और देखने के लिए बेंगलुरु पैलेस, टीपू सुल्तान का समर पैलेस, नंदी हिल्स और भी बहुत कुछ था, लेकिन इन सबके बीच मैंने आईआईएससी (Indian Institute of Science) को चुना।
इस कैंपस के क़रीब पहुँचते ही वहाँ की हवा में कुछ अलग महसूस हुआ—एक प्रकार की बौद्धिक शांति, एक आत्मीय ऊर्जा जो शहर की तेज़ रफ़्तार के बीच भी IISc के चारों ओर जैसे ठहर जाती है। जब मैंने भारतीय विज्ञान संस्थान के मुख्य द्वार से भीतर क़दम रखा, तो लगा मानो किसी और ही संसार में प्रवेश कर गया हूँ। वह संसार जहाँ विचार जन्म लेते हैं, प्रयोग आकार पाते हैं और भविष्य की परिकल्पनाएँ वर्तमान में रच दी जाती हैं। उस यात्रा ने केवल मेरी आँखों को ही नहीं, बल्कि मेरे अंतर्मन को भी एक नई दृष्टि से भर दिया।
भारतीय विज्ञान संस्थान—सिर्फ़ तीन शब्द नहीं, बल्कि एक विचार है, एक स्वप्न है, एक ऐसी चुपचाप जलती लौ है, जो भारत के बौद्धिक क्षितिज पर सौ वर्षों से अधिक समय से टिमटिमा रही है। यह एक ऐसा स्थान है—जहाँ समय स्थिर लगता है और जहाँ दीवारें तक सोचती हैं। जब कोई पहली बार बेंगलुरु के उस भाग में प्रवेश करता है, जहाँ यह संस्थान स्थित है, तो शहर की शोरगुल भरी सड़कों से निकलकर एक अलग ही संसार में प्रवेश होता है; एक ऐसी दुनिया जहाँ पेड़ बातें करते हैं, हवा में जिज्ञासा घुली होती है और हर कोना किसी महान् प्रयोग की गवाही देता लगता है।
IISc (Indian Institute of Science) की कहानी साधारण इतिहास नहीं है। यह उस समय की बात है, जब भारत पर औपनिवेशिक शासन था, जब विज्ञान और तकनीक जैसे शब्द आम जनमानस के जीवन का हिस्सा नहीं थे; लेकिन एक व्यक्ति—जमशेदजी टाटा—उस समय भी भविष्य देख रहे थे। एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर रहे थे, जहाँ भारत वैज्ञानिक रूप से आत्मनिर्भर हो, जहाँ ज्ञान की साधना हो और नवाचार का बीज बोया जाए। उन्होंने इस विचार को लेकर जब ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया, तब बहुत लोगों ने इसे एक दिवास्वप्न कहा; लेकिन दिवास्वप्न भी यदि सच्ची नीयत और गहरी दृष्टि से देखा जाए तो वह यथार्थ बन जाता है—और यही हुआ। मैसूर के तत्कालीन महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने न केवल इस विचार को समर्थन दिया, बल्कि भूमि और आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस सहयोग से 1909 में IISc की नींव पड़ी और भारत को मिला अपना पहला महान् शोध संस्थान।
इस संस्थान की आत्मा सिर्फ़ उसकी इमारतों या पाठ्यक्रमों में नहीं बसती, वह तो उन अनगिनत छात्रों, प्रोफ़ेसरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों में जीवित है, जिन्होंने वर्षों तक यहाँ रुककर विज्ञान की दुनिया को नई दिशा दी। एक शुद्ध वैज्ञानिक वातावरण में साँस लेना एक विलक्षण अनुभव है। सुबह की ठंडी हवा, पुराने समय की लाल पत्थरों से बनी प्रयोगशालाएँ, वृक्षों की छाया में चलती धीमी बातचीत—यह सब एक साहित्यिक पृष्ठभूमि जैसा लगता है, जहाँ वैज्ञानिक रचनात्मकता एक कविता बनकर बहती है।
यह संस्थान समय के साथ बदलता गया, लेकिन इसकी आत्मा-नींव में वही रहा—ज्ञान और अनुसंधान। यहाँ भौतिकी, रसायन, जैविक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिज़ाइन और अब नीति जैसे विषयों में शोध होता है, लेकिन इन विषयों की सीमाओं के पार भी कुछ चलता रहता है—एक गहन मानवीय खोज। यह केवल शोध-पत्रों का केंद्र नहीं, बल्कि एक विचारशाला है, जहाँ भारत के लिए सोचा जाता है, जहाँ मानवता के कल्याण के लिए प्रयोग होते हैं।
IISc की प्रसिद्धि केवल भारत तक सीमित नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसे विज्ञान के क्षेत्र में भारत की पहचान के रूप में देखा जाता है। जब इस संस्थान के वैज्ञानिक कोई शोध प्रकाशित करते हैं, तो वह दुनिया भर में पढ़ा जाता है। यहाँ से निकले वैज्ञानिकों ने न केवल भारत की संस्थाओं में, बल्कि विश्व के बड़े विश्वविद्यालयों और अनुसंधान केंद्रों में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया है। वे जहाँ भी गए, अपने साथ एक भारतीय वैज्ञानिक परंपरा लेकर गए—जो केवल ज्ञान की नहीं, नैतिकता, परिश्रम और सामाजिक उत्तरदायित्व की परंपरा है।
भारतीय विज्ञान संस्थान का परिसर किसी तपोवन से कम नहीं। यह केवल इमारतों का समूह नहीं, बल्कि एक जीवंत इकाई है, जो हर पल धड़कती है, साँस लेती है, सोचती है। बेंगलुरु के हरे-भरे वातावरण में फैला यह परिसर एक आत्मीय शांति से भरा होता है। यहाँ की सड़कें वृक्षों से घिरी हुई हैं, और दिनभर पक्षियों की चहचहाहट किसी गूढ़ संगीत की तरह सुनाई देती है। जब सूरज की पहली किरण पुराने भवनों की दीवारों से टकराती है, तो ऐसा लगता है जैसे ज्ञान स्वयं अपने हाथों से प्रकाश फैला रहा हो।
यहाँ जीवन का हर पहलू अनुसंधान के इर्द-गिर्द घूमता है। एक शोधकर्ता की दिनचर्या किसी आम व्यक्ति से बिल्कुल भिन्न होती है। सुबह की ताज़गी में वह किसी पुराने विचार को नए रूप में समझने की कोशिश करता है। दुपहर की गहरी शांति में वह किसी जटिल समीकरण से जूझता है, और रात की ख़ामोशी में वह अपनी डायरी में कुछ ऐसा लिखता है, जिसे केवल वही समझ सकता है—जिसने प्रयोगशालाओं में घंटे बिताए हों, असफलताओं को स्वीकार किया हो और फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी हो।
IISc में केवल विज्ञान नहीं पढ़ाया जाता, यहाँ सोचने की स्वतंत्रता दी जाती है। यहाँ की लाइब्रेरी, जिसे ‘जे.आर.डी. टाटा मेमोरियल लाइब्रेरी’ कहा जाता है—केवल पुस्तकों का भंडार नहीं, बल्कि समय का संग्रहालय है। वहाँ रखी किताबें और शोध-पत्र केवल ज्ञान के स्रोत नहीं, बल्कि वे पगचिह्न हैं जिन पर चलकर आज के शोधकर्ता नए रास्ते तलाशते हैं। किसी शांत दुपहर वहाँ बैठकर किसी पुराने वैज्ञानिक के लिखे हुए पत्रों को पढ़ना एक अनोखा अनुभव है, जैसे समय स्वयं आपको अपनी गोद में लेकर कहानियाँ सुना रहा हो।
लेकिन केवल सुविधाएँ और संसाधन ही किसी संस्थान को महान् नहीं बनाते, जो बात IISc को विशेष बनाती है, वह है—यहाँ की शोध की संस्कृति, संवाद और प्रश्न करने की संस्कृति। यहाँ एक विद्यार्थी को सिखाया नहीं जाता, बल्कि उसे प्रेरित किया जाता है, कि वह स्वयं प्रश्न पूछे, स्वयं उत्तर खोजे, स्वयं ग़लतियाँ करे और उन्हीं ग़लतियों से कुछ नया सीखे। यहाँ प्रयोगशालाओं में केवल उपकरण नहीं चलते, यहाँ विचारों की रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, और कई बार एक क्षण में जन्मा विचार वर्षों की मेहनत को नया आयाम दे देता है।
संस्थान ने कई ऐसे वैज्ञानिक दिए हैं, जिनके बिना भारत की वैज्ञानिक यात्रा अधूरी होती। होमी भाभा, सी.वी. रमन, सतीश धवन, के.एस. कृष्णन जैसे नाम केवल व्यक्ति नहीं, बल्कि युग हैं। इन वैज्ञानिकों ने न केवल शोध किया, बल्कि संस्थान और राष्ट्र दोनों के निर्माण में भूमिका निभाई। डॉ. सी.वी. रमन ने यहीं कार्य करते हुए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, और उनकी यह यात्रा हर उस छात्र के लिए प्रेरणा है, जो कभी इसी संस्थान की प्रयोगशाला में अपने पहले प्रयोग के लिए काँपते हुए हाथ से कोई यंत्र उठाता है।
इस संस्थान ने भारत को केवल वैज्ञानिक नहीं दिए, बल्कि नेतृत्व भी दिया। सतीश धवन ने जहाँ अंतरिक्ष अनुसंधान को नया आयाम दिया, वहीं रघुनाथ माशेलकर जैसे वैज्ञानिकों ने नवाचार और औद्योगिक अनुसंधान में क्रांति लाई। यह संस्थान आज भी भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है। विज्ञान केवल प्रयोगशालाओं में सीमित नहीं रहता, वह जब समाज की समस्याओं से जुड़ता है, तभी उसका असली स्वरूप प्रकट होता है और IISc इसी दर्शन पर कार्य करता है।
हर महान् संस्था को समय-समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और IISc भी इससे अछूता नहीं रहा। एक ओर जहाँ इसकी प्रतिष्ठा दिन-ब-दिन बढ़ती रही है, वहीं दूसरी ओर बदलते समय और वैश्विक तकनीकी परिदृश्य ने इसके सामने नए प्रश्न रखे। जैसे-जैसे विज्ञान की धाराएँ जटिल होती गईं, संस्थान को अपने पाठ्यक्रम, शोध पद्धतियों और संरचनाओं में परिवर्तन लाना पड़ा। लेकिन यह परिवर्तन एक सहज आत्मसात की प्रक्रिया की तरह था—बिना अपनी आत्मा को बदले, बाहरी रूप को नया रूप देना।
IISc के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह रही है कि वह अपनी परंपरा और नवीनता के बीच संतुलन बनाए रखे। यह संस्थान सदैव अपने मूल्यों—गहराई, गंभीरता और शोध की सच्ची भावना—से समझौता नहीं करता। लेकिन वही मूल्यमूलक शिक्षा जब आज के तेज़ गति वाले टेक्नोलॉजी-प्रेरित विश्व से टकराती है, तो कई बार सवाल उठते हैं कि क्या यह संस्थान पर्याप्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? पर सच्चाई यह है कि धीमी गति से चलने वाली नदी ही सबसे गहरी होती है। IISc की गति भले ही सतह पर धीमी दिखे, लेकिन उसकी गहराई आज भी अपार है।
आज जब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, जैव सूचना विज्ञान और अक्षय ऊर्जा जैसे विषयों में पूरी दुनिया में तीव्र शोध हो रहा है, IISc भी इन सभी क्षेत्रों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यहाँ के वैज्ञानिक न केवल वैश्विक शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो रहे हैं, बल्कि नई तकनीकों का विकास कर रहे हैं, जो भारत की आवश्यकताओं के अनुकूल हों। एक उदाहरण के रूप में, हाल ही में संस्थान ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाली जल शुद्धिकरण तकनीक विकसित की, जो विज्ञान के साथ-साथ सामाजिक ज़िम्मेदारी का भी परिचायक है।
यह संस्थान केवल शहरी भारत के लिए काम नहीं करता, इसकी सोच पूरे भारत के लिए है—उस भारत के लिए जो गाँवों में बसता है, जहाँ तक विज्ञान की रोशनी पहुँचनी अभी बाक़ी है। IISc की कई परियोजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी हैं, जो सीधे आम जनता को प्रभावित करती हैं। यही वह दृष्टि है जो इसे केवल एक अकादमिक संस्था नहीं, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन का साधन बनाती है।
इस संस्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह केवल वर्तमान में नहीं जीता। यह भविष्य को देखता है—उस भारत को जिसे हम अभी कल्पना में देखते हैं। यहाँ शोध करने वाले छात्र न केवल किसी तकनीक को बेहतर बनाना चाहते हैं, बल्कि वे उस तकनीक के नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों पर भी विचार करते हैं। एक शोधकर्ता जब यहाँ से निकलता है, तो वह केवल एक विशेषज्ञ नहीं होता, वह एक विचारशील नागरिक होता है, जो अपने ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने के लिए करता है।
IISc की प्रयोगशालाओं में केवल यंत्र नहीं चलते, वहाँ सपने आकार लेते हैं—ऐसे सपने जो भारत को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जो हमारे देश की वैज्ञानिक चेतना को मज़बूत करते हैं। यह संस्थान न केवल हमें यह सिखाता है कि कैसे सोचें, बल्कि यह भी सिखाता है कि कैसे सोच को कार्य में बदला जाए। और यही कारण है कि हर वर्ष जब देश के कोने-कोने से युवा इस संस्थान में प्रवेश करते हैं, तो वे केवल छात्र नहीं होते—वे भविष्य के निर्माता होते हैं।
IISc का भविष्य भी उतना ही उज्ज्वल है—जितना उसका इतिहास। आने वाले वर्षों में जब भारत वैश्विक मंच पर एक वैज्ञानिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, तो उस नींव में IISc के प्रयास, सोच और समर्पण की स्पष्ट छाप होगी। यह संस्थान उस भारत का निर्माण कर रहा है, जो न केवल तकनीकी रूप से सशक्त होगा, बल्कि संवेदनशील और उत्तरदायी भी होगा।
आज जब कोई युवा शोधकर्ता इस संस्थान के प्रवेश द्वार से भीतर आता है, तो वह केवल एक डिग्री की तलाश में नहीं आता, वह अपने भीतर के उस जिज्ञासु बच्चे को जीवित रखने आता है, जिसने कभी तारों की ओर देखकर सवाल किए थे, जिसने कभी नदी के पानी में रसायन की परतें देखी थीं, जिसने कभी मशीनों की ध्वनि में संगीत महसूस किया था। वह यहाँ आता है क्योंकि उसे लगता है कि यहीं वह अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकेगा—या शायद और भी बेहतर, नए प्रश्न गढ़ सकेगा।
भारतीय विज्ञान संस्थान केवल एक संस्थान नहीं, एक तीर्थ है—विज्ञान का, विचार का, और सबसे बढ़कर, उस निरंतर जिज्ञासा का जो मानव को पशु से मनुष्य बनाती है। इसकी ईंटों में श्रम की गंध है, इसके पेड़ों की छाया में स्वप्न पलते हैं, और इसकी ख़ामोश दीवारें उन असंख्य रातों की साक्षी हैं, जब किसी शोधकर्ता ने नींद त्यागकर देश और मानवता के लिए एक नया विचार खोजा। इस संस्थान का हर पत्थर समय के साथ एक कथा बन गया है—कभी रमन की, कभी धवन की, तो कभी किसी ऐसे अनाम छात्र की जिसने अपनी चुप साधना में किसी समस्या का हल ढूँढ़ निकाला।
IISc की महानता इस बात में नहीं है कि यहाँ कितने नोबेल पुरस्कार विजेता पढ़े या पढ़ाए हैं, बल्कि इस बात में है कि इसने कितनों को उनकी जिज्ञासा के साथ जीने का साहस दिया। इसने कितनों को वह मंच दिया, जहाँ वे अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकें, चाहे वे विचार कितने भी अपारंपरिक क्यों न रहे हों। इस संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने “ग़लती करने की स्वतंत्रता” दी और यही वह गुण है जो किसी भी रचनात्मक समाज की आधारशिला होता है।
जब हम भारत की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब हम विज्ञान आधारित विकास की कल्पना करते हैं, जब हम नवाचार को संस्कृति में बदलने की बात करते हैं—तो उस हर कल्पना के केंद्र में कहीं-न-कहीं IISc की भूमिका होती है। वह भूमिका जो प्रत्यक्ष भले ही न दिखे, लेकिन अंत:सलिला की तरह बहती रहती है—हर प्रयोगशाला, हर कक्षा, हर विचार-विमर्श में।
इस संस्थान ने यह सिद्ध कर दिया है कि उत्कृष्टता कोई तात्कालिक घटना नहीं होती, वह एक निरंतर प्रक्रिया होती है—जिसमें धैर्य होता है, साधना होती है, और सबसे ज़रूरी, एक उद्देश्य होता है जो स्वयं से बड़ा हो। जब कोई छात्र यहाँ से निकलता है, तो वह अपने साथ सिर्फ़ एक डिग्री नहीं ले जाता—वह एक दृष्टिकोण, एक दायित्व, और एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता लेकर जाता है—कि वह अपने ज्ञान का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उस समाज के लिए करेगा, जिसने उसे यह अवसर दिया।
आज जब हम एक तेज़ी से बदलती दुनिया में खड़े हैं, जहाँ तकनीक और मानवीय मूल्य एक अजीब टकराव में हैं, IISc एक ऐसे संतुलन की तरह उभरता है, जो ज्ञान और करुणा दोनों को साथ लेकर चलता है। यह संस्थान हमें सिखाता है कि विज्ञान केवल तथ्यों का संकलन नहीं, बल्कि एक दृष्टि है—एक ऐसी दृष्टि जो अंधकार में भी आशा का स्रोत बन सके।
और अंत में, जब हम भविष्य की ओर देखते हैं—एक ऐसे भारत की कल्पना करते हैं जो विश्वगुरु हो, नवाचार का अग्रदूत हो, और मानवता का मार्गदर्शक हो—तो हमें उस रास्ते पर IISc की छाया स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि यह छाया केवल एक संस्थान की नहीं, एक विचार की है—एक ऐसे विचार की जिसने कभी एक स्वप्नदृष्टा उद्योगपति के मन में जन्म लिया था और आज करोड़ों भारतीयों की चेतना का हिस्सा बन गया है।
इसलिए जब भी अगली बार आप IISc के परिसर से गुज़रें, तो वहाँ की हवा को एक बार साँसों में भरिए। वहाँ की मिट्टी को एक बार स्पर्श कीजिए। शायद आप महसूस करें कि वहाँ कुछ है—जो अनकहा है, अलिखित है, परंतु अत्यंत सजीव है। वह ‘कुछ’ ही IISc है—हमारे वैज्ञानिक स्वप्नों की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
