'मैं एक सतत अलक्षित अवाँगार्द हूँ'
 हिन्दवी डेस्क
06 जुलाई 2024
हिन्दवी डेस्क
06 जुलाई 2024
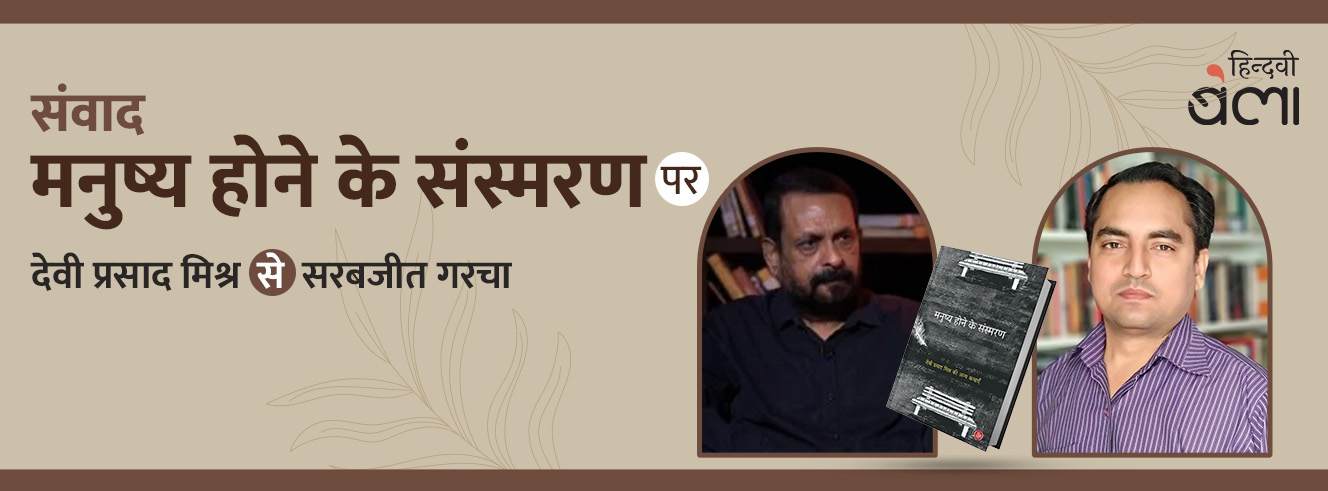
सुख्यात कवि-कथाकार देवी प्रसाद मिश्र की किताब मनुष्य होने के संस्मरण हाल के दिनों में चर्चा में रही है। इस पुस्तक की अन्य कथाओं पर यहाँ उनसे एक बातचीत की है—सरबजीत गरचा ने जो अँग्रेज़ी भाषा के जाने-माने कवि-अनुवादक हैं।
सरबजीत गरचा : कथाओं के अन्यत्व पर इतना ज़ोर क्यों? अपनी प्रस्तावना में आपने इन्हें कवितात्मक कथाएँ और कथात्मक कविताएँ भी कहा है। किताब की कई कहानियाँ फ़्लैश फ़िक्शन के दायरे में भी फ़िट होती दिखाई देती हैं, लेकिन फिर भी आप उन्हें फ़्लैश फ़िक्शन नहीं मानते। क्यों?
देवी प्रसाद मिश्र : कथाओं के अन्यत्व पर ज़ोर देने की कोई व्यवस्थित योजना नहीं थी। मैं जो लिख रहा था वह किसी फ़ार्मैट या संरचना या प्रविधि में फ़िट नहीं हो रहा था। न वह कविता थी और न परंपरागत कहानी। और जैसा कि मैंने किताब की भूमिका में कहा है कि वह लघु कथा का सरलीकरण तो बिल्कुल नहीं थी। तो जो कुछ हुआ वह आवयविक तौर पर विकसित हुआ। इस तरह कवितात्मक कथाएँ और कथात्मक कविताएँ बनने लगीं। बिखरना इनकी ख़ूबी है। आप अच्छा सवाल करते हैं कि फ्लैश फ़िक्शन ये क्यों नहीं हैं? बुनियादी बात तो यह है कि हम अपनी वैधताओं के लिए पश्चिम के प्रतिमानों का मापक लेकर क्यों बैठ जाएँ। यह भी है कि पश्चिम के फ्लैश फ़िक्शन का उत्स काफ़्का के अवधारणात्मक अनुच्छेद हैं जबकि अन्य कथाओं में मेटाफ़िज़िकल पंचतंत्रीयता है। विवरण कथा होने की लालसा से भरे हैं। आप पूछते हैं—कथाओं के अन्यत्व पर इतना ज़ोर क्यों? मैं कहता रहा हूँ कि अन्य वह है जो मुख्य और प्रमुख नहीं है, लेकिन प्रखर होने से उसे रोका नहीं जा सकता। वह सबसे पीछे की बेंच से से की गई हूटिंग है—असहमति की प्रविधि। जो चला आ रहा है उसको मैं चुनौती देता रहता हूँ। सबवर्जन—तोड़फोड़ मेरे स्वभाव में है। मैं एक सतत अलक्षित अवाँगार्द हूँ। सतत विपक्ष। अब विपक्ष ही कला-पक्ष है।
मेरी परिकल्पना के अन्य और वैकल्पिक की मेरी परिकल्पना कहीं एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। मेरी कविता ‘जिधर कुछ नहीं’ में भी ये आग्रह अलक्षित नहीं रह जाते।
सरबजीत गरचा : अपनी लंबी कविता ‘जिधर कुछ नहीं’ में आप एनसायक्लोपीडिक-बृहत्-हैं और मनुष्य होने के संस्मरण में मिनिमलिस्ट! एक रचनाकार में ये ध्रुवांतताएँ?
देवी प्रसाद मिश्र : रचना में कोई फ़ॉर्मूला चलता नहीं। कह लीजिए कि रचना पूर्व निर्धारित का सबवर्जन करती है। आपका सोचा हुआ धरा रह जाता है। क्रिएटिविटी की इस आकस्मिकता के सामने सिर झुकाना पड़ता है। जो इसके विरुद्ध जाते हैं, वे रचना में फ़ॉर्मूला की आत्महीनता को संपोषित करते हैं। वस्तु शिल्प की माँग करती है और शिल्प रिसीविंग एंड पर होगा—यह किसने कहा। तो जो ज़्यादा बड़ा सच है, वह है एक द्वंद्वात्मक अवस्थिति का निर्माण। शिल्प वस्तु में परिवर्तन के जो आग्रह करता है, उस पर कम बातचीत हुई है। उसे निरा रूपवाद कहकर टाला नहीं जा सकता। मैं देख रहा हूँ कि रूप और प्रविधि अंतर्वस्तु में आलोड़न और विकलता भर रहे हैं, उसे वक्र और संस्तरीय बनाते जा रहे हैं।
सरबजीत गरचा : इन कहानियों की घड़ी की सुइयाँ जाने-पहचाने समय से धीरे चलती हैं। एक नीम अँधेरा फैला हुआ है, जो किताब से बाहर आता हुआ महसूस होता है। यद्यपि रोशनी का उल्लेख भी है, लेकिन आप जो दिक्-काल दिखा रहे हैं, वह अँधेरे से बुना हुआ क्यों लगता है?
देवी प्रसाद मिश्र : सारी कहानियों में आप समय के बीतने के धीमेपन और अँधेरे के रंग को देख पाए तो शायद इसलिए कि आपकी संवेदना एक बेहतरीन कवि की है। घड़ी की सुइयाँ बहुत धीमी हैं, क्योंकि चेतना का उठान बहुत शिथिल है। प्रतिगामिता के दौर में समय ठहरा हुआ लगेगा—पराभव-बोध का अँधेरा छाया जो है। लेकिन तब मुक्तिबोध के काम की याद आती है जिनकी कहानियों में अँधेरा हटता नहीं, लेकिन अँधेरे पर बातचीत भी ख़त्म नहीं होती। और कौन नहीं मानता कि वह युगांतरकारी संवाद है। अन्य कथाएँ अँधेरे कोने की फुसफुसाहट हैं जिनमें संवेदना के रास्ते पर चलकर विवेक की कौंध दिख सकती है और फ़ेबल की अतिरंजनाओं में यथार्थ की निहंगता।
सरबजीत गरचा : आपने सारे किरदारों और जगहों को अनाम रखा है। एक जगह धारवाड़ का उल्लेख ज़रूर है, और दो जगह ऋत्विक घटक का भी; लेकिन केवल संवाद में। लगभग सभी घटनाएँ क़स्बों या महानगरों के हाशिए में स्थित गली-मोहल्लों, सस्ते होटलों, कोठरियों, थिएटरों, ख़स्ता-हाल इमारतों या उजाड़ रेलवे स्टेशनों में घटती हैं। अनाम और त्यक्त के प्रति अपने इस ऑब्सेशन के बारे में बताएँ।
देवी प्रसाद मिश्र : जिन भू-भागों का आप ज़िक्र कर रहे हैं, वे इस पृ्थ्वी का अन्य हैं। ठीक कह रहे हैं आप कि वे अनाम और त्यक्त हैं। वे साभ्यतिक लैंडस्केप से लगभग बहिष्कृत हैं। वे वैचारिक अपारथाइड का शिकार हैं। सरब बाबू, आपने कितनी सूक्ष्मता से इस किताब को पढ़ा है; यह पता लग रहा है। आपने ही बताया कि आपने इसे तीन बार पढ़ा। यह सर्वनामों के ज़रिए लिखी गई किताब है। सर्वनाम मनुष्य की बुनियादी पहचान है। मैं, तुम, वह—में पूरी सृष्टि समाहित है। नाम बाद में आता है। नाम आता है तो अपने साथ पूर्वग्रह भी लाता है। लेकिन मैं सर्वनामों में किताब को लिख ले जाऊँ, ऐसा कोई फ़ैसला मैंने नहीं किया था। तो जो हुआ वह आयोजित था जो यह भ्रम दे सकता है कि मैंने इसको लेकर कोई पूर्व निर्णय किया था। बीसियों सालों में लिखी गई कथाओं में अगर इस तरह की कोई अंत:सूत्रता मिलती है तो समझ लेना चाहिए कि कोई मूलगामी अवधारणा है जो कथाओं की मूल प्रेरणा है। यह मूलगामिता है मनुष्य को इसकी निचाटता में पाने की यत्नशीलता। सर्वनाम मनुष्यता का सारतत्त्व जान पड़ते हैं। मैं, तुम, वह—में पूरी सृष्टि समाहित हो सकती है; लेकिन इस तरह से किसी सारतत्त्ववाद या छूँछ दार्शनिकता का निर्माण नहीं किया गया है, बल्कि लोगों को उनके स्वायत्त व्यक्तित्व में विवृत किया गया है। इस तरह मनुष्यता की कोई मोनोलिथ नहीं, बल्कि गहरी लोकतांत्रिक और विविध छवियाँ सामने आती हैं। वे विखंडितों का रक्तपात हैं। इसीलिए यहाँ स्त्री के कितने ही शेड्स मिलेंगे और वे सभी विचलित करने वाले हैं, क्योंकि वे भारतीय विपत्तियों के बीचोबीच हैं।
सरबजीत गरचा : इन कहानियों में समाज की क्रूरता और कुरूपता के कई दृश्य हैं जिनमें पीड़ितों की बेचारगी और चुप्पी घुली है। इनके बरअक्स प्रेम, आशा, आस्था और कोमलता के भी दृश्य हैं; लेकिन इन सब पर दुख की बारिश के छींटें हैं। एक कहानी में एक पात्र बुद्ध की वह बात भी याद करता है कि दुनिया में दुख वैसे ही व्याप्त है, जैसे समुद्र में नमक। क्या यह बात आपकी कहानियों पर भी लागू होती है?
देवी प्रसाद मिश्र : इन कहानियों में दुख व्याप्त है। अधीनता भी इन कहानियों की अंतर्वस्तु है और दासत्व भी। भारतीय लोकतंत्र का जो बहुत हल्ला मचाते हैं, वे देखें कि यह लोकतंत्र विफल है। आधिपत्य और अधीनता में बँटा यह समाज प्रसन्न लोकतंत्र नहीं हो सकता। बुद्ध ने जो बात अपने समय के बारे में कही थी, वह दुख का वातावरण ख़त्म नहीं हो रहा। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा बताया था। हिंस्त्र लालसा। यह लालसा ही बटोरने का प्रणोदक है। यही है जो विषमता और हिंसा को जन्म देती है और जो अधिसंख्य के दुख का कारण बनती है। इस संतप्त समाज को वर्णित करते हुए आप बहुत आशावादी नहीं हो सकते। लेकिन यह दुख दुखवाद की नियति नहीं हो सकता। जनक्षेत्र को रणक्षेत्र में बदलने की ऐतिहासिक अनिवार्यता से इनकार नहीं किया जा सकता।
सरबजीत गरचा : एक कहानी है, ‘दो कवियों को मार देने या उनके आत्महंता होने का मामला’, जिसमें डार्क ह्यूमर का प्रभावशाली इस्तेमाल करते हुए समकालीन कविता-परिदृश्य और कवि-जीवन पर कुछ रोचक टिप्पणियाँ की गई हैं। उसी में एक यादगार वाक्य भी है : ‘‘यह छोटी-छोटी इलाक़ाई असहमतियों का युग है।’’ ये असहमतियाँ क्या हैं, और क्या इन्हें सहमतियों में तब्दील किया जा सकता है?
देवी प्रसाद मिश्र : पटना में एक काव्य-पाठ हुआ। वहाँ मैं एक कवि के साथ एक गेस्ट हाउस में ठहरा। हम लोग बहुत सारी बातें करते रहे। तो यह थी इस कहानी की उत्प्रेरणा। लेकिन इस कहानी में लिखी बातें वही नहीं थीं जो उस कक्ष में हुईं। वे कुछ और बातें थीं। थीं वे भी साहित्य से संबंधित लेकिन कड़वाहट उनमें नहीं थी। बहरहाल, कहानी पर लौटें तो ये वे असहमतियाँ हैं जो वाद-विवाद और प्रतिवाद की संस्कृति को संभव बनाती हैं। हाल के कुछ सालों में दलित उभार और स्त्री-पक्ष ने अपने मत को बहुत तीव्रता और ललकार के साथ रखा। इसकी जो वैचारिकी निर्मित हुई है उसने सबाल्टर्न विचार को बहुत दूर तक अग्रसारित किया। यह वंचितों की आवाज़ों को केंद्र में लाना था। यह अन्य का अनन्य बनना था कि कोई भी विमर्श दलित, आदिवासी और स्त्री को बाहर रखकर नहीं किया जा सकता। लेकिन असहमति पैथोलॉजिक घृणा से संचालित नहीं हो सकती।
सरबजीत गरचा : हिंदी के गिरोहवाद को लेकर आप बहुत शंकालु रहे हैं।
देवी प्रसाद मिश्र : गिरोहवाद की मुश्किल यह होती है कि वह मनोवाद से संचालित होता है और अपने गिरोह के लिए सर्वानुमतिवाद का छद्म निर्मित करता है और दूसरे को डिलेटिमाइज़ करने का वातावरण बनाता है। इस तरह तर्क का स्थानापन्न प्रतिहिंसा होता है। गिरोहवाद अमूमन बुनियादी लोकतंत्र को भूलकर नात्सियों की तरह व्यवहार करने लगता है। तब गाली-गलौज और पत्थरबाज़ी शुरू हो जाती है। इस तरह तर्क नहीं पत्थर बटोरने पर ज़ोर होता है और दो मुर्दे किसी तीसरे मुर्दे को उठाकर कहते हैं कि यह है समकालीन रचना का मसीहा। यह है आपस में चीज़ों को निर्धारित करने वाला मनोवाद और गिरोहवाद। इसमें इस बात की प्रतीक्षा नहीं है कि इस कविता में है क्या, क्योंकि सब कुछ एक गिरोह को तय करना है। जब एक बात को बहुत दुहराया जाता है तो लोगों को लग सकता है कि इस कविता में कुछ होगा, लेकिन पता यह लगता है कि पौने तीन सौ पेज की किताब में कविता के कंकाल बंद हैं। अच्छी बात यह है कि अब रेडक्शनिस्ट रचना का ज़माना लद गया। ज्ञानात्मक संवेदन और संवेदनात्मक ज्ञान का सम्मिलन नहीं है तो आपकी रचना कूड़ेदान में फेंक दी जाएगी। लेकिन बड़े और जनोन्मुख ऐस्थेटिक्स की जगह गुलेलबाज़ी और हूटिंग नहीं हो सकती। बौद्धिक जोकरई साल डेढ़ साल के बाद थक जाती है। इस ट्रॉलिंग का शिकार मैं रहा हूँ। मेरे मन में लिहाज़ रहा है, लेकिन धुरीहीन ग़ुंडई का करारा, युक्तियुक्त और पोलेमिकल जवाब देने में ही मेरा भरोसा है :
बाहम सुलूक थे उठाते थे नर्म गर्म
काहे को मीर कोई दबे जब बिगड़ गई
सरबजीत गरचा : किताब में ‘काले से ढँका हुआ सफ़ेद’ शीर्षक की एक कहानी है, जिसमें एक अधेड़ आदमी दफ़्तर जाने की बजाय अचानक घर लौट जाता है और वहाँ पत्नी को एक युवा के साथ हमबिस्तर पाता है। वह खिड़की के पास मंत्रमुग्ध-सा खड़ा इस दृश्य को देखता रहता है और इस बात का पूरा ख़याल रखता है कि उस लंबी प्रेम-क्रीड़ा में कोई बाधा न पड़े, क्योंकि—आप ही के शब्दों में—‘‘इससे बेहतर उसने कुछ भी नहीं देखा था।’’ इस दृश्य से सहसा हारुकी मुराकामी की कहानी पर आधारित फ़िल्म ‘ड्राइव माय कार’ के ऐसे ही एक दृश्य की याद ताज़ा हो जाती है।
देवी प्रसाद मिश्र : मैंने इस कहानी को नहीं पढ़ा है। फ़िल्म देखी हाल में। लेकिन उस समय तक मैं कहानी लिख चुका था। दरअस्ल, यह दृश्य उस समाज का दृश्य है जहाँ पुरुषवाची स्वामित्व का निरसन होता है। यह संबंधों की प्रतिसृष्टि निर्मित करना है। यह स्त्री पर एकाधिकारवाद का निषेध है और उसके चयन के अधिकार का उत्सव। यौनिक नैतिकता के दो प्रतिमान नहीं हो सकते। तो यह कहानी नैतिकता के पौरुषेय निर्माण का प्रत्याख्यान है।
सरबजीत गरचा : क्या आपका लेखन फ़िल्मों से प्रभावित है? अगर है, तो किस हद तक?
देवी प्रसाद मिश्र : सोने के पहले मैं एक फ़िल्म देखता हूँ, मोबाइल पर, जो विश्व सिनेमा का हिस्सा हुआ करती है। मैंने फ़िल्म सोसायटी चलाने में अहम भूमिका निभाई इलाहाबाद में। विश्व सिनेमा ने मुझे बचाया। मैंने बहुत सारा सिनेमा देखा है और देख रहा हूँ। जिसको विश्व सिनेमा कहते हैं, वो। तो मैं बिंब और प्रतिबिंब से निर्मित होता गया। मैं कह सकता हूँ कि महान् सिनेमा बेदख़ली का सिनेमा है। मैं डिसलोकेशन की कथाओं से भरता चला गया। इस तरह मेरा अवर्णीकरण, विवर्णीकरण और बेहदीकरण हुआ!!! जो अवचेतन में है वह ज़रूर रचनाओँ में आता होगा। मुझे लॉन्ग टेक अच्छे लगते हैं। इन कहानियों में भी लॉन्ग टेक का उजाड़ है। मेरी स्त्रियाँ विश्व सिनेमा की स्त्रियाँ हैं—स्वतंत्र, स्वच्छंद, ऐंद्रिय और बोहेमियन।
सरबजीत गरचा : आपको इस पुस्तक में चित्र और रेखांकन डालने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? इससे पहले, 2022 में छपी आपकी कविता की किताब ‘जिधर कुछ नहीं’ भी चित्रांकित थी। क्या प्रकाशक और उनके संपादक आसानी से इस बात के लिए तैयार हो गए?
देवी प्रसाद मिश्र : हेम ज्योतिका को मैं काम करते देखता रहता हूँ। मैं डार्क हूँ, वह प्रकाश हैं। बहुत नाज़ुक मौक़ों पर उन्होंने मुझे जीवन दिया। उन्होंने मुझे नष्ट होने से बचाया। मैं कभी प्रफुल्ल नहीं होता, वह कभी ग़मगीन नहीं हो सकतीं। मैं नाउम्मीद रहता हूँ, उनका आशावाद अजेय रहता है। अजीब बात है कि चित्र उनके भी लेकिन डार्क हैं। कथाएँ भी डार्क ही हैं। तो इस तरह एक सिंबियासिस बन गई। हेम का कहना था कि कहानियाँ चित्रात्मक हैं। कहानी के कवर ने तो बहुतों को विचलित किया जिसमें बेंच पर काँटेदार बाड़ रखी है। यानी जो बैठने की जगह है वह यातना की जगह है। जो अनुराग का स्थान है, वह वधस्थल है। इस एक चित्र ने पूरी किताब और कह लीजिए समय को भी परिभाषित कर दिया। अन्य चित्रों ने कहानियों को और विडंबनात्मक बना दिया।
सरबजीत गरचा : आपकी कहानी ‘पेड़ और आदमी’ में पेड़ों को बेइंतहा प्यार करने वाला जो आदमी है, क्या वह पूरी तरह काल्पनिक है, या आप ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं? उसी तरह ‘निम्फ़ो’ शीर्षक की कहानी में छह पुरुषों को छोड़ने वाली सुंदर लड़की को भुला पाना मुश्किल है। इस कहानी की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
देवी प्रसाद मिश्र : ‘पेड़ और आदमी’ का पेड़ों को बेहद प्यार करने वाला आदमी शायद मैं ही हूँ जो भले ही पर्यावरणविद् या ऐक्टिविस्ट जैसा न भी हो तो। यह कहानी पोस्ट ह्युमेनिज़्म का अच्छा उदाहरण है, यद्यपि जब इस कहानी को लिखा तो इसकी दार्शनिकता के बारे में मैं कम ही जानता था। पटपड़गंज की सोसायटी में एक जामुन का पेड़ था जिसके नीचे बच्चे खेला करते थे। तो उस जामुन के पेड़ और बच्चों के लगते जमघट ने इस कहानी को जन्म दिया। इसमें मैं भी एक पात्र बनता गया। सोसायटी के सामने पार्क था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। वहाँ मुझे यह याद आया कि मैंने जब भी छक्का मारने की कोशिश की तो मैं आउट हो गया। तो वह बात भी कहानी में आ गई। दरअस्ल, इस कहानी का बूढ़ा और जवान दोनों मैं ही हूँ—कहानी में हम विभाजित हैं। इस कहानी का जवान आत्म-विच्छिन्न है। बूढ़ा उसकी संपूर्णता है। कक्षा आठ तक मैं फ़ुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी था और हॉकी भी खेलता था। मेरे भीतर का खेल और संगीत कैसे नष्ट हुए, इसका मैं निरुपाय साक्षी हूँ। आज यह कहने का मन हो रहा है कि कविताओं ने इन दोनों चीज़ों का वध किया।
‘निम्फ़ो’ के पात्र को मैंने हाल में जाना। उससे सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी थी। ऐसी उपस्थिति कि जैसे आग को बुझाने की कोशिश की जा रही हो। वह गार्ड रूम में नियुक्त हुई थी। वह बहुत निर्णायक आवाज़ में कहा करती थी कि जिम से निकलिए टाइम हो गया। बहुत कम उम्र में उसके जीवन में छह लोग आ गए थे। न वह अपने सौंदर्य को सँभाल पा रही थी और न उसके संपर्क में आने वाले पुरुषों को। एक दिन मैंने सुना कि उसकी हत्या उस आदमी ने कर दी जिसके साथ वह ब्याही गई थी। मुझे लगा कि मैं यह पहले से जानता था—एक सचमुच स्वतंत्र स्त्री की हत्या होगी ही। मुझे फिर भी नहीं लगता कि केवल एक स्त्री ने इस कहानी को जन्म दिया। इसके पीछे पुर्तगाली फ़िल्मकार अलमदवोर की तमाम फ़िल्में रही होंगी और मोराविया का वह प्रसिद्ध उपन्यास ‘द वुमन ऑफ़ रोम और लार्स वॉन ट्रायर की डिप्रेशन त्रयी—‘एंटी क्राइस्ट’, ‘मेलानकोलिया’ और ‘निम्फ़ोमेनिअक’ की आख़िरी फ़िल्म जो दो भागों में है। इस छोटी-सी कहानी में मेरे जीवन का बहुत कुछ संचित है जो प्रकट होता है। उन रचनाओं में व्यक्त यातना का सत्व इस कहानी में है। ‘निम्फ़ो’ का मायने है—इच्छाओं के अतिरेक से भरी स्त्री। प्रेम की भूखी प्यासी। दुनिया में उसके होने का ऐस्थेटिक्स कितना क्रांतिकारी है, कह नहीं सकता। लेकिन ‘निम्फ़ो’ लिखकर मैं रुक नहीं गया हूँ। मैंने ‘बोहेमियन होने की उदासी’ जैसी कविता लिखी है।
सरबजीत गरचा : किताब में काफ़ी कथाएँ केवल एक वाक्य में ख़त्म हो जाती हैं। क्या उन्हें फ़िल्मों की पटकथा जैसी वन-सेन्टेंस समरी समझा जाए? कहानियों के अनकहे को पाठक कुछ हद तक समझ सकता है, लेकिन अगर यह अनकहा विशाल हो तो उसे कैसे पढ़ना-समझना चाहिए?
देवी प्रसाद मिश्र : एक लाइन वाली कहानियों का संबंध फ़िल्मों के कारोबार से है, जहाँ वन लाइनर की परंपरा है। लेकिन जैसा कि आपने बहुत सूझ के साथ कहा कि उसकी विशाल विस्तारधायिता के लिए पाठक अध्यवसाय करे। यह तो ठीक ही है कि सारे काम लेखक ही क्यों करे! महान् लेखन पाठक को झिंझोड़ता और जागृत करता है। उन्हें इमैनेंट नहीं रहने देता, ट्रांसेडेंट होने के लिए उत्पेरित करता है।
सरबजीत गरचा : कहानी और कविता की किताब में एक बात समान है—कहीं से भी पढ़ना शुरू किया जा सकता है। लेकिन आपकी किताब को पढ़कर लगता है कि आप कहानियों के क्रम के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। क्या आप पाठकों से यह अपेक्षा रखते हैं कि वे आपके बनाए क्रम का ध्यान रखें या जैसे चाहें वैसे पढ़ें?
देवी प्रसाद मिश्र : आपने अगर यह मार्क किया कि इसका क्रम बनाने में बहुत श्रम किया गया है तो यह आपके सूक्ष्म निरीक्षण का कमाल है। ये कथाएँ कथाहीनता से निकलती हैं और कथा बनती हैं। कह लीजिए कि मैं कथाओं को पुनर्परिभाषित करना चाह रहा हूँ। इन कहानियों में आदिमता और आधुनिकता के दो दिल धड़कते हैं। इनमें फ़ेबल की आदिमता है और कहानी की अंतर्दृष्टि की आधुनिकता। मनुष्य के फ़ेल होने का बड़ा आकार वहाँ बनता है। बहरहाल, उसकी जिजीविषा के बड़े दृश्य भी यहाँ मौजूद हैं।
सरबजीत गरचा : एक कहानी का शीर्षक है—‘ये धुआँ’, जिसमें एक पेड़ एक आदमी को ‘कॉमरेड’ कहकर संबोधित करता है। क्या आप यह मानते हैं कि पेड़ लेफ़्टिस्ट होते हैं?
देवी प्रसाद मिश्र : क्या पेड़ लेफ़्टिस्ट होते हैं—यह एक बड़ी कविता की पंक्ति है। लेफ़्टिस्ट पेड़ नहीं होंगे तो कौन होगा! वे हरीतिमा का मेटाफ़र, विचार और यथार्थ हैं। उन्हीं पर औद्योगिक और कारपोरेट पूँजी का सबसे बडा हमला हुआ है। भारत की सबसे प्रामाणिक क्रांति जंगलों को बचाने के लिए लड़ी गई। वह इस बात का प्रतीक था कि मनुष्य के सबसे अच्छे दोस्त पेड़ हैं। उत्तर मनुष्य का दर्शन भी यही बात कह रहा है कि मनुष्य तो फ़ेल हो गया है। वह अपनी मानवीय अस्मिता को पेड़ों के सान्निध्य में जाकर ही पुनर्प्राप्त कर सकता है। पेड़ों के कटने का संगठित प्रतिरोध आदिवासी करते रहे हैं। पेड़ और मनुष्य के इस संबंध को जो विचार प्रगाढ़ बनाता है—वह है मार्क्सवाद। लगे यह कितना ही क्लीशेड, लेकिन हमारी शोषक दुनिया में लेफ़्ट का कोई विकल्प नहीं। पूँजीवादी अमेरिका और यूरोप में अगर कोई वैचारिक परंपरा आगे बढी है तो वह मार्क्सवाद के तत्त्वावधान में ही अग्रसर हुई है। ग्राम्शी, अडोर्नो, हरबर्ट मारक्यूज़, फूको, देरीदा, लाकां, दुलूज़, आलेन बादिऊ—सब मार्क्स से जूझ रहे हैं। इसीलिए अशोक वाजपेयी का भारत भवन वाला काम घड़ी की सुइयों को पीछे करने का काम था। भारत में वाम-विरोध मनुष्य-विरोध है। यह भी कहना पड़ेगा कि आज के अशोक वाजपेयी बहुत बदले हुए हैं। फ़ाशीवाद-विरोध ने उनकी वैचारिक जड़ता को नष्ट करने में बड़ी भूमिका निभाई। हिंदी की आदिवासी, दलित और स्त्री के जानिब से लिखी कविता वाम या वामोन्मुख कविता ही है। इसलिए पेड़ ही नहीं, पूरा अरण्य ही लेफ़्टिस्ट है। नहीं है तो होना चाहिए। जो इसके बाहर हैं, वे कभी वैध नहीं दिखेंगे।
सरबजीत गरचा : मैंने इस समय के महान् नाटककार महेश एलकुंचवार को ‘मनुष्य होने के संस्मरण’ की एक प्रति भेजी थी। उनका जवाब आया : I am reading Devi Prasad Mishra Jee’s ‘मनुष्य होने के संस्मरण’। It is fascinating, both stylistically and content wise. His paucity of expression is amazing. देवी जी, इन कहानियों की जागृत और स्वप्नावस्था की इस भाषा तक आप कैसे पहुँचे?
देवी प्रसाद मिश्र : क्या आप सोचते हैं कि इस सवाल का उत्तर मैं दे सकता हूँ। भाषा को आप चुनते हैं या भाषा आपको चुनती है? मैं कहना यह चाहता हूँ कि लेखन जागृत और स्वप्न के बीच का उनींदापन होता है। इस तरह से देखूँ तो आपने सवाल को बहुत मार्मिक सूझ के साथ फ़्रेम किया है। यह क्रिएटिव ज़ोन है, जहाँ काफ़ी कुछ बस में होता है और काफ़ी कुछ बस में नहीं होता। यहाँ अर्जित किया विज़न काम करता है। तो रचना संचित का अभिप्राय होती है, जहाँ चेतन और अवचेतन की संश्लिष्टता उसे रूप देती है। तब भाषा या शैली को चुनने का सवाल गौण हो जाता है। जाते-जाते मैं असद ज़ैदी की वह टिप्पणी ज़रूर याद करना चाहूँगा जो उन्होंने ‘जलसा’ के संपादक के तौर पर इन कहानियों को छापने के दौरान फ़ोन पर की कि ये कहानियाँ कुछ प्रूव नहीं करना चाहतीं। इस अर्थगर्भ वाक्य को डिकोड करने का टास्क मैं पाठकों पर छोड़ता हूँ।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
