ये day वो day और हाथी
 सुषमा कुमारी
15 मई 2025
सुषमा कुमारी
15 मई 2025
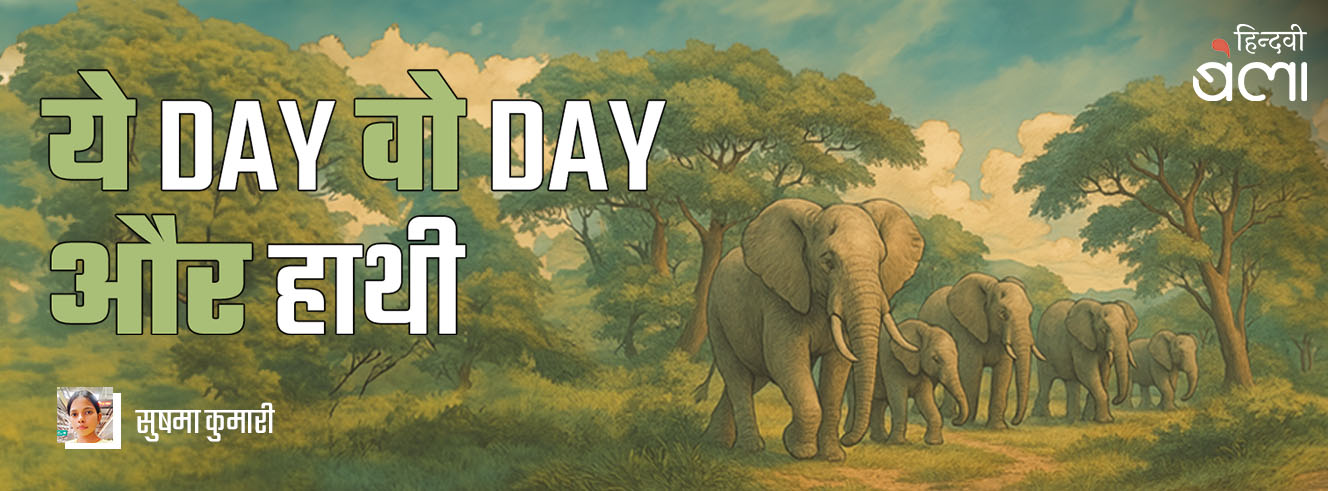
वर्ल्ड अर्थ डे और हाथी का कोई सीधा संबंध नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे ‘वर्ल्ड अर्थ डे’ पर हाथी याद आता है। हाथी का इतिहास संघर्षों की मिट्टी में दबा हुआ है। वह न पूरी तरह से जंगल का हुआ, न ही पूरी तरह से गाँव या शहर का। उसकी बड़ी काया उसकी ताक़त है और कमज़ोरी भी। वह बिगड़ जाए तो दबंग है और अपने में रहने वाला मनजोगी भी। इंसानों के साथ उसका संबंध घनिष्ठ रहा है। हाथी ने जिसके आँगन का पानी पिया उसके लिए युद्ध भी किया है। वर्चस्व की भावनाओं ने इंसानों को उनके जीवन का खलनायक अधिक बनाया है।
मैं छोटी थी। गाँव में किसी की शादी थी। ब्याह खत्म होने के बाद बाक़ी की कुछ रस्मों के लिए सारी औरतें ‘डीह बाबा’ के यहाँ जाने की तैयारी करने लगीं। औरतों की उस टोली में मैंने एक अच्छा-सा फ्राक पहना और दादी के साथ शामिल हो गई। रास्ते भर मेरे ज़ेहन में किसी मंदिर का नक़्शा घूमता रहा। पर जब मैं वहाँ पहुँची तो एक बड़े से वृक्ष के नीचे मिट्टी के हाथी-घोड़े पाए। औरतें गीत गा रही थीं और कुछ रस्में कर रही थीं। फ़ुर्सत में रात को दादी से मैंने पूछा, ‘‘दादी ये डीह बाबा कौन हैं?’’ दादी ने बताया कि डीह बाबा गाँव के देवता हैं। एक तरह से गाँव के रक्षक हैं। हाथी-घोड़े उनकी सवारी हैं। गाँव में कोई भूत-प्रेत हो या आफ़त-बिपत ‘डीह बाबा’ के अनुमति के बिना गाँव में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। उस दिन से वे हाथी-घोड़े मुझे ‘डीह बाबा’ का पर्याय लगने लगे। ‘डीह बाबा’ की शक्ति से मैं बहुत प्रभावित हुई। फिर दादी की बताई बात इस तरह ज़ेहन में बैठी कि आज भी जब किसी यात्रा पर निकलती हूँ और किसी नए स्थान में प्रवेश करती हूँ तो मन ही मन ‘डीह बाबा’ की अनुमति लेकर मंगलमय यात्रा की कामना करती हूँ।
बचपन का एक छोटा दृश्य और याद आ रहा है, जिसमें सुबह-शाम हाथीवान हाथी को हमारे घर के सामने से लेकर आया-जाया करता था। सूरज की पहली किरण के साथ धमक-धमक कर हाथी निकल पड़ता था। छोटे बच्चे चिल्लाते ताली बजाते और कुत्ते दूर से भोंकते हुए उसके आगे-पीछे घूमते रहते। शाम को जब हाथी लौटता तो उसकी पीठ पर ढेर सारा पत्तों का गट्ठर होता। सुंदर और बड़ा हाथी, उसकी सूँड़ पर रंगों से कलात्मक फूल और पत्ते बने रहते। वह किसका हाथी था ठीक से याद नहीं। शायद गाँव के किसी जमींदार का होगा। जिज्ञासा हमेशा यह रहती कि हर सुबह समय निकालकर कौन उस हाथी को कलात्मक रूप से सजाता था। आर्थिक रूप से हाथी के ख़र्चे का वहन करना तो आम आदमी के बस की बात नहीं थी। धीरे-धीरे हाथी की कहानी ज़ेहन से ओझल हो गई। गाँव भी आना-जाना कम हो गया। फिर बाद में किसी ने बताया था कि अब गाँव में हाथी नहीं आता-जाता।
हम शहर में बस चुके थे। शहर बड़ा था और मुहल्ला छोटा। मुहल्ला छोटा इसलिए भी था कि इसमें छोटे-मोटे काम और मेहनत-मज़दूरी करने वाले लोग अधिक थे। ज़्यादातर लोग अपना गाँव-घर छोड़ कर आए थे हमारी तरह। एक दिन हमारे मुहल्ले में सर्कस देखने की होड़ मची, पर मेरे घर से कोई नहीं गया और इस तरह मैं अपने जीवन में कभी भी सर्कस देखने नहीं जा पाई। लोगों ने बताया वहाँ हाथी के करतब भी दिखाया जाता है। सर्कस का हाथी जंगल से आया था या मेरे गाँव से... यह बात उन दिनों मेरे ज़ेहन में घूमती रही। कुछ रोज़ बाद यह ख़बर भी सुनने को मिली थी कि एक बाघ करतब दिखाते वक़्त एक लड़की को मार कर खा गया। सर्कस और बाघ की कहानी कई दिनों तक तरह-तरह से लोगों के बीच घूमती रही।
तीसरी बार और कहें तो कई बार हाथी से फिर मिलना हुआ, अपने ही शहर के चिड़ियाघर में। बाक़ायदा हाथियों को घेराबंदी करके रखा गया था। सुरक्षा के प्रबंध और वहाँ के गार्ड इतने चुस्त थे कि हाथी भागना चाहे भी तो भाग नहीं पाए। जो भी लोग हाथी को देखने जाते, वे दूर से कुछ खाने का सामान फेंक देते; जबकि सामने के बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा होता, जानवरों को खाने की चीजें देना वर्जित है। हाथी खुले में रखे गए थे। कुछ पेड़ों को काट कर उनके अहाते में डाल दिया गया था; जिस पर वे बैठते, खेलते या अपनी देह रगड़ते। धूप-गर्मी, बारिश भी उन तक सीधे पहुँचती जो एकदम उन्हें नेचुरल फ़ीलिंग देती। हाथी के साथ लगभग सभी जानवरों को इसी तरह से रखा गया था। जो अधिक शक्तिशाली या ख़तरनाक लगते उनकी घेराबंदी उतनी ही सशक्त कर दी जाती। फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, चिड़ियाघर का मोह टूट गया।
मैंने एक और जगह हाथी को देखा था—‘म्यूजियम’ में। वहाँ मृत हाथियों और पशुओं के खोल में भूसा भरकर एयर टाइट शीशे में बंद करके रखा गया था। (उनके अंदर भूसा था या कुछ और यह ठीक से पता नहीं है) वहाँ हाथियों के पूर्वजों ‘मैमथ’ का कंकाल भी देखने को मिला। यह मृत हाथियों की उपयोगिता थी और भविष्य के लिए जीवों का संग्रह। यहाँ काँच को तोड़ कर कोई जीव नहीं भाग सकता था। ‘म्यूजियम’ का जादू ऐसा था कि किसी भी जीव की आँखों में ग़ौर से देखिए तो वह आपको जीवित लगेगा।
दीपावली में जब हम मिट्टी के घरौंदे बनाते थे तो बाज़ार से मिट्टी के छोटे-छोटे हाथी-घोड़े और काम करते हुए गुड्डे-गुड़िया ख़रीदते थे। छठ पूजा में आज भी किसी मन्नत के पूरे हो जाने पर औरतें ‘कोशी’ भरती हैं। ‘कोशी’ मिट्टी का छोटा-सा परात होता है; जिसके कोनों पर मिट्टी के छोटे दीये लगे होते हैं, जो हाथी की पीठ पर होता है। इसी में फल-प्रसाद रख, दिया जलाकर औरतें पूजा करती हैं। यानि हाथी किसी न किसी रूप में हमेशा से हमारे आस-पास ही रहा है।
भारतीय सिनेमा और छोटे परदे पर भी हाथी से जुड़ी फ़िल्में और सीरियल बनाए गए, जिनमें 1971 में ‘हाथी मेरे साथी’ जैसी फ़िल्म को बहुत पसंद भी किया गया था। ऐसे ही एक दिन टीवी पर शिव जी का कोई सीरियल चल रहा था, जिसमें भगवान शिव ने क्रोध में आकर बालक गणेश का शिश धड़ से अलग कर दिया था। पार्वती माँ का रोना-बिलखना देख शिव ने अपने सेवकों से एक ऐसे हाथी का शीश लाने का आदेश दिया, जिसकी माँ उसकी तरफ़ पीठ करके सोई हो। आदेश के अनुसार सेवक भी ऐसे शिशु हाथी का सिर ले आए। बालक गणेश को हाथी का सिर लगा कर जीवित कर दिया गया। माँ पार्वती अपने पुत्र को पाकर ख़ुश हो गईं। पर जिस हथिनी का बच्चा लाया गया था, उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया गया। हथिनी के हिस्से में बलिदान आया। उसे यह सोचकर ख़ुश होना है कि उसके पुत्र का शीश अब देवता बन चुका है और लोक में उसकी पूजा होगी। यह प्रलोभन या संतोष का भाव हथिनी के ही हिस्से में क्यों आया? क्या आज भी हाथियों के साथ मनुष्य ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहा?
मेरे प्रिय लेखक विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें हाल ही में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, के एक उपन्यास ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ के नए संस्करण [हिन्द युग्म प्रकाशन, 2023] के आवरण पर एक हाथी का चित्र है; जिसकी पीठ पर दो लोग बैठे हैं। यह आवरण बहुत सुंदर और मनमोहक है। यह आवरण उस समन्वय को भी दर्शाता है, जो एक समय आदमी और हाथी के बीच था। सिर्फ़ हाथी ही क्यों? हमारी सभ्यता और संस्कृति में प्रकृति और जीवों के लिए हमेशा से स्थान रहा है। हमारे स्थापत्य और कला-कर्म इसके सुंदर उदाहरण हैं।
इसी कड़ी में संजीव का उपन्यास ‘रह गईं दिशाएँ इसी पार’ याद आ रहा है। शुरुआत में यह पुस्तक मुझसे बिल्कुल भी पढ़ी नहीं जा रही थी, फिर भी मैंने इसे जारी रखा। जैसे-जैसे उपन्यास आगे बढ़ता गया वैसे-वैसे हताशा बढ़ती गई, कहीं गला सूख गया तो कहीं आँखें बंद हो गईं। समाज का ऐसा जीवंत यथार्थ जिसे स्वीकार करना मेरे लिए कठिन होता जा रहा था। आज सिर्फ़ समय ही नहीं, बल्कि आदमी भी बदला है और आदमी इतनी बुरी तरह बदला है कि उसे पाशविक कहना भी अब सही नहीं लगता। अपनी अतृप्त भौतिक आकांक्षाओं के पीछे वह कैसे ख़ुद को, इस पृथ्वी को और जीवन की नई संभावनाओं को नष्ट करता जा रहा है, इसे इस उपन्यास में देखा जा सकता है।
‘रामायण’, ‘महाभारत’, ‘पंचतंत्र’ या अन्य प्राचीन पुस्तकों में मनुष्य के साथ हमें प्रकृति और पशुओं का समावेश दिखाई पड़ता है। उस समय के लेखकों ने समाज में प्रकृति और पशुओं की सहभागिता को न केवल स्वीकार किया, बल्कि स्थान भी दिया था। हिंदी साहित्य में भी हम प्रेमचंद के यहाँ ‘पूस की रात’, ‘दो बैलों की कथा’ या फिर महादेवी वर्मा के यहाँ ‘गिल्लू’, ‘नीलू’, ‘सोना’ इत्यादि को देख सकते हैं। जगह-जगह कई साहित्यकारों ने उस परंपरा को अपने रचना-संसार में स्थान दिया है। चिंता का विषय यह है कि प्रकृति और पशुओं के साथ समन्वय और संवेदना का भाव आज पुस्तकों तक ही सिमट कर रह गया है।
क्रूरता और हिंसा मनुष्य के नए चेहरे हैं। वह इसी रूप में आज सबसे अधिक जाना जाता है। पर्वत, समुद्र, धरती और आसमान हर कहीं वह अपना वर्चस्व चाहता है। आधुनिक तकनीक मनुष्य के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार साबित हुई है, जिसके सहयोग से वह हर कहीं अपनी मौजूदगी स्थापित कर रहा है। पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों का शोषण और दोहन मनुष्य के लिए एक खेल है। इस खेल में उसने पारंगतता हासिल कर ली है। पृथ्वी का बढ़ता तापमान, आतंकवाद, पर्यावरण की समस्या, वनों का क्षरण, सूखती नदियाँ, प्रदूषित परिवेश, युद्ध... यहाँ तक की पशुओं पर ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से प्रयोग करना सबमें कहीं न कहीं हम मनुष्यों का ही हाथ है। हाथियों के साथ क्या होता आया है और क्या हो रहा है, उससे भी हम भली-भाँति परिचित हैं।
इस प्रवृत्ति के साथ हम जिस दिशा में और जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उससे हम मनुष्य कभी नहीं बन पाएँगे। बंगाल में किसी बंगाली दंपति से पूछिए, ‘‘आप अपने बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हैं? आपका बच्चा पढ़-लिखकर क्या बनेगा?’’ आपको उत्तर मिलेगा हम अपने बच्चे को मनुष्य बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं और वह पढ़-लिखकर सबसे पहले मनुष्य बनेगा। बच्चों को मनुष्य बनाने यह संस्कार बंगालियों को बंगाल के बुद्धिजीवों से मिला है। स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर भी जगह-जगह अपनी रचनाओं में मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखने की बात करते हैं। आज हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं या किसी बड़े पोस्ट पर कोई अधिकारी हैं या कुछ और; पर आज हम पूर्ण मनुष्य नहीं हैं। हमारे आस-पास जितनी भी परिघटनाएँ घट रही हैं, उसका कारण साफ़ तौर पर मनुष्यता का अभाव है। आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती अपने अंदर के मनुष्य और मनुष्यता को बचाए रखना है और यही सबसे बड़ा सहयोग या उपहार है—‘वर्ल्ड अर्थ डे’, ‘पर्यावरण दिवस’ ‘विश्व वृक्ष दिवस’ या अन्य ऐसे दिवसों के लिए जिसका पालन और संकल्प हम बस एक दिन के लिए करते हैं।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
