यह ‘जल तू जलाल तू’ फ़िल्म की समीक्षा नहीं है
 विभांशु कल्ला
01 मई 2025
विभांशु कल्ला
01 मई 2025
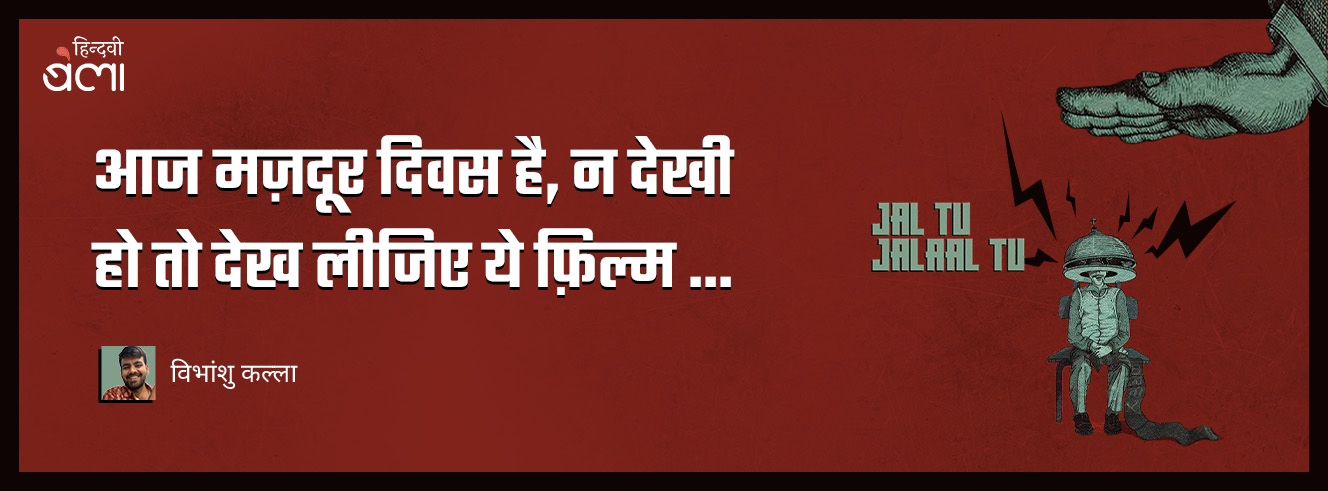
‘‘एक ज़माने पहले की बात है’’, लेकिन वो कौन-सी बात है जिसके बदलने से ज़माना बदल जाता है? ज़माना, जब कॉटन के साथ पॉलिस्टर मिलाया जाना बहुत प्रचलित बात नहीं थी, जब ‘टाटा-बिरला’ शब्द-युग्म लोकप्रिय मुहावरे की तरह इस्तेमाल होता था, तब के बॉम्बे में उत्तर भारतीयों के ख़िलाफ़ कोई सक्रिय हिंसात्मक नफ़रत नहीं थी, कानपुर पूरब का मैन्चेस्टर कहलाए जाने लायक़ था। आपातकाल के दौरान रेल के कर्मचारी चक्का जाम करने में सफल हुए थे, बॉम्बे शहर की हड़ताल के आगे ‘ग्रेट’ शब्द जोड़ा गया था। अख़बारों में लेबर बीट कवर करने वाले पत्रकार थे, अख़बारों का अपना यूनियन था जिसमें संपादक से लेकर प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले मज़दूर सदस्य थे। अधिकतर सिनेमा हॉल में सिर्फ़ एक ही स्क्रीन होती थी, सिनेमा टिकट और मक्की की फुलिया जेब में रखने की पर्याप्त जगहें थीं, तब कहानी का किरदार मज़दूर होते हुए भी फ़िल्म का हीरो होने की पूरी संभावना रखता था। दिमाग़ पर ज़्यादा ज़ोर न डालने पर भी ‘दो बीघा ज़मीन’, ‘नया दौर’, ‘पैग़ाम’, ‘काला-पत्थर’, ‘क़ुली’ जैसी दर्जन भर से अधिक फ़िल्में आँखों के सामने तैर जाती है, जिन्हें हमारी पीढ़ी ने जी क्लासिक और जी सिनेमा पर देखा है। अस्सी के दशक के साथ शुरू हुए ‘समानांतर सिनेमा' में भी मज़दूरों का जीवन और राजनीति अपनी जटिलताओं के साथ मौजूद रहे।
आर्थिक सुधारों के बाद के चमकीले सपनों वाली दुनिया में मज़दूरों की उपस्थिति की कोई विशेष ज़रूरत नहीं समझी गई। इस पूरी आर्थिक निर्मिति के केंद्र में मज़दूरों से अधिक से अधिक काम, और कम से कम मेहनताना वाली व्यवस्था थी। मज़दूरों का मज़दूर के तौर पर राजनीति में शामिल होना इस व्यवस्था के लिए ख़तरा था। टीवी ब्रॉडकास्ट, म्यूज़िक कैसेट, फ़िल्म कैसेट ने फ़िल्म उद्योग की बुनावट को बदला, बड़े सिनेमा हॉल में बड़ी संख्या में आने वाले दर्शक अब सिनेमा उद्योग की ज़रूरत नहीं रह गए थे। इन परिस्थितियों में नई चमक और ख़्वाबों वाले सिनेमा में मज़दूर का ग़ायब होना स्वाभाविक ही था। इस दौर के बहुत देर बाद सिनेमा में जब यथार्थ फिर से लौटा भी तो अपनी पूरी संजीदगी के बावजूद उत्पादन प्रणाली के हिस्से के तौर पर मज़दूर उससे ग़ायब था।
इस पूरे परिदृश्य में बहुत कम बार ही मज़दूरों के जीवन पर बनी कोई फ़िल्म देखने को मिलती है। MAMI फ़िल्म फ़ेस्टिवल की एक शृंखला के तहत IPhone से शूट की गईं चार शॉर्ट फ़िल्मों को प्रदर्शित किया गया। इसी शृंखला में डायरेक्टर प्रतीक वत्स निर्देशित ‘जल तू जलाल तू’ आज के समय के मज़दूर सवाल और राजनीति की एक झलक पेश करती है। यह फ़िल्म भी तब संभव हो पाई, जब अपने शॉर्ट-फ़ॉर्म और प्रयोगशीलता के कारण कम संसाधनों के साथ बनाई जा सकती थी। इसके साथ ही इसकी बहुत व्यवसायिक आकांक्षाएँ न होना इस विषय पर फ़िल्म बनाने की छूट दे पाता है।
अंतोन चेख़व की लघुकथा ‘एक सरकारी क्लर्क की मौत’ के रूपांतरण पर आधारित होने के बावजूद यह फ़िल्म कहानी से इतर अपनी स्वतंत्र और मौलिक पहचान बनाने में कामयाब हुई है। इस फ़िल्म की कामयाबी सिर्फ़ एक मौलिकता की खोज तक सीमित नहीं है, उसने हमारे समय, हमारे ज़माने के मज़दूर-सवाल को अच्छे से जज़्ब किया है। मूल सवाल पर फिर से लौटते है, किन बातों में परिवर्तन हुआ कि हम मज़दूरों के संदर्भ में आज के समय को पहले के समय से अलग करके देख सकते हैं? दूसरे तरीक़े से पूछे तो यह फ़िल्म जिस ज़मीन पर बनी है वह पहले से किस तरह अलग है?
अस्सी के दशक के बाद उत्पादन-प्रणाली बहुत तरीक़ों से बदली है, औद्योगिक इकाइयाँ बहुत से छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट दी गई है, अब पहले की बड़ी संख्या में मज़दूरों वाली फ़ैक्ट्री की तुलना में कम संख्या के मज़दूरों वाली छोटी औद्योगिक इकाइयाँ होती है। छोटी इकाई होने के कारण फ़ैक्ट्री स्तर का ट्रेड यूनियन देखने को नहीं मिलता, जिससे मज़दूरों को अपने स्तर पर ही अकेले बार्गेन करना पड़ता है। इस पूरे दौर में नई तकनीक के सहारे उत्पादकता में वृद्धि हुई है, लेकिन उत्पादकता में वृद्धि के अनुपात में मज़दूरों के मेहनताने में और अधिक कमी देखने को मिली है। काम के घंटे बढ़े हैं। आर्थिक सुधारों के नाम पर मज़दूरों के हक़ के क़ानूनों को बदल दिया गया है। तुरंत भर्ती, तुरंत छँटनी के चलते स्थायी रोज़गार में कमी हुई है और मज़दूरों में असुरक्षा की भावना लगातार बढ़ी है। ये वो ज़मीन है जिस पर 'जल तू जलाल तू' की कपड़ा-फ़ैक्ट्री खड़ी है।
ऐसी फ़ैक्ट्री जिसमें घंटियाँ उत्पादकता के दबाव का क्रूर स्वर है, वह स्वर जिससे मज़दूरों की जैविक क्रियाएँ तक नियंत्रित की जाती है। मज़दूर का सोना, खाना, पीना, हगना, मूतना या हँसना भी फ़ैक्ट्री के अस्तित्व के ख़िलाफ़ बग़ावत है। एक और घंटी है, जिससे सुपरवाइज़र नियंत्रित होता है। ऑर्डर जिसे पूरा किया जाना है, पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा है। हर बार बड़ा ऑर्डर, कम समय में पूरा करके देना है। तय समय में अगर ऑर्डर पूरा नहीं किया तो फ़ैक्ट्री ख़तरे में है, फ़ैक्ट्री का ख़तरा टालने की ज़िम्मेदारी मज़दूरों के कंधों पर है। लेकिन आख़िर मज़दूर एकजुट होकर इसे बदल क्यों नहीं देता?
‘जल तू जलाल तू’ यहाँ देख सकते हैं : YouTube
फ़िल्म के तीस मिनट ख़त्म हो जाने के बाद असल जीवन में लगातार यही सवाल बना रहता है, आख़िर हमारे देश में श्रम क़ानूनों को 4 लेबर कोड में बदल दिया गया, इसके ख़िलाफ़ मुखर प्रतिरोध क्यों नहीं हुआ? क्या मज़दूर वर्ग को किसी थोपी हुई विचारधारा के कारण अपने जीवन के संघर्ष दिखाई देना बंद हो गए? या बदली उत्पादन प्रणाली में संगठित प्रतिरोध करना मुश्किल हो गया? अगर पूँजीवाद के भीतर से अस्थिरता जन्म लेती है तो यह व्यवस्था स्थिरता कैसे पा गई? ये मुश्किल सवाल है, एक अकादमिक बहस में अगर जवाब देना हो तो फिर भी कुछ तर्क दिया जा सकता है, लेकिन अगर मज़दूरों को संगठित करने की कार्य-योजना बनाने के समय इन सवालों का सामना हो तो कोई बना-बनाया जवाब हल नहीं दे पाता है। अनामिका हक्सर की फ़िल्म ‘घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रिया हूँ' में लाल बिहारी सपने में ख़ुद को बोल्शेविक क्रांति का झंडा उठाए देखता है। नंदिता दास की फ़िल्म ‘ज्विगाटो’ में मानस के सपने में लेबर डिपार्टमेंट में चल रही भर्ती आती है। फ़िल्म बनाने के बाद कपिल शर्मा अपने शो में ‘ज़ोमैटो’ के संस्थापक को बुलाता है। सदर बाज़ार के बारा टोटी में अशरफ़ भाई रहते थे, जो करावल नगर में रहने वाली सईदा को नहीं जानते थे। लेकिन A Free Man का लेखक अमन सेठी, Many Lives of Syeda लिखने वाली नेहा दीक्षित को ज़रूर जानता होगा। किसी शॉर्ट फ़िल्म की समीक्षा लिखना या नवउदारवाद को आम बोली में समझा पाना मुश्किल काम है। और सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, ‘असंगठित’ कहलाए जाने वाले मज़दूर को संगठित कैसे किया जाए? संगठन के बिना सिनेमा, शहर और समाज में उसकी अदृश्यता बनी रहेगी।
लड़ जाता है आदमी, तो बढ़ जाता है आदमी।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
