विभाजन-विस्थापन-पुनर्वासन की एक विस्मृत कथा
 यतीश कुमार
11 अप्रैल 2025
यतीश कुमार
11 अप्रैल 2025
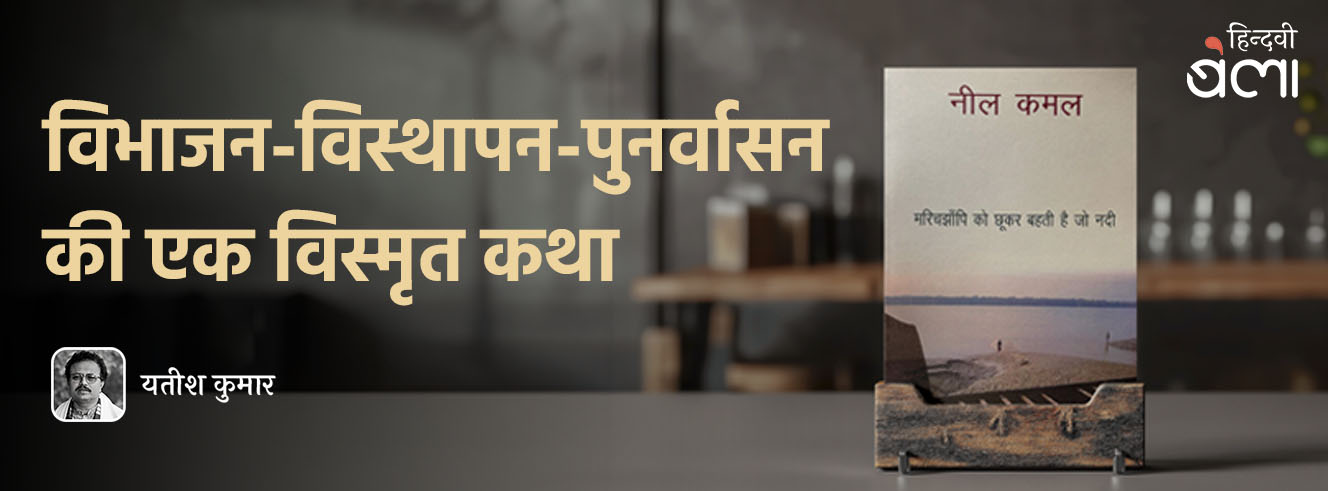
पहले पन्ने पर लेखक ने इस उपन्यास (‘मरिचझाँपि को छूकर बहती है जो नदी’) का मर्म लिख दिया है—“विभाजन, विस्थापन एवं पुनर्वासन की एक विस्मृत कथा”। यह पंक्ति पढ़ते ही आप सहज से थोड़े सजग पाठक में बदल जाते हैं। आप इस बात के लिए स्वयं को तैयार करते हैं कि आपके हाथ में सरसरी तौर पर नहीं बल्कि धैर्य के साथ पढ़ने वाली किताब है। पहले पन्ने से आगे बढ़ते हुए यूँ प्रतीत होता है, जैसे—लेखक, दृश्यों की व्याख्या, अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए कर रहा है, जैसे कभी संजय ने धृतराष्ट्र को कुरुक्षेत्र में घटती सभी घटनाओं का हाल सुनाया होगा, लगभग वैसी ही अनुभूति यहाँ पढ़ते समय होती है; लगता है जैसे पढ़ नहीं, सुन रहे हैं आप।
मरिचझाँपी के शरणार्थियों के तेरह महीने की गाथा में जीवन के कितने ही रूप छिपे हैं, कितनी यातनाओं की टेर दबी है! पढ़ते हुए सोचने लगा कि क्या कोरानखाली नदी की छुअन इस द्वीप के पाँव पखारते हुए, वहाँ की बात क्या उसी तरह से कह पाएगी—जिस तरह से घटनाओं ने बीते काल में करवट ली है?
लेखक निर्जन द्वीप पर जब सबसे पहले पाँव रखने का ऐतिहासिक दृश्य रच रहे हैं, तो ऐसा महसूस हो रहा है कि वह पाँव मेरे हैं और वह पहला मानव भी मैं ही हूँ; और दुःख नदी के उस पार कहीं छूट गया हो जैसे। सोचने लगा लेखक ने बनदेवी के बदले बनबीवी शब्द का प्रयोग क्या सोचकर किया होगा, पर अभी मन इन झंझटों में फँसना नहीं चाहता, अभी तो बस दृश्यों के साथ रहने का मन है। अभी तो बस एक गाँव के नवनिर्माण की प्रक्रिया का साक्षी हो रहे हैं बस।
उपन्यास ‘मरिचझाँपि को छूकर बहती है जो नदी’ में जानकारियों को बहुत सलीक़े से प्रस्तुत किया गया है, जैसे नाव के प्रकार, द्वीप पर पेड़ों के प्रकार, फूलों का विवरण, मछलियों के प्रकार, ऋतुओं के बदलने का विवरण और वह भी समय की बदलती आहटों के संग, लोक-व्यंजन के कई प्रकार और इन सब जानकारियों के संग विविध शरणार्थी शिविरों की जानकारियाँ भी आपको पढ़ने को मिलेंगी।
किताब में कई जगह संवाद वाले अंश में, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कोई बांग्लाभाषी हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा प्रयास उपन्यास की ज़मीन की भाषा के साथ चलने की ओर एक संकेत भी है, और इसी के साथ यह बताना भी ज़रूरी है कि यहाँ संवाद पुल हैं, छोटी-छोटी कहानियों के बीच, जो इस किताब में अनगिन किरदारों के जीवन के इर्द-गिर्द रचे गए हैं। यहाँ विभाजन का इतिहास अपनी कहानी कहते हुए ऐसा प्रतीत होता है, जैसे—एक छतनार पेड़ को उसकी ज़मीन से उखाड़कर सुदूर कहीं फिर से रोपा जाए तो उसकी पत्तियों में जो उदासी बची रहती है, उसी उदासी की गाथा इस उपन्यास की मूल जड़ में भी बसी है।
कल्पनाशीलता और शोध का संतुलित मिश्रण करते हुए नील कमल ने इस बार विस्थापन की पृष्ठभूमि पर मुक्ति संग्राम का पक्ष रखा है, और ऐसा करते हुए लेखक का झुकाव कल्पना से ज़्यादा शोध की ओर झुकता दिखा है। भौगोलिक विस्थापन की विभीषिका निश्चित ही इस उपन्यास के घटना क्रम का केंद्रीय बिंदु है। इस केंद्रीय बिंदु से बनती आवृत्ति में पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान का अत्याचार और बांग्लादेश की आज़ादी की कथा है, जिसे छूते हुए लेखक विस्थापित लोगों की गाथा का मानवीय पक्षों के साथ हुए खिलवाड़ को राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक मूल्यों पर कसने का सुंदर प्रयास कर रहा है, इस उपन्यास के माध्यम से।
छागल की प्रसव पीड़ा और फिर प्रसव करवाने का दृश्य बहुत मार्मिक, जीवंत और आश्चर्यचकित करने वाला है। “ग़ुलाम मोहम्मद नहीं आया” इस एक पंक्ति का आयाम, इसका फ़लक इतना बड़ा है, इसकी डोर इतिहास के उस पल को बाँधकर, खींचकर हम सबके सामने प्रस्तुत करती है—जब बांग्लादेश की सीमा पर यह सब घट रहा था। इस एक पंक्ति में विश्वास का स्तंभ ध्वस्त होता दिखेगा, जीवन पुर्ज़ा-पुर्ज़ा खुलता दिखेगा, अपने समय को दर्ज करता हुआ। पैसा, अपना ढोलक और पीटता दिखेगा। आँसू का, उस विहंगम आवाज़ में वाष्प बनना दिखेगा। रसरंजन के बदले लेखक जलजोग शब्द का प्रयोग करता है। कितना सुंदर प्रयोग है, मयनोशी के बदले में जलजोग शब्द का सच! प्रेम धर्म को कितनी आसानी से दरकिनार कर सकता है, यह जतिन माझी के किरदार से समझा जा सकता है। यहाँ तो जाली प्रेम का यह असर है, अस्ल प्रेम तो दुनिया बदल दे। बादल की दुनिया अपना स्वरूप प्रेम में बदल रही है।
इस उपन्यास में बाहरी कुरूपता और आंतरिक सुंदरता दोनों को बहुत सुंदर तरीक़े से कई किरदारों के भीतर पिरोया गया है। बादल, मेघना, जतिन और हसीना जैसे किरदार ऐसे ही उदाहरण हैं। जब यह लिखा-पढ़ा, कि गिरिंद्रकिशोर ज़मींदार बेटियों को बुलावा संदेश अब्दुल के हाथ भेज रहे हैं, तो कितना सुख मिला धर्म की ग़ायब दीवार को देखते हुए, जबकि यह अंदेशा पढ़ते हुए बना हुआ है कि रज़्ज़ाक़ जैसे क़ायदे आज़म के अंध समर्थक इस अदृश्य दीवार को सब की दृष्टि के सामने लाने से बाज़ भी नहीं आने वाले। उपन्यास ऐसे अंदेशों के साथ आगे बढ़ता जाता है।
कितना सुख है इसे बार-बार पढ़ने और समझने में कि भाषा आंदोलन में भाषा ने धर्म को परास्त कर दिया। “आमार सोनार बांग्ला आमी तोमाय भालोबाशी” में कितनी शक्ति होगी, जिसे टूटने में आज पचास साल से ज़्यादा लगे। ‘खुलना’ का धागा ‘श्रीनगर’ से कैसे जुड़ा है, इसे बहुत कम शब्दों में लेखक ने समझाने का सार्थक प्रयास किया है। देखते-ही-देखते कोई कैसे अपने ही देश में परदेसी हो जाता है।
इस किताब के किरदार अलग-अलग दिशाओं से आती रोशनी हैं, जिन्हें मिलकर इंद्रधनुष बनना है। लेखक ने इस इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा चटक रंग, लाल के बनाए हैं, जो देखते-देखते सुर्ख़ हो रहे हैं। घटनाओं का चक्र कई बार ऐसा आता है कि आप खो जाते हैं, सोचने लगते हैं—अब आगे क्या होने वाला है। कई किरदारों को पढ़ते हुए लगता है, इस किरदार की ज़रूरत कहाँ थी, पर थोड़ी दूर चलते ही उसका महत्त्व उभर आता है। हसीना और जतिन ऐसे ही किरदार हैं।
इस किताब को पढ़ते हुए, मैं इच्छामती नदी की मनःस्थिति की कल्पना करने लगा। दो देशों को जोड़ने वाली, जिसे पार कर लेने का अर्थ लेखक ने बताया है—‘भय से मुक्ति’। उस एक पल में नदी दर्द और चीत्कार में डूबी दिखी। ठग और लुटेरों का पनाह बनती दिखी नदी, जिस नदी का नाम इच्छामती हो, वह किसी की इच्छा पूरी नहीं कर पाती, निःसहाय दिखी नदी। इस विडंबना से बड़ी एक विडंबना का ज़िक्र लेखक ने किया है, जब इस डूबते समय में भी लोग ईश्वर को सिर पर ढो रहे हैं, मूर्तियों को सम्भाले। बादल की माँ भी उनमें से एक है।
एक सौ पचास पन्नों के बाद बनबीवी नाम से पर्दा उठता है। बन बीवी के साथ अब भाई शाहजंगली को भी समझना होगा। अमलेंदु जिस स्मृति की खोज में निकला है, पढ़ते हुए लगता है, उसका सिरा लेखक भी अपने हाथों में लिए धूम रहा है। उपन्यास लिखने में जो श्रमसाध्य शोध लेखक ने किया है, वह हिस्सा, जैसे उसकी यात्रा-वृत्तांत का हिस्सा बनकर उपन्यास में जगह पा रही है। यह वृतांत सौ पचास नहीं बल्कि बीस हज़ार से ज़्यादा लोगों के बसने और उजड़ने का है।
क्या आपको बाघ के आने से डर नहीं लगता? जैसे सवाल का जवाब कितनी सहजता से गाँव की साधारण स्त्री दे देती है, यह कह के कि, शहर में क्या आपको गाड़ी-घोड़ा से डर लगता है? इतना सरल जवाब थोड़ी देर के लिए आपको स्तब्ध कर देता है। यह उपन्यास लोक-कथाओं की झलक तो दिखाता ही है, साथ ही रह-रह कर एक डाक्यूमेंट्री फ़िल्म की तरह सुंदरवन और उनके द्वीपों की जानकारियों को भी आपके सामने रखता चलता है। अमलेंदु की खोज एक तरफ़ और दूसरी तरफ़ समय की अपनी पुकार, जिसमें विस्थापन की समाहित अपनी व्यथा। समय की करवट में आप पश्चिम बंगाल से रायपुर “माना ट्रांजिट कैंप” कब पहुँच जाते हैं, पता ही नहीं चलता। उपन्यास इस कैंप के तहत राज्यों के आंतरिक राजनीतिक मतभेदों को उजागर करता है, साथ ही आदिवासियों के भीतर का संशय शरणार्थियों को लेकर कैसे बढ़ता गया इसको भी दर्ज करता है। अलका सरावगी का उपन्यास ‘कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए’ में भी ऐसा ही विवरण विस्तार से ‘माना ट्रांजिट कैंप’ और विस्थापन को लेकर मिलता है, पर आदिवासियों की प्रतिक्रिया शरणार्थियों को लेकर कैसी है, यह नील कमल विस्तार से लेकर आते हैं।
वास्तु हारा उद्द्बास्तू के कठोर जीवन की मार्मिक कथा का सबसे बड़ा सच, बंगाल में तख़्ता बदली से जुड़ा है। जातीय समीकरण में निचली जाती का ज़्यादा होना भी एक कोण है, जिसकी ओर इशारा कर रही है यह किताब। दमन की नीति का आधार जाति के इस बिंदु का होना, सच में भीतर तक दहला दे रहा है। ‘मणिकर्णिका’ संस्मरण में इस बिंदु को अलग से लिखा है डॉक्टर तुलसी राम ने, जो कम्युनिस्ट पार्टी की एक अलग तस्वीर खींचती है। सोशलिस्ट पार्टी की मज़बूती, सत्ता को कितनी खल रही है और समय देखते राजनीति का अपना स्टैंड कैसे बदल जाता है, उसकी झलक यहाँ देखने को मिलेगी। यह बदला हुआ स्टैंड कितना भयावह होकर अपना असर लिए शरणार्थियों पर गाज़ की तरह गिरता है, यह इस उपन्यास में शोधपूर्ण तरीक़े से दर्ज है। सुल्तान गाज़ी जैसे किरदार, सरकार के इरादे का सही आईना लिए घूम रहे हैं। इन सब के बाद ‘सिटीजंस फ़ॉर डेमोक्रेसी’ समिति की मरिचझाँपी यात्रा रद्द होना आख़िरी भरोसे का कलश टूटने जैसी घटना है।
सच में मरिचझाँपि को छूकर बहती नदी में बहुत गन्दैला पानी बह चुका है, परंतु भटकती आत्माओं की नाव अब भी वहीं चक्कर लगा रही है। उन आत्माओं की मुक्ति के यज्ञ में आहुति की तरह का प्रयास है यह किताब।
इस किताब को पढ़ते हुए हितेंद्र पटेल की किताब—‘आधुनिक भारत का ऐतिहासिक यथार्थ’ की बात याद आ गई, जिसका तात्पर्य यह है कि “इतिहास का अधूरा सच साहित्य की खिड़की से ही दिख पाता है”। नील कमल ने एक ऐसी ही खिड़की खोली है, जिससे आप इतिहास के उस अधूरे कड़वे सच के बेहद क़रीब जा सकते हैं। सराहनीय और प्रशंसनीय है, यह मृतप्राय भूगोल को ज़िंदा करने का यह अथक अनूठा प्रयास नील कमल का। नील कमल की दस साल की मेहनत और शोधपूर्ण लेखनी आप सब तक पहुँचे ताकि अबूझ को जान पाने में आपको मदद मिले।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
