समीक्षा : सूर्यबाला के पहले उपन्यास का पुनर्पाठ
 यतीश कुमार
30 अगस्त 2025
यतीश कुमार
30 अगस्त 2025
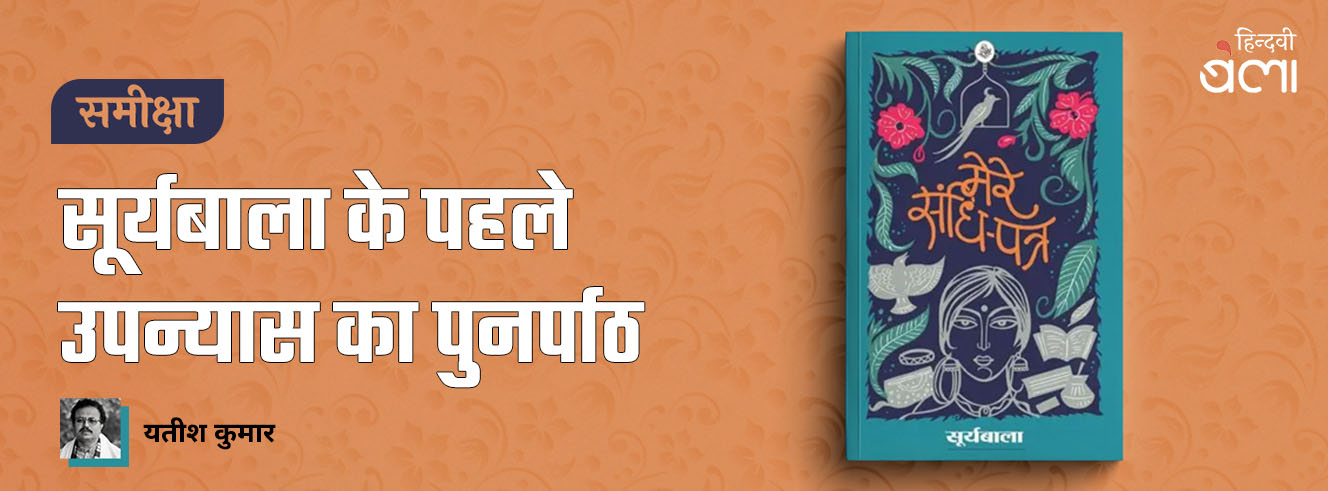
हिंदी साहित्य में जिसे साठोत्तरी रचना पीढ़ी के नाम से जाना जाता है, सूर्यबाला उसकी एक प्रमुख हस्ताक्षर हैं। उनकी साहित्यिक पहचान की नींव उनके पहले ही उपन्यास ‘मेरे संधि-पत्र’ से जुड़ी है। मैं इस किताब तक कुछ देर से पहुँचा, लेकिन किताब खोलते ही सबसे पहले यह बात समझ में आई कि इस किताब की उम्र, मेरी उम्र से ज़्यादा है। इस बात ने भी मेरी पठनीयता को और धीरज प्रदान किया और कहा इसे बिल्कुल फूँक-फूँक कर पढ़ना होगा।
शुरुआती पन्नों में ही देख रहा हूँ कि कितनी सरलता से बातों-ही-बातों में गहन बातें कही जा रही हैं। ढेर सारे सहज और भावनापूर्ण संवाद हैं। एक के बाद एक, जिसे पढ़ते हुए मन भींग रहा है। ‘उचारते हुए’ जैसे शब्दों का प्रयोग या ‘हथेलियों को जैसे इलहाम आया हो’ जैसी पंक्तियाँ, भाषा पर लेखक की मज़बूत पकड़ से परिचय करवा रही है। ‘मेढकी को ज़ुकाम हो रहा है न’ जैसे संवादों में चुहल का अभिनव पुट इसे रोचक बना रहा है। जब झुंड को शिष्ट मंडल ठिठोली में सूर्यबाला कहती हैं, तो लगता है कितनी बारीकी पर ध्यान दिया गया है। भाषा यहाँ गुदगुदाने, चरचने और थहाने के बीच टहलती हुई नज़र आ रही है।
अभी मैं इस उपन्यास में अथाह समंदर के ऊपर कश्ती-सी लग रही मुस्कान को तीरते देख रहा हूँ। गहन बातों में सहज कहन से, पढ़ने की सलाहिय्यत सीख रहा हूँ। तपस्या और माँ दो शब्दों को एकमय होते देख रहा हूँ। माँ का मतलब समंदर, पर्वत और आकाश होना समझ रहा हूँ। इस उपन्यास के पाठ के बीच अनिर्वचनीय अनुभूति उभर रही है, जिसके लिए उपयुक्त शब्द ढूँढ़ रहा हूँ। ढूँढ़ते-ढूँढ़ते मेरी नज़र ‘गर्दख़ोर’ शब्द पर आकर चिपक गई। एक शब्द पूरे व्यक्तित्व को बयान कर सकता है और परिस्थिति को भी। इसका ऐसा प्रयोग देखकर अभी हैरान ही होता हूँ कि तभी एक पंक्ति ने जैसे तमाचा जड़ दिया। लिखा है—‘छह साल तो हो गए सूखी पड़ी हो’। इस एक पंक्ति ने कितनी कड़वी बात कह दी कि मन कसैला हो गया। जिस किरदार पर बिजली गिरी होगी, उसकी लेखिका के मन का क्या हुआ होगा! अब भी यही सोच रहा हूँ। आगे लिखा है—‘रामकली, यह अनकही अतल की पीड़ा कैसे गोताख़ोरों-सी टोह लेती है तू’, इस एक वाक्य में स्निग्ध स्नेह के साथ-साथ दो असमान सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच, कितनी सुंदर आपसी समझ का प्रतिबिंब दिख रहा है। यह है लेखन की असली ताक़त— मतलब संप्रेषण की शक्ति।
ऋचा और रिंकी के किरदार रह-रह कर ‘मासूम’ फ़िल्म की उर्मिला मातोंडकर और मिनी मल्होत्रा यानी ‘मिनी’ की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही मासूम, सचेत और भीतर से टटोलते हुए। किरदारों की अगराती ख़ुशी में ख़ुश होना और आँखों में उठते जलजले को अपनी आँखों में महसूस करना, ख़ुद से पूछते प्रश्न, जिनका उत्तर किरदार ख़ुद ढूँढ़ रहा हो, उस ढूँढ़ में शामिल हो जाना, इस किताब के जादू का असर है। ऐसा जादू जिसमें एक पाठकीय साझेदारी, संवाद की तरह पंक्ति-दर-पंक्ति बहती है। बहुत समय बाद ऐसी किताब पढ़ रहा हूँ, जिसमें हर पैराग्राफ़ संवाद के साथ बढ़ रहा है। यहाँ तक कि परिस्थितियों का वर्णन भी अनुभव की तरह भीतर उतरता है। ‘कल से टेबल से इनकी प्लेट ग़ायब कर देंगे। पापा खाना खाएँगे न, वही इनके पेट में जाएगा’, यह एक साधारण-सी पंक्ति नहीं, बल्कि घर के भीतर माँ की अदृश्य होती पहचान का एक मूक प्रतिरोध है। अस्मिता के इस शाश्वत प्रश्न को दोहरा रही है, जिसमें बदलाव आज भी बहुत धीमी गति से आ रहा है। सूर्यबाला ने इस प्रतिरोध का एक रूप ऋचा की बनाई पेंटिंग में रचा है। माँ और प्रकृति को एक-दूसरे के प्रतिबिंब की तरह रेखांकित करना न केवल एक कलात्मक दृष्टि है, बल्कि उपन्यास के मर्म को गहराई से समझाने की एक संवेदनशील कोशिश भी है। जैसे रंगों में उकेरा गया स्त्री होने का मौन भाष्य। कभी-कभी साहित्य सिर्फ़ कहानी नहीं कहता, वह पाठक को आईना भी थमाता है और यह उपन्यास ऐसा ही एक आईना है, जिसमें हम सिर्फ़ ऋचा और रिंकी को नहीं, ख़ुद को भी देखते हैं।
पिता रायजादा का रूढ़िग्रस्त तावीज़ पहनना, उनके रह-रह कर उभरते संवादों से साफ़ झलकता है, जिसे उनकी पत्नी हर बार सबके सामने सँभालती रहती हैं। हर उस संवाद में कटाक्ष का नस्तर है, जो किरदारों को आत्ममंथन के उस पल में सन्नाटे की शमशीर बन चीर देती है। यहाँ सवाल, मुक्का तान कर खड़े हैं और यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि आख़िर बीते पचास सालों में समाज असल मायने में कितना बदला है। इन सब प्रश्नों के बीच यह किताब, मृदु और संयत स्त्री के जीवन के हिलोरों की ताकीद करती है। यह जो स्वीकार रूपी शत्रु, स्त्री के जीवन में सर्प बनकर रह रहा है, उस स्वयं से कैसे लड़ा जाए, किताब में इस विडंबना की कहानी रची गई है। एक बात जो इस किताब को और अलग बनाती है, वह है कथानकों का बदलना। पहले ऋचा, फिर रिंकी और अंत में शिवा, जो इस पूरे उपन्यास के केंद्र में है, स्वयं अपनी बात रख रही है। यह इस किताब के केंद्रीय विषय को तीन नज़रों से देखते हुए रोचकता बनाए रखते हैं।
‘कब किस बाट से तौली जाऊँगी?’ जैसे प्रश्नों के बीच कई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि मन डूबने लगता है। फिर हवा का रुख़ बदलता है और बाँध तोड़ने के इंतज़ार में खड़ी शिवा के मन के अँधेरे में, बदलियों के टुकड़े मदिर बयार लिए एक पतंगी आकाश बन कर आता है। यहाँ से हवा अपनी दिशा बदल लेती है। अपनी पहचान को खोना और फिर दोबारा न पाने की स्वयं से जिरह करती शिवा को पता है कि अभ्यस्त छद्म से इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिल सकती। ‘मन नहीं कर रहा’ को मन के ढूँढ़ लेने के तर्क से जोड़ना कितना तर्कसंगत लगा। असल में समर्पण के साथ शमित होना आसान नहीं, यह इस किताब को पढ़ते हुए भी महसूस होता है।
दिल से मथकर निकले शब्द यहाँ बारम्बार पढ़ने को मिलेंगे, जैसे ‘यह शब्द उन्होंने ऐसे नहीं बोला है। उसे दूध की धार से धोकर, नन्ही पंखुड़ियों से सँवारकर, धीमे से मेरे सामने रख दिया है।’ इन पंक्तियों के बीच का छिपा दर्शन भाव, रह-रह कर वाचाल हो उठता है और कहने लगता है—‘क्रोध, लोभ, घृणा और दया—इन पर कभी उम्र का आधिपत्य रहता है? तब मोह को ही क्यों अपवाद मान लें हम।’ शेष रह जाती हैं दो जिए हुए रातों की स्मृति, और उनके साथ स्वीकृति पत्र व संधि पत्र का चमकता साटन।
इन बातों से परे भी यह उपन्यास कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। अपनी कथावस्तु में विशिष्ट, विषय पर केंद्रित, विचारों में सामाजिक चेतना के साथ-साथ दार्शनिक दृष्टिकोण का स्पर्श, कथन का एक अलग ही अंदाज़, और भाषा में असाधारण सहजता व संप्रेषण शक्ति का समुचित संतुलन।
इस किताब से गुज़रते हुए एक बार भी यह एहसास नहीं हुआ कि मैं पचास वर्ष पूर्व लिखा गया उपन्यास पढ़ रहा हूँ। हर पंक्ति में समकालीन जीवन की सजीव धड़कन सुनाई दे रही थी। मन स्वतः ही इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मुझे सूर्यबाला का लिखा और पढ़ना है। शब्दों के सटीक और संवेदनशील प्रयोग को समझने के लिए और उनके अनुभव-संपन्न दृष्टिकोण से समाज को नए सिरे से देखने के लिए। एक लंबे विराम के बाद पढ़ने की दुनिया में लौटे पाठक की ओर से, उन्हें दिल से धन्यवाद।
~~~
यतीश कुमार को और पढ़िए : विभाजन-विस्थापन-पुनर्वासन की एक विस्मृत कथा | बहुत कुछ खोने के अँधेरे में किसी को बचाने की कहानियाँ
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
