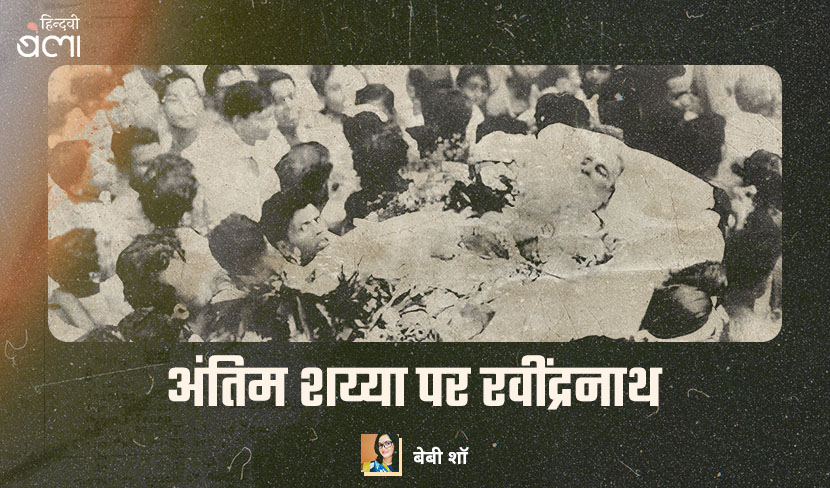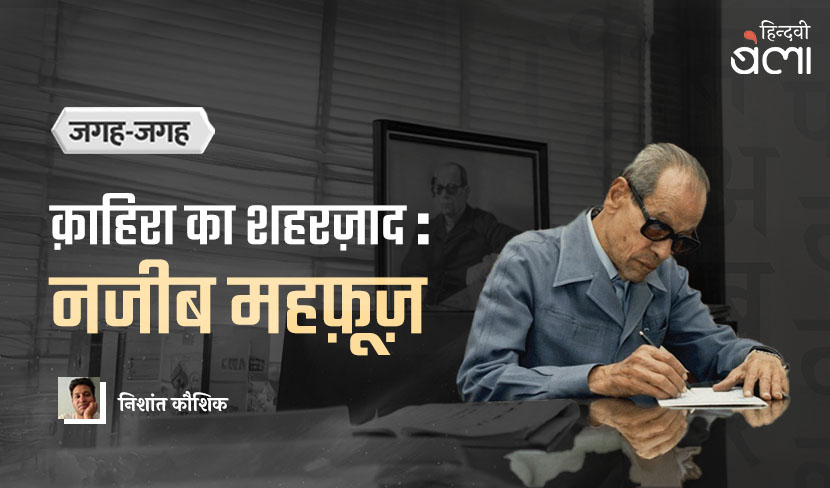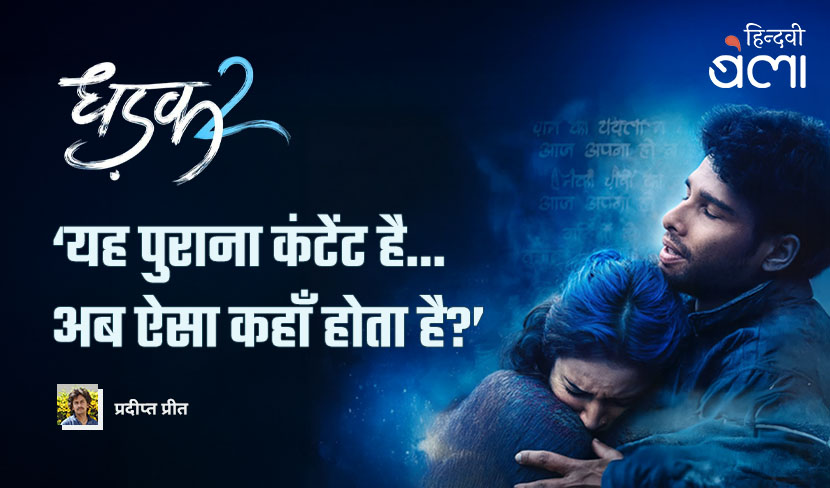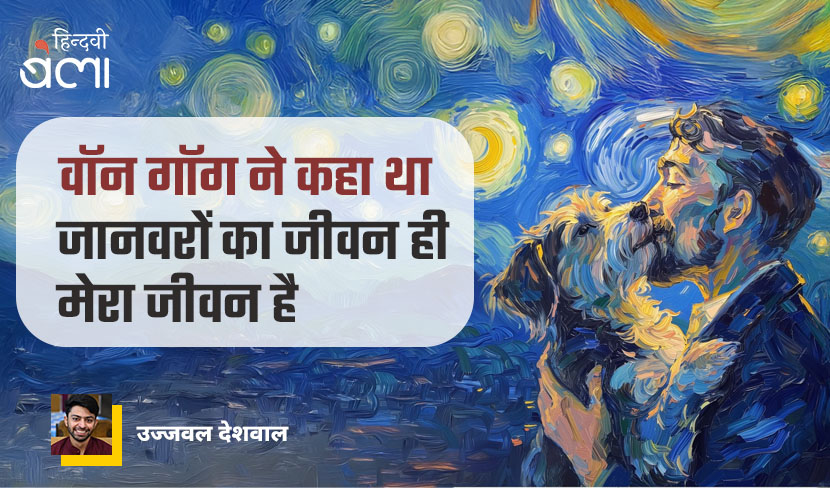शारदा सिन्हा : ‘हमरा के कहाँ छोड़ले जाइछी रे गवनवा...’
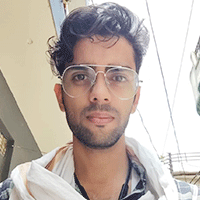 केतन यादव
06 नवम्बर 2024
केतन यादव
06 नवम्बर 2024

‘अपने त जाय छी प्रभु देस रे बिदेसवा से, हमरा के...’ पर कहाँ जा पाएँगी इस देस से? काश ‘घोड़ा के लगमवा’ थाम के रोका जा सकता। काश ‘सँईया कलकतवा से’ आ सकते। किसे कहेंगे इस महादेस के मन की आवाज़ अब; ठीक वैसे ही जैसा-जैसा हमने देखा जैसा भोगा।
केवल भोजपुरी, मैथिली, मगही और बज्जिका के क्षेत्र के लोग ही नहीं, बल्कि इसके बाहर के भी वे सभी लोग जो इस आवाज़ को सुनकर पूरबी और बिहारी हो जाते थे—थोड़ी देर के लिए उन कोटि-कोटि कंठों की आवाज़ मानो छिन गई, क्योंकि गायन तो अभी मृत्यु से पूर्व तक चल रहा था और न जाने कितने गीत सुनने बाक़ी हो सकते थे।
शारदा सिन्हा ने तीन पीढ़ियों के आंचलिक लोगों को अपनी आवाज़ दी। कहीं दूर जब कोई ग्रामीण स्त्री नाम नहीं स्मरण कर पाती तो बोलती थी ‘बाबू उनकर गनवा लगावा, अरे उहे जिनकर छठवा में बजेला।’ क्या छठ में केवल शारदा सिन्हा के गीत बजते हैं? नहीं! अब बहुत सारी आवाज़ें हैं। फिर भी वही एक आवाज़ क्यों? दरअस्ल केवल छठ नहीं सावन, चैती, विदाई, हल्दी, मटकोड़वा, देवी गीत, शंकर के गीत, विद्यापति के गीत, घर छूट जाने के गीत, ओखल से धान का गीत, उबटन का गीत, दुआरपूजा के गीत, प्रिय के आने का गीत, प्रिय के न आने का गीत, प्रिय के भूल जाने का गीत, प्रिय को ताना मारने-कोसने का गीत... कितना कहूँ, मेरी पूरी प्लेलिस्ट है जो सालों से गीतों को चुनचुनकर संजोयी है मैंने।
कितनी बार जब अपने अंचल को याद करने के लिए कुछ नहीं सूझता तो हम हेड-फ़ोन लगाकर शारदा सिन्हा के गानों को सुन लेते। हाय विस्थापन की पीड़ा को वैसी आवाज़ कौन दे सकेगा अब? हमारे माँओं-दादियों के न व्यक्त होने वाले दुख, खीज, उत्साह, उलाहना को इतनी खनकती आवाज़ में कौन कह सकेगा।
हर भाषा के पास बहुत से गायक हैं, लेकिन हमारी भाषा के पास—पूर्ण सांस्कृतिकबोध के रूप में अभिव्यक्ति के लिए शारदा सिन्हा थीं। पितृसत्ता में जकड़ी स्त्रियों को टीस कहने के लिए—गाँव में बियाह का माटिकोड़वा और दुआरपूजा का जब मौक़ा मिलता था, तो वे जी-भरकर गरियाती थीं। लोग बहुत धीरज से उसे सुनते थे, मानो बोल रहे हों कि कह लेने दो आज। ‘लोगवा देत काहें गारी’ के आश्चर्य से।
हमारे यहाँ साँझ का दीपक ‘जगदम्बा घरे दियरा बार अइली’ के प्रार्थना से गाया जाता था। पूजा के फूल किस उपक्रम से तोड़ के लाए गए—‘कौन मुहे शिव जोगी लवनी फुलवरिया’ और पीड़ा ऐसी कि आवाज़ आराध्य के साथ चली जाने का निवेदन कर उठती—‘बाबा लेले चलियो हमरो अपन नगरी’।
हाय पूरब बिहार सहित इस देश का आंचलिक उत्सवधर्मी समाज—हमारे गाँव की स्त्रियाँ जो अपनी पीड़ा, अपना सारा दुख, जीवन भर के प्रसंगों में गा-गाकर कहती हैं। फिर होश आता ‘आज धनवा कुटाउ चारु बरवा से’ जब नई-नई ब्याहता अपनी बीमारी सास या ननद से नहीं कह सकती और पति को बिना बहुत सारे संदर्भ बताए, डॉक्टर के पास पत्नी को लिए जाने की बात कहनी होती तो वह ब्याहता पति के मुँह से ही कहलवाती—‘पटना से बैदा बुलाई दा, बेमरा गइलीं गुईंया’
‘कुछओ न बोलब तोसे तनिक बतादा, कइली का कसूर इहे तनिक बतादा’ कह-कहकर गाँव की स्त्री, पति को बुलाती है कि बस एक बार लौट आओ वही सईंया जो अब ‘डुमरी के फूल’ की तरह हो चुका, दिखाई नहीं देता।
बंगाल किसी विदेश की तरह रहा, पूर्वांचल और बिहार की स्त्रियों के लिए। पति के वहाँ चले जाने के बाद हमेशा उनके नहीं आने का डर लगा रहता। कितने गीतों में यह भय है जिसमें ‘सईंया कलकतवा से’ बुला लेने की बात है। न जाने किस हालत में पति होगा, यह सोच-सोच कर वह स्त्रियाँ गली जाती हैं। बंगाल की जादूगरनी स्त्रियों के जादू-टोने से बचाने के लिए ‘अचल सुहाग’ माँगती हैं, ‘बाबा हे बड़ेसर’ से। पति को वह कुछ भी करके अपने पास बुला लेना चाहती हैं, मानो अबकि लौटा तो पानी-रोटी खाकर जी जाएँगे, लेकिन वापस जाने नहीं देंगे। कल्पना और भ्रम में ही वह मान-मनौव्वल चलता है—‘कइलीं हम कवन कसूर नयन मोसे दूर कइला बलमू’, ‘परदेसिया ये बलमवा से नाही अइले ना, निर्मोहिया रे बलमवा’ और पति के लौटने की सूचना पर खत का जवाब देती ‘लेहले अइहा हो, पिया सेन्हुर बंगाल के’
‘नहियर में रहली बड़ा रे सुख पइली’ कहकर ससुराल में अपनी खीज भी व्यक्त कर लेतीं और शारदा सिन्हा के किसी विदा गीत को सुनकर वापस उसी समय में लौट कर रोने लगती हैं गाँव की भोली औरतें—‘निमिया तले डोली रख दे मुसाफिर’। स्कूल जाते समय अम्मा जब गाल दबाकर भर कपार तेल छोपकर बाल झारतीं तो वह दृश्य शारदा सिन्हा के गीत ‘मोरे बबुआ को नजरियो न लागे’ में इस तरह रुपाकार हो उठता कि यह सब लिखते हुए, मेरी आँख बार-बार भर जा रही है। स्क्रीन पर आँसू गिर रहा है और लिखने की कोशिश में की-पैड फिसल जा रहा है।
लोक की स्त्रियाँ शास्त्र नहीं बूझती हैं, लेकिन शास्त्र का ऐसा प्रतिकार करती हैं कि कोई जवाब नहीं होता। देवी-देवता बहुत सारे अर्थों में भीतर का दुख कहने के साधन होते हैं। शारदा सिन्हा का एक इतना मार्मिक गीत है, जिसमें कमल के पत्ते पर सोने वाली नाज़ुक पार्वती को सपना आता है कि शिव उनकी सौतन लाए हैं, इस सपने का पूरा वृत्तांत उन स्त्रियों की आशंका है, सिहरन है जो पति के किसी और स्त्री के हो जाने के दुख को बयाँ करता है—‘पुरइन के पात पर सुतली गउर देइ, सपना देखलीं अजगूत हे... दूर ही देस बाजन एक बाजत, किनकर होवेला बियाह हे’।
शारदा सिन्हा के गाए गीतों में केवल लोक का रोमानी पक्ष ही नहीं लोक की आलोचना भी है। उसकी विद्रूपता, विडंबना के रूप में सामने आती है और वह भी इतनी बलवती होकर कि उसका अपील सम्मोहनकारी होता और ‘काठ के करेजा’ को भी पिघला देता।
बाल-विवाह की विद्रूपता इस तरह आती है उनके यहाँ—‘सूतल चलि अइली बाबा के भवनवा, अचके में आयल कहाँर।’ उस छली हुई बच्ची को पिता के घर छूटने का पता तब चलता है, जब कहाँर के डोली उठने पर हचका लगता है। बियाह के गीत तो इतने हैं कि पूरब और बिहार का कोई मंगल काम इन गीतों के बिना पूरा न हो।
पापा बताते थे कि नब्बे के दशक में ‘95 में जब बुआ की शादी हुई और ‘99 में उनकी तब शारदा सिन्हा के गाने कैसट पर ख़ूब बजे थे। इस घर में विवाह का माहौल है, इसको व्यक्त करने के लिए उनके गीत ही समर्थ रहे। ‘हरे हरे हरे दादा बसवा कटहिया, ऊँचे ऊँचे मड़वा छविया हो’ गीत से जहाँ माड़ो बाँधा जाए तो ‘जो (जौ) रे गेहूमवा (गेहूँ) के उबटन, राई सरसो के तेल अउरी फुलेल, दुलरउती बेटी बइठे ली उबटन’ से बेटी को उबटन लगता रहा, ‘हरि हरि दुबिया बछरुओ ना चरे गे माई हमरो सुंदर दुलहा मौरीयो ना पेन्हे गे माई’ गीत से मौरी परछाता तो बारात के परछने के अनेक गीत तो चुमावन के रसम में सबसे पहले ‘दादी चुवाहि सरबस लुटावे’ से शुभारंभ होता।
‘अगे माइ हरदी हरदिया दूब पातर न’ सहित कितने हल्दी के गीत, सिंदुरदान के समय ‘उड़ी रे गवनवा से अइलँ सुंदर दुलहा बैठी गइलईं ससुरे दुआरी रे गवनवा’ तो ‘दुलहा सुंदर मुख मनहो नहीं’ गीत से सम्धन को कोसना। कितने-कितने गीत एक साथ याद आ रहे हैं। मानो हम पुरबियों के घर बियाह ही न हो पाए शारदा सिन्हा के गीत के बिना।
छठ पर किस विधि लौटूँ। जो सुनने को मिल रहा है, हाँ वह पूरी तरह सच है। शारदा सिन्हा और छठ एक दूसरे के पर्याय हैं। छठ का प्रसार बिहार और पूर्वांचल के गाँव-कस्बों से होकर देश-विदेश तक हुआ। आज साउंड पर शारदा सिन्हा के छठ गीत दिवाली के बाद बजते ही दूर बैठे प्रवासी का मन ऐसे मचल उठता है और गाँव लौटने के लिए सरकार की सारी यातायात व्यवस्था की कलई खुल जाती है। दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित देश के सभी बड़े रेलवे और बस स्टेशनों की हालत कैसी होती है, यह आजकल आपको सामने ही दिख रहा होगा।
वह कौन-सी आवाज़ है? वह कौन-सा आकर्षण है? अरे, वह कौन-सा पर्व है जिसके लिए पुरबिए और बिहारी एक नहीं कितनों की संख्या में ट्रेन के शौचालय में सफ़र करके लौटे और यह दृश्य देखकर केवल निरुत्तर ही हुआ जा सकता है।
क्या ही विडंबना है कि छठ के गीतों से अपना अस्तित्व गढ़ने वाली और छठ के गीतों को अस्तित्व देने वाली शारदा सिन्हा की मृत्यु छठ के समय ही हुई। मुझे नहीं पता इस आश्चर्य को इस विडंबना को मैं किस वैज्ञानिक तार्किक चिंतन से कहूँ। प्रकृति का यह कैसा खेल है? कोई व्यक्ति किस निष्ठा से किस समर्पण से अपने आपको किसी असीम में आत्मविलीनीकरण कर सकता है कि उसका होना-नहीं होना, उसी से जुड़ जाए। इस आश्चर्य को हम घटित होता देख रहे हैं और बरसों तक आश्चर्य से ही याद रखेंगे।
शारदा सिन्हा गातीं तो छठ का हर घाट ‘पटना के घाट’ हो जाता। शारदा सिन्हा जगातीं ‘उठा सुरुज भइले बिहान’ तभी सूरज जगते। ‘ओ दीनानाथ’ की टेर में पृथ्वी से कौन-सा वह महास्वर किसी हीलियम के तारे नहीं बल्कि पृथ्वी पर जीवन देने वाले सूर्य को पुकारते थे? वह कौन-सी कृतज्ञता है, आभार ज्ञापन है, जो डूबते-उगते सूरज को ये स्त्रियाँ शारदा सिन्हा के गीतों में प्रगट करतीं। ‘पहिले पहिल’ छठ करने वाले से लेकर जीवन भर छठ का व्रत निभाने वाली व्रती के लिए शारदा सिन्हा की आवाज़ सम्बल है। आशा की पतली किरण है जो भोर में फूटती है, पूरे उजाले के इंतज़ार और तसल्ली में व्रती खड़े रहते शीतल जल में। ‘कौने खेते जन्मल धान सुधान हो’ कहकर फल-फूल-पान इकट्ठा करती है और ‘केरवा के पात’ के झुरमुट में से सूरज को देखकर न जाने कौन-सा प्रकाश, कौन-सा उजाला पूरब की औरतें खोजती हैं।
कहने को इतना कुछ है। मेरे आस-पास मेरा पूरा वातावरण शारदा सिन्हा के हर तरह गीतों से निर्मित है। सैकड़ों गीत मुझे याद हैं, जिन्हें मैं केवल उनकी आवाज़ में सुनना चाहता। शारदा सिन्हा का कोई भी गीत अभी भी सुनकर वही अनुभव हो जाता है जो उस गीत का अनुभव है। कितना कुछ भरा है भीतर... मैं शायद उसका एक अंश भी नहीं कह सकता बल्कि बहुत कुछ कहने के बाद भी कितना कुछ है जो नहीं कहा जा सकता। अरे हम किस विधि, किस उपक्रम से अपनी यह भावुकता व्यक्त करें! कौन-सा ऐसा वाक्य होगा जो सब कुछ कह जाए। अपनी ‘दुलरउती बेटी’ को कैसे विदा करे पुरबिए और बिहारी? कैसे?
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
07 अगस्त 2025
अंतिम शय्या पर रवींद्रनाथ
श्रावण-मास! बारिश की झरझर में मानो मन का रुदन मिला हो। शाल-पत्तों के बीच से टपक रही हैं—आकाश-अश्रुओं की बूँदें। उनका मन उदास है। शरीर धीरे-धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। शांतिनिकेतन का शांत वातावरण अशांत
10 अगस्त 2025
क़ाहिरा का शहरज़ाद : नजीब महफ़ूज़
Husayn remarked ironically, “A nation whose most notable manifestations are tombs and corpses!” Pointing to one of the pyramids, he continued: “Look at all that wasted effort.” Kamal replied enthusi
08 अगस्त 2025
धड़क 2 : ‘यह पुराना कंटेंट है... अब ऐसा कहाँ होता है?’
यह वाक्य महज़ धड़क 2 के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यह ज्योतिबा फुले, भीमराव आम्बेडकर, प्रेमचंद और ज़िंदगी के बारे में भी कहा जा रहा है। कितनी ही बार स्कूलों में, युवाओं के बीच में या फिर कह लें कि तथा
17 अगस्त 2025
बिंदुघाटी : ‘सून मंदिर मोर...’ यह टीस अर्थ-बाधा से ही निकलती है
• विद्यापति तमाम अलंकरणों से विभूषित होने के साथ ही, तमाम विवादों का विषय भी रहे हैं। उनका प्रभाव और प्रसार है ही इतना बड़ा कि अपने समय से लेकर आज तक वे कई कला-विधाओं के माध्यम से जनमानस के बीच रहे है
22 अगस्त 2025
वॉन गॉग ने कहा था : जानवरों का जीवन ही मेरा जीवन है
प्रिय भाई, मुझे एहसास है कि माता-पिता स्वाभाविक रूप से (सोच-समझकर न सही) मेरे बारे में क्या सोचते हैं। वे मुझे घर में रखने से भी झिझकते हैं, जैसे कि मैं कोई बेढब कुत्ता हूँ; जो उनके घर में गंदे पं