लोक : भोजपुरी लोकगीत : विस्मृत धरोहर
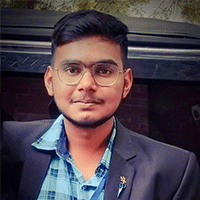 विशाल कुमार
24 अक्तूबर 2025
विशाल कुमार
24 अक्तूबर 2025

भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह सामाजिक पहचान, वर्ग, जाति और सत्ता संरचनाओं से निर्मित राजनीति की भी वाहक होती है। इसे ‘प्रतीकात्मक पूँजी’ के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो किसी समाज की सांस्कृतिक और राजनीतिक दृश्यता को भी निर्धारित करती है।
भोजपुरी भाषा—बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कई ज़िलों में बोली जाती है। इसका एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है और ऐतिहासिक विरासत भी; लेकिन कहीं-न-कहीं वर्तमान समय में भोजपुरी अपनी सांस्कृतिक पूँजी को सुरक्षित रखने में असफल साबित हुई है। अधिक आश्चर्यजनक तो यह है कि ख़ुद इसको बोलने वाले भी इसकी भाषायी परंपरा और इतिहास के पुनः अधिग्रहण की ओर अपेक्षित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी उपेक्षा के कारण संपूर्ण भाषा को एक ही ढांचे में रखकर, उसे अश्लील और फूहड़ बताया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सांस्कृतिक श्रेणीकरण में अक्सर इसे निम्न स्थान पर रखा जाता है। फ़िल्मों में और मनोरंजन जगत में भोजपुरी, नौकरों की और निम्न वर्ग की भाषा बनकर रह गई है, जिसे मज़ाक़िया और हास्यास्पद ढंग में दिखाया जाता है।
भोजपुरी भाषा अपनी लोकगीतों की परंपरा से सदैव संपन्न रही है, किंतु आज की युवा पीढ़ी इस धरोहर से मुख्यतः अनभिज्ञ है। सवाल यह है कि कितने युवा ऐसे हैं जो भिखारी ठाकुर, बिहारी लाल यादव या महेंद्र मिश्र जैसी विभूतियों से परिचित हैं?
भोजपुरी लोकगीतों की जड़ें मौखिक भाषा परंपरा में रही हैं, पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से इनका संचरण होता रहा है, लेकिन वैश्वीकरण और आधुनिकता की वजह से अधिकांश युवा आज गाँवों से पलायन कर रहे हैं या गाँव में रहने के बावजूद सामूहिकता अब वैसी नहीं बची, जो पहले हुआ करती थी। लोकगीत—उस सामुदायिकता की अमूल्य धरोहर हैं, जिनमें ग्रामीण जीवन और कृषि केंद्रित समाज का सुंदर चित्रण निहित है। यह लोकगीत न केवल लोक के साझेपन का प्रतीक है, बल्कि उनके निकट समाज की गतिशीलता का भी रचनात्मक प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं। चूँकि उस क्षेत्र के लोक-कवि स्वयं उसी लोक का हिस्सा होते थे, इसलिए वे अपने समकालीन समय के प्रमुख विषयों पर गहरी पकड़ रखते थे और लोक-काव्य के माध्यम से ग्रामीण जीवन के संघर्ष, दुख और तकलीफ़ों को आमजन की भाषा में अभिव्यक्त करते थे। साथ ही वे कला को सामाजिक संवाद का माध्यम बनाकर समाज में प्रचलित कुरीतियों से भी संघर्ष स्थापित करते थे।
‘बिदेसिया’, ‘गबरघिचोर’, ‘बेटी बेचवा’, और ‘बिधवा बिलाप’ जैसी कालजयी रचनाएँ गढ़कर भोजपुरी के ‘शेक्सपीयर’ कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने यह सिद्ध किया था कि कला एक स्वायत्त अभिव्यक्ति भर नहीं, बल्कि सामाजिक संवाद और परिवर्तन का माध्यम भी होती है। इन नाटकों के ज़रिए वह सीधे ग्रामीण जीवन की समस्याओं से टकराते थे। प्रवास, दहेज, जातिगत संरचनाएँ, असमान विवाह, मद्यपान, विधवापन और स्त्री-पीड़ा जैसे मुद्दों को प्रकाशित करते थे। साथ ही उनका, ‘नाच’ और ‘गवनहरी’ जैसी विधाओं के साथ उसे तहज़ीब और समेकित मंचन से लोक के बीच स्थापित करने में भी प्रमुख योगदान रहा था। उन्होंने पितृसत्तात्मक समाज में लौंडा नाच जैसी अनूठी अभिव्यक्ति की शैली को स्थापित किया, जिसे समाज ने बाद में चलकर मनोरंजन के माध्यम के रूप में स्वीकृति दी। पुत्रवध, भाई विरोध जैसे नाटकों से बदलते समाज के परिवर्तित होते ढांचे पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। व्यंग्य के ज़रिए ही सही लेकिन लोक को समझाने में वह सफल रहे। ‘बेटी बेचवा’ नाटक का सामाजिक संदेश केवल रंगमंच तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने ग्रामीण चेतना की गहराइयों तक प्रवेश किया। अनेक गाँवों में इस नाटक के माध्यम से स्त्री-वेदना का ऐसा जीवंत चित्रण हुआ कि स्त्री-पुरुष सभी की आँखों में उस पीड़ा की छवि उतर आई—जब एक पिता चंद पैसों के लिए अपनी बेटी को ब्याह के नाम पर एक वस्तु की तरह बेच देता है। यह नाटक उन लोक-वृत्तों को स्पर्श करता है, जहाँ बेटियों का अस्तित्व बाज़ारू मूल्य से तय होता है। आज भी मेलों और हाटों के ऐतिहासिक दस्तावेज़ इस सामाजिक विडंबना की गवाही देते हैं, जहाँ कभी ‘लड़कियों के बाज़ार’ जैसे क्रूरतम यथार्थ देखे गए थे। धनबाद ज़िले के कुमारधुबी क्षेत्र में इस नाटक का मंचन एक ऐतिहासिक क्षण बन गया, जब पाँच सौ से अधिक प्रवासी श्रमिकों ने एक शिव मंदिर में एकत्र होकर यह सामूहिक संकल्प लिया कि वे अब अपनी बेटियों का विवाह वृद्ध पुरुषों से मात्र धन के लोभ में नहीं करेंगे। यह केवल एक नाटकीय प्रभाव नहीं था—यह एक सामूहिक आत्मबोध था, जो लोकनाट्य की चेतना से जन्मा था।
आज़ादी के पूर्व, भोजपुरी बाहुल्य क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पलायन की रही है, जहाँ बड़ी संख्या में पुरुषों को ‘गिरमिटिया मज़दूर’ बनकर विदेशी बाग़ानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। बचे हुए पुरुष ‘पूरब’ की ओर रोज़गार की तलाश में पलायन करते थे, इसलिए अधिकांश लोक- कवियों ने पलायन की पीड़ा पर कई रचनाएँ लिखी हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध भिखारी ठाकुर के द्वारा रचित ‘बिदेसिया’ है—जिसमें वह पीछे छूट गई महिलाओं (पत्नियों) का अकेलापन और विरह प्रदर्शित करते हैं, भिखारी ठाकुर ने प्रवास को व्यक्तिगत त्रासदी ना मानकर सामुदायिक समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है। बिखरे हुए दुख को सामूहिक शिकायत में बदलकर उन्होंने दर्शकों को विमर्श के लिए बाध्य किया। बिदेसिया नाटक का मंचन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, उसने स्त्री की पीड़ा को समाज के सामने रखा, जिसमें एक स्त्री अपने पति का इंतज़ार कर रही है और किसी अजनबी से—जो कि विदेश की ओर जा रहा है—अपनी वेदनाएँ प्रकट करती है।
‘पूरब’ के क्षेत्रों की—लोक-कवियों ने अलग-अलग तरह से भर्त्सना की है क्योंकि कलकत्ता और उसके आस-पास के इलाक़े रोज़गार का बड़ा केंद्र बन चुके थे, जो हज़ारों युवाओं को आकर्षित करते थे। भिखारी ठाकुर की एक प्रसिद्ध रचना का अंश इस भाव को स्पष्ट करता है—
पियवा मोर हो मत जा विदेशवा,
पूरब देश में टोना बेसी बा
पानी बहुत कमजोर
मत जा पूरबवा ए राजा मोर
इसमें एक पत्नी अपने पति से पूरब न जाने की विनती कर रही है, उसे अपने पति की चिंता तो है ही—साथ ही यह आशंका भी छिपी है कि कहीं उसका पति पराए के आकर्षण में पड़कर उससे दूर न हो जाए।
पूरबी धारा के पुरोधा, पुरबिया सम्राट ‘महेंद्र मिश्र’ ने भी अपने कई रचनाओं के द्वारा स्त्री के बिछोह और बिरह को रेखांकित किया है। ‘सैया लिहले ना खबरिया न’, ‘पपीहा के बोलिया’ तथा ‘अंगुली में डसले बिया नगीनिया’ काफ़ी प्रचलित गीत है, जो स्त्री के विरह को उजागर करते हैं।
अंगुरी में डंसले बिया नगिनिया रे, ए ननदी, दियरा जरा द,
दियरा जरा द, अपना भईया के बोला द।
पोरे-पोरे उठेला लहरिया रे, ए ननदी, अपना भइया के बुला द
पूरब गइनी रामा, पछिम गइनी, कतहूं ना मिलल शहरिया रे, ए ननदी, दियरा जरा द
अंगुरी में डंसले बिया...
तड़पेला देहिया जइसे, जल बिन मछरिया, रेगनीं के कांट भइल, बिजुरिया रे, ए ननदी, दियरा जरा द...
अंगुरी में डंसले बिया…
ग़ौरतलब है कि पुरुष होते हुए भी महेंद्र मिश्र ने स्त्री-पीड़ा का अत्यंत सूक्ष्म और संवेदनशील रूपांतरण किया है। उनके गीत ‘नगिनिया’ में यह पीड़ा प्रेम-वियोग के संकेत के रूप में सामने आती है। इसी तरह उनके दूसरे प्रचलित गीत ‘उद्धव-गोपी संवाद’ में भी उन्होंने पलायन और प्रवास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जोड़ते हुए स्त्री-वेदना को समाज के समक्ष सशक्त ढंग से प्रस्तुत किया है।
केवल पुरुष ही नहीं, आगे चलकर महिलाओं ने भी लोकगीतों के परंपरा को अपनी सशक्त आवाज़ दी। इनमें विंध्यवासिनी देवी, शारदा सिन्हा व वर्तमान समय में कल्पना पटवारी प्रमुख है। विंध्यवासिनी देवी ने सात हज़ार से भी ज़्यादा लोकगीतों का संग्रह तैयार किया और रामायण को भी भोजपुरी मैथिली में रूपांतरित किया। वह रेडियो प्रसारण के माध्यम से भोजपुरी को जन-जन तक पहुँचाने वाली पहली महिला बनीं।
शारदा सिन्हा जिन्हें ‘स्वर कोकिला’ के नाम से भी जाना जाता है, उनका योगदान भी लोकगीतों की धरोहर के संरक्षण में अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहा है, उन्होंने कई विवाह और सोहर गीतों को अपनी आवाज़ देकर अमर कर दिया। विशेष रूप से छठ गीतों में तो उनकी एक अलग पहचान है। कहते हैं छठ शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा है।
इनके लोक संगीतों ने केवल परंपरागत विधाओं को ही नहीं सँजोया, बल्कि समकालीन सामाजिक प्रश्नों को भी स्वर दिया। प्रवास और पलायन जैसे विषयों पर भी उन्होंने अपनी कला के माध्यम से गहरी अभिव्यक्ति दी। इसी संदर्भ में उनका एक अत्यंत लोकप्रिय गीत है—
पनिया के जहाज से पलटनिया बनी अईह पिया...
ले ले अईह हो,
पिया सेन्दूर बंगाल के, ले ले आईह हो…
इसमें एक स्त्री परदेस जा रहे पुरुष से अपने सिंदूर को बरकरार रखने की अपेक्षा रखती है, और साथ ही उसे सैनिक के रूप में वापस लौटते हुए देखती है।
लोकगीतों ने आम महिलाओं को भी अभिव्यक्ति का और उनकी स्वायत्तत पहचान को स्थापित करने का माध्यम प्रदान किया है। लोक की ख़ासियत ही यह है कि वह सिर्फ़ कलाकारों तक सीमित नहीं रहता बल्कि जन-जन तक पहुँचता है और कई सारे लोक तो समाज का सामूहिक सृजन हैं, जो लोक से कलाकार तक पहुँचते हैं। विवाह, प्रसव, कृषि कार्य या त्यौहार के अवसर पर जब महिलाएँ समूह में गाती हैं, तो वह एक अस्थाई सामूहिक मंच बना लेती हैं—जहाँ उनकी आवाज़ प्रमुख हो जाती है। यह उस चुप्पी को तोड़ता है जो सामान्यतः पितृसत्तात्मक ढांचे में उन पर थोपी जाती है। जब स्त्री की शिकायतें पूरे गाँव के सामने मंचित होती है, तो वह कहीं-न-कहीं सामाजिक वैधता पाती है और उनके निजी दुख सामूहिक विवेचना का विषय बनता है। शादी विवाह के अवसर में अगर आप देखें जब महिलाएँ समूह में गा रही होती हैं, तो वह अपने आप को सारे बंधनों से स्वच्छंद और मुक्त पाती हैं। ‘डोमकच’ (जलुआ) एक ऐसी ही विधा है, जहाँ महिलाएँ बारात में सारे पुरुषों के जाने के बाद, व्यंग्य के ज़रिए ही सही पितृसत्तात्मक सत्ता पर चोट करती है, जिसमें घर की कुछ महिलाएँ पुरुषों के पोशाक पहनकर पुरुष का पात्र निभाती हैं। डोमकच या कुछ कजरी गीतों में महिलाएँ व्यंग्य और हास्य का सहारा लेकर पति, ससुराल वालों के सामाजिक बंधनों पर कटाक्ष करती हैं। यह एक प्रतीकात्मक प्रतिरोध है, जिसमें अस्थाई रूप से भूमिकाओं को उलट दिया जाता है और सत्ता संरचना पर कटाक्ष होता है।
हालाँकि लोकगीतों के दो पक्ष है, एक पक्ष यह है कि इसके द्वारा महिलाएँ समाज द्वारा थोपे गए संरचनात्मक बंधनों का प्रतिरोध करती है, वहीं दूसरी ओर, अनेक बार अनजाने में वे उसी ढाँचे को पुनः स्थापित करने का साधन भी बन जाती हैं। विशेषकर विवाह-संबंधी गीतों में यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ नवविवाहिता को एक आदर्श पत्नी और बहू बनने का उपदेश दिया जाता है। इसे एक प्रचलित लोकगीत से समझा जा सकता है, जो कि नवविवाहिता के स्वागत गान के रूप में गाया जाता है—
नइ के चलॶ ए कनिया, नइ के चलॶ न
जइसे बसवा नवेला ओईसे न के चलॶ न...
कइसे नइ अम्मा कइसे नइ न
हमार नैहर के घूमलका देहिया कइसे नइ न
हमार पापा के दुलारल देहिया कइसे नइ न’
इस गीत में जहाँ एक ओर नवविवाहिता को बांस जैसे झुककर चलने को कहा जा रहा है, वहीं स्त्री की ओर से इस पर प्रतिरोध भी दर्ज है।
ऐसे कई उदाहरण लोकगीतों में विद्यमान हैं, जहाँ ग्रामीण संस्थान, निजी जीवन के साथ ही सामूहिक पीड़ा के भी सारे पहलू दर्ज है। ज़रूरत है तो इन्हें बचाकर रखने की, भोजपुरी भाषी समाज को भाषायी गौरव को पुनः प्राप्त करने के लिए, अपने इतिहास को जानना और सहेजना होगा। ग्रामीण जीवन के क्षरण के साथ-साथ अनेक लोक-विधाएँ भी धीरे-धीरे समाप्त होती जा रही हैं। अतीत में कृषि चक्र के साथ गहरे रूप से जुड़े गीत और सामूहिक प्रस्तुति ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। रोपनी और कटनी के समय विशिष्ट अवसरों पर सामूहिकता में गाए जाने वाले गीत केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थे, बल्कि वे श्रम को सांगीतिक लय प्रदान करते हुए सामुदायिकता की अनुभूति को भी गहरा करते थे। ‘चैती’, ‘फगुआ’, ‘झिझिया’, ‘पीड़िया’, ‘कजरी’ और ‘बारहमासा’ जैसी विधाएँ वर्ष भर की ऋतु-चक्र को सांगीतिक रूप से अभिव्यक्त करती थीं। इन गीतों में जहाँ एक ओर ऋतु-परिवर्तन का काव्यात्मक चित्रण मिलता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संबंधों, भावनात्मक अनुभवों और ग्रामीण जीवन की सामूहिक चेतना का भी कलात्मक रूपांतरण देखने को मिलता है।
ग़ौरतलब है कि हमसे ज़्यादा प्रयास और अच्छा काम उन देशों में हो रहा है, जहाँ बड़ी संख्या में 19वीं सदी में प्रवासी जाकर बसे। यूनेस्को ने 2016 में ‘भोजपुरी लोकगीत : गीत-गवाई’ को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया। यह परंपरा मुख्य रूप से मॉरीशस में प्रचलित है, जहाँ भोजपुरी बोलने वाले समुदाय के लोग इस गीत को विवाह के पूर्व के अनुष्ठानों में गाते हैं।
भोजपुरी लोकगीतों का सबसे विशिष्ट पहलू है इसका ‘प्रवासी स्वरूप’। 19वीं सदी में जब हज़ारों मज़दूर गिरमिटिया अनुबंध पर कैरेबियन, फ़िजी, मॉरीशस और अफ़्रीका ले जाए गए, तो वे भोजपुरी लोकगीतों को भी साथ ले गए। वहाँ ये गीत स्थानीय संस्कृति से मिलकर एक हाइब्रिड रूप में विकसित हुए। आज भी त्रिनिदाद एंड टोबैगो, सुरिनाम, फ़िजी और मॉरीशस में भोजपुरी लोकगीत, ख़ासकर चौता, सोहर और बिदेसिया, सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बने हुए हैं।
ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ लोकगीतों की परंपरा पूरी तरह से लुप्त हो गई है। आज भी अनेक कलाकार इस सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और जीवित रखने में सक्रिय हैं। भरत शर्मा, विष्णु ओझा, मदन राय, कल्पना पटवारी और चंदन तिवारी जैसे युवा कलाकार अपनी पूरी क्षमता से इस प्रयास में योगदान दे रहे हैं। विशेष रूप से भरत शर्मा को वर्तमान समय में निर्गुण के सरताज के रूप में सम्मानित किया जाता है; बिरह और वियोग जैसे पारंपरिक गीतों में उनकी पकड़ दृढ़ है।
साथ ही, उन्होंने आधुनिक समाज में प्रचलित कुरीतियों पर भी कई गीत रचे हैं। इनमें दहेज प्रथा पर उनकी प्रतिक्रिया विशेष रूप से उल्लेखनीय है।
जनतीं जे जारल जइबू आग में,
दहेज के पाप नाहीं करती हो बेटी ससुरा में भेज के…
यह गीत 21वीं सदी में उसी प्रभाव और सामाजिक चेतना का माध्यम बन गया है, जिसे 20वीं सदी में ‘बेटी बेचवा’ गीत के माध्यम से लोक समुदाय में प्रदर्शित किया गया था।
आज भी जब वैश्वीकरण और आधुनिकता ग्रामीण सामूहिकता को चुनौती दे रही है, तब यह आवश्यक हो जाता है कि भोजपुरी भाषी समाज अपनी धरोहर को पुनः प्राप्त करने और संरक्षित करने के लिए सजग बने। ग्रामीण उत्सवों, विवाह, छठ पर्व, नाच-गान और प्रवासी गीत जैसे माध्यम लोक गीतों को जीवित रख सकते हैं और सामाजिक चेतना को अगली पीढ़ी तक पहुँचा सकते हैं। यह स्वीकार करना कि लोकगीत केवल अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक चेतना और सामूहिक स्मृति का माध्यम हैं, हमारे लिए एक ज़िम्मेदारी बन जाता है।
भोजपुरी लोकगीतों का अध्ययन, संरक्षण और पुनरुत्थान केवल भाषा और संस्कृति की रक्षा नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन, स्त्री-शक्ति और सामाजिक न्याय की स्थायी अवधारणाओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का एक अनिवार्य माध्यम है। इसके संरक्षण और प्रसार में हम जितना जागरूक रहेंगे, हमारी सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक संवेदनशीलता उतनी ही सशक्त होगी।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
