क्या एडम और ईव ब्लैक थे?
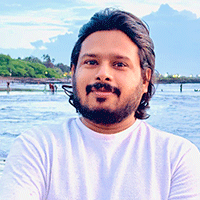 शिवेन्द्र
06 अप्रैल 2025
शिवेन्द्र
06 अप्रैल 2025
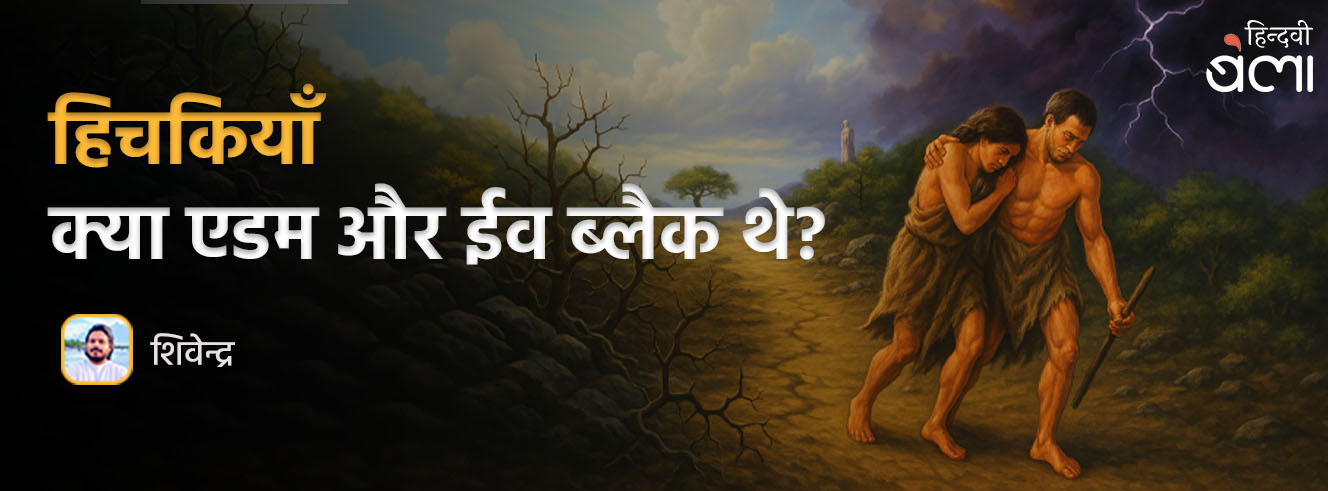
‘क्या एडम और ईव ब्लैक थे?’
इन सात शब्दों का गल्प और यथार्थ से गहरा संबंध है और इसे मैं वैसे ही साबित करूँगा जैसे नौंवी कक्षा में हमसे यह सिद्ध करवाया जाता था कि √2 (रूट टू) एक अपरिमेय (Irrational) संख्या है। तो सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि—क्या एडम और ईव ब्लैक थे?
इसका गल्प और यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। वैसे क्या आपने ध्यान दिया कि इस सवाल में सात नहीं छह शब्द हैं और एक प्रश्न चिह्न। इस प्रश्न-चिह्न का एक छोटा-सा इतिहास है, जिसे यहाँ जान लेना समीचीन होगा—पहले लैटिन में किसी प्रश्न को इंगित करने के लिए वाक्य के अंत में क्वेस्टियो शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। जल्द ही क्वेस्टियो को लिखते समय जगह बचाने के लिए, क्यू-ओ (q-o) कर दिया गया। बाद में ओ सिर्फ़ एक बिंदु बन गया और क्यू एक घुमावदार रेखा, जिससे हमें हमारा वर्तमान प्रश्नचिह्न मिला। वैसे तो लिपि के आ जाने के बाद से संकेत गौण होते चले गए, पर हम चाहे किसी भी भाषा में सोचते और रचते हों, आज भी संकेतों के बिना हमारा काम नहीं चल सकता और साहित्य में तो संकेत हस्ताक्षर की तरह होते हैं। शब्दों के लय के बीच छुपे संकेतों के द्वारा ही हम किसी भी रचनाकार को जानते-पहचानते और सेलिब्रेट करते हैं।
ख़ैर, पहले हमने माना था कि—क्या एडम और ईव ब्लैक थे? इसका गल्प और यथार्थ से कोई संबंध नहीं है। अब आइए इस समीकरण को आगे बढ़ाते हैं। नौंवी कक्षा में जब हमें यह रटाया गया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तब यह मानते ही कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं है, पता नहीं कैसे हमें यह छूट मिल जाती थी कि अब हम यह लिख सकें कि √2=a/b, जहाँ a और b सह-अभाज्य संख्याएँ हैं अर्थात् एक के अतिरिक्त उनका कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका कारण ना तब समझ आया था और ना ही अब तक आया है, पर यह गणित का आख्यान नहीं है, इसलिए हम पहले गल्प और यथार्थ को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे भले ही यह सवाल साहित्य के नौंवी कक्षा का ही क्यों न हो!
एक मिनट, पता नहीं क्यों गल्प और यथार्थ के बारे में सोचना शुरू करते ही मुझे हिचकी आने लगती है। अब चाहे तो परंपरावादी लेखकों की तरह मैं भी यह कह सकता हूँ कि हिचकी भगवान की कृपा या डिवाइन-इंटरवेन्ससन से आती है या भावुक प्रेमियों की तरह यह कि ज़रूर मेरा कोई प्रिय मुझे याद कर रहा होगा या युधिष्ठिर की तरह आधा-अधूरा सच बोलकर, हमेशा साहित्य के महाभारत में अव्वल रहने वाले सुविधाभोगियों की तरह कुछ ऐसा, जिससे कभी मेरी विचार-प्रक्रिया का पता ही न चल पाए, पर इस सबसे बचते हुए मैं अपनी हिचकियों के आत्म तक जाने की कोशिश करूँगा, ताकि गल्प और यथार्थ के चारों ओर गोल-गोल घूमने की बजाय हम सीधे उनकी नाभि तक पहुँच सके।
तो मेरी पहली हिचकी एक दार्शनिक प्रमाण है। एक दर्शन है अद्वेतवाद, जिसे जन्म तो बौद्ध धर्म ने दिया, पर उसे गोद ले लिया गौड़पादाचार्य ने और फिर शंकराचार्य ने उसे पाल पोसकर बिल्कुल अपना बना लिया। वही शंकराचार्य जगत और ईश्वर के संबंध को समझाने के लिए एक नर्तक का उदाहरण देते हैं। वह कहते हैं कि जब नर्तक नाचता है तो उससे नाच पैदा होता है और जैसे नाच और नर्तक को अलग-अलग नहीं किया जा सकता, ठीक उसी तरह ईश्वर और संसार को अलग-अलग समझना अज्ञान है। अब यह बात सच है या नहीं, मैं यह नहीं जानता, पर गल्प और यथार्थ के संदर्भ में भी मुझे शंकर का यह तर्क बहुत सटीक लगता है, इसलिए मैं सिर्फ़ यह कहना चाहता हूँ कि गल्प और यथार्थ भी दो नहीं हैं, वह बस हमें दिखते दो हैं पर अस्ल में वह हैं अद्वैत।
अब सवाल यह उठता है कि जब दोनों एक ही हैं तो फिर इन्हें लेकर इतने विवाद, बहस और आयोजन क्यों होते रहते हैं? ओह! यह हिचकी, एक बार फिर से शुरू हो गई। यह यथार्थवादियों की हिचकी है। वैसे तो चार्वाक और प्लेटो बहुत पहले ‘मैं कहता आख़िन की देखी’ जैसी बातें कर गए थे और फिर जॉन लॉक और कांट जैसे अनुभववादियों (empiricist) ने भी इस राह आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया था, पर यथार्थवाद को सही ज़मीन तभी मिल पाई, जब डार्विन, कार्ल मार्क्स और फ़्रायड ने क्रमशः जीव, जगत और मन को, आसमान में रहने वाले ईश्वर से बिल्कुल जुदा कर दिया और फिर जब नीत्शे ने अपना ज़हर बुझा ख़ंजर ईश्वर के सीने में उतारा और फिर भी वह चुप रहा तो यथार्थवादियों का हौसला बढ़ता चला गया और वे चित्रकला, साहित्य और कला के हर रूप पर हावी होते चले गए, जिसमें अगर देखा जाय तो कोई बुराई नहीं थी। पर अति सर्वत्र वर्जयेत और उससे भी बढ़कर कलाकार एक ही बात से बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं और अगर वे कुछ नया न भी कर पाए तो भी वे हर सत्ता को रोटी की तरह, तवे पे उलटते-पलटते रहने के लिए कसमसाय रहते हैं और फिर हर नई आमद पुरानों से दो-दो हाथ करना चाहती है। शायद इन्हीं सब मिले-जुले कारणों से जन्म हुआ कलावाद का।
अब यह हिचकी अचानक से नाराज़ क्यों लग रही है? कहीं यह कलावादियों की हिचकी तो नहीं? हाँ-हाँ समझ गया। स्वस्फूर्त कला को भला कौन रोक सकता है। कह लो जो तुम्हें कहना है।
पहली बात तो यह कि तुम हमारा ग़लत इतिहास बयान कर रहे हो। कलावाद का जन्म कोई आधुनिक घटना नहीं है। बल्कि प्लेटो द्वारा कवियों को देश निकाला दिए जाने के तुरंत बाद, उनके शिष्य अरस्तू ने काव्यकला को नीतिशास्त्र से अलग करते हुए, एकमात्र आनंद को कला का लक्ष्य घोषित कर दिया था। आगे चलकर जिस फ़्रांस में यथार्थवाद ने ज़ोर पकड़ा, वहीं से ‘कला कला के लिए’ वाली धारा पूरे वेग से उमड़ी। तुम्हारी हिंदी में भी पूरा का पूरा एक काल चला है—रीतिकाल और जब प्रेमचंद यथार्थवाद का परचम लहरा रहे थे, तब भी प्रसाद ‘आँसू’ का महाआख्यान रच रहे थे।
“ठीक है, सुन लिया मैंने तुम्हें। अब अपनी ये हिचकियाँ बंद करो, तो मैं भी अपनी कुछ बातें कह लूँ?”
ख़ुदा ख़ैर करे। बंद हो गईं हिचकियाँ। कितनी देर के लिए पता नहीं, पर इससे पहले कि वह फिर हाज़िर हो जाए, मैं गल्प और यथार्थ के संबंध को आगे बढ़ाता हूँ। हाँ तो जैसा कि मेरी नाराज़ हिचकी कह रही थी, यह सच है कि कला और यथार्थ का झगड़ा बहुत पुराना है और कलावादी चित्रकार जेम्स एबॉट मैकनील ह्वीस्लर (1834-1903 ई.) और अँग्रेज़ी के प्रख्यात समालोचक रस्किन के बीच यह झगड़ा इस हद तक बढ़ गया था कि रस्किन ने यहाँ तक कह दिया था कि ह्वीस्लर अपने चित्रों के माध्यम से दर्शकों के चेहरों पर रंगभरी प्यालियाँ उँड़ेल देता है, जिससे नाराज़ होकर ह्वीस्लर ने रस्क्नि पर मुक़द्दमा कर दिया और उस मुक़द्दमे को जीत भी लिया; पर इसके बदले ह्वीस्लर को मिला सिर्फ़ एक फादिंग (इंग्लैंड में प्रचलित सबसे छोटा सिक्का)। आज के शब्दों में कहें तो एक रुपया। मतलब कला और यथार्थ की लड़ाई में कभी किसी को ढेले भर से अधिक हासिल नहीं हो सकता। उसके विपरीत अगर दोनों एक हो जाएँ, एक दूसरे से गलबहियाँ कर लें तो अनमोल हो सकते हैं। इस वजह से भी मैं दोनों को अलग-अलग नहीं बल्कि एक ही मानने का पक्षधर हूँ।
नहीं नहीं नहीं। अब और हिचकी नहीं। क्या कहा तुम एक कथाकार की हिचकी हो? यार अब यह धर्मसंकट में डाल दिया तुमने मुझे। चलो ठीक है, जो भी कहानी सुनानी है, जल्दी से सुनाकर ख़त्म करो।
तो मित्रो, एक समय की बात है—दो आदमी थे, एक का नाम था कला और दूसरे का यथार्थ। एक की आत्मा बेचैन रहती थी और दूसरे के घर के पिछवाड़े जब तब साँप निकल आते थे। दोनों परेशान थे। कला ने घोर साधना की और यथार्थ अपनी समस्या को लेकर पूरी दुनिया घूम गया। आख़िरकार कला को स्वप्न में और यथार्थ को एक गुणी आदमी से पता चला कि एक जंगल में एक जादुई लकड़ी है, जिससे दोनों की समस्या का समाधान हो सकता है। बस अंतर इतना था कि कला को उस लकड़ी से बाँसुरी बनाना था और यथार्थ को लाठी। दोनों भागते हुए उस जंगल में पहुँचे और एक साथ उस जादुई लकड़ी को उठा लिया। फिर क्या था दोनों लड़ पड़े। दोनों एक-दूसरे को यह समझाने की कोशिश करने लगे कि उनके लिए यह जादुई लकड़ी कितनी ज़रूरी है। यथार्थ का कहना था कि मेरे घर में आग लगी है और तुम्हें बाँसुरी बजानी है, जबकि कला का मानना था कि अगर अंदर सुकून न हो तो बाहर के साँप को मारने का कोई फ़ायदा नहीं। दोनों एक दूसरे से असहमत थे और इसलिए उनकी वह लड़ाई आज तक जारी है।
अब सवाल यह उठता है कि वह जादुई लकड़ी दोनों में से किसे मिलनी चाहिए? कौन उसका ज़्यादा हक़दार है? किसे उसकी ज़्यादा ज़रूरत है? कला को या यथार्थ को? इसका उत्तर मैं आप लोगों की अपनी संवेदना, समझ और ज़रूरत पर छोड़ता हूँ और यहाँ सिर्फ़ यह बताकर, यह कहानी ख़त्म करना चाहता हूँ कि उस जादुई लकड़ी का नाम था—गल्प। बिना गल्प के न कोई कला निखर सकती है और न ही कोई यथार्थ ग्राह्य बन सकता है, इसलिए साहित्य का सबसे ज़रूरी तत्व है—गल्प।
अगर हिचकियों ने आपको भटका न दिया हो तो आपको याद होगा कि हम यह साबित करने निकले थे कि—क्या एडम और ईव ब्लैक थे? इसका गल्प और यथार्थ से गहरा संबंध है। अब चूँकि हम दोनों यह कुछ हद तक समझ चुके हैं, इसलिए नौंवी कक्षा वाले अपने गणित को आगे बढ़ा सकते हैं। उस गणित में बहुत सारा गुणा-भाग और वैल्यू के अदला-बदली के बाद यह निकलकर आता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी आरंभिक सोच को ग़लत साबित करता है और फिर खट्ट से यह सिद्ध हो जाता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी तक हमने कोई ऐसा गुणा-भाग नहीं किया है, जिससे ‘क्या एडम और ईव ब्लैक थे?’ का गल्प और यथार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। यह स्थापना ग़लत साबित हो सके और वैसे तो साहित्य में गणितबाज़ी दिन-पर-दिन बढ़ती ही जा रही है, फिर भी इस स्थापना को ग़लत ठहराने का कोई गणित नहीं है मेरे पास। फिर हम क्या करें?
अगर आपको याद हो तो मैंने ऊपर छह शब्दों और एक प्रश्नचिह्न का ज़िक्र किया था। अब वही प्रश्नचिह्न हमारे काम आने वाला है। वैसे यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि ‘क्या एडम और ईव ब्लैक थे?’ यह प्रश्न गैलियानो का है। वह अपनी किताब ‘Mirrors: The story of almost everything’ की शुरुआत इसी प्रश्न से करते हैं। ऐसा क्यों, यह तो उनसे किसी ने नहीं पूछा, पर अगर इसकी गहराई में जाएँ तो इस एक पंक्ति में अतीत और आधुनिकता, मिथ और साइयन्स, कला और विचार एक साथ मौजूद हैं। लगभग पूरी दुनिया में एडम और ईव को उसी तरह प्रथम पुरुष और स्त्री माना जाता है, जैसे हमारे यहाँ मनु और सतरूपा को, पर विज्ञान यह कहता है कि पहले होमोसेपियंस अफ़्रीका में जन्मे और इस समय हम चहुंतरफ़ा विज्ञान से घिरे हुए हैं। फिर भी शायद ही हमारा ध्यान इस पर गया होगा कि क्या एडम और ईव या आदम और हव्वा या मनु और सतरूपा अफ़्रीका में जन्में लोगों की तरह ब्लैक थे?
इसमें हमारी भी कोई ख़ास ग़लती नहीं है। अगर किसी की ग़लती है तो वह हमारी कंडिशनिंग की, पर गैलियानो सिर्फ़ एक वाक्य से, सिर्फ़ छह शब्दों और एक प्रश्नचिह्न से हमें हमारी कंडिशनिंग से बाहर निकाल लाते हैं। वह यथार्थ को नहीं छोड़ते और न ही कला को अपने हाथ से छिटकने देते हैं, क्योंकि वह गल्प नामक जादुई छड़ी का, बिल्कुल सटीक इस्तेमाल करना जानते थे। मतलब गल्प वह हुनर है जिसमें कला और यथार्थ एक साथ मौजूद होते हैं और साहित्य का गल्प, साधारण गल्प से इस मायने में अलग होता है कि वह सिर्फ़ हमारा मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि हमें हमारी कंडिसिनिंग से बाहर भी निकालता है, हमसे कुछ कठिन सवाल भी पूछता है और हमारी ठहरी हुई यात्रा को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है और गैलियानों का एक वाक्य इन सारी शर्तों को पूरा करता है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि ‘क्या एडम और ईव ब्लैक थे?’ इसका गल्प और यथार्थ से गहरा संबंध है।
इति सिद्धम।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
