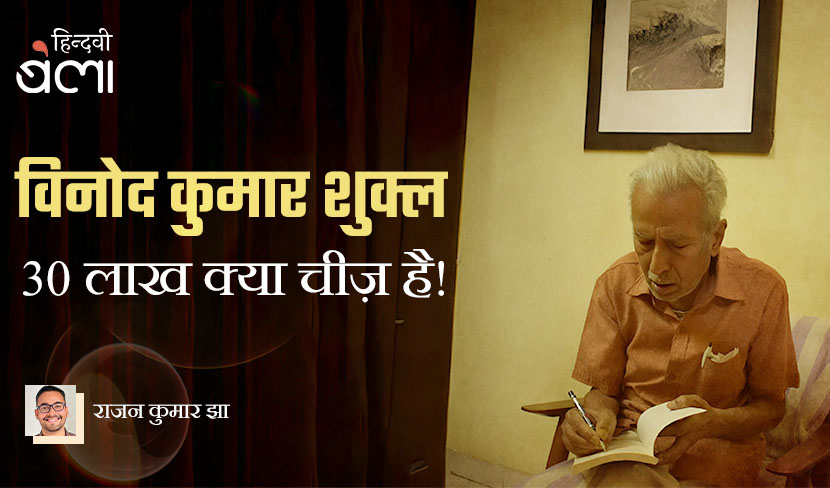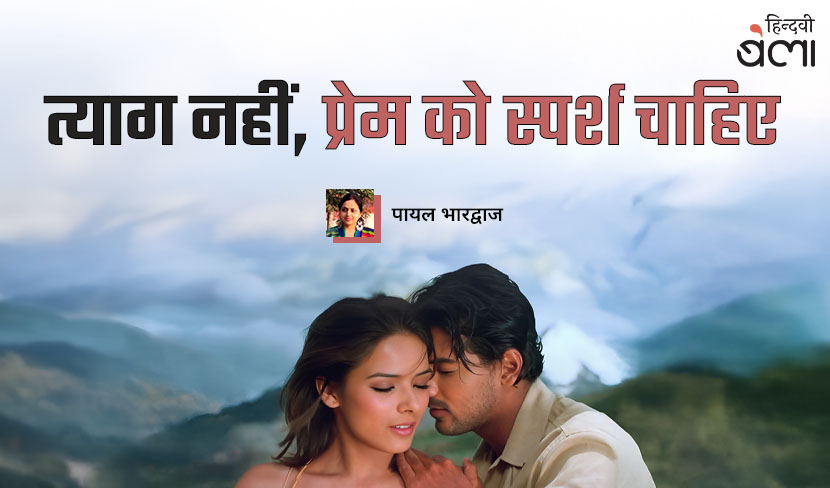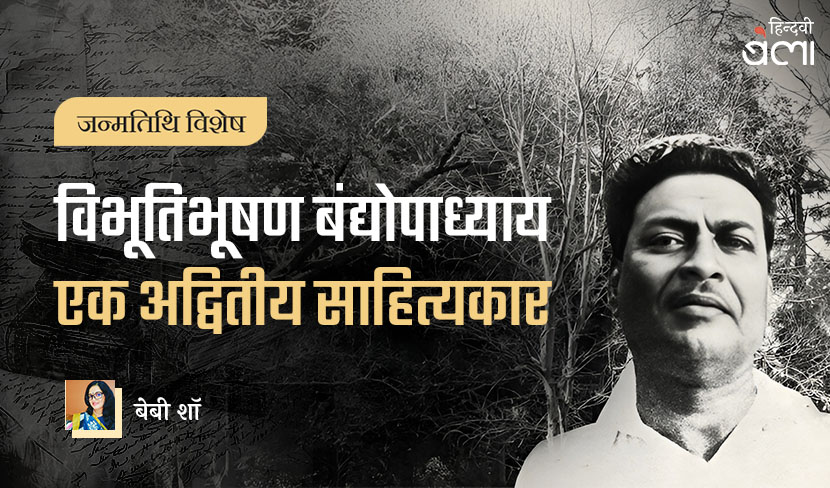सिनेमा में प्रेमचंद : साहित्य, बाज़ार और प्रतिरोध
 ध्रुव हर्ष
23 अक्तूबर 2025
ध्रुव हर्ष
23 अक्तूबर 2025

“जिन हाथों में फ़िल्म की क़िस्मत है, वे बदक़िस्मती से इसे इंडस्ट्री समझ बैठे हैं। इंडस्ट्री को ‘मज़ाक़’ और इसलाह से क्या निस्बत? वह तो एक्सप्लायट करना जानती है और यहाँ इंसान के मुक़द्दसतरीन (पवित्रतम) जज़्बात को एक्सप्लायट कर रही है। बरहना (नग्न) और नीम-बरहना (अर्द्ध नग्न) तस्वीरें, क़त्ल-ओ-ख़ून और जान की वारदातें, मार-पीट, ग़ुस्सा, जज़्बात और नफ़्सानियत ही इस इंडस्ट्री के औज़ार हैं और इन्हीं से वह इंसानियत का ख़ून कर रही है।”
ये प्रेमचंद के शब्द हैं। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह अपने लेखन को लेकर कितने संजीदा और ईमानदार थे। वह लेखक होने की ज़िम्मेदारी को बख़ूबी समझते थे, इसलिए उनका लेखन कुछ भी महज़ कह लेने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उस दौर की प्रतिनिधि आवाज़ बनकर उभरा। नहीं तो ‘सोज़े वतन’ (1910) लिखने के बाद उनपर अँग्रेज़ बहादुर सिडिशन का मुक़दमा न चलाते। वह तीखी-से-तीखी बात भी बड़े सहज होकर कहते। यदि उनके वाक्य-विन्यास व शब्द संरचना की बात करें, तो उनकी लेखनी में किसी कुशल पटकथाकार की तरह देसी और दृश्यात्मक तत्वों का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। ख़ैर, उनका फ़िल्मों में सफल न होना एक अलग विषय है। और वह भी किसी एक फ़िल्म से प्रेमचंद जैसे महान् लेखक की सफलता और असफलता का आकलन नहीं किया जा सकता है। साहित्य लेखन में अच्छा ख़ासा मुक़ाम हासिल करने के बाद उन्होंने फ़िल्मों की तरफ़ रुख़ किया था। वजह आर्थिक तंगी थी या कि सिनेमा ने वाक़ई में उन्हें अपनी तरफ़ आकर्षित किया था, यह कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हालाँकि, कुछ लेखों, दस्तावेज़ों और पत्रों को पढ़ने से यह बात सामने आई है कि ऐसा उनका फ़िल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ‘हंस’ और ‘जागरण’ पत्रिकाओं के संपादन में हुई आर्थिक हानि की वजह से उन्होंने फ़िल्मों के लिए लिखने का मन बनाया था। ख़ैर, उन्हें इस बात से शिकायत ज़रूर थी कि लोग उनकी वाहवाही तो ख़ूब करते हैं, लेकिन किताबें तो उतनी बिकती नहीं। मुंबई पहुँचने के बाद प्रेमचंद ‘अजंता सीनेटोन’ नाम की एक कंपनी में कहानी और संवाद लेखक का पदभार सँभालते हुए अपनी पत्नी शिवरानी देवी को पत्र लिखते हैं, “अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि यहाँ रह भी सकूँगा या नहीं। जगह बहुत अच्छी है, साफ़-सुथरी सड़कें, हवादार मकान, लेकिन जी नहीं लगता। जैसी कहानियाँ मैं लिखता हूँ, उन्हें निभाने के लिए यहाँ कोई एक्ट्रेस नहीं है। मेरी एक कहानी यहाँ सबको अच्छी लगी, लेकिन यहाँ की एक्ट्रेस उसे निभा नहीं सकती। उसे निभाने के लिए कोई पढ़ी-लिखी एक्ट्रेस रखनी पड़ेगी। मैं तो ऐसी ही कहानियाँ लिखूँगा। इन लोगों की इच्छानुसार तो मैं लिख नहीं सकता।” और उसी दिन अपने साथी और लेखक जैनेंद्र कुमार को लिखते हैं, “पत्र पहुँचा। मकान ले लिया। यहाँ दुनिया दूसरी है, यहाँ की कसौटी दूसरी है। अभी तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ।” और फिर 24 जून 1934 को पत्नी को इस संबंध में फिर से अपने विचार लिखते हैं, “यह एक बिल्कुल नई दुनिया है। साहित्य से इसका बहुत कम सरोकार है। इन्हें तो रोमांचकारी, सनसनीखेज़ तस्वीरें चाहिए। अपनी व्याप्ति को ख़तरे में डाले बग़ैर, मैं जितनी दूर तक डायरेक्टरों की इच्छा पूरी कर सकूँगा, उतनी दूर तक करूँगा; मुझे करना पड़ेगा। ज़िंदगी में समझौता करना ही पड़ता है। आदर्शवाद महँगी चीज़ है और बाज़ औक़ात उसको दबाना पड़ता है।”
इन पत्रों को पढ़ने पर यह बात साफ़ ज़ाहिर होती है कि प्रेमचंद एक क़िस्म के पशोपेश में थे। वह साहित्य और सिनेमा के बीच सामंजस्य बिठाने और उसके पेचोख़म को समझने में लगे थे, या यह भी कह सकते हैं कि वह ख़ुद को समझाने में लगे हुए थे, क्योंकि यह रास्ता उन्होंने ख़ुद चुना था। यह द्वंद्व हर संजीदा लेखक के अंदर होता है जो सिनेमा को एक कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम मानता है। वह इस बात को स्पष्ट भी करते हैं कि सिनेमा एक अलग मीडियम है, जिसमें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं।
अमृतराय ने ‘प्रेमचंद : क़लम का सिपाही’ में ‘मज़दूर’ फ़िल्म की विस्तार से जानकारी दी है। अमृतराय लिखते हैं, “गोदान पर काम चल रहा था, मगर चींटी की चाल से। उधर ‘मज़दूर’ बनना शुरू हो गई थी। जैसा कि ज़ियाउद्दीन बर्नी साहब कहते हैं, जो उन दिनों बंबई में ही थे और मुंशीजी से अक्सर मिलते रहते थे, और जिसकी तसदीक़ उसके निर्देशक मोहन भवनानी ने भी की, इस फ़िल्म की कहानी का ढांचा कंपनी ने तैयार किया था और उस पर चमड़ी और गोश्त मुंशीजी साहब ने मढ़ दिया था।” हालाँकि कहानी अति नाटकीय थी, जिसका उद्देश्य यह दर्शाना था कि पूँजीपति उदार और उन्नत विचारों का होकर देश का, जनता का कितना भला कर सकता है। बात थोड़ी प्रेमचंद के मन की थी और नहीं भी। इतने कम समय में उन्होंने मोटा-मोटी फ़िल्म जगत की मिज़ाज को बख़ूबी समझ लिया था और वे अपने चुनाव से ख़ुश नहीं थे। इतने कम समय में मुंबई फ़िल्म जगत की जो तस्वीर उन्होंने सबके सामने रखी, उसका आज भी सूरत-ए-हाल कमोबेश वही है। मतलब बाज़ार का वही स्वभाव है, किसी भी हाल में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना। फ़िल्म को कला की अभिव्यक्ति से ज़्यादा एक इंडस्ट्री की तरह शुरुआत से देखा जाता रहा है। जिसमें रचनात्मकता की गुंजाइश; क्या चलेगा, क्या नहीं, इस पर निर्भर होता है, जबकि क्रिएटिविटी का मतलब नयेपन और प्रगतिशील होने से है।
जहाँ साहित्य विषमताओं और बने-बनाए ढर्रे को तोड़ने की बात करता है, वहीं सिनेमा ख़ासा एक पैटर्न और फ़ार्मूले पर काम करता है, जिसमें वह लेखक से फ़िल्म सफल होने की गारंटी फ़िल्म के निर्माण से पहले ही चाहता है। आज जब फ़िल्म जगत के लोग किसी विषय को कहानी कम और कंटेंट ज़्यादा समझते हैं, तो कला कम और बाज़ार में बना एक उत्पाद ज़्यादा दिखता है।
जब प्रेमचंद मुंबई गए थे, उस समय सिनेमा को किसी जादुई आविष्कार की तरह देखा जाता था। तब तक हिंदी फ़िल्मों ने लोगों की चेतना को बड़े पैमाने पर प्रभावित करना शुरू कर दिया था। फ़िल्मों को लेकर आम जनता का रुझान बढ़ने लगा था। सिनेमा के अस्तित्व में आने से बहुत सारे मिथक टूट गए थे। थिएटर और लेखन से तमाम लोगों ने फ़िल्मों की तरफ़ शिफ्ट कर लिया था। इस वजह से हो सकता है कि प्रेमचंद ने फ़िल्मों में हाथ आजमाने की सोची हो। मुंबई पहुँचने के बाद उन्होंने अजंता सीनेटोन कंपनी के लिए ‘द मिल/मज़दूर’ (1934) नाम की एक फ़िल्म लिखी, जो कि उनकी लिखी पहली और आख़िरी फ़िल्म थी। फ़िल्म को मुंबई में प्रतिबंधित कर दिया गया। बॉम्बे बोर्ड ऑफ़ सर्टिफिकेशन (बीबीएफ़सी) ने कहा कि यह फ़िल्म बॉम्बे प्रेसीडेंसी क्षेत्र में प्रदर्शन के उपयुक्त नहीं है। वजह उस समय फ़िल्म बोर्ड के मेंबर रहे मुंबई के जाने-माने उद्योगपति और मिल ओनर्स एसोसिएशन के सभापति सर जीजाभाई स्वयं ही फ़िल्म के ख़िलाफ़ थे। निर्माता और सेंसर बोर्ड के बीच बहुत रस्साकशी हुई। उस समय मुंबई के पुलिस कमिश्नर मिस्टर विल्सन के सुझाव से कई कट लगने के बाद भी फ़िल्म से प्रतिबंध नहीं हटा। चूँकि ज़्यादातर सिनेमाघर टेक्सटाइल मिलों के आस-पास थे, इस वजह से फ़िल्म बोर्ड को यह डर था कि फ़िल्म देखकर मिल मज़दूर कहीं मालिकों के ख़िलाफ़ लामबंद होकर आंदोलन न करने लगे। कई लोगों ने निर्देशक और निर्माता को ये भी सलाह दी कि फ़िल्म का क्लाइमेक्स गांधीवादी कर दो; फ़िल्म रिलीज़ होने में आसानी होगी। संभवतः इसी उठापटक और अपने विषयवस्तु से इतनी छेड़छाड़ और सेंसरशिप देखकर प्रेमचंद आहत हुए और वह 1934 में ही मुंबई (बॉम्बे) से वापस बनारस चले गए। उनकी मायानगरी से बेरुख़ी की एक वजह ये भी हो सकती है।
कुछ लेखों से यह भी पता चलता है कि 1934 में इस फ़िल्म को पंजाब सेंसर बोर्ड से प्रमाण पत्र लेकर लाहौर के इंपीरियल सिनेमाघर में रिलीज़ किया गया था। मुंबई सेंसर बोर्ड में फँसने की वजह से फ़िल्म पहले से ही चर्चित हो गई थी। फ़िल्म के निर्माता मोहन भवनानी का कहना था, “पहले ही रोज़ साठ हज़ार मज़दूरों की भीड़ सिनेमा हॉल के फाटक पर जमा हो गई थी और सात रोज़ तक कुछ इसी तरह का हाल बना रहा। फाटक पर भीड़ की रोकथाम के लिए पुलिस और मिलिट्री का बंदोबस्त करना पड़ा। आख़िरकार पंजाब सरकार ने भी घबराकर ‘मिल मज़दूर’ पर रोक लगा दी।”
ख़ैर, बाद में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ अन्य शहरों में भी फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, लेकिन वहाँ पर भी फ़िल्म की बदक़िस्मती ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। एक अफ़वाह यह भी थी कि दिल्ली में कोई मज़दूर किसी मिल मालिक के कार के सामने आकर लेट गया था, जिससे अच्छा ख़ासा हंगामा खड़ा हो गया। बाद में हड़ताल और आंदोलनों की वजह से फ़िल्म दिल्ली में भी रोक दी गई। इससे जुड़ा एक दिलचस्प वाक़या है—कहते हैं कि प्रेमचंद के प्रिंटिंग प्रेस के मज़दूरों ने भी फ़िल्म से प्रेरित होकर हड़ताल कर दी थी। जितना बड़ा काम फ़िल्म निर्माण है, उससे बड़ा काम फ़िल्म को दर्शकों के बीच पहुँचाना होता है। इसमें किसी लेखक का अधिकार अपने विषय पर तभी तक रहता है, जब तक वह उस विषय पर काम कर रहा होता है। इसलिए आपने अक्सर सुना होगा कि किताब अच्छी थी, लेकिन फ़िल्म उतनी अच्छी नहीं बन पाई। इसी वजह से बहुत सारे बड़े लेखक फ़िल्मों में उतने सफल नहीं हो पाए। ऐसे साहित्यकारों की एक बड़ी फ़ेहरिस्त है, जिसमें प्रेमचंद से लेकर रेणु और काशीनाथ सिंह जैसे बड़े नाम शामिल हैं।
उदाहरण के तौर पर ‘मिडनाइट्स चिल्ड्रेन’ सलमान रश्दी का चर्चित उपन्यास है। उस पर दीपा मेहता ने 2012 में ‘मिडनाइट्स चिल्ड्रेन’ नाम से ही एक फ़िल्म बनाई; पटकथा स्वयं उपन्यास के लेखक रश्दी ने लिखी, फिर भी फ़िल्म उपन्यास के मुक़ाबले कमज़ोर साबित हुई। इसलिए जब किसी कहानी या उपन्यास पर फ़िल्में बनती हैं तो ऐसा होना लाज़िमी है। इसलिए लेखक, फ़िल्मकार और निर्माता के बीच ये द्वंद्व चलते रहते हैं।
रह रहकर फ़िल्म ‘मज़दूर’ को कई बार रिलीज़ और री-रिलीज़ करना पड़ा। सन् 1937 में एक बार फिर फ़िल्म के मामले को उभारा गया। कई हिंसात्मक दृश्य को काट-छाँटकर फ़िल्म को रिलीज़ किया गया। अमेरिका की मशहूर पत्रिका ‘एशिया’ में फ़िल्म पर एक रिव्यू छपा, जिसमें फ़िल्म के कथानक पर खुलकर बात की गई थी।
हालाँकि, कुछ लेखों और पत्रों से यह भी बात सामने आई है कि प्रेमचंद की मृत्यु के बाद ‘द मिल/मज़दूर’ को 5 जून 1939 को मुंबई समेत उत्तर भारत के अलीगढ़ और लखनऊ जैसे कुछ और शहरों में रिलीज़ किया गया। इस फ़िल्म में प्रेमचंद ने सरपंच का एक छोटा-सा किरदार भी किया था। फ़िल्म की कहानी में एक नौजवान अपने पिता के टैक्सटाइल कंपनी का मालिक बन जाता है, लेकिन वह मिल के मज़दूरों पर अत्याचार करता है। हालाँकि मिल मालिक की बहन मज़दूरों के साथ उनके हक़ के लिए खड़ी होती है। फ़िल्म की विषयवस्तु पूँजीवादी संरचना के मुफ़ीद नहीं थी। ऐसा नहीं कि फ़िल्म का कथानक कमज़ोर था या प्रेमचंद को फ़िल्म मीडियम का अंदाज़ा नहीं था, बल्कि तब तक वह हिंदी साहित्य के स्टार लेखक बन चुके थे। उनका लेखन फ़िल्म के माध्यम से आम जन मानस तक अगर बिना किसी रोकथाम के पहुँचता, तो सराहना होनी तय थी। फ़िल्म के दौरान वह काफ़ी बेचैन थे और अपने लेखों और पत्रों में इसका इज़हार भी करते रहे। उन्होंने फ़िल्म माध्यम को लेकर एक लेखक के तौर पर अपनी विवशता भी प्रकट की, लेकिन फिर भी उन्होंने समझौता नहीं किया, क्योंकि उनका मूल स्वभाव तो प्रतिरोध और मार्जिनलाइज्ड क्लास के साथ खड़े होने का ही था। वह स्वभाव से एगेलिटेरियन थे। वह हरगिज़ इंसान और इंसान के बीच के अंतर को कम करने और एक हद तक सबको एक पायदान पर लाने के हिमायती थे। फ़िल्म को हर दौर में कहीं-न-कहीं एक सोशियो-पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया गया है। कभी-कभी फ़िल्म निर्माण से लेकर रिलीज़ तक के बीच में एक निर्देशक और निर्माता को न जाने कितने समझौते करने पड़ते हैं। जो फ़िल्म प्रेमचंद ने मज़दूरों के अधिकार और प्रतिरोध के लिए लिखा था, वो फ़िल्म दर्शकों तक पहुँचते-पहुँचते कुछ और हो गई थी। कैसी विडंबना है कि उसी फ़िल्म के प्रचार में फेरबदल के बाद यह लिखा गया कि मिल मालिक और मिल मज़दूर इसे साथ देखें तो हड़ताल रोकी जा सकती है। हो सकता है, यह सब होता देखकर प्रेमचंद ने अपने आपको ठगा हुआ महसूस किया हो। एक लेखक के पास उसके ज़मीर से बढ़कर कुछ नहीं होता और जब उसे यह महसूस होता है कि कुछ ग़लत हो रहा है, तो मन दुखी होता है। प्रेमचंद 26 दिसंबर, 1934 को इंद्रनाथ मदान को लिखते हैं, “सिनेमा साहित्यिक आदमी के लिए ठीक जगह नहीं है। मैं इस लाइन में यह सोचकर आया था कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकने की कुछ संभावनाएँ इसमें दिखाई देती थीं, लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि यह मेरा भ्रम था और अब मैं फिर साहित्य की ओर लौट रहा हूँ। सच तो यह है कि मैंने लिखना कभी बंद नहीं किया। मैं उसे अपने जीवन का लक्ष्य समझता हूँ।”
इसके पंद्रह दिन बाद वह अपने साथी जैनेंद्र को एक और पत्र लिखते हैं, “फ़िल्मी हाल क्या लिखूँ। ‘मिल’ यहाँ पास न हुआ। लाहौर में पास हो गया और दिखाया जा रहा है। मैं जिन इरादों से आया था, उसमें एक भी पूरा होता नज़र नहीं आता। ये प्रोड्यूसर जिस ढंग से कहानियाँ बनाते आए हैं, उसकी लीक से जौ भर भी नहीं हट सकते। वल्गैरिटी को ये लोग एंटरटेनमेंट वैल्यू कहते हैं। राजा-रानी, उनके मंत्रियों की नक़ली लड़ाई, यही उनके मुख्य साधन हैं। मैंने सामाजिक कहानियाँ लिखी हैं, जिन्हें शिक्षित समाज भी देखना चाहे, लेकिन ऐसी फ़िल्म करते हुए इन लोगों को संदेह होता है कि चले या न चले। यह साल तो पूरा करना है ही। क़र्ज़दार हो गया था, क़र्ज़ा पटा दूँगा, मगर और कोई लाभ नहीं। उपन्यास के अंतिम पृष्ठ लिखने बाक़ी हैं, उधर मन ही नहीं जाता। यहाँ से छुट्टी पाकर अपने पुराने अड्डे पर जा बैठूँ। वहाँ धन नहीं है, मगर संतोष अवश्य है। यहाँ तो जान पड़ता है कि जीवन नष्ट कर रहा हूँ।”
प्रेमचंद की इस बात से यह स्पष्ट होता है कि वह इस माध्यम को किस हद तक समझते थे। वह यथार्थवादी सिनेमा के हिमायती थे। उन्होंने स्टूडियो कल्चर से हटकर फ़िल्म को रियल लोकेशन पर फ़िल्माए जाने की तारीफ़ की थी। वह जिस तरीक़े की कहानी लिख रहे थे या जिस क़िस्म के सिनेमा के पैरोकार थे, वैसी विषयवस्तु और फ़िल्मों ने इटली और फ़्रांस में ‘इतालवी नव-यथार्थवाद’ और ‘फ़्रेंच नुवाल’ जैसा आर्टिस्टिक मूवमेंट खड़ा कर दिया था। बिमल रॉय जिस ‘दो बीघा ज़मीन’ (1953) की वजह से दुनिया में सराहे गए, वैसी फ़िल्मों के लिए प्रेमचंद ने उस दौर में सबसे पहले सोचा। जिसको बाद में ऋत्विक घटक और सत्यजीत रे ने एक ऊँची उड़ान दी। यह फ़िल्म जगत की बदक़िस्मती है कि वह उन्हें समझ नहीं पाए और बाद के फ़िल्म समीक्षकों और आलोचकों ने उनके ‘सिनेमा एप्रोच’ पर कभी ध्यान नहीं दिया; नहीं तो प्रेमचंद आज साहित्य ही नहीं बल्कि सिनेमा के भी जाने-माने हस्ताक्षर कहलाते और आज वह दुनिया के फ़िल्म स्कूलों और विश्वविद्यालयों में किसी फ़िल्म थ्योरिस्ट्स की तरह पढ़ाये जा रहे होते। उनकी मुंबई में उपस्थिति भले बमुश्किल साल भर की रही हो, लेकिन वह फ़िल्म जगत के लिए, सिनेमा के प्रेमियों, लेखकों और विद्यार्थियों के लिए एक महत्त्वपूर्ण घटना है, जिस पर अमल करने की ज़रूरत है।
फ़िल्मी जीवन से उनका मन उचट गया था। प्रेमचंद ने अपने इन्हीं विचारों के कारण डायरेक्टर हिमांशु राय का उनकी कंपनी में नौकरी करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। जैनेंद्र कुमार ने दिल्ली में ‘मज़दूर’ फ़िल्म देखी, तो प्रेमचंद से उसकी कमज़ोरियों की शिकायत करते हैं, तो वह उत्तर में जैनेंद्र को लिखते हैं, “मज़दूर तुम्हें पसंद न आया। यह मैं जानता था। मैं इसे अपना कह भी सकता हूँ, नहीं भी कह सकता। इसके बाद एक रोमांस जा रहा है। वह भी मेरा नहीं है। मैं उसमें बहुत थोड़ा-सा हूँ। ‘मज़दूर’ में भी मैं थोड़ा-सा हूँ, नहीं के बराबर। फ़िल्म में डायरेक्टर सब कुछ है। लेखक क़लम का बादशाह क्यों न हो, यहाँ डायरेक्टर की अमलदारी है और उसके राज्य में उसकी (लेखक की) हुकूमत नहीं चल सकती। हुकूमत माने तभी वह रह सकता है। वह यह कहने का साहस नहीं रखता, मैं जनरुचि को जानता हूँ। इसके विरुद्ध डायरेक्टर ज़ोर से कहता है, मैं जानता हूँ, जनता क्या चाहती है, और हम जनता की इसलाह करने नहीं आए हैं। हमने व्यवसाय खोला है, धन कमाना हमारी ग़रज़ है। जो चीज़ जनता माँगेगी, वह हम देंगे। इसका जवाब यही है, अच्छा साहब, हमारा सलाम लीजिए। हम घर जाते हैं। वहीं मैं कर रहा हूँ। मई के अंत में बंदा काशी में उपन्यास लिख रहा होगा। और कुछ मुझमें नई कला न सीख सकने की भी सिफ़त है। फ़िल्म में मेरे मन को संतोष नहीं मिला। संतोष डायरेक्टरों को भी नहीं मिलता, लेकिन वे और कुछ नहीं कर सकते, झख मारकर पड़े हुए हैं। मैं और कुछ कर सकता हूँ, चाहे वह बेगार ही क्यों न हो, इसलिए चला जा रहा हूँ। मैं जो प्लॉट सोचता हूँ, उसमें आदर्शवाद घुस आता है और कहा जाता है उसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं होता। इसे मैं स्वीकार करता हूँ… मेरे लिए अपनी वही पुरानी लाइन मज़े की है, जो चाहा लिखा…।”
प्रेमचंद कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए इंसान थे। हर चीज़ पर बहुत पैनी और साफ़ नज़र। आप उनका चाहे जो भी काम उठाकर देख लीजिए, उन्हें आप मज़बूती से दबे-कुचलों, वंचितों और शोषितों के साथ खड़ा हुआ पाएँगे। वह आपको समझौता करते हुए विरले दिखते हैं। नहीं तो वह इतने बड़े फ़नकार होने के बावजूद भी कभी फटे जूते में नहीं दिखाई देते, और यही प्रेमचंद हैं जो कभी अपनी ग़ैरत को ताक पर नहीं रखते हैं, बल्कि एक तटस्थ सिपाही की तरह अपने धर्म पर अडिग दिखाई पड़ते हैं।
प्रेमचंद के देह त्यागने के बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ी। वह अब तक भारत के सबसे अधिक पढ़े जाने वाले आधुनिक लेखकों में हैं। उनकी कई कहानियों, उपन्यासों पर फ़िल्में बनी हैं। अब वह फ़िल्में दर्शकों की कसौटी पर कितनी खरी उतरीं, यह बात तो फ़िल्म समीक्षक और इतिहासकार ही बता पाएँगे। प्रेमचंद के प्रशंसक फ़िल्मकारों में सत्यजित रे का नाम सबसे ऊपर है। सत्यजित रे की फ़िल्म ‘शतरंज के खिलाड़ी’ में उन्होंने अवध के नवाबों की शान-शौकत और काहिलपन को बड़ी ख़ूबसूरती से दिखाया है। हालाँकि सत्यजीत रे कोई नई कहानी गढ़ सकते थे, फिर भी उन्हें लखनऊ को दिखाने के लिए प्रेमचंद का चश्मा ज़्यादा सटीक लगा। ख़ैर, फ़िल्म प्रेमचंद की कहानी, उसके कलाकारों; जिसमें मशहूर अभिनेता अमजद ख़ान, संजीव कुमार, फ़ारूख़ शेख़ जैसे दिग्गज कलाकारों और सत्यजित रे के निर्देशन की वजह से बहुत चर्चित तो हुई, लेकिन उतनी बड़ी सफलता नहीं हासिल कर सकी। अगर आप ग़ौर करें, तो सत्यजित रे की फ़िल्मों में प्रेमचंद की कहानियों की परछाई दिखती है, भले ही ‘पाथेर पांचाली’ को विभूतिभूषण बंदोपाध्याय ने लिखा हो। विमल रॉय के निर्देशन में बनी फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ (1953) को देखने पर लगता है कि यह विषयवस्तु तो प्रेमचंद की है। ख़ैर, फ़िल्म ‘दो बीघा ज़मीन’ को कुछ लोग मानते हैं कि उसपर इतालवी फ़िल्मकार विटोरियो डी सिका की फ़िल्म ‘बाइसिकल थीव्स’ (1948) का प्रभाव है। उस दौर की फ़िल्मों और साहित्य ने एक-दूसरे को काफ़ी हद तक गढ़ा है। यहाँ तक कि कभी-कभी तो यह कह पाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि साहित्य ने सिनेमा को प्रभावित किया है या कि सिनेमा ने साहित्य को। फ़्रांस, रूस और इतालवी नव-यथार्थवाद ने उस दौर के साहित्य को भी अच्छा-ख़ासा प्रभावित किया। रूसी साहित्य और सिनेमा ने तो वहाँ की क्रांति में बड़ा योगदान दिया है। प्रेमचंद के साहित्य पर भी रूसी साहित्य और वहाँ के लेखकों का अच्छा-ख़ासा प्रभाव देखा जा सकता है। जब वह अपनी लेखनी में ‘सोशल रियलिज्म’ की बात करते हैं, तो वह लियो टॉलस्टॉय की तरह जान पड़ते हैं। प्रेमचंद की कहानियाँ आम इंसानों के संघर्षों का दस्तावेज़ हैं, जिसे पढ़ने पर लगता है कि समाज को वाक़ई इस दिशा में सोचने की ज़रूरत है। वह फ़्योदोर दोस्तोयेवस्की की तरह मनुष्य के मनोविज्ञान और उसके अंतर्मन में चल रही ऊहापोह और पेंचीदगी को दर्शाते हैं। जिसने मैक्सिम गोर्की और प्रेमचंद को पढ़ा है, उन्हें प्रेमचंद रूसी लेखक मैक्सिम गोर्की की तरह कामगारों और मज़दूरों के लिए खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। यह एक लेखक का एक्टिविज़्म है, जिसमें वह दिखता तो नहीं, लेकिन होता ज़रूर है। जिस तरीक़े से प्रेमचंद साहित्य के साथ अपने विचारों का सामंजस्य बिठाते हैं, वैसा सिनेमा में कर पाना बड़ा मुश्किल काम था। फ़िल्म के निर्माण में कइयों के दख़ल से बहुत कुछ परिवर्तित हो जाता है, और जब फ़िल्म बाहर आने में सफल नहीं होती है, तो बाक़ी सभी कन्नी काट लेते हैं और इसका ठीकरा लेखक और निर्देशक पर फोड़ा जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा साहित्यकार फ़िल्मों में उतनी ही सफलता अर्जित करे, जितनी कि उसने साहित्य जगत में हासिल की है, लेकिन प्रेमचंद की लेखनी में हर वो तत्व है जो उन्हें एक सफल पटकथा लेखक बनने से कभी नहीं रोक पाती। प्रेमचंद के मृत्यु के बाद उनकी प्रसिद्धि और बढ़ी, उन्हें बहुत सारे उपनामों से नवाज़ा जाने लगा; किसी ने कथा सम्राट कहा, तो किसी ने उन्हें भारत का चार्ल्स डिकेंस। उनके उपन्यासों और कहानियों पर कुछ चुनिंदा फ़िल्मकारों ने फ़िल्में बनाईं, जिसमें सत्यजित रे की ‘शतरंज के खिलाड़ी’ (1977), ओम पुरी और स्मिता पाटील अभिनीत सत्यजित रे की दूसरी फ़िल्म ‘सद्गति’ (1981), हृषिकेश मुखर्जी के निर्देशन में बनी सुनील दत्त और साधना अभिनीत ‘गबन’ (1966), के सुब्रह्मण्यम के निर्देशन में 1938 में बनी फ़िल्म ‘सेवासदनम्’ जिसमें महान् भारतरत्न स्वर कोकिला एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी ने मुख्य भूमिका निभाई है। ‘सेवासदनम्’ मुंशी प्रेमचंद के उर्दू उपन्यास ‘बाज़ार-ए-हुस्न’ पर आधारित है, जिसमें दिखाया गया है कि एक स्त्री किन परिस्थितियों में पड़कर वेश्यावृति की राह पर चली जाती है। कृषेन चोपड़ा के निर्देशन में 1959 में बनी फ़िल्म ‘हीरा मोती’ दो बैलों, हीरा और मोती, और उनके मालिक झूरी के बीच अगाध प्रेम, वफ़ादारी और स्वतंत्रता के बंधन को बख़ूबी दिखाती है। सत्यजित रे की तरह मृणाल सेन ने तमिल में प्रेमचंद की कहानी ‘कफ़न’ पर आधारित फ़िल्म ‘ओका ओरी कथा’ (1977) बनाई, जिसकी विषयवस्तु मूलतः ग़रीबी और सामाजिक न्याय है। त्रिलोक जेटली के निर्देशन में बनी ‘गोदान’ (1963) भी सामाजिक और आर्थिक विषमता पर आधारित है। इसमें राजकुमार, कामिनी कौशल, महमूद और शशिकला ने अभिनय किया है। गोदान को साहित्यिक दृष्टिकोण से भारतीय आधुनिक साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कृति माना जाता है। चूँकि ‘गोदान’ मुंशी प्रेमचंद की सबसे उत्कृष्ट कृति है, इसलिए फ़िल्म की काफ़ी चर्चा रही। ये प्रेमचंद के साहित्य पर आधारित कुछ महत्त्वपूर्ण फ़िल्में हैं, जिसमें उनकी लेखनी और उसके फ़िल्मांकन को जाना और समझा जा सकता है।
हालाँकि सिनेमा और प्रेमचंद के लिहाज़ से ये बहुत ही सीमित काम है, जोकि उन जैसे महान् लेखक और उनके साहित्य कर्म के आधार पर यदि आकलन किया जाये तो बहुत कम है। जिस तरह से इंग्लैंड में चार्ल्स डिकेंस के उपन्यासों ने समाज में कई बदलाव लाए, ठीक वैसे ही मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन से समाज में बहुत सारे परिवर्तन लाए और जन-जीवन को प्रभावित किया है। यकीनन ये बातें अगर फ़िल्मों में निरंतर आती रहती, तो उसका असर और व्यापक होता। जिस तरह BBC और HBO ने एक समय ब्रिटेन के लगभग सारे बड़े लेखकों और उनकी कृतियों पर फ़िल्में बनाई, जिसमें शेक्सपियर, जार्ज बर्नार्ड शा, हार्डी, लॉरेंस और जेन ऑस्टेन जैसे अनगिनत नाम शामिल हैं। वहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा फ़िल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित होती हैं, जिससे उनकी सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाती है और लेखक रिलेवेंट बना रहता है। यदि पश्चिम की तरह भारत में भी साहित्यिक कृतियों पर फ़िल्में बनती, तो निसंदेह प्रेमचंद को भारत का डिकेंस न कहना पड़ता। बनिस्बत इसके कि उनके साहित्य पर प्रत्यक्ष रूप से उतना अच्छा काम नहीं हुआ, जितना कि वह डिज़र्व करते हैं। हालाँकि उनसे लिया हर किसी ने है, चाहे सलीम-जावेद हों या फिर अगली पीढ़ी के लेखक। बिना प्रेमचंद को पढ़े ‘दीवार’ जैसी फ़िल्म नहीं लिखी जा सकती है। प्रोलिटेरिएट और बुर्जुआ संघर्षों को अगर फ़िल्मों ने कहीं से समझा है, तो इसमें प्रेमचंद के साहित्य की महती भूमिका है। प्रेमचंद के साहित्य पर सिनेमा जगत को पुनः सोचने की आवश्यकता है। उनकी लगभग सारी कृतियों पर अच्छी फ़िल्में बनाई जा सकती हैं; कुछ एक रचनाओं का समय, काल और परिस्थिति के हिसाब से रूपांतरण भी किया जा सकता है। पॉपुलर कल्चर में आने से हमारे साहित्यकार इस दौर में और रिलेवेंट होंगे और उनकी पहुँच जन सामान्य तक होगी।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
23 सितम्बर 2025
विनोद कुमार शुक्ल : 30 लाख क्या चीज़ है!
जनवरी, 2024 में मैंने भोपाल छोड़ दिया था। यानी मैंने अपना कमरा छोड़ दिया था। फिर आतंरिक परीक्षा और सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए जाना भी होता तो कुछ दोस्तों के घर रुकता। मैं उनके यहाँ जब पहुँचा तो पाया
05 सितम्बर 2025
अपने माट्साब को पीटने का सपना!
इस महादेश में हर दिन एक दिवस आता रहता है। मेरी मातृभाषा में ‘दिन’ का अर्थ ख़र्च से भी लिया जाता रहा है। मसलन आज फ़लाँ का दिन है। मतलब उसका बारहवाँ। एक दफ़े हमारे एक साथी ने प्रभात-वेला में पिता को जाकर
10 सितम्बर 2025
ज़ेन ज़ी का पॉलिटिकल एडवेंचर : नागरिक होने का स्वाद
जय हो! जग में चले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को। जिस नर में भी बसे हमारा नाम, तेज को, बल को। —दिनकर, रश्मिरथी | प्रथम सर्ग ज़ेन ज़ी, यानी 13-28 साल की वह पीढ़ी, जो अब तक मीम, चुटकुलों और रीलों में
13 सितम्बर 2025
त्याग नहीं, प्रेम को स्पर्श चाहिए
‘लगी तुमसे मन की लगन’— यह गीत 2003 में आई फ़िल्म ‘पाप’ से है। इस गीत के बोल, संगीत और गायन तो हृदयस्पर्शी है ही, इन सबसे अधिक प्रभावी है इसका फ़िल्मांकन—जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। इस गीत का वीड
12 सितम्बर 2025
विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय : एक अद्वितीय साहित्यकार
बांग्ला साहित्य में प्रकृति, सौंदर्य, निसर्ग और ग्रामीण जीवन को यदि किसी ने सबसे पूर्ण रूप से उभारा है, तो वह विभूतिभूषण बंद्योपाध्याय (1894-1950) हैं। चरित्र-चित्रण, अतुलनीय गद्य-शैली, दैनिक जीवन को