भाषाई मुहावरे को मानवीय मुहावरे में बदलने का हुनर
 शाहबाज़ अली ख़ान
24 नवम्बर 2024
शाहबाज़ अली ख़ान
24 नवम्बर 2024
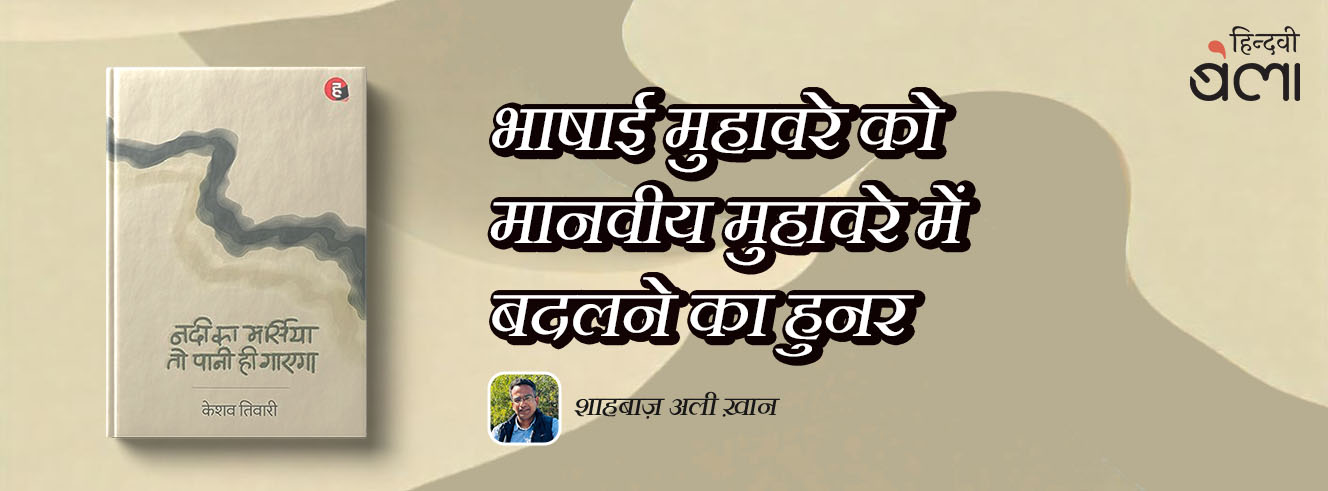
दस साल बाद 2024 में प्रकाशित नया-नवेला कविता-संग्रह ‘नदी का मर्सिया तो पानी ही गाएगा’ (हिन्द युग्म प्रकाशन) केशव तिवारी का चौथा काव्य-संग्रह है। साहित्य की तमाम ख़ूबियों में से एक ख़ूबी यह भी है कि वहाँ सामान्य से दिखने वाले दृश्यों की अपनी अर्थ-छवियाँ होती हैं। मगर उन अर्थ-छवियों को खींच कर बाहर लाने के लिए जिस दृष्टि की आवश्यकता होती है, वह विरल है। बल्कि यह कहें कि विशिष्ट दृश्यों को देखना अपेक्षाकृत सरल है, सामान्य दृश्यों को देखने के लिए केवल आँख की ही नहीं, दृष्टि की भी दरकार होती है। पुरखे शायर जब यह कहते हैं—“रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं क़ायल/जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है” तो रक्त की एक सर्वथा नई परिभाषा प्रस्तुत करते हैं। पाठक को एक नई दृष्टि देते हैं।
जब कबीर कहते हैं—सुखिया सब संसार है, खावै अरु सोवै/दुखिया दास कबीर जागै अरु रोवै, तो जागने और दुख के संबंधों को देखने की एक भिन्न दृष्टि देते हैं। चैत किसके घर नहीं आता है? चैत के पीलेपन को किसने नहीं अनुभव किया है? लेकिन उसके पीलेपन के पीछे उदासी का एक रंग है जो गाँव-गिराँव छोड़कर जाने वालों के चेहरे पर फैल गया है, यह केशव तिवारी की इन पंक्तियों में दिखाई देता है—
खेत सजे हैं
और लोग बेघर हो रहे हैं
यही है चैत का पीला रंग
जो तमाम चेहरों पर फैला पड़ा है...
केशव की कविताई का सबसे विशिष्ट पक्ष, जीवन के सामान्य दृश्यों का विशिष्ट अर्थ-बोध से परिपूर्ण होना है। यही उनका सर्वाधिक सशक्त पक्ष है। उनकी कविताओं की आधारभूत संरचना करुणा से उपजती है। ऋतुओं का गीत हो या नदियों का मर्सिया हो; स्त्रियों के अंतर्मन की टोह हो या खेत-खलिहान की पीड़ा हो; छीज रहे मूल्यों की चिंता हो या स्मृतिहीनता का संकट हो; पुरखे कवियों की याद हो या कवि का कहा सच भी हो जाने की कामना हो; इन सबको कारुणिक दृष्टि से देखा जाना इन कविताओं की मार्मिकता तथा प्रासंगिकता में संवर्धन करता है। उनके काव्य-जगत में करुणा का यह विस्तार उनकी आत्म-आलोचनात्मक जीवनानुभूतियों से संसर्ग के कारण संभव हो पाता है।
साहित्यकार पर दोहरा दबाव होता है। वह अपने समय के मर्म की पड़ताल करते हुए पाठकों के मर्म को स्पर्श करता है। उनको जगाता है। कुशल रचनाकार मार्मिक दृश्यों को रचते समय कोरी भावुकता से भी बचता है और उसे थोथे ज्ञान से बच कर निकलने की कला भी आती है। केशव सिद्धहस्त कवि हैं। किसी घटना या दृश्य को कविता में संवेदना और विचार को जिस बिंबात्मक कला के साथ वर्णित करते हैं, वह पाठक के अंतर्मन पर दबाव और बेचैनी पैदा करती है। पाठक पर उस संवेदनात्मक बिंब को ग्रहण करने का दबाव बनता है और जब एक बार पाठक उसे ग्रहण कर लेता है, तब कवि की काव्य-संवेदना पाठकीय भावनाओं का संस्कार करती है और इस प्रक्रिया में वह व्याकुलता का अनुभव करता है।
‘तमिलनाडु के एक समुद्र-तट पर’ कविता में मदद की गुहार के बीच, भाषा की दीवार का खड़ा हो जाना, ऐसा बिंब है जो पाठक को कचोटता है। आज जब अस्मिताओं के पहचान के दौर में हम सब ‘स्व’ से आगे निकलकर कुछ सोच न पा रहे हों, वहाँ किसी व्यक्ति का दुख यह है कि वह किसी अन्य भाषी के दुख को सुन नहीं सका क्योंकि वह उस भाषा को नहीं समझ पा रहा था। विनोद कुमार शुक्ल की कविता ‘हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था’ में मनुष्य एक-दूसरे की अनुभूतियों को उसके शारीरिक क्रियाओं से जानता है, मगर केशव की कविता में दुख इस बात का है कि अपनी पीड़ा किसी अन्य से साझा न कर पाना भी एक ऐसी असहायता है जो दूर तक कचोटती है और यह चुभन तब और भी गहरी हो जाती है, जब सुनने वाला/वाली अन्य भाषी हो।
केशव तिवारी की पूरी काव्य-संवेदना में कह पाने से अधिक, न कह पाने का दुख अधिक है। व्यक्त के बीच में जो अव्यक्त है, उसे पाठक तक किस रूप में प्रेषित करना है, जिससे उसकी संवेदनाओं का संस्कार हो सके, केशव की कविता में संभव होती दिखाई देती है—
वह जान गई थी—
मैं तमिल नहीं समझता
आज भी बार-बार परेशान करता है
उसकी भाषा से अपरिचय
कोई तकलीफ़ ज़रूर थी उसे
जो थम नहीं रही थी उससे
पीड़ा की ऐसी वाचालता
कभी न देखी
न सुनी
यही कारण है कि कवि जिससे भी मिलता है (ख़्वाह वह कोई अन्नानास बेचने वाली बुढ़िया हो, कोई गाइड हो या नदी हो या कोई पठार हो), उसके कहे गए से ज़्यादा, उसके न कहे गए को समझने की कोशिश करता है और इस समझने की प्रक्रिया में कवि अपना बौद्धिक दंभ प्रदर्शन नहीं करता है, बल्कि विनीत होकर उनके अव्यक्त को समझने की कोशिश करता है; जैसलमेर के उस गाइड के मन की बात को पढ़ता है कि हम अभिजात बौद्धिकता की जुगाली करते हुए जिस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, वह गाइड उसे एक झटके में तोड़ देता है—
जाते-जाते कह रहा हो जैसे
आते रहिए आपके आने से ही
यहँ बहुत कुछ चलता है
इतिहास की ऊँट-गाड़ी से
उसका वर्तमान जुता है
इसे किसी और से बेहतर समझता है वह।
जिस समाज की ‘फ़्लैट-संस्कृति’ में अपने पड़ोसियों का हाल-ख़बर न हो; जहाँ सुनाई वही दे रहा हो, जो कर्कश आवाज़ का मालिक हो; जहाँ दिखावे और नुमाइश का दृश्य ही चहुँओर व्याप्त हो; जहाँ अश्लीलता ही किसी की ताक़त हो और किसी की ताक़त अश्लीलता में तब्दील होकर देश के नक्शे में शामिल हो गई हो; ऐसे समाज में अव्यक्त को न समझ पाने की पीड़ा जिसको साल रही हो कि
जो रात मेड़ पर बैठा मिला था
सिरहाने बैठा-सा लग रहा है
क्या कुछ कहना चाहता है
जो उस वक्त नहीं कह पाया
दूसरे की पीड़ा को न समझ पाने की ऐसी कवि-कातरता, पाठक को व्याकुल तो करती है और भयभीत भी करती है कि कितने ऐसे थे जिसे उसने भी कभी समझने की चेष्टा तक नहीं की। पाठक की विकलता यह है कि क्या कवि की इस पीड़ा को भोगने के लिए वह भी अभिशप्त तो नहीं है—
कोई चूक
कुछ रह गया हो जो
कुछ-न-कुछ तो ज़रूर
बेध रहा होगा इसे
ये मेरे ही सिरहाने क्यों बैठा है
कब तक बैठा रहेगा
क्या यह रोज़ अब इसी तरह आएगा
कहीं-न-कहीं यह धीरे-धीरे
मेरे रतजगे में न शामिल हो जाए।
कविता की यह एक ऐसी किताब है जो मनुष्य और प्राकृतिक परिदृश्य के बीच एक पुल का काम करती है। कविता का शीर्षक ही इस बात की गवाही देता है। छोटी नदी हो या बड़ी नदी, समुद्र हो, पहाड़ हों या खेत-खलिहान हों, केशव की दृष्टि उनको समेट लेती है, जिससे पाठक का प्रकृति से जो मानवीय रिश्ता होना चाहिए, उससे वह संपन्न होता है। प्राकृतिक परिदृश्यों वाली कविताओं (स्त्री के अंतर्मन की टोह वाली कविताओं में भी) में कवि (कवि के ही शब्दों में—‘और कवि कविता से कुछ दूर/थोड़ा दिखता/ थोड़ा ओझल....) पाठक और अपनी कविता से कुछ दूरी पर खड़ा होता है। कुछ बंद-बंद-सा, कुछ छोड़ता हुआ-सा दिखायी देता है, मानो पाठक के हवाले कर रहा हो। ‘अब देखो’ कविता में मनुष्य और प्राकृतिक परिदृश्य के संबंध को जिस रूप में कविता उद्घाटित करती है, उस मुकम्मल बिंब का आस्वाद पाठक पूरी तरह से ले लेता है—
मदुरै से रामेशवरम के रास्ते
सड़क के साथ
एक हरा समुद्र
यात्रा कर रहा था
ताड़ के पेड़ भी सहयात्री थे
रास्ते में एक जगह
एक बुढ़िया
खट्मिठ्ठे अनानास पर
लाल मिर्च और नमक रखे बैठी थी
रुक कर जैसे ही खाने के लिए बढ़ा
एक टुकड़ा मुँह में डाला ही था
कि उसने झुर्रीदार आँख से देखते हुए
मानो कहा—अब देखो समुद्र!
‘अब देखो समुद्र’ ऐसी पंक्ति है जो इस साधारण-से दृश्य को कविता में बदल दे रही है और पाठक को आमंत्रित कर रही है कि अब पढ़ो कविता! अब देखो प्रकृति और मनुष्य का रिश्ता! इसी प्रकार ‘नदी का मर्सिया तो पानी ही गाएगा’ कविता में कवि साफ़ तौर पर घोषणा करता है कि मनुष्य इसी प्रकृति का अंग है, वह उसका मालिक नहीं है। जो मालिक बनता है, वह धूर्त है। उसका अपने परिवेश से खोखला रिश्ता है। प्रकृति उन चतुर लोगों की शिनाख़्त करती है और जो उसके हमदर्द हैं, उनको खोजती है—
मनिहारपुर के घाट के पत्थर पर
उन औरतों की बिवाई फटी एड़ियों के
घिसने के निशान खोज रहा है
चतुर कवि तो कविता में गाल बजाएगा
नदी का मर्सिया तो पानी ही गाएगा
क्योंकि बिवाई फटी एड़ियों वाली औरत नदी के दुख को जानती है लेकिन सैलानी को नदी की पीड़ा नहीं नज़र आती है उसे केवल अपने उल्लास से मतलब है—
उर्मिल,
मैं तुम्हारे विशाल बाँध पर खड़ा हूँ
सैलानियों के उल्लसित चेहरे देख रहा हूँ।
कवि प्राकृतिक परिदृश्य को कुछ इस प्रकार सृजित करता है कि उसकी कविताओं से शोषण और असमानता को रेखांकित किया जा सकता है। इस संग्रह की कविताओं में संवेदना, सौंदर्य, विस्मय और वैचारिक उत्तेजना, चारों मौजूद हैं। केशव की कविताई पाठकों के कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है, इससे पहले की देर हो जाए।
शोषण और असमानता को रेखांकित करने वाले साहित्य में स्त्री का होना, कोई चौंकाऊ विचार नहीं है। यह लाज़िमी है। स्त्री के विभिन्न रूप हैं। उसके संघर्ष के अनेक आयाम हैं। स्त्री-संघर्ष की छवियाँ इस संग्रह की कविताओं में ध्यान खींचती हैं। पहले, बाज़ार मुक्त करता और फिर बाज़ार ही गुलाम बनाता है, यह अब वैचारिक क्षेत्र में ढकी-छिपी बात नहीं रह गई है। बाज़ार सपने दिखा कर लूटने वाला ‘फ़्राडिया’ है।
ज़ाहिर है जिसके सपनों पर सबसे ज़्यादा पाबंदी होगी, उसे सपने देखने की सबसे ज़्यादा लत होगी। बाज़ार ऐसे लोगों की ही तलाश करता है। भारतीय संस्कृति में वैसे ही ‘पराधीन सपनेहू सुख नाहिं’ वाली स्त्री की पीड़ा अकथनीय है। बाज़ार स्त्री की इस पीड़ा को भुनाना जानता है। वह मुनाफ़ा कमाना जानता है। आज टीवी पर दिखाए जाने वाले विज्ञापन में सर्वाधिक बिकने वाली ‘हॉटेस्ट प्रॉपर्टी’ माँ है। हर आयुवर्ग की माँ है, क्योंकि बाज़ार माँ के नाम पर मुनाफ़ा कमाना जानता है। हर चमकते विज्ञापन के मुँह पर स्त्री का चेहरा है। आज बाज़ार महानगरों से निकल कर गाँवों और क़स्बों तक में पैर पसार चुका है—
ये किसी महानगर से नहीं
किसी आसपास के क़स्बे से
आकर डोर टू डोर
बेच रही हैं सामान।
जागरुक व्यक्ति बाज़ार के इस अंधाधुंध फैलाव समझता है और स्त्री के चेहरे पर मुनाफ़े के पुते ‘मेकअप’ के पीछे की साज़िश को भी समझता है। केशव भी उन्हीं जागरुक लोगों में से हैं जो इसे समझ रहे हैं कि बाज़ार स्त्री को साहस देता है, मुक्ति देता है लेकिन इस मुक्ति का दाम चुकाना पड़ता है। इससे सावधान रहने की ज़रूरत है—
यही बाज़ार इनकी क़ैद और रिहाई है
यहीं उपजता है इनके स्वप्न देखने का साहस
और यहीं उन सपनों का श्मशान भी है।
अंतर्मन की रेकी करने में केशव माहिर हैं। स्त्री-अंतर्मन की जटिल परतें भी उनकी कविता में खुलती दिखाई देती हैं। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री मात्र देह बन कर रह जाती है, किंतु उसकी आंतरिक इच्छा होती है कि कोई उसके मन को सुने। उसके अंतर्मन की पीड़ा, व्याकुलता तथा व्यथा को सुनने के लिए स्त्री के मन में झाँकना पड़ता है। यदि वह अपनी व्यथा नहीं सुना पाती तो किसी संवेदनशील व्यक्ति को उसके अंतर्मन को न केवल सुनना होता है, दूसरों को उसे सुनाना भी पड़ता है। साहित्य की संवेदनशीलता का विस्तार इसी प्रकार से होता है। भारतीय स्त्री के सम्मुख उसकी अपनी इच्छाएँ हैं, तो दूसरी तरफ़ सामाजिक मर्यादाएँ हैं। अपनी इच्छाओं पर पहरेदारी करती हुई स्त्री सामाजिक मर्यादाओं की देहरी लाँघ नहीं पाती। परिणामस्वरूप उसके भीतर की पीड़ा और बेचैनी उदासीनता में तब्दील हो जाती है। उसके मन के तार कभी बजते नहीं, उसके मन के तारों के भीतर सामाजिक लोकाचार को विश्रृंखलित करने वाले कौन सी स्वर लहरियाँ छिपी हैं, वह किसी को सुनाई नहीं देते क्योंकि वह उसे जीवन भर मन के जंग लगे बक्से में बंद रखती है। अपनी इच्छाओं को दमन करते-करते भारतीय गृहस्थ स्त्री ‘जोगी’ ही बन जाती है। संभवतः यही कारण है कि इस कविता संग्रह के पहली कविता स्त्री अंतर्मन की पीड़ा को उद्घाटित करने वाली कविता है और कविता अपने शीर्षक ‘जोग’ से ही अन्यत्र इशारा कर देती है—
लड़की क्या जाने
माँ के मन का कौन-सा तार
जोगी की सारंगी के
किस तार से जुड़ा है
एक आवाज़ की तड़प
सुरों की बेचैनी के साथ
लौटा रहा है जोगी
जोगी जानता है कि
जागे हुए सुरों के साथ
पूरी ज़िंदगी जागना पड़ता है।
केशव की कविताई मुख्य रूप से करुणा उपजाती है किंतु उनकी कविता में शोषण की व्यवस्था और पाखंड की संस्कृति के प्रति आक्रोश का स्वर भी अत्यंत तीखा है। शोषण और पाखंड के जड़ की शिनाख़्त कर लेना भी किसी विद्रोह से कम नहीं है। साहित्यकार उन स्थलों को चिह्नित करता है जहाँ शोषण किया जा रहा हो। वह मानवता का संवेदनशील पक्षधर होते हुए मनुष्यता को अपमानित करने वाली प्रवृत्तियों को ज़रूर उजागर करता है। मनुष्य की मुक्ति का स्वप्न प्रेम और करुणा आधारित समाज में संभव है, शोषणविहीन समाज में संभव है। यही कारण है कि चेतनासंपन्न रचनाकार सर्वप्रथम शोषकों की पहचान करते हुए पाठकों के मन में वितृष्णा पैदा करता या करती है—
मैं उन तमाम घूसख़ोरों को जानता हूँ
जो सरकारी नौकरी से रिटायर हो
गाँव आते-जाते हैं
गाँव में छूट गए मित्रों को
किसी के खेत से चना उखाड़ने
किसी के आम तोड़ने के जुर्म में
चोर-लिहाड़ा और क्या-क्या कहते सुनता हूँ
कहने वालों के मुँह पर
थूक देने का मन होता है
क्योंकि मुझे उनके बारे में पता है सब कुछ।
केशव की कविता में जो हाशिये पर हैं, उनके अव्यक्त दुख, व्यथा एवं पीड़ा को न समझ पाने, न व्यक्त कर पाने की कातरता और क्षोभ है तो दूसरी तरफ़ शोषकों की पहचान करने का दावा भी है और यह दावा केवल कवि का व्यक्तिगत दंभ नहीं है; वह सभी कवियों की तरफ़ से यह अभिमानपूर्वक कहता है कि—
युद्ध और वसंत का
क्या रिश्ता हो सकता है?
इसका जवाब
एक कवि के पास होता है
वह वसंत के फूलों को ही नहीं
आततायी की आँखों को भी पहचानता है।
यही कारण है कि केशव की कविता पूरी दुनिया में हो रहे शोषण पर अँगुली उठाने का अधिकार रखती है और आलोकधन्वा की तर्ज़ पर—
जो मेरी साँस
लाहौर और कराची और सिंध तक उलझती है?
उनकी ‘आवाज़’ रोहिंग्या, कश्मीर, फ़िलिस्तीन और सीरिया के दुखों से पिघली हुई है—
कितने रोहिंग्या
कितने फ़िलिस्तीनी
कितने कश्मीरियों
कितने सीरियाइयों को
सुनाई पड़ती होंगी ये आवाज़ें।
कवियों की शोषण और पाखंड पर अँगुली उठाने की इसी प्रवृत्ति को और अधिक विस्तार देते हुए केशव भारतीय समाज और संस्कृति के पाखंड पर तंज़ भी करते हैं और निराशा भी प्रकट करते हैं। भारत में नदियों का महात्म्य ढकी-छुपी बात नहीं है। नदी को न केवल माँ बल्कि देवी का दर्जा दिया गया और भारत में नदियों की पूजा की जाती है। पौराणिक तथा धार्मिक पुस्तकों में नदियों के महत्त्व को गीत गाया गया है। नदियाँ भारतीय समाज एवं संस्कृति की प्राणदायिनी शक्ति रही हैं किंतु क्या नदियों की पूजा भर करना ही किसी समाज और संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता हो सकती है? नहीं! सभी जानते हैं भारतवासी अपनी नदियों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अब पूजी जाने वाली प्राणदायिनी नदियाँ प्राण हरने वाली बन गयी हैं, क्योंकि हम भारतवासी न केवल एक नागरिक रूप में ‘फ़ेल’ हो चुके हैं बल्कि एक भक्त के तौर पर भी केवल पाखंड ही हमारा सर्वस्व बन चुका है। भारत में बड़ी नदियाँ दूषित हैं तो, छोटी नदियाँ मृत हो चुकी हैं। आज नदियों का पानी दूषित और ज़हरीला हो चुका है लेकिन हम अपनी धार्मिक आस्था की डुबकी उसी में मार रहे हैं; कवि इस बजबजाते हुए पाखंड को पाठकों के सामने रखता है कि—
तुम लाख जिसे देवताओं की नदी मानते हो
हरदम उसे माँ-माँ कहते हो
कितने भी प्यासे हो पर
कड़ा घाट पर
उसका एक चुल्लू
काला पानी नहीं पी सकते
इन हँसते धर्मसिक्त चेहरों का भय
अगर तुम्हें नहीं दिखता तो मुझे
तुम्हारी बीनाई पर कुछ भी नहीं कहना
और इस त्रासदी को व्यक्त करता है कि वह व्यक्ति अभागा है जिसके सामने उसकी प्रिय नदी मृतप्राय हो जाये और उसके दुख को कोई सुनने वाला न रहे। कवि कोई ऋषि-मुनि नहीं किंतु उसका दुख जब अपनी सीमा को पार कर जाता है, तब वह नदियों के हत्या करने वालों को कवि-अभिशाप देता है, और नदी से ही अपने दुख को सुनाता हुआ कहता है कि—
वे क्या समझेंगे मेरी तकलीफ़
जो तुम्हारी
इस हालात के ज़िम्मेदार हैं
उन पर गिरेगी जेठ में चाकी
मेरा दुख समझो तुम सिंधु
क्या कोई अभागा कवि
अपनी प्रिय नदी का
मर्सिया लिखना चाहेगा?
स्मृतियाँ जीवन की गतिशीलता, व्यापकता तथा संभावनाओं को व्यक्त करती हैं। स्मृति वह हिस्सा है जिससे पाठक को रचनाकार के बौद्धिक एवं संवेदन पक्ष की सच्ची झलक मिलती है। कोई किसी को किस रूप में याद करता है, उससे याद करने वाले के नैतिक एवं ईमानदाराना सोच की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। स्मृति और याद रखने की प्रक्रिया हमेशा से साहित्य में एक महत्त्वपूर्ण, बल्कि एक प्रमुख विषय रही है। कैसे कोई व्यक्ति अपने अतीत को याद करता है और कैसे वह इसके आधार पर किसी की पहचान को निर्मित करता है। वह अतीत और वर्तमान के बीच संबंधों की फिर से जाँच करता है, और पहचान के निर्माण के लिए स्मृति द्वारा पूरे किए जाने वाले कई कार्यों को उजागर करता है। हमारी स्मृतियाँ अत्यधिक चयनात्मक होती हैं, और उनका प्रतिपादन संभावित रूप से हमें याद करने वाले के वर्तमान, उसकी इच्छा और इन्कार के बारे में अधिक बताता है। इससे किसी के इतिहास-बोध और सांस्कृतिक-बोध का पता चलता है। केशव का काव्य स्मृतियों का एक ऐसा कोलाज है जिसमें सबके अपने-अपने हिस्से हैं। चाहे वह गाँव-गिराँव हो, शहर हो, नदी हो, पहाड़ हो, खेत-खलिहान हो, मित्र हों, बुज़ुर्ग हों, कोई राहगीर हो, कोई बग़लगीर हो, जो भी एक बार कवि की समृति का हिस्सा बना, केशव की कविता में उसको स्थान मिला। और जिनसे केशव नहीं मिले, लेकिन जिनके होने से कवि की संवेदना का निर्माण हुआ है, वह भी उनकी याद में शामिल है। यही कारण है कि केशव को अपने पुरखे कवियों और उनकी कविताओं की याद बार-बार आती है।
काव्य-संवेदना के निर्माण एवं विस्तार में पूर्ववर्ती कवियों की दृष्टि एवं संवेदना की बड़ी भूमिका होती है। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरवर्ती कवियों की काव्य-सर्जना इनसे प्रभावित होती है, किंतु एक ईमानदार कवि वह है जो अपने पुरखे कवियों को बारंबार याद करे। केशव अपने इन पूर्ववर्ती कवियों को याद कर, वर्तमान के धुंधले आईने को साफ़ करने की कोशिश करते हैं। वह कवि होने की ज़िम्मेदारी का भाव इन कवियों से ग्रहण करते हैं :
मीर
आख़िर क्या माँगा था मीर ने
यही न कुछ देर चैन से सोना चाहता हूँ
त्रिलोचन और मान
लगा तिरलोचन और मान ही नहीं
अवधी में इनका भी कारोबार चलता है
मजाज़ (पूरी कविता, ‘मजाज़ की क़ब्र देख कर’ शीर्षक से) को केशव याद कर अपने कवि होने के कर्तव्य-निर्वहन को भी याद रखते हैं—
कवि के ऊपर
कविता के अलावा
राजनीति का भी ज़िम्मा आन पड़ा है
वह चुप भी कैसे बैठ सकता है
उसकी राजनीति ही
जनता की राजनीति है
उसकी कविता
उसी राजनीति की कविता है।
कवि होने की यह ज़िम्मेदारी पीड़ा और व्यथा को जन्म देती है क्योंकि कवि को जब लगता है कि वह उन ज़िम्मेदारियों को ठीक से उठा नहीं पा रहा है, तो वह अपराधबोध की पीड़ा का अनुभव करता है—
कविता में जिए अपने अपराधबोध को
कुछ कम कर सकते हो
आह! कितना मासूम बयान!
कितना पीड़ादायक!
प्रशंसा, निंदा, महत्त्वकांक्षा से मुक्त ‘भादो में हथिया की शरण चाहने वाला’ कवि काव्य-प्रक्रिया को लेकर अपना पक्ष रखता है कि रचनाकार को अपनी रचना में स्वयं की उपस्थिति से बचना चाहिए, कविता को ख़ुद कवि की उपस्थिति से बचाना चाहिए—
और कवि कविता से कुछ दूर
थोड़ा दिखता
थोड़ा ओझल...
ऐसा इसलिए कि कवि को कविता की ताक़त पता है—
...कहावत है कि थके के लिए
नदी से बड़ा संगी नहीं
और हारे के लिए
कविता से बड़ा संगाती।
आडंबरहीन भाषा में संवेदना और विचार से भरपूर काव्य-सृजन करना कठिनतर कार्य है। केशव भाषाई मुहावरे को मानवीय मुहावरे में परिवर्तित कर देने में सक्षम हैं। हमारी दुनिया के व्यावहारिक हिस्सों से गहन कविता बनाने की केशव की क्षमता उन विशेषताओं में से एक है जो उनकी कविता के बारे में बहुत आकर्षक लगती है। साहित्य में वही बचा रहेगा जिसकी चिंता के तार जीवन की अकथनीय पवित्रता से जुड़े रहेंगे। ‘नदी का मर्सिया तो पानी ही गाएगा’ इस दृष्टि से एक पठनीय एवं संग्रहणीय काव्य-संग्रह है, जिसके चिंता के तार जीवन की इसी अकथनीय पवित्रता से जुड़े हुए हैं।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
