बेदिल की दिल्ली
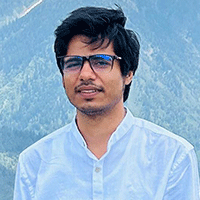 रविंद्र कुमार
10 अक्तूबर 2025
रविंद्र कुमार
10 अक्तूबर 2025

विगत कई दिनों से हमारा मन दिल्ली से बाहर कहीं दूर जाने को छटपटा रहा था। लगभग दो महीने से राजधानी के एक बंद 20×20 के किराये के कमरे में कैद रहते-रहते दिमाग, दिल और शरीर—सब सुस्त और कुछ-कुछ रोबोट जैसे हो चले थे। दिल्ली में रहना अपने-आप में एक चुनौती है—ख़ास तौर पर जब आप सारी उम्र हरियाणा के एक छोटे-से गाँव की खुली हवा में रहे हों और अचानक आपको महानगर के एक डिब्बेनुमा कमरे में लाकर पटक दिया जाए कि लो, अब यही तुम्हारा घर है।
दिल्ली की रोज़मर्रा की ज़िंदगी ने हमें बुरी तरह पस्त कर रखा था। घर से बाहर निकलो तो तुरंत मुँह पर बदबू और धूल-धक्कड़ का थपेड़ा पड़ता है। रिक्शा से लेकर कार और बसों तक के बिना रुके बजते तेज़ हॉर्न कानों में पिघला सीसा घोलते हैं। गली में क़दम रखते ही आस्था की प्रतीक गाय माता अपने अवशेषों समेत दर्शन देती हैं—इधर-उधर बिखरे गोबर के ढेर, मानो सड़क पर कोई आधुनिक कला की प्रदर्शनी लगी हो। लोगों द्वारा जगह-जगह पान-गुटखा चबा-चबा कर थूका गया लाल धब्बा, हर कोने पर फैले कुरकुरे-चिप्स के ख़ाली पैकेट, ठंडे-मीठे या नमकीन पानी की तरह-तरह की खाली बोतलें—ये सब मिलकर शहर के ‘सौंदर्य’ को चार चाँद लगाते हैं। सड़कें आधी तो ठेलों और फुटपाथी दुकानों ने घेर रखी हैं, बची-खुची जगह पर गाड़ियाँ ऐसे पार्क हैं मानो सड़क के साइड में गाड़ी पार्क करना संविधान में लिखा हो; और इसी वजह से (और भी कई वजहों के कारण) दिल्ली में लगभग हर जगह ट्रैफ़िक रेंगता हुआ चलता है। पाँच–दस मिनट की बारिश हो जाए तो आपको हर 500 मीटर पर छोटे-छोटे ‘स्विमिंग पूल’ बीच सड़क पर भी दिख जाते हैं। ऊपर से दिल्ली के गाड़ी-चालकों का हाल यह कि हर कोई मानो एक-दूसरे पर चढ़ जाने को आतुर है और ट्रैफ़िक नियमों की ऐसी-तैसी करते हुए अपना रास्ता बनाने में लगा है।
हालाँकि यह सब बयाँ करना भी एक तरह का ‘प्रिविलेज’ ही है, क्योंकि मेरे घर से 500 मीटर दूर मेन रोड के डिवाइडर पर नज़ारा और भी विचलित करने वाला है। ऊँची मेट्रो लाइन के ठीक नीचे बने उस डिवाइडर पर राजस्थान से आए नट–बाज़ीगर/बंजारा जैसे कुछ खानाबदोश परिवारों ने अपना डेरा जमा रखा है। इनके इतिहास में जाना विषयांतर हो जाएगा, तो यहीं बने रहते हैं—आप थोड़ा गूगल बाबा से पूछिए। हाँ, तो डेरा क्या है—इधर-उधर फैले मैले-कुचैले गद्दे, नीले तिरपाल के बड़े पॉलीथिन जिनको बाँधकर छत बनाई गई है, दो-चार ईंटों को जोड़कर बना हुआ चूल्हा वहीं पर। उसी फुटपाथ–डिवाइडर पर उनका खाना बनता है, बच्चे यहीं सोते-जागते हैं। बच्चे चौराहे की लाल बत्ती पर भीख माँगते दिख जाएँगे, मर्द पास के ढाबों–ठेलों पर मज़दूरी ढूँढ़ते हैं, औरतें भी दो पैसे कमाने के लिए या तो भीख माँगती हैं या कुछ-न-कुछ छोटा-मोटा काम करती होंगी। उनके ठीक सामने सड़क पर बड़े-बड़े विज्ञापन बोर्ड चमक रहे हैं—“सोने के कंगन ले लो।” विज्ञापनकर्ता दावा करता है: “हम ही सबसे शुद्ध गहने बनाते हैं।” बगल में ही यूपीएससी कोचिंग सेंटर के पोस्टर चिपके हैं—“UPSC फ़ाउंडेशन बैच, GS बैच, CSAT बैच…” और जाने क्या-क्या। उत्तर भारत में जवान हुए लड़के-लड़कियों का सपना होता है कि वे कलेक्टर बनें; बनने न भी दें तो भी एक बार तो भैया UPSC का इम्तहान देना है—क्योंकि UPSC कोचिंग के मास्टर लोगों का दावा है कि “एक बार कलेक्टर बन गए तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमेंगे… सोचो, कितने लोग सलाम ठोकेंगे! असली नौकरी तो भारत में एक ही है—IAS, बाकी सब नौकरियाँ हैं,” और मान लो अगर कलेक्टर न भी बने तो “इतना कुछ सीख जाओगे, इतना कुछ सीख जाओगे—पता नहीं कितना कुछ सीख जाओगे!” कोई कहता है कि UPSC का इम्तहान दिया हुआ आदमी “ढंग” का आदमी बन जाता है। मगर उधर पहुँचना है तो पहले इधर आना होगा—हमें बस डेढ़–दो लाख रुपये पकड़ा दो, फिर हम आपको कलेक्टर बना देंगे; कलेक्टर न तो अच्छे इंसान तो बना ही देंगे। उसके बाद चाहो तो जो ये फुटपाथ पर नरक से बदतर जीवन जी रहे हैं, उनके लिए कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकते हो!
इसको पढ़ें वाले मित्रों, घबराइए मत—ये सिर्फ़ एक डिवाइडर की कहानी नहीं है। दिल्ली में ऐसे असंख्य डिवाइडर हैं, फुटपाथ हैं, और उन पर रहने वाले अनगिनत लोग—कूड़े के ढेर के पास, खुले गटरों के सामने, नालों के ऊपर, रेलवे लाइनों के किनारे, फ़्लाइओवरों के नीचे—जहाँ भी इंसानी सोच की सीमा ख़त्म होती है और पाताललोक की सीमा शुरू होती है; वहीं कोई न कोई ज़िंदगी पल रही है, किसी-न-किसी परिवार ने तंबू ताना हुआ है।
मैं भी मुद्दे से भटककर ‘तत्सथ’ यूट्यूब वाले भैया की तरफ़ देश की सामूहिक बदहाली का लेखा-जोखा लेने बैठा। ख़ैर, वापस आता हूँ अपनी रामकहानी पर—क्योंकि हर किसी को अपनी ही पड़ी है। इस घुटन भरे माहौल से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने और मेरी पत्नी निशा ने तय किया कि कहीं तो निकल ही चलते हैं—भले ही दो-चार दिन ही सही, खुली हवा में साँस लेने। अधिकांश उत्तर भारतियों की तरह पहले ख़याल आया कि पहाड़ों की तरफ़ चलें और किसी हिल स्टेशन पर चिप्स–कुरकुरे चबाते हुए, गला फाड़कर ‘काँव-काँव’ करते हुए वहाँ की शांति में ख़लल डाला जाए। मगर फिर तुरंत फ़ितरत ने लगाम लगाई—पहाड़ों की सैर में अच्छा-ख़ासा ख़र्चा हो जाएगा और पॉकेट इस वक़्त इजाज़त नहीं दे रहा था। तब सोचा, अपने कुछ पुराने दोस्तों से ही मिला जाए, जिनसे मिलने की तमन्ना काफ़ी समय से दिल में थी।
यही सोचकर हमने कानपुर जाने का फ़ैसला किया, जहाँ मेरे परम मित्र—और अंग्रेज़ी जुमला उधार लूँ तो ‘फ़्रेंड, फ़िलॉसफ़र, गाइड’—रमाशंकर सिंह रहते हैं। उनसे मिले भी अरसा हो गया था... और दिल्ली से निकलने का मक़सद तो हल होना ही था—तो प्लान बना कानपुर का। अब सवाल था सफ़र के साधन का—तो भई, हर आम हिंदुस्तानी की तरह हमने भी भारतीय रेल पकड़ने की ठानी।
वंदे भारत
हमारी ट्रेन थी नई-नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस, जो सुबह छह बजे दिल्ली से कानपुर (और आगे बनारस तक भी जाती है) जाती है। पत्नीजी ने रेल-यात्राएँ ज़्यादा नहीं की थीं, मगर मैं तो अपने “पूर्वजन्म” (यानी कॉलेज के बाद सरकारी नौकरी की परीक्षाओं) के चक्कर में उत्तर से दक्षिण तक ट्रेन से नाप चुका हूँ। सोचा, इस बार आधुनिक वंदे भारत आज़माते हैं। टिकट आसानी से मिल गई। शायद इसलिए कि बाकी मेल–एक्सप्रेस के मुक़ाबले वंदे भारत की टिकट महँगी होती है और बहुत लोग उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते—कम-से-कम मुझे तो यही वजह समझ आई।
सुबह चार बजे नींद से लड़खड़ाते हम उठे और स्टेशन जाने के लिए रैपिडो से कैब बुक की। इतनी सुबह सड़कें सुनसान तो थीं, लेकिन जिस कबाड़ गाड़ी ने हमें पिकअप किया, वह अपनी ही चिंता का विषय थी। पहला सवाल मैंने ड्राइवर से यही पूछा, “भाई, ये गाड़ी के टायर निकलकर भाग तो नहीं जाएँगे न?” बंदे ने मुँह फैलाकर कहा, “नहीं सर, बस शॉकर की थोड़ी दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है!” फिर उसने डैशबोर्ड से लटक रही लाल–नीली तारों को ज़रा हिलाया-डुलाया और बड़े जोश से हॉर्न बजाकर गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी।
रास्ते भर, अपनी आदत अनुसार, मैं उससे इधर-उधर की बातें करने लगा (ध्यान रहे, मैं कोई टैक्सी-एथनोग्राफ़ी नहीं कर रहा था, बस यूँ ही गप्प मार रहा था)। लड़का करीब 22–23 साल का दुबला-पतला नौजवान था, यूपी के किसी गाँव से। और लगभग हर ओला/रैपिडो ड्राइवर की तरह उसने भी वही जुमला सुना दिया—“सर, घर की मजबूरियाँ थीं, पढ़ाई नहीं कर पाया।” फिर जैसे मेरी उत्सुकता को भाँपकर जोड़ने लगा कि दिल्ली में कैसे वो सीमित कमाई में गुज़र करता है। बातचीत को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने मुस्कुराकर पूछ लिया, “शादी-वादी या कोई गर्लफ़्रेंड-वर्लफ़्रेंड है?” पता नहीं मेरी बात ने गाड़ी की तार को छेड़ा या इसके दिल की—वो एकदम भावुक आवाज़ में बोला, “सर, बड़ी दर्दभरी दास्तान है… मत पूछो, वरना रो दूँगा।” अब हमारी उत्सुकता तो और बढ़ गई—मैंने कहा, “भाई, अब तो बतानी ही पड़ेगी! इतना ‘ट्रेलर’ दिखा दिया है तो ‘पिक्चर’ भी सुना दो, बस रोना मत—नहीं तो मज़ा नहीं आएगा।” साइड सीट पर पत्नीजी हल्की खीज के साथ बोलीं, “रहने भी दो, क्यों बेचारे के ज़ख्म कुरेद रहे हो।” मगर मैं ठहरा किस्सागो क़िस्म का इंसान—सो ड्राइवर को उकसाते हुए बोला, “अगर रोना आ गया तो मत सुनाओ, पर मेरा दिल कहता है, तुम हँसाते-हँसाते रोओगे नहीं।” लड़का थोड़ा सहज हुआ और हँसते हुए बोल पड़ा, “एक लड़की थी, जिसके चक्कर में बरबाद हो गया… और आख़िर में उसकी शादी किसी और से हो गई!”—टिपिकल प्रेमकहानी निकली। ख़ैर, वो रोया तो नहीं, पर पुरानी याद में खोकर गाड़ी ज़रा आड़ी-तिरछी चलाने लगा, तब मुझे ही संभालना पड़ा—“कोई नहीं भाई, छोड़ो उन बातों को। आगे और भी गाड़ियाँ—मतलब लड़कियाँ—आएँगी।” इतना सुनते ही वो अपने झटकेदार शॉकर वाली गाड़ी को फिर पटरी पर ले आया।
स्टेशन पहुँचे तो आँखों में नींद और हाथों में दो छोटे बैग थे। प्लेटफ़ॉर्म के मुख्य द्वार पर क़दम रखते ही हमें अपने महान देश की विकास-यात्रा का साक्षात दर्शन हुआ। सवेरे के अँधेरे में सैकड़ों लोग बिना चादर–तकिया–पलंग के ठंडे फ़र्श पर यूँ ही सोए पड़े थे। नज़ारा इतना मार्मिक था कि कोई विदेशी फ़ोटोग्राफ़र दो-चार फ़ोटो खींचकर उस पर भावुक टिप्पणी लिख दे तो वर्ल्ड प्रेस फोटो जैसी प्रतियोगिता जीत ले। वहीं किसी प्रगतिशील विश्वविद्यालयी युवा कवि के लिए यह दृश्य एक दर्दभरी कविता का बीज साबित हो सकता था, या कोई कथाकार यहाँ से अपने उपन्यास के पात्र जुटा सकता था। किसी शोधार्थी को तो मानो ‘रेडीमेड’ एथनोग्राफ़िक डेटा मिल जाए! हम अपने भारी क़दम सँभालते-सँभालते उन सोए शरीरों के बीच से गुज़रे और मन ही मन चिर-परिचित मध्यमवर्गीय राग आलापा कि “इसमें मेरा कोई कुसूर नहीं, ये तो संस्थागत समस्याएँ हैं।” प्लेटफ़ॉर्म की तरफ़ बढ़ चले।
उसी सुबह टाइम स्लॉट में वंदे भारत की दो-तीन ट्रेनें अलग-अलग जगहों के लिए चलने वाली थीं। हम पहले हड़बड़ी में प्लेटफ़ॉर्म ग्यारह पर जा पहुँचे, फिर अनाउंसमेंट ठीक से सुनने पर लगा—नहीं, 16 नंबर पर जाना है। भला हो पत्नी जी के ‘कॉमन सेंस’ का कि उन्होंने भागमभाग रोककर सही ट्रेन के सही प्लेटफ़ॉर्म पर हमें समय रहते पहुँचा दिया। भारतीय रेलवे का वह प्लेटफ़ॉर्म भी किसी औसत प्लेटफ़ॉर्म जैसा ही था—दीवार पर एक-आध बंदर उछलकूद मचा रहा था, कोने में पान की पीक से लाल हुई दीवारें थीं, कानों में गूँजती ‘चाय, चाय… गरम चाय” की आवाज़ें, आधे जागे, आधे सोए लोग, और सिर पे बोझ लादे इधर-उधर दौड़ते क़ुली।
अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी वंदे भारत ट्रेन लेट है। हमने सोचा—कुछ मिनट की ही बात होगी, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। मगर मिनट से घंटे होने में देर न लगी—ट्रेन कुल डेढ़ घंटे लेट आई। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, “कोई बात नहीं, इतने बड़े देश में इतना तो होता रहता है—और मैं जापान में नहीं हूँ कि रेलवे वाले ‘सॉरी’ कहेंगे; और यह भी गनीमत है कि ये डेढ़ ही घंटा लेट है, नहीं तो भारतीय रेल कई-कई बार तो...”
ख़ैर, ट्रेन आते ही लोगों में अफ़रा-तफ़री मच गई। ध्यान रहे—सबकी आरक्षित सीटें थीं, फिर भी धक्का-मुक्की का वह नज़ारा जो मैंने सिर्फ़ हिंदुस्तान में ही देखा है—हर कोई जैसे ओलिंपिक दौड़ का धावक बनकर प्लेटफ़ॉर्म पर भाग पड़ा—“हम फ़र्स्ट! हम फ़र्स्ट!” मेरी बीवी ने मुस्कुराते हुए इस हरकत को अपने अंदाज़ में समझाया, “बेचारा आम भारतीय जीवन भर कहीं न कहीं लाइन में लगकर धकियाया जाता है। ऐसे में जब मौक़ा मिलता है, तो वो चाहकर भी ख़ुद को रोक नहीं पाता—सबसे आगे निकलकर अपना काम पहले निपटाने में ही सुरक्षा महसूस करता है। पीछे वाला भाड़ में जाए! क्योंकि सच तो यह है कि पीछे वाले को मौक़ा मिलते ही वो भी यही करेगा... और यूँ ही क्रम चलता रहेगा।” मुझे उसकी इस ‘सोशियोलॉजिकल’ व्याख्या पर हँसी भी आई और कुछ सोचने पर भी मज़बूर हुआ।
ख़ैर, किसी तरह हमने भी भीड़ के सैलाब के साथ कोच में एंट्री मार ली और अपनी सीट ढूँढ़कर राहत की साँस ली। कोच वाक़ई उम्मीद से बढ़कर साफ़-सुथरा और नई चमक लिए था—नरम नीली रंग की सुंदर सीटें, बड़ी खिड़कियाँ और एसी के बावजूद ताज़गी भरी महक (पुरानी ट्रेनों में जो सीलन और पसीने का मिश्रित इत्र फैला रहता है, उससे मुक्त)। पाँच मिनट बाद हमारी सीट पर दो बोतल ‘रेल नीर’ पानी आ गया—वह भी मुफ़्त! और साथ में एक प्लास्टिक की पाउच में इंस्टैंट चाय का पाउडर, जिसे गर्म पानी मिलाकर पीना था। गर्म पानी मिलाते ही वो पाउडर—देखते ही देखते—हमारे सामने बेस्वाद पतली चाय में बदल गया। बहरहाल, निशुल्क (जिसका शुल्क टिकट में पहले से जुड़ा है) चीज़ों में अधिक शिकायत भी नहीं करनी चाहिए।
ट्रेन चल पड़ी और हमने कानपुर की ओर अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में मैंने पत्नी को विवेक देबरॉय की भारतीय रेलवे पर लिखी किताब से निकले कुछ क़िस्से और रेलवे के इतिहास की जानकारी सुना-सुनाकर बोर करने की कोशिश की, मगर उसने बोर होने से साफ़ इनकार कर दिया। सो हम दुनिया-जहान की बातें करने लगे—अपनी ज़िंदगी, ज़माने की हालत, सिस्टम के हाल-चाल वगैरह पर खुलकर चर्चा हुई। कुछ देर बाद नाश्ता भी परोसा गया—क्या था, याद नहीं, पर स्वाद काफ़ी अच्छा लगा था। तय समय 10 बजे की बजाय लगभग दोपहर 12 बजे हमारी ट्रेन ने कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर प्रवेश किया।
कानपुर
प्लेटफ़ॉर्म पर उतरते ही मैंने तुरंत अपने मेज़बान रमाशंकर सिंह को कॉल मिलाया। उन्होंने अपना पता भेजा और हम स्टेशन के बाहर आकर ऑटो-रिक्शा में सवार हो गए। मुश्किल से दो मिनट हुए होंगे कि ऑटोवाले ने हमारी वार्तालाप सुनकर पूछा, “भइया, आप लोग हरियाणवी हो क्या?” मैं हँसा और बोला, “हाँ भाई, हरियाणा से ही हैं। माफ़ करना—इसमें मेरा दोष नहीं है!” वह भी हँस पड़ा। शायद मेरे लहजे से उसे कुछ अजीब लगा हो।
कुछ ही देर में ऑटो ने हमें उस पते पर पहुँचा दिया जहाँ हमारे मित्र रहते थे। डॉ. सिंह घर के बाहर ही खड़े मिले और हमें देखते ही बाँहें फैलाकर मुस्कुराते हुए स्वागत किया। हमने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाए और उनके पीछे-पीछे बिल्डिंग के अंदर दाख़िल हो गए। ऊपर उनके फ़्लैट तक जाने के लिए एक पुरानी शैली की ऐतिहासिक लिफ़्ट थी—वही लोहे की खींचने वाली जालीदार दरवाज़े वाली, जैसी नब्बे की हिंदी फ़िल्मों में दिखाई देती थी। जाली का दरवाज़ा दोनों हाथों से खींचकर खोला, अंदर घुसे, फिर पीछे खींचकर बंद किया।
फ़्लैट के मेन गेट पर नेम-प्लेट लगी थी : रमाशंकर सिंह, ख़ुशबू सिंह।” मेरे दिमाग़ ने दौड़ लगाई कि इसे “Drs. Singh” भी लिखा जा सकता था क्या? ख़ैर, दरवाज़े पर दस्तक देते ही अंदर से हमारे नन्हे मेज़बान अनघ प्रकट हुए—सिंह दंपति के प्यारे बेटे। उसने मिलते ही मासूमियत भरा, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से अति-प्रयुक्त सवाल दाग़ा, “मेरे लिए क्या लाए?” हम तैयार थे—मुस्कुराकर तुरंत एक खिलौना डायनासोर बैग से निकाला और उसके हाथ में दे दिया। बस, फिर क्या—बच्चे का चेहरा ऐसा खिल उठा मानो सचमुच जुरासिक पार्क के दर्शन हो गए हों।
घर में प्रवेश करते ही हमें पानी पिलाया गया और साथ में दी गई एक आम के रंग की पेड़े जैसी मिठाई—जिसका स्वाद किसी चॉकलेट जैसा था। मैं जहाँ से आता हूँ, वहाँ पानी के साथ केवल पानी ही पिलाया जाता है—मगर इधर पानी के साथ मिठाई! बाद में इसका एक छोटा-सा ‘एक्सप्लेनेशन’ अभिलेखागार सूरज सिंह ने दिया था। ख़ैर, पानी पीकर हम कुछ साँस में साँस लाए। फिर मेरा पहला काम था—डॉ. सिंह की होम लाइब्रेरी पर नज़र डालना। एक कमरे की दीवार पर अलमारियों में सजी किताबें ही किताबें—इतिहास, साहित्य, राजनीति—हर विषय का ख़ज़ाना। उनकी किताबों की संख्या शायद एक ढंग के क़स्बाई पीजी कॉलेज की लाइब्रेरी को टक्कर देती होगी—बल्कि दस-बीस ज़्यादा ही होंगी! कमाल यह कि उन्हीं अलमारियों के पास एक सुंदर झूला भी लटका था—जिस पर बैठकर आप मज़े से पढ़ भी सकते हैं या यूँ ही झूले का आनंद ले सकते हैं। मैंने मन ही मन ठाना कि कभी पैसा हुआ तो ऐसा झूला तो ज़रूर ख़रीदूँगा अपने लिए… किताबें तो ख़ैर… घर में किताबें होना, आदमी का किताब पढ़ पाना और पढ़ पाने की फ़ुर्सत होना—गहरे राजनीति से ‘लोडेड’ स्टेटमेंट्स हैं…
अगले कुछ घंटे बड़े सुकून से गुज़रे—स्वादिष्ट दोपहर का भोजन, अध्ययन, शाम तक मेज़बान–मेहमान का सायं-प्रसंग (यानी चाय–पानी) और ज्ञान–विज्ञान पर शास्त्रार्थ। बात-से-बात कई बार इस तरफ़ भी गई कि—अमेरिका में क्या होता है और अपने यहाँ क्या नहीं होता। इसी बातचीत में शाम के 5 बज गए और तय हुआ कि ज़रा बाहर घूम आया जाए। मेज़बान ने सुझाव दिया कि यहाँ से पास में ही एक ऐतिहासिक जगह ‘बिठूर’ है, घुमा लाते हैं। मुझे तो मानो मन की मुराद मिल गई—नए शहर में हैं और कोई ऐतिहासिक स्थल देखने को मिल जाए, इससे अच्छा क्या! फिर क्या—उन्होंने अपनी कार निकाली, हम सब (मैं, पत्नीजी, सिंह दंपति और उनके नन्हे अनघ) गाड़ी में लद लिए।
बिठूर
गंगा नदी किनारे कानपुर के पास बसा बिठूर इतिहास में गहरा महत्व रखता है। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद अंग्रेज़ों ने अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पुणे से निर्वासित करके यहीं बिठूर में रखा था। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब पेशवा (धोंदू पंत) ने यहीं बिठूर को अपना मुख्यालय बनाया और मराठा विरासत को उत्तर भारत में जीवित रखा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कानपुर के विद्रोह की कमान नाना साहेब के हाथ में थी और बिठूर उस विप्लव का केंद्र बन गया था। कहा जाता है, नाना साहेब ने अपने प्रमुख साथियों—तात्या टोपे व झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई—के साथ मिलकर यहीं बिठूर के किले की प्राचीर पर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ रणनीति बनाई थी! इसके साथ ही रोचक तथ्य यह है कि लक्ष्मीबाई का बचपन भी बिठूर में ही बीता था; बचपन में ‘मनुबाई’ के रूप में वे पेशवा के दरबार में पली-बढ़ीं। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर में ब्रिटिश सेना से लड़ाई के बाद नाना साहेब यहीं लौटे थे। अंग्रेज़ों ने बाद में इस क्षेत्र पर क़ब्ज़ा करके नाना साहेब का महल और बिठूर के घाटों को तोपों से उड़ा दिया—आज उस समय का सिर्फ़ किला–खंडहर बाकी है, जो गंगा तट पर ख़ामोशी से उन दिनों की गवाही देता है। बिठूर में अब उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा एक स्मृति पार्क विकसित किया गया है, जिसमें 1857 स्मारक संग्रहालय भी है; वहाँ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े दुर्लभ दस्तावेज़, चित्र, सिक्के, हथियार और अन्य वस्तुएँ सहेजकर रखी गई हैं!
हम लोग बिठूर में घाट किनारे गाड़ी से उतरे और आसपास टहलते हुए बतकही करते रहे। सूरज डूबने को था और गंगा का विस्तार सुनहरी आभा लिए शांत बह रहा था। कुछ स्थानीय श्रद्धालु घाट पर स्नान–पूजन में लगे थे। इसके बाद हम गए—वो संग्रहालय और किले के अवशेष देखने—नाना साहेब की हवेली, जहाँ क्रांति के बीज पनपे। इतिहास की किताबों में पढ़ा बहुत कुछ आँखों के सामने घूम रहा था।
शाम घिरने लगी तो हम वापसी के लिए चल पड़े। कानपुर शहर की तरफ़ लौटते समय गाड़ी की हेडलाइट सड़क के गड्ढों को चकमा देती आगे बढ़ रही थी। रास्ते में जगह-जगह नर्सिंग होम और हॉस्पिटल के बड़े-बड़े होर्डिंग्स टँगे दिखे—लगता है, कानपुर में चिकित्सा-व्यवसाय ख़ूब फल-फूल रहा है। सड़क की हालत ने महसूस करा दिया कि इंफ़्रास्ट्रक्चर यहाँ भी अपने देश के औसत मानकों को ही फ़ॉलो करता है। लेकिन इन सबके बीच हमारी बातचीत का केंद्र हमारे नन्हे सहयात्री अनघ बने रहे। अनघ ने कार में बैठे-बैठे हमें कई क़िस्से सुनाए—जिनमें “अंगुलिमाल” का किस्सा मुझे याद है—कई नए जुमले सुनाए; मसलन उसने खिड़की के बाहर मुँह करके कहा, “देखो, हवा का झुमका!” फिर एक बार अपने पापा की किसी हरकत पर मुँह फुलाकर बोला, “आज पापा ने ‘टू मच’ कर दिया, मगर मैंने ‘टू मच’ नहीं किया।” उस नन्ही ज़ुबान से निकले “टू मच” पर हम ख़ूब हँसे। सचमुच, बच्चों की नज़र से दुनिया कितनी अलग और रंगीन दिखती है।
कुल मिलाकर कानपुर में बिठूर वाली हमारी यह छोटी-सी यात्रा बहुत सुखद रही। घर लौटकर रात को बढ़िया भोजन और बातचीत का दौर फिर चला। कब आधी रात हुई, पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह हमें वाराणसी के लिए निकलना था, तो काफ़ी रात गए सोने गए।
वाराणसी
अगले दिन सुबह-सवेरे फिर वही वंदे भारत एक्सप्रेस पकड़नी थी, जो कानपुर से चलकर क़रीब चार-पाँच घंटे में वाराणसी पहुँचा देती है। मैं वाराणसी (बनारस) कई बार पहले जा चुका था, मगर पत्नीजी कभी नहीं गई थीं। ऊपर से वे काशी के अस्सी और व्योमेश शुक्ल जी की किताबों की बड़ी प्रशंसक हैं, तो उनकी तीव्र इच्छा थी कि चलते-चलते बनारस भी घूमा जाए। सो हमने कानपुर से वाराणसी के लिए उसी वंदे भारत में सीट बुक करा ली। सुबह नाश्ता-वाश्ता कर मेज़बान से विदा ली और 10 बजे वाली ट्रेन पकड़ने स्टेशन पहुँचे।
ट्रेन के हमारे डिब्बे में इस बार पिछली सीट पर एक परिवार अपने नन्हे बच्चे के साथ सफ़र कर रहा था। बच्चा अत्यंत उत्साहित था और ट्रेन को ‘टेन-टेन’ कहकर चिल्लाते हुए उछल रहा था। ख़ैर, हमारी सीट पर फिर से रेल नीर आ गया, जिसे पीते-पाते बात निकली कि इस मासूम बच्चे जैसा उत्साह हमने शहरों की भागदौड़ में कब का खो दिया है। हमने आपस में ये भी चर्चा की कि आजकल के बच्चों को किस माहौल में पालना और उन्हें ज़िम्मेदार इंसान बनाना—एक चुनौती होता जा रहा है। हम पैरेंटिंग पर दार्शनिक बातें कर ही रहे थे कि अचानक हमारी ज्ञान-चर्चा को विराम लग गया—एक अप्रत्याशित ‘रासायनिक हमला’ हो चुका था!
हमारे आगे या पीछे किसी सहयात्री ने ज़ोरदार, ज़हरीली गैस छोड़ी थी—और उसका असर ऐसा था कि मेरा मुँह कड़वाहट से भर गया। हम तुरंत सतर्क हुए; एक-दूसरे की तरफ़ देखकर नाक बंद करने की कोशिश की। फिर कुछ पलों में दूसरा वार हुआ। डिब्बे में हलचल-सी मच गई—कुछ सीट आगे से ‘हाय राम!’ जैसी आवाज़ आई, पीछे कोई अंग्रेज़ी में बड़बड़ाया। हम तो मन ही मन “अब तुम ही रखवाले” का जाप करने लगे कि प्रभु इस गैसीय युद्ध से मुक्ति दिलाएँगे तो जीवन भर सादा भोजन खाएँगे!हर 10-15 मिनट के अंतराल पर ये गैसीय गोले फिर चलने लगे। मेरी पत्नी मुझे कनखियों से देख रही थी कि कहीं ये करतूत मेरे पेट की तो नहीं। मैंने भी भौंहें चढ़ाकर आश्वस्त किया कि भाई, ये पाप मेरे सिर न मढ़ो। ख़ैर, करीब आधे घंटे तक यह नाक-झुनझुनी युद्ध चला। जब पास वाले रेस्टरूम का दरवाज़ा बंद हुआ और भीतर किसी की मौजूदगी दर्ज हुई, तब जाकर कोच में कुछ देर के लिए युद्धविराम हुआ। मेरी सोच में यह एक अलग ही तरह का भारतीय रेल अनुभव था—लोग कहते थे, कभी खाने में छिपकली निकल आती है, कभी कॉकरोच, लेकिन यह तो गज़ब हुआ कि कोई अज्ञात योद्धा अपनी आंतरिक आर्टिलरी से पूरे डिब्बे को हिला रहा था!
पहले दिन के सफ़र, रात की कम नींद, ऊपर से इन गैस-बमों की मार—इन सब ने हमें थोड़ा सुस्त कर दिया था। दुपहर क़रीब दो बजे हम वाराणसी पहुँचे तो मन में बस एक ही ख़याल था कि जल्दी से कहीं आराम मिले। स्टेशन पर उतरते ही मैंने अपने पुराने मित्र विकास आनंद को फ़ोन लगाया, जो BHU कैंपस में ही रिसर्च स्कॉलर थे। हमारे लिए यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस में कमरे की व्यवस्था डॉ. सिंह ने करवा दी थी। उधर से विकास भाई का फ़ोन भी आ गया—उन्होंने बताया कि गेस्ट हाउस कैंपस के भीतर है, “मैं आकर मिलता हूँ।” हम ऑटो लेकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के मेन गेट की ओर चल दिए।
क़रीब 15 मिनट की ऑटो-यात्रा में ही वाराणसी शहर की पहली झलक मिल गई—हवा में धूल, कई जगह जाम, सड़क पर जगह-जगह छोटे-मोटे गड्ढे; मानो कानपुर से वाराणसी ‘कॉम्पिटिशन’ चल रहा हो। पत्नी निशा अपने मन में बनारस की जो छवि लेकर आई थीं, वो शायद इस शुरुआती मंज़र से मेल नहीं खा रही थी। ऑटो वाले ने BHU के सिंहद्वार पर हमें उतार दिया। वहाँ से अंदर कैंपस में जाने के लिए बैटरी रिक्शे खड़े थे। जैसा निर्देश मिला था, हमने एक बैटरी रिक्शा लिया और कैंपस के भीतर की सड़कों पर चले। भारत के किसी भी बढ़िया विश्वविद्यालय की तरह BHU का कैंपस एक अलग ही दुनिया है—चौड़ी, साफ़ सड़कें; हरियाली से भरा वातावरण; ख़ूबसूरत भवन; तरह-तरह के विभागों की कतार; और पैदल घूमती नौजवान छात्र-छात्राओं की टोलियाँ। माहौल में एक जोश और तरंग थी। कैंपस में घुसते ही मुझे अपने IIT मद्रास के दिन याद आ गए। मैंने मुस्कुराकर निशा से कहा, “जैसे हर इंसान को अपना गुज़रा ज़माना सबसे अच्छा लगता है, वैसे ही हर इंसान को अपना वाला कैंपस सबसे बढ़िया ही लगता है—जैसे मुझे लग रहा कि मेरा कैंपस इससे बढ़िया था, जबकि हक़ीक़त ये है कि सबका अपना-अपना चार्म है!” वो भी हँस दीं।
BHU गेस्ट हाउस पहुँचकर हमने चेक-इन किया। दो दिन के लिए कमरा बुक था। अंदर जाकर देखा तो कमरा ठीक किसी OYO होटल जैसा था—साफ़-सुथरा बिस्तर, हवादार खिड़की, अटैच्ड बाथरूम और नब्बे मॉडल का पुराना एसी। मैंने मज़ाक़ में निशा से कहा, “यार, ‘गेस्ट हाउस’ और ‘रेस्ट हाउस’ का ज़िक्र हमने अब तक सिर्फ़ हिंदी उपन्यासों में पढ़ा था... ज़िंदगी में आज पहली बार सच में देख लिया!” फ़्रेश होकर थोड़ा आराम किया—तब तक शाम हो चली थी।
BHU कैंपस
तब तक हमारे साथी विकास भाई अपने एक दोस्त शुभम के साथ हमें लेने गेस्ट हाउस आ पहुँचे। योजना बनी कि पहले चाय-वाय पी जाए, फिर शहर घूमा जाएगा। विकास BHU में ही रिसर्चर थे, तो कैंपस और शहर से भली-भाँति वाक़िफ़ थे। सबसे पहले वे हमें कैंपस के मशहूर विश्वनाथ मंदिर (जिसे वहाँ VT भी कहते हैं) की ओर ले चले।
रास्ते में एक चाय की टपरी पर रुके, मगर वहाँ छात्रों की भीड़ थी—तो तय हुआ कि कहीं दूसरी जगह चलते हैं। VT के सामने हमने कोल्ड कॉफ़ी ली और वहाँ से मंदिर चले गए। मंदिर कैंपस के बीचोंबीच एक विशाल स्तंभ जैसा भवन है, जिसकी ऊँची शिखर दूर से ही दिखती है। मंदिर के ठीक सामने ही सड़क पर चौराहा है, जहाँ ऑटो-रिक्शे, कैंपस बसें और दुकानें हैं। आसपास किताबों की दुकानों से लेकर चाय–नाश्ते और पूजन-सामग्री की कई छोटी-बड़ी दुकानें सजी थीं। माहौल में हलचल थी—सैलानी, तीर्थयात्री, छात्र—सब मंदिर की ओर आ-जा रहे थे।
मंदिर के मुख्य फाटक पर प्रवेश करते ही हमने एक अनूठा दृश्य देखा—एक स्केच आर्टिस्ट बाहर चौक पर बैठा एक अधेड़ उम्र के सज्जन का ‘लाइव स्केच’ बना रहा था। सामने बोर्ड लगा था—“Live Sketch बनवाएँ: 15 मिनट में।” उसकी बगल में कौतूहल से तमाशबीनों की छोटी भीड़ खड़ी थी। हमने भी क़रीब जाकर देखा—लगभग पैंतीस बरस का एक ठिक-ठाक तंदुरुस्त युवक, जिसने अमिताभ बच्चन स्टाइल में बाल संवारे थे, जींस–टीशर्ट पहने तन्मयता से चारकोल पेंसिल चला रहा था। उसके हाथों में ऐसी सफ़ाई और आँखों में ऐसा फोकस था कि देखना बनता था। मेरे मन में तुरंत ख्याल आया—क्यों न अपनी पत्नी का स्केच बनवा डालूँ? मैंने झिझकते हुए निशा से पूछा, “बनवाएँ क्या?”—उसने कंधे उचका दिए—‘जैसी तुम्हारी मर्ज़ी’ वाला भाव था। तो मैंने आगे बढ़कर उस कलाकार से पूछा, “भाई साहब, हमारा भी स्केच बना दोगे?”—उसने बिना नज़र हटाए जवाब दिया, “यही तो करने के लिए बैठे हैं, आप 15–20 मिनट बाद आइए।” हमने सोचा—तब तक मंदिर घूम लेते हैं।
हमने मंदिर परिसर के भीतर प्रवेश किया। बिरला परिवार द्वारा बनवाया गया यह विश्वनाथ मंदिर बेहद भव्य और स्वच्छ था—सफ़ेद संगमरमर-से चमकते फ़र्श, ऊँचे खंभे और बीच में गर्भगृह, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। हम दर्शन के लिए लाइन में नहीं लगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य धार्मिक से ज़्यादा पर्यटन वाला था। एक ओर खड़े होकर देखा—कुछ श्रद्धालु शिवलिंग पर फल–फूल चढ़ा रहे थे, वहीं पुजारी लगातार एक पात्र से दूध की धारा शिवलिंग पर अर्पित करते जा रहे थे। हमने जेब से फ़ोन निकाले और स्मृति हेतु दो-चार तस्वीरें खींच लीं। मुख्य शिवलिंग के ऊपर चाँदी-सा चमकता छत्र था। स्तंभों पर बारीक नक्काशी थी, जो आधुनिक वास्तु में पारंपरिक ‘टच’ दे रही थी। कुछ देर वहाँ बिताकर हम बाहर लॉन में आ गए।
बाहर मंदिर परिसर के बगीचे में टहलते हुए विकास भाई ने हमें एक पेड़ की ओर इशारा करके कहा, “वो देखो, सामने सिंदूर का पेड़ लगा है।” हमने चौंककर पूछा, “अच्छा! सिंदूर का पेड़ भी होता है?” असल में हाल के महीनों में न्यूज़ और सोशल मीडिया पर हर जगह “ऑपरेशन सिंदूर” की चर्चा सुन रहे थे; इसलिए “सिंदूर” शब्द कान में पड़ते ही हमारी भी नाड़ियों में हलचल-सी मच गई—बड़े कौतूहल से हम उस पेड़ को देखने लपके। पास जाकर देखा तो पता चला—यह सच में सिंदूर का फ़ूल है, जिसके फल/बीज से सिंदूर बनाया जाता है। ख़ैर, हमारा VT मंदिर का “ऑपरेशन सिंदूर” संपन्न हुआ।
कुछ देर बाद हम वापस मंदिर गेट के बाहर उस स्केच वाले कलाकार के पास पहुँचे। उन्होंने वादे के मुताबिक 15–20 मिनट में निशा का स्केच तैयार कर दिया था। ड्रॉइंग शीट पर बना चेहरा निशा से काफ़ी मेल खा रहा था, बस गाल और ठोड़ी ज़रा गोल-मटोल हो गई थी। निशा ने स्केच देखते ही नाक सिकोड़कर कहा, “ये मेरा स्केच नहीं लगता… इसमें तो मैं बहुत मोटी दिख रही हूँ।” मैंने हँसकर जवाब दिया, “अरे पगली, तुम ही हो—बस ज़रा चेहरे पर चमक बढ़ गई है।” कलाकार ने भी हामी भरी—“मैडम, मैंने बस थोड़ा स्माइल ज़्यादा कर दिया है, बाकी आँख–नाक सब आपका ही बनाया है!” हमने उसे 500 रुपये फ़ीस अदा किए और स्केच को रोल करके सँभाल लिया। यह हमारे सफ़र की एक ख़ूबसूरत यादगार के तौर पर साथ रहने वाला था।
अब बारी थी बनारस के घाटों की। एक ऑटो लेकर हम लोग दशाश्वमेध घाट की ओर चल पड़े, जहाँ शाम की मशहूर गंगा आरती देखने का प्लान था।
गंगा आरती
वाराणसी की गंगा आरती विश्वप्रसिद्ध है—हर शाम ढलते सूरज के बाद सैकड़ों लोग घाट पर इकट्ठा होकर गंगा की आरती का दिव्य नज़ारा देखने आते हैं। पंडितों द्वारा बड़े-बड़े दीयों और धूप–दीप से की जाने वाली इस आरती में सामूहिक भक्ति और उत्सव का अनोखा मेल देखने को मिलता है। हमने भी सुना था कि यहाँ की आरती देखे बिना यात्रा अधूरी है, इसलिए उत्साहित थे। सितंबर का महीना था, बारिश का मौसम पूरा उतरा नहीं था, तो गंगा उफ़ान पर थी। घाटों की सीढ़ियाँ आधी पानी में डूबी हुई थीं, हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी।
आरती शुरू होने का समय क़रीब सात या साढ़े सात बजे था, लेकिन हम सवा छह के आस-पास ही पहुँच गए—सोचा था, पहले जाकर बढ़िया जगह घेर लेंगे। पर नज़ारा देखकर दंग रह गए—आरती स्थल की तरफ़ तो तिल धरने की भी जगह नहीं बची थी! लगा मानो शहर भर की भीड़ आज ही उमड़ आई हो। सैकड़ों लोग घाट की सीढ़ियों पर खड़े; कुछ बैठने की जगह घेरकर टिके हुए; और ‘लेट कमर्स’ (हमारी तरह) भीड़ को चीरते आगे बढ़ने की जुगत में थे। हर किसी की चाहत कि आरती बिलकुल सामने से देखें। धक्का-मुक्की का आलम ये कि लगा—अगर ज़ोर लगाकर घुसने की कोशिश की तो या तो खुद गिरेंगे या दूसरों को गिरा देंगे।
उसी अफ़रा-तफ़री में एक किनारे से आवाज़ लगाते कुछ लोकल युवक भी दिखे—“भाई साहब, नीचे जगह नहीं है। ऊपर बालकनी से आराम से देखेंगे? सौ रुपये लगेंगे बस—आ जाइए, शांति से आरती देखिए।” हम समझ गए—ये प्राइवेट दुकानों के मालिक पैसे लेकर पर्यटकों को ‘व्यूइंग स्पॉट’ ऑफ़र करते हैं। हर तीर्थ-स्थल पर ऐसा जुगाड़ होता ही है—बिठूर में भी एक नाव वाला उफ़नती गंगा में लोगों को नाव से घुमाने के लिए कन्विन्स कर रहा था! हम दोनों ने एक-दूसरे को देखा और कहा—“भीड़ में घुसने से तो बेहतर है, चलो थोड़ा खर्च कर लेते हैं।” फिर तुरंत विचार बदल भी गया—“नहीं, इसमें क्या मज़ा कि पैसे देकर देखें?” तभी बूंदाबांदी थोड़ी तेज़ होने लगी। पत्नी ने हल्के रूखे स्वर में कहा, “छोड़ो, नहीं देखनी—भीग भी जाएँगे फ़ालतू में।” मैंने कहा, “ठीक है, रहने देते हैं… कभी फिर आएँगे तो आराम से देख लेंगे।” इस तरह आरती शुरू होने कुछ समय बाद ही हम घाट की सीढ़ियों से किनारे हट गए। मन में हल्का अफ़सोस तो रहा कि पास से पूरा अनुभव नहीं कर पाए, मगर जो झलक मिली—वो भी ख़ूब थी।
भीड़ और भीगन से बचते-बचाते हम नज़दीकी गली में आ गए। बनारस की गलियाँ भी किसी भी भारतीय शहर की गलियों जैसी ही हैं—तंग रास्ते, भीड़, गंदगी, सड़क पर कब्ज़ा करती सजी-धजी दुकानें, रिक्शा–बाइक के हॉर्न, चिल्ल-पों। हमने सोचा—चलो एक बढ़िया चाय पी जाए। पास ही दुकानों की लाइन में चाय का स्टॉल दिख गया। चाय की चुस्कियों के साथ हम उस शाम के रोमांच और अव्यवस्था—दोनों को डिस्कस करते रहे। भीड़-भाड़, गंदगी, ऑर्गनाइज़ेशन की कमी—इन पर थोड़ी देर बड़बड़ाए—फिर बोले, “छोड़ो इन बातों को और खाने का कुछ जुगाड़ करते हैं।” तो एक किलोमीटर दूर पैदल चलने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट मिला—जैसा कोई भी उत्तर भारतीय रेस्टोरेंट हो सकता है, वैसा ही; वही पनीर, आलू, अलाना–फलाना—आप रोहतक में हों या कानपुर में या बनारस में—कोई अंतर नहीं मिलेगा; वही ‘सेम टू सेम’। स्वाद थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकता है, मगर मसाले, शक्ल-सूरत, बनाने का तरीक़ा—सब सेम।
रात काफ़ी हो चली थी। हम वापस गेस्ट हाउस लौट गए। कपड़े वगैरह बदलकर सोने की तैयारी की। अगली सुबह एक और कोशिश थी—सुबह-ए-बनारस देखने की, यानी सूर्योदय के वक्त घाट पर जाना। कहते हैं, बनारस का सवेरा दुनिया भर में मशहूर है—सूरज की पहली किरण और गंगा की लहरें; उसे देखने रोज़ सैकड़ों लोग जुटते हैं। हमने भी अलार्म 4:30 का लगा लिया और सो गए।
बनारसी नाश्ता और सारनाथ की सैर
सुबह चार बजे के आसपास हमारी नींद खुली तो पाया—बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है! अँधेरा छाया था और पानी ऐसा बरस रहा था, मानो बादल फट पड़ा हो। नींद से बोझिल आँखें मलते हुए मैंने खिड़की से झाँका और तुरंत कंबल ओढ़कर फिर सोने में भलाई समझी। पत्नी ने एक बार पूछा भी—“क्या करें?”—मैंने कहा, “बारिश में क्या ख़ाक देख पाएँगे घाट—सो जाओ।” हम दोनों फिर नींद के आगोश में चले गए। अगली बार 7 बजे के करीब आँख खुली तो देखा—बारिश हल्की तो हुई थी मगर बंद नहीं। उदास मन से मैंने कहा—“चलो, आज हमारी किस्मत में घाट देखना नहीं लिखा।” तभी 8 बजे के आसपास विकास का फ़ोन आया—“मैं गेस्ट हाउस के बाहर खड़ा हूँ, तैयार हो जाओ।” ओह! हम तो मानो ऊँघ ही रहे थे—तुरंत फ़्रेश हुए, तैयार होकर नीचे भागे। हमें नाश्ता और घूमने के लिए विकास के साथ जाना था। हम गेस्ट हाउस का नाश्ता छोड़कर इसलिए निकले थे कि बनारसी स्टाइल नाश्ता चखा जाए—जिसका खूब नाम सुन रखा था (चाहे ‘काशी का अस्सी’ उपन्यास हो या बनारस पर लिखी अनेक किस्से–कहानियाँ—सबमें वहाँ के स्वाद का बखान रहता है)—तो भला हम होटल का टोस्ट–बटर क्यों खाते!
विकास हमें लंका इलाक़े की एक मशहूर जलेबी–कचौड़ी की दुकानों की तरफ़ ले गए। रात भर की बारिश के कारण किचकिच का माहौल था। ऐसे में सड़क किनारे कुछ हलवाइयों जैसी दुकानें दिखीं—वही हमारी मंज़िल थी। पतली-सी गलीनुमा दुकान, आगे लकड़ी के तख़्त पर कड़ाही चढ़ी हुई, जिसमें गोल-गोल पूड़ियाँ तली जा रही थीं। बगल की कड़ाही में सुनहरी जलेबियाँ पक रही थीं। आलू–मटर की मसालेदार सब्ज़ी भी बड़े भगोने में तैयार थी। चारों ओर एक अजीब-सी गंध का मिश्रण—तेल–घी जो भी रहा हो—उसकी महक। हमने दुकान के अंदर पाँव रखा और लकड़ी की बेंच पर जगह सँभाली। विकास ने दुकानदार को इशारे से ऑर्डर दे दिया—तुरत-फुरत चार पूड़ियाँ दोने में परोसकर एक आदमी हमारे सामने रख गया; साथ में कटोरी में आलू वाली सब्ज़ी थी। नाश्ता शुरू किया। पहला कौर लेते ही समझ आ गया कि बनारसी नाश्ते की इतनी चर्चा क्यों है—हमने दो पूड़ियाँ सफ़ाचट कर डालीं। तीसरी की तरफ़ हाथ बढ़ाया ही था कि पेट ने संकेत दिया—बस भाई, बस! वरना अगले स्थान तक पहुँचते-पहुँचते हालत ख़राब हो जाएगी। अभी सुबह के केवल साढ़े आठ बजे थे और हम इतनी भारी चीज़ें खा चुके थे—तो थोड़ा संयम बरतना पड़ा।
अब आगे कार्यक्रम था—सारनाथ जाने का। सारनाथ, वाराणसी से लगभग 10 किमी दूर, वह स्थान है जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान-प्राप्ति के बाद पहला उपदेश अपने शिष्यों को दिया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के पवित्रतम स्थलों में एक है और भारतीय इतिहास में भी इसका अहम स्थान है। हम दिल्ली की DTC-नुमा बस से करीब आधे घंटे में सारनाथ पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही जो बात महसूस हुई, वो यह कि सारनाथ काफ़ी साफ़-सुथरा और शांत था—BHU वाले इलाक़े के मुक़ाबले शायद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की देखरेख के कारण यहाँ कचरा या अव्यवस्था अपेक्षाकृत कम थी। ख़ैर, हम ऐतिहासिक खंडहरों की ओर चल दिए।
सबसे पहले हम उस मृगदाव पार्क (हिरण उद्यान) में गए, जहाँ एक विशाल, गोलाकार, ईंट-निर्मित स्तूप खड़ा है। यही प्रसिद्ध ‘धमेख स्तूप’ है—जो उसी जगह पर बना है, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पाँच साथियों को ‘धर्मचक्र-प्रवर्तन सूत्र’ सुनाया था। आज यह एक ठोस स्तूप के रूप में आसमान को छूता दिखता है, लेकिन ढाई हजार साल पहले यहीं पर बुद्ध ने अहिंसा, मध्यमार्ग और चार आर्य सत्यों का पाठ पढ़ाया था। वहाँ खड़े होकर मैं आँखें बंद कर ज़रा कल्पना में डूबा—“ढाई हज़ार वर्ष पूर्व कोई तपस्वी इसी भूमि पर चला होगा—अपने मन और समाज के सवालों का हल खोजते हुए… यहीं कुछ शिष्य उम्मीद भरी निगाहों से उसके पास बैठे होंगे और उस महान आत्मा ने उन्हें जीवन का मार्ग समझाया होगा।” वह स्थान एक अजीब-सी आध्यात्मिक शांति से भरा लगा।
फिर हम आगे बढ़े और एक पुरानी नींव/चबूतरे को देखा, जिस पर सूचना-पट्ट लगा था—यहीं सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया अशोक स्तंभ कभी खड़ा था। यही वह जगह है, जहाँ से खुदाई में अशोक स्तंभ के शीर्षभाग—चार सिंहों वाली मूर्ति—निकाली गई थी, जिसे भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। मुझे उस स्थान को देखकर रोंगटे खड़े हो गए—सोचिए, तीसरी सदी ईसा-पूर्व में सम्राट अशोक के बनाए स्तंभ को यहाँ लोगों ने देखा होगा; फिर वो सदियों तक ज़मीन में दबा रहा और आज—आजाद भारत की हर सरकारी मोहर पर उसी की छाप है।
अब अगला पड़ाव था—सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय। हमें बताया गया कि संग्रहालय के अंदर कैमरा ले जाना मना था—मगर इस बार पता नहीं क्या हुआ कि हमें फ़ोन ले जाने दिया गया। हमने पाँच रुपये की टिकट ली और चल पड़े संग्रहालय देखने। भीड़ बहुत कम ही थी। हल्की पीली रोशनी वाले इस संग्रहालय में क़दम रखते ही ऐसा लगा जैसे सीधे इतिहास के किसी गलियारे में प्रवेश कर गए हों। यहाँ पर बहुत सारी विशाल प्रस्तर-प्रतिमाएँ दिखीं—पाँचवीं शताब्दी ईस्वी की बनी भगवान बुद्ध की मूर्ति, जो ध्यान-मग्न अवस्था में थी। आगे चलने पर अनेक पुरानी मूर्तियाँ, शिलालेख, मिट्टी के बर्तन, सिक्के करीने से सजे थे। और ठीक बीचोंबीच प्रदर्शनी-कक्ष में, गोल घुमावदार शोकेस में रखी थी—अशोक स्तंभ की मूल शेरों वाली मूर्ति! जी हाँ—चार सिंहराज पीठ-से-पीठ सटाए, विशाल मुद्रा में खड़े हुए; और नीचे विशाल पत्थर का गोल चक्र तथा हाथी–घोड़े–बैल आदि उकेरे हुए—यही हमारा राष्ट्रीय चिह्न है। उसे वास्तविक रूप में अपने सामने पाकर दिल की धड़कन तेज़ हो गई। पत्थर पर महीन उकेरण और दमक—देखते ही बनती थी। हम कुछ देर अपलक उसे निहारते रहे। सोचा—कितने लोग रोज़ नोटों पर, सरकारी निशान पर इसको देखते हैं, मगर शायद ही जानते हैं कि असलन यह कितनी सदियों पुरानी विरासत है और कहाँ से आई है।
संग्रहालय में लगभग एक घंटा बिताकर हम बाहर निकले तो सूरज सिर पर चढ़ आया था। हल्की गर्मी महसूस होने लगी थी, लेकिन मन प्रफुल्लित था। सारनाथ ने हमारे मन को एकदम शांत और पुण्य-अनुभूति से भर दिया था।
बनारस की इस छोटी-सी यात्रा का यह अंतिम पड़ाव था। दो दिन पहले हम दिल्ली की बंद चारदीवारी से ऊबे हुए निकले थे, और इन दो दिनों में जितना कुछ देख–सुन लिया था—वह जीवन भर याद रहने वाला था। दिल्ली की आपाधापी, कानपुर–बिठूर का इतिहास और वाराणसी–सारनाथ की संस्कृति—इन सबने मिलकर हमें अपने देश को बाहरी और भीतरी—दोनों नज़रियों से देखने का एक नया परिप्रेक्ष्य दिया।
•••
रविंद्र कुमार को और यहाँ पढ़िए : मृत्यु ही जीवन का सबसे विश्वसनीय वादा है
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

