आपातकाल से अघोषित आपातकाल के बीच
 हिन्दवी डेस्क
21 सितम्बर 2024
हिन्दवी डेस्क
21 सितम्बर 2024
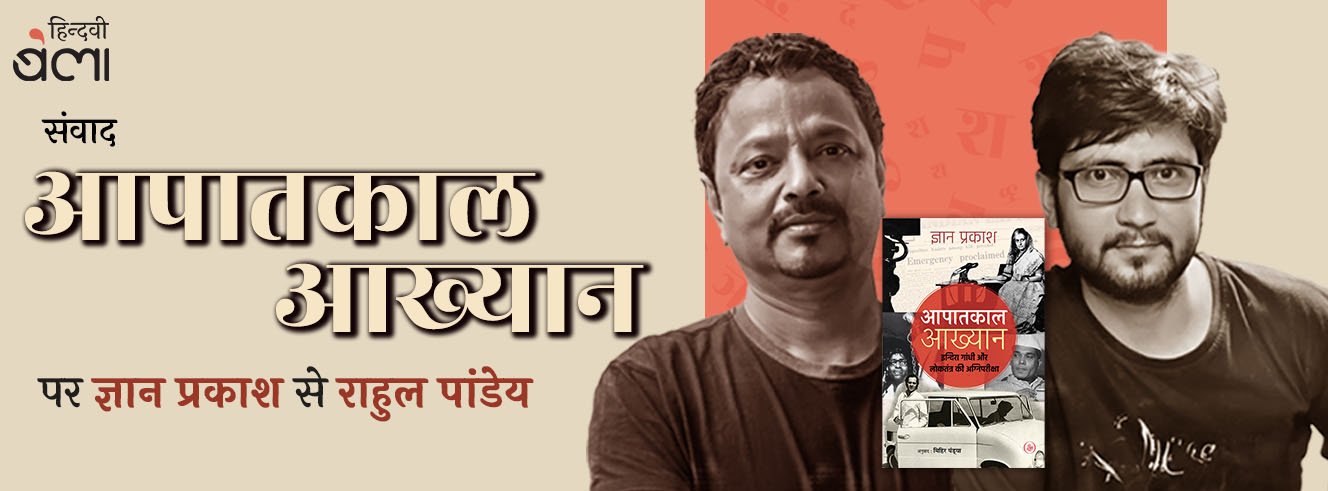
गए दिनों ज्ञान प्रकाश की किताब ‘आपातकाल आख्यान’ आई। राजकमल प्रकाशन से आई इस किताब में, उन्होंने 1975 में लगी इमरजेंसी की चर्चा की है। ज्ञान प्रकाश अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर हैं। यहाँ प्रस्तुत है इस किताब के बहाने ज्ञान प्रकाश और राहुल पांडेय की बातचीत के प्रमुख अंश :
भारतीय लोकतंत्र में अधिनायकवाद को कब-कब देखते हैं?
एक तो इसकी जो एक धारा है, वह हमारे संविधान में थोड़ी-बहुत पहले से ही है। और इसकी जो जड़ है, वह ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय की है। 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया एक्ट बना था, उसमें बहुत से ऐसे प्रावधान थे, जिसमें सत्ता को बहुत ज़्यादा ताक़त दी गई थी। जब हमारा संविधान बना, तो उस समय एक आशा थी कि देश के नेता सत्ता को ज़िम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, और जैसा सब जानते हैं कि 1975 में आपातकाल में इंदिरा गांधी ने हमारे संविधान के जो बहुत से अधिकार थे, उनको निलंबित कर दिया।
1977 में जब आपातकाल ख़त्म हुआ, उस समय के बहुत से क़ानून थे जिनको जारी रखा गया। अब पिछले दस सालों में उन क़ानूनों को और ज़्यादा लागू किया गया है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय से ही क़ानून में ऐसी बहुत-सी धाराएँ हैं, जिसमें सत्ता को तानाशाही टाइप की पावर दी जाती है, और उसका सत्ता ने इस्तेमाल किया है। अक्सर कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है और फिर आपातकाल आ जाता है।
क्या यह आपस में विरोधाभास नहीं?
देखिए संविधान में दो प्रवृत्तियाँ हैं।
एक है कि लोकतंत्र में जनता को अधिकार हो। अँग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़ाई थी, वह जनता ने इसलिए लड़ी थी कि उसे अधिकार हो।
दूसरी प्रवृत्ति यह है कि सत्ता को ताक़त हो। उसका कारण यह भी था कि जब हमारी आज़ादी हुई और बँटवारा हुआ तो उस समय माहौल ऐसा था कि देश के नेताओं को यह ज़रूरत लगी कि सत्ता के पास ऐसी ताक़त हो जो देश की एकता को बनाए रखे। तो इन दोनों धाराओं में परस्पर विरोध चलता रहा।
जैसे मैंने अपनी किताब में लिखा है कि उस समय एक आशा थी कि एक नाज़ुक संतुलन बना रहेगा इन दोनों धाराओं में। यह संतुलन 1975 में पहले सत्ता की तरफ़ झुका और उसके बाद फिर अब 2014 से उसको और इस्तेमाल किया गया है। इससे जनता का जो अधिकार है, उसकी जो आवाज़ है, उसको नियंत्रण में रखने के लिए सरकार ने अपनी जितनी ताक़तें हैं, उसका इस्तेमाल किया है।
आजकल इसको बहुत लोग अघोषित आपातकाल कहते हैं। इसी पर आते हैं। पिछले दिनों संसद में इमरजेंसी का ज़िक्र किया। इमरजेंसी का सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और फिर स्पीकर ओम बिरला ने भी किया। यह बच्चों वाली तू-तू मैं-मैं टाइप के सवाल होते हैं कि आपने किया, हमने नहीं किया। इसका मक़सद है कि लोकतंत्र के सामने जो वाक़ई चुनौती है उसको नज़रअंदाज़ करके सबको उसी तक सवाल सीमित रखें।
मेरी किताब से ये तक़रीर है कि 1975 में जो हुआ उसको हम ऐतिहासिक और लंबे दौर में अगर देखें तो वो चुनौती केवल प्रक्रियाओं की चुनौती नहीं थी। वो चुनौती थी जिसके बारे में अम्बेडकर ने 1949 में कहा था, जब उन्होंने संविधान प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी, 1950 को देश आज़ाद होगा। उसमें एक तरफ़ तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ़ सामाजिक और आर्थिक असमानता ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकती। उस समय आशा थी कि संविधान और आज़ादी मिलने के बाद राजनीतिक और आर्थिक समानता आएगी जो सही मायने में लोकतंत्र को स्थापित करेगी।
अम्बेडकर का कहना था कि लोकतंत्र का मतलब केवल उसकी प्रक्रिया नहीं होती। लोकतंत्र का मतलब होता है—रोज़मर्रा के जीवन में सबकी समानता। जिसमें हर मनुष्य का एक मूल्य हो और उस मूल्य को समझा जाए और किया जाए। तो वह नहीं हुआ और 1975 में जब इंदिरा गांधी के सामने सत्ता का संकट आया, उसके पीछे यह बड़ी पृष्ठभूमि थी।
आजकल जब बात होती है इमरजेंसी के बारे में, तो लोकतंत्र की इस चुनौती को नज़रअंदाज़ किया जाता है। यह एक मामला है देश में, जिसका अभी तक समाधान नहीं किया गया है।
ऐसे में सवाल तो यह भी उठता है कि आपकी किताब भी तो इसी समय आ रही है? इसका क्या महत्त्व है फिर?
चूँकि इमरजेंसी की बात आजकल उठाई जाती है, लेकिन जब उठाई जाती है तो सीमित रूप से केवल संविधान और लोकतंत्र की प्रक्रियाओं के बारे में उठाई जाती है। लेकिन लोकतंत्र की जो असली चुनौती है, उसके बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। वही मैंने किताब में लिखा है कि 1947 से जो चुनौती थी, उसका समाधान नहीं हुआ। इसीलिए 1975 में एक संकट आया।
इंदिरा गांधी के जो अपने कारण थे, वे तो उस समय का नज़दीकी मामला था। मेरे ख़याल से आज की चुनौती की जो गंभीरता है, लोग उसका कम मूल्यांकन करते हैं। इसके कारण ये हैं कि 1975 में जो इमरजेंसी हुई, वो तो केवल 21 महीने तक रही। आज हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया दस साल से एक तानाशाही की तरफ़ बढ़ती जा रही है।
आपातकाल समय पर कैसे-कैसे निशान छोड़ रहा है?
दोनों समय की तुलना करें—1975 के और आज के। एक तो यह है कि एक की अवधि हुई इक्कीस महीना और दूसरे की दस साल। दूसरी बात यह है कि ज़माना बदल गया है। मीडिया को देखिए कि उस समय इंदिरा गांधी को यह ज़रूरत पड़ी कि प्रेस पर सेंसरशिप करें। आज सत्ता को इसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि प्रेस उनके हाथ में है। केवल जम्मू-कश्मीर को छोड़कर बाक़ी किसी जगह उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरी बात यह कि इंदिरा गांधी के पास कोई ज़मीनी ताक़त नहीं थी। यूथ कांग्रेस का कोई ऐसा असर नहीं था।
यही अगला सवाल था इंदिरा की इमरजेंसी का। वो पूरी तरह से सरकारी मशीनरी पर निर्भर थी या उसमें प्राइवेट सहयोग था?
इंदिरा गांधी की इमरजेंसी पूरी तरह से सरकारी मशीनरी पर निर्भर थी। उनके पास कोई ज़मीनी ताक़त नहीं थी, जिस पर वह निर्भर कर सकें। उसके मुक़ाबले आज की सत्ता के पास आरएसएस है, बजरंग दल है, उनके पास विश्व हिंदू परिषद है। ऐसी बहुत-सी संस्थाएँ हैं, जिससे वह अपनी विचारधारा को लोगों पर थोप सकते हैं।
यह थोपने की ताक़त इंदिरा गांधी को नहीं थी और उनके पास ऐसी कोई संस्था नहीं थी, जिससे वह यह काम सफलतापूर्वक करा पाएँ। एक और फ़र्क़ है कि आज जो सत्ता और कॉर्पोरेट तालमेल है यह उस समय नहीं था। कॉरपोरेट पावर भी उतनी नहीं थी। कॉरपोरेट पावर का समर्थन आज के माहौल को भी बहुत अलग कर देता है। इन कारणों से मैं समझता हूँ कि आज की जो स्थिति है, उसमें लोकतंत्र की चुनौती और ज़्यादा गंभीर है।
इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लागू की तो यह उनकी एक कमज़ोरी की निशानी थी। उनको यह करना पड़ा क्योंकि उस समय जेपी आंदोलन हो रहा था। उसके पहले नक्सलवादी आंदोलन हुआ था। इन सबको कंट्रोल करने के लिए अपनी कमज़ोरी के कारण उन्होंने इमरजेंसी लागू की। आज सत्ता को उस तरह की कमज़ोरी महसूस नहीं होती क्योंकि उनके पास बहुत-सी शक्तियाँ हैं। मीडिया की, कॉरपोरेट पावर की, आरएसएस की। इसलिए वह एक तरह का अधिनायकवाद स्थापित कर सकते हैं, बिना उसको संवैधानिक तरह से लागू किए।
~~~
किताब यहाँ से ख़रीद सकते हैं : https://rajkamalprakashan.com/aapatkal-aakhyan-indira-gandhi-aur-loktantra-ki-agni-pariksha.html
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
