व्यक्ति से प्रकाश-स्तंभ बनने की यात्रा
 रोहिणी अग्रवाल
15 दिसम्बर 2024
रोहिणी अग्रवाल
15 दिसम्बर 2024
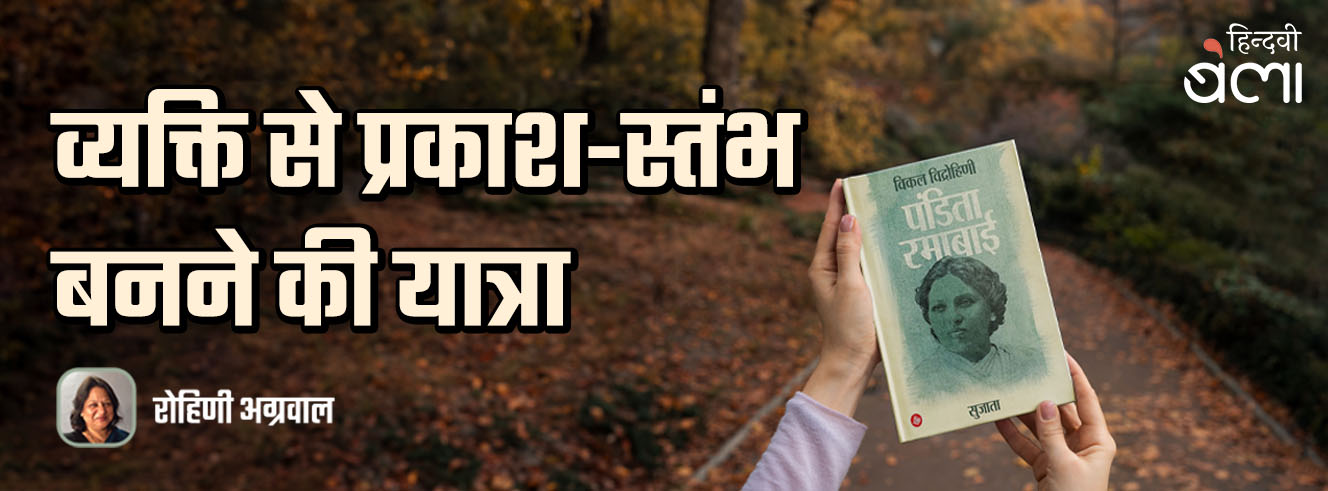
विचारहीनता ने आज जिस प्रकार तमाम राजनीतिक-सांस्कृतिक-साहित्यिक परिदृश्य को अपनी गिरफ़्त में ले लिया है, और भावनाओं के उकसावे को ही वैचारिक ताक़त का नाम दिया जाने लगा है, उससे यह बात और ज़्यादा पुष्ट होती है कि विवेकशील समाज की रचना के लिए ‘विचार’ को संप्रेषण और संवाद का ज़रूरी हिस्सा बनाया जाए। ऐसा विचार जो विश्लेषण और तर्क-बुद्धि से अनुस्यूत तो हो ही, संवेदना और एम्पैथी को भी सहज भाव से साथ लेकर चले। नफ़रत और उन्माद के जिस दोराहे पर आज हम ठिठके खड़े हैं, वहाँ इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत का पुनरावलोकन जितना जरूरी है; उतना ही मानीख़ेज़ है आत्मावलोकन कि सदियों की संघर्ष-यात्रा के बाद एक क़ौम के तौर पर आख़िर हम पहुँचे कहाँ है।
इस दृष्टि से सुजाता की पुस्तक ‘विकल विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई’ का प्रकाशित होना और इस पर सुधि साहित्य-समाज का ध्यानाकर्षित होना आश्वस्त करता है। यह पुस्तक एक कैंडिड प्रतिबद्धता के साथ पंडिता रमाबाई (1858-1922) के जीवन-संघर्ष के समानांतर भारतीय नवजागरण आंदोलन से गुजरते हुए तीन तथ्यों को सामने लाती है। एक, तमाम दुर्बलताओं, द्वंद्वों,अनिश्चयों और भावनात्मक झंझावातों में ऊभ-चूभ करता व्यक्ति—यदि चाहे तो अपनी अंतर्शक्तियों को थहाकर न केवल एक ठोस ‘व्यक्तित्व‘ बनता है, बल्कि सपनों को साकार करने की श्रमसाध्य साधना में ‘संस्था‘ भी बन सकता है।
दूसरे, व्यक्ति की जीवन-यात्रा उसके निजी जीवन का संकुचित आख्यान मात्र नहीं होती। वह अपने युग के प्रभावों-दबावों-संघातों से दिशा और गति पाते हुए पूरे युग के भीतर छिपी वैचारिक उथल-पुथल को भी साक्षात् करती है, और अपनी प्रखरता में उसे ‘रचती‘ भी है।
तीसरे, व्यक्ति का संघर्ष जब बृहत्तर सामाजिक सरोकारों से जुड़कर समय-समाज की जातीय चेतना का उत्कर्ष बन जाता है, तब वह वर्षों के फ़ासले पर खड़े पाठक को आत्म-साक्षात्कार का विश्लेषणात्मक विवेक भी देता है कि स्वयं उसके समय की विकास-यात्रा का चरित्र कितना उदार, प्रगतिशील एवं लोकतांत्रिक है।
‘विकल्प विद्रोहिणी पंडिता रमाबाई’ पुस्तक पढ़ते हुए निरंतर दो स्मृतियाँ ताज़ा होती रहीं—जीवनी विधा के रूप में ‘आवारा मसीहा’ का कला-वैभव, और मदर टेरेसा की लार्जर दैन लाइफ़ छवि। लेकिन आलोच्य पुस्तक का मूल्यांकन करने के क्रम में जिस घटक ने सर्वाधिक प्रभावित किया, वह है विषय-चयन के पीछे सक्रिय लेखकीय दृष्टि। बेशक पंडिता रमाबाई इस पुस्तक का केंद्रीय विषय/चरित्र/लक्ष्य हैं, लेकिन डेढ़ सौ बरस बाद अतीत के उस पन्ने को पलटते हुए लेखिका दरअस्ल वर्तमान की विभीषिकाओं पर भी उँगली रखती चलती हैं।
गहन शोध, साक्षात्कार और यात्राओं के बाद जुटाई गई सामग्री का उपयोग जीवनीकार की मेधा और रचनात्मकता को दर्शाता है। लेखिका विष्णु प्रभाकर की तरह उपलब्ध सामग्री में रचनात्मक सौंदर्य (जिसमें संवेदना और कल्पना का सहमेल साँस की तरह रहता है) का आलोड़न तो पैदा नहीं करतीं, लेकिन वैचारिकता के भीतर तर्क, संतुलन और प्रामाणिकता को पिरोकर इसे उन्नीसवीं सदी की एक महत्त्वपूर्ण विचार-यात्रा का दस्तावेज़ बना देती हैं।
उनकी नायिका अपने घुमंतू, स्वप्नदर्शी, विद्रोही पिता का ही अक्स है। साथ ही संस्कृत की प्रकांड पंडित, धर्मशास्त्री और निर्भीक। लेकिन यदि इतना भर उनका परिचय होता तो समय की शिला पर उत्कीर्ण दिशा-निर्देशक ताक़त के रूप में उनका स्मरण न किया जाता। दुखों के बीच वह निरंतर अपने को माँजती रहीं, असफलताओं के बीच संघर्ष और स्वाध्याय कर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती रहीं; माता-पिता के बाद महज़ 24 वर्ष की अवस्था में इकलौते भाई और पति को खोकर भी स्थितप्रज्ञ बनी रहीं।
अनाथ पुत्रहीन (पुत्रीवती) विधवा के रूप में तत्कालीन भारत में जाने कितनी-कितनी स्त्रियाँ वैधव्य और यौन-शोषण के दोहरे अभिशाप तले ज़िंदा लाश बनी रहती थीं। रमाबाई यदि ‘व्यक्ति‘ से ‘व्यक्तित्व‘ की यात्रा तय कर पाईं तो महज़ अपनी उस ज़िद की वजह से कि लाचारगी उनके ललाट की लिपि कदापि नहीं बनेगी। वह स्वयं अपना रास्ते खोजेंगी। आत्मान्वेषण और आत्म-परिष्कार की यह संकल्प-दृढ़ता ही दरअस्ल रमाबाई को रचती है जो पुणे के रूप में उनकी कर्मस्थली का निर्धारण करती है; स्त्री-नियति को स्त्री-अस्मिता की भास्वरता देने के लिए हिंदू धर्म-ग्रंथों की नि:संग तार्किक पुनर्पड़ताल का साहस देती है; और स्त्री-गतिशीलता को एक नए स्त्री-समय का उदय मान इंग्लैंड-अमेरिका प्रवास के लिए प्रेरित करती है।
दोनों बाँहों में आसमान भरने के लिए ज़रूरी होता है ‘कुएँ का मेंढक‘ प्रवृत्ति को तिलांजलि देना। रमाबाई का दौर हिंदू धर्म को जड़ीभूत कर देने वाली धर्म की अंदरूनी विकृतियों से दो-दो हाथ करने का था। लेकिन दुर्भाग्यवश राजा राममोहनराय की मृत्यु और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अकेले पड़ जाने के कारण समाज सुधार का बौद्धिक संवेदनात्मक आवेग धीरे-धीरे भाववाद के रोमानी राष्ट्रवाद में रिड्यूस होने लगा था।
राष्ट्र-प्रेम की मोटी पहचान थी अपने धर्म और संस्कृति पर गर्व। इसलिए श्रेष्ठता-ग्रंथि (कि हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति ही विश्व में सर्वश्रेष्ठ है) ने समाज सुधारकों और सांस्कृतिक एम्बेस्डरों को इस सूक्ष्म भाव से हिंदू धर्म-प्रचारकों के रूप में तब्दील किया कि वे पितृसत्ता और वर्ण व्यवस्था के विभाजनकारी अमानवीय प्रपंचों को देख-बूझ ही न सके। या चूँकि ‘मनुष्य‘ की अवधारणा में वे स्वयं थे—सवर्ण पुरुष समाज—इसलिए अपने पार शायद उन्हें ‘अन्य‘ कुछ दिखता भी न हो। रमाबाई यहीं इसी बिंदु पर एक आप्लावनकारी चेतना-लहर के रूप में अपने समय के मिसोजिनिस्ट समाज से टकराती दीखती हैं।
पहले अपनी पुस्तकों/व्याख्यानों के जरिए मनुस्मृति एवं हिंदू धर्मशास्त्रों के स्त्री-द्वेषी चरित्र को उजागर करते हुए, फिर स्त्री के लिए समान शिक्षा, स्वतंत्रता, अधिकारों, और अर्थोपार्जन की बात करते हुए। इस समूची प्रक्रिया में पुस्तक जिस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, विवेकानंद, एनी बेसेंट, रवींद्रनाथ टैगोर आदि ‘महान विभूतियों‘ को पुरुष के कट्टरपंथी स्त्रीद्वेषी वर्ग-चरित्र रूप में उकेरती है, वह न केवल भारतीय नवजागरण आंदोलन के अंतर्विरोधों को प्रामाणिकता के साथ उभारता है, बल्कि उस सेंटीमेंट के हमारे 21वीं सदी के समय में भी घुलमिल जाने की विडंबना को प्रकट करता है।
यही इस पुस्तक की ताक़त भी है कि हिंदुत्ववादियों के दुराग्रहों से टकराने के लिए वह जिस शख़्सियत को चुनती है, वह कन्वर्टेड ईसाई और स्त्री होने के कारण दोनों मोर्चों पर ‘अकेली’ और ‘निहत्थी’ स्त्री है। शायद यही वह बिंदु है जो रमाबाई की वैचारिक संघर्ष-यात्रा को तमाम अकेली औरतों के सहमेल की सघन संयुक्त सांस्कृतिक यात्रा बना देता है।
अनाथ परित्यक्ता हिंदू विधवा स्त्रियों के अलावा तमाम अज्ञात कुलशील ‘पतित’ स्त्रियों के उद्धार के लिए ‘शारदा सदन‘, ‘कृपा सदन‘, ‘मुक्ति मिशन‘ जैसी संस्थाओं को शुरू करना; हंटर कमीशन के समक्ष उपस्थित होकर स्त्रियों के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई की वकालत करना; लड़कियों के लिए स्कूल खोलना और फिर शिक्षित स्त्रियों को आर्थिक स्वावलंबन सुलभ कराना; किंडरगार्टन स्कूलों की स्थापना; प्रिंटिंग प्रेस लगाना—उनके समाज-सुधारक रूप की कुछ बानगियाँ हैं।
साथ ही प्रत्यक्ष होता है उनका परोपकारी वत्सल रूप जो अकाल और प्लेगपीड़ित समय में सामर्थ्य से अधिक संख्या में दुरदुराई लड़कियों को शरण-स्वाभिमान-भविष्य देता है। सुजाता की विशेषता है कि पुस्तक में वह रमाबाई को अलौकिक शक्ति की तरह चित्रित नहीं करतीं, वरन् अपने द्वंद्वों से निरंतर दो-दो हाथ करती सामान्य स्त्री की तरह उकेरती हैं जो प्रतिकूलताओं से यथाशक्ति जूझ रही है। वह अनपेक्षित परिस्थितियों में अपनी ही बुद्धि से निर्णय लेती है; मनोबल तोड़ने के लिए फैलाए गए भ्रांत लोकापवाद का मज़बूती से मुकाबला करती है; संस्था के आर्थिक संसाधनों पर पकड़ बनाए रखती है; और इस प्रक्रिया में एक आधुनिक चेतना से संपन्न प्रगतिशील स्त्री का मानक रचती है।
रमाबाई के समानांतर पुस्तक में ताराबाई शिंदे, रख्माबाई, आनंदीबाई गोपाल, रमाबाई रानाडे, एनी बेसेंट, स्वर्णकुमारी देवी आदि अनेक स्त्रियाँ आई हैं; लेकिन वैचारिक एवं सामाजिक मोर्चे पर जिस मिशनबद्ध भाव से रमाबाई सन्नद्ध योद्धा की भांति निरंतर संघर्षशील रही हैं, वह अन्य की तुलना में उन्हें अविस्मरणीय बनाता है। लेकिन विचलित करने वाला सवाल तो यह है कि रमाबाई के दैहिक अवसान के बाद उनकी विचार-यात्रा का अंत क्यों हुआ?
विचार-यात्रा ज्योति-स्फुलिंग की तरह होती है और विचारक /समाजसुधारक एक ‘विशिष्ट‘ व्यक्ति। जिस भारतीय समाज में तेंतीस करोड़ देवी-देवताओं और बारह ज्योतिर्लिंगों के अलावा कितने ही मंदिरों-पीपलों को बनवाने/पूजने की परंपरा आज भी जीवित हो, वहाँ समाज की पुनर्रचना करने वाली लार्जर दैन लाइफ़ उदात्त विभूतियों की प्रतिष्ठा का भाव क्यों नहीं उमड़ता? धर्म न कटु तिक्त सामाजिक यथार्थ से बड़ा है, न व्यक्ति की निजता, स्वायत्तता और मानवीय गरिमा से। ‘मनुष्य‘ हुए बिना वह मनुष्य-समाज की विविध संस्थाओं का नियमन नहीं कर सकता। फिर क्यों वह बाध्यकारी घेरेबंदी का रूप लेकर व्यक्ति की चेतना को जकड़े रहता है? क्यों बुद्ध से लेकर गांधी-अंबेडकर तक प्रत्येक समाज-सुधारक को ‘मूर्ति’ में ढाल कर विचारधारा को तहख़ाने में फेंक दिया जाता है?
यह पुस्तक प्रत्यक्षत: इन सवालों पर विचार नहीं करती, लेकिन उपभोग और आस्वाद के घुप्प अँधेरे में डूबे समकालीन समाज के बीचोबीच रमाबाई को चेतना की मशाल के रूप में प्रतिष्ठित कर जाती है, ताकि अपनी-अपनी मनुष्यता को चीन्ह कर हर हाथ स्वयमेव मशाल बन जाए।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
