रविवासरीय : 3.0 : ‘बुद्धि की आँखों में स्वार्थों के शीशे-सा!’
 अविनाश मिश्र
13 अप्रैल 2025
अविनाश मिश्र
13 अप्रैल 2025
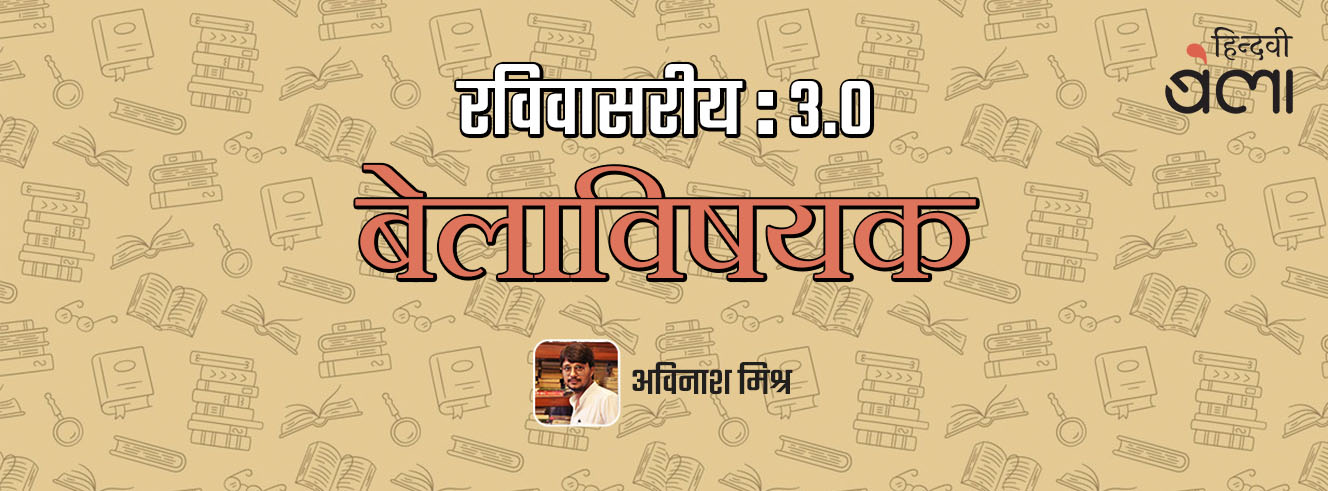
• गत बुधवार ‘बेला’ के एक वर्ष पूर्ण होने पर हमने अपने उद्देश्यों, सफलताओं और योजनाओं का एक शब्दचित्र प्रस्तुत किया। इस शब्दचित्र में आत्मप्रचार और आभार की सम्मिलित शैली में हमने लगभग अपना ही प्रशस्तिगान किया। वह अवसर ही ऐसा था। लेकिन अब वक़्त पुन: आत्मान्वेषण पर लौट आने का है।
• गत वर्ष की शुरुआत में हमने ‘बेला’ के शुभारंभ के लिए 9 अप्रैल की तिथि चुनी थी। यह तिथि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और राहुल सांकृत्यायन की जन्मतिथि के रूप में समादृत है। इससे पूर्व वर्ष 2020 में हमने ‘हिन्दवी’ के शुभारंभ के लिए 31 जुलाई यानी प्रेमचंद-जयंती की तारीख़ चुनी थी। इससे हमारे वैचारिक रुझान की एक तस्दीक़ हो सकती है, हालाँकि हम यह भी मानते हैं कि प्रतिकार और कदाचार दोनों पर ही किसी विशेष रंग और विचार का एकाधिकार नहीं है।
• ‘बेला’ पर फ़रमाइशी लेखन प्रकाशित नहीं होता है। इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है; क्योंकि ‘बेला’ पर प्रकाशन के लिए आई रचनाएँ, समीक्षाएँ और सूचनाएँ इतनी ज़्यादा हैं कि हम अपनी सारी नियमितता के बावजूद उन्हें ही समय पर प्रकाशित नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम फ़िलहाल रचनाएँ नहीं, क्षमा माँगने की स्थिति में हैं।
दरअस्ल, तात्कालिक महत्त्व की चीज़ों को हमें जल्द प्रकाशित करना पड़ता है; क्योंकि एक वक़्त के बाद, वे उतनी प्रासंगिक नहीं रह जाती हैं। हम यह मानते हैं कि स्थायी महत्त्व की रचनाएँ धैर्य से सबल होती हैं।
• रचनाओं का आकांक्षित मंगल उनके अभ्यस्त संस्कार के अंतराल में रहता है। ये संस्कार विकसित करने में प्रकाशन-स्थलों का महत्त्वपूर्ण योगदान है, जहाँ से एक रचनाकार की कमज़ोर रचनाएँ बार-बार वापस आती हैं। उन्हें अस्वीकृत किया जाता है या थोड़ी गुंजाइश होने पर पुन: उन पर काम करने, फिर भी बात न बनने पर एक बार और काम करने के लिए कहा जाता है... अंततः प्रकाशन बहुत प्रतीक्षा, परिश्रम और अध्यवसाय का परिणाम है। ऐसी प्रक्रियाओं से गुज़रकर ही स्थायी महत्त्व की रचनाएँ आकार लेती हैं; फिर कहीं जाकर इनका एक संग्रह बनता है और उसके लिए भी वैसी ही प्रतीक्षा, मेहनत और अध्ययनशीलता की दरकार होती है—जैसी रचना-प्रकाशन के लिए। रचे जाने का जो आंतरिक अचीवमेंट होता है—वह महफ़िलों, जनसंपर्कों और जल्दबाज़ियों से हासिल नहीं हो सकता। महफ़िलों, जनसंपर्कों और जल्दबाज़ियों से जो हासिल होता है; वह हम अपने आस-पास रोज़-ब-रोज़ देख ही रहे हैं।
• इस समय जब लेखक प्रसिद्धि, स्वीकृति और वैधता पाने के लिए लिटरेरी एजेंटों, प्रकाशकों और सोशल मीडिया के प्लान ख़रीद रहे हैं; सब तरफ़ प्रबुद्धता और संदिग्धता का अजब संगम है, कवियों-लेखकों की भाषा—कवियों-लेखकों की भाषा-सी नहीं लग रही है; ऐसे में हम यह बताना ज़रूरी समझते हैं कि हम गढ़ी गई छवियों, छद्म आभामंडलों और क़िस्तों पर ख़रीदे गए ब्लू टिकों से आक्रांत, भयभीत और प्रभावित नहीं होते हैं।
• जैसे संसार की सारी प्रकाशन-संस्थाएँ मानती हैं; हम भी यह मानते हैं कि लेखक के विचार लेखक के ही होते हैं और संपादक, प्रकाशक, प्रकाशन-स्थल उन्हें सामने भर लाते हैं... ताकि अभिव्यक्ति, हस्तक्षेप और संवाद की संस्कृति सुरक्षित रहे। लेकिन हिंदी में गठजोड़ और स्वार्थ इस क़दर प्रबल हैं कि लोग दिमाग़ और आँख मूँदकर संदेह करते हैं, और इस तरह ही विश्वास।
• इस दृश्य में ‘बेला’ की भूमिका-मंशा बीच बहस में कूदने की नहीं है। हम या तो बहस शुरू करते हैं या उसका पटाक्षेप करते हैं, हालाँकि कवि कह चुका है :
बहस नहीं चल पाती
हत्याएँ होती हैं
फिर जो बहस चलती है
उसका भी अंत हत्याओं में होता है
• ‘बेला’ पर हम न Provoke करते हैं, न Provoke होते हैं।
• हिंदी में इधर सादा चीज़ों का प्रचार-प्रसार करने की कोशिशें कुछ ज़्यादा ही की जाने लगी हैं; इससे प्रतीत होता है कि मानो हिंदी एक बीमार भाषा है और इसे अपनी स्वस्थ, चटक और उल्लसित परंपरा याद नहीं है। यों भी नहीं है कि यह सादगी उच्च विचारों से संचालित हो या उस ओर अग्रसर हो। यह सादापन प्राय: अपनी कायरताओं, धूर्तताओं और धाँधलियों को छुपाने के लिए गंभीरता का आवरण धारण करता है।
• कुणाल कामरा के हास्यबोध, व्यंग्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक स्वयं के प्रसंग में हुए व्यंग्य से अत्यंत आहत हो उठते हैं, मंडलियाँ बनाकर अनैतिकतापूर्ण ढंग से हमलावर होते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, संपादकीय विवेक और स्वतंत्रता की हत्या करते या चाहते हैं... यह एक चुनी हुई दृष्टिहीनता है, जो आपको और चाहे जो बना दे—ईमानदार, नैतिक और लोकतांत्रिक नहीं बना सकती।
• इस बार ग्यारहवाँ बिंदु यही है कि ग्यारहवाँ बिंदु नहीं है।
•••
इस स्तंभ में प्रस्तुत कविता-पंक्तियाँ आलोकधन्वा की एक कविता ‘सफ़ेद रात’ से हैं। ‘बेलाविषयक’ के शीर्षक के रूप में प्रस्तुत कविता-पंक्ति गजानन माधव मुक्तिबोध की एक कविता ‘चाँद का मुँह टेढ़ा है’ से है। अन्य रविवासरीय : 3.0 यहाँ पढ़िए — गद्यरक्षाविषयक | पुष्पाविषयक | वसंतविषयक | पुस्तकविषयक | प्रकाशकविषयक | प्रशंसकविषयक | भगदड़विषयक | रविवासरीयविषयक | विकुशुविषयक | गोविंदाविषयक | मद्यविषयक | नयानगरविषयक | समीक्षाविषयक
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
14 अप्रैल 2025
इलाहाबाद तुम बहुत याद आते हो!
“आप प्रयागराज में रहते हैं?” “नहीं, इलाहाबाद में।” प्रयागराज कहते ही मेरी ज़बान लड़खड़ा जाती है, अगर मैं बोलने की कोशिश भी करता हूँ तो दिल रोकने लगता है कि ऐसा क्यों कर रहा है तू भाई! ऐसा नहीं
08 अप्रैल 2025
कथ्य-शिल्प : दो बिछड़े भाइयों की दास्तान
शिल्प और कथ्य जुड़वाँ भाई थे! शिल्प और कथ्य के माता-पिता कोरोना के क्रूर काल के ग्रास बन चुके थे। दोनों भाई बहुत प्रेम से रहते थे। एक झाड़ू लगाता था एक पोंछा। एक दाल बनाता था तो दूसरा रोटी। इसी तर
16 अप्रैल 2025
कहानी : चोट
बुधवार की बात है, अनिरुद्ध जाँच समिति के समक्ष उपस्थित होने का इंतज़ार कर रहा था। चौथी मंजिल पर जहाँ वह बैठा था, उसके ठीक सामने पारदर्शी शीशे की दीवार थी। दफ़्तर की यह दीवार इतनी साफ़-शफ़्फ़ाक थी कि
27 अप्रैल 2025
रविवासरीय : 3.0 : इन पंक्तियों के लेखक का ‘मैं’
• विषयक—‘‘इसमें बहुत कुछ समा सकता है।’’ इस सिलसिले की शुरुआत इस पतित-विपथित वाक्य से हुई। इसके बाद सब कुछ वाहवाही और तबाही की तरफ़ ले जाने वाला था। • एक बिंदु भर समझे गए विवेक को और बिंदु दिए गए
12 अप्रैल 2025
भारतीय विज्ञान संस्थान : एक यात्रा, एक दृष्टि
दिल्ली की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी के बीच देश-काल परिवर्तन की तीव्र इच्छा मुझे बेंगलुरु की ओर खींच लाई। राजधानी की ठंडी सुबह में, जब मैंने इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा शुरू की, तब मन क





