ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उपजी भाषा और कथा
 रमाशंकर सिंह
30 दिसम्बर 2024
रमाशंकर सिंह
30 दिसम्बर 2024
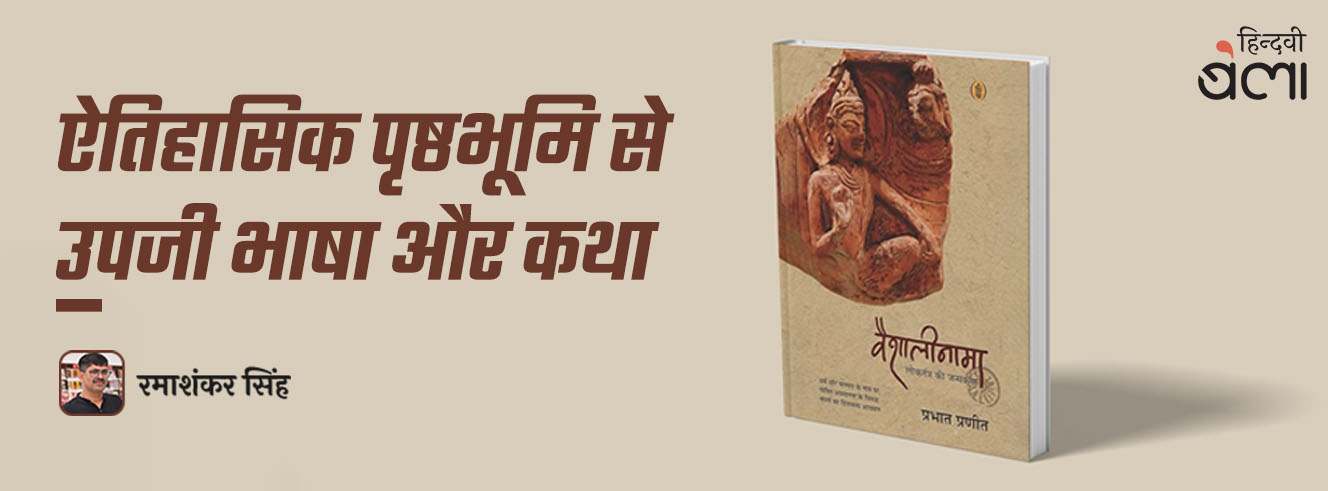
भारत में लोकतंत्र एक परंपरा के रूप में मौजूद रहा है—इस तथ्य पर काशीप्रसाद जायसवाल से लेकर अमर्त्य सेन ने अपने-अपने तरीक़े से लिखा है। प्राचीन भारत में गणराज्य, शासन-पद्धति और प्रतिदिन के राजनय पर काशीप्रसाद जायसवाल ने मॉडर्न इंडिया में जो लेख लिखे, वे आज़ादी के आंदोलन के दौरान सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले लेख हुआ करते थे। उससे आज़ादी की लड़ाई में लगे राष्ट्रवादी नेताओं को बड़ी सहायता मिली थी।
अमर्त्य सेन ने लोकतंत्र के विचार को पूरी तरह से पश्चिमी मानने के बजाय उसे भारतीय संदर्भों में देखने की सलाह दी है, हाँ उन्होंने उसके सीमित सामाजिक आधार की तरफ़ इशारा भी किया है। इसी तरह डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने संविधान सभा में बौद्ध धर्म और उसकी लोकतांत्रिक परिपाटियों की प्रशंसा की थी।
अभी कुछ वर्षों से भारत को ‘मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी’ कहने का चलन बढ़ा है। इस विचार पर विद्वानों ने मतभेद जताया है कि यदि भारत में बहुत पहले लोकतंत्र था, तो वह कैसा था? वह किसके हितों की बात करता था? उसका सामाजिक आधार क्या था? यह सवाल प्रभात प्रणीत के सामने भी रहा होगा। उन्होंने इसका जवाब अपनी औपन्यासिक कल्पनाशीलता, ऐतिहासिक समझ और सामाजिक संवेदनशीलता के साथ दिया दिया है।
‘वैशालीनामा : लोकतंत्र की जन्मकथा’ 216 पृष्ठों का एक सामान्य उपन्यास प्रतीत होता है जो शुरू में महत्त्वाकांक्षी तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन धीरे-धीरे गति पकड़ लेता है और उस पूरे वातावरण को पेश करता है जिसमें अतीत की याद है, विभिन्न जातियों में बँट चुके समाज की अपनी सामूहिक दिक़्क़तें हैं और उससे निकल जाने की एक छटपटाहट है।
यदि प्रभात प्रणीत फ़्रांस में ‘लोकतंत्र की जन्मकथा’ लिख रहे होते तो संभवतः वहाँ के राजन्य वर्ग और उसकी फ़्रांसीसी क्रांति से उसकी मुलाक़ात का ज़िक्र करते। भारत में लोकतंत्र किसी क्रांति से नहीं बल्कि धीमे-धीमे समाज के भीतर से ही विकसित होने का प्रयास कर रहा था।
यह उपन्यास अपने पात्रों की अंतर्दशाओं के चित्रण से यह दिखाता है कि उनके अंदर क्या चल रहा है और वे उसे किस तरह प्रकट कर रहे हैं। जब वे अपनी बात कहना चाह रहे हैं तो उनकी सामाजिक पहचान आड़े आ जाती है। यह उपन्यास तीन चीज़ों को एक साथ पेश करता है : युवराज नाभाग और सुप्रभा की प्रेमकथा, बौद्धकालीन भारत का सामाजिक परिदृश्य और लोकतंत्र के उदय की कश्मकश।
वास्तव में, ‘वैशालीनामा’ के केंद्र में प्रेम का निर्मल और उदात्त चित्रण इसे पठनीय और स्थाई महत्त्व की कृति बनाता है। प्रभात प्रणीत का प्रेम का चित्रण सूक्ष्म और स्वाभाविक है, जो उस समय की राजनीतिक और सामाजिक जटिलताओं के लिए एक प्रतिपक्ष के रूप में भी कार्य करता है। यह चित्रण मानवीय भावनाओं की सार्वभौमिक और शाश्वत प्रकृति को उजागर करता है, जिससे उपन्यास केवल एक ऐतिहासिक विवरण नहीं बल्कि एक गहरी व्यक्तिगत कहानी भी बन जाता है और इसके कारण पाठक, ख़ासकर युवा पाठक इससे तेज़ी से जुड़ते हैं।
इस उपन्यास को पढ़ते हुए जो चीज़ सबसे बेहतर लगती है, वह है इतिहास के प्रति उपन्यासकार का बर्ताव। आमतौर ऐसे उपन्यासों में वर्तमान के दबाव में बहुत सारी ‘आधुनिक और प्रगतिशील बातें’ अतीत की कल्पनाशीलता में शामिल कर दी जाती हैं। इससे कोई कविता या उपन्यास हमारे आधुनिक चित्त को बहुत भा जाता है, लेकिन इतिहास वर्तमान की सुविधा के हिसाब से तो नहीं चलता है। उसकी अपनी गति और दिक़्क़त है। इसके कारण ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाले लेखकों में यह अंतर्द्वंद्व भी पनपता है कि अतीत को किस तरह से अपने पाठकों के सामने पेश करे कि कहानी इतिहास के ख़िलाफ़ न चली जाए और इतिहास की रक्षा भी हो। यह द्वंद्व आचार्य चतुरसेन, वृंदावनलाल वर्मा, महाश्वेता देवी और यशपाल सहित उन सभी कथाकारों के समक्ष था जिन्होंने ऐतिहासिक कथानकों के आधार पर कुछ लिखा है।
इस उपन्यास में उपन्यासकार ने इसे नाभाग के द्वारा इसे द्वंद्व को दिखाया है। नाभाग वज्जि का भावी सम्राट है और उसे एक साधारण लेकिन अपूर्व सुंदरी सुप्रभा से प्रेम हो जाता है। इसके बाद उस समय के सामाजिक मूल्यों, नाभाग की अपनी प्रगामी चेतना और जीवन मूल्य तथा वृद्धों की पुरानी मान्यताओं में संघर्ष उपजता है। इसे एक लंबे कालखंड में अवस्थित करते हुए उपन्यासकार वहाँ तक ले जाता है जहाँ उसका बेटा जवान हो जाता है और वह कहानी को पूरा करने की ताक़त हासिल कर लेता है।
उपन्यास के मध्य तक आते-आते लगता है कि इतिहासचक्र नाभाग और उसकी प्रेयसी जो अब उसकी पत्नी है, को पीस देगा लेकिन उसका बेटा भालांदन उसे दूसरी दिशा में मोड देता है। वह अपनी माँ वैश्य वंशानुक्रम का ताना सुनता है, लेकिन वस्तुस्थितियों को बदलकर ‘लोकतंत्र के जन्म’ का वातावरण सृजित करता है।
यहाँ पर एक उपन्यास से एक प्रसंग उद्धृत करना उचित होगा : “नाभाग ने वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहा, ‘‘यह केवल मेरे या देवी सुप्रभा के जयकार का समय नहीं है, यह वज्जि राज्य, इसे स्थापित करनेवाले महाराज नाभानेदिष्ट और यहाँ के समस्त नागरिकों के जयकार का समय है। यह आप सभी की जय है, जीत है। आज से अभी से यह वज्जि राज्य विगत दो दशक की पीड़ा से मुक्त होकर एक नये समाज और राज्य के निर्माण हेतु अग्रसर हो चुका है। बाक़ी बातें और चीज़ें तो शनैः-शनैः होंगी, किंतु एक बात की घोषणा मैं आप लोगों के समक्ष अभी ही कर देना चाहता हूँ। आज से, अभी से इस राज्य का हर नागरिक यही सोचे, समझे और अपने अंत:करण में बैठा ले कि ‘मैं अब अपनी मिट्टी का स्वयं स्वामी हूँ, अपनी धरती का राजा स्वयं हूँ।’ कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी का स्वामी नहीं, इस राज्य में हर कोई राजा है, हर कोई प्रजा है। राजसिंहासन पर बैठने वाला जिसे राजा के नाम से पुकारा जाएगा वह प्रजा का प्रतिनिधि भर है, वह राजा प्रजा की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए प्रजा द्वारा ही नियुक्त प्रतिनिधि है, प्रजा राजा से ऊपर है। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि राजकाज और प्रशासन में नागरिकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो ताकि नागरिकों की प्राथमिकताएँ ही राजा व राज्य की प्राथमिकता बनी रहे एवं शासन में नागरिकों की सीधी भागीदारी हो।’’
इस उपन्यास का सबसे सराहनीय पहलू इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से उपजी भाषा है। प्रणीत ने जिस सृजनात्मक भाषा और परिवेश को उस कालखंड के लिए गढ़ा है, वह अत्यंत प्रभावशाली है। यह युग के प्रति उनकी गहरी समझ और समर्पण को दर्शाता है, जो कई अनुभवी लेखकों के लिए भी चुनौतीपूर्ण होता है।
इस उपन्यास को पढ़ते हुए, ख़ासकर आरम्भिक हिस्सों को पढ़ते हुए पाठकों को यशपाल के उपन्यास ‘दिव्या’ की भाषा की याद आ सकती है, लेकिन यशपाल की भाषा काफ़ी चुस्त थी। वह शब्दों का कम इस्तेमाल करते थे। प्रभात प्रणीत इस मामले में थोड़ा उदार हैं और वह शब्दों को थोड़ा और विस्तार देते हैं, लेकिन बाद में भाषा सरल होती गई है। सबसे ख़ास बात यह है कि उपन्यास अपने पाठक को इससे जोड़े रहता है, कुछ जगहों पर उसकी धुकधुकी भी चलने लगती है जो एक अच्छे साहित्य की निशानी भी है कि वह पाठक की मनोदशा में बेचैनी पैदा करे। यह उपन्यास यह सब करता है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
