एकतरफ़ा प्यार को लेकर क्या कह गए हैं ग़ालिब
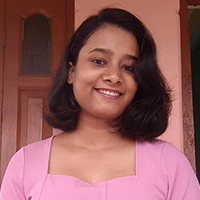 अनामिका झा
26 सितम्बर 2024
अनामिका झा
26 सितम्बर 2024
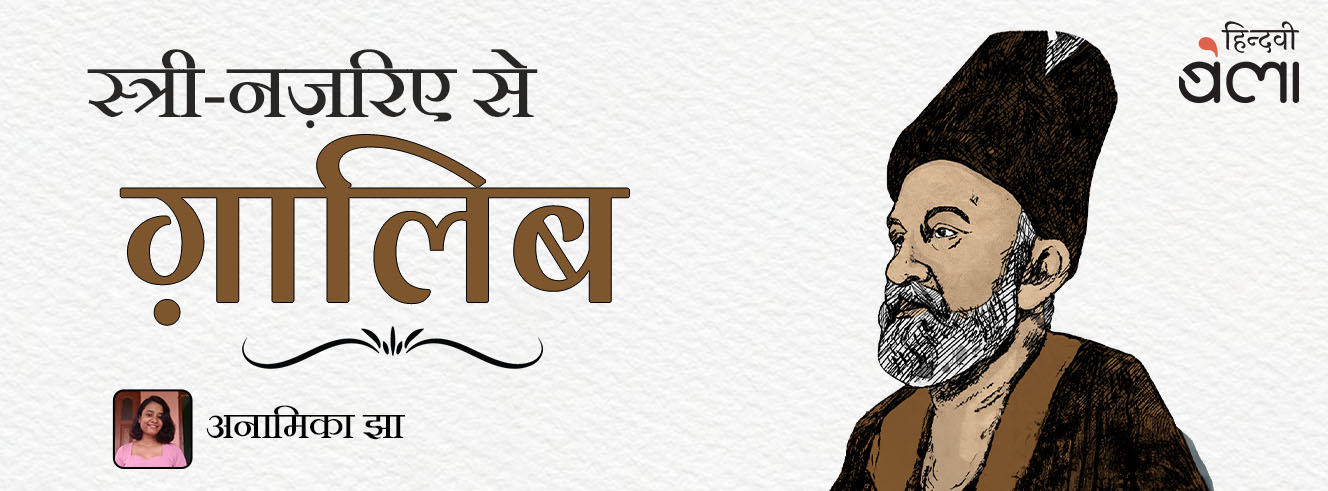
हैं और भी दुनिया में सुख़न-वर बहुत अच्छे
कहते हैं कि ‘ग़ालिब’ का है अंदाज़-ए-बयाँ और
दुनिया में कई ‘सुख़न-वर’ हुए हैं। अच्छे-से-अच्छे हुए हैं और आगे भी होंगे, पर ग़ालिब की इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि उनका ‘अंदाज़-ए-बयाँ’ सबसे जुदा है—जैसे उपरोक्त शे’र में ही हमें उनकी शब्दों से खेलने की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें ग़ालिब ने ‘और’ शब्द का प्रयोग दो बार किया है और दोनों ही ‘और’ का अर्थ एक-दूसरे से अलग है।
ग़ालिब के साहित्य में एक ओर जहाँ प्रेम का अनन्य रूप देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर उनके समय-समाज-परिवेश की परिस्थितियों, परेशानियों और ना-उम्मीदी के दौर का भी चित्र प्रस्तुत होता है। उनकी सोच अपने समय-समाज से आगे होते हुए भी, उनकी चिंता में उनका समाज और उसकी तकलीफ़ें मौजूद हैं। तत्कालीन समाज की समस्याओं से ग़ालिब ख़ुद को अलग नहीं करते। उन्होंने अपनी कविता में तत्कालीन समय-समाज के संघर्ष को भी जगह दी है, जैसे—
ग़म अगरचे जाँ-गुसिल है प कहाँ बचें कि दिल है
ग़म-ए-इश्क़ गर न होता ग़म-ए-रोज़गार होता
इस शे’र में ग़ालिब ने तत्कालीन समय के रोज़गार की समस्या को रेखांकित किया है। संघर्ष के उस दौर में ग़ालिब ने अपनी शाइरी के माध्यम से ना-उम्मीदी से निकलने के लिए जिजीविषा और आशा जगाने का प्रयास किया है।
ग़ालिब के शे’र परत-दर-परत खुलते हैं। जैसे यह शे’र—
ग़म-ए-हस्ती का ‘असद’ किस से हो जुज़ मर्ग इलाज
शम्अ हर रंग में जलती है सहर होते तक
पढ़ने वाले को शे’र की पहली पंक्ति से किसी को भी ग़ालिब के घोर निराशावादी होने का भ्रम हो सकता है, यह सोचकर कि उन्होंने जीवन के संघर्ष, जीवन के दुख का इलाज मौत बताया है। लेकिन दूसरी पंक्ति में हमें जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण मिलता है। कि जैसे एक शमा की नियति है कि वह सहर यानी सुबह (प्रकाश) होने तक जलती जाए वैसे ही हमारा भी कर्त्तव्य है जीए जाना।
जीवन का रास्ता चाहे जितना संघर्षमय हो, लेकिन इसका विकल्प कभी अपने जीवन को ख़त्म करना नहीं हो सकता। इस शे’र में हमें तमाम निराशाओं के बीच ज़िंदगी के प्रति चाहत का स्वर मिलता है।
ग़ालिब के अशआर के अनेकों अर्थ निकाले जा सकते हैं—जितनी निगाहें उतने अर्थ। जैसे यह शे’र—
दाम-ए-हर-मौज में है हल्क़ा-ए-सद-काम-ए-नहंग
देखें क्या गुज़रे है क़तरे पे गुहर होते तक
इसका शाब्दिक अर्थ यह है कि बारिश की बूँद जब सीप में जा गिरती है, तो वह मोती बन जाती है। यही है क़तरे का गुहर होना। पर वह बारिश की बूँद जो आसमान से गिरती है, उसके लिए सैकड़ों मगरमच्छ मुँह खोले, जाल बिछाए रहते हैं, जिनसे बच कर ही बूँद सीप में जा सकती है।
इस शे’र को स्त्री दृष्टि से भी व्याख्यायित किया जा सकता है। यहाँ बारिश की बूँद की तुलना हम स्त्री से कर सकते हैं। एक स्त्री को अपने जीवन में सैकड़ों ऐसे मगरमच्छ मिलते हैं, जो मुँह बाये उसे दबोचने की फ़िराक़ में रहते हैं और स्त्री को इन सभी जालसाज़ी से बचकर अपने जीवन के संघर्षपथ पर निरंतर बढ़ते रहना होता है, सीप में जाकर मोती बनकर निखरने के लिए।
ग़ालिब ने अपने अशआर में अक्सर मा’शूक़ा को ऐसा दिखाया है, जो उससे प्रेम करने वालों की उपेक्षा करे, जो बहुत निष्ठुर हो; यानी आज कल की चलताऊ भाषा में कहें तो वह जो ‘भाव’ नहीं देती।
उदाहरणार्थ अशआर—
दाग़-ए-दिल गर नज़र नहीं आता
बू भी ऐ चारा-गर नहीं आती
अर्थात् यदि तुम्हें मेरा जला हुआ दिल नज़र नहीं भी आता हो लेकिन क्या जले हुए दिल की गंध भी तुम तक नहीं पहुँच पा रही?
हम हैं मुश्ताक़ और वो बे-ज़ार
या इलाही ये माजरा क्या है
ग़ालिब इसमें सवाल करते हैं कि आख़िर क्या बात है कि यहाँ वह उससे बात करने के लिए उत्सुक बैठे हैं और वहाँ वह रूठी बैठी है? क्या बात है कि वह मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं?
मैं भी मुँह में ज़बान रखता हूँ
काश पूछो कि मुद्दआ क्या है
ग़ालिब यहाँ कह रहे हैं कि उनके मुँह में भी ज़बान है, लेकिन मा’शूक़ा उनसे पूछ ही नहीं रही कि आखिर बात क्या है? मा’शूक़ा उनके पक्ष को नज़रअंदाज़ किए जा रही है। उनकी स्थिति उसे विचारणीय ही नहीं लग रही।
इन अशआर में ग़ालिब की बेबसी, कसक और उनके अफ़सोस का स्वर मिलता है और मा’शूक़ा की जो छवि बनती दिखती है, वह बेशक एक निष्ठुर व्यक्ति की है।
अब आज कल लड़की अगर ‘भाव’ नहीं दे तो लड़की के बारे में कितनी बातें बनाई जाती हैं कि लड़की ऐसी है, वैसी है, ख़ुद को ज़्यादा समझती है। हिंदी सिनेमा में तो ऐसा एक गाना भी है—“ख़ुद को क्या समझती है, इतना अकड़ती है, कॉलेज में नई-नई आई एक लड़की है”। लेकिन ग़ालिब ने अपनी कविता में कभी यह शिकायत करने के लहज़े से नहीं कहा है। न ही ग़ुस्सा, उतारने या बदला लेने के लहज़े से कहा है। जैसा आज कल का चलन है कि “ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतक़ाम देखेगी”। हमें यह लहज़ा उनकी कविता में नहीं दिखता। उनकी कविता में जो लहज़ा मिलता है, उसके बारे में सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का यह कवितांश सटीक लगता है—
मैंने कब कहा
कोई मेरे साथ चले
चाहा ज़रूर!
यह चाह मिलती है ग़ालिब की कविता में। उदाहरणार्थ—
मैं बुलाता तो हूँ उस को मगर ऐ जज़्बा-ए-दिल
उस पे बन जाए कुछ ऐसी कि बिन आए न बने
यानी वह सीधे यह नहीं कह रहे कि मैं बुलाऊँ और वह आ जाए। बल्कि यह कह रहे हैं कि मैं उसको बुलाता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाए कि उसका ‘नहीं आना’ न हो। मिलने की जितनी तड़प इनके भीतर है, उतनी ही तड़प उसके भीतर भी हो जाए और वह उनसे मिलने आ जाए।
खेल समझा है कहीं छोड़ न दे भूल न जाए
काश यूँ भी हो कि बिन मेरे सताए न बने
मतलब यह कि उसके द्वारा जो मैं सताया जाता हूँ। यह उसके लिए भले खेल है, लेकिन ग़ालिब को यही भाता है। वह कहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि उसका काम मुझे बिना सताए बने ही नहीं क्योंकि अगर वह ग़ालिब को नहीं सताए तो उनका क्या होगा?
यह सब वह केवल चाह रहे हैं कि ऐसा हो और इसी चाह को, अपने-आप को अभिव्यक्त करने के लहज़े से ही लिख भी रहे हैं। कभी-कभी तो ग़ालिब मा’शूक़ा का ऐसा चित्र खींचते हैं कि मुँह से ‘आह!’ और ‘वाह!’ दोनों एक साथ ही निकलता है। उदाहरणार्थ उनका यह शे’र—
मरता हूँ इस आवाज़ पे हर चंद सर उड़ जाए
जल्लाद को लेकिन वो कहे जाएँ कि हाँ और
इस शे’र में जल्लाद के सिर काटने का जो दृश्य बनता है, वह सोचने में ही कितना भयावह है और ऐसे में ग़ालिब कहते हैं कि वह उस आवाज़ पे मरते हैं, जो जल्लाद को यह कह रही है कि ‘हाँ, और काटो, अच्छे से काटो!’ अपनी मरने की स्थिति में भी मा’शूक़ा की ऐसी निष्ठुरता पर ग़ालिब को प्रेम ही आ रहा है।
उपरोक्त उल्लिखित अशआर में किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं है। ग़ालिब किसी पर दोष डालते भी हैं तो मा’शूक़ा पर नहीं, बल्कि कभी क़िस्मत पर, जैसे—
ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता
यानी हमारी क़िस्मत में ही मा’शूक़ा से मिलना नहीं था, इसलिए नहीं मिल सके। तो कभी समय की कमी पर, जैसे–
हम ने माना कि तग़ाफ़ुल न करोगे लेकिन
ख़ाक हो जाएँगे हम तुम को ख़बर होते तक
अर्थात्, हम मानते हैं कि तुम मेरी उपेक्षा नहीं करोगे, लेकिन इससे पहले कि तुमको ख़बर हो हम मर चुके होंगे। पहले का ज़माना मोबाइल-इंटरनेट का नहीं था, जिससे मिनटों में ही ख़बर दूसरे तक पहुँचाई जा सकती हो। उस समय ख़बर पहुँचाने के लिए चिट्ठी भेजी जाती थी, जिससे ख़बर पहुँचने में कई-कई दिन समय लगता था, चूँकि यातायात के भी उतने साधन नहीं थे।
ग़ालिब की शाइरी में हमें जो प्रेम-संबंधी विचार मिलते हैं, प्रेम के विषय में ऐसे आधुनिक विचार आज भी विरले ही मिलते हैं। ग़ालिब के लिए प्रेम कभी ज़बरदस्ती की बात नहीं थी। प्रेम को उन्होंने एक नैसर्गिक प्रक्रिया के रूप में ही दर्शाया है जिसमें ज़बरदस्ती का कोई स्थान नहीं था। उदाहरणार्थ ग़ालिब का बहुप्रचलित शे’र—
इश्क़ पर ज़ोर नहीं है ये वो आतिश ‘ग़ालिब’
कि लगाए न लगे और बुझाए न बने
इश्क़ पर किसी प्रकार के ज़ोर का कुछ प्रभाव नहीं होता। इश्क़ वह आग है जो न ज़बरदस्ती लगाई जा सकती है और एक बार इश्क़ हो जाने पर न बुझाई जा सकती है। यह प्रक्रिया उतनी ही नैसर्गिक है जितनी ओस की बूँद का सूरज की किरण पड़ने से फ़ना हो जाना।
परतव-ए-ख़ुर से है शबनम को फ़ना की तालीम
मैं भी हूँ एक इनायत की नज़र होते तक
ग़ालिब कहते हैं कि जैसे सूरज की किरण से ओस की बूँद धीरे-धीरे, लेकिन स्वाभाविक रूप से, भाप में तब्दील हो कर फ़ना हो जाती है, वैसे ही प्यार की ‘एक’ दृष्टि ही मुझे मिटा देने के लिए काफ़ी है। यानी प्यार की यह प्रक्रिया भी नैसर्गिक है। ग़ालिब का प्रेम एक तरफ़ा है और उनके इस प्रेम का स्वर ‘इंतज़ार’ और ‘चाह’ है। अपने एक तरफ़ा प्यार को जब ग़ालिब अपनी कविता में व्यक्त करते हैं तो उसमें दोषारोपण या बदले की भावना का स्वर नहीं मिलता, बल्कि निःस्वार्थ इंतज़ार का भाव मिलता है। उदाहरण के लिए ग़ालिब का यह शे’र—
ये न थी हमारी क़िस्मत कि विसाल-ए-यार होता
अगर और जीते रहते यही इंतिज़ार होता
ग़ालिब कहते हैं कि अपने यार से मिलने की उनकी चाह ‘चाह’ ही रह गई क्योंकि उनकी किस्मत में ही मिलना नहीं था। मिलन की इस अधूरी चाह लेकर ही वह मर भी गए। लेकिन आगे वह कहते हैं कि अगर वह जीवित भी रहते हैं तो उनकी बस यही चाह होती कि उससे मिल सकें। और तब भी वह उसी प्रकार से इंतज़ार करते। यह इंतज़ार भी वही इंतज़ार होता जो कि मृत्यु से पहले था। इसलिए इनका एक तरफ़ा प्रेम निःस्वार्थ है, क्योंकि अपनी चाहत और इंतज़ार में ग़ालिब कभी यह नहीं सोचते थे कि एक-न-एक दिन वह भी मुझसे प्यार करेगी। ग़ालिब किसी भी तरीक़े से प्रेम में किसी पर कुछ थोपना नहीं चाहते थे। बस अपनी चाहत को व्यक्त करते थे।
एक तरफ़ा प्रेम को लेकर ग़ालिब की ऐसी सुलझी हुई मानसिकता इसलिए भी है कि वे रिश्ते पर ज़ोर डालते हैं। उनके लिए रिश्ते का अधिक महत्त्व है। यह बात हम उनके इस शे’र से समझ सकते हैं—
तुम जानो तुम को ग़ैर से जो रस्म-ओ-राह हो
मुझ को भी पूछते रहो तो क्या गुनाह हो
हिंदी-साहित्य के इतिहास के अनुसार आधुनिक काल की शुरुआत भले 1850 ई. से मानी जाती है। लेकिन ग़ालिब अपनी कविता के माध्यम से, इससे भी पहले से, अपने आधुनिक होने का परिचय देते हैं। ग़ालिब की सोच तत्कालीन समय-समाज से आगे और आधुनिक तो थी ही, साथ-ही-साथ समकालीन समय-समाज की सोच से भी कई मायनों में आगे और आधुनिक थी।
हुई मुद्दत कि ‘ग़ालिब’ मर गया पर याद आता है
वो हर इक बात पर कहना कि यूँ होता तो क्या होता
ग़ालिब अपनी कविता में दूसरों से प्रश्न भी करते हैं और आत्मालोचना भी। ग़ालिब की कविता हमें दर्शन की ओर ले जाती है। इनकी कविता से हमें ज़िंदगी के प्रति नया दृष्टिकोण मिलता है, तमाम निराशाओं के बीच आशा मिलती है। प्रेम जैसे विषय पर, जिसको समाज आज भी ‘आपत्तिजनक’ समझता है, उनके यह खुले विचार जैसे प्रेम को नैसर्गिक बताना, बजाय अपनी मर्ज़ी को थोपे, निःस्वार्थ इंतज़ार और चाह रखना—उनके स्त्रीवादी नज़रिए को ही दर्शाता है।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
