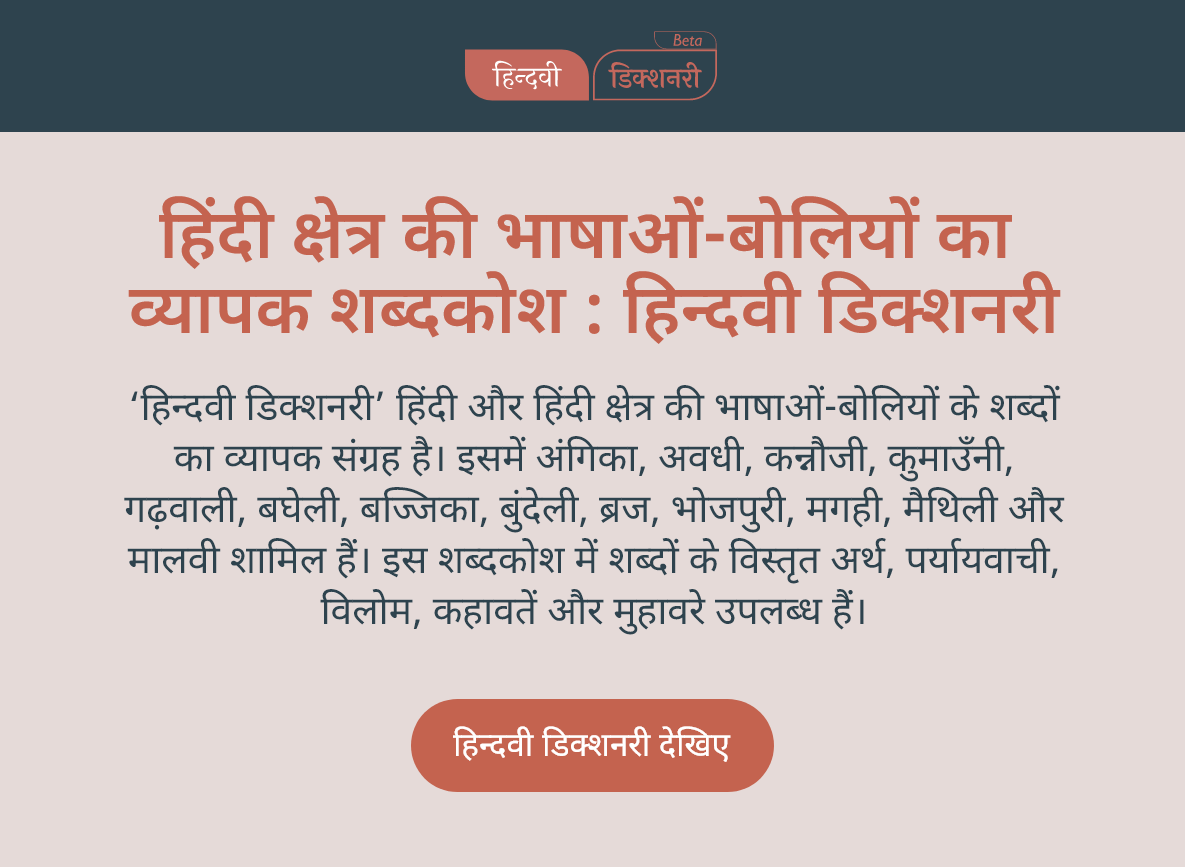प्राचीन भारत में मदनोत्सव
prachin bharat mein madnotsaw
संस्कृत के किसी भी काव्य, नाटक, कथा और आख्यायिका को पढ़िए, वसंत ऋतु का उत्सव उसमें किसी-न-किसी बहाने अवश्य आ जाएगा कालिदास तो वसंतोत्सव का बहाना ढूँढते रहते से लगते हैं। मेघदूत वर्षा ऋतु का काव्य है, पर यक्षप्रिया के उद्यान के वर्णन के प्रसंग में प्रिया के नूपुरयुक्त वाम-चरणों के मृदुल आघात से कंधे पर से फूट उठने वाली अशोक और मुखमदिरा से सिंच कर खिल उठने की लालायित वकुल की चर्चा उसमें आ ही गयी है। वस्तुतः अशोक और बकुल को इस प्रकार खिला देने का उत्सव वसंत में ही मनाया जाता था। वसंत का समय प्राचीन भारत में उत्सवों का काल हुआ करता था! कामसूत्र में इस समय के कई उत्सवों की चर्चा आती है। इनमें दो बहुत प्रसिद्ध है—मदनोत्सव और सुवसंतक। कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने दोनों को एक मान लिया है, पर अन्य ग्रंथों से स्पष्ट है कि ये दोनों उत्सव अलग-अलग दिनों को मनाए जाते थे। भोजदेव के अनुसार सुवसंतक वसंतावतार का उत्सव है—आजकल का वसंत पंचमी का उत्सव। मदनोत्सव होली के रूप में आज भी पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।
मदनोत्सव के उल्लासमय रूप
पुराने ग्रंथों से पता चलता है कि फागुन से आरंभ करके चैत के महीने तक वसंतोत्सव कई प्रकार से मनाया जाता था। इसके दो रूप बहुत प्रसिद्ध थे—एक सार्वजनिक धूमधाम का और दूसरा कामदेव के पूजन का। सम्राट हर्षदेव की रत्नावली नाटिका में इन दोनों प्रकार के उत्सवों का बड़ा ही सरस और जीवंत वर्णन मिलता है। उस दिन सारा नगर पुरवासियों की करतलध्वनि, मधुर संगीत और मृदंग के मादक घोष से मुखरित हो उठता था। नागर जन मदमत्त हो उठते थे। राजा अपने ऊँचे प्रासाद की सबसे ऊँची चंद्रशाला में बैठकर नगरवासियों के आमोद-प्रमोद का रस लेते थे। नागरिकाएँ मधुमास से मत्त होकर सामने पड़ जाने वाले किसी भी पुरुष को पिचकारी (शृंगक) के रंगीन जल से सराबोर कर देती थीं। राजमार्गों के चौराहों पर मर्दल नाम के ढोल और चर्चरी गीत की ध्वनियाँ मुखरित हो उठती थीं। सुगंधित पिष्टातक (अबीर) से दिशाएँ रंगीन हो उठती थीं। केशर मिश्रित पिष्टातक से राजपथ और प्रामाद इस प्रकार आच्छादित हो उठते थे कि प्रातःकालीन उषा की छाया का भ्रम होने लगता था। नागरजनों के शरीर पर शोभमान हेमालंकार और सिर पर धारण किये हुए अशोक के लाल-लाल फूल इस सुनहरी आभा को और भी बढ़ा देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि कुबेर को भी अपनी समृद्धि से जीतने का दावा करने वाली सारी नगरी सुनहरी रंग में डुबो दी गयी है—
कीर्णे:पिष्टातकौधै: कृतदिवसमुखै: कुङ्कुस्नातगौरै:
हेमलंकारभाभिर्भरनमितशिखै: शेखरै: कैङ्किरातैः।
एषा वेषाभिलक्ष्यस्वविभवविजिताशेषवित्तेशकोषा
कौशाम्बी शातकुम्भद्रवखचितजनेवैकपीता विभाति।
(रत्नावलि-1.11)
उस दिन बड़े घरों के सामने आँगन में फव्वारे पूरे वेग से छूटते रहते थे और नागरिकाओं की, अपनी पिचकारी में पानी भरने की उल्लास-लालसा को पूरा करने में सहायक हुआ करते थे। इस स्थान पर पौर-युवतियों के बराबर आते रहने से उनके सीमंत से सिंदूर और कपोलों से अबीर झरते रहते थे और सारा फ़र्श लाल कीचड़ से भर जाता था, फ़र्श सिंदूरमय हो उठता था—
धारायन्त्रविमुक्तसंततपयःपूरप्लुते सर्वतः
सद्यःसान्द्रविमर्दकर्दमकृतक्रीडे क्षणं प्रांगणे।
उद्दामप्रमदाकपोलनिपतत्सिन्दूररागारुणैः
सैन्दूरीक्रियते जनेन चरणन्यासे: पुरः कुट्टिमम्॥
मगर इस उत्सव का सर्वाधिक हुड़दंगी रूप वार-वनिताओं के मुहल्ले के वर्णन में मिलता है। निस्संदेह यह होली का पुराना रूप है।
इसके साथ ही इस उत्सव का एक शांत स्निग्ध चित्र भी मिलता है। भवभूति के मालती-माधव नामक प्रकरण में एक मदनोत्सव का चित्र है। इसमें पता चलता है कि मदनोद्यान—जो विशेष रूप से इस उत्सव के लिए ही बनाया जाता था—इसका मुख्य केंद्र हुआ करता था। इसमें कामदेव का मंदिर हुआ करता था। इसी उद्यान में नगर के स्त्री-पुरुष एकत्र होकर भगवान कंदर्प की पूजा करते थे। यहाँ पर लोग अपनी-अपनी इच्छा के अनुसार फूल चुनते, माला बनाते, अबीर-कुंकुम से क्रीड़ा करते और नृत्य-गीत आदि से मनोविनोद किया करते थे। इस मंदिर में प्रतिष्ठित परिवारों की कन्याएँ भी पूजनार्थ आया करती थीं और मदन देवता की पूजा करके मनोवांछित वर की प्रार्थना करती थीं। जनता की भीड़ प्रातःकाल से ही शुरू हो जाती थी और संध्याकाल तक अबाध गति से आती रहती थी। मालती-माधव से पता चलता है कि अमात्य भूरिवसु की कन्या मालती भी इस उद्यान में कंदर्प पूजन के लिए आई थी। इस पूजन में धार्मिक बुद्धि की प्रधानता होती थी और शोरगुल और हुड़दंग का नाम भी नहीं था। यह मंदिर नगर के बाहर हुआ करता था।
कामदेव की पूजा
मदन देवता की एक पूजा चैत्र के महीने में होती थी। अशोक वृक्ष के नीचे मिट्टी का कलश स्थापित किया जाता था। सफ़ेद चावल भरे जाते थे। फलों और ईख का रस पूजा में नैवेद्य थे। कलश को सफ़ेद वस्त्र से ढका जाता था। चंदन भी उस पर सफ़ेद ही छिड़का जाता था। कलश के ऊपर ताम्र पत्र पर केले के पत्ते रखे जाते थे, जिस पर कामदेव और रति की प्रतिमा उतारी जाती थी और नाना भाँति के गंध, धूप, नृत्य, गीत आदि से देवताओं को तृप्त किया जाता था। यह मत्स्यपुराण की बात है। इसके दूसरे दिन चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को भी पूजा होती थी। लोग व्रत रखते थे।
शिल्परत्न, विष्णुधर्मोत्तर पुराण आदि ग्रंथों में कामदेव की प्रतिमा बनाने की विधियाँ दी गई हैं। विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार उसके आठ भुज हैं, चार पत्नियाँ; परंतु शिल्परत्न में केवल यही कहा गया है कि वह अपूर्व सुंदर हो और उसकी बाईं ओर अभिलाषवती रति और दाहिनी ओर गृहकर्मनिरता प्रीति, ये दो पत्नियाँ हों। स्थाई मंदिरों में दोनों प्रकार की मूर्तियाँ बनती थी, पर अशोक वृक्ष के नीचे जो मूर्ति बनती थी वह द्विभुज ही होती होगी। रत्नावली नाटिका में राजा को अशोक वृक्ष के नीचे बैठा देखकर रत्नावली को भ्रम हो गया था कि कामदेव साक्षात् आकर पूजा ग्रहण करते हैं।
अशोक के फूल खिलाने का अनुष्ठान
कालिदास के ‘मालविकाग्निमित्र’ और श्री हर्षदेव की ‘रत्नावली’ में इस उत्सव के सर्वाधिक सरस अनुष्ठान, अशोक में पुष्प ले आने का विवरण मिल जाता है। भोजराज और श्री हर्षदेव की गवाही पर कहा जा सकता है कि उस दिन सुंदरियाँ कुसुंभी रंग की साड़ी पहनती थीं। तुरंत स्नान करने से रानी वासवदत्ता की शरीर-कांति और भी निखर आई थी, वह कौसुंभराग से रंजित साड़ी पहनकर जब अशोक वृक्ष के नीचे कामदेव की पूजा कर रही थी तो उसके साड़ी का लाल पल्ला फड़फड़ा उठा था। उस समय राजा को ऐसा लगा था, जैसे तरुण प्रवाल विटप की लता ही लहरा उठी हो—
प्रत्यग्रमज्जनविशेषविविक्तकान्तिः
कौसुम्भरागरुचिरस्फुरदंशुकान्ता।
विभ्राजसे मकरकेतनमर्च्चयन्ती
बालप्रवालविटपिप्रभवा लतेव।
‘मालविकाग्निमित्र’ से पता चलता है कि मदन देवता की पूजा के बाद ही अशोक में फूल खिला देने का अनुष्ठान होता था। ‘रत्नावली’ में भी इसकी चर्चा है। इस अनुष्ठान का रूप इस प्रकार था—कोई सुंदरी सर्वाभरणभूषिता होकर, पैरों को अलक्तकराग से रंजित करके, नूपुर सहित बाएँ चरण से अशोक वृक्ष पर आघात करती थी। इधर नूपुरों की हल्की झनझनाहट, उधर अशोक का सोल्लास कंधे पर से ही फूल उठना। साधारणतः रानी यह कार्य करती थीं। पर ‘मालविकाग्निमित्र’ में बताया गया है कि उस दिन रानी के पैरों में चोट आ गई थी, इसलिए उन्होंने मालविका को भेज दिया था। मालविका अशोक वृक्ष के पास गई, पल्लवों का गुच्छा हाथ में पकड़ा और बाएँ पैर से अशोक पर मृदु आघात किया। कालिदास की लेखनी ने इस मादक चित्र को अपूर्व गरिमा से भर दिया है।
काम देवता क्या हैं?
परब्रह्म की उस मानसिक इच्छा का, जो संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होती है, मूर्तरूप ही 'काम' है। जब यह सृष्टि-रचना के अनुकूल होती है तो विष्णु और शिव का साक्षात् रूप कही जाती है। गीता में श्रीकृष्ण ने कहा है कि मैं जीवमात्र में धर्म के अविरुद्ध रहने वाला 'काम' हूँ, परंतु जो व्यक्तिगत इच्छा धर्म के विरुद्ध जाती है, वह अपदेवता है। काम का एक रूप धर्म के अविरुद्ध जाने वाला है, दूसरा धर्म के विरुद्ध जाने वाला। पहला साक्षात् विष्णुरूप है। ब्रह्मसंहिता में कहा गया है कि जो आनंद और चेतनामय रस से मन को भरता है, प्राणियों के मन में 'स्मर' या 'काम' रूप से प्रतिफलित होता है और इस प्रकार अशेष भुवनों को जीतकर नित्य विराजमान है, उस आदिपुरुष गोविंद को मैं स्मरण करता हूँ। मत्स्यपुराण में 'कामनाम्ना हरेरर्चा' कहकर बताया गया है कि वस्तुत: 'काम' नामक हरि की ही पूजा की जाती है। इसलिए मंदिर और मूर्ति बनाकर जिस देवता की पूजा की जाती है, वह साक्षात् विष्णु ही हैं। श्रीकृष्ण-गायत्री और काम-गायत्री में कोई फ़र्क़ नहीं है।
परंतु इसका एक दूसरा रूप भी है जो व्यक्ति के विवेक को दबा देता है। पश्चिम में 'किउपिद्' नामक देवता (या अपदेवता) को अंधा माना गया है, क्योंकि वह विवेक को नष्ट करता है, मनुष्य को अंधा बना देता है। शिव ने इसी मादक मदन देवता को भस्म किया था। उसके भावात्मक 'मनसिज' रूप को बचा लिया था। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे शास्त्रों में वार-वनिताओं के लिए जिस मदनमूर्ति का विधान किया गया है, उसकी आँखों पर सोने के पत्तर की पट्टी बँधवा दी जाती है। 'किउपिद्' देवता की तरह उसे अंधा तो नहीं कहा गया, पर अंधे-जैसा बना अवश्य दिया गया है। ‘हैमनेत्र परावृतम्' में पट्टी सोने की होने पर भी दृष्टि शक्ति का अभाव तो हो ही जाएगा। कामदेव वसंत ऋतु का मित्र है। परंतु ‘कुमारसंभव’ में वर्णित वसंत अकाल का वसंत है; अस्वाभाविक, बलादानीत, अपदेवता! शिव ने इसी को ज्ञान के नेत्र उन्मीलित करके भस्म किया था।
मदनोत्सव की सुरुचिपूर्णता
शास्त्रों में काम के बाण और धनुष फूलों के बताए गए हैं। अरविंद, अशोक, आम, नवमल्लिका और नीलोत्पल, ये उसके पाँच बाण हैं, जिन्हें क्रमशः उन्मादन, तापन, शोषण, स्तंभन और सम्मोहन भी कहा गया है।
संसार की लगभग सभी सभ्य आदिम जातियों में वसंत काल में उद्दाम यौवनोन्माद के उत्सव पाए जाते हैं। कहीं-कहीं ये उत्सव बहुत ही स्थूल यौन-वासना के रूप में पाए जाते हैं और कहीं संयत और सुरुचिपूर्ण रूप में। प्राचीन भारत में इस उत्सव के उद्दाम रूप को संयत, सुरुचिपूर्ण और धर्माविरुद्ध देवता के रूप में सँवारने का सफल प्रयत्न किया गया था। अपेक्षाकृत निम्न स्तर के लोगों में सदा वह सीमातिक्रमण करके प्रकट होता रहा और दुर्भाग्यवश अब भी किसी-न-किसी रूप में जी रहा है, परंतु इस सहज उद्दाम लीला को शांत, संयत और शिष्ट रूप में ढालने का प्रयत्न अवश्य ही श्लाघ्य माना जाएगा। आदिम सहजात वृत्तियों को सुरुचिपूर्ण, संयत और कल्याणमुखी बनाकर ही मनुष्य 'मनुष्य' बना है, नहीं तो वह पशु ही रह गया होता। प्राचीन भारत के मदनोत्सव में मनुष्य के इस प्रयत्नशील तत्व की ही चरितार्थता प्राप्त होती है।
- पुस्तक : निबंध गरिमा (नवल किशोर एम ए) (पृष्ठ 67)
- संपादक : नवल किशोर (एम ए)
- रचनाकार : हज़ारी प्रसाद द्विवेदी
- प्रकाशन : जयपुर पब्लिशिंग हाउस
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.