रविवासरीय : 3.0 : हिंदी में विश्व कविता का विश्व
 अविनाश मिश्र
20 अप्रैल 2025
अविनाश मिश्र
20 अप्रैल 2025
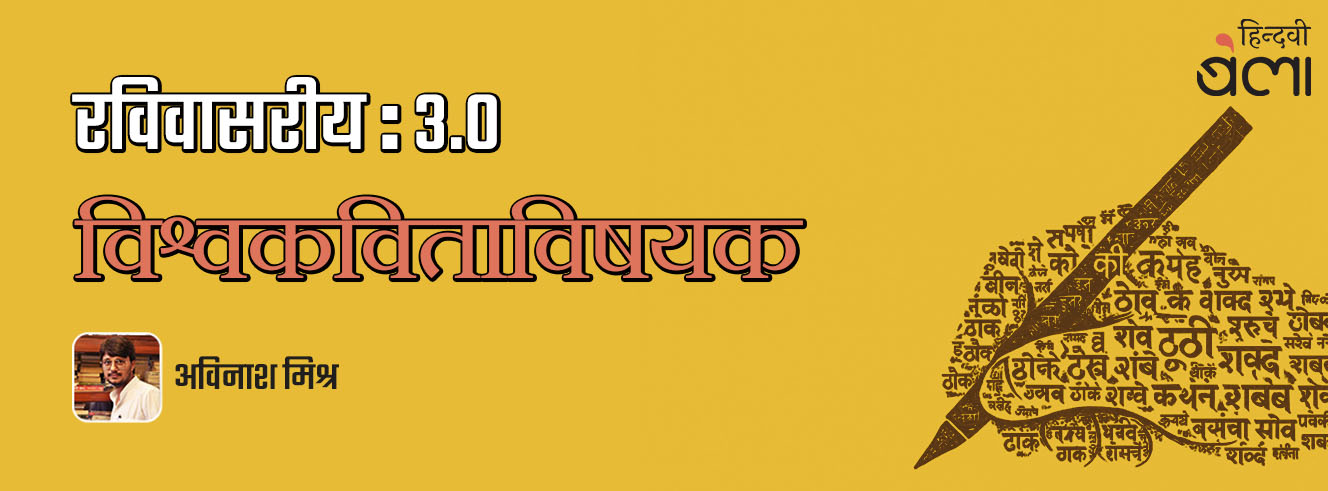
• गत सौ-सवा वर्षों की हिंदी कविता पर अगर एक सरसरी तब्सिरा किया जाए और यह जाँचने-जानने के यत्न में संलग्न हुआ जाए कि हमारी हिंदी दूसरी भाषाओं में उपस्थित सृजन के प्रति कितनी खुली हुई है; तब यह तथ्य एक राह की तरह प्रकट होता है कि हिंदी का संसार अपनी सीमाओं और संसाधनों के स्थायी विलाप के बावजूद एक बेहद खुला हुआ संसार है, जिसमें अपनी शक्ति भर अपने समय में कहीं पर भी किसी भी भाषा में हो रहे उल्लेखनीय सृजन को अपनी सीमाओं और संसाधनों में ले आने की सदिच्छा है।
• हिंदी भाषा और साहित्य के संसार के लिए कुएँ का रूपक गढ़ने वाले इस संसार के सबसे दयनीय व्यक्तित्व हैं। दरअस्ल, वे ख़ुद ही एक ऐसे कुएँ में पड़े हुए हैं—जो भरा तो हिंदी के जल से ही है; लेकिन न वह अपने स्रोत देख पाता है, न अपनी नदियाँ, न अपने सागर-महासागर।
• हिंदी संसार इतना व्यापक, इतना घटनाबहुल और इतना ज़्यादा उत्पादकतायुक्त है कि यहाँ बहुत सारे ज़रूरी काम और कामगार, कृतियाँ और कृतिकार समय पर मूल्यांकित-विश्लेषित नहीं हो पाते हैं। इस संसार में शोर बहुत आग्रही, उपद्रवी और हावी है; वह इतना ज़्यादा स्थान, समय और संलग्नता ले लेता है कि बहुत सारी प्रकृति अनदेखी-अनसुनी-अनछुई रह जाती है।
• आज से क़रीब पाँच वर्ष पूर्व विश्व कविता पर एकाग्र पत्रिका ‘तनाव’ में प्रकाशित काव्यानुवादों के तीन खंड [संपादक : वंशी माहेश्वरी, संभावना प्रकाशन और रज़ा फ़ाउंडेशन का सह-प्रकाशन, प्रथम संस्करण : 2020] क्रमशः ‘दरवाज़े में कोई चाबी नहीं’, ‘प्यास से मरती एक नदी’ और ‘सूखी नदी पर ख़ाली नाव’ शीर्षक से प्रकाशित हुए।
विश्व कविता का हिंदी अनुवाद में यह कथित रूप से सबसे बड़ा संचयन है। इसमें 33 देशों की 28 भाषाओं के 103 कवियों की कविताओं के 48 कवियों और विद्वानों द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद शामिल हैं। रज़ा पुस्तक माला के प्रधान संपादक और रज़ा फ़ाउंडेशन के तत्कालीन प्रबंध न्यासी अशोक वाजपेयी के शब्दों में : ‘‘यह अत्यंत मूल्यवान् सामग्री पत्रिका के रूप में खो न जाए, इस ख़याल से हमने वंशी माहेश्वरी से आग्रह किया कि वह अब तक ‘तनाव’ में प्रकाशित सभी अनुवादों से चयन कर उन्हें तीन खंडों में पुस्तकाकार एकत्र और संयोजित कर दें।’’ [प्रथम खंड, पृष्ठ : 8]
• ‘तनाव’ का पहला अंक वर्ष 1972 के दिसंबर में आया था। इस प्रवेशांक से 12 वर्ष पूर्व ‘देशांतर’ [अनुवाद और संकलन : धर्मवीर भारती, भारतीय ज्ञानपीठ, प्रथम संस्करण : 1960] का प्रकाशन हुआ था। ‘देशांतर’ में 21 देशों के 113 कवियों की 161 कविताओं के एक ही कवि-विद्वान-व्यक्ति [धर्मवीर भारती] द्वारा किए गए हिंदी अनुवाद हैं। गए सौ वर्षों की हिंदी कविता में आधुनिक काव्य-बोध निर्मित करने में ‘देशांतर’ का आरंभिक योगदान अद्वितीय, अविस्मरणीय और अमूल्य है।
‘देशांतर’ कुछ इस प्रकार की एक आधारभूत परिघटना है, जिसके पीछे से कुछ और आगे से कई दिशाएँ फूटती हैं। यह अलग बात है कि ‘देशांतर’ के वक्तव्य में दावा कम, संकोच ज़्यादा नज़र आता है : ‘‘यह संकलन समूचे आधुनिक काव्य का सर्वांग-संपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, यह मेरा दावा क़तई नहीं है। यह केवल उसके वैविध्य की बानगी प्रस्तुत करता है।’’ [धर्मवीर भारती, देशांतर, पृष्ठ : 5]
• सांस्कृतिक धाराओं की परस्पर समझ के लिए अनुवाद-कर्म एक पवित्र, प्रासंगिक और महत्त्वपूर्ण कर्म है। आधुनिक हिंदी कविता के संदर्भ में यह समझ बहुत प्रारंभ, लगभग छायावाद के दौर, से ही व्यवहार में व्यक्त होना शुरू हो गई थी। हिंदी के अधिकांश श्रेष्ठ कवियों के परिचय में उनके अनुवाद-कर्म का उल्लेख पाया जा सकता है। यह उल्लेखनीयता एक अदेखे संसार को देखने, उससे गुज़रने, उसे समझने और समझकर अपने संसार का अंश बना लेने के विवेक से संभव हुई है। इसने हमारे सांस्कृतिक-साहित्यिक क्षितिज को व्यापक किया है और हमारे परिसर तथा दृष्टि को अब तक संकीर्ण होने से बचाए रखा है।
• ‘देशांतर’ और ‘तनाव’-काल के बीच भी हिंदी में विश्व कविता के अनुवाद के आयोजन पत्र-पत्रिकाकार, पुस्तिकाकार और पुस्तकाकार भी समय-समय पर होते रहे हैं। ये यत्न सरकारी, अर्द्धसरकारी, ग़ैरसरकारी, संस्थागत, व्यक्तिगत सभी तरह के रहे; लेकिन यह बेखटके कहने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि निरर्थकता के स्थायी और अनिवार्य प्रतिशत के बावजूद इस काम का बहुत सारा अंश असरकारी [प्रभावी] है। ‘दिनमान’, ‘पहल’, ‘पूर्वग्रह’, ‘साक्षात्कार’, ‘सदानीरा’ और साहित्य अकादेमी की कोशिशें इस सिलसिले में देखी जा सकती हैं।
सदिच्छा अपनी जगह है और गुणवत्ता अपनी जगह [जिस पर यहाँ आगे बात होगी]; लेकिन इस प्रकार के प्रयत्न स्वागत-योग्य ही माने जाने चाहिए, क्योंकि इनसे हिंदी के आतिथ्यपूर्ण स्वभाव का संकेत मिलता है।
‘तनाव’-काल की अवधि के दरमियान ही हिंदी में विश्व कविता के अनुवाद का एक वृहद पुस्तकाकार यत्न वर्ष 2003 में भी नज़र आया था। ‘रोशनी की खिड़कियाँ’ [चयन, संयोजन और अनुवाद : सुरेश सलिल, मेधा बुक्स] शीर्षक से प्रकाशित यह चयन 20वीं सदी की विश्व कविता से है और इसमें 31 भाषाओं के 112 कवियों की कविताओं को शामिल किया गया।
‘न सीमाएँ न दूरियाँ’ [अनुवाद : कुँवर नारायण, वाणी प्रकाशन, प्रथम संस्करण : 2017] शीर्षक से विश्व कविता से कुछ अनुवादों का प्रकाशन भी कोई बहुत प्राचीन घटना नहीं है।
इस प्रसंग में ‘तनाव’ में प्रकाशित काव्यानुवादों के तीनों खंड सबसे नवीनतम दस्तावेज़-संकलन हैं। इनके ज़रिये गत 50 वर्षों की हिंदी में विश्व कविता के विश्व का अर्थ एक जगह एकत्र है। इनकी नवीनता इस बात में भी है कि इसमें हमारी सामूहिकता का दृश्य है। यह किसी अकेले व्यक्ति का काम न होकर, एक साहित्य-समाज का काम नज़र आता है। इसमें हमारे समय के कई क़ाबिल और ज़रूरी हाथों ने सहयोग दिया है। इस संदर्भ में यह सूची प्रमाण की तरह प्रस्तुत है :
रघुवीर सहाय, कुँवर नारायण, विष्णु खरे, अशोक वाजपेयी, सोमदत्त, कमलेश, प्रयाग शुक्ल, गिरधर राठी, शिवकुटी लाल वर्मा, लक्ष्मीधर मालवीय, प्रेमलता वर्मा, सुरेश सलिल, चंद्रप्रभा पांडेय, कांता, रमेशचंद्र शाह, नंदकिशोर आचार्य, दिविक रमेश, मंगलेश डबराल, असद ज़ैदी, उदय प्रकाश, अवधेश कुमार, विनय दुबे, वरयाम सिंह, त्रिनेत्र जोशी, प्रभाती नौटियाल, वीरेंद्र कुमार बरनवाल, भारत भारद्वाज, विभा मौर्य, उदयन वाजपेयी, अनिल जनविजय, संगीता गुंदेचा, हेमंत जोशी, अक्षय कुमार, हरिमोहन शर्मा, मधु शर्मा, सईद शेख़, उज्ज्वल भट्टाचार्य, अशोक पांडे, शिवप्रसाद जोशी, राजुला शाह, पीयूष दईया।
• एक शताब्दी से अधिक के आधुनिक अनुभव के बावजूद हिंदी में अनुवाद-कर्म से संबद्ध सबसे दुर्बल पक्ष अब भी यह है कि हिंदी में ज़्यादातर अनुवाद आज भी अँग्रेज़ी के माध्यम से किए जाते हैं। इस प्रकार देखें, तब देख सकते हैं कि हिंदी में विश्व कविता या साहित्य का अनुवाद पढ़ रहा व्यक्ति; दरअस्ल—विश्व कविता या साहित्य का कम, अनुवाद का अनुवाद अधिक पढ़ रहा होता है। सीधे मूल भाषाओं से अनुवाद की परंपरा और प्रक्रिया हिंदी में अत्यंत अविकसित है। सीधे मूल भाषाओं से अनुवाद की माँग हिंदी में कोई नई माँग नहीं है। यह कई अवसरों पर कई बार की जा चुकी है। प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न विश्व-भाषाओं में स्नातक-परास्नातक हुए छात्र और शोधार्थी जिन भिन्न-भिन्न गलियों में गुम हो जाते हैं, दुर्भाग्य से उनमें से एक भी हिंदी साहित्य में उपस्थित अनुवाद-परंपरा की ओर नहीं मुड़ती है। कवि कह गया है : ‘तुझसे भी दिल-फ़रेब हैं ग़म रोज़गार के...’ [फ़ैज़ अहमद फ़ैज़, सारे सुख़न हमारे, पृष्ठ : 33, राजकमल प्रकाशन, संस्करण : 2000]
• अनुवाद-कर्म—जिसके बारे में मितभाषी छवि के मालिक निर्मल वर्मा कहते हैं : ‘‘अनुवाद का काम न केवल कुछ हद तक किसी लेखक के आरंभिक वर्षों में उसकी आर्थिक कठिनाई हल कर देता है, बल्कि ‘मनोवैज्ञानिक थेरेपी’ की तरह उसके संताप और अकेलेपन को भी दूर करता है।’’ [रत्न-कंगन तथा अन्य कहानियाँ, अलेक्सांद्र कुप्रीन, अनुवाद : निर्मल वर्मा, पृष्ठ : 9, वाणी प्रकाशन, संस्करण : 2010]—हमारे यहाँ अब तक व्यवसाय नहीं बन पाया है—विशेष रूप से साहित्यिक अनुवाद-कर्म। इसमें अधिकांश प्रसंगों में न संतोषजनक भुगतान/मानदेय है, न रोज़गार की संभावनाएँ। यहाँ अनुवाद-कर्म भी साहित्य-सेवा या स्वांतः सुखाय कर्म के अंतर्गत ही आता है। इसलिए हिंदी में प्रतिभाशाली, विशुद्ध और पेशेवर अनुवादक नहीं हैं। हिंदी-प्रकाशन-जगत् में एक अनुवादक के लिए कोई ढाँचा, कोई तय मूल्य, कोई सम्मान नहीं है। इसलिए इस तरफ़ साहित्यप्रेमी या विशुद्ध साहित्यकार ही आकर्षित होते हैं। उनके लिए आर्थिक प्रश्न हमेशा दूसरे प्रश्न होते हैं। वे अपने लिखने-पढ़ने के काम की तरह ही अनुवाद करते हैं—प्रेम की मज़दूरी, Labour of love, [निर्मल वर्मा के अनुवाद-कर्म के संबंध में प्रयुक्त गगन गिल का पद] समझकर या संपादकों से मित्रता या उनके आग्रह के वशीभूत होकर... और इस तरह वे इसमें ‘मनोवैज्ञानिक थेरेपी’ की तलाश भी कर लेते हैं। वे बहुत ठोस रूप से महज़ अनुवाद करने के लिए अनुवाद नहीं करते हैं, क्योंकि वे मूलतः अनुवादक नहीं होते हैं।
इस सबके समानांतर एक सिलसिला विदेशी दूतावासों का भी चलता रहता है। यह सिलसिला काफ़ी लाभकारी है और हिंदी में अनुवाद-कर्म के प्रचलित, सुपरिचित और समकालीन ढाँचे में अलग ही नज़र आता है। एक समय में एक-दो प्रतिभावान्, योग्य और समीकरणवादी कवि-लेखक-अनुवादक पूरी तरह इस सिलसिले पर ही निर्भर होकर लंबे समय तक आत्मनिर्भर बने रहते हैं। उनके जीवन अर्थ-लाभ, सराहना और सम्मान के साथ सुविधापूर्ण ढंग से गुज़र जाते हैं; और हिंदी को भी संसार की कुछ उत्कृष्ट कृतियों-रचनाओं के ठीक-ठाक अनुवाद प्राप्त हो जाते हैं। इसके बावजूद हिंदी में आज एक साथ बेरोज़गार और अनुवादक होना किसी भी दृष्टि से एक बेहतर स्थिति नहीं है। वहीं दूसरी तरफ़ हमारी हिंदी में कुछ ऐसे अनुवादक भी सक्रिय हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी काव्यानुवाद में गुज़र गई। हज़ारों पन्नों और कई किताबों में उनके किए काव्यानुवाद बिखरे हुए और संगृहीत हैं, लेकिन उनके यहाँ एक भी कविता का अनुवाद सलीक़े और ठिकाने का नहीं है। इस क़दर होने में उन्हें न तो कोई विशेष अर्थ-लाभ हुआ, न सराहना मिली, न ही कोई सम्मान मिला।
यहाँ अब इस स्तंभ के केंद्रीय विषय पर वापस आते हैं। ‘तनाव’ में प्रकाशित काव्यानुवादों के तीनों खंडों में कुछ कवियों के अनुवाद सीधे उनकी मूल भाषा से हिंदी में संभव हुए हैं। यह जानना दिलचस्प है कि इन कविताओं के अनुवादक उन अर्थों में मूलतः हिंदी कवि-लेखक नहीं हैं; जिन अर्थों में एक हिंदी कवि-लेखक को जानने का चलन है, जैसे : प्रेमलता वर्मा [स्पैनिश], रेनाता चेकाल्स्का [पोलिश], कुमकुम सिंह [तुर्की], शारका लित्विन [चेक], सईद शेख़ [फ़िनिश], हेमंत जोशी [फ़्रेंच], उज्ज्वल भट्टाचार्य [जर्मन], हरिमोहन शर्मा [पोलिश], प्रभाती नौटियाल [स्पैनिश], विभा मौर्य, [स्पैनिश], मीना ठाकुर [स्पैनिश], तोमोको किकुची [जापानी], लक्ष्मीधर मालवीय [जापानी], त्रिनेत्र जोशी [चीनी], दिविक रमेश [कोरियन], अनिल जनविजय [रूसी], वरयाम सिंह [रूसी]। वहीं इन खंडों में मूलतः हिंदी कवियों द्वारा किए गए संसार के अत्यंत समादृत कवियों के अनुवाद पढ़कर दिलचस्पी का यह प्रसंग एक विचित्र स्वरूप ले उठता है। इस वैचित्र्य को यहाँ कुछ आगे उद्घाटित करेंगे, इससे पहले समकालीन हिंदी काव्य-भाषा और शिल्प पर कुछ कहना प्रसंगोचित होगा।
समकालीन हिंदी कविता जो अपने मूल और कुल असर में ‘नई कविता’ के दौर का विस्तार है; उसका केंद्रीय, प्रचलित और सम्माननीय हिस्सा प्राय: अनूदित होने की या विश्व कविता जैसा या उसके समकक्ष नज़र आने की महत्त्वाकांक्षा में संभव हुआ है। यह यों ही नहीं है कि बीते कुछ दशकों में कुछ प्रतिष्ठित कवियों, आलोचकों और अनुवादकों के द्वारा किए गए इस प्रकार के दावे कानों, आँखों और दिमाग़ों में पड़ते रहे हैं कि समकालीन हिंदी कविता विश्व की किसी भी भाषा की समकालीन कविता से श्रेष्ठ या उसके जोड़ की है। ये ऐसे दावे हैं, जिनसे हिंदी की बिल्कुल आती हुई कविता में भी गर्वांकुर फूटने लगते हैं। इस स्थिति में हिंदी कविता स्वयं भी इस सबसे फलभारावनत होते हुए, अब बहुधा कहीं भी कैसे भी किसी भी भाषा में अनूदित होने के लिए ही लिखी जाती है!
इसके फलस्वरूप हिंदी कविता पराग्वे, मेडागास्कर, टिम्बकटू, होनोलूलू, तेहरान, तिब्बत, नार्वे, स्वीडन, आइसलैंड, प्रशिया, आर्मीनिया, पुर्तगाल, सिंगापुर, इंडोनेशिया में तो ख़ूब पढ़ी जाती है; लेकिन हिंदी में नहीं! यहाँ व्यक्त विचार में व्यंग्य और विडंबना को समझने की ज़रूरत है, जिसके अंतर्गत इतना ही बहुत है कि हिंदी कविता का अनुवाद पहले हिंदी में ही हो जाए। वह अपनी कहन और प्रयोगशीलता में वैश्विक होने से पहले भारतीय, और अनुवादनीय होने से पहले पठनीय होने की कोशिश करे। वह अपने बहुत अपने व्यापक समाज में अपनी उपेक्षित स्थिति को महसूस करते हुए अपने से बाहर भी देखे और अपनी वास्तविक पहुँच का सच्चा मूल्यांकन करने के बाद अपनी बहुत सीमित जगह और संकुचित पाठक-वर्ग को ध्यान से समझे।
अब यहाँ पूर्व अनुच्छेद में उल्लिखित वैचित्र्य को उद्घाटित करने का समय है। ‘तनाव’ में प्रकाशित काव्यानुवादों के तीनों खंडों में मूलतः हिंदी कवियों द्वारा किए गए संसार के अत्यंत समादृत कवियों के अनुवाद पढ़कर पता लगता है कि हमारे समकालीन प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी कविता का साँचा कहाँ से पाया है! इस तलाश में होर्हे लुई बोर्हेस की कविताएँ कुँवर नारायण के अनुवाद में कुँवर नारायण की कविताओं जैसी लगती हैं। मिक्लोश राद्नोती की कविताएँ विष्णु खरे के अनुवाद में विष्णु खरे की कविताओं जैसी लगती हैं। इस क्रम में हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, पाते हैं कि यान्निस रित्सोस की कविताएँ मंगलेश डबराल के अनुवाद में मंगलेश डबराल की कविताओं जैसी लगती हैं। सोमदत्त, कमलेश, रमेशचंद्र शाह द्वारा किए गए अनुवादों का भी यही हाल है और उदय प्रकाश, असद ज़ैदी द्वारा किए गए अनुवादों का भी। फ़र्नांदो पेसोआ की कविताएँ गिरधर राठी के अनुवाद में गिरधर राठी की कविताओं जैसी लगती हैं और ओसिप मान्देल्स्ताम की कविताएँ प्रयाग शुक्ल के अनुवाद में प्रयाग शुक्ल की कविताओं जैसी। गिरधर राठी और प्रयाग शुक्ल तो इतने समर्थ अनुवादक हैं कि वे संसार के विशिष्ट से विशिष्ट कवि की कविताओं को अपनी कविताओं जैसा बना डालते हैं या बहुत संभव है कि इन्होंने अपनी कविताओं को संसार के बड़े कवियों की कविताओं के अनुवाद सरीखा बना डाला हो। कवि कह गया है : ‘‘मूल जानना बड़ा कठिन है—नदियों का, वीरों का।’’ [रामधारी सिंह दिनकर, रश्मिरथी, पृष्ठ : 20, लोकभारती प्रकाशन, संस्करण : 2009]
यहाँ अशोक वाजपेयी के इस कथ्य से भी गुज़रते चलें : ‘‘अनुवाद में कविता का दूसरा जीवन शुरू होता है। अपनी कविताओं को दूसरी भाषा में देखना-सुनना, कुछ विचित्र-सा अनुभव है : आप अपने को ही पहचान नहीं पाते, फिर भी यक़ीन करते हैं कि दूसरी भाषा में आप ही हैं। ध्वनियाँ, अनुगूँजें आदि सब अलग होती हैं और फिर भी आपकी कविता है—कई बार यह सोचकर अपने अबोध भरोसे पर अचरज होता है।’’ [कविता : क्या कहाँ क्यों; पृष्ठ : 245, राजकमल प्रकाशन, संस्करण : 2021]
• ‘तनाव’ में प्रकाशित काव्यानुवादों के तीनों खंडों में अनूदित कवि की वे काव्यात्मक विशेषताएँ और उपलब्धियाँ जो कविताओं के अनुवाद से पूर्व अनुवादक द्वारा दिए गए गद्य/नोट/भूमिका आदि में बताई गई हैं, वे प्राय: कविताओं में नज़र नहीं आती हैं। इस प्रसंग में प्रस्तुत कविताएँ—जैसा कि कहा गया—अनुवादक की अपनी कविताओं या बहुत सारी आधुनिक/समकालीन हिंदी कविताओं जैसी लगती हैं। यहाँ आकर ही यह लगता है कि अनुवाद या तो सच में बहुत मुश्किल काम है या फिर वह भाषा और रचना के विरुद्ध एक भारी साज़िश है। साज़िश—महाकवियों की कविता का अनुवाद करके अपनी जैसी कविता [जो कि उनके जैसी होने की कोशिश में अपने जैसी नहीं हो पाई है] को वैध मनवाने के उपक्रम से उत्पन्न साज़िश।
इन तीनों खंडों में बहुत कम हिंदी कवि-अनुवादक ही इस वैचित्र्य से बच पाए हैं—रघुवीर सहाय, अशोक वाजपेयी और उदयन वाजपेयी के नाम इस क्रम में लिए जा सकते हैं। इन कवियों ने अपने द्वारा किए गए काव्यानुवादों को अपनी कविता जैसा होने-लगने से बचाया है। यह श्रम और प्रतिभापूर्ण सँभाल इनके किए गए अनुवादों को विशिष्ट बनाती है। इसके अतिरिक्त सीधे मूल भाषाओं से बहुत कुशलतापूर्वक किए गए अनुवाद भी इन खंडों का एक विशेष आकर्षण हैं। इसके साथ ही ‘तनाव’ की अभावग्रस्त और संघर्षमय तीर्थयात्रा पर वंशी माहेश्वरी की प्रस्तावना पढ़कर हिंदी में एक लघु पत्रिका के निरंतर बने रहने के संकटों से दो-चार हुआ जा सकता है। हिंदी में ‘तनाव’ का महत्त्व, अनुवाद-कर्म की स्थिति और अनुवाद-प्रक्रिया के मर्म के लिए उदयन वाजपेयी और गिरधर राठी की वे टिप्पणियाँ भी पढ़ने-योग्य हैं; जो उन्होंने क्रमशः फ़्रांसीसी कवि फ़्रेंक आंद्रे जाम, यीव बोनफ़्वा और जर्मन कवि बेर्टोल्ट ब्रेष्ट की कविताओं के अनुवाद से पूर्व इस संचयन के पहले और दूसरे खंड में दी हैं। उदयन अपनी टिप्पणी में कहते हैं :‘‘अनुवाद करते समय हम दरअस्ल कृति के एक्सेंट को ही अपनी भाषा के विन्यास में पकड़ने की कोशिश करते हैं। [प्रथम खंड, पृष्ठ : 361]
दूसरे खंड में प्रस्तुत ब्रेष्ट की कविताओं के अनुवाद गिरधर राठी ने रायनर लोत्स के साथ मिलकर सीधे जर्मन से किए हैं। इस प्रसंग में अनुवादक-द्वय कहते हैं : ‘‘ब्रेष्ट के अनुवाद का, किसी भी कविता के अनुवाद का, सुगमतम उपाय सब जानते हैं : अपनी प्रचलित-परिचित काव्य-भाषा में, जानी-मानी लयों में, सुग्राहय रूपकों-छंदों-काव्यचित्रों में उनका उलथा कर देना। इस तरह का एक ‘खरा और सच्चा’ ब्रेष्टीय काव्य-संसार रच देना आसान है। किसी हद तक यह तरीक़ा उपयोगी भी है। पर इस सहजयान में ब्रेष्ट की वे सारी सिर-तोड़ चेष्टाएँ—जो उसे अपने ढंग का अकेला कवि बनाती हैं—गुम हो जाने का पूरा-पूरा ख़तरा है।’’ [पृष्ठ : 105]
वहीं यीव बोनफ़्वा की कविताओं के अनुवाद के प्रसंग में गिरधर राठी फ़रमाते हैं : ‘‘न सिर्फ़ इन कविताओं के अनुवाद के बारे में, बल्कि कविता के अनुवाद के बारे में भी बहुत तरह के संकोच हैं। एक ओर ओक्ताविओ पाज़ जैसे कवि मानते हैं कि कविता का अनुवाद स्वयं उसी भाषा में भी नहीं हो सकता। पर दूसरी ओर ऐसे भी उदाहरण हैं, जो अनुवाद-कर्म में आस्था बढ़ाते हैं। हंगरी के निर्वासित कवि जॉर्ज फ़ालुदी ने 15वीं सदी के विख्यात फ़्रांसीसी कवि विलों का हंगारी [मॉजॉर] भाषा में जो अनुवाद किया था, 1930 के आस-पास, वह मूल से भी बेहतर बताया जाता है। उसके 30 संस्करण हो चुके हैं। ऐसा ही उदाहरण उमर ख़य्याम का फ़िट्ज़जेराल्ड कृत अनुवाद है। कहते हैं इसमें मूल ख़य्याम को तहस-नहस कर दिया गया है—फिर भी उस अनुवाद की अपनी ही कशिश है। ...दरअस्ल, अनुवाद से बढ़कर उबाऊ काम संसार में नहीं है। इसके बावजूद अनुवाद-कर्म आकर्षक है—कभी-कभी रचनात्मक स्वार्थों के कारण अनिवार्य भी।’’ [द्वितीय खंड, पृष्ठ : 427-428]
अंततः इन खंडों के पाठ से इस तथ्य से भी वाक़िफ़ हुआ जा सकता है कि अक्सर ख़राब और महीन महत्त्ववाले कवि, अपने जैसे ही ख़राब और महीन महत्त्ववाले कवियों को अपनी भाषा में अनुवाद के लिए चुन लेते हैं। उनके चुनाव में कवियों, कविताओं और जगहों की वर्तनी में सावधानी, शुद्धता और एकरूपता का अभाव भी यत्र-तत्र चुभता रहता है।
• यह एक कठिन सचाई है कि संसार की बहुत सारी महत्त्वशाली कविता अनुवाद से परे है, लेकिन फिर भी विश्व कविता और साहित्य से गंभीर परिचय के लिए अनुवाद ही एकमात्र माध्यम है। इस निर्भरता और मूल से अपरिचित पाठकीय विवशता के विश्व में किसी रचना का अनुवाद पूरी तरह बेहतर बन पड़ा है या नहीं, इसे जानने का एकमात्र आधार और शर्त शायद उसका संप्रेषणीय और पठनीय होना ही है। अनुवादक मूल से अनुवाद करते हुए, अपनी क्षमता और योग्यता भर—महज़ शाब्दिक होने से बचकर, भाव-रक्षा में संलग्न होते हुए—अनुवाद को मूल के समीप रखने की कोशिश करते हैं। अँग्रेज़ी से अनुवाद करते समय भी उनकी कोशिश रहती है कि हिंदी अनुवाद भरसक अँग्रेज़ी अनुवाद के निकटतम हो। इतने पर भी अनुवाद का अप्रिय होना अनुवादक की सीमा है, उसका दोष नहीं। एक अनुवादक का कार्य प्रत्येक भाषा और समाज में इसलिए सदा सार्थक, स्वागत-योग्य और प्रासंगिक बना रहेगा; क्योंकि वह अपरिचय को नष्ट कर नए परिचय संभव करता है। ‘तनाव’ में प्रकाशित काव्यानुवादों के तीनों खंडों की प्रासंगिकता, अनिवार्यता और उपयोगिता को भी इस संदर्भ में ही ग्रहण करना चाहिए।
•••
अन्य रविवासरीय : 3.0 यहाँ पढ़िए — गद्यरक्षाविषयक | पुष्पाविषयक | वसंतविषयक | पुस्तकविषयक | प्रकाशकविषयक | प्रशंसकविषयक | भगदड़विषयक | रविवासरीयविषयक | विकुशुविषयक | गोविंदाविषयक | मद्यविषयक | नयानगरविषयक | समीक्षाविषयक | बेलाविषयक
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
