कहानी : रिपोर्टर
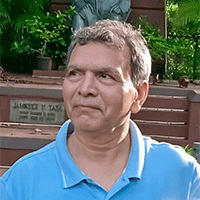 जयशंकर
07 नवम्बर 2025
जयशंकर
07 नवम्बर 2025

अक्टूबर आ गया। मौसम करवटें लेने लगा है। प्रभु अपना चश्मा खोज रहे हैं। रात में कहीं रखा गया था। चाय उबलकर देगची से बाहर निकलने लगी। प्रभु ने गैस बंद किया। सुबह-सुबह ही उनके मन में क्या-क्या आने लगा था? वह सब उनके जीवन में इतने पहले घटा था कि अब के जीवन में उन सबका ज़रा-सा भी महत्त्व नहीं रह गया था। प्रभु के मन में यह सवाल जागा ही था कि क्या कुछ ऐसा होता भी है कि जिसका महत्त्व जीवन भर बना रहता है? तभी चाय की देगची से उबाल उठने लगा। काली चाय का कत्थई उबाल।
“यह क्या है कि कभी अपना ही जिया गया इतनी ज़्यादा दूर खड़ा नज़र आने लगता है?
उनके भीतर यह सवाल उठा था। अक्टूबर शुरू ही हुआ है। सुबह सर्द होने लगी है। पंखों को कम गति पर रखना पड़ रहा है। गरम कपड़े बाहर निकल आए हैं। सुबह-सुबह अपने पुराने कोट को देखकर ही प्रभु के मन में बीस बरस पुराने अपने बस्तर के दिन लौटने लगे थे। उन दिनों वे रिपोर्टर थे।
जगदलपुर में बीते हुए अपने तीन बरस, जब वह रिपोर्टर की हैसियत से वहाँ गए थे। चालीस बरस के रहे होंगे। प्राइमरी स्कूल में जाती दो किशोरियों के पिता। तब पत्नी भी एक स्कूल में पढ़ा रही थी। माँ-बाप गुज़र गए थे। दादा-दादी भी। वह छत्तीसगढ़ में अकेले ही रहे। उनका परिवार महाराष्ट्र के एक शहर में, जो उनके बचपन का शहर रहा था।
प्रभु ने सोचा कि यह सब कैसे होता होगा कि आदमी का जन्म कहीं और होता है, वह नौकरी कहीं और करने लगता है, बीमार किसी दूसरे शहर में होता है और मरता किसी और ही जगह पर है। उनके पिता वैष्णो देवी में मरे थे। उनकी लाश को ट्रेन में लाया गया था। वह मंदिर की चढ़ाई चढ़ते वक़्त हार्ट अटैक का शिकार हुए थे। वह जाना ही नहीं चाह रहे थे। उनकी किसी ने भी नहीं मानी।
“क्या यह सब पहले से तय हो जाता होगा... पिता पहली बार इतनी दूर के लिए अपने घर से बाहर निकले थे... आख़िरी बार भी... जीवन भर अपनी स्टेशनरी की दुकान सम्हालते रहे थे।”
बिस्कुट का डिब्बा ख़ाली था। बिस्कुट का भूरा चूरा नज़र आ रहा था। शारदा के लिए लाना पड़ेगा। वह अपनी सुबह की दवाई चाय-बिस्कुट लेने के बाद ही लेती है। प्रभु ने हैंगर से शर्ट निकाला। मरीना मार्ट पड़ोस में ही था। इस वक़्त तक खुल ही जाता है। आकाशवाणी पर भूले-बिसरे गीत आ रहे थे। अमीरबाई कर्नाटकी का कोई गाना। उन्होंने बाहर से दरवाज़े को भिड़ा दिया। शारदा अपने कमरे में सो रही थी। इधर की कुछ दवाइयों से उनकी नींद देर से खुल रही है। सितंबर में ही उनकी पत्नी की सर्जरी हुई है। रिटायर हो जाने के दो बरसों के बाद।
प्रभु के मन में बस्तर के उन दिनों ने लौटना शुरू कर दिया है। वह ख़ुद को ऐसे हज़ारों लोगों के बीच में देख रहे थे, जिनकी ज़िंदगी में अभाव ही अभाव थे। वहाँ कच्ची सड़कें तक नहीं थीं। बहुत सारे ग्रामीणों के लिए न स्कूल, कॉलेज थे और न अस्पताल। लोग घंटों पैदल चलकर बाज़ार पहुँचते थे। इन लोगों के घरों में न बिजली थी और न ही नल से पानी आता था। वहाँ प्रभु ख़ुद को कितना ज़्यादा अमीर, सुखी और सौभाग्यशाली महसूस किया करते थे। उनके पास अपनी स्कूटर थी।
“तुम लोगों को पता ही नहीं कि हम कितनी ज़्यादा सुख-सुविधा के बीच में रह रहे हैं?” वह अपने शहरी दोस्तों से कहते।
“सवाल उनकी ज़िंदगी को सरल बनाने का तो है ही, लेकिन बड़ा सवाल उन पर हो रहे अन्यायों, अत्याचारों पर ध्यान दिलाने का भी होना चाहिए।”—उनका कोई दोस्त कहता।
“मुझे नहीं लगता है कि उनके बारे में बता देना ही काफ़ी होगा।”
“हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं।”
“आप सोचते हैं कि लोगों की कठिनाइयों को लोग जानते नहीं हैं... हमारी निगाहों में भी तो इतना कुछ आता रहता है... क्या हम कुछ ठोस क़दम नहीं उठा सकते हैं... ऐसा कुछ की कोई बदलाव आ सके... वहाँ कुछ लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं।”
“तुम्हारा अपना ध्यान अच्छी रिपोर्टिंग पर होना चाहिए... एक रिपोर्टर यही कर सकता है।” इतना कहकर घोष साहब अपनी कुर्सी से उठ जाते। वैसे भी उनको प्रभु से बात करना कठिन महसूस होता था। वह बूढ़े हो रहे थे। कभी कलकत्ता से आकर छत्तीसगढ़ के इस इलाक़े में बस गए होंगे। अब यहाँ उनका अपना मकान था। नाती-पोती वाले हो चुके थे। कभी प्रभु के जैसी सोच लिए रहे भी होंगे। अब उनको प्रभु का सोचना-समझना ज़रा-सा भी नहीं जँचता है। वह बीच-बीच में प्रभु को समझाते रहते हैं—“तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारा अपना परिवार भी है... इस इलाक़े में रिपोर्टिंग करना ख़तरों से ख़ाली नहीं है... हर पत्रकार पर पुलिस की निगरानी रहती है।”
घोष साहब का इस तरह का कुछ कहा जाना, इतना ज़्यादा डरा-डरा रहना, प्रभु को अखरता था। अपनी उम्र का चालीसवाँ पार ही किया था। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को, आपातकाल के समय देखे हुए बीस बरस भी नहीं हुए थे। अपने ख़ाली समय को सरकार और समाज व्यवस्था से असहमति जताते विचारों को पढ़ा करते थे। सत्ता पर सवाल खड़ा करती हुई कविताओं से उनका घना रिश्ता बन रहा था। प्रभु जान रहे थे कि उनके आस-पास बहुत कुछ ऐसा घट रहा है जो नहीं घटना चाहिए।
“हर बात की क़ीमत मामूली लोग ही क्यों चुकाते हैं?” प्रभु ख़ुद से सवाल करते रहते।
“दुनिया ऐसी ही रहती आई है... इस दुनिया को बदलना असंभव है... गांधी तक ज़्यादा कुछ नहीं बदल सके थे।”
“मैं बदलने की बात कहाँ कर रहा हूँ... मैं तो सिर्फ़ अन्याय को अन्याय कहने की बात कह रहा हूँ...”
यह अख़बार में चाय पीने के वक़्त की बातचीत हुआ करती थी। कभी-कभार गंभीर हो जाती लेकिन अक्सर हल्की-फुल्की, बेसिर पैर की उथली बातें हुआ करती थीं। प्रभु संकल्प लेते कि अब दुबारा कभी इन लोगों के बीच कोई गंभीर सवाल खड़ा नहीं करेंगे। कुछ दिनों तक अपनी चुप्पी साथ बनाए भी रखते लेकिन फिर अजीब-सा अकेलापन घेरने लगता। छोटी, पिछड़ी, नयी और अजनबी जगह थी। अख़बार में काम कर रहे लोगों के अलावा किसी को जानते-पहचानते नहीं थे। फिर रहना तो इनके बीच ही था। महीने में एक-दो दिनों के लिए ही अपने शहर और घर में लौट पाते थे।
“बेचैनियों से बचे रहना मुश्किल होता है”—पत्नी से कहते।
“इसे मैं बेचैनी नहीं बेबसी कहूँगी... बेचैन आदमी रास्ता निकालता है... तुम दस बरस से पत्रकार रहे हो... तुम्हें अपनी बात रखना आना चाहिए” शारदा बार-बार कहती थी। शारदा में साहस की कमी नहीं रही। जो मन में आता उसे कह सकती थी, कहना जानती थी। शारदा को प्रभु का नर्वस बने रहना कभी समझ में नहीं आया था।
“अपनी बात अच्छी तरह रखना पड़ता है... अपनी बात पर गहरा भरोसा रहना चाहिए... मजबूत विश्वास ही कुछ कर सकता है।”
“वह सुनना ही नहीं चाहते हैं।”
“यह कहने से काम नहीं चलता है... फिर तो दुनिया कभी नहीं बदलेगी।”
“दूसरों को समझाना हमेशा से ही मुश्किल रहता आया है... हर कोई थक ही जाता है।”
“फिर भी समझाने वाले लोग आते रहे हैं... गांधी नहीं आए थे?”
प्रभु को अपनी पत्नी की बातें अर्थपूर्ण नज़र आती थीं। वह कभी भी तर्क के लिए तर्क करती नज़र आती थी। कई बार यह होता कि वह चुप रह जाती। उसे अपनी सीमाओं का ध्यान आ जाता। प्रभु अपनी सीमाओं को भूल जाते। उन इलाक़ों में भी बहस करने लगते जिनके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं रहता था।
यह इलाक़ा उनके अपने पारिवारिक जीवन का था। वहाँ दो-दो लड़कियाँ बड़ी होती जा रही थीं। दोनों ही बेटियों का किशोर जीवन समाप्त हो चुका था। सिर्फ़ उनकी माँ ही उनकी जवानी के शुरुआती दिनों की मन:स्थितियों को समझना चाहती रही थी। प्रभु बीच-बीच में आते ज़रूर थे, लेकिन अपनी बेटियो के संग अपना ज़्यादा वक़्त नहीं गुज़ारते थे। अपने शहर में आने के बाद का उनका ज़्यादातर वक़्त परिवार में नहीं, प्रेस क्लब में बीतता था। वहाँ पर प्रभु बीयर, कॉफ़ी या चाय के संग घंटों अपने पत्रकार दोस्तों के साथ बने रहते थे। ये सब लोग उनके पुराने दोस्त थे।
“तुम्हें थोड़ा समय अपनी बेटियों को भी देना चाहिए... अब ये जवान होने लगी हैं...।”
“तुम तो हो... फिर तुम टीचर भी हो... उनको तुमसे कितना कुछ मिल सकता है... मैं उन्हें क्या बता सकता हूँ?”
“तुम पिता हो... उनके लिए तुम्हारी जगह बिल्कुल अलग है... वह जगह मैं कभी नहीं ले सकती हूँ... बच्चों के लिए पिता कुछ और ही होते हैं।”
“मेरी बस्तर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नीरस रहती है... वहाँ ढंग से बात करने के लिए तरसता रहता हूँ... यहीं कुछ लोगों से संवाद हो पाता है...।”
जगदलपुर छोटी-सी ही जगह थी। शुरुआत में प्रभु वहाँ अपनी जड़े जमा नहीं पा रहे थे। वहाँ अपना दोनों वक़्त का खाना ख़ुद तैयार करते थे। कपड़े और बर्तन का काम भी उनका ही था। पुरानी जीप से इधर-उधर रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता था। न जाने का कोई तयशुदा वक़्त रहता और न ही लौटने का। घर में अकेले ही रहते थे, इसीलिए किसी औरत को घर में काम के लिए रखने में हिचकते रहते थे। उनके स्वभाव के कारण अख़बार के ज़्यादातर लोग उनसे दूर-दूर ही बने रहते। प्रभु किसी की चापलूसी नहीं कर सकते थे। दूसरों से हमेशा सहमत होते रहना उनको आया ही नहीं था। उनके संपादक घोष साहब पर संपादक होने का नशा छाया रहता था।
“हमारा काम तथ्यों को बाहर ले आना है... उनको छिपाना नहीं है...” प्रभु अपनी बात पर अड़ जाते।
“हम यह सब छाप न सकेंगे” घोष साहब कहते।
“नाम तो मेरा रहेगा... आप क्यों डर रहे हैं... मैनेजमेंट से मैं बात करूँगा।”
“हमें अख़बार चलाना है... बारह लोगों की रोज़ी-रोटी इस अख़बार से जुड़ी है।”
“मेरी भी तो नौकरी है..”
“आपकी बात अलग है… मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ... आपको अपनी रिपोर्ट को बदलना पड़ेगा।”
प्रभु को इतनी मेहनत और लगन से बनी रिपोर्ट को अख़बार में जगह न मिलने की बात से निराशा मिलती थी। धीरे-धीरे उनसे रिपोर्टिंग का काम वापस लिया जा रहा था। जो लोग स्टील प्लांट के लिए जगह लेना चाह रहे थे, उनके राजनैतिक रिश्ते बहुत मज़बूत थे। अख़बार ऐसे लोगों से अपने संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता था। इसीलिए प्लांट के खड़े होने के विरोध में हो रही गतिविधियों की ख़बरें रोकी जाने लगी थीं। स्थानीय लोगों की विरोध की आवाज़ों को दबाया जा रहा था।
“अब सब तरफ़ यही हो रहा है” कोई साथी पत्रकार कहता।
“मैं यह सब नहीं सह सकूँगा।”
“तब तुम्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा।”
“यह मुझे मंजूर होगा...।”
इस तरह कुछ दिनों के बाद प्रभु ने अपना इस्तीफ़ा सौंप दिया था। दूसरे अख़बारों ने भी उनको काम नहीं दिया। इधर कुछ किताबों के अनुवाद का काम कर रहे हैं। अँग्रेज़ी में लिखी जा रही कुछ पॉपुलर क़िस्म की किताबों के अनुवाद में उनका मन कम ही लगता है। वह इस बात को भी एक तरह का समझौता ही समझते हैं, लेकिन अपने इस चुनाव को पत्रकार बने रहने से बेहतर महसूस करते हैं। यहाँ पर उनकी आत्मा उन्हें उतना धिक्कारती नहीं है। कम से कम यहाँ वह किसी अन्याय, किसी अत्याचार के होने में अपना साथ नहीं दे रहे हैं। जगदलपुर का जीवन साफ़-सुथरा महसूस नहीं हो रहा था। उनकी समझ में आने लगा है कि देर-सबेर इस माहौल के आने का अनुमान उनके साथ रहने ही लगा था। देश और दुनिया में आज़ादी पर ख़तरा मंडराने ही लगा था। बाज़ार की ताक़त बहुत ज़्यादा बढ़ने ही लगी थी। कभी-कभार बड़ी बेटी कहती है—“आपके अकेले ऐसे होने से क्या हो जाएगा... यहाँ हर कोई पैसा कमाना चाह रहा है।”
“यह मैं नहीं जानता... लेकिन मैं सच को झूठ नहीं कह सकता हूँ।”
“आप अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अपने आपको बहलाना चाहते हैं...।”
प्रभु जानते हैं कि यह उनकी बड़ी बेटी का नहीं, उनकी पत्नी का वाक्य है। इस वाक्य को वह बरसों से सुनते आ रहे हैं। उनकी दाम्पत्य ज़िंदगी की शुरुआत में ही उनकी पत्नी ने उनसे अध्यापन की तरफ़ बढ़ने की बात कही थी। वह अपने ही स्कूल में उनके लिए बात करना चाह रही थी। अध्यापक हो जाने के बाद ट्रेनिंग का कोर्स संभव हो जाता और वह अपने ही शहर में अध्यापक की हैसियत से बने रह सकते थे।
“मैंने पत्रकारिता को अपना बहुत सारा समय दिया है... मेरी इसमें रुचि है... मैं कभी भी अच्छा टीचर नहीं बन सकूँगा... यह ख़ुद को छलना रहेगा।”
“इससे क्या फ़र्क़ पड़ जाएगा?” पत्नी झल्ला जाती थी।
“मुझे पड़ता है।”
तब वे दोनों ही पच्चीस-छब्बीस के रहे होंगे। दोनों के पास ही धीरज की गहरी कमी थी। प्रभु के भीतर की बौद्धिक जिज्ञासाएँ पकने लगी थीं। वे अपने कम्फ़र्ट जोन से बाहर निकलना चाहते थे। एक ही बच्ची जन्मी थी और उसकी देखभाल उसके दादा-दादी कर सकते थे। प्रभु रायपुर आ गए। अँग्रेज़ी दैनिक था। बरसों से वहाँ का संस्करण निकल रहा था। शहर भी ठीक-ठाक था। बीच-बीच में अपने शहर में भी आ जाते। उनके शुरुआती दस बरस अच्छे ही रहे। स्थानीय ख़बरों को तैयार करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ प्रवास के अपने शुरुआती दिनों में ही प्रभु को आदिवासियों की ज़िंदगी का संघर्ष समझ में आने लगा था। वह पहली बार जान रहे थे कि उनके जीवन में सिर्फ़ संगीत, नृत्य, सादगी और शराब नहीं, तरह-तरह के संघर्ष हैं, उन पर होते तरह-तरह के अन्याय और अत्याचार हैं। प्रभु के मन में रची-बसी आदिवासियों के जीवन की रोमांटिक छवि टूटने-बिखरने लगी थी। रायपुर के आस-पास के जंगलों और खदानों में मज़दूरों, किसानों और आदिवासियों का जल, जंगल और जमीन का संघर्ष बढ़ता जा रहा था। प्रभु यह सब देख रहे थे। अपने इस तरह के अहसासों और अनुभवों के चलते ही उन्होंने बस्तर जाने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। वहाँ जाने के लिए कम लोग ही तैयार रहते थे। पत्नी ने भी अपनी असहमति जताई थी। उनका बीच-बीच में अपने शहर लौटना मुश्किल होता गया था। जगदलपुर से रायपुर आने में ही घंटों लग जाते। फिर वहाँ से अपने शहर तक आना और समय माँगता था।
जब प्रभु बस्तर में रहने लगे, तब वहाँ उनके रिपोर्टर ने बहुत गहराई से जानना शुरू किया था कि आज़ादी के चालीस बरसों के बाद भी, उनका देश कहाँ खड़ा है, किस तरह खड़ा है, खड़ा भी है या लड़खड़ा रहा है। वहाँ उनका लोगों से मिलना-जुलना शुरू हुआ। कुछ लोग बाहर से आकर उस इलाक़े के आदिवासियों के बीच काम भी कर रहे थे। उनमें डॉक्टर और अध्यापक थे। लेखक, पत्रकार और राजनैतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग भी। वहाँ पर स्टील प्लांट के खड़े किए जाने का विरोध और आंदोलन चल रहा था। स्थानीय लोग विरोध में शामिल हो रहे थे। कुछ दिन ठीक-ठाक बीते लेकिन बाद में प्रभु पहले मलेरिया और बाद में टाइफाइड के शिकार हो गए। खाने-पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उनकी जगह कोई रिपोर्टर वहाँ जाने से कतराता भी रहता था। घर में अपनी बीमारी की बात बताना नहीं चाहते थे। किसी तरह अपने सहकर्मियों की मदद से अपनी रिपोर्ट तैयार करते रहे थे। ऐसे वक़्त में वहीं के कुछ पढ़े-लिखे लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा मदद की थी। प्रभु स्वस्थ हो गए और इन लोगों के बीच ही उठने-बैठने लगे। इनमें ही कुछ लोग बस्तर को बरसों से जानते आए थे। इन लोगों को बस्तर की सच्चाइयों का पता था।
“यहाँ की सच्ची ख़बरें कौन लिखता है?”
“इतने अख़बार निकलते हैं?” प्रभु जवाब देते।
“उन अख़बारों का इनकी ज़िंदगी की सच्चाइयों से कोई लेना-देना नहीं रहता है... इनकी तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हैं।”
“और हमारा अख़बार?”
“आपके अख़बार के मालिकों की ही यहाँ स्टील प्लांट खड़े किए जाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है।”
“आप उन लोगों को जानते हैं?”
“कभी यहाँ के कुछ पत्रकार हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे... उनमें से कुछ लोग आपके अख़बार में अभी भी काम कर रहे हैं”—डॉक्टर कह रहे थे।
“आप घोष साहब की बात कर रहे हैं?”
“आप समझ गए... उनके जगदलपुर के बंगले में कभी गए हैं?”
धीरे-धीरे प्रभु उस इलाक़े के अंतर्विरोधों, विरोधाभासों को जानने-समझने लगे थे। पूरी दुनिया की निगाहें बस्तर के घने जंगलों, वहाँ की खनिज संपदा पर ठहरने लगी थी। बस्तर से ढेर सारा पैसा बनाया जा सकता था। प्रभु की समझ में आने लगा था कि जो दिखता है, वही यथार्थ नहीं होता है। यथार्थ की कई-कई परतें हो सकती हैं। वह कहीं-कहीं प्याज के छिलकों की तरह, एक के बाद एक निकलता चला जाता है।
अब प्रभु की निगाहें बस्तर के जनजीवन को और अच्छी तरह, गंभीरता लिए हुए देखने लगी थीं।
“इनके साथ छल किया गया है... हज़ारों बरसों से ये जंगलों को सम्हालते आए हैं... ये जंगल इनके ही हैं”—औरतों की डॉक्टर ने कहा था।
“आप यहाँ कैसे आईं?”
“इसी इलाक़े की एक लड़की हमारे शहर के नर्सिंग होम में मरी थी... बच्चे को जन्म देने के बाद उसका ख़ून बहना बंद ही नहीं हो रहा था।”
“यह कब की बात होगी?”
“पाँच बरस पहले... तभी मैंने और मेरे डॉक्टर पति ने यहाँ प्रैक्टिस करने का मन बनाया था।”
“वह यहीं प्रैक्टिस करते हैं?”
“वह गाँवों में घूमते हैं... मैं नर्सिंग होम सम्हालती हूँ... हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं।”
यह सब जानना प्रभु के लिए तसल्ली का सबब बनता गया था। वह डॉक्टर दम्पत्ति के घर जाने लगे थे। उनकी कुछ शामें उनके घर और नर्सिंग होम में कटने लगी थी। डॉक्टर दम्पत्ति लगभग पाँच बरसों से उस इलाक़े को देखते आ रहे थे।
शुरू-शरू में प्रभु के लिए यह जानना कठिन रहा कि उस इलाक़े के पढ़े-लिखे लोगों पर पुलिस महकमे की निगरानी बनी रहती थी। खुफ़िया विभाग का एक आदमी उनका भी पीछा करता रहता था। आस-पास में एक कोयला खदान के मज़दूर संगठित हो रहे थे, हड़ताल कर रहे थे। उसकी रिपोर्टिंग के वक़्त ही एक आदमी ने प्रभु से तरह-तरह के सवाल पूछना शुरू कर दिया था।
“यहाँ नक्सलवाद पनप रहा है” खुफ़िया विभाग के आदमी ने कहा था।
“वे लोग यहाँ क्यों आएँगे... यह इलाक़ा इतना ज़्यादा कटा हुआ है।”
“कलकत्ता यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है... वे लोग पूरे देश में फैल रहे हैं।”
नक्सलवाद का तो नहीं, लेकिन प्रभु को यह पता चलता जा रहा था कि उस इलाक़े में बेरोज़गारी बढ़ती जा रही थी, खेती के हाल बुरे थे, मामूली लोगों पर ज़िंदगी का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। जंगलों की अवैध कटाई जारी थी।
“ग़रीबी आती नहीं है बल्कि वह कभी जाती ही नहीं”—डॉक्टर के यहाँ आते एक युवक ने कहा था।
उन दिनों में ही प्रभु महीने भर की छुट्टियाँ लिए हुए, अपने शहर आए थे। बड़ी बेटी की कबड्डी खेलते हुए हड्डी टूट गई थी। उसे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। मार्च-अप्रैल के दिन थे। इम्तिहानों के दिन। उनकी पत्नी को स्कूल से छुट्टियाँ मिलना मुश्किल था। प्रभु भी पहली बार इतनी छुट्टियाँ मुश्किल से ही ले पाए थे।
पर जब छुट्टियों के बाद अपनी नौकरी पर लौटे तब तक दफ़्तर में काफ़ी कुछ बदल गया था। अब उनको रिपोर्टर का नहीं, सहायक संपादक का ज़िम्मा निभाना था। दफ़्तर में ही रहते हुए तरह-तरह की संपादकीय ज़िम्मेवारियाँ निभाना। पहले-पहले उनको लगा कि यह सब उनकी अनुपस्थिति में किया गया कोई कामचलाऊ फैसला होगा, लेकिन घोष साहब ने बताया कि अब उनका विभाग बदल दिया गया है।
“आपकी आख़िरी रिपोर्टिंग पर मैंनेजमेंट नाराज़ थी”—एक सहकर्मी ने बताया था।
“लेकिन मज़दूरों पर लाठीचार्ज किया गया था... मैं ख़ुद अस्पताल में तीन-तीन घायल मज़दूरों से मिला था।”
“आपकी रिपोर्ट छपी ही नहीं थी।”
“यह सब घोष साहब की करतूत होगी... मुझे उनकी नियत पर शक हो रहा है।”
“और किसकी करतूत हो सकती है?”
“मैं उनसे बात करूँगा।”
“कोई फ़ायदा नहीं है... उनकी मुख्यमंत्री तक पहुँच है... विधायक उनेक घर आते रहते हैं...।”
प्रभु धीरे-धीरे इस सच्चाई को जान रहे थे। इस बात पर भी अगर वह लड़ते हैं तो उन्हें अख़बार से बाहर निकलकर लड़ना होगा। अख़बार में वह अकेले पड़ गए थे। बाहर से उनको अपनी लड़ाई में मदद मिल सकती थी। ट्रेड यूनियन से जुड़े कुछ लोग उनके साथ आ सकते थे। कुछ और लोग भी थे जो उनके साथ सहानुभूति महसूस कर रहे थे। पर नौकरी के बिना प्रभु वहाँ कैसे रह सकते थे? शहर में बेटियाँ बड़ी हो रही थीं। उनकी पढ़ाई-लिखाई के ख़र्चों में इज़ाफ़ा हुआ था। माता-पिता की मौत के बाद उनकी पेंशन का आना बंद हो चुका था। घर किराये से लिया गया था। पत्नी प्राइमरी की टीचर थी और प्राइमरी स्कूल को सरकारी ग्रांट नहीं मिलती थी। वैसे भी उनकी पत्नी, उनकी दोनों बेटियाँ उनके अपने शहर में न होने से बहुत सारी परेशानियों को झेल ही रहे थे। उनका अपना ही नहीं, उनके परिवार का जीवन भी जटिल, कठिन होता गया था। बड़ी बेटी पैसों के लिए प्राइमरी के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी थी।
धीरे-धीरे प्रभु को अपने आस-पास की परिस्थितियों को देखकर आने वाला ग़ुस्सा, हमेशा बना रहता तनाव, अपने लिखे गए से किसी सच को बाहर ले आने की आकांक्षा धुँधली पड़ती गई। बस्तर में नौकरी से इस्तीफ़ा देने के बाद के तीन महीने जैसे-तैसे बीत ही गए। उन दिनों में अपमानित होते रहे। अपनी छोटी-छोटी भूलों के लिए अपने सीनियर लोगों का ग़ुस्सा झेलते रहे। अपने प्रवास में बस्तर की जिन जगहों ने तसल्ली दी थी, वहीं जाते हुए, डॉक्टर दम्पत्ति के घर में, बस्तर क्लब के क़रीब की पब्लिक लाइब्रेरी में अपना वक़्त बीताते रहे थे।
प्रभु के लिए अपनी ही ज़िंदगी के वे दिन, बीस बरसों के बाद, किसी और की ज़िंदगी के दिनों में बदल गए हैं। यह होता है। जीवन का कोई भी इम्प्रेशन हमेशा ही साथ बना नहीं रह सकता। ज़िंदगी का बड़ा से बड़ा अनुभव, एक वक़्त के बाद धुँधला और मैला हो ही जाता है। प्रभु अपने घर की छोटी-सी बाल्कनी से, सप्तपर्णी के पेड़ों पर लद आए फूलों की तरफ़ देख रहे हैं। अब बहुत से फूल झर गए हैं। सितंबर के अंत-अंत तक इन फूलों की बहार थी।
प्रभु का बचपन भी इसी इलाक़े में बीता था। बरसों से इस इलाक़े, इन रास्तों को जानते आए हैं। बहुत-बहुत पहले, सर्दियों की शुरुआत के दिनों में, सप्तपर्णी के पेड़ों की इन कतारों के नीचे से गुज़रना, उनके नीचे गिरे हुए फूलों की वजह से, एक प्यारा-सा अनुभव हुआ करता था। यह भी सर्दियों की शुरुआत के ही दिन हैं, लेकिन न अब उतने फूल बाहर आते हैं और न ही उनके नीचे से गुज़रने पर कोई विस्मय, कोई लालसा बाहर आती है। क्या यह उनकी उम्र की वजह से हुआ है?
सप्तपर्णी से सुबह के अपने इस वक़्त में प्रभु को कॉलेज के दिनों की अपनी शांति निकेतन की यात्रा की याद आ रही है। वहीं पहली बार प्रभु ने इस पेड़ को जाना और पहचाना था।
प्रभु सोच रहे हैं कि धीरे-धीरे कितना कुछ बदल जाता है, पीछे चला जाता है, गुम जाता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं। बीच-बीच में, कभी-कभार वही सब कुछ बाहर भी आ जाता है।
शारदा जगी होती तो प्रभु इस बात को उनसे साझा कर सकते थे। शारदा अभी भी सो ही रही थी। रेडियो पर सुबह के समाचार आ रहे थे। वह अभी भी देश-विदेश के समाचारों को ध्यान से सुनते हैं। अभी भी उनकी दुनिया की राजनीति में दिलचस्पी ज़रा-सी भी बुझी नहीं है। इधर-उधर के अख़बारों को कभी घर में, कभी पब्लिक लाइब्रेरी में जाकर पढ़ते रहते हैं।
दोनों बेटियों के विवाह हो चुके हैं। छोटी इसी शहर में रहती है। बीच-बीच में अपने घर आ जाती है। अपने पिता के लिए कविता की कोई किताब, कोई पत्रिका या अख़बार लाती रहती है। उनकी पत्नी को उतना नहीं, लेकिन दोनों ही बेटियों को अपने पिता का अब रिपोर्टर न होना अखरता रहता है। यह बात उन दोनों को ही सालती रहती है कि अपनी जीविका के लिए प्रभु को घटिया उपन्यासों तक के अनुवाद करने पड़ते हैं।
अब प्रभु पहले की तरह अपने पत्रकार मित्रों से बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते हैं। अनुवाद का काम उनका काफी वक़्त ले लेता है। इधर घर का पूरा खर्च प्रभु के कमाने से ही चल रहा है। शारदा को पेंशन नहीं मिलती है। वह इधर बीमार भी रहने लगी है। अभी भी शारदा को लगता ही रहता है कि अगर प्रभु पत्रकार की जगह, अध्यापक हो जाते तो उन सबकी ज़िंदगी कुछ और ही हो सकती थी, कुछ और ज़्यादा बेहतर, कुछ और ज़्यादा सहनीय और सुंदर हो सकती थी। प्रभु पहले भी अपनी पत्नी से इस बात पर अपनी असहमति जताते रहे थे, आज भी जताते हैं। अब भी उनके भीतर कोई स्वप्न, भले ही कभी-कभार अगर जागता है तो वह एक अच्छा रिपोर्टर होने का स्वप्न ही होता है। एक अच्छा रिपोर्टर, जो दुर्भाग्यवश वह बन नहीं सके थे, बनते-बनते रह गए थे और अब शायद वह कभी रिपोर्टर बन भी नहीं सकेंगे।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
