जीम अब्बासी के उपन्यास ‘सिंधु’ के बारे में
 अर्जुमंद आरा
22 नवम्बर 2024
अर्जुमंद आरा
22 नवम्बर 2024
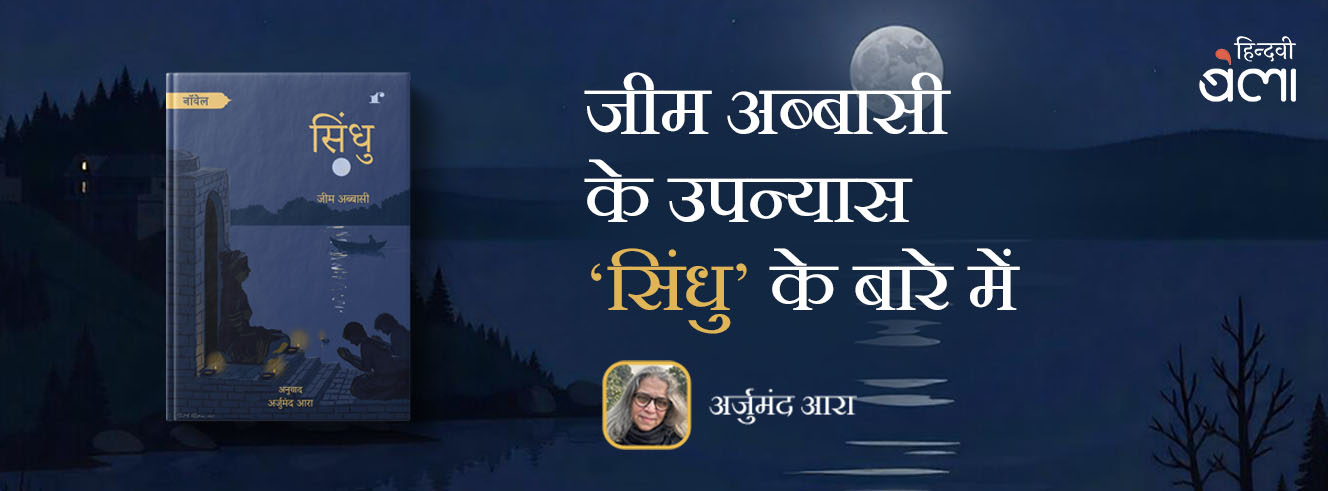
जीम अब्बासी सिंध (पाकिस्तान) के समकालीन लेखक हैं, जिन्होंने कुछ वर्ष पहले ही उर्दू में लिखना शुरू किया है। एक कहानी संग्रह ‘ज़र्द हथेली और दूसरी कहानियाँ’(2020), और दो उपन्यास ‘रक़्स-नामा’ (2023) और ‘सिंधु’ (2024) प्रकाशित हुए हैं। इस लघु उपन्यास में उन्होंने सिंधु घाटी में पनपने वाली सभ्यता को अपनी कल्पनाशक्ति से जीवन दिया है। एक प्राचीन कालखंड पर, और वह भी अत्यंत प्राचीन काल के ऐसे पहलू पर लिखना जिसके रहस्यों से बहुत कम पर्दा हटा है, उपन्यास को कोरी कल्पना पर आधारित कहानी या एक जटिल और नीरस रचना बना सकता था, लेकिन ‘सिंधु’ की कहानी का ताना-बाना लेखक ने सहज ढंग से बहुत क़ायल करने वाले अंदाज़ में ऐतिहासिक तथ्यों के इर्द-गिर्द बुना है।
सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता के विषय में जो कुछ भी साक्ष्यों और तथ्यों के रूप में मिला है तथा पुरातत्वशास्त्रियों और इतिहासकारों ने जिसका ब्योरा हम तक पहुँचाया है—वह अपने-आप में दिलचस्प है और कौतूहल को बढ़ाता है; लेकिन कोई रचनाकार उनके वर्णन में क्या-क्या छिपा हुआ देख और पढ़ सकता है, यह अगर समझना हो तो ‘सिंधु’ को ज़रूर पढ़ना चाहिए।
इस उपन्यास की एक बड़ी ख़ूबी यह है कि लेखक ने हड़प्पा और मोअनजो-दड़ो (लोकप्रिय नाम ‘मोहनजोदड़ो’) के उपलब्ध ऐतिहासिक साक्ष्यों से अवांछित आज़ादी नहीं ली है। सिंधु के तटीय क्षेत्र में पनपने वाले सामाजिक जीवन (रहन-सहन, परंपराएँ) और रोज़गार (खेती-बाड़ी, ईंट-भट्टे) आदि का आपस में तार्किक संबंध है। खुदाई में मिलने वाली मुहरों, बर्तनों, मूर्तियों आदि के आधार पर इस इलाक़े की मान्यताओं, रीति-रिवाज और सामाजिक और प्रारंभिक राजनैतिक व्यवस्थाओं की एक दिलकश और मोहक दुनिया इस उपन्यास में उकेरी गई है।
व्यवस्था मातृसत्तात्मक दर्शाई गई है जो ज़रा चौंकाती है, लेकिन अविश्वसनीय नहीं लगती। दक्षिणी भारत और उत्तर-पूर्व के इलाक़ों की संस्कृतियों से विषय में तो यह पढ़ा था कि यहाँ आज भी ऐसी परंपराएँ और रीति-रिवाज मौजूद हैं, जो एक प्राचीन मातृसत्तात्मक व्यवस्था के गवाह हैं, लेकिन कभी इस पर विचार नहीं किया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी नारी-केंद्रित निज़ाम पनपा होगा या पनप सकता था।
ख़ैर जब मैंने ‘सिंधु’ में पढ़ा तो ध्यान में आया कि नर्तकी की सुप्रसिद्ध मूर्ति और औरतों और लड़कियों की दीगर मूर्तियाँ उस समाज में नारी के महत्त्व को यक़ीनन नुमायाँ करती हैं, और हज़ारों की संख्या में मिलने वाली लिंग और योनि की आकृतियों के आधार पर भी ऐसा प्रतीकात्मक कथानक रचा जा सकता है, जिसमें औरत-मर्द की समानता या नारी वर्चस्व को अहमियत दी गई हो।
इसी कालखंड की अन्य सभ्यताएँ (नील के डेल्टा में मिस्र की तहज़ीब दजला-फ़रात के साहिलों पर सुमेरियाई तहज़ीब) भी इसकी पुष्टि करती हैं कि उनकी पौराणिक कथाओं, भित्ति-चित्रों और मूर्तियों आदि से यह स्पष्ट है कि उनके सामाजिक जीवन में भी औरत हरगिज़ कमतर नहीं थी; और न वैसी तुच्छ और निरादर थी जो वह वैश्विक सभ्यता के विकास के साथ भोग की वस्तु के रूप में परिवर्तित होती गई। इसलिए ‘सिंधु’ में औरत के किरदार को जिस तरह केंद्र में रखा गया—वह भी कल्पना मात्र नहीं कहा जा सकता। खुदाई में मिलने वाली नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति को अब्बासी ने क़बीले की मुखिया माता नाओड़ी के रूप में कल्पित किया है।
जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता में धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक जीवन और रीति-रिवाज की बात है तो ज़ाहिर है कि उनका लेखा-जोखा नहीं मिलता इसलिए एक रचनाकार उनका चित्रण प्रकृति के साथ इंसान के रिश्तों पर आधारित कर सकता है, यानी प्रकृति की शक्तियों पर मानव की निर्भरता और टकराव के रिश्तों से ही यह कहानी विकसित कर सकता है, और ‘सिंधु’ में जीम अब्बासी ने इस पहलू को भी ख़ूबी से निभाया है। उन्होंने प्राचीन मुहरों पर मिले पीपल और दोसिंघे (गाय/बैल प्रजाति) के नक़्श को उपन्यास के कथानक में नुमायाँ स्थान दिया है, जिससे हम तुरत वह रिश्ता देख लेते हैं जो आज भी हिंदुस्तान की धार्मिक मान्यताओं में पीपल, नंदी और पशुपति की उपासना के रूप में मौजूद है।
खुदाई में हज़ारों की संख्या में लिंग और योनि की आकृतियाँ मिली हैं, जो प्रजनन और सृष्टि के प्रतीक हैं, जिससे ज़ेहन में आता है कि कालांतर में सृष्टि और सृजन के प्रतीक के तौर पर शिवलिंग की पूजा की परंपरा इन साक्ष्यों से असंबद्ध नहीं हो सकती। अलबत्ता योनि की पूजा इतिहास के किस अज्ञात पड़ाव पर त्याग दी गई (असम में कामाख्या मंदिर अपवाद है), कहना मुश्किल है। ऐसा ग़ालिबन पितृसत्तात्मक व्यवस्था के मज़बूत होने के साथ हुआ होगा। खुदाई में इन प्रतीकों के मिलने से यह ख़याल गुज़रता है कि यह सभ्यता वास्तव में एक निरंतर जारी सभ्यता है, और किसी कालखंड में पूर्णतया नष्ट नहीं हुई।
उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों की खुदाइयों में मिलने वाले पुरातत्वीय साक्ष्यों से अंदाज़ा होता है कि अस्ल में जिसको हम सिंधु घाटी की तहज़ीब कहते हैं—उसका कोई एक सीमित प्रांतीय अस्तित्व नहीं बल्कि यह एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है जो दूर-दूर तक फैला हुआ है; और चूँकि प्रारंभिक निशान सिंध में मिले इसलिए ‘सिंधु घाटी की सभ्यता’ के नाम से पहचानी गई।
बाद में बहुत-सी तहज़ीबों का इस महान् सभ्यता में मेल-जोल, मिश्रण और विलय हुआ लेकिन अपनी जड़ों में (धार्मिक मान्यताओं, रीति-रिवाज, संस्कार, परंपराओं के रूप में) यह आज भी पुरानी पहचान से जुड़ी है। बस इतना ही हुआ कि कुछ तो प्राकृतिक और कुछ मानव रचित तबाहियों के सबब कुछ-न-कुछ इलाक़े उजड़ते रहे, नए बसते रहे, आबादी पलायन और स्थानांतरण करती रही, वग़ैरह-वग़ैरह। यह संभावनाएँ प्राकृतिक भी हैं और तार्किक भी। ऐसी ही एक संभावना का सिरा पकड़कर उपन्यासकार जीम अब्बासी ने भी एक बस्ती/इलाक़े के सामाजिक जीवन और फिर उसके उजड़ने की कहानी की रचना की है।
‘सिंधु’ का एक दिलचस्प उल्लेख वह लगा जब लेखक ने सिंध की रिवायती चादर ‘अजरक’ के निशान इस प्राचीन सभ्यता में तलाश किए। खुदाई में मिलने वाली मुखिया, पुजारी या राजा की मूर्ति के शरीर पर लिपटी हुई चादर पर तीन पत्तियों वाले फूल बने हैं। लेखक ने इसे सिंध की पारंपरिक चादर ‘अजरक’ के प्रारंभिक नमूने के तौर पर देखा है, जो सिंध की स्थानीयता के साथ इतिहास के जुड़ाव की दिलचस्प कल्पना है। इससे अंदाज़ा होता है कि लेखक का इस तहज़ीब की निरंतरता पर आग्रह है। मुझे भी उसकी कल्पना पर बिलकुल ऐतराज़ नहीं, बल्कि यह उपन्यास को दिलकश ही बना रही है। हो सकता है कि कल को ऐसी कड़ियाँ मिल जाएँ जो छपाई और रंगों की इस कला के किसी चरण को इस प्रागैतिहासिक काल से मिला दें, बिल्कुल वैसे-ही-जैसे बाद के दौर में पीपल और पशुपति की उपासना का रिश्ता प्राचीन मुहरों से जुड़ता है।
बहरहाल, एक बुज़ुर्ग या मुखिया की यह मूर्ति उस इलाक़े की तहज़ीब का निहायत अहम प्रतीक है, जिसके आस-पास एक स्पष्ट सामाजिक और राजनैतिक या धर्म-केंद्रित व्यवस्था रची जा सकती थी। और यह एक सामने का और क़ायल करने वाले कथानक बन सकता था, लेकिन जीम अब्बासी ने यह आसान राह नहीं चुनी, बल्कि उन्होंने किसी भी प्रकार के विकसित निज़ाम को परिचित कराने से गुरेज़ किया है। वह परिवार, समाज, धर्म/आस्था और अर्थव्यवस्था को प्रारंभिक चरणों में पेश करते हैं।
विकास के इन चरणों को उपन्यासकार ने गतिशील रखा है और उनमें बदलाव की प्रक्रिया को व्यक्तिगत और गिरोही स्वार्थों के टकराव, तथा एक सत्ता की सिमटती हुई बिसात और दूसरी बिसात के बिछने के इशारे दे कर शामिल किया है। ये काम तलवार की धार पर चलने जैसा था और लेखक बख़ूबी इससे गुज़र गया है। मातृसत्ता से पितृसत्ता की तरफ़ प्रस्थान को उसने बहुत अच्छे ढंग से उपन्यास के अंतिम हिस्से में शामिल करते हुए पितृसत्ता के प्रतीक पात्र को तीन-पत्ती के फूल वाली चादर से सुशोभित कर के उसका रिश्ता इतिहास से जोड़ दिया है।
आख़िरी बात उपन्यास की भाषा के संबंध में कहना चाहती हूँ। एक पुरानी कहानी किसी भी भाषा में सुनाई जाए, उसकी आधुनिकता को पुरातनता में नहीं बदला जा सकता। एक क़दीम तहज़ीब को, जो विकास के काफ़ी शुरुआती दौर में है, आख़िर एक विकसित और आधुनिक ज़बान में बयान करने के लिए कौन-सा तरीक़ा अपनाया जा सकता था? उस प्राचीनता का एहसास कराने, और हमें आज की ज़िंदगी से काटकर एक पुरातन द्वीप में ले जाने के लिए जीम अब्बासी ने भाषा को गोया एक नाव की तरह प्रयोग किया है।
भाषा की कश्ती पर सवार होकर पाठक इतिहास के दरिया में उतरता है और उसका मल्लाह, यानी हमारा लेखक उसे ‘सिंधु’ के टापू पर छोड़ आता है कि जाओ अब जी भर कर सैर करो! भाषा की यह कश्ती पुरातन ही लगनी चाहिए; और उतनी ही अजनबी भी कि हम अपनी जानी-पहचानी दुनिया से ख़ुद को कहीं दूर महसूस कर सकें। इसके लिए जीम अब्बासी ने पात्रों और जगहों के नाम ऐसे रखे हैं जो हिंदी उर्दू भाषी पाठकों के लिए अजनबी हैं। फिर वे पात्र गुफ़्तुगू में कुछ ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं जिनकी संरचना वर्तमान उर्दू-हिंदी मुहावरे और वाक्य विन्यास से अलग हैं। वाक्य-संरचना का यह स्ट्रोक वो चप्पू है जो नाव को एक ख़ास रफ़्तार से द्वीप के निकट करता जाता है।
तीसरा औज़ार कल्पित प्राचीन जीवन शैली और विचार-तंत्र को उपन्यास की बुनत में शामिल करना है, जो आज के नगरीय परिवेश में पले-बढ़े पाठक को तुरंत ही एक प्राचीन और अनोखी दुनिया में पहुँचा देता है। और इस तरह ख़ास शब्दवाली और वाक्य-विन्यास की मदद से अजनबियत का चोला पहनाई गई भाषा में, और एक प्राचीन जीवन शैली और विचार-तंत्र के मिश्रण से जीम अब्बासी ने एक ऐसा संसार रचा है जिसकी नींव ऐतिहासिक साक्ष्यों और तथ्यों पर खड़ी की गई है। ऐसा दिलकश और जादुई उपन्यास तोहफ़े में देने के लिए जीम अब्बासी का शुक्रिया।
ज़ीशान साहिल की नज़्म ‘मोअनजो-दड़ो’ (मोहनजोदड़ो) की कुछ पंक्तियों के साथ, जिनमें अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त देखती हूँ, अपनी बात ख़त्म करती हूँ :
पुरानी बस्तियाँ दरयाफ़्त करने वाले कहते हैं
किसी ज़माने में ये शहर दरियाई बंदरगाह था
इसे देखने वालों का ख़याल है
बारिश में ये शहर अब भी बहुत ख़ूबसूरत लगता है
मैंने ये शहर नहीं देखा
मगर मुझे लगता है जैसे मैं इसी शहर में रहता हूँ।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
