हिमाचल के दुर्लभ कठार और पेछियों के ख़ाली पेट
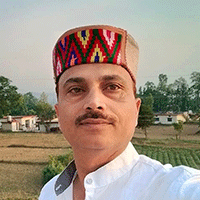 अनंत आलोक
02 सितम्बर 2024
अनंत आलोक
02 सितम्बर 2024

हिमाचली गाँवों में एक समय था, जब पेछियों के पेट साल भरे-भरे रहते थे। उस समय जब कोई बच्चा ज़्यादा खाता था—तो उसे एक विशेषण से नवाज़ा जाता था कि इसका पेट तो पेछी है, जो कभी भरता ही नहीं। आज यह विशेषण भी बेमानी लगते हैं। पेछी क्या होती है—इसके लिए चलते हैं एक सफ़र पर। हाँ, इतिहास के उस सफ़र पर जहाँ पोड़ा है, कोठड़ी है, और भी न जाने क्या-क्या रोमांचकारी वस्तुएँ स्थितियाँ और स्थान हैं।
कविता-कहानी-ग़ज़ल से कुछ फ़ुर्सत मिली तो एक योजना बनी कि इतिहास की सैर पर निकला जाए। देश में लॉकडाउन लगा था और बाहर निकलना बंद था, लेकिन हमारा मन, ऐसा वाहन है जो ख़ुद ही वाहन भी है और सवार भी। बस इसी मनरूपी वाहन पर सवार होकर निकल पड़ा इतिहास की सैर पर। मन के एक कोने में लगे जालों के आवरण हटाए तो कुछ वस्तुएँ सामने आईं। कुछ और परतें हटाते गए, और पिछले सारे अनुभवों के पोड़ों-कोठड़ियों के द्वार खुलते गए।
आप सोच रहे होंगे यह पोड़ा-कोठड़ी क्या बला है? सही सोच रहे हैं आप—आज की तारीख़ में ये चीज़ें अब बहुत कम देखने में आती हैं। गाँव-गाँव में नए आलिशान मकान बन गए हैं, इन्हीं मकानों में बन गए हैं ख़ूबसूरत, आधुनिक साज-सज्जा से सुसज्जित बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम। कमाल देखिए न, हमने नए मकान बनाने के साथ-साथ उनके नाम भी आयातित ही रख लिए हैं। ऐसे मकान विदेशों में बनते हैं और हमने यहाँ अपने देश में बनाए तो उनके नाम भी अँग्रेज़ी। क्या अपने नाम भी नहीं दे सकते हैं हम अपने मकानों को?
पोड़ा पुराने समय की बैठक होती थी और उसके अंदर कोठड़ी यानि स्टोररूम हुआ करता था। मैं और मेरा मन इस विचार के भीतर और भीतर चलते गए और सब कुछ ज्यों किसी फ़िल्म की भाँति सामने आता गया।
गाँव की इन पोड़ा-कोठड़ियों के द्वार लाँघते ही सबसे पहले एक पोड़ा आया। बाहर जूते उतारकर हम भीतर दाख़िल हुए तो सामने ही कठार, दीवार की पीठ से पीठ सटाए खड़ा था। मैंने उसकी बक्खी और छाती पर ऐसे मुक्का मारा जैसे जिगरी यार कई दिनों के बाद मिलने पर एक-दूसरे को मारते हैं।
उसके दिल की धड़कन धक्-धक् कर रही थी। यानि वह अंदर से भरा पड़ा था, ख़ुशहाल, अनाज से भरा-पूरा। कठार के दो पेट थे। एक में मक्की और दूसरे में गेहूँ। वैसे तो किसी कठार की क़द-काठी पर निर्भर करता है कि उसमें कितना अनाज आएगा लेकिन मेरे सामने जो कठार था उस में कम-से-कम दस बोरियाँ अनाज तो आराम से आ जाता। यानि दोनों ख़ानों में दस क्विंटल अनाज होगा।
कठार घनाभ के आकार का होता है, जिसमें खेर, शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके सिर के ऊपर इसी के आकार के ढक्कन रहते हैं, जिन्हें पूरा खोलकर ऊपर से अनाज आराम से डाला जा सके। चार पड़े पायों पर चार खड़े पाये रहते हैं, जिनके बीच में आवश्यकता अनुसार खड़ी-पड़ी फ़्रेम्स रहती हैं। उन फ़्रेम्स के बीच में डिज़ाइनदार दिल्ले—जैसे पुराने दरवाज़ों में—लगे रहते हैं। हाथ से बने ख़ूबसूरत नक़्क़ाशी के सुंदर दिल्ले, ऐसे लगे रहते हैं जैसे दरवाज़े के पल्लों पर छोटे-छोटे दरवाज़े लगा दिए हों।
अनाज बाहर निकालने के लिए दोनों ख़ानों के एकदम नीचे, उसके पाँव के पास ऐसे खाँचे बने रहते हैं—जैसे पोस्ट-बॉक्स के नीचे चिट्ठियाँ निकालने के लिए | इन पर लकड़ी का ही एक छोटा-सा शटर लगा रहता है, जिसे ऊपर-नीचे सरकाकर खोला और बंद किया जा सकता है। इस शटर का आकर इतना होता है जिसमें आराम से हाथ अंदर जा सके और अनाज कहीं अंदर जम जाए या अड़ जाए तो बाजू डालकर या फिर लकड़ी के किसी डंडे की मदद से अनाज निकाला जा सके। मैंने शटर खोला तो मक्की के दाने यूँ बाहर आने लगे ज्यों स्वर्ण मोतियों की कोई थेली फट गई हो।
कठार में साल भर के लिए अनाज सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके शिल्प की एक और ख़ासियत है कि इसको कीलों से जोड़ा नहीं जाता बल्कि इस के हर भाग में जोड़ के लिए खाँचे बने होते हैं। इन खाँचों के अंदर ही हर भाग को फ़िट किया जाता है और ज़रूरत पड़ने पर आराम से खोलकर अलग-अलग किया जा सकता है।
इसमें केवल दो स्थानों पर ही कील का प्रयोग होता है। पहला—तो उस छोटे से शटर में खाँचों को जोड़ने के लिए, जबकि वहाँ भी कई मिस्त्री स्वयं बाँस की कीलें बनाकर प्रयोग करते हैं। दूसरा—इसके ऊपर लगे भारी भरकम ढक्कन को क़ब्ज़ों के साथ जोड़ने के लिए, अन्य किसी भी जगह कील का इस्तेमाल नहीं होता।
हम अंदर कोठरी में गए तो दो-तीन छोटी-बड़ी पेछियाँ कोनों में बैठी नज़र आईं। सबके सिर पर टोपियाँ लगी थी। हू-ब-हू ऐसी टोपियाँ जैसी असम के लोग किसी त्यौहार विशेष पर पहनकर नाचते हैं। बस अंतर इतना भर कि असम के लोगों की टोपियाँ सर से कुछ बाहर की ओर फैली रहती हैं, जबकि इनकी टोपियाँ एकदम कनपटी पर फ़िट बैठी हुई थी। मैंने इनकी कमर पर हाथ रखा तो एकदम सुडौल काया, कहीं से दब नहीं रही थी। इनकी टोपियाँ उतारकर देखी, सब गले तक अनाज से भरी पड़ी थीं।
हिमाचल के गाँवों में पहले इतना अनाज होता ही था कि साल भर, पेट भर खाने के बाद भी बचा रहता था। कहीं-कहीं तो अभी भी होता है और इतना कि प्रतिदिन घर की महिलाएँ दो जनों की रोटियाँ अतिरिक्त बनाकर रखती थीं। क्या पता कब-कौन भूला-भटका, भूखा-प्यासा आ जाय। कोई गाँव का ही जन बैठने आ गया और हम रोटी खा रहे हैं तो उसे भी रोटी ज़रूर दी जाती थी। बल्कि दी जाती है, गाँव में आज भी। जी भरकर खाने और खिलाने के बाद भी नई फ़सल आने तक पिछला अनाज बचा रहता था।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे पेछियों की। पेछी यानि एकदम गोल-मटोल फूले पेट वाली बाँस की बुनी हुई—कुई। कुई यानि कुएँ की पत्नी। कुआँ तो बड़ा होता है, वह छोटी होती है। लेकिन इतनी छोटी भी नहीं कि उसके अंदर इतनी जगह न रहे कि उसमें दो जन आराम से समा जाएँ।
कठार पुल्लिंग में आता है तो पेछी स्त्रीलिंग में आती है। इसीलिए कभी-कभी अधिक वजन वाले पुरुषों को कठार और स्त्रियों को पेछी की संज्ञा दी जाती थी गाँव में। पेछी बनाने का कार्य वही लोग करते थे जो बाँस की टोकरियाँ, किल्टा, छाबड़ी आदि बनाते हैं।
बस पेछी के लिए बाँस बहुत लगता है। एक पेछी में कम से दस किल्टों का बाँस लग जाया करता है, और शायद ज़्यादा भी। अब आप जो नहीं जानते सोच रहे होंगे यह किल्टा क्या होता है? किल्टा बाँस का एक ऐसा बड़ा पात्र है, जिससे गोबर उठा कर खेतों में डाला जाता है। यह हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर यानि लगभग हर पहाड़ी इलाक़े में होता है। इसे पीठ पर उठाया जाता है।
आपने टेलीविजन पर देखा होगा कि असम की महिलाएँ अपनी पीठ पर किल्टा उठाये चाय की पत्तियाँ तोड़ती हैं। ये आकार में कुछ छोटे होते हैं, क्योंकि महिलाएँ इतना ही भार उठा सकती हैं। पुरुषों के लिए बड़े आकार के किल्ते, घिल्ले होते हैं, जिसमें कम से कम पचास किलोग्राम गोबर तो आ ही जाता है। हालाँकि हिमाचल के अधिकतर गाँवों में महिलाएँ भी यही किल्टे उठा लेती हैं।
नेपाल में खेती-बाड़ी का काम क्योंकि अधिकतर महिलाएँ ही करती हैं। उनके मर्द लोग दूर देशों में जाकर काम करते हैं, तो वहाँ भी महिलाएँ अपनी पीठ पर किल्टे उठाए देखी जा सकती हैं। हिमाचल में इसे कई स्थानों पर घिल्ला भी कहा जाता है।
विकास एक दरिया की भाँति होता है। वह अपने साथ कुछ सुविधाएँ बहा लाता है तो कुछ को बहाकर ले भी जाता है। विकास का दरिया जिधर से गुज़रता है, वहाँ बदलाव होना तो स्वाभाविक है।
यह परंपरागत साधनों, सुविधाओं और संस्कृति के रूप-स्वरूप को अपनी धारा में बहाकर कहीं ज़मींदोज़ कर देता है, तो वहीं कुछ नई परम्पराएँ, सुख-सुविधाएँ, संसाधन रीति-रिवाज़ों को स्थापित भी करता है। जिस प्रकार पुरातन संस्कृति धीरे-धीरे कहीं खो जाती है, उसी प्रकार जो सुख-सुविधाएँ, जो वस्तुएँ, जो संस्कृति आज है वह भी कल नहीं होगी।
सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मानव ही—एक ऐसा प्राणी है जो निरंतर आगे की बात सोचता है, यानि वह विकास चाहता है। पशु-पक्षी ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि वे मनुष्य की तरह सभ्य नहीं है। उनकी अपनी अलग सभ्यता, अलग संस्कृति है। वे बदलते समय के साथ ख़ुद को समायोजित करते हैं। परंपराओं, संस्कृति को बदलने का सामर्थ्य उनमें नहीं है।
भारत देश कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी हमारे देश में इतना अनाज पैदा होता है कि सब के लिए भरपेट भोजन मिल जाय। यह बात अलग है कि उचित प्रबंधन के अभाव में लोग भूख से मर भी जाते हैं। लाखों टन अनाज मूषक उदर पूर्ति करने के बाद भी निर्यात किया जाता है। अनाज भंडारण के जिन परंपरागत साधनों की हमने ऊपर बात की वे आज भी बहुत से घरों में मौजूद हैं।
इस यात्रा में बहुत से संस्कृतिकर्मी, लेखक और समाज-सेवक हमें मिले, जिनमें राजू वैदिक, राजू फागड़ी, तारा चंद, कमलेंद्र सिंह और सोलन से अनीता शर्मा ने इस शोध-आलेख में चित्र और जानकारी उपलब्ध करवाएँ। इन सबके सहयोग से कठारों की कुछ तस्वीरें प्राप्त हुईं, जो आने वाले समय में शायद ही देखने को मिले। इनमें से कुछ लोगों के अपने घर पर ये कठार हैं और कुछ ने गाँव के किसी अन्य घरों से ये तस्वीरें पाठकों और शोधार्थियों के लिए उपलब्ध करवाई हैं। उत्तराखंड से शिवदीप सिंह प्रखर ने बताया कि इसे कोठला, बखार, बखारी भी कहते हैं।
समय के पाँव तले धीरे-धीरे ये सब परंपराएँ और चीज़ें मानों कुचली जा रही हैं। आने वाले समय में न तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी और न ही इन के बारे में कोई जानकारी रखने वाला ही मिलेगा। केवल तस्वीरों में ही इनके दर्शन हो पाएँगे वह भी तब अगर इनकी तस्वीरों और जानकारियों को हम आज कहीं लिखकर या संरक्षित करके रख देते हैं।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट

