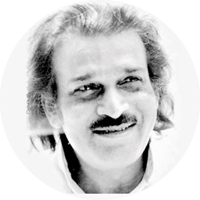फिर बाढ़ आ गई होगी उस नदी में
पास का फुटहिया बाज़ार बह गया होगा,
पेड़ की शाखों में बँधे खटोले पर
बैठे होंगे बच्चे किसी काछी के
और नीचे कीचड़ में खड़े होंगे चौपाए
पूँछ से मक्खियाँ उड़ाते।
मेरी निगाह कुछ कमज़ोर हो गई है।
दिल्ली की सड़कें दिखती हैं जैसे कुआनो नदी—
नदी जो एक कुएँ से निकली है
जिसे मैं अपने बचपन में
कभी खोज निकालने का उत्साह रखता था।
कुआनो नदी—
सँकरी, नीली, शांत
अभी भी बहती रहती है रात-दिन मेरे सामने
अदेखे को पाने का उत्साह कुरेदती हुई।
बरसात में अपना पाट चौगुना करती
आस-पास के गाँवों को डुबाती
शहर की ऊँची सड़क के
दोनों ओर की नीची ज़मीन को
हरहराते नाले-सा बनाती।
अभी भी मैं एक लंबी शहतीर
अपने घर के दालान से सड़क तक रखकर
वह हरहराता जल पार कर जाता हूँ
जब कि मेरे पिता जाँघ तक धोती उठाए
पानी को हलकोरते आते हैं
कलल-कल, कलल-कल
ज्यों ही आने लगती है अँधेरे में आवाज़
मैं लालटेन लेकर बाहर दौड़ता हूँ
शायद यह रोशनी काम आ जाए।
मछलियाँ, जोंक, पनियल साँप
सबके अलग-अलग ढंग हैं पानी में चलने के
मैं आज भी उनका गवाह हूँ
बड़े ध्यान से मैंने देखा है उन्हें।
पीले-पीले मेढकों की छपाक से ही
मैं बता सकता हूँ पानी यहाँ कितना गहरा है
और बरसात ख़त्म होने पर
इसे सूखने में कितने दिन लगेंगे।
बादल झमाझम बरस रहे हैं
या बरस कर निकल गए हैं
या बरसने के लिए घिघिया रहे हैं
कुआनो नदी वैसी ही पसरी रहती है
हर समय मेरी आँखों के सामने।
बहुत ग़रीब ज़िला है वह बस्ती—
जहाँ मैंने इसे पहली बार देखा था।
मेरे नाना इस नदी में कूद पड़े थे
और निकाल लिए गए थे
ज़िंदगी से ऊब कर मर नहीं सके।
तट पर न रेत थी न सीपियाँ
सख़्त कँकरीली ज़मीन थी काई लगी,
कहीं-कहीं दलदल था, झाड़ियाँ थीं दूर तक
जिनमें सोते कुलबुलाते रहते थे
और चिड़ियाँ एक टहनी से दूसरी टहनी पर
शोर करती झूलती रहती थीं।
बहुत सँभलकर मैं जब भी जाता हूँ
नरसल की हरी छड़ियाँ काटकर लाता हूँ
उनसे लिखने की क़लमें बनाता हूँ
दूसरे उनसे पिपिहरी भी बना लेते हैं
जिसे बड़े शान से बाँसुरी कहते हैं,
उन पिपिहरियों की आवाज़
आज भी सुनाई देती है मुझे
दिल्ली की इन सड़कों पर।
यह नदी मुर्दघाट के लिए मशहूर है।
कुआनो जाने का मतलब
किसी को फूँकने जाना है।
मेरे पिता को हर शव-यात्रा में जाने का शौक़ था।
अक्सर वह आधी-आधी रात लौटते
और लकड़ियाँ गीली होने की शिकायत करते।
माँ से कहते—''कुछ लोग अभागे होते हैं,
उनकी चिता ठीक से नहीं जलती''
और हर अभागे की यही आख़िरी कहानी
मैं आज भी सुनाता हूँ।
इस नदी के किनारे
कोई मेला नहीं लगाता।
न ही पूर्णिमा-स्नान होते हैं।
एक मंदिर है
जो बहुत कम खुलता है
जिसकी सीढ़ियाँ
अहदियों के बैठने के काम आती हैं।
मैं अक्सर वहाँ बैठा रहता हूँ
और दालान के कोने में
टूटा, जाला लगा चमड़े का
एक बहुत पुराना बड़ा ढोल टँगा
देखता रहता हूँ जो अब बजता नहीं
और तेज़ हवा में
खड़खड़ाते विशाल झीने पीपल के पेड़ से
दैवी स्पर्श की तरह
किसी जालीदाप पीले पत्ते के अपने ऊपर
गिरने की प्रतीक्षा करता रहता हूँ।
पुल पर—
दही के मटके लिए एक-एक बार अहीरों को
जाते देखता हूँ
वे सब शहर में दही बेचकर गाँव लौटते होते हैं
कभी-कभी किसी के सिर पर लकड़ियों
के बोझ भी होते हैं
या गठरियाँ, ख़रीदे-सौदे-सुलुफ़ की
उनकी परछाइयाँ शांत हरे जल पर अच्छी लगती हैं।
तट से लगा हुआ एक बाँध है
जिस पर ऊँचे-ऊँचे छायेदार दरख़्त हैं।
जिनके नीचे से सड़क जाती है
कई तीखे घुमाव लेती,
सड़क पर अधिकतर बैलगाड़ियाँ चलती हैं
कभी-कभी कोई एक्का भी
पर्दा बाँधे, औरतों-बच्चों को बैठाए डगमगाता,
और फिर एक सायकिल धूल से भरी हुई,
भेड़-बकरियों के गल्ले,
नए ख़रीदे रँगे सींगों वाले बैल घंटियाँ बजाते
जिनकी आवाज़ धीरे-धीरे दूर होती जाती है।
पीला-पीला सूरज आसमान में डूबता है—
और तभी एक तेज़ नारी-कंठ सुनाई देता है—
‘लाली हो लाली’
और सड़क पर, पुल पर, पेड़ों पर अँधेरा छा जाता है।
मेरी निगाह कुछ कमज़ोर हो गई है।
इस नदी का
इस शहर से कोई संबंध नहीं है।
फिर भी नदी शहर की है।
इसको कोई पियरी नहीं चढ़ाता
न आदमी रामनामी डाले
सुबह तड़के भागते दिखाई देते हैं,
न अधेड़ औरतें ठाकुर जी का
सिंहासन लिए बतियाती जाती हैं।
दूधवाले पानी मिलाने
या प्राइमरी स्कूल के शिक्षक निवृत्त होने
अवश्य यहाँ रुकते हैं
और बंदर शाखों से उतर कर
इसके किनारे बैठे रहते हैं।
धूप में शहर की गंदगी
यहाँ साफ़ होती है
धोबी कपड़े धोते हैं,
आवारा औरतें सिगरेट पीती
गुनगुनाती-लिपटती
अपने ग्राहकों के साथ घूमती हैं।
रात में अक्सर क़त्ल होते हैं
लाशें कई-कई दिनों की पाई जाती हैं।
किसी स्त्री का फेंका हुआ
नया जन्मा बच्चा
कभी ज़िंदा कभी मरा मिल जाता है।
शाम होते ही पुलिस
भारी टार्चों से रोशनी फेंकती
पुल पर गश्त लगाती है
और सियार हुआँ-हुआँ करते हैं।
चमगादड़ों के उड़ने से
शाखें खड़खड़ाती हैं
और किसी अकेली चिता की
आख़िरी लपटें, बड़े-बड़े दहकते
अंगारों की आँखों से देखती हैं,
ऊपर आसमान में तारे होते हैं
नीचे नदी चुपचाप बहती जाती है।
यह नदी कगारे नहीं काटती
अपना पाट नहीं बदलती
जैसे बहती थी वैसे बहाती है।
आज भी इसके किनारों के गाँवों में
सिंघाड़ों के तालों में
बड़े-बड़े मटके औंधाए
मैं खटिकों को नंग-धड़ंग पानी में घुसे
सिंघाड़े तोड़ते देखता हूँ।
और खटकिनों को तार-तार कपड़ों में
अपना पुष्ट युवा शरीर लिए
घर-घर हँसी और सिंघाड़े बेचते हुए,
लोहारों की धौकनी के सामने
घोड़े-सा मुँह लटकाए
खुरपी, कुदाल और नाल बनाते हुए,
बढ़इयों को ऐनक का शीशा
सूत से कान में बाँधे
बँसखट के पाये गढ़ते हुए,
और किसी बूढ़े फेरीवाले को
बिसातखाने का सामान गले में लटकाए
हर घर के सामने कमर झुकाए
झिक-झिक करते हुए।
बरसात का पानी
आज भी गाँवों में भरता है
बिना जगत के कुओं के भीतर चला जाता है।
आदमी और चौपाए
खरवा के घायल पैर की उँगलियाँ
और खुर लिए लँगड़ाते चलते हैं,
सुअर लोटते हैं,
पानी में बैठी औरतें खाना पकाती हैं
उनके चूल्हों में टीन की चादरें लगी होती हैं
नीचे पानी रहता है
ऊपर लकड़ियाँ धुआँ उगलती हैं
कभी-कभी लपट भी
जिससे अदहन खौल जाता है,
एक और कुत्ते हाँफते बैठे रहते हैं
और दूसरी ओर उनके बच्चे,
जिनकी आँखें अँधेरे में जलती
मिट्टी के तेल की ढिबरियों-सी दिखाई देती हैं।
ढिबरियाँ—जो शाम को केवल घंटे-भर के लिए जलती हैं
फिर रात-भर अँधेरा छाया रहता है,
यह अँधेरा हर दूसरे महीने
भरों के घरों में आग लगाने पर टूटता है
फूस के घर जलकर राख हो जाते हैं।
भर—जो मजूरी पूरी न पड़ने पर चोरी करते हैं
और एक-दूसरे पूरी न पड़ने पर चोरी करते हैं
और एक-दूसरे को दुश्मन मान
उनका घर जलाते रहते हैं
उनकी औरतें रात-दिन आपस में
झगड़ती हैं, गालियाँ देती हैं
अघुआती हैं, बेसुरी आवाज़ मे रोती हैं
और बच्चे नाक बहाते नंगे इधर-उधर
हर खुले दरवाज़े की ताक में घूमते हैं।
और इन सबके बीच
कुआनो निर्लिप्त भाव से बहती रहती है।
अपना पाट नहीं बदलती।
इस नदी ने मुझे अंधा कर दिया है
मुझे कुछ दिखाई नहीं देता
अपनी ही आकृति क्रूर-कठोर लगती है।
एक बंजर भूमि में
बढ़े हुए नाख़ून लिए मैं खड़ा हूँ
जैसे उनसे ही नई फ़सलें उगा लूँगा
जैसे उन्हीं के सहारे
नहरें खींचता
मैं उन खेतों में ले जाऊँगा
जहाँ काँसे की चूड़ियाँ खनकाती
औरतें मुँह अँधेरे दौरियाँ चलाती हैं
निराई और बोआई के गीत गाती हैं
और कटी हुई फ़सलों के बीच
पीली धोती अनवासे
एक साँवली लड़की दौड़ती हुई दिखाई देती है।
नाख़ून दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं
और ज़मीन उसी अनुपात से बंजर होती जा रही है
और नदी हर दिल में उसी रफ़्तार से शांत
हर विवशता का उपहास-सा करती।
अभी एक डाँगर बहता हुआ निकल गया
अभी एक आदमी बहता हुआ चला जाएगा
जिसकी लाश पर कौए बैठे होंगे
जिन्हें मैं अक्सर दिल्ली की इन सड़कों पर
उड़ता हुआ देखता हूँ
शायद ये हंस हो!
मेरी निगाह कुछ कमज़ोर हो गई है
कुआनो नदी
सँकरी, नीली, शांत
जाने कब होगी
अक्षितिज, लाल, उद्याम।
बहुत ग़रीब है यह धरती
जहाँ यह बहती है।
- पुस्तक : प्रतिनिधि कविताएँ (पृष्ठ 112)
- रचनाकार : सर्वेश्वरदयाल सक्सेना
- प्रकाशन : राजकमल प्रकाशन
- संस्करण : 1989
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi volutpat porttitor tortor, varius dignissim.
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.