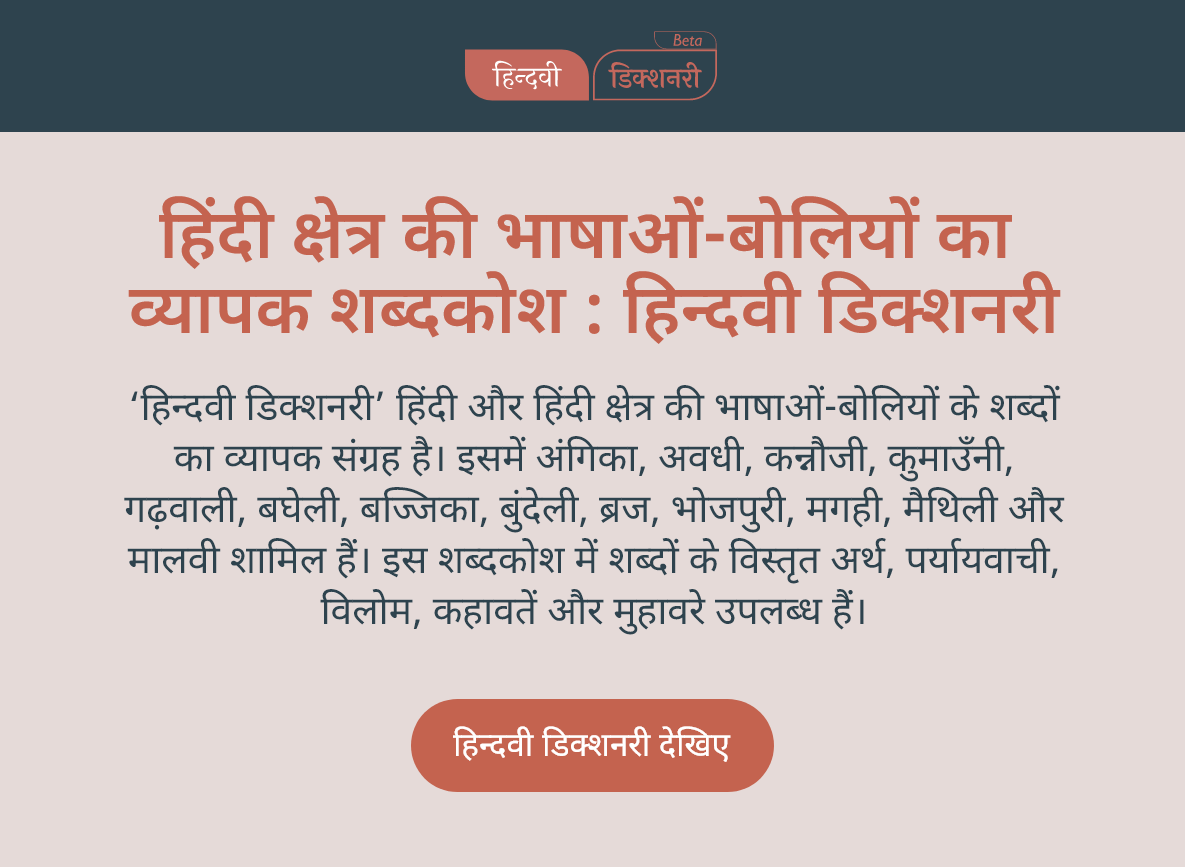मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है
manushy hi sahity ka lakshay hai
हजारीप्रसाद द्विवेदी
Hajariprasad Dwivedi

मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है
manushy hi sahity ka lakshay hai
Hajariprasad Dwivedi
हजारीप्रसाद द्विवेदी
और अधिकहजारीप्रसाद द्विवेदी
मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को परदु:ख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। मैं अनुभव करता हूँ कि हम लोग एक कठिन समय के भीतर से गुज़र रहे हैं। आज नाना भाँति के संकीर्ण स्वार्थों ने मनुष्य को कुछ ऐसा अंधा बना दिया है कि जाति-धर्म-निर्विशेष मनुष्य के हित की बात सोचना असंभव सा हो गया है। ऐसा लग रहा है कि किसी विकट दुर्भाग्य के इंगित पर दलगत स्वार्थ से प्रेम ने मनुष्यता को दबोच लिया है। दुनिया छोटे-छोटे संकीर्ण स्वार्थों के आधार पर अनेक दलों में विभक्त हो गई है। अपने दल के बाहर का आदमी संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। उसके रोने-गाने तक पर असदुद्देश्य का आरोप किया जाता है। उसके तप और सत्य-निष्ठा का मज़ाक उड़ाया जाता है। उसके प्रत्येक त्याग और बलिदान के कार्य में भी ‘चाल’ का संधान पाया जाता है और अपने-अपने दलों में ऐसा करने वाला सफल नेता भी मान लिया जाता है; परंतु मेरा विश्वास है कि ऐसा करने वाला आदमी सबसे पहले अपना ही अहित करता है। बड़े-बड़े राष्ट्रनायक जब अपनी विराट अनुचरवाहिनी के साथ इस प्रकार का गंदा प्रचार करते हैं, तो ऊपर-ऊपर से चाहे जितनी भी सफलता उनके पक्ष में आती हुई क्यों न दिखाई दे, इतिहास विधाता का निष्ठुर नियम-प्रवाह भीतर-ही-भीतर उनके स्वार्थों का उन्मूलन करता रहता है। इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों और राष्ट्रों की चिताभूमि को कुचलता हुआ आगे बढ़ रहा है, फिर भी गंदे तरीक़े सुधारे नहीं गए हैं, बल्कि उनको और भी कौशलपूर्ण और प्रभावशाली बनाया जाता रहा है। जो लोग दृष्टा हैं, वे इस ग़लती को समझते हैं; पर उनकी बात मदमत्त व्यक्तियों की ऊँची गद्दियों तक नहीं पहुँच पाती। संसार में अच्छी बात कहने वालों की कमी नहीं है, परंतु मनुष्य के सामाजिक संगठन में ही कहीं कुछ ऐसा बड़ा दोष है, जो मनुष्य को अच्छी बात सुनने और समझने से रोक रहा है। आज की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि अच्छी बात कैसे कही जाए, बल्कि यह है कि अच्छी बात को सुनने और मानने के लिए मनुष्य को तैयार कैसे किया जाए?
इसीलिए साहित्यकार आज केवल कल्पनाविलासी बनकर नहीं रह सकता। शताब्दियों का दीर्घ अनुभव यह बताता है कि उत्तम साहित्य की सृष्टि करना ही सबसे बड़ी बात नहीं है। संपूर्ण समाज को इस प्रकार सचेतन बना देना परमावश्यक है, जो उस उत्तम रचना को अपने जीवन में उतार सके। साहित्यिक सभाएँ यह कार्य कर सकती हैं। संपूर्ण जनसमाज को उत्तम साहित्य सुनाने का माध्यम बना सकती हैं। इस विशाल देश में शिक्षा की मात्रा बहुत ही कम है। जिन देशों में शिक्षा की समस्या हल हो चुकी है, उनके साहित्यिकों की अपेक्षा यहाँ के साहित्यिकों की ज़िम्मेदारी कहीं अधिक है। फिर हमने जिस भाषा के साहित्य-भंडार को भरने का व्रत लिया है, उसका महत्त्व और भी अधिक है। वह भारतवर्ष के केंद्रीय प्रदेशों की भाषा है, कई करोड़ आदमियों की ज्ञानपिपासा उसे शांत करनी है। इसलिए उसे संपूर्ण ज्ञान-विज्ञान का वाहन बनाना है।
हम लोग जब हिंदी की ‘सेवा’ करने की बात सोचते हैं, तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव-समाज की सेवा, जिसके विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आपके लिए लिखा जाता है, उसकी क्या क़ीमत है, मैं नहीं कह सकता; परंतु जो साहित्य मनुष्य-समाज को रोग-शोक, दारिद्रय-अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। उसी महत्त्वपूर्ण साहित्य को हम अपनी भाषा में ले आना चाहते हैं। मैं मनुष्य की इस अतुलनीय शक्ति पर विश्वास करता हूँ कि हम अपनी भाषा और साहित्य के द्वारा इस विषम परिस्थिति को बदल सकेंगे।
परंतु हमें सावधानी से सोचना होगा कि हिंदी बोलने वाला जनसमुदाय क्या वस्तु है और वास्तव में वह परिस्थिति क्या है, जिसे हम बदलना चाहते हैं। काल्पनिक प्रेत को घूँसा मारना बुद्धिमानी का काम नहीं है। नगरों और गाँवों में फैला हुआ, सैकड़ों जातियों और संप्रदायों में विभक्त, अशिक्षा, दारिद्रय और रोग से पीड़ित मानव-समाज आपके सामने उपस्थित है। भाषा और साहित्य की समस्या वस्तुतः उन्हीं की समस्या है। क्यों ये इतने दीन-दलित हैं? शताब्दियों की सामाजिक, मानसिक और आध्यात्मिक ग़ुलामी के भार से दबे हुए ये मनुष्य ही भाषा के प्रश्न हैं और संस्कृति तथा साहित्य की कसौटी हैं। जब कभी आप किसी विकट प्रश्न के समाधान का प्रयत्न कर रहे हों तो इन्हें सीधे देखें। अमेरिका में या जापान में ये समस्याएँ कैसे हल हुई हैं, यह कम सोचें; किंतु असल में ये हैं क्या और किस या किन कारणों से ये ऐसे हो गए हैं, इसी को अधिक सोचें। बड़े-बड़े विचारकों ने इस देश के जनसमुदाय के अध्ययन का प्रयत्न किया है, अब भी कर रहे हैं; पर ये अध्ययन या तो इन्हें अच्छी प्रजा बनाने के उद्देश्य से किए गए हैं या वैज्ञानिक कुतूहल-निवारण के उद्देश्य से। इनको इस दृष्टि से देखना अभी बाक़ी है कि वे मनुष्य कैसे बनाए जाएँ। हमारी भाषा, हमारा साहित्य, हमारी राजनीति—सब कुछ का उद्देश्य यही हो सकता है कि इनको दुर्गतियों से बचाकर किस प्रकार मनुष्यता के आसन पर बैठाया जाए।
हमारा यह देश जातिभेद का देश है। करोड़ों मनुष्य अकारण अपमान के शिकार हैं। निरंतर दुर्व्यवहार पाते रहने के कारण उनके अपने मन में हीनता की गाँठ पड़ गई है। यह गाँठ जब तक नहीं निकल जाती तब एक भारतवर्ष की आत्मा सुखी नहीं रह सकती। कर्म का फल मिलता ही है। इससे बचने का उपाय नहीं है। जिन लोगों को अकारण अपमान के बंधन में डालकर हमने अपमानित किया है, वे लोग सारे संसार में हमारे अपमान के कारण बने हैं।
हमें सावधानी से उनकी वर्तमान अवस्था का कारण खोजना होगा। ये अनादिकाल से हीन नहीं समझे जाते रहे हैं। नाना प्रकार की ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण परंपरा के भीतर से गुज़र कर भारतवर्ष की सैकड़ों जातियों वाला समाज तैयार हुआ है। इस शतच्छिद्र कलश में आध्यात्मिक रस टिक नहीं सकता। आजकल हम लोग को हिंदू-मुसलमानों की मिलन-समस्या से बुरी तरह चिंतित हैं। निःसंदेह यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। इस महान प्रश्न ने हमारे समस्त जीवन को गंभीरतापूर्वक विचारने के लिए चुनौती दी है। हम अपनी भाषा के क्षेत्र में भी इस कठिन समस्या से हतबुद्धि हो रहे हैं। हमारे बड़े-बड़े विचारकों ने प्रत्येक क्षेत्र में सुलह करने का व्रत लिया है; परंतु मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी कठोर समस्या का सामना हमें हिंदू-हिंदू मिलन के लिए ही करना है। अशांति के चिह्न अभी से प्रकट होने लगे हैं। जब हम भाषा या साहित्य विषयक किसी प्रश्न का समाधान करने बैठें तो केवल वर्तमान पर दृष्टि निबद्ध रखने से हम घोखा खा सकते हैं। मुझे अपनी बुद्धि या दीर्घदर्शिता का गर्व नहीं है, लेकिन जो कुछ अनुभव करता हूँ, उसे ईमानदारी से प्रकट करने से शायद कुछ लाभ हो जाए, इसी आशा से ये बातें कह रहा हूँ। सैकड़ों व्यर्थ कल्पनाओं की भाँति ये अनंत वायुमंडल में विलीन हो जाएँगी। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यों-ज्यों हमारे देशवासियों में आत्मचेतना का संचार होता जाएगा, त्यों-त्यों हिंदू-समाज की भीतरी समस्याएँ उग्र रूप धारण करती जाएँगी। राजनीतिक बंधनों के दूर होते ही हमारी मानसिक या आध्यात्मिक ग़ुलामी का बंधन और भी कठोर प्रतीत होगा। दो-सौ वर्षों की राजनीतिक ग़ुलामी को तोड़ने में हमें जितना प्रयास करना पड़ा है, उससे कहीं अधिक प्रयास करना पड़ेगा इस सहस्त्राधिक वर्षों की सामाजिक और आध्यात्मिक ग़ुलामी की ज़ंजीरों को तोड़ने में।
कवि ने बहुत पहले सावधान किया है, “जिसे तुमने नीचे फेंक रखा है, वह तुम्हें नीचे से जकड़कर बाँध लेगा; जिसे पीछे डाल रखा है, वह पीछे खींचेगा। अज्ञान के अंधकार की आड़ में जिसे तुमने ढक रखा है, वह तुम्हारे समस्त मंगल को ढककर घोर व्यवधान की सृष्टि करेगा। हे मेरे दुर्भाग्य ग्रस्त देश! अपमान में तुम्हें समस्त अपमानितों के समान होना पड़ेगा।”
शताब्दियों के विकट अपमान की प्रतिक्रिया कठोर होगी। उसके लिए हमें तैयार होना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जब भाषा और साहित्य के मसले पर विचार किया जाता है तो इस तथ्य को बिल्कुल भुला दिया जाता है। हिंदूओं की अपनी भीतरी समस्याएँ भी हैं और उन भीतरी समस्याओं के लिए जो विचार-विनिमय हुए हैं या हो रहे हैं, वे नाना कारणों से संस्कृत-साहित्य से अधिक प्रभावित हुए हैं। वे किसी के प्रति घृणा या अदूरदर्शिता के कारण नहीं हुए हैं। छोटी कही जाने वाली जातियों में ऊपर उठने की आकांक्षा स्वाभाविक है और उसके लिए उनका संस्कृत-साहित्य की ओर झुकना भी अस्वाभाविक नहीं है। यदि संस्कृत बहुल भाषा के व्यवहार और समस्त जातियों के ब्राह्मण या क्षत्रिय कहे जाने से सात करोड़ आदमियों में अपने को हीन समझने की मनोवृत्ति कुछ कम होती है, तो ऐसा करना वांछनीय है या नहीं, यह मैं देश के नेताओं के विचारने के लिए छोड़ देता हूँ।
एक ज़माना था जब भाषा-विज्ञान और नृतत्त्व-शास्त्र की घनिष्ठ मैत्री में विश्वास किया जाता था। माना जाता था कि भाषा से नस्ल की पहचान होती है परंतु शीघ्र ही यह भ्रम टूट गया। देखा गया है कि ये दोनों शास्त्र एक-दूसरे के विरुद्ध गवाही देते हैं। भारतवर्ष भाषा-विज्ञान और नृतत्त्व-शास्त्र के कलह का सबसे बड़ा अखाड़ा सिद्ध हुआ है। वर्तमान हिंदू-समाज में एक-दो नहीं, बल्कि दर्ज़नों ऐसी जातियाँ हैं, जो अपनी मूल भाषाएँ भूल चुकी हैं और आर्यभाषा बोलती हैं। ब्राह्मण-प्रधान धर्म ने जातियों का कुछ इस प्रकार स्तर-विभाग स्वीकार किया है कि निम्न श्रेणी की जाति हमेशा अवसर पाने पर ऊँचे स्तर में जाने का प्रयत्न करती है। इस देश में जाने किस अनादिकाल से संस्कृत भाषा का प्राधान्य स्वीकार कर लिया गया है कि प्रत्येक नस्ल और फ़िर्के के लोग अपनी भाषा को संस्कृत श्रेणी की भाषा से बदलते रहे हैं। ग्रियर्सन ने अपने विशाल सर्वे में एक भी ऐसा मामला नहीं देखा, जहाँ आर्यभाषा—संस्कृत श्रेणी की भाषा—बोलने वाले किसी जनसमुदाय ने अन्य से अपनी भाषा बदली हो, यहाँ तक कि आर्यभाषा की एक बोली के बोलने वाले ने भी दूसरी बोली को स्वीकार नहीं किया है।
स्पष्ट है कि इस देश में संस्कृत-प्राधान्य कोई नई घटना नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि इस भाषा का सहारा लेकर जातियाँ ऊपर उठी हैं। मैं केवल उन तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूँ, जिनके आधार पर मेरी यह धारणा बनी है कि इस देश के करोड़ों मनुष्यों में आत्मचेतना भरने का काम बहुत दिन से संस्कृत भाषा करती आई है और आगे भी करती रहेगी, ऐसी संभावना है। यह न समझिए कि जो लोग संस्कृत बहुल भाषा का व्यवहार कर रहे हैं, वे किसी संप्रदाय के प्रति द्वेषवश और घृणावश करते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि ऐसी बेतुकी बातों पर भी आसानी से विश्वास कर लिया जाता है।
दीर्घकाल से ज्ञान के आलोक से वंचित इन मनुष्यों को हमें ज्ञान देना है। शताब्दियों से गौरव से हीन इन मनुष्यों में हमें आत्मगरिमा का संचार करना है। अकारण अपमानित इन मूक नर-कंकालों को हमें वाणी देनी है। रोग, शोक, अज्ञान, भूख, प्यास, परमुखापेक्षिता और मूकता से इनका उद्धार करना है। साहित्य का यही काम है।
इससे छोटे उद्देश्य को मैं विशेष बहुमान नहीं देता। आप क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे और किस भाषा में लिखेंगे, इन प्रश्नों का निर्माण इन्हीं की ओर देखकर कीजिए। यदि इनको मनुष्यता के ऊँचे आसन पर आप नहीं बैठा सकते तो साहित्यिक भी नहीं कहे जा सकते; और यह कहना ही आवश्यक है कि स्वयं मनुष्य बने बिना, स्वयं छोटे-छोटे तुच्छ विवादों से ऊपर उठे बिना, कोई भी व्यक्ति दूसरे को नहीं उठा सकता है। साहित्य के साधकों को मनुष्य की सेवा करनी है तो देवता बनना होगा। नान्यः पंथा विद्यतेऽयनाय।
शायद मेरी ही भाँति आप भी इतना अवश्य स्वीकार करते हैं कि इस बहुधा-विभक्त जनसमुदाय को संबद्ध बनाना है। यदि यह बात सत्य है तो मैं समझता हूँ, अभी हमने साहित्य का आरंभ ही नहीं किया है। हिंदी में कितने जनसमूह के परिचायक ग्रंथ हमने लिखे हैं? इस विशाल मानव समाज की रीति-नीति, आचार-विचार, आशा-आकांक्षा, उत्थान-पतन समझने के लिए हमारी भाषा में कितनी पुस्तकें हैं? इनके जीवन को सुखमय बनाने के साधनों, इनकी भूमि, इनके पशु, इनके विनोद-सहचर, इनके पेशे, इनके विश्वास, इनकी नई-नई मनोवृत्तियों का हमने क्या अध्ययन प्रस्तुत किया है? कहाँ है वह सहानुभूति और दर्द का प्रमाण, जिसे आप गणदेवता के सामने रख सकेंगे? हिंदी की उन्नति का अर्थ उसके बोलने और समझने वालों की उन्नति है।
अपना यह देश कोई नया साहित्यिक प्रयोग करने नहीं निकला है। इसकी साहित्यिक-परंपरा अत्यंत दीर्घ, धारावाहिक और गंभीर है। साहित्य नाम के अंतर्गत मनुष्य जो कुछ भी सोच सकता है, उस सबका प्रयोग इस देश में सफलतापूर्वक हो चुका है। वह अपनी भाषा का दुर्भाग्य है कि हमारी प्राचीन चिंतनराशि को उसमें संचित नहीं किया गया है। संस्कृत, पालि और प्राकृत की बढ़िया पुस्तकों के जितने उत्तम अनुवाद अंग्रेज़ी, फ़्रेंच और जर्मन आदि भाषाओं में हुए हैं, उतने हिंदी में नहीं हुए। परंतु दुर्भाग्य भी लाक्षणिक प्रयोग है और यह वस्तुतः उस विशाल मानव-समाज का दुर्भाग्य है, जो भाषा के ज़रिए ही ज्ञान-अर्जन करना चाहता है या करता है। यह विशाल साहित्य अपनी भाषाओं में यदि अनूदित होता तो हमारा साहित्यिक सहज ही उन सैकड़ों प्रकार के अपप्रचारों और हीन भावनाओं का शिकार होने से बच जाता, जो आज संपूर्ण समाज को दुर्बल और परमुखापेक्षी बना रहे हैं। विभिन्न स्वार्थ के पोषक प्रचार इस देश की अतिमात्र विशेषताओं का डंका प्रायः पीटा करते हैं।
इतिहास को कभी भौगोलिक व्याख्या के भीतर से, कभी जातिगत और कभी धर्मगत विशेषताओं के भीतर से प्रतिफलित करके समझाया जाता है कि हिंदुस्तानी जैसे हैं, उन्हें वैसा ही होना है और उसी रूप में बना रहना ही उनके लिए श्रेयस्कर है। इतिहास की जो अभद्र व्याख्या इन भिन्न-भिन्न विशेषताओं के भीतर से देखने वाले प्रचारकों ने की है, वह हमारे रोम-रोम में व्याप्त होने लगीं हैं। अगर इस ज़हर को दूर करना है तो प्राचीन ग्रंथों के देशी प्रामाणिक संस्करण और अनुवाद करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अपनी भाषा में प्राचीन ग्रंथों को हमें सिर्फ़ इसलिए नहीं भरना है कि हमें दूसरे स्वार्थी लोगों के अपप्रचार के प्रभाव से मुक्त होना है। विदेशी पंडितों ने अपूर्व लगन और निष्ठा के साथ हमारे प्राचीन शास्त्रों का अध्ययन, मनन और संपादन किया है। हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए; परंतु यह बात भूल नहीं जाना चाहिए कि अधिकांश विदेशी पंडितों के लिए हमारे प्राचीन शास्त्र नुमाइशी वस्तुओं के समान हैं। उनके प्रति उनका जो सम्मान है, उसे अंग्रेज़ी के ‘म्यूज़ियम इंटरेस्ट’ शब्द से भी समझाया जा सकता है। नुमाइश में रखी हुई चीज़ों को हम प्रशंसा और आदर की दृष्टि से देखते हैं, परंतु निश्चित जानते हैं कि हम अपने जीवन में उनका व्यवहार नहीं कर सकते। किसी मुग़ल सम्राट का चोगा किसी प्रदर्शिनी में दिख जाए तो हम उसकी प्रशंसा चाहे जितनी करें, पर हम निश्चित जानेंगे कि उसको हमें धारण नहीं करना है। परंतु भारतीय शास्त्र हमारे देशवासियों के लिए प्रदर्शिनी की वस्तु नहीं हैं, वे हमारे रक्त में मिले हुए हैं। भारतवर्ष आज भी उनकी व्यवस्था पर चलता है और उनसे प्रेरणा पाता है। इसीलिए हमें इन ग्रंथों का अपने ढंग से संपादन करके प्रकाशन करना है, इनके ऐसे अनुवाद प्रकाशित करने हैं, जो पुरानी अनुश्रुति से विच्छिन्न और असंबद्ध भी न हों और आधुनिक ज्ञान के आलोक में देख भी लिए गए हों। यह बड़ा विशाल कार्य है। संस्कृत भारतवर्ष की अपूर्व महिमाशालिनी भाषा है। वह हज़ारों वर्षों के दीर्घकाल में और लाखों वर्गमील में फैले हुए मानव-समाज के सर्वोत्तम मस्तिष्कों में विहार करने वाली भाषा है। उसका साहित्य विपुल है। उसका साधन गहन है और उसका उद्देश्य साधु है। उस भाषा को हिंदी-माध्यम से समझने का प्रयत्न करना भी एक तपस्या है। उस तपस्या के लिए संयम तथा आत्मबल की आवश्यकता है। हमें अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर गंभीरतापूर्वक उसके अध्ययन में जुट जाना चाहिए। हिंदी को संस्कृत से विच्छिन्न करके देखने वाले उसकी अधिकांश महिमा से अपरिचित हैं।
महान कार्य के लिए विशाल हृदय होना चाहिए। हिंदी का साहित्य सचमुच महान कार्य है, क्योंकि उससे करोड़ों का भला होना है। हम आजकल प्रायः गर्वपूर्वक कहा करते हैं कि हिंदी बोलने वालों की संख्या भारतवर्ष में सबसे अधिक है। मैं समझता हूँ, यह बात चिंता की है, क्योंकि हिंदी बोलने वाले जन-समूह की मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक भूख मिटाने का काम सहज नहीं है।
भारतवर्ष के पड़ोसी देशों में आजकल हिंदी-साहित्य पढ़ने और समझने में तीव्र लालसा जाग्रत हुई है। चीन से, मलय से, सुमात्रा से, जावा से—समस्त एशिया से माँग आ रही है। एशिया के देश अब अंग्रेज़ी पुस्तकों में प्राप्त सूचनाओं से संतुष्ट नहीं हैं। वे देशी दृष्टि से देशी भाषा में लिखा हुआ साहित्य खोजने लगे हैं। आगे यह जिज्ञासा और भी तीव्र होगी। मुझे चिंता होती है कि क्या हम अपने को इस उठती हुई श्रद्धा के उपयुक्त पात्र सिद्ध कर सकेंगे? जिस दिन इतिहास-विधाता हमें ठेलकर विश्व-जनता के दरबार में ला पटकेंगें, उस दिन तक क्या हम इतना भी निश्चय कर सके होंगे कि हमारी भाषा कैसी होगी, उसमें भिन्न-भिन्न भाषाओं के शब्दों का अनुपात क्या होगा और शब्दों के ‘शुद्ध’ और ‘गैर-शुद्ध’ उच्चारणों में से कौन-सा अपनाया जाएगा?
समूचे जनसमूह में भाषा और भाव की एकता और सौहार्द का होना अच्छा है। इसके लिए तर्क-शास्त्रियों की नहीं, ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों की आवश्यकता है, जो समस्त बाधाओं और विघ्नों को शिरसा स्वीकार करके काम करने में जुट जाते हैं। वे ही लोग साहित्य का भी निर्माण करते हैं और इतिहास का भी। आज काम करना बड़ी बात है। इस देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, स्पृश्य हैं, अस्पृश्य हैं, संस्कृत हैं, फ़ारसी हैं—विरोधों और संघर्षों की विराट वाहिनी है; पर सबके ऊपर मनुष्य है। विरोधों को दिन-रात याद करते रहने की अपेक्षा अपनी शक्ति का संबल लेकर उसकी सेवा में जुट जाना अच्छा है। जो भी भाषा आपके पास है, उससे बस मनुष्य को ऊपर उठाने का काम शुरू कर दीजिए। आपका उद्देश्य आपकी भाषा बना देगा।
अच्छी बात करने वालों की कमी इस देश में कभी नहीं रही है। आज भी बहुत ईमानदारी और सच्चाई के साथ अच्छी बात करने वाले आदमी इस देश में कम नहीं हैं। उन्होंने प्रेम और भ्रातृभाव का मंत्र बताया है। आदिकाल से महापुरुषों ने प्रेम और सौहार्द का संदेश सुनाया है। कहते हैं, व्यासदेव ने अंतिम जीवन में निराश होकर कहा था कि मैं भुजा उठाकर चिल्ला रहा हूँ कि धर्म ही प्रधान वस्तु है, उसी से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, पर मेरी कोई सुन नहीं रहा है—
ऊर्ध्वबाहुविरौम्येष नैव कश्चिच्छुणोति मे।
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्म किं न सेव्यताम्॥
ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि समाज के ऐतिहासिक विकास, आर्थिक संयोजन और सामाजिक संगठन के मूल में ही कुछ ऐसी ग़लती रह गई है कि एक दल जिसे धर्म समझता है, दूसरा उसे नहीं समझ पाता। इस वैषम्य को ध्यान में रखकर ही प्रेम सौहार्द का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। दही में जितना भी दूध डालिए, दही होता जाएगा। शंकाशील हृदयों में प्रेम की वाणी भी शंका उत्पन्न करती है।
मेरी अल्प बुद्धि में तो यही सूझता है कि समाज के नाना स्तरों के लिए अलग-अलग ढंग की भाषा होगी। नाना उद्देश्यों की सिद्धि के लिए नाना भाँति के प्रयत्न करने होंगे। सारे प्रतीयमान विरोधों का सामंजस्य एक ही बात से होगा—मनुष्य का हित।
भारत के हज़ारों गाँवों और शहरों में फैली हुई सैकड़ों जातियों और उप-जातियों में विभक्त सभ्यता को नाना सीढ़ियों पर खड़ी हुई यह जनता ही हमारे समस्त वक्तव्यों का लक्ष्यीभूत श्रोता है। उसका कल्याण ही साध्य है; बाक़ी सबकुछ साधन है—संस्कृत भी और फ़ारसी भी, व्याकरण भी और छंद भी, साहित्य भी और विज्ञान भी, धर्म भी और ईमान भी। हमारे समस्त प्रयत्नों का एकमात्र लक्ष्य यही मनुष्य है। उसको वर्तमान दुर्गति से बचाकर भविष्य में आत्यंतिक कल्याण की ओर उन्मुख करना ही हमारा लक्ष्य है। यही सत्य है, यही धर्म है। सत्य वह नहीं है जो मुख से बोलते हैं। सत्य वह है जो मनुष्य के आत्यंतिक कल्याण के लिए किया जाता है। नारद ने शुकदेव से कहा था कि सत्य बोलना अच्छा है, पर हित बोलना और भी अच्छा है। मेरे मत से सत्य वह है, जो भूत-मात्र के आत्यंतिक कल्याण का हेतु हो—
सत्यस्य वचनं श्रेय: सत्यादपि हितं वदेत्।
यद्भूतहितमत्यंतमेतत् सत्यं मतं मम्॥
यही सर्वभूत का आत्यंतिक कल्याण साहित्य का चरम लक्ष्य है। जो साहित्य केवल कल्पना-विलास है, जो केवल समय काटने के लिए लिखा जाता है, वह बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी चीज़ वह है, जो मनुष्य को आहार-निद्रा आदि पशु सामान्य धरातल से ऊपर उठाता है। मनुष्य का शरीर दुर्लभ वस्तु है, इसे पाना ही कम तप का फल नहीं है; पर इसे महान लक्ष्य की ओर उन्मुख करना और भी श्रेष्ठ कार्य है।
इधर कुछ ऐसी हवा बही है कि हर सस्ती चीज़ को साहित्य का वाहन माना जाने लगा है। इस प्रवृत्ति को ‘वास्तविकता’ के ग़लत नाम से पुकारा जाने लगा। तरह-तरह की दलीलें देकर यह बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि मनुष्य की लालसोन्मुख वृत्तियाँ ही साहित्य के उपयुक्त वाहन हैं। मुझे किसी मनोरोग के विपक्ष में या पक्ष में कुछ भी नहीं कहना है। मुझे सिर्फ़ इतना ही कहना है कि साहित्य के उत्कर्ष या अपकर्ष के निर्णय की एकमात्र कसौटी यही हो सकती है कि वह मनुष्य का हित साधन करता है या नहीं। जिस बात के कहने से मनुष्य पशु-सामान्य धरातल के ऊपर नहीं उठता, वह त्याज्य है। मैं उसी को सस्ती चीज़ कहता हूँ। सस्ती इसलिए कि उसके लिए किसी प्रकार के संयम या तप की ज़रूरत नहीं होती। धूल में लोटना बहुत आसान है परंतु धूल में लोटने से संसार का कोई बड़ा उपकार नहीं होता और न किसी प्रकार के मानसिक संयम का अभ्यास ही आवश्यक है। और जैसा कि रविंद्रनाथ ने कहा कि यदि कोई नि:संकोच धूल में लोट पड़े तो इसे हम बहुत बड़ा पुरुषार्थ नहीं कह सकते। हम इस बात को डरने योग्य भी नहीं मानेंगे; परंतु यदि दस-पाँच भले आदमी ऊँचे गले से यही कहना शुरू कर दें कि धूल में लोटना ही उस्तादी है तो थोड़ा डरना आवश्यक हो जाता है। भय का कारण इसका सस्तापन है। मनुष्य में बहुत सी आदिम मनोवृत्तियाँ हैं, जो ज़रा-सा सहारा पाते ही झनझना उठती हैं। अगर उनको भी साहित्य-साधना का बड़ा आदर्श कहा जाने लगे तो उस मानने और पालन करने वालों की कमी नहीं रहेगी। ऐसी बातों को इस प्रकार प्रोत्साहित किया जाता है कि मानो यह कोई साहस और वीरता का काम है।
पुरानी सड़ी रूढ़ियों का मैं पक्षपाती नहीं हूँ, परंतु संयम और निष्ठा पुरानी रूढ़ियाँ नहीं हैं। वे मनुष्य के दीर्घ आयास से उपलब्ध गुण हैं और दीर्घ आयास से ही पाए जाते हैं। इनके प्रति विद्रोह प्रगति नहीं है। आदिम युग में मनुष्य की जो वृत्तियाँ अत्यंत प्रबल थीं, वे निश्चय ही अब भी हैं और प्रबल भी हैं। परंतु मनुष्य ने अपनी तपस्या से उनको अपने वश में किया है और वश में करने के कारण वह उनको सुंदर बना सका है। मनुष्य के रंगमंच पर आने के पहले प्रकृति लुढ़कती-पुढ़कती चली आ रही थी। प्रत्येक कार्य अपने पूर्ववर्ती कार्य का परिणाम है। संसार की कार्य-कारण परंपरा में कहीं फाँक नहीं थी। जो वस्तु जैसी होने को है, वह वैसी होगी। इसी समय मनुष्य आया। उसने इस नीरंध्र ठोस कार्य-कारण परंपरा में एक फाँक का आविष्कार किया। जो जैसा है, उसे वैसा ही मानने से उसने इंकार कर दिया। उसे उसने अपने मन के अनुकूल बनाने का प्रयत्न किया। सो मनुष्य की पूर्ववर्ती सृष्टि किसी प्रकार बनती जा रही थी, मनुष्य ने उसे अपने अनुकूल बनाना चाहा—यहीं मनुष्य पशु से अलग हो गया। वह पशु-सामान्य धरातल से ऊपर उठा। बार-बार उसे उसी धरातल की ओर उन्मुख करना प्रगति नहीं, यह पीछे लौटने का काम है। मैं मानता हूँ कि न तो कभी ऐसा समय रहा है, जब लालसा को उत्तेजना देने वाला साहित्य न लिखा गया हो और न कोई ऐसा देश है जहाँ ऐसी बातें न लिखी गई हों; परंतु मेरा विश्वास है कि मनुष्य सामूहिक रूप से इस ग़लती को महसूस करेगा और त्याग देगा। यह ठीक है, कि मनुष्य का इतिहास उसकी ग़लतियों का इतिहास है, पर यह और भी ठीक है कि मनुष्य बराबर ग़लतियों पर विजय पाता आता है। लालसा को उत्तेजना देने वाला साहित्य उसकी ग़लती है। एक-न-एक दिन वह इस पर अवश्य विजय पाएगा।
सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है। उसके साथ समझौता नहीं हो सकता। साहित्य के चरम सत्य को पाने के लिए भी उसका पूरा-पूरा मूल्य चुकाना ही समीचीन है। जो लोग पद-पद पर सहज और सीधे साधनों की दुहाई दिया करते हैं, शायद किसी बड़े लक्ष्य की बात नहीं सोचते। मनुष्य को उसके उच्चतर लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए उसके प्रतिदिन के व्यवहार में आने वाली वृत्तियों के साथ सुलह करने से काम नहीं चलेगा। कठोर संयम और त्याग द्वारा ही उसे बड़ा बनाया जा सकेगा। जो बात एक क्षेत्र में सत्य है, वह सभी क्षेत्रों में सत्य है—साहित्य में, भाषा में, आचार में, विचार में, सर्वत्र। भाषा को ही लीजिए। मनुष्य अपने आहार और निद्रा के साधनों को जुटाने के लिए जिस भाषा का व्यवहार करता है, उसकी अनायास लब्ध भाषा है; परंतु यदि उसे इस धरातल से ऊपर उठाना है तो उतने से काम नहीं चलेगा। सहज भाषा आवश्यक है। पर सहज भाषा का मतलब है सहज ही महान बनाने वाली भाषा, रास्ते में बटोरकर संग्रह की हुई भाषा नहीं।
सीधी लकीर खींचना टेढ़ा काम है। सहज भाषा पाने के लिए कठोर तप आवश्यक है। जब तक आदमी सहज नहीं होता तब तक भाषा का सहज होना असंभव है। स्वदेश और विदेश के वर्तमान और अतीत के समस्त वाङ्मय का रस निचोड़ने से वह सहज भाव प्राप्त होता है। हर अदना आदमी क्या बोलता है या क्या नहीं बोलता, इस बात से सहज भाषा का अर्थ स्थिर नहीं किया जा सकता। क्या कहने या क्या न कहने से मनुष्य उस उच्चतर आदर्श तक पहुँच सकेगा, जिसे संक्षेप में ‘मनुष्यता’ कहा जाता है, यही मुख्य बात है। सहज मनुष्य ही सहज भाषा बोल सकता है। दाता महान होने से दान महान होता है।
जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया है, वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषाशास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती, कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली, क्योंकि वे सहज हो सके। उनमें दान करने की क्षमता थी! शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृत्व नहीं मिलता, अपन को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर महासहज के समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। जो अपने को नि:शेष भाव से दे नहीं सका, वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएँगे यह ग़लत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन करो—इसके लिए तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने को नि:शेष भाव से दान कर देने की ज़रूरत है।
हिंदी साधारण जनता की भाषा है। जनता के लिए ही उसका जन्म हुआ था और जब तक वह अपने को जनता के काम की चीज़ बनाए रहेगी, जनचित्त में आत्म-बल का संचार करती रहेगी, तब तक उसे किसी से डर नहीं है। वह अपने आपकी भीतरी अपराजेय शक्ति के बल पर बड़ी हुई है, लोक-सेवा के महान व्रत के कारण बड़ी हुई है और यदि अपनी मूल शक्ति के स्रोत को भूल नहीं गई तो निस्संदेह अधिकाधिक शक्तिशाली होती जाएगी। उसका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वह विरोधों और संघर्षों के बीच ही पली है। उसे जन्म के समय ही मार डालने की कोशिश की गई थी, पर वह मरी नहीं है, क्योंकि उसकी जीवनी-शक्ति का अक्षय स्रोत जनचित्त है। वह किसी राजशक्ति की उँगली पकड़कर यात्रा तय करने वाली भाषा नहीं है, अपने आपकी भीतरी शक्ति से महत्त्वपूर्ण आसन अधिकार करने वाली अद्वितीय भाषा है।
शायद ही संसार में ऐसी कोई भाषा हो, जिसकी उन्नति में पद-पद पर इतनी बाधा पहुँचाई गई हो, फिर भी जो इस प्रकार अपार शक्ति संचय कर सकी हो। आज वह सैकड़ों ‘प्लेटफ़ार्मों’ से, कोड़ियों से, विद्यालयों से और दर्जनों प्रेसों से नित्य मुखरित होने वाली परम शक्तिशालिनी भाषा है। उसकी जड़ जनता के हृदय में है। वह करोड़ों नर-नारियों की आशा और आकांक्षा, क्षुधा और पिपासा, धर्म और विज्ञान की भाषा है। हिंदी सेवा का अर्थ करोड़ों की सेवा है। इसका अवसर मिलना सौभाग्य की बात है।
(दो)
वास्तव में हमारे अध्ययन की सामग्री प्रत्यक्ष मनुष्य है। आपने इतिहास में इसी मनुष्य की धारावाहिक जययात्रा की कहानी पढ़ी है, साहित्य में इसी के आवेगों, उद्वेगों और उल्लासों का स्पंदन देखा है, राजनीति में इसकी लुका-छिपी के खेल का दर्शन किया है, अर्थशास्त्र में इसी की रीढ़ की शक्ति का अध्ययन किया है। यह मनुष्य ही वास्तविक लक्ष्य है। आप इससे सीधा संबंध जोड़ने जा रहे हैं। यह जो प्रत्यक्ष मनुष्य का पढ़ना है, वही बड़ी बात है। हमारी शिक्षा का अधिक भाग जिन सब दृष्टांतों का आश्रय लेता है, वे हमारे सामने नहीं आते। हमारा इतिहास पढ़ना तब तक व्यर्थ है, जब तक हम उसे इस जीवंत मानव-प्रवाह के साथ एक करके न देख सकें। हमारे देश का इतिहास—यदि वह सचमुच ही हमारे देश का है—आज भी निश्चय ही हमारे घरों में, गाँवों में, जातियों में, खंडहरों में और इस देश के ज़र्रे-ज़र्रे में अपना चिह्न छोड़ता जा रहा है। जब तक देश के इन प्रत्येक कणों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध नहीं स्थापित होता तब तक हम इतिहास का वास्तविक ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकेंगे? हममें से जो कोई भी अपने को शिक्षित समझता हो, उसे अपनी उच्च अट्टालिका से नीचे उतरकर अपने देश के इर्द-गिर्द फैले हुए विशाल जनसमूह, विस्तृत भूखंड और सजीव चिंता-प्रवाह को ही प्रधान पाठ्य-पुस्तक बनाना होगा। पुस्तकें इसी महाग्रंथ को समझाने का साधन मानी जानी चाहिए। नोटों और कुंजियों को उत्पन्न करने वाली मनोवृत्ति का निर्दयतापूर्वक दमन कर देना चाहिए। हम लोग नृतत्त्व के ग्रंथ न पढ़ते हों सो बात नहीं है, किंतु जब हम देखते हैं कि ग्रंथ पढ़ने के कारण हमारे घरों के निकट जो चमार, धीवर, कोढ़ी, कुम्हार लोग रहते हैं, उनके पूरे परिचय पाने के लिए हमारे हृदयों में ज़रा भी उत्सुकता नहीं उत्पन्न होती तब अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि पुस्तकों के संबंध में हमें कितना अंध-विश्वास हो गया है, पुस्तकों को हम कितना बड़ा समझते हैं और पुस्तकें वस्तुतः जिनकी छाया हैं, उनको कितना तुच्छ मानते हैं। यह ढंग ग़लत है। इसमें सुधार होना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में ‘सेकेंड हैंड’ ज्ञान की प्रधानता स्थापित होना वांछनीय नहीं है। दुर्भाग्यवश अपने देश में ऐसे ही ज्ञान की प्रधानता स्थापित हो गई है। हमें यदि सचमुच कुछ नया करना है तो बड़े विकट प्रयास करने पड़ेंगे। समूचे देश के मस्तिष्क में जो जड़-संस्कार पैदा कर दिए गए, उनसे जूझना पड़ेगा, इसका समर्थन तभी हो सकता है, जब हम दृढ़ होकर प्रत्यक्ष ज्ञान की ओर अग्रसर हों।
आप में से अधिकांश का मार्ग शायद मातृभाषा और उसके साहित्य द्वारा देश की सेवा करना हो। यह बड़ा उत्तम मार्ग है। परंतु हमें अच्छी तरह समझ लेने की आवश्यकता है कि साहित्य-सेवा या मातृभाषा की सेवा का क्या अर्थ है। किसे सामने रखकर आप साहित्य लिखने जा रहे हैं? आपके वक्तव्यों का लक्ष्यीभूत श्रोता कौन है? हिंदी भाषा कोई देवी-देवता की मूर्ति का नाम नहीं है। हिंदी की सेवा करने का अर्थ हिंदी की प्रतिमा बनाकर पूजना नहीं है। यह लाक्षणिक प्रयोग है। इसका अर्थ है—हिंदी के माध्यम द्वारा समझने वाली विशाल जनता की सेवा। कभी-कभी हम लोग इस भाषा से प्राप्त होने वाले अन्यायों से विक्षुब्ध होकर ग़लत ढंग के स्वभाषा-प्रेम का परिचय देते हैं। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने साहित्य से प्रेम होना बुरी बात नहीं है, पर जो प्रेम ज्ञान द्वारा चालित और श्रद्धा द्वारा अनुगमित होता है, वही प्रेम अच्छा है। केवल ज्ञान बोझ है, केवल श्रद्धा अंधा बना देती है। हिंदी के प्रति जो हमारा प्रेम है, वह भी ज्ञान द्वारा चालित और श्रद्धा द्वारा अनुगमित होना चाहिए। हमें ठीक-ठीक समझना चाहिए कि हिंदी की शक्ति कहाँ है? हिंदी इसलिए बड़ी नहीं है कि हममें से कुछ लोग इस भाषा में कहानी या कविता लिख लेते हैं या सभा-मंचों पर बोल लेते हैं। नहीं, वह इसलिए बड़ी है कि कोटि-कोटि जनता के हृदय और मस्तिष्क की भूख मिटाने में यह भाषा इस देश में सबसे बड़ा साधन हो सकता है। हमारे पूर्वजों ने दीर्घकाल की तपस्या और मनन से जो ज्ञानराशि संचित की है, उसे सुरक्षित रखने का यह सबसे मज़बूत पात्र है, अकारण और सकारण शोषित और पोषित, मूढ़, निर्वाक जनता तक आशा और उत्साह का संदेश इसी जीवंत और समर्थ भाषा के द्वारा पहुँचाया जा सकता है। यदि देश में आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को हमें जनसाधारण तक पहुँचाना है तो इसी भाषा का सहारा लेकर हम यह काम कर सकते हैं। हिंदी इन्हीं संभावनाओं के कारण बड़ी है। यदि वह यह कार्य नहीं कर सकती तो ‘हिंदी-हिंदी’ चिल्लाना व्यर्थ है। यदि वह यह काम कर सकती है तो उसका भविष्य अत्यंत उज्ज्वल है। यदि वह इन महान उद्देश्यों के अनुकूल है तो फिर वह इस देश में हिमालय की भाँति अचल होकर रहेगी। हिमालय की ही भाँति उन्नत, उतनी ही महान हिंदी जनता की भाषा है। जनता के लिए ही उसका जन्म हुआ था और जब तक वह जनता के चित्त में आत्मबल संचारित करती रहेगी, उसके हृदय और मस्तिष्क की भूख मिटाती रहेगी, तब तक उसका जीवन सार्थक है। जो लोग इस भाषा और उसके साहित्य की सेवा करने का व्रत करने जा रहे हों, उन्हें यह बात कभी नहीं भूलनी चाहिए।
भारतवर्ष क्या है? अनादिकाल के नाना जातियाँ अपने नाना भाँति के संस्कार, रीति-रस्म आदि लेकर इस देश में आती रही हैं। यहाँ भी अनेक प्रकार के मानवीय समूह विद्यमान रहे हैं। ये जातियाँ कुछ देर तक झगड़ती रही हैं और फिर रगड़-झगड़कर, ले-देकर पास-ही-पास बस गई हैं—भाइयों की तरह। इन्हीं नाना जातियों, नाना संस्कारों, नाना धर्मों, नाना रीति-रस्मों का जीवंत समन्वय यह भारतवर्ष है। विदेशी पराधीनता ने इसके स्वाभाविक विकास में बाधा पहुँचाई है। उसका बाह्यरूप विचित्र-सा दिखाई दे रहा है। इसी वैचित्र्यपूर्ण जनसमूह को आशा और उत्साह का संदेश देना साहित्य-सेवा का लक्ष्य है। हज़ारों गाँवों और शहरों में फैली हुई, शताधित जातियों और उप-जातियों में विभक्त, सभ्यता के नाना स्तरों पर ठिठकी हुई यह जनता ही हमारे समस्त प्रयत्नों का लक्ष्य है। इसका कल्याण ही साध्य है। बाक़ी सब कुछ साधन है। आपने जो अपनी भाषा पर अधिकार प्राप्त किया है, वह अपने आप में अपना अंत नहीं है। वह साधन है। इसे भाषा के सहारे आपको इस जनता तक पहुँचना है। इसको निराशा और पस्त हिम्मती से बचाना आपका कर्तव्य है; परंतु यह कोई सरल काम नहीं है। केवल कुछ अच्छा करने की इच्छा मात्र से यह काम नहीं होगा। आज की समस्याएँ बड़ी उलझनदार और जटिल हैं। बिजली की बत्ती मुँह से फूँककर नहीं बुझाई जाती है। यह समझने की ज़रूरत है कि जो दुर्गति आज हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, उसका वास्तविक कारण क्या है? साहित्य का साधक केवल कल्पना की दुनिया में विचरण करके, केवल ‘हाय-हाय’ को या ‘वाह-वाह’ की पुकार करके अपने सामने की कुत्सित कुरूपता को नहीं बदल सकता। हमें उस समूची विद्या को सीखना पड़ेगा, जो विश्व-रहस्य से नए-नए द्वार खोल रही है, जो प्रकृति के समस्त गुप्त भंडार पर धावा बोलने के लिए बद्धपरिकर है, जो मनुष्य को असीम सुख और समृद्धि तक ले जा सकती है, फिर हमें उस स्वार्थ-शक्ति को भी समझना है, जो इस विद्या का ग़लत प्रयोग करने वाले मनुष्य को सर्वत्र लांछित और अपमानित कर रही है। साहित्य का कारोबार मनुष्य के समूचे जीवन को लेकर है। जो लोग आज भी यह सोचते हैं कि साहित्य के लिए कुछ ख़ास-ख़ास विषय ही पढ़ने के हैं, वे बड़ी ग़लती करते हैं। आज की जनता की दुर्दशा को यदि आप सचमुच ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं तो आप चाहे जो भी मार्ग लें, राजनीति से अलग होकर नहीं रह सकते, अर्थनीति की उपेक्षा नहीं कर सकते और विज्ञान की नई प्रवृत्तियों से अपरिचित रहकर कुछ भी नहीं कर सकते। साहित्य केवल बुद्धि विलास नहीं है। वह जीवन की वास्तविकता की उपेक्षा करके सजीव नहीं रह सकता।
साहित्य के उपासक अपने पैर के नीचे की मिट्टी की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम सारे बाह्य जगत को असुंदर छोड़कर सौंदर्य की सृष्टि नहीं कर सकते। सुंदरता सामंजस्य का नाम है। जिस दुनिया में छोटाई और बड़ाई में, धनी और निर्धन में, ज्ञानी और अज्ञानी में, आकाश-पाताल का अंतर हो वह दुनिया बाह्य सामंजस्य नहीं कही जा सकती और इसलिए वह सुंदर भी नहीं है। इस बाह्य असुंदरता के ढूह में खड़े होकर आंतरिक सौंदर्य की उपासना नहीं हो सकती। हमें उस बाह्य असौंदर्य को देखना ही पड़ेगा। निरन्न, निर्वसन जनता के बीच खड़े होकर आप परियों के सौंदर्य-लोक की कल्पना नहीं कर सकते। साहित्य सुंदर का उपासक है; इसलिए असामंजस्य को दूर करने का प्रयत्न पहले करना होगा; अशिक्षा और कुशिक्षा से लड़ना होगा; भय और ग्लानि से लड़ना होगा। सौंदर्य और असौंदर्य का कोई समझौता नहीं हो सकता। सत्य अपना पूरा मूल्य चाहता है। उसे पाने का सीधा और एकमात्र रास्ता उसकी क़ीमत चुका देना ही है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे देश का बाह्य रूप न तो आँखों की प्रीति देने लायक है, न कानों को, न मन को न बुद्धि को। यह सचाई है।
यदि किसी देश का बाह्य रूप सम्मान योग्य तथा सुंदर नहीं बन सका है तो समझना चाहिए कि उस राष्ट्र की आत्मा में एक उच्च जगत का निर्माण किया जाना शुरू नहीं हुआ है, अर्थात् वहाँ सच्चे साहित्य के निर्माण का श्रीगणेश नहीं हुआ है। साहित्य ही मनुष्य को भीतर से सुसंस्कृत तथा उन्नत बनाता है और तभी उसका बाह्य रूप भी साफ़ और स्वस्थ दिखाई देता है। और साथ ही बाह्य रूप के साफ़ और स्वस्थ होने से आंतरिक स्वास्थ्य का भी आरंभ होता है। दोनों ही बातें अन्योन्याश्रित हैं। जबकि हमारे देश में नाना भाँति के कुसंस्कार और गंदगी वर्तमान है जबकि हमारे समाज का आधा अंग पर्दे में ढका हुआ है, जब कि हमारी नब्बे फ़ीसदी जनता अज्ञान के मलबे के नीचे दबी हुई है तब हमें मानना चाहिए कि अभी दिल्ली बहुत दूर है। हम साहित्य के नाम पर जो कुछ कर रहे हैं और जो कुछ दे रहे हैं, उसमें कहीं बड़ी भारी कमी रह गई है। हमारा भीतर और बाहर आप ही साफ़-स्वस्थ नहीं है। साहित्य की साधना तब तक बाध्य ही रहेगी जब तक हम पाठकों में एक ऐसी अदमनीय आकांक्षा जाग्रत न कर दें जो सारे मानव-समाज को भीतर से और बाहर से सुंदर तथा सम्मान योग्य देखने के लिए सदा व्याकुल रहे। अगर यह आकांक्षा जागृत हो सकी तो हममें से प्रत्येक अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार उन सामग्रियों को ज़रूर संग्रह कर लेगा जो उक्त इच्छा की पूर्ति की सहायक हैं। अगर यह आकांक्षा जाग्रत नहीं हुई तो कितनी भी विद्या क्यों न पढ़ी हो, वह एक जंजाल मात्र सिद्ध होगी और दुनियादारी और चालाकी का ढकोसला ही बनी रहेगी। जो साहित्यिक-निष्ठा के साथ इच्छा को लेकर रास्ते पर निकल पड़ेगा वह स्वयं अपना रास्ता खोज निकालेगा। साधन की अल्पता से कोई महती इच्छा आज तक नहीं रुकी है। भूख होनी चाहिए, एक बार भूख होने पर खाद्य-सामग्री जुट ही जाती है पर खाद्य-सामग्री के भरे रहने पर भूख नहीं लगती है। गरुड़ ने उत्पन्न होते ही कहा, “माँ, बहुत भूख लगती है।” माता विनता घबराकर विलाप करने लगी कि इस प्रचंड क्षुधाशाली पुत्र को अन्न कहाँ से दें। पिता कश्यप ने आश्वासन देकर कहा था, “कोई चिंता की बात नहीं। महान् पुत्र उत्पन्न हुआ है; क्योंकि उसकी भूख महान् है।” हमारी भाषा को भी इस समय प्रचंड साहित्यिक क्षुधा वाले महान पुत्र की आवश्यकता है। जब तक हमारी मातारूपी भाषा के गर्भ से ऐसे कृती पत्र पैदा नहीं होते, तभी तक वह विनता की तरह कष्ट पा रही है। जिस दिन ऐसे पुत्र पैदा होंगे, उस दिन मातृभाषा धन्य हो जाएगी।
इस देश में हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ब्राह्मण हैं, चांडाल हैं, धनी हैं, ग़रीब हैं—विरुद्ध संस्कारों और विरोधी स्वार्थों की विराट वाहिनी हैं। इसमें पद-पद पर ग़लत समझे जाने का अंदेशा है, प्रतिक्षण विरोधी स्वार्थों के संघर्ष में पिस जाने का डर है, संस्कारों और भावावेशों का शिकार हो जाने का अंदेशा है; परंतु इन समस्त विरोधों और संघातों से बड़ा और सबको छापकर विराज रहा है मनुष्य। इस मनुष्य की भलाई के लिए आप अपने आपको नि:शेष भाव से देकर ही सार्थक हो सकते हैं। सारा देश आपका है। भेद और विरोध ऊपरी हैं। भीतरी मनुष्य एक हैं। इस एक को दृढ़ता के साथ पहचानने का यत्न कीजिए। जो लोग भेद-भाव को पकड़कर ही अपना रास्ता निकालना चाहते हैं, वे ग़लती करते हैं। विरोधी रहे हैं तो उन्हें आगे भी बने ही रहना चाहिए, यह कोई काम की बात नहीं हुई। हमें नए सिरे से सब कुछ गढ़ना है; तोड़ना नहीं है, टूटे को जोड़ना है। भेद-भाव की जयमाला से हम पार नहीं उतर सकते। कबीर ने हैरान होकर कहा था—
कबीर इस संसार को समझाऊँ कैं बार।
पूंछ जु पकड़ें भेद का, उतरा चाहै पार॥
मनुष्य एक है। उसके सुख-दुःख को समझना, उसे मनुष्यता के पवित्र आसन पर बैठाना ही हमारा कर्तव्य है।
- पुस्तक : अशोक के फूल (पृष्ठ 192-214)
- रचनाकार : आचार्य हज़ारी प्रसाद द्वेवेदी
- प्रकाशन : सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.