ज़िंदगी की बे-अंत नैरंगियों का दीदार
 तसनीफ़ हैदर
09 जनवरी 2025
तसनीफ़ हैदर
09 जनवरी 2025
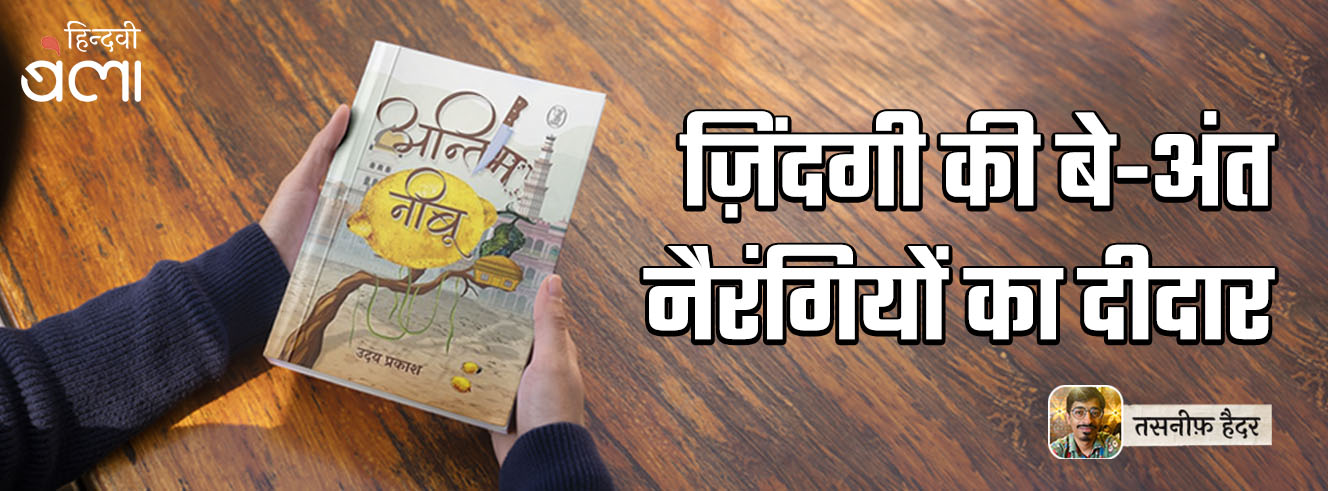
कहानी एक ऐसा हुनर है जिसके बारे में जहाँ तक मैं समझा हूँ—एक बात पूरे यक़ीन से कही जा सकती है कि आप कहानी में किसी भी तरह से उसके कहानी-पन को ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी अफ़सानवियत को कुचल नहीं सकते।
उदय प्रकाश की एक ख़ास बात यह है कि उनके यहाँ कहानी इतने सीधे और सच्चे अंदाज़ में आप पर उतरती है कि आप उसके हिसार में ख़ुद को घिरा हुआ महसूस करते हैं। जिस तरह ज़िंदगी का कोई मक़सद नहीं, ज़रूरी नहीं कि हर कहानी आपको किसी मंज़िल या मक़सद तक पहुँचा देगी। कभी-कभी वह आपको यूँ ही छोड़ जाती है—अधूरा, अकेला और बेचैन, मगर यही तो हर बड़े कहानीकार का आहंग है कि वह आपको ज़िंदगी की तरह ही कहानी के दर्शन कराता है।
उदय प्रकाश की इस किताब में शामिल क़रीब दस-ग्यारह कहानियाँ अपने इसी जादुई आहंग में ख़ुद को सजा-बनाकर आपके सामने पेश कर देती हैं, अगर आप मक़सद ढूँढ़ना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, नहीं तो बस इनके साथ चलते चलिए, कहानी का लुत्फ़ भी रास्ते की तरह, सफ़र की तरह लीजिए और ज़िंदगी की बे-अंत नैरंगियों का दीदार करते चलिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी किसी ख़ास धागे से बँधा नहीं है। ये आज़ाद कठ-पुतलियों का निगार-ख़ाना है।
कहानियों के इस होशरुबा उजाले में सबसे पहले उन्वान वाली कहानी पर ही बात कर लेते हैं। इस कहानी में जिन दत्तात्रेय का किरदार गढ़ा गया है, वह ख़ासा दिलचस्प है। कहानी अपने आपमें कुछ हक़ीक़त और कुछ एजाज़ यानी हक़ीक़त से परे की दुनिया से तअल्लुक़ रखती है।
उदय प्रकाश किंवदंतियों, प्राचीन क़िस्सों और मज़हबी हवालों से कई दफ़ा ऐसे ज़बरदस्त नुक़्ते निकालते हैं कि लुत्फ़ आ जाता है। कोरोना महामारी या वबा ने इंसान को इंसान से दूर किया, फ़ासलों की एक नई दुनिया पैदा की। क़रीब मत आओ, एक हाथ का फ़ासला बनाए रखो। ये लोगों को बचाने के लिए लोगों को लोगों से दूर करने की कोई बड़ी कार-आमद साज़िश की तरह हम सब पर मुसल्लत हुई।
फिर हमने देखा कि हम इसमें अपनी इंसानियत से भी दूर होते चले गए और वहाँ पहुँच गए—जहाँ बस ख़ुद को बचा लेने की धुन सिर पर सवार थी। ऐसे में हमने अपना आपा खोया, थालियाँ बजाईं, तालियाँ पीटीं और सड़क पर मज़दूरों, कामगारों को मरते, कुचलते, कुत्तों के आगे से बीन कर खाना खाते देखा और ज़िंदगी की बेशर्म ख़्वाबगाह में जस-के-तस बने रहे। ऐसे में हमें बचा लेने वाले किसी भी हथियार तक हम अपनी रसाई, अपनी पहुँच चाहते थे।
मगर दत्तात्रेय जैसे लोग भी हैं, जो इंसानियत को बचाने की फ़िक्र में हैं। उनकी निगाह में अपने बग़ीचे में लगा वह ‘अंतिम नीबू’ आ गया है, जिसकी मदद से ऐसा करना संभव है। अंत तो आप कहानी पढ़कर भी मालूम कर सकते हैं, हालाँकि उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। मगर यह कहानी आपको कुछ ऐसा दे जाती है, जिसमें किसी ‘अन्य’ में बदल जाने का सलीक़ा आप पर रौशन होता है। इसमें एक जगह वह लिखते हैं :
“जब तक आप दूसरा नहीं बनते, तब तक न दूसरे की भाषा समझ सकते हैं, न ‘अन्य’ किसी का जीवन। बाघ और इंसान में यही फ़र्क़ होता है, क्योंकि बाघ न हिरण बन सकता है; न गाय।”
यह पूरी कहानी हमारे अपने दौर में ख़ुद से दूसरे तक न पहुँच पाने की त्रासदी को भी बयान करती है और पहुँचने के संघर्ष को भी। मैं इसे कोविड काल पर लिखी हिंदुस्तानी ज़बानों की बेहतरीन कहानियों में सर-ए-फ़ेहरिस्त रख सकता हूँ।
कहानी के फ़न में उदय प्रकाश को जो महारत हासिल है, वह आपको उनके किसी भी अफ़साने को पढ़ते हुए पता चल सकती है। वह उन लेखकों में से हैं, जिनकी महज़ एक कहानी पढ़कर भी आप उनकी हुनरमंदी और कहानी पर उनकी गिरफ़्त के क़ाइल हो सकते हैं। इस किताब में शामिल दूसरे अफ़सानों पर मैं बहुत तफ़सील से तो रौशनी नहीं डाल सकता, अलबत्ता कुछ टिप्पणियाँ कर सकता हूँ, जिससे आपको इन्हें पढ़ने की तहरीक मिले।
‘अनावरण’ एक मज़ेदार और हमारी समाजी ना-बराबरी पर एक चोट है। कोई बहुत बड़ा दुख, हद से गुज़रकर दवा बनता हो या नहीं, मगर समाज के बड़े दुख गहरी शक्ल लेते ही मज़ाक़ में ज़रूर बदल जाते हैं। एक ऐसे हँसते हुए ज़ख़्म में जिसका मुँह बंद करना आसान नहीं होता। यह हमारी खिल्ली भी उड़ाते हैं और हमें शर्मिंदा भी करते हैं।
‘अनावरण’ कहानी भी एक ऐसे ही समाजी मसले की तरफ़ हमारा ध्यान दिलाती है, जहाँ हमने ग़रीबों, दुखियारों और बेचारों को चोर बनने पर महज़ इसलिए मजबूर किया है, क्योंकि वे अब हमारी दया के भी पात्र नहीं रहे। हम नाम-ओ-शोहरत के लिए पुतले, पुल और सड़क बनवा सकते हैं; मगर किसी की ख़ामोशी से मदद का जज़्बा हमारे तथाकथित नेताओं के लिए किसी तरह की कशिश नहीं रखता, इसलिए यह कहानी भी हमारे दुखों की तरह ही रंगीन और मज़ेदार है।
‘जज साहब’ एक और अनोखी कथा है, उसमें इंसानी फ़ितरत के सियाह-ओ-सफ़ेद रंगों से अलग ऐसे रंग पेश किए गए हैं जो हमें ख़ुद को न समझने की समझ प्रदान करते हैं। मैं इस कहानी के साथ काफ़ी अरसे तक रह सकता हूँ। नबोकोव ने कहा था कि असल चीज़ ‘पुनर्पाठ’ है। मैंने इस कहानी को दो से ज़्यादा बार पढ़ा है, यह मेरे अंदर गहरी उतरी हुई ज़िंदा कहानियों का हिस्सा बन गई है। कुछ खोकर उसे ढूँढ़ने की तग-ओ-दौ यानी दौड़-भाग में जिस तरह हम सब मसरूफ़ हैं, यह कहानी उस का बेहतरीन इस्तिआरा है, उसकी ख़ूबसूरत तस्वीर है।
उदय प्रकाश के यहाँ बयान की गई बातों से ज़्यादा कहानी पढ़ते समय आपको अव्यक्त चीज़ों पर गहरा ध्यान देना पड़ेगा, वरना कहानी का दामन हाथ से छूट चलेगा। ‘जज साहब’ भी ऐसा ही एक अफ़साना है, इसे महज़ एक इंसान की कहानी समझकर पढ़ने से आप भूल करेंगे और उससे बड़ी भूल होगी उस पहेली को सुलझाने की कोशिश करना, जो लोग नैयर मसूद की कहानियों के अंत की गिरहें खोलने में किया करते हैं।
एक कहानी इस संग्रह में है, जिसका शीर्षक है—‘मठाधीश’। एक आम से कुत्ते और इंसान के बीच की ऐसी कहानी जो एक साथ कई चीज़ों पर रोशनी डालती है। इंसान की हिंसक प्रवृत्ति, उसका ज़ालिमाना रुझान और कमज़ोरों के साथ उसका सुलूक। साथ-ही-साथ कुत्ते के रूप में जो रूपक तराशा गया है, वह भी दबे-कुचले और पिसे हुए आम आदमी को बहुत अच्छी तरह दर्शाता है। साथ में कहानी के अंत में मठाधीशों पर जिस तरह शिकंजा कसा गया है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। दरअस्ल, इस तरह की कहानी पढ़ते हुए मुझे दो कहानियों का एक साथ ख़याल आया जो इस कहानी के मुक़ाबले में काफ़ी लंबी और अलग हैं, मगर उनमें भी कुत्ते को बहुत अच्छी तरह इंसानी सूरत-ए-हाल को दिखाने समझाने के लिए इस्तेमाल किया गया है।
एक बुल्गाकोव की रूसी कहानी ‘दि डॉग्स हार्ट’ और दूसरे योगेंद्र आहूजा की एक कहानी ‘डॉग स्टोरी’। हालाँकि उदय प्रकाश ने अपनी कहानी को मुख़्तसर और अलग पैराए में बयान किया है और इसी वजह से वह भी पढ़ने वाले पर एक देर तक असर छोड़ने की ताक़त रखने वाली कहानी है। बहरहाल, उनकी इस तरह की कहानी का मक़सद एक तरह से समाज में फैली ना-बराबरी और ज़ुल्म की रिवायत पर चोट करना ही है। इसी किताब में कहानी ‘आचार्य का कुत्ता’ भी है और वह भी बड़ी दिलचस्प है।
एक और कहानी जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, वह है—‘वही मसीहा वही सलीब’। यह बहुत आम-सी लगने वाली कहानी है और सच पूछिए तो यह कहानी इस संग्रह की दूसरी कहानियों के मुक़ाबले में उतनी गहराई से शायद असर न कर पाए, मगर इसकी अहमियत यह है कि यह हज़ारों बरस के फैले हुए ज़माने में अलग-अलग मसीहाओं के साथ ज़माने के किए गए सुलूक और फिर उनकी पूजा के ढोंग को उजागर करती है।
साहिर लुधियानवी ने अपनी नज़्म ‘जश्न-ए-ग़ालिब’ में कहा था :
गांधी हो कि ग़ालिब हो इंसाफ़ की नज़रों में
हम दोनों के क़ातिल हैं, दोनों के पुजारी हैं
यही बात इस कहानी में बड़े सलीक़े और एक ज़माने की सिलसिलेवार तरतीब से कही गई है। इसी तरह ‘इक्कीसवीं सदी के पंचतंत्र में बुद्धिजीविता उर्फ़ अच्छे दिनों की तलाश भी’ एक बहुत अनूठी कथा है। ऐसी कहानियों में एक क़िस्म के ‘माइक्रो फ़िक्शन’ का-सा लुत्फ़ होता है और उदय प्रकाश को इस में भी कमाल हासिल है।
‘बिजली का बल्ब और मौत का फ़ासला’ यह भी एक छोटे पैराए की ऐसी कहानी है, जिसमें मौत के अचानक सवार हो जाने के डर और इंसान के दुनिया से झट-पट रुख़सत हो जाने के अनोखे ख़याल से तारी होने वाले दुःख को दर्शाया गया है। मुझे इस कहानी को पढ़ते हुए नैयर मसूद की कई ऐसी कहानियाँ याद आईं, जिनमें इसी तरह के इंसानी ख़ौफ़ को रेखांकित किया गया है। ‘मौत’ यूँ भी लेखकों के लिए एक मु'अम्मे और एक पहेली की-सी हैसियत रखती है, इंसान की फ़ितरत में उसे क़ुबूल करने का हौसला आज तक ठीक तरह से पैदा नहीं हो पाया है।
मंटो ने तो इस पर बड़ी सख़्त टिप्पणी की थी और मौत को क़ुदरत की एक ख़ामी और बदसूरत चीज़ क़रार दिया था। पुनर्जन्म, मोक्ष, जन्नत, दोज़ख़, आफ़्टर-लाइफ़ या जो भी कुछ कह लें, ये सब हमारे इसी हौसले की कमी और पस्ती के दूसरे नाम हैं। ग़ालिब ने कहा था :
मौत का एक दिन मुअय्यन है
नींद क्यों रात भर नहीं आती
यह इसी तरह की बात है कि इंसान इस बारे में जितना सोचेगा, उतना इस सच से फ़रार के रास्ते ढूँढ़ निकालेगा।
बहरहाल, यह कहानी-संग्रह उदय प्रकाश के अफ़सानवी सफ़र की एक छोटी-सी झलक ही है, लेकिन इसके ज़रिए आप उन तक पहुँचने की रंगीन सीढ़ियों का पता लगा सकते हैं। मैंने उनकी बहुत सारी दूसरी और अहम कहानियाँ पढ़ी हैं, जो उनके लेखन के आकाश पर सूरज की तरह हमेशा चमकती रहेंगी।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
