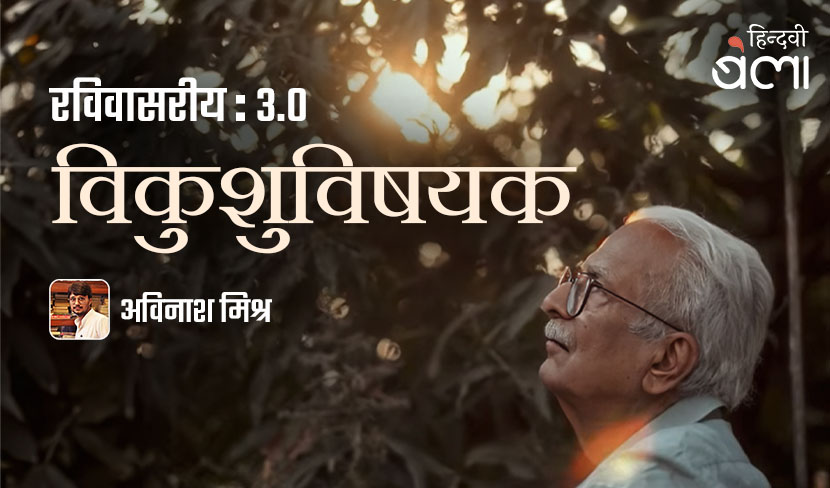रविवासरीय : 3.0 : इन पंक्तियों के लेखक का ‘मैं’
 अविनाश मिश्र
27 अप्रैल 2025
अविनाश मिश्र
27 अप्रैल 2025

• विषयक—‘‘इसमें बहुत कुछ समा सकता है।’’
इस सिलसिले की शुरुआत इस पतित-विपथित वाक्य से हुई। इसके बाद सब कुछ वाहवाही और तबाही की तरफ़ ले जाने वाला था।
• एक बिंदु भर समझे गए विवेक को और बिंदु दिए गए। इस प्रकार एक आकाश संभव हुआ—कहीं भी न अँटता हुआ, सब वक़्त सिर पर सवार... विषय ही विषय!
• विषयक-शिल्प इन पंक्तियों के लेखक को वर्ष 2019 के अंतिम महीने में आई महामारी के बाद 2020 में हुई देशव्यापी तालाबंदी के दरमियान मिला। वे मार्च-अप्रैल के अत्यंत अनिश्चित और भयभीत महीने थे। ये महीने बाक़ी महीनों से मिलकर इस अनिश्चितता और भय को और विस्तार और विशाल आकार दे रहे थे। यह सिलसिला कहाँ रुकेगा? इस प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं था। सब तरफ़ भ्रम था। यह यथार्थ—कविता, कथा और कथेतर की पकड़ से बाहर चला गया था। यह और कितना बाहर जाएगा, कहना कठिन था। इस काठिन्य में टिप्पणीकारों का काम आसान हो चुका था। वे व्याकुलता की नाट्यशाला में ख़ुद को रोज़-रोज़ काटते हुए व्यतीत हो रहे थे। वे संकट में नहीं, संकट के सुख में थे।
• डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स का महत्त्व कोविड-काल से पहले भी था, बल्कि बारहा यों भी महसूस किया गया कि यह महत्त्व प्रिंट में प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं से अधिक ही है। इस बीच कोविड ने जैसे सब जगह सब माध्यमों को प्रभावित किया, वैसे ही प्रिंट-पत्रिकाओं को भी। यह प्रभाव इसलिए और भी अधिक विकराल हो गया, क्योंकि हिंदी की लगभग सभी प्रिंट-पत्रिकाओं की अपनी रनिंग वेबसाइट्स/ब्लॉग्स/सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स नहीं थे। दरअस्ल, यह करना कभी उनकी प्राथमिकताओं में रहा नहीं और यह दुखद है कि अधिकांश मामलों में अब तलक नहीं है। वे लगभग न सीखने की सौगंध लेकर ही काम करते आए हैं और कर रहे हैं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें एक आलस्य, पिछड़ापन और जड़ता है।
डिजिटल माध्यमों को लेकर नाक-भौंह ही नहीं, अपना सब कुछ बहुत सिकोड़ने के बावजूद हिंदी साहित्यकारों और बौद्धिकों के बीच इसे लेकर पर्याप्त गंभीरता रही है। यह अलग बात है—वे शुरू से ही इस बात का पाखंड करते आए हैं कि वे इन माध्यमों को लेकर सहज और सीरियस नहीं हैं। लेकिन अब यह दिखावा व्यर्थ है और इसलिए तार-तार है।
इस स्थिति में जहाँ तक कोविड-काल में फँसे हिंदी साहित्यकारों और बौद्धिकों की डिजिटल उपस्थिति का प्रश्न है, मार्च-2020 से लेकर अब तक हिंदी के अनंत चैरकुट्य और प्रदर्शनप्रियता में हिंदी साहित्य और इसकी गंभीरता का; इसकी ज़रूरत और जगह का जितना नुक़सान फ़ेसबुक-इन्स्टाग्राम की लाइव सुविधा ने किया है, उतना आज तक किसी और माध्यम ने नहीं किया। इसने हिंदी लेखक को पूरी तरह एक्सपोज़ करके उसे हास्यप्रद, दयनीय और प्रचार-पिपासु बना दिया। साहित्यिक गोष्ठियाँ, साहित्योत्सव और इस सदी में प्रकट हुए अखंड अहमक़ों के वर्चस्व वाले लिट्-फेस्ट भी ये करते आए हैं; लेकिन उनमें कम से कम लेखक को यात्रा, जीवंत सामाजिक संपर्क और कभी-कभी मानदेय जैसे सुख तो मिलते हैं; पर फ़ेसबुक-इन्स्टाग्राम-लाइव और वेबिनारादि ने लेखकों-कलाकारों को लगभग मुफ़्त का माल बना दिया। वे इतने खलिहर, सर्वसुलभ, सहज उपलब्ध हैं; इस वास्तविकता के उद्घाटन का श्रेय कोविड-काल, फ़ेसबुक-इन्स्टाग्रामादि की लाइव सुविधा, वेबिनारादि के साथ-साथ हिंदी साहित्य और संस्कृति-जगत की कोरोजीवी प्रतिभाओं को जाता है।
महामारी में और संभवतः कभी भी लाइव न आने का निर्णय इन पंक्तियों के लेखक ने बहुत आरंभ में तब ही कर लिया था, जब एक रोज़ लॉकडाउन में ‘राजकमल प्रकाशन समूह’ के फ़ेसबुक पेज पर लाइव से जूझती एक छवि को कुछ देर के लिए देखा था। अनद्यतन और अमरता की अड़चन से ग्रस्त बुज़ुर्गों को यहाँ क्या ही कहा जाए; लेकिन इसके बाद जब कई शोला जवान और नाज़ुक प्रतिभाएँ अपना क़ीमती और युवा वक़्त बार-बार फ़ेसबुक लाइव में गँवाती दिखीं, तो उन्हें देखकर दुख कम—एक मीठी ख़ुशी अधिक होती रही! इस मीठी ख़ुशी को केवल वही समझ सकता है, जिसने लॉकडाउन के दिनों में अपना समय कुछ अपरिहार्य कामों के साथ-साथ रचने-पढ़ने में लगाया हो।
यह दुर्भाग्य है कि लिखने से पहले लिखे को बेच लेने की व्यवस्था कर लेने वाले युग में; हिंदी की कथित मुख्यधारा को यह भी समझ में नहीं आया कि ‘हिन्द युग्म’ के लेखक-अलेखक जिन्हें प्रचार-प्रसार का सर्वाधिक ज्वर चढ़ता रहता है, वे क्यों कोविड-काल में फ़ेसबुक-इन्स्टाग्राम के लाइव प्रसारणों और वेबिनारादि से क़रीब-क़रीब दूर ही रहे। हिंदी की यह कथित मुख्यधारा फ़ेसबुक के उन फ़ेसों की शनाख़्त भी नहीं कर पाई, जो लाइव की वकालत करते हुए हिंदी की गोबराट्टालिका के गिरिराज बने रहे!
• यहाँ आकर इस स्थिति को भी समझना होगा कि डिजिटल माध्यमों ने जन, जनवादियों और जनविरोधियों तीनों को ही हड़बड़युक्त, अति उत्तेजित और त्वरित तौर पर प्रतिक्रियामय बनाया है। इसने धैर्यशीलता, विचारोत्तेजकता और सहिष्णुता सरीखे मूल्यों को लगभग विदाई दे दी है। आज डिजिटल माध्यमों पर सक्रियता और इन मूल्यों का निर्वाह एक साथ असंभव है। इस दृश्य को निरर्थक किस्म की विवादात्मकता ने भी बहुत ख़राब अर्थों में असर-अंदाज़ किया है। अब कोई भी मुँह उठाकर भाषा और साहित्य के बारे निर्णायक राय दे सकता है! इसके लिए साहित्य-साधक होना तो छोड़िए, अब साहित्य-रसिक होना भी ज़रूरी नहीं रहा!
• मिख़ाइल नईमी की ‘द बुक ऑफ़ मिरदाद’ के प्रथम और द्वितीय अध्याय में ‘मैं’ शब्द के प्रयोग पर बहुत सारी विचारणीय पंक्तियाँ हैं। यह पुस्तक जिस परिवेश में घटित होती है; उसमें सभी भिक्खुओं के लिए बातचीत के दौरान जितना संभव हो सके, ‘मैं’ शब्द के प्रयोग के निषेध का प्राचीन नियम है। प्रथम अध्याय में जब प्रधान महंत और वरिष्ठ भिक्खु [शम आदम] एक सामूहिक चर्चा के दौरान इस निषिद्ध शब्द—‘मैं’—का बार-बार प्रयोग करते हैं और टोके जाने पर भी सँभलते-रुकते नहीं हैं, तब वहाँ इस नियम पर ही बहस होने लगती है। यह बहस धीरे-धीरे आरोप-प्रत्यारोप में बदलती है और आरोप-प्रत्यारोप हंगामे में—जहाँ बोला तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन सुना-समझा कुछ भी नहीं जाता। अंततः सबकी नज़रें मिरदाद पर आकर थम जाती हैं, जिन्होंने सात सालों से कभी अपना मुँह नहीं खोला था। इसके बाद अगले यानी दूसरे अध्याय में मिरदाद ‘मैं’ पर एक अद्भुत प्रवचन देते हैं। इस प्रवचन की याद यहाँ रविवासरीय : 3.0 के इस अंतिम स्तंभ में इसलिए आई कि इन पंक्तियों के लेखक ने अपनी अब तक की सारी लिखाइयों में ‘मैं’ शब्द के प्रयोग से बचने की भरसक कोशिश की है। वह बहुत बार असफल हुआ है। एक सतत जारी असफलता में, यह असफलता पैबंद सरीखी है।
विषयकविषयक लिखते हुए भी इन पंक्तियों के लेखक ने मैं शब्द का निषेध करने का संकल्प किया, लेकिन कुछ माह पूर्व एक शोधार्थी [जन्म : 1988] ने इन पंक्तियों के लेखक की ही एक पुस्तक के संदर्भ में इस तरफ़ ध्यान दिलाया कि मैं के निषेध के लिए इन पंक्तियों के लेखक का प्रयोग करना शब्द और वक़्त की बहुत बर्बादी है... जैसे मुझे यानी इन पंक्तियों के लेखक को पता ही नहीं कि शोधार्थियों का वक़्त कितना क़ीमती है!
बहरहाल, इन पंक्तियों का लेखक आगे के बिंदुओं में मैं शब्द का निषेध कर पाने में एक बार फिर से असफल होने जा रहा है।
• विषयकारंभ जब हुआ, तब सब तरफ़ लिखने-पढ़ने की लड़ाई बदल रही थी और कविता की समझ और गद्य की पहचान भी। इस प्रचलन में कथेतर बह रहा था और मेरे भीतर—कहनेतर।
मैं अपने मस्तिष्क में एक महाभारत रचता रहता था...
• मुझे अफ़सरों की कविताओं से, अध्यापकों की आलोचना से और पत्रकारों की कहानियों से चिढ़ थी। ये तीनों ही प्रजातियाँ साहित्य की शत्रु हैं और साहित्यकार होना चाहती हैं।
• मैं यहाँ कुछ और आत्म-स्तवन में जाऊँ, तब कह सकता हूँ कि मैं कहने को कहने की सारी शैलियों में समोना चाहता था। मुझे पता नहीं था कि इस सब कुछ का अंततः क्या होना था या नहीं होना था। इस असमंजस में बहुत कुछ कहना हुआ—इस तरह का कि जिसमें अब तक सिर्फ़ रहना ही हुआ।
• विषयक-विस्तार में मेरे समकालीन साहित्य के नियम मेरे ज़्यादा काम नहीं आए। समकालीनत्व में रंग सीमित, ख़तरे प्रत्याशित और मार्ग तय थे। मैं इस संदर्भ में अ-समकालीन होना चाहता था। मैं सचमुच का सांस्कृतिक-साहित्यिक भार चाहता था। मैं चाहता था कि मैं अपने विषय का मर्मज्ञ दिखने लगूँ। मैं चाहता था कि मैं दुखने लगूँ।
• लेखकों के लिए लेखन क्या है, इसका एक रूढ़ और रोमानी उत्तर ही अब भी सबसे सच्चा और प्रासंगिक है; और वह यह है कि लेखकों के लिए लेखन साँस लेने जैसा है। लिखना या लिखने के बारे में सोचना बंद कर देने पर भी; जीते चले जाने वाले व्यक्तित्व और चाहे जो कुछ हों, लेखक नहीं हो सकते। यह दुर्लभ आस्था किसी रचनाकार में तब उत्पन्न होती है, जब वह पूरी तरह सब समय अपनी कला-रचना में डूबा रहता है। इस डूब के बाहर दीखता हुआ भी, वह इस डूब में ही होता है। जब तक साँसें समाप्त नहीं हो जातीं, इस डूब से मुक्ति नहीं।
मैं लिखने के लिए बिल्कुल सुबह का, सूर्योदय से पूर्व का, होती हुई सुबह का समय पसंद करता हूँ।
मैं इन सुबहों में सपाटपन से दूरी चाहता था।
मैं सारी दिशाएँ चाहता था।
मैं सारी दिशाओं से फूटती हुईं और बहुत सारी दिशाएँ चाहता था।
मैं अब इस सिलसिले को यहीं विराम दे रहा हूँ—इस विषयक को अंतिम करते हुए।
मैं मूलतः कवि हूँ और कभी-कभी मुझे लगता है कि मैं इस पृथ्वी पर अंतिम कवि हूँ। यह स्थिति एक व्यापक अर्थ में मुझे उस समूह का एक अंश बनाती है, जहाँ सब कुछ एक लगातार में अंतिम हो रहा है। मैं इस यथार्थ में बहुत कुछ बार-बार नहीं, अंतिम बार कह देना चाहता हूँ। मैं अंतिम रूप से चाहता हूँ कि सब अंत एक संभावना में बदल जाएँ और सब अंतिम कवि पूर्ववर्तियों में।
धन्यवाद!
•••
अन्य रविवासरीय : 3.0 यहाँ पढ़िए — गद्यरक्षाविषयक | पुष्पाविषयक | वसंतविषयक | पुस्तकविषयक | प्रकाशकविषयक | प्रशंसकविषयक | भगदड़विषयक | रविवासरीयविषयक | विकुशुविषयक | गोविंदाविषयक | मद्यविषयक | नयानगरविषयक | समीक्षाविषयक | बेलाविषयक | विश्वकविताविषयक
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
24 मार्च 2025
“असली पुरस्कार तो आप लोग हैं”
समादृत कवि-कथाकार विनोद कुमार शुक्ल 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। वर्ष 1961 में इस पुरस्कार की स्थापना ह
09 मार्च 2025
रविवासरीय : 3.0 : ‘चारों ओर अब फूल ही फूल हैं, क्या गिनते हो दाग़ों को...’
• इधर एक वक़्त बाद विनोद कुमार शुक्ल [विकुशु] की तरफ़ लौटना हुआ। उनकी कविताओं के नवीनतम संग्रह ‘केवल जड़ें हैं’ और उन पर एकाग्र वृत्तचित्र ‘चार फूल हैं और दुनिया है’ से गुज़रना हुआ। गुज़रकर फिर लौटना हुआ।
26 मार्च 2025
प्रेम, लेखन, परिवार, मोह की 'एक कहानी यह भी'
साल 2006 में प्रकाशित ‘एक कहानी यह भी’ मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध आत्मकथा है, लेकिन मन्नू भंडारी इसे आत्मकथा नहीं मानती थीं। वह अपनी आत्मकथा के स्पष्टीकरण में स्पष्ट तौर पर लिखती हैं—‘‘यह मेरी आत्मकथा
19 मार्च 2025
व्यंग्य : अश्लील है समय! समय है अश्लील!
कुछ रोज़ पूर्व एक सज्जन व्यक्ति को मैंने कहते सुना, “रणवीर अल्लाहबादिया और समय रैना अश्लील हैं, क्योंकि वे दोनों अगम्यगमन (इन्सेस्ट) अथवा कौटुंबिक व्यभिचार पर मज़ाक़ करते हैं।” यह कहने वाले व्यक्ति का
10 मार्च 2025
‘गुनाहों का देवता’ से ‘रेत की मछली’ तक
हुए कुछ रोज़ किसी मित्र ने एक फ़ेसबुक लिंक भेजा। किसने भेजा यह तक याद नहीं। लिंक खोलने पर एक लंबा आलेख था—‘गुनाहों का देवता’, धर्मवीर भारती के कालजयी उपन्यास की धज्जियाँ उड़ाता हुआ, चन्दर और उसके चरित