हिंदू कॉलेज में मेरे अंतिम दिन
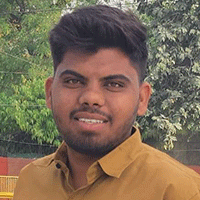 प्रमोद प्रखर
21 मई 2024
प्रमोद प्रखर
21 मई 2024

समय गुज़रता है...ना जल्दी, ना देर से, बस अपनी ही रफ़्तार से। यह जानते हुए भी लग रहा है कि पिछले तीन साल कितनी जल्दी गुज़र गए। कॉलेज का सफ़र रह-रहकर याद आ रहा है। उम्मीदों से शुरू हुआ सफ़र निराशा के बवंडर से होते हुए भावुकता तक पहुँचता है, उदास कर देता है। क्यों? पता नहीं।
ग्रेजुएट होने आए थे, होने भी वाले हैं। फिर यह मायूसी क्यों? वह भी ऐसी जो रंग-बिरंगी टिप्पणियों से ढकी सफ़ेद शर्ट पहनने से भी मिट नहीं रही है और ना ‘फेयरवेल’ के मनमोहक बुलावे देखकर। सच है भाई! समय रेत-सा नहीं फिसलता बल्कि सूरज-सा मन मोहते हुए उगता है, तपन देता हुआ चढ़ता है और फिर शांत होते-होते ऐसा डूबता है कि एक बिंदु पर व्यक्ति स्थिर होकर सोचने पर मजबूर हो ही जाता है।
एक
यह राजस्थान की एक अक्टूबर की दुपहर है।
ग़मगीन! गाँव में रेवड़ चराने वाला सोलह-सत्रह साल का एक लड़का मर गया। टाँके में डूबने से। लाश अभी-अभी आई है। चारों तरफ़ मातम पसरा है। भीगी-नम आँखें एक रेखीय होकर श्मशान की तरफ़ बढ़ रही है। अंतिम क्रियाएँ हुईं। लोग लौटे, इस लौटती भीड़ का हिस्सा मैं भी था। उदास और शोकमग्न लेकिन घर पहुँचते-पहुँचते फोन में नोटिफ़िकेशन आया। चैक किया। दिल थम गया। यह दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाख़िले का रिजल्ट था।
उस समय सूतक पर गहरा विश्वास रखने वाला लड़का भला कैसे इस रिजल्ट को चैक कर लेता! घर आया। नहाया। रिजल्ट देखा—लगा कि सपना पूरा हो गया। मनचाहे कॉलेज में एडमिशन। मनचाहा—मतलब सिर्फ़ मनचाहा। कॉलेज देखना तो दूर, मैं तब तक कभी दिल्ली भी नहीं आया था। शाम होते-होते एडमिशन कंफ़र्म हुआ। पिता ने मज़दूरी से कमाएँ कुछ हज़ार दिए। सॉरी! उनकी आय के हिसाब से ‘कुछ’ नहीं बल्कि ‘बहुत कुछ हज़ार’। ई-मित्र पर फ़ीस जमा हुई। एडमिशन कंफ़र्म! लेकिन, ऐसा भी कभी होता है कि सपने आसानी से पूरे हो जाए।
इस केस में भी ऐसा ही होना था। एक कठिनाई बाक़ी थी, जो दूसरे दिन उगते सवेरे के साथ आई। एडमिशन-पोर्टल की ओर से एक और नोटिफ़िकेशन—‘Your admission has been cancelled!’. यह परेशानी भर नहीं बल्कि आँखों में नमी का निमंत्रण भी था। आनन-फ़ानन में कॉल हुए। पँद्रह बाई दस का बड़ा मकान मेरे लिए रणभूमि बन गया।
फ़ाइनली, कॉलेज एडमिशन के इंचार्ज़ से बात हुई और फिर डिपार्टमेंट की टीआईसी से। एक डॉक्यूमेंट की कमी थी। उस दिन पहली बार मेल किया। वो भी इंग्लिश में—कॉलेज ने एडमिशन से पहले ही एक कला सिखा दी। व्हाट्सऐप से पीछे की यह कला, मुझे उस दिन व्हाट्सऐप से बहुत आगे की जान पड़ी। शाम आते-आते सब ठीक हुआ। एडमिशन हो गया।
लेकिन यह क्या? क्लासेज़ तो ऑनलाइन ही होनी हैं। ख़ुशी थोड़ी कम हो गई। एक उम्मीद थी कि कभी तो कॉलेज खुलेगा। तब जाएँगे।
सबसे ख़ास बात—उस दिन पहली बार मैंने मम्मी-पापा को उदास देखा। क्यों? इसका जबाब तो आगे मिलना था।
दो
धुँध भरी सुबह। फ़रवरी का महीना।
मैं जल्दी जागा हूँ। दिन भी 14 फ़रवरी का था। अब कहूँ तो क्रश को प्रपोज़ करने का और तब कहता तो—सेटिंग को सेट करने का। मोहब्बत का बुलावा आ चुका है। आज दिल्ली निकलना है। परसों कॉलेज खुल जाएँगे। ट्रेन की टिकट किसी सीनियर ने बुक करवा दी है। मुझे तो आती नहीं। गाँव का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन अस्सी किलोमीटर दूर है। वहीं से ट्रेन है। एक सस्ते से ट्रोली बैग में ठूँस-ठूँसकर सामान भरा जा चुका है।
पिता ने पास बुलाकर एक नोटों की गड्डी दी और ख़ूब सारी हिदायतें। गड्डी सँभालते हुए लगा कि बेटे की मोहब्बत सिर्फ़ बॉलीवुड फ़िल्मों में बाप को परेशानी नहीं देती। यह धोरों में भी उतनी ही प्रैक्टिकल बात है।
चूरू से दिल्ली महज़ पाँच घंटे का रास्ता है। मगर गाँव के किसी मज़दूर के घर पैदा होने वालों को शायद पीढ़ियाँ लग जाती हैं। यह रास्ता तय करने में। इन पाँच घंटों ने सिखाया कि ‘एकांत’ और ‘अकेलापन’ एक नहीं बल्कि अलग-अलग बातें हैं। अकेलापन शून्यता भरता है या ऋण-वृद्धि की ओर ले जाता है, जबकि एकांत कुछ और होता है। थोड़ा सकारात्मक और शुभ।
पाँच घंटे बीते—ट्रेन सराय रोहिल्ला उतरी। बंगाल के एक सीनियर आने वाले थे। कॉलेज-सीनियर नहीं। किसी एक भाई जी के जानकार—‘भैया’ शब्द मेरी डिक्शनरी में बाद में जुड़ा। स्टेशन की भीड़ को देखकर लगा कि इन सबको मिलाकर ‘धीरवास बड़ा’ तो नहीं पर कम से कम एक ‘धीरवास छोटा’ तो और बसाया जा सकता है।
भैया आए! रिक्शा लिया। ना साज-सज्जा। ना कोई म्यूज़िक और ऊपर से कानफोड़ू शोर के साथ जाम। मैं इन सबसे दूर किसी फ़िल्मी हीरो-सा प्रदूषण भरी हवा में बाल-उड़ाने की झूठी कोशिशें करता रहा। कमरे पर पहुँचे। गलियाँ देखीं। कल्चरल शॉक तो पता नहीं लेकिन कंस्ट्रक्शन शॉक लग चुका था।
उस रात लगा कि अगर सुबह का नाश्ता गाँव में, लंच ट्रेन में और डिनर दिल्ली में हो सकता है तो कुछ भी संभव है। सब जैसा सोचा था—वैसा नहीं है, लेकिन कर लेंगे।
तीन
मई की चिलचिलाती दुपहर।
मैं पहाडगंज से नॉर्थ-कैंपस आया हूँ। कोई क्लास नहीं है लेकिन उस कमरे में क्या करता—जहाँ पाँच मज़दूर रहते हैं। रातभर ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और दिन में सोने आते हैं। मैं दिनभर कॉलेज रहता हूँ। कभी क्लासेज़ में, कभी लाइब्रेरी में, कभी कैंटीन में और कभी-कभी कॉलेज के बाहर रोड के सहारे बनी छोटी-छोटी बेंचनुमा दीवारों पर। सड़क-किनारे भटक रहा हूँ, तभी सामने ट्रैफ़िक के बीच पेन बेचती हुई माँ-बेटी को देखता हूँ।
दिमाग़ में कुछ मचलता है और फोन निकालकर किसी सोशल मीडिया हैंडल पर लिख रहा हूँ, “भटकते पाँव जब आराम माँगने लगते हैं, तो बस कहीं से ऑटो पकड़कर ‘हिंदू’ (डीयू का कॉलेज) के बाहर किसी दरख़्त के नीचे लगी किनारी-पट्टी पर बैठ जाता हूँ। इस चौवालिस डिग्री-सेल्सियस की तपती धूप में भी वही एक जगह है, जहाँ आकर कुछ सुकून मिलता है।
ध्यान आता है कि बोतल का पानी ख़त्म होने को है। उठता हूँ और ख़ुद को रामजस के सामने वाले DTC बस-स्टैंड की तरफ़ बेतरतीबी से घसीटते हुए चलता हूँ। वहीं हाइवे के बीचों-बीच फटी साड़ी और टूटी चप्पलें पहने एक अम्मा खड़ी हैं, जिसके एक हाथ में दस-बीस पेन और दूसरे हाथ में उसकी आठ-नौ साल की बेटी का हाथ है।
बेटी की हालत धूप की वजह सें बीमारों से बदतर नजर आती है, लेकिन अम्मा का ध्यान सिर्फ़ रेड-लाइड पर रुकती शीशाबंद चमचमाती कारों पर है। जिनके रुकते ही दारुण स्वर में एक ही अपील, “बाबूजी! पेन ले लो।। दो दिन से कुछ नहीं खाया।” गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं, अम्मा हट जाती है और अगली बार फिर यही सीन दोहराया जाता है।
फ़र्क़ बस अम्मा के पैरों और बेटी के चेहरे पर दिखता है। अम्मा के पैर दुगुनी तेजी से पेन बेचना चाहते हैं और बेटी का चेहरा मुरझाता चला जाता है। इन सबसे दूर मैं बस जड़वत होकर यह सब देख रहा हूँ, वह महिला इसे नोट करती है और ट्रैफ़िक से चिल्लाती है, “ओए! क्या देख रहा है। आगे जा ना।” शायद उसे लगता है कि ऐसा करके मैं उसकी हताशा, निराशा और घटती ऊर्जा का मज़ाक़ बना रहा हूँ, लेकिन वो नहीं जानती कि मैं उसमें ख़ुद के अंतर्मन की परछाई को निहार रहा हूँ।
चार
यह दिन सितंबर का है।
दिल्ली की आदत हो गई है। रहने में मुश्किल, बस की भीड़, सड़कों पर रेत की तरह जमा ट्रैफ़िक, मेट्रो की ठंडी हवा, रोटियों की जगह वेज़ रोल—समय ने सब सामान्य बना दिया है। कॉलेज आना-जाना नियमित होने लगा है। लोगों से जान-पहचान बढ़ी है। ज़िंदगी लोक से रॉक की तरफ़ बढ़ रही है लेकिन एक चीज़ कम है और वो है—कॉलेज पॉलिटिक्स। सबकुछ रास्ते पर आ जाए तब इंसान को व्यसन सूझने लगते हैं। राजनीति—जो ख़ुद में एक व्यसन है।
दोस्तों के बीच हॉस्टल की चर्चा छिड़ी। बॉयज़ हॉस्टल रिनोवेशन के नाम पर शुरुआत से ही बंद था। कॉलेज-एडमिन को लग रहा था कि यह कोई बड़ा मसला है नहीं। लाल-दीवारों में बसने वालों को अक्सर किताबी-समस्याएँ ही दिखती हैं, ज़मीनी नहीं। हमने ज़मीन पकड़ने की तैयारी की। एक वीडियो बनाया। ‘हल्ला बोल, हॉस्टल खोल’ के पोस्टर छपे और दूसरी सुबह एक भीड़ प्रिंसिपल ऑफ़िस के सामने। हंगामा मच गया।
कोविड के बाद यह पहली बार था कि यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में धरना हो रहा था। भाषण हुए, नारे लगे। प्रिंसिपल कभी अपने ऑफ़िस, कभी हमारे पास, कभी स्टाफ़ रूम में। आँसू और इमोशन सब हुआ—हमने कुछ ठीक ही खिचड़ी पका दी थी, लेकिन प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल ठहरीं—कितनों को ही पानी पिलाया था।
शाम होते-होते एक नोटिस बच्चों को पकड़ाया। सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे स्टूडेंट्स का कॉलेज होने का दंभ भरने वाले कॉलेज के बच्चे नोटिस लेकर भाग छूटे। बड़ी मुश्किल से नोटिस की छीना-झपटी हुई। फट गया। जोड़कर पढ़ा। लिखा था—Renovation work of Hindu College Boys Hostel will start from next week.
पहले मुँह से गाली निकली। प्रिंसिपल के लिए नहीं साथ वालों के लिए। पर क्या किया जा सकता था! बाहर जाएँ तो ठहरना नामुमकिन होता है, लेकिन संतोष हुआ कि विश्वविद्यालय में धरने वाली छात्र-राजनीति शुरू तो हुई। उस शाम इंस्टाग्राम की स्टोरीज़ फोटोज़ से लद गई। एक दोस्त नेता बना और हम रणनीतिकार। किसी एक स्टोरी ने नीली शर्ट वाली फ़ोटो पर लिखा—PK—not by name but work.
एक दोस्त के मुताबिक़, प्रिंसिपल के बेहद ख़ास और हिंदी विभाग के प्रोफ़ेसर ने दूसरे दिन अपनी क्लास में ज़िक्र करते हुए कहा भी, “वो नीली शर्ट वाला लड़का, बड़ा सुलझा लगता है। बोलता अच्छा है।”
पाँच
इसी सप्ताह का कोई दिन।
आज कॉलेज आया हूँ। सीमा मैम की आख़िरी क्लास थी। तालीम सर की भी। चारों तरफ़ भावुकता पसरी हुई है। कोई जूनियर जब आकर कहता है, “भैया! अब तो बस दो-चार दिन और!” तो मन करता है कि बोल दें अगले सेमेस्टर में मिलेंगे। पर अब कहाँ अगला सेमेस्टर। अब तो सिर्फ़ फ़ेयरवेल बचा है। कॉलेज की सोसायटियों ने भी विदा-अनुभव लिखवा लिए हैं। कल एक सोसायटी का फ़ेयरवेल है, परसों डिपार्टमेंट का और फिर एक सोसायटी का। उसके बाद कुछ दिन की छुट्टियाँ, परीक्षाएँ और सबके अपने-अपने रास्ते।
किसी को रेलवे स्टेशन जाना है तो किसी को ओल्ड राजेंद्र नगर लेकिन सभी उदास हैं। जिन कमरों में बैठकर इस वक्त के जल्दी ख़त्म होने की दुआएँ माँगा करते थे, आज वहीं बैठकर सोच रहे हैं कि कुछ दिन और...! लेकिन समय तो अपनी रफ़्तार से चलता है। आपको भी चलाता है। सिखाता है।
इस समय और इस संस्थान ने बहुत कुछ सिखाया है। भाषा, पढ़ना, लिखना। खान-पान के तौर-तरीके़। अलग-अलग संस्कृतियाँ। हेयर स्टाइल। बोलना। प्रेजेंट करना और भी कितना कुछ! हालाँकि कहा जा सकता है, दिल्ली रहे तो सीख गए। लेकिन मैं दिल्ली रहा ही क्यों? क्योंकि 'हिंदू' में पढ़ा। 'हिंदू' ने अच्छे छात्र से ज़्यादा संजीदा इंसान बनाया। इतना कि अब मैं किसी दोस्त की महिला-मित्र को कनखियों से ताकता नहीं बल्कि सम्मान से ‘हैलो’ और कंफ़र्टेबल होने पर हाथ भी मिला लेता हूँ।
कैंटीन में काम करने वालों को ‘भैया/दादा’ बुलाने लगा हूँ। ऊँची आवाज़ में बात आवश्यक होने पर ही करता हूँ। सीखने का क्रम जारी है। अगले संस्थान में भी बहुत कुछ सीखेंगे। पर बहुत कुछ भूलेंगे नहीं। वह अनलर्न 'हिंदू' बहुत हद तक करवा चुका है। इन सबके बावजूद जब डीपीएस से आए किसी दोस्त से कॉलेज की आलोचना सुनता हूँ, तो लगता की अगर 'हिंदू' नहीं आता तो क्या कभी इन बातों को सुन और समझ पाता? शायद नहीं। यह सब सोचते हुए मालूम चला कि आख़िर क्यों तमाम कमियों-ख़ामियों के बावजूद क्यों ज़रूरी है—इन सार्वजनिक संस्थानों का बचा रहना। अगर ऐसे संस्थान ना होते तो मैं ना उनके पास बैठ पाता और न कहा समझ पाता।
अब तो मन होता है कि एग्जाम ख़त्म होने के बाद गाँव जाकर पापा को धन्यवाद कहूँ—उनके संघर्ष के लिए। एड्डी पर कभी ना ठीक होने वाली चोट लिए काम पर निकलने वाला मेरा पिता—मेरा हीरो है। मेरे संघर्ष में मुझसे ज़्यादा उनका संघर्ष है। 'हिंदू' न आता तो यह कभी नहीं समझ पाता।
आज ही किसी ने पूछा भी कि क्या 'हिंदू' को भूल जाओगे? हाँ कर देता, अगर मुझे पीट-पीटकर ‘क’ लिखना सिखाने वाले शिक्षक को भूल गया होता। अब सारी तकलीफ़ें, नयापन, हैरानियाँ और परेशानियाँ और पिटाई नज़र आती हैं। सबको इसी तरह पिटना ही होता है। किसी एक पीढ़ी को थोड़ा ज़्यादा। ख़ुशकिस्मत हूँ कि मेरे परिवार की वो पहली पीढ़ी—मैं हूँ।
बाक़ी हिंदू रहेगा। ग्रेजुएशन की किसी मार्कशीट से ज़्यादा दिल में। सीखने-सिखाने-समझने की सीढ़ी बनकर। लोगों से ज़्यादा गलियारे याद आएँगे। मुझे ही नहीं सारे हिंदू वालों को हिंदू याद आता है। यहाँ एक लाइन चलती है—Once a Hinduite, Always a Hinduite!
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
