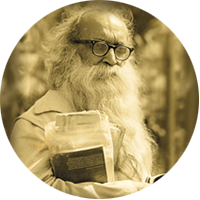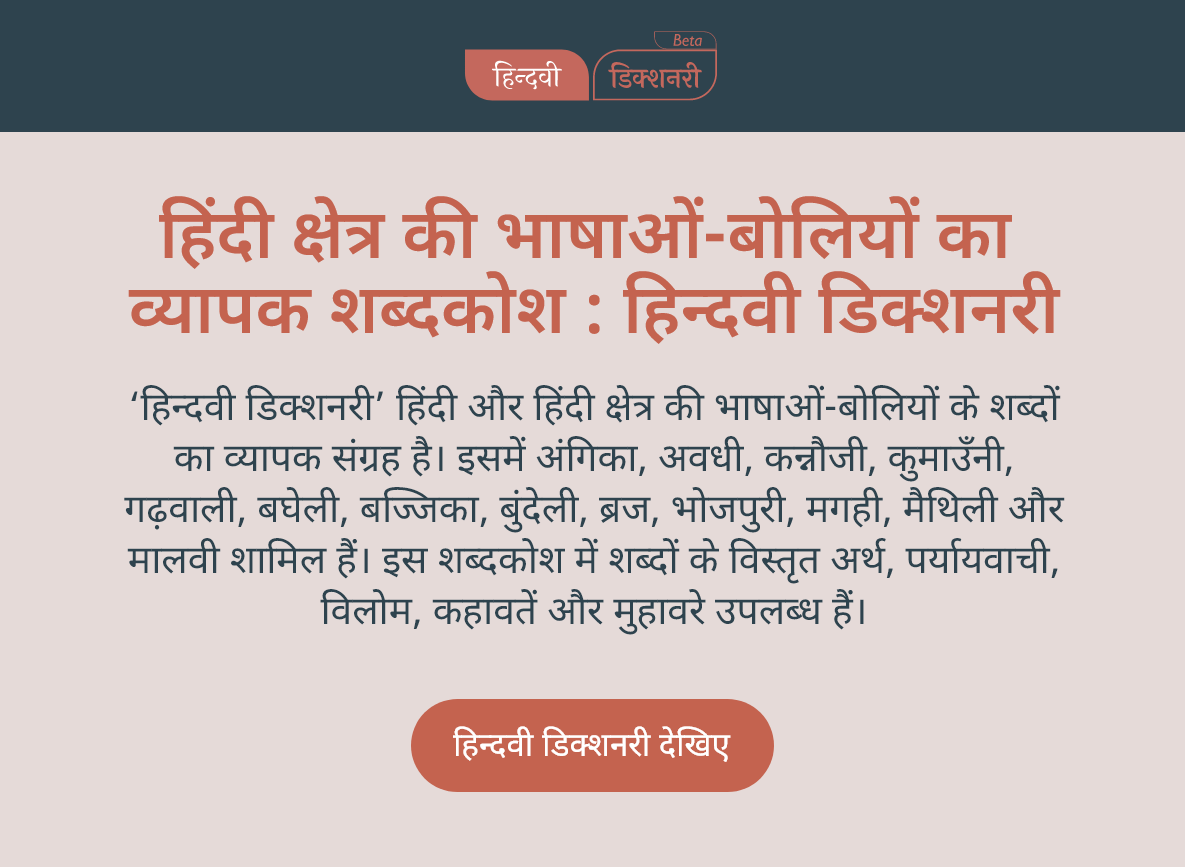गाजर के गर्म हलवे की ख़ुशबू से सारा कमरा महक उठा था और यदि किसी दावत की सबसे बड़ी ख़ूबी यही है कि हर खाना बड़े सलीके से तैयार किया जाए और 'मामूली से मामूली चीज़ में भी एक नया ही ज़ायका पैदा कर दिया जाए तो निस्संदेह दिल्ली की वह दावत मुझे सदा याद रहेगी।
इतनी भी क्या ख़ुशी है, मैं सोच रहा था, इतना तो नफ़ासत हसन पहले भी कमा लेता होगा। डेढ़ सौ रुपए के लिए उसने अपनी आज़ादी बेच दी और अब ख़ुश हो रहा है। वह तो शुरू से बाग़ियाना तबीयत का आदमी मशहूर है। उसकी कहानियाँ प्रगतिशील साहित्य में विशेष स्थान पाती रही हैं। फिर यह नौकरी उसने कैसे कर ली! ग़रीबों पर ज़ुल्म ढाए जाते हैं, ज़िंदगी की हतक की जाती है, सरमायादार मकड़ी की तरह बराबर अपना जाला बुनते रहते हैं और ग़रीब किसान-मज़दूर आप-से-आप इस जाले में फँसते चले जाते हैं—इन विचारों का मालिक आज ख़ुद मक्खी की तरह इस जाले में फँस गया और इस ख़ुशी में यार-दोस्तों को दावत दे रहा है। पर मैंने अपने विचारों का असर अपने चेहरे पर ज़ाहिर न होने दिया।
दावत में कई लेखक सम्मिलित थे। मैं सोचने लगा—हिंदुस्तान की आज़ादी के संबंध में इन हैट पहनने वाले लेखकों से अधिक सहायता की आशा न रखनी चाहिए। ब्राउनिंग का विचार— 'कुछ चाँदी के सिक्कों के बदले में वह हमें छोड़ गया।' मेरी कल्पना में फैलता चला गया। इन प्रतिक्रियावादियों को यह गुमान कैसे हो गया कि वे प्रगतिशील साहित्य की चर्चा करके सुनने वालों की आँखों में धूल डाल सकते है? कहाँ आज़ादी का वास्तविक आदर्श, और कहाँ यह चाँदी की ग़ुलामी! नफ़ासत हसन के गोरे चेहरे पर हँसी नाच रही थी। सच पूछो तो यह हँसी मुझे बड़ी भयानक दिखाई देती थी।
गाजर का हलवा सचमुच बहुत स्वादिष्ट था और मेरे विचारों पर छा रहा था। चुंबक इतना समीप हो और लोहे के कण खिंचे न चले आएँ, यह कैसे हो सकता है? यदि यह हलवा न होता तो मैंने नफ़ासत हसन को और भी अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखा होता।
बहुतों के नामों से में अपरिचित था (यह और बात है कि कई चेहरे मेरे लिए नए न थे।) विशेष रूप से मौलाना नूर हसन आरज़ू को तो इससे पहले कभी फ़ोटो में भी न देखा था। उनकी आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगी। शीघ्र ही मैंने उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया। यह अनुभव होते देर न लगी कि उन्हें ऐसी-ऐसी युक्तियाँ याद हैं कि अवसर आने पर वे अपने प्रतिद्वंद्वी को घास के तिनके के समान अपने पथ से उड़ा दें। आयु से वे कोई वृद्ध न थे, अधेड़ ही थे। पर नए युग से इतना ही संबंध रखते थे कि सरकारी नौकरी के कारण पाजामे और शेरवानी से मुँह मोड़कर अँग्रेज़ी फ़ैशन का सूट पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था।
बर्फ़ में लगी हुई गँडेरियों के ढेर पर सब लेखक बढ़-बढ़कर हाथ मार रहे थे। जैसे ही गॅँडेरी का गुलाब में बसा हुआ रस गले से नीचे उतरता, मौलाना आरजू की आँखों में एक नई ही चमक आ जाती।
नफ़ासत हसन कह रहा था—ये गॅँडेरियाँ तो ख़ासतौर पर मौलाना ही के लिए मँगवाई गई हैं।
ख़ूब! मौलाना बोले—और गाजर का हलवा भी शायद मेरे ही लिए बनवाया गया था।
जी हाँ!
नफ़ासत हसन की बेबाक निगाहें मौलाना की शोख़ आँखों में गड़कर रह गईं। कुछ लोगों का विचार था कि उसे अपने विभाग में नौकरी दिलाने में मौलाना का बहुत हाथ था, पर स्वयं नफ़ासत हसन ऐसा आदमी न था कि कल्पना में भी किसी का आभार मान सकता। उसका विचार था कि स्वयं समय की करवट के कारण ही वह इस नौकरी को प्राप्त कर सका है। और गाजर का स्वादिष्ट हलवा और गुलाब में बसी हुई गँडेरियाँ किसी मौलाना का एहसान उतारने के ख़याल से पेश नहीं की गईं।
मौलाना इधर बहुत मोटे हो गए थे और वे हैरान थे कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहर में लगातार कई बरस गुज़ारने के बाद भी नफ़ासत हसन ने अपनी बैठक में एक-आध बड़ी कुर्सी रखने की आवश्यकता क्यों महसूस न की थी। अब तक बढ़इयों ने बड़ी-बड़ी कुर्सियाँ बनाना बिल्कुल छोड़ तो नहीं दिया। यह और बात है कि नए ज़माने के लोग अब कभी इतने मोटे न हुआ करेंगे। अपनी गोल-गोल घूमती हुई आँखें उन्होंने मेरी तरफ़ फेरी और मैंने देखा कि उनमें ग़रूर और ग़म गले मिल रहे हैं और वे बीते वक़्तों को वापस आता देखने के लिए बेक़रार हो रहे हैं।
धीरे-धीरे महफ़िल छिदरी होती गई। नए मित्र यह विचार लेकर लौटे कि नफ़ासत हसन एक आनंदप्रिय और मित्रों के काम आने वाला आदमी है, यह अलग बात है कि वह रस्मी शिष्टाचार में नहीं पड़ता। है भी ठीक—मित्रता होनी चाहिए स्वतंत्र कविता-सी—तुक और छंद के बंधन से मुक्त!
मौलाना बराबर जमे हुए थे। मुझसे पूछने लगे, साहब,, सॉमरसेट मॉम का मुताला किया है आपने?
उन्होंने यह बात इस लहज़े में पूछी थी कि मुझे गोलमोल जवाब पर उतरना पड़ा—साहब, कहाँ तक मुताला किया जाए। अनगिनत पुस्तकें हैं और अनगिनत लेखक। अब में सॉमरसेट मॉम का ध्यान रखूँगा।
तो यह कहिए न कि आपने सॉमरसेट मॉम की कोई किताब नहीं पढ़ी।
अब में समझा कि सॉमरसेट मॉम कोई लेखक हैं। मैंने झेंपते हुए कहा—जी हाँ, यही समझ लीजिए।
तो इसका यही मतलब हुआ न कि आपने योंही उमर ज़ाया की। इस पर नफ़ासत हसन बिगड़ उठा। गर्मागर्म बहस छिड़ गई। पता चला कि मौलाना ने नफ़ासत हसन के लिए सॉमरसेट मॉम की चर्चा की थी। एक दिन स्वयं नफ़ासत हसन ने यही प्रश्न मौलाना से किया था और जब उन्होंने मेरी तरह बात टालनी चाही तो वह कह उठा था, 'तो इसका यही मतलब हुआ न कि आपने अब तक यों ही उमर जाया की।’
इधर मौलाना ने अँग्रेज़ी साहित्य में प्रवेश कर लिया था, पर नफ़ासत हसन अब तक यही समझता था कि यह केवल एक दिखावा है और अँग्रेज़ी साहित्य की नई प्रवृत्तियों से उन्हें कोई लगाव नहीं है। जब भी वह उनके हाथ में कोई अँग्रेज़ी पुस्तक देखता, उसके मन में व्यंग्य जाग उठता, जैसे साँप के सिर में ज़हर जाग उठता है। इस दिखावे की आख़िर क्या ज़रूरत है? बेहूदा दिखावा! नया रंग तो सफ़ेद कपड़े पर ही ठीक चढ़ता है। मौलाना बड़ी सरल और प्रभावमयी भाषा में कविता लिखते थे। लेख भी लिखते थे। कहानी के क्षेत्र में उन्होंने कोई यत्न न किया था। हाँ, जब कोई घटना सुनाते तो यही गुमान होता कि कोई कहानी जन्म ले रही है। और यदि उस समय कोई आदमी उनकी प्रशंसा कर देता तो खाहमखाह उनकी आँखों में बहुत ऊँचा उठ जाता। दाद पाकर ही वे दाद दे सकते हों, यह बात न थी। प्रायः वे किसी ऐसे मुआवज़े के बिना ही नवयुवक लेखकों की पीठ ठोंकते रहते थे। उनका यह सरपरस्ताना स्वभाव ही नफ़ासत हसन के समीप वह दोष था, जिसके कारण, जैसा कि उसका विचार था, न वह पुराने युग का प्रतिनिधित्व करने में समर्थ हुए थे और न नए युग से ही संबंध जोड़ सके थे।
नफ़ासत हसन जब भी मौलाना के विरुद्ध विष उगलता, मुझे यों लगता कि साहित्य का नया युग अपने से पहले युग का अपमान कर रहा है। यह तो अपना ही अपमान है। ऊपर से इसका घिनौनापन आँख से कितना ही ओझल क्यों न रहे, पर जब यह बात समझ में आ जाती है कि साहित्य एक ऐसी वस्तु है जिसका विकास होता है तो कोई भी लेखक अपना यह व्यवहार जारी नहीं रख सकता।
हाँ, तो सॉमरसेट मॉम वाला व्यंग्य नफ़ासत हसन न सह सका। बोला, बस, बस, चुप रहिए, इतनी ज़बान न खोलिए।
नफ़ासत हसन की ज़बान पर रंदा चलने का गुमान होता था। मौलाना ने थोड़ा घूरकर उसकी ओर देखा और बोला, इतने गर्म क्यों होते हो मियाँ? उम्र ही में सही, मैं तुम्हारे बाप के बराबर हूँ।
बस, बस, यह शफ़कत अपने ही पास रखिए। मुझे नहीं चाहिए यह कमीनी शफ़कत...यह सरपरस्ताना शफ़कत बड़े आए हैं मेरे बाप...बाप...इतनी ज़बानदराज़ी!
मौलाना ने अब तक यही समझा था कि वे विनोद की सीमा पर ही खड़े हैं। मामला तो दूसरा ही रंग धारण कर चुका था। उनके चेहरे पर क्रोध की तह चढ़ गई। बोले, एक सुसरे सॉमरसेट मॉम की ख़ातिर क्यों मेरी हतक करने पर तुले हो, मियाँ?...कमबख़्त सॉमरसेट मॉम!
बात तू-तू, मैं-मैं का रूप धारण कर गई। मुझे तो यही आशंका हुई कि कहीं दोनों लेखक हाथापाई पर न उतर आएँ।
नफ़ासत हसन उस दिन मेज़बान था और घर पर आए हुए मेहमान की शान में हर तरह की ज़बानदराज़ी से उसे परहेज़ करना चाहिए था। फिर यह मेहमान कोई मामूली आदमी न था, उसका एक समकालीन लेखक था। उम्र में उससे बड़ा और भाषा पर अधिकार की दृष्टि से उससे कहीं बढ़कर। मैं सोचने लगा कि सॉमरसेट मॉम पर नफ़ासत हसन इतना क्यों फ़िदा है? वह भी मौलाना की तरह एक आदमी ही तो है, कोई फ़रिश्ता नहीं है और मैं तो समझता हूँ कि हर लिहाज़ से नफ़ासत हसन के कमरे में पड़ी हुई किसी भी हल्के-भूरे रंग की कुर्सी से मौलाना ज़्यादा क़ीमती थे। नफ़ासत हसन इतना गर्म क्यों हो गया था? वह शायद अपने मेहमान को कुर्सी से उठा देना चाहता था। यह ठीक है कि मौलाना का व्यंग्य ज़रा तीखा था, पर था तो आख़िर यह व्यंग्य ही और उत्तर इसका अगर व्यंग्य से ही दिया जाता तो यह अशोभन प्रदर्शन तो न हुआ होता।
सॉमरसेट मॉम आख़िर क्या लिखता होगा? क्या उसे अपनी जन्म-भूमि इंग्लिस्तान में भी नफ़ासत हसन जैसा कोई मर-मिटने वाला प्रेमी नसीब हुआ होगा। मुझे यह संदेह हुआ कि नफ़ासत हसन के बहुत से वाक्य, जिन्हें वह मौक़ा- बेमौक़ा निहायत शान से अपनी बात-चीत और लेखनी में नगीनों की तरह जड़ने में होशियार सुनार बन चुका है, अवश्य विलायत की किसी फ़ैक्ट्री से ढल कर आए हैं, उसकी अपनी रचना हरगिज़ नहीं। मैं सोचने लगा कि सर्वप्रथम कब सॉमरसेट मॉम की लेखनी ने उस पर जादू-सा कर दिया था और क्या यह जादू कभी ख़त्म भी हो सकता है?
एक दिन उसने मुझसे पूछा, औरत किस वक़्त सुंदर लगती है? मुझे कोई उत्तर न सूझा। मैंने कहा, आप ही बताइए।
वह बोला- हाँ, तो सुनो जब उसे तीन दिन से बुख़ार आ रहा हो और उसके हाथों की रगें नीली पड़ जाएँ तब औरत कितनी सुंदर लगती है, कितनी सुंदर!
मैंने सोचा शायद यह नगीना भी सॉमरसेट मॉम की फ़ैक्ट्री से बनकर आया हो।
मैंने नफ़ासत हसन से कहा, ग़ुस्सा थूक दो मियाँ। सॉमरसेट मॉम तो एक देवता है।
वह बोला, और मैं?
आप भी देवता हैं, मियाँ।
मैंने उसे बताया कि देवताओं में तीन बड़े देवता हैं—ब्रह्मा, विष्णु और शिव। तीनों की अपनी-अपनी विशेषता है, जिसके कारण वे इतने लोकप्रिय बन गए हैं। ब्रह्मा जन्म देता है, विष्णु पालन करता है और शिव ठहरे मृत्यु का नाच नाचने वाले नटराज!
नफ़ासत हसन का ध्यान अब मेरी तरफ़ खिंच गया। उधर मौलाना की आँखों में भी ग़ुस्सा ठंडा पड़ गया था और वे मेरी बातों में दिलचस्पी ले रहे थे। मैंने बताया कि हर लेखक विभिन्न अवस्थाओं में ब्रह्मा, विष्णु और शिव होता है। जब वह कोई कृति सृजने में सफल होता है उसे ब्रह्मा कहा जा सकता है। जब वह उस रचना को सम्हालकर रखता है और यथासंभव उसमें सुधार भी करता है, उस समय वह विष्णु के सदृश होता है और जब वह अपने ही हाथ से किसी रचना के टुकड़े-टुकड़े कर डालता है तो वह शत-प्रतिशत शिव का रूप धारण कर लेता है।
मौलाना बोले, बहुत ख़ूब! आपकी कल्पना धन्य है!
मैंने झट से कह दिया, मेरी कल्पना! नहीं, मौलाना, नहीं। यह मेरी कल्पना नहीं। मतलब यह कि यह मेरा मौलिक विचार नहीं।
तो किसका ख़याल पेश कर रहे हैं आप?
बंबई की पी० ई० एन० सोसायटी में बुलबुले-हिंद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने मेरे एक भाषण पर सदारत करते हुए यह विचार पेश किया था।
बहुत, ख़ूब! बुलबुले हिंद ने आपके भाषण पर सदारत की थी ! हाँ, तो अब कोई मौलिक विचार हो जाए ज़रा!
मौलिक! मौलिक की भी ख़ूब कही। मुझे तो सिरे से यही शक हो रहा है कि मौलिक नाम की कोई चीज़ होती भी है या नहीं।
नफ़ासत हसन बौखलाया, क्या कह रहे हो, मियाँ? सुनिए मैं एक ख़याल पेश करता हूँ—जैसे ही भोर की पहली किरण आँखें मलती हुई धरती पर उतरी, पास की कच्ची दीवार अँगड़ाई ले रही थी।
मौलाना ने कहा—दीवार अँगड़ाई ले रही थी?
मैंने बीच-बचाव करते हुए कहा, इस समय नफ़ासत हसन एक ब्रह्मा हैं, मौलाना!
ब्रह्मा!
जी हाँ, ब्रह्मा, और न जाने कब तक वह विष्णु बना यह ख़याल सम्हालकर रखेगा और फिर जाने कब स्वयं अपने ही हाथों इस ख़याल का गला घोंट डालेगा। उसे स्वयं अपनी रचना पर हँसी आएगी—केवल हँसी—यदि यह विचार उसका शत-प्रतिशत मौलिक विचार नहीं है, और पूरी-पूरी शर्म, यदि यह सचमुच उसका शत-प्रतिशत मौलिक विचार है।
नफ़ासत हसन चाहता तो झट मेरे विचार का प्रतिवाद कर देता, पर वह चुप बैठा रहा। शायद वह कुछ झेंप-सा गया था और अपने हीन-भाव को छिपाने का यत्न कर रहा था।
मौलाना बोले, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के बारे में आज मैं कुछ और भी सुनना चाहता हूँ।
मैंने कहा—सुनिए विष्णु और शिव के हज़ारों मंदिर हैं और ब्रह्मा का एक भी मंदिर नहीं है कहीं।
ब्रह्मा का एक भी मंदिर नहीं?
जी नहीं! सुनिए तो, बड़ी दिलचस्प कहानी है। एक बार विष्णु और ब्रह्मा में यह मुक़ाबिला हो गया कि कौन पहले शिवलिंग की गहराई और ऊँचाई का पता लगा सकता है। विष्णु जड़ की तरफ़ चल पड़े और ब्रह्मा चोटी की तरफ़। ब्रह्मा ऊपर चढ़ते गए पर शिवलिंग की चोटी कहीं नज़र न आई। ऊपर से एक चमेली का फूल गिरता आ रहा था। ब्रह्मा ने पूछा किधर से आना हुआ!
फूल बोला, शिवलिंग की चोटी से!ब्रह्मा ने पूछा, कितनी दूर है वह चोटी?फूल ने कहा, दूर—बहुत दूर!
ब्रह्मा चमेली के फूल के साथ पीछे को हो लिए। रास्ते में उन्होंने इस फूल को इतना-सा झूठ बोलने के लिए राज़ी कर लिया कि वह विष्णु के सामने यह कह दे कि वे दोनों ख़ास शिवलिंग की चोटी से आ रहे हैं। पर शिव तो ठहरे अंतर्यामी, ब्रह्मा और चमेली को बड़ी भारी सज़ा दी गई—रहती दुनिया तक ब्रह्मा का कहीं मंदिर न बनेगा और चमेली किसी मंदिर में पूजा में न चढ़ाई जाएगी!
नफ़ासत हसन बोला, पर यह तो नया ज़माना है। अब तो शायद ब्रह्मा का मंदिर बन जाए कहीं और मेरा यक़ीन है, अगर ब्रह्मा पर कोई फूल चढ़ेगा तो वह चमेली का फूल ही होगा।
नफ़ासत हसन ने उस समय यही सोचा होगा कि यद्यपि अब तक वह स्वयं एक ब्रह्मा ही है, क्योंकि उसके प्रकाशक ने उसकी कहानियों का बृहद् संग्रह प्रकाशित करने से अभी तक संकोच ही किया है। पर जैसे ही यह पुस्तक प्रकाशित होगी, उसकी ख्याति के वास्तविक मंदिर का निर्माण होते देर न लगेगी और इस मंदिर में चमेली के ही फूल उस पर चढ़ाए जाया करेंगे।
अपने संबंध में इस तरह की ग़लतफ़हमी रखने में उसके दो-चार गहरे दोस्तों का ही हाथ था। उनका विचार था कि उषा के घूँघट खोलने से पहले की सारी कालिमा और लालिमा, अँधियारे और उजियाले की काना-फूसियाँ, उसके स्वभाव में उल्लेखनीय हैं और यदि वह आरंभ में रूसी कहानियों के अनुवाद में अपनी उठती जवानी का ज़ोर लगाने के स्थान पर मौलिक कहानियाँ लिखने की ओर अग्रसर हुआ होता तो आज उसका नाम प्रथम कोटि के प्रगतिशील कहानी-लेखकों में गिना जाता। उनका यह भी ख़याल था कि अब भी गिरे हुए बेरों का कुछ नहीं बिगड़ा यदि यह शत-प्रतिशत प्रगतिशील कहानी-लेखक शत-प्रतिशत तिकड़मबाज़ भी होता गया तो वह निस्संदेह हिंदुस्तान भर के कहानी-साहित्य की चोटी पर नज़र आएगा।
एक बार मित्रों ने उसे बताया कि वह बड़ा स्पष्टवादी है और सपनों में भी यह विचार उसका पीछा करने लगा कि निस्संदेह वह बड़ा स्पष्टवादी है। यही वह गुण है जो शत-प्रतिशत मौलिक कहानी-लेखक को जीवन के अध्ययन में वास्तविक सहायता दे सकता है। जब इस नौकरी के लिए उसने प्रार्थना-पत्र भेजा तो उससे पूछा गया कि उसने किस विषय में अपना ज्ञान चरम सीमा तक पहुँचाया है। निस्संकोच उसने लिख भेजा—मैंने अपने जीवन का अधिकतर समय वेश्याओं का अध्ययन करने में गुज़ार दिया है। यद्यपि इस स्पष्टवादिता से कहीं अधिक एक सिफ़ारिश ने ही उसे यह नौकरी दिलाने में मदद दी थी, पर वह नए मिलने वालों के सम्मुख अपनी इस स्पष्टवादिता की चर्चा किया करता था। स्पष्टवादिता—शत-प्रतिशत स्पष्टवादिता! मैंने सोचा शायद इस स्पष्टवादिता की सीमा ने घर की दीवारों तक पैर न फैलाए होंगे। घर में आकर तो प्रायः बड़े-बड़े प्रगतिशील लेखक भी भीगी बिल्ली बनने पर मजबूर हो जाते हैं।
यह ठीक है कि उसकी प्रगतिशीलता बहुत हद तक नग्न वासना की चर्चा से घिरी रहती थी, पर कुछ समय से उसके मन में यह वहम समा गया था कि वह किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु के चारों ओर अपनी कहानी को घुमा सकता है। अपनी एक कहानी में उसने एक पत्थर की गाथा प्रस्तुत की थी, जो एकाएक किसी अविवाहिता के उठते-मचलते उरोज से टकराने के लिए व्याकुल हो उठा था। आदमी बदस्तूर आदमी है, पर पत्थर अब पत्थर ही नहीं है। यह बात उसने बड़ी गहराई से लिखी थी। मनोविज्ञान की सीमाएँ अब सिकुड़ी न रहेंगी, पत्थर अब पत्थर ही नहीं है, न बिजली का खंभा बिजली का खंभा ही। वह चाहता तो अपने सिगरेट केस में भी दिल डाल देता और इसके गिर्द मनोविज्ञान का बारीक़ जाल बुन देता।
उसकी भाषा न बहुत कठिन थी, न बहुत आसान। यहाँ वहाँ नई-नई उपमाएँ भी हाज़िर रहती थीं। अभी उसे किसी का फूला हुआ थैला देखकर गर्भवती के पेट का ध्यान आ गया, अभी किसी की मानसिक दुर्बलता उस कन्या-सी नज़र आई जो आँधी में अपनी साड़ी न सम्हाल पा रही हो। किसी के बोल सोडे के बुलबुले थे तो किसी की नाक चीनी की प्याली की ठूँठनी-सी।
शाम हो चली थी। नफ़ासत हसन उठकर खड़ा हो गया और अपनी उँगलियों से बालों में कंघी करता हुआ छज्जे पर आ गया। निकलसन रोड पर समीप के टेलर मास्टर की दुकान में बिजली के कुमकुमे रोशन हो चुके थे। छज्जे पर खड़ा-खड़ा नफ़ासत हसन बोला, मौलाना! चलो, लगे हाथों सरदारजी से ही मिलते आएँ।
मैं हैरानी से अपनी सीट में दुबका बैठा था। मैंने सोचा यह सरदारजी कौन हैं, जिनसे मिलने के लिए नफ़ासत हसन इतना उत्सुक नज़र आता है। फिर मुझे ध्यान आया कि वह केवल अपने 'विभिन्नता के लिए विभिन्नता' के दृष्टिकोण के अनुसार ही मुझसे भी किसी लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति से मिलना चाहता है। यद्यपि स्वयं उसके चेहरे पर दाढ़ी तो दाढ़ी, मूँछ तक का चिन्ह हर दूसरे तीसरे दिन मिटा डाला जाता था। इससे पहले भी उसने एक लेखक की मूँछों को केवल इसलिए पसंद किया था कि ये मूँछें मौलाना को नापसंद थीं। मुझे विश्वास था कि यदि मौलाना ने उन मूँछों की प्रशंसा में एक-आध बात कह दी होती तो वह झट कह उठता, 'मौलाना! आपकी अँधाधुंध, पसंद की तो हद हो चुकी है। लाहौल विला कुव्वत! आपने भी ख़ूब आदमियों में आदमी चुना!'
ये सरदारजी कौन हैं? यह प्रश्न मेरे मन में फैलता चला गया। उनसे परिचित होने की इच्छा देखकर नफ़ासत हसन ने मुझे भी साथ ले लिया। वह एक विचित्र मस्ती की अवस्था में सीढ़ियों से उतर रहा था। अपने पैरों को वह ज़रूरत से अधिक ज़ोर से फेंकता था और फट-फट की आवाज़ से शोर पैदा करता हुआ पड़ोसियों के आराम में विघ्न डाल रहा था। इस प्रकार की हरकत को वह आजादी समझता था और वह इसे किसी भी मूल्य पर देने को तैयार न था।
एक बड़े लंबे-चौड़े बाज़ार में घूमते-घामते हम आख़िर सरदारजी की दुकान में पहुँच गए। पता चला कि नफ़ासत हसन इस्म-बा-मुसम्मा है2? क्योंकि शराब की दुकान, जहाँ उसने सरदारजी से भेंट करने का समय निश्चित किया था, सख़्त बदबूदार जगह थी। मेज़ पर संगमरमर की सिलों पर सोडा और ह्विस्की जमी हुई थी और हमारी सीट के समीप ही टूटे हुए कुल्हड़ों का अंबार लग रहा था। बगल में एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी टाँगें एक टूटी सी अलमारी के ऊपर टिकाए अपना मुँह पूरी तरह खोले बेहोश पड़ा था। कुल्हड़ों के इतना समीप होने के कारण उसका खुला हुआ मुँह स्वयं एक कुल्हड़ सा दिखाई देता था। एक क्षण के लिए मुझे गुमान हुआ कि नफ़ासत हसन इसी व्यक्ति से मिलने आया है, मानो अपने आप से, अपने सुंदर नाम से न्याय करने आया है। थोड़ी देर के बाद नफ़ासत हसन ने अपनी रूखी आवाज़ से, जिससे हमेशा की तरह खाहमखाह रंदा चलने का गुमान होता था, पुकारा—ओ मियाँ जुम्मा! लाओ तो सरदारजी को।
मियाँ जुम्मा एक झाड़न से बोतल साफ़ कर रहा था। दिन के समय यह इसी झाड़न से सड़क पर से उड़कर आने वाली गर्द को शीशों पर पड़ी हुई पेस्ट्री या कुल्हड़ों के बीच में तने हुए जालों को साफ़ किया करता था। कुछ देर बाद जुम्मा ने ह्विस्की की एक बोतल और सोडे की दो बोतलें मेज़ पर ला रखीं।
सरदारजी के व्यक्तित्व से परिचित होते देर न लगी। पर मैं बदस्तूर कहानियों की दुनिया में घूम रहा था। मैंने यों ही नफ़ासत हसन से पूछ लिया—आपके अफ़साने तो बहुत जमा हो गए होंगे?
उस समय तक वह सोडा और ह्विस्की को मिला चुका था। मैंने सरदार जी से परिचित होने से इंकार कर दिया था, इसलिए उसने और मौलाना ने गिलास टकराए और अपने-अपने मुँह से लगा लिए। वह एक घूँट गले से नीचे उतारते हुए बोला—
मैं अफ़साने कभी इकट्ठे नहीं करता। मेरे अफ़साने कबूतर के बच्चे हैं जिन्हें में लिखता हूँ और कहता हूँ, 'ओ कबूतर के बच्चों! उड़ जाओ’ और वे उड़ जाते हैं।
इस उपमा की मैंने बहुत प्रशंसा की। सच पूछो तो उस समय मेरे मन में आइनस्टीन के सापेक्षवाद का सिद्धांत स्पष्ट हो गया था। हर वस्तु से दूसरी वस्तु का कुछ-न-कुछ संबंध अवश्य है—अफ़साने का कबूतर के बच्चे से, दुश्चरित्र नारी की मुस्कान का गंदी नाली में फूटते हुए बुलबुले से, भोर की पहली किरण का अंगड़ाई लेती दीवार से, नफ़ासत हसन का चर्खे से...
उस समय मैं सोचने लगा—ये उपमाएँ, विचित्र और खींचा-तानी द्वारा प्रस्तुत की हुई उपमाएँ, इस महामहिम लेखक के मस्तिष्क में कहाँ से जन्म लेती है। फिर मुझे झट ख़याल आया कि यह तो एक सीधी-सादी सी क्रिया है। स्वयं नफ़ासत हसन ने मुझे बताया था कि उसे कब्ज़ की शिकायत कभी नहीं होती। कुछ लेखक तो सख़्त कब्ज़ के बीमार नज़र आते हैं। बेचारे बहुत जोर लगा कर लिखते हैं। मैने सोचा इस लिहाज़ से तो नफ़ासत हसन हर रोज़ दूध के साथ अत्रीफल जम्मानी3 खाता है। यही कारण है कि वह पत्थर, बुलबुले, रणधीर पहलवान, पुस्तक, मेज़, कुर्सी, क़लम-दावात अर्थात् दुनिया भर की हर चीज़ पर लिखकर इनके संग्रहों के नाम दौड़ो, भागो, रोओ, पीटो रख सकता है।
पर मैं बहुत देर तक इन कहानियों की दुनिया में न रह सका। उस समय तक दोनों साहित्यकार ह्विस्की की बोतल आधी के लगभग ख़त्म कर चुके थे। सहसा उन्हें क़िस्म-क़िस्म की शराब को मिलाकर पीने की धुन समाई। चुनाँचे जुम्मा मियाँ ने बहुत सी बोतलों से एक-एक पेग उँड़ेला और फिर सब को ह्विस्की में उँड़ेल दिया। उस समय मौलाना शराब में अपने आपको खो चुके थे। शायद उन्होंने इसीलिए नफ़ासत हसन की साहित्यिक प्रवृत्तियों को सराहना चाहा और एक पेग गले से नीचे उतारते हुए उन्होंने नफ़ासत हसन को एक थपकी दी और बोले, शाबाश बर-ख़ुर्दार...लिखे जाओ!
नफ़ासत हसन, जो सरदार जी के मकान की फ़िजा से ख़ूब परिचित था और जो बिना बौखलाए बहुत से पेग पी सकता था, बोला, बस बस मौलाना, यही एक बात है जो मुझे सिरे से नापसंद है। इस बेहूदा सरपरस्ती की मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आपकी तारीफ़ और बुराई की मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। समझे आप! अगर आपने मेरी कहानियाँ पढ़ीं तो इससे मेरा कुछ सँवर नहीं गया और अगर नहीं पढ़ीं तो कुछ बिगड़ा नहीं।
मौलाना को इस बेजा बात-चीत से बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने मेज़बान के कंधे को थपकते हुए बोले, बर-ख़ुर्दार! अगर तुम कहानी लिखने के बदले मिट्टी का तेल भी बेचा करते तो भी मेरे दिल में तुम्हारी ऐसी ही इज़्ज़त होती।
यों दोनों साहित्यकार तो आपस में गंभीरता से वार्तालाप कर रहे थे, पर मैं उस वातावरण में बौखला-सा गया। फिर मुझे यों लगा कि ये साहित्यकार मेरी तरह परहेज़गार हैं और शराब वास्तव में मैं पी रहा हूँ।
एक और पेग गले से नीचे उतारने के बाद नफ़ासत हसन ने पापड़ का एक टुकड़ा मुँह में डाला और कहा, मौलाना! मैं लिखना चाहता हूँ, बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ। मेरी कभी किसी चीज़ से तसल्ली नहीं होती...।
और अभी नफ़ासत हसन ने अपनी बात ख़त्म भी न की थी कि मुझे ख़याल आया कि उसकी तसल्ली कैसे हो सकती है, क्योंकि उसके अफ़साने तो कबूतर के बच्चे हैं और जब तक वे कबूतर के बच्चे रहेंगे, फुर्र से नफ़ासत हसन के पास से उड़ जाया करेंगे। आख़िर नफ़ासत हसन ने कोई छतनारा भी तो नहीं लगाया ताकि बेचारे उसी पर कभी-कभी आकर बैठ जाएँ और अपने पिछले मालिक को देख लें। अब वे अनगिनत आवारा आत्माओं की तरह सीमाहीन गगन में पर फड़फड़ाते फिर रहे हैं।
नफ़ासत हसन अपनी बात को जारी रखते हुए बोला, बस एक चीज़ लिख लूँगा—एक चीज़—तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। इस के बाद मैं मर भी जाऊँ तो भी यही समझेंगा कि मैंने ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा काम किया है।
मौलाना के और मेरे यथार्थ और काल्पनिक नशे हिरन हो गए। हम दोनों का ध्यान उस कहानी का प्लाट सुनने के लिए नफ़ासत हसन के पतले और दुर्बल चेहरे की ओर खिंच गया। नफ़ासत हसन बोला, मैं उन दिनों बंबई में रहता था। मेरे मकान का एक दरवाज़ा एक ग़ुसलख़ाने में खुलता था। उस ग़ुसलख़ाने के दरवाज़े में एक झिरी थी। बस उसी झिरी में से मैं कुँआरी लड़कियों को नहाते हुए देखता था। अधेड़ उम्र की और बूढ़ी औरतों को भी। इसके अलावा नौजवान मर्द भी नहाने के लिए आया करते थे और जैसा कि आपको मालूम है, इंसान आम ज़िंदगी में वह हरकतें नहीं करता जो वह ग़ुसलख़ाने में करता है।
मैं इस बात को समझ न सका, लेकिन मेरे सामने आइनस्टीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत था, इसलिए मैंने कोई विशेष परवाह न की और सुनता चला गया। नफ़ासत हसन बोला, बस उस ग़ुसलख़ाने में नहाने वालियों और नहाने वालों के बारे में लिखकर मर जाऊँ तो मुझे कोई अफ़सोस न होगा। उस कहानी का नाम रखूँगा—एक झिरी में से—और मर जाऊँगा।
मुझे नफ़ासत हसन की इस हरकत पर बहुत हँसी आई और मेरा जी चाहने लगा कि यदि में इसका संस्मरण लिखकर मर जाऊँ तो मुझे भी ज़िंदगी में कोई हसरत न रह जाएगी।
मौलाना, जो नफ़ासत हसन की इन बेतुकी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे, कुछ न बोले। न जाने नफ़ासत हसन के दिल में ख़ुद ही ख़याल आया कि उसने मौलाना का अपमान किया है। वह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। चुंबन के लिए उसने अपना दायाँ गाल मौलाना के सामने पेश कर दिया। मौलाना ने प्रसाद के रूप में एक चुंबन ले लिया। इस के बाद नफ़ासत हसन ने बायाँ गाल पेश कर दिया। मौलाना के निकट अब प्रसाद की समस्या नहीं थी, पर उन्होंने चुंबन ले लिया।
मैं उनकी आपस की लड़ाई की आशा कर रहा था, लेकिन अचानक मौलाना ने उठकर बड़े निश्छल भाव से सीने पर हाथ रखते हुए कहा, देखो भाई, अब तुम मानोगे, मैं सॉमरसेट मॉम हूँ।
नफ़ासत हसन ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, मैं सॉमरसेट मॉम हूँ।
मौलाना ने कोई प्रतिवाद न किया, बल्कि अपने सीने पर हाथ रखकर बोले मैं सॉमरसेट मॉम हूँ।
फिर नफ़ासत हसन की ओर संकेत करते हुए मौलाना बोले, तुम सॉमरसेट मॉम हो...हम दोनों सॉमरसेट मॉम हैं... जो है सॉमरसेट मॉम है, जो नहीं है, वह भी सॉमरसेट मॉम है...सॉमरसेट मॉम है...।
- पुस्तक : मंटो: मेरा दुश्मन (पृष्ठ 245)
- संपादक : उपेन्द्रनाथ अश्क
- रचनाकार : देवेंद्र सत्यार्थी
- प्रकाशन : नीलाभ प्रकाशन
- संस्करण : 1956
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.