नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन
ne aur apratyashit vishyon par lekhan
नोट
प्रस्तुत पाठ एनसीईआरटी की कक्षा बारहवीं के पाठ्यक्रम में शामिल है।
जिस तरह हम बोलते हैं
उस तरह तू लिख
और इसके बाद भी
हमसे बड़ा तू दिख।
—भवानी प्रसाद मिश्र
हिंदी कवी
• आपने पिछली फ़िल्म कब देखी थी? शायद हफ़्तेभर पहले देखी हो या शायद महीनेभर पहले! देखने के बाद फ़िल्म के बारे में दोस्तों से बातचीत ज़रूर की होगी। उन्हें बताया होगा कि अच्छी लगी या नहीं। अच्छी लगने या न लगने के कारणों पर भी चर्चा हुई होगी। अब सोचिए कि क्या उस फ़िल्म के बारे में अपने ख़यालात को आप एक व्यवस्थित लेख की शक्ल दे सकते हैं?
• अगर आपने फ़िल्म सिनेमाघर में देखी हो, तो उस सिनेमाघर का पूरा माहौल आपके जेहन में होगा—टिकट खिड़की पर लगी लाइन, उस लाइन में चलने बाली बतकही और ठेलमठेल, खाने-पीने की चीज़ों के जगमगाते काउंटर, आगे की संभावित फ़िल्मों के चित्ताकर्षक पोस्टर, सिनेमाघर की लॉबी की अपनी ख़ास महक वग़ैरह, वग़ैरह। क्या आप स्मृति और अनुभव में बसे उस सिनेमाघर को शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेर सकते हैं?
• आपने आज सुबह का अख़बार देखा होगा। पूरा न भी देखा हो, तो कम-से-कम ख़ास-ख़ास ख़बरों पर एक नज़र दौड़ाई होगी। उन ख़बरों को देखते हुए अपने समय और समाज की जो तस्वीर आपके मन में बनती है, क्या उसे आप एक लेख में व्यक्त कर सकते हैं?
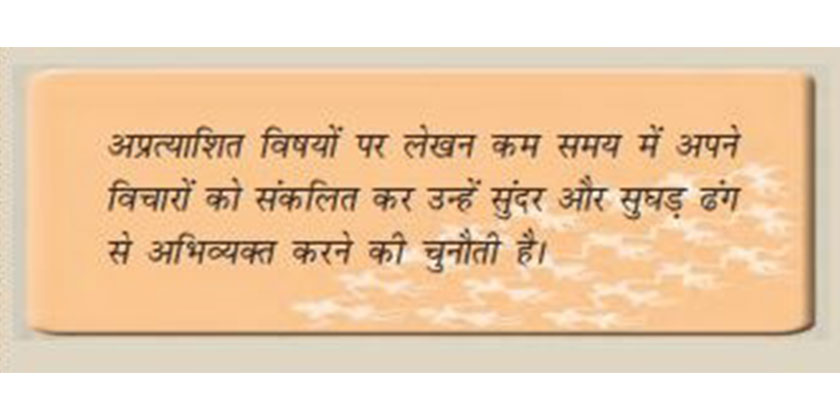
कहने की ज़रूरत नहीं कि लेख की शक्ल देना, उसे शब्दों के सहारे पन्नों पर उकेरना—यह सब ज़्यादातर लोगों के लिए ख़ासा मुश्किल काम है। जिन विचारों को कह डालता हमारे लिए क़तई कठिन नहीं होता, उन्हें लिख डालने का निमंत्रण एक चुनौती की तरह लगने लगता है। ऐसा क्यों है? होने को इसके अनगिनत कारण होंगे, पर एक कारण हमारे काम का है और वह यह कि हम में से ज़्यादातर लोग आत्मनिर्भर होकर लिखित रूप में अभिव्यक्ति का अभ्यास ही नहीं करते। अभ्यास के हर मौक़े को हम रटंत पर निर्भर होकर गँवा बैठते हैं। रटंत का मतलब है, दूसरों के द्वारा तैयार की गई सामग्री को याद करके ज्यों-का-त्यों प्रस्तुत कर देने की कुटेव (बुरी लत)। इस कुटेव का शिकार हो जाने पर असली अभ्यास या रिवाज़ का मौक़ा ही कहाँ मिलता है?
ज़ाहिर है, लेखन का आशय यहाँ यांत्रिक हस्तकौशल से नहीं है। उसका आशय भाषा के सहारे किसी चीत पर विचार करने और उस विचार को व्याकरणिक शुद्धता के साथ सुसंगठित रूप में अभिव्यक्त करने से है। याद रखें, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं, स्वयं विचार करने का साधन भी है। विचार करने और उसे व्यक्त करने की यह प्रक्रिया निबंध के चिरपरिचित विषयों के साथ आमतौर पर घटित नहीं हो पाती। इसका कारण यह है कि उन पर तैयारशुदा सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहती है और हम कुछ नया सोचने-लिखने की ज़हमत उठाने के बजाए उसी सामग्री पर निर्भर हो जाते हैं। मौलिक प्रयास एवं अभ्यास को बाधित करनेवाली यह निर्भरता हमारे अंदर लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित नहीं होने देती। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम निबंध के परंपरागत विषयों को छोड़कर नए तरह के विषयों पर लिखने का अभ्यास करें। यही अभ्यास हमें अपने मौलिक अधिकारों में से एक अभिव्यक्ति के अधिकार का पूरा-पूरा उपयोग कर पाने की सामर्थ्य देगा।
ऐसे लेखन के लिए आपको जिस तरह के विषय दिए जा सकते हैं, उनकी संख्या अपरिमित है। आपके सामने की दीवार, उस दीवार पर टँगी घड़ी, उस दीवार में बाहर की ओर खुलता झरोखा कुछ भी उसका विषय हो सकता है। ऐसे विषय भी हो सकते हैं, जिनमें इनके मुक़ाबले खुलापन थोड़ा कम हो और ‘फ़ोकस’ अधिक स्पष्ट हो। जैसे टी.वी. धारावाहिकों में स्त्री, बहुत ज़रूरी है शिक्षा, इत्यादि।
यहाँ जितने विषय एक झटके में सुझा दिए गए, ज़ाहिर है, वे बहुत अलग-अलग प्रकृत्ति के हैं और इसीलिए आपसे इनकी माँग भी अलग-अलग क़िस्म की होगी। कोई विषय आपको तार्किक विचार प्रक्रिया में उतारना चाहता है, कोई आपसे यह माँग करता है कि जो कुछ आपने देखा-सुना है या देख-सुन रहे हैं, उसे थोड़ी बारीकी से पुनः संकलित करते हुए एक व्यवस्था में ढाल दें, कोई अपनी स्मृतियों को खँगालने के लिए आपको प्रेरित करता है, तो कोई अनुभव को सैद्धांतिक नज़रिए से जाँचने परखने के लिए आपको उकसाता है। इन माँगों के जवाब में आप जो कुछ लिखेंगे, वह कभी निबंध बन पड़ेगा, कभी संस्मरण, कभी रेखाचित्र की शक्ल लेगा, तो कभी यात्रावृत्तांत की। इसीलिए हम उसे एक सामान्य नाम देंगे—लेख, ताकि आपको ऐसा न लगे कि हम आप पर किसी विधा विशेष के भीतर ही लेखन करने का दबाव बना रहे हैं।
अब सवाल है कि ऐसा लेख प्रस्तुत करने की चुनौती सामने हो, तो क्या करना चाहिए? कहने की ज़रूरत नहीं कि लिखने का कोई फ़ॉर्मूला आज तक दुनिया में नहीं बना। अगर फ़ॉर्मूला होता, तो कंप्यूटर हमारे मुक़ाबले बेहतर लेखक साबित हो सकता था। वस्तुतः लेखन की रचनात्मकता का पूरा संबंध फ़ॉर्मूले का वजूद न होने की इसी सचाई से है। इसके बावजूद यहाँ कुछ ऐसे सुझाव दिए जा सकते हैं, जो अचानक सामने आए विषय से मुखामुखम होने में आपकी मदद कर सकते हैं।
अव्वल तो यह ध्यान में रखें कि इस तरह के लेखन में विषय दो खंभों के बीच बंधी रस्सी की तरह नहीं होता, जिस पर चलते हुए हम एक क़दम भी इधर-उधर रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह तो खुले मैदान की तरह होता है, जिसमें बेलाग दौड़ने, कूदने और कुलाँचे भरने की छूट होती है। दरअसल, दिए गए विषय के साहचर्य से जो भी सार्थक और सुसंगत विचार हमारे मन में आते हैं, उन्हें हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। हाँ, अपेक्षाकृत स्पष्ट फ़ोकस वाले विषय मिलने पर (मसलन, टी.वी. धारावाहिकों में स्त्री) इस विचार प्रवाह को थोड़ा नियंत्रित रखना पड़ता है। इन पर लिखते हुए विषय में व्यक्त वस्तुस्थिति की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत खुलापन रखनेवाले विषयों पर अगर हम शताधिक कोणों से विचार कर सकते हैं, तो उनसे भिन्न, किंचित केंद्रित प्रकृति के विषयों पर विचार करने के कोण स्वाभाविक रूप से थोड़े कम होते हैं। लेकिन इतना तय है कि किसी भी विषय पर एक ही व्यक्ति के जेहन में कई तरीक़ों से सोचने की प्रवृत्ति होती है। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ हो, तो सबसे पहले दो-तीन मिनट ठहर कर यह तय कर लें कि उनमें से किस कोण से उभरनेवाले विचारों को आप थोड़ा विस्तार दे सकते हैं। यह तय कर लेने के बाद आप एक आकर्षक-सी शुरुआत पर विचार करें। हाँ, ये ख़याल रहे कि वह शुरुआत आकर्षक होने के साथ-साथ निर्वाह-योग्य भी हो। ऐसा न हो कि आगे आप जो कुछ कहना चाहते हों, उसे इस प्रस्थान के साथ सुसंबद्ध और सुसंगत रूप में पिरो पाना आपके लिए मुमकिन न हो। इसलिए शुरुआत से आगे बात कैसे सिलसिलेवार बढ़ेगी, इसकी एक रूपरेखा आपके जेहन में होनी चाहिए। वस्तुतः सुसंबद्धता किसी भी तरह के लेखन का एक बुनियादी नियम है। ख़ासतौर से, जब विषय पर विचार करने की चौहद्दियाँ बहुत सख़्ती से तय न कर दी गई हों, उस सूरत में सुसंबद्धता बनाए रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। जब चौहद्दियाँ सख़्ती से तय कर दी गई हों, तब बाहरी/आरोपित अनुशासन ही विचार प्रवाह में कमोबेश आंतरिक संबद्धता कायम कर देता है।
विवरण-विवेचन के सुसंबद्ध होने के साथ-साथ उसका सुसंगत होना भी अच्छे लेखन की एक ख़ासियत है। आपकी कही गई बातें न सिर्फ़ आपस में जुड़ी हुई हों, बल्कि उनमें तालमेल भी हो। अगर आपकी दो बातें आपस में ही एक-दूसरे का खंडन करती हों, तो यह लेखन का ही नहीं, किसी भी तरह की अभिव्यक्ति का एक अक्षम्य दोष है।
सुसंबद्धता और सुसंगति को और बेहतर तरीक़े से समझने के लिए एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। मान लीजिए मौसम की चर्चा करते-करते आप एकाएक राजनीति पर बात करने लगें और ऐसा करने का कोई ठोस आधार या कारण मसलन, समानता के आधार पर कोई व्यंग्य करना या इन दोनों का कोई पारस्परिक प्रभाव रेखांकित करना प्रकट न हो, तो आपकी बातों में संबद्धता का अभाव दिखेगा। इसी तरह मौसम की चर्चा करते हुए आप किसी ख़ास दिन, समय और स्थान के मौसम को एक बार ख़ुशगवार बताएँ और दूसरी बार उबाऊ, तो आपकी बातें असंगत जान पड़ेंगी। आप अपनी कही हुई बात को इस तरह ख़ुद ही झुठला दें, तो कौन आपको पढ़ना चाहेगा? इसलिए लेख चाहे वह संस्मरणात्मक हो, रेखाचित्रात्मक हो अथवा वैचारिक, उसकी सुसंबद्धता और सुसंगति के प्रति हर लेखक को सचेत होना चाहिए। वैसे हमारे सोचने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से इन गुणों को धारण करती ही है, फिर भी सचेत न रहने पर, संभव है, ये गुण कहीं-कहीं नदारद हो जाएँ।
यह भी उल्लेखनीय है कि सामान्यतः निबंधों या आलेखों/प्रश्नोत्तरों में जहाँ ‘मैं’ शैली का प्रयोग वर्जित होता है, वहीं इस तरह के लेखन में ‘मैं’ की आवाजाही बेरोकटोक चल सकती है। यहाँ विषय की प्रकृति में ही निहित होता है कि लेख में व्यक्त विचारों में आत्मनिष्ठता और लेखक के व्यक्तित्व की छाप होगी। इसलिए अन्यत्र वस्तुनिष्ठता के आग्रह से ‘मैं’ शैली को भले ही ठीक न माना जाता हो, यहाँ उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता।
आइए, अब आपके सामने कुछ नमूने पेश करें। सबसे पहले तीन नमूने एक ही विषय—‘दीवाल घड़ी’ पर। यह बिलकुल खुला हुआ विषय है। विषय प्रस्तावित करनेवाला यहाँ किसी तरह की चौहद्दी नहीं बाँध रहा, वह आपको इस बात की छूट दे रहा है कि इस विषय के साथ आपके ज़ेहन में जो भी ख़याल उभर रहे हैं, उन्हें सुसंगत तरीक़े से शब्दबद्ध करें। अगर वह ‘दीवाल घड़ी की उपयोगिता’, ‘दीवाल घड़ी का इतिहास’ जैसा कोई विषय प्रस्तावित करता, तो बात और थी। वहाँ ढीला-ढाला ही सही, एक बंधन होता और आप उसकी मर्यादा का ध्यान रखते हुए लेखन करते। पर यहाँ आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया है। आप जिस दिशा में जाकर जुगाली करना चाहते हैं, करें! इन तीन नमूनों को देख कर यह बात आपके सामने साफ़ हो जाएगी।

दीवाल घड़ी-1
उसे देखते ही किसी फ़िल्म का एक ख़ूबसूरत सा दृश्य याद आता है। घड़ियों की एक दुकान में नायक-नायिका की मुलाक़ात होती है। हर तरफ़ भाँति-भाँति की घड़ियाँ टँगी हैं। बारह बजने ही वाले हैं। ज्यों ही नायक कुछ कहना चाहता है। और वह कुछ बड़ा ही मानीखेज़ है—घड़ियों की सुइयाँ बारह पर पहुँच जाती हैं और एक-एक कर सारी घड़ियों से बारह बार घंटी बजने की आवाज़ उठने लगती है। अगले कुछ सेकेंड तक ऐसा संगीतमय शोर गूँजता रहता है कि नायक हकला कर चुप रह जाता है। घड़ियों ने मानो उसका मंच ही छीन लिया हो। फिर नायक-नायिका, दोनों इस मधुर विडंबना पर मुस्कुराते हुए एक-दूसरे को देखते रह जाते हैं...यह ख़ूबसूरत दृश्य मेरी याददाश्त में उसी तरह टँगा है, जिस तरह दीवार पर घड़ी टँगी होती है। कहीं आती-जाती नहीं, हमेशा स्थिर, फिर भी गतिशील!
ऐसी कई स्मृतियाँ दीवाल घड़ी के साथ जुड़ी हैं। मेरे घर में जब पहली दीवाल घड़ी ख़रीदकर आई (वही अभी तक की आख़िरी भी है), तो उसे टाँगने की जुगत में पूरा घर जिस तरह लगा रहा, उसकी याद आते ही बेसाख़्ता हँसी छूट जाती है। हम सब उस दिन अंकल पोज़र की मुद्रा में थे। हर कोई भवनशास्त्र से लेकर सौंदर्यशास्त्र तक का विशेषज्ञ होने का दावा कर रहा था। ‘घड़ी यहाँ टँगनी चाहिए’। ‘नहीं, वहाँ टँगनी चाहिए। कील ऐसे ठोंकी जानी चाहिए, ‘नहीं, वैसे ठोंकी जानी चाहिए’ ‘घड़ी हाथ की पहुँच में होनी चाहिए’, ‘नहीं, पहुँच से बाहर होनी चाहिए’। ये सारी बहसें हम तमाम विशेषज्ञों के बीच चलती रहीं और अंत में जब सर्वसम्मति से किसी फ़ॉर्मूले के तहत काम संपन्न हो पाया, तब तक दीवार पर कम से कम छह जगह उसे टाँगे जाने की कोशिशों के निशान छूट चुके थे। अगली दीवाली पर उन गड्डों के भरे जाने तक दीवाल घड़ी तारों के बीच चमकते धवल चाँद की तरह स्थापित रही। चाँद तो अब भी है, पर तारे नहीं रहे। यह चाँद ऐसा है, जो तक़रीबन सभी मध्यवर्गीय घरों में पाया जाता है। मेरी ही तरह उन घरों के बाशिंदों के मन में भी उसे लेकर कुछ-न-कुछ यादें बसी होंगी। यह कितना अजीब है कि जो प्रतिक्षण समय के बीते जाने पर टकटकी लगाए रखता है, वही हमारे भीतर समय को कहीं स्थिर भी कर देता है।
दीवाल घड़ी-2
वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ़-सुथरी दीवार पर कील के सहारे टँगी हुई। कील दिखती नहीं। इसका मतलब यह कि कील पर उसके टँगे होने का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है। लेकिन तर्कशास्त्रियों ने तो तर्कसंगत अनुमान को भी प्रमाण की हो श्रेणी में रखा है। इसलिए तर्क पर आधारित यह अनुमान बिलकुल निरापद है कि घड़ी कील के सहारे टँगी है... वह अपनी जगह बिलकुल स्थिर है, पता नहीं कब से, लेकिन चल रही है। उसके काँटों में एक अनवरत चक्रीय गति है। चक्र या वृत्त की न कोई शुरुआत होती है, न उसका अंत होता है। इस तरह इन काँटों की चक्रीय गति हमें बताती है कि समय अनादि अनंत है। घड़ी को दीवार के आसन पर बिठाकर मानों यही बताते रहने का ज़िम्मा सौंप दिया गया है कि समय लगातार बीत रहा है, पर ख़त्म होने के लिए नहीं। यह विरोधाभास-सा लगता है ना। किसी झुके हुए मर्तबान से लगातार पानी गिर रहा है, पर न पानी कम होता है, न मर्तबान ख़ाली होता है। ग़ौर करें तो यह विरोधाभास नहीं है। समय अनंत है, पर हम सबका अपना-अपना समय अनंत नहीं। घड़ी के चक्र में हर थोड़ी-थोड़ी दूरी पर जो लकीरें हैं, वे समय के कृत्रिम खंड ही सही, वे हमें बताती हैं कि हर इंसान का हर चीज़ का और हर काम का अपना समय होता है। वह शुरू भी होता है और ख़त्म भी। याद आता है, कौन बनेगा करोड़पति का वह छोटा-सा बहुचर्चित जुमला ‘तो आपका समय शुरू होता है अब।’
दीवाल घड़ी-3
वह मेरे ठीक सामने है, एक साफ़-सुथरी दीवार पर कील के सहारे टँगी हुई। बिलकुल स्थिर है अपनी जगह पर, पता नहीं कब से, पर लगातार चल रही है, हिंदी में टिक्-टिक्-टिक्-टिक् और अँग्रेज़ी में टिक्-टॉक, टिक्-टॉक। उसे अँग्रेज़ी या हिंदी नहीं आती, पर दोनों तरह के भाषा-भाषी उसकी पदचाप को अपने-अपने तरीक़े से सुनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुत्तों को अँग्रेज़ी या हिंदी नहीं आती, पर अँग्रेज़ी समाज के लिए वह बाउ-बाउ करता है और हिंदी समाज के लिए भौं-भौं! टिक्-टिक् या टिक्-टॉक की पदचाप के साथ लगातार चलायमान यह घड़ी सामने की दीवार पर एक ख़ूबसूरत-सी बिंदी के समान दिख रही है। कमरे की चारों दीवारों पर कहीं भी और कुछ नहीं है—न कोई पेंटिंग, न कैलेंडर। ऐसे में इस गोलाकार घड़ी का वजूद सिर्फ़ उपयोगितावादी नहीं लगता। वह ख़ूबसूरती के लिए भी है। दीवार की हल्की पीली रंगत के साथ उसका भूरा रंग एक नयनाभिराम कंट्रास्ट रचता है और उसकी अनथक चलती सुइयाँ दीवारों की स्थिरता के बीच एक जीवंत स्पंदन भरती हैं। दीवारों की ख़ामोशी और स्थिरता के बीच वह ऐसी दिखती है, मानो कोई बच्चा चुपचाप बैठे रहने की सज़ा निभा रहा हो, पर उसकी आँखें लगातार बोल रही हों। हाँ, वह बोल रही है, न अँग्रेज़ी में, न हिंदी में, बल्कि एक ऐसी ज़़ुबान में, जिसे इस धरती पर रहनेवाला हर समझदार इंसान समझता है। कुछ ज़्यादा नहीं है उसके पास कहने के लिए। वह तो सिर्फ़ इतना कह रही है कि वक़्त किसी के लिए नहीं ठहरता। बात बड़ी है, भले ही इस घड़ी की सुइयाँ मेरी क़लम के आकार से ज़्यादा बड़ी न हों। बस, एक चीज़ अखरती है। लगानेवाले ने उसे ऐसी जगह लगाया है कि उसे देखो, तो खिड़की की तरफ़ पीठ करनी पड़ती है। काश, ऐसा न होता।
इन नमूनों में से पहला मुख्यतः स्मृति-आधारित है। दीवाल घड़ी को देखकर जो यादें मन में उभर आई हैं, उन्हें लेखक एक तरतीब दे रहा है। तरतीब देने के सिलसिले में ध्यान इस बात का रखा गया है कि वे स्मृतियाँ पाठक को दिलचस्प जान पड़ें; साथ ही, यथासंभव उन स्मृतियों से कहीं एक-दो वाक्यों में ऐसा निचोड़ निकाला जाए कि वे किसी सामान्य सत्य यानी एक बड़े धरातल पर अनुभव किए जानेवाले सत्य की ओर इशारा करने लगें।
दूसरा नमूना दार्शनिक मिज़ाज का है। यहाँ लेखक दीवाल घड़ी को देखता है और रोज़मर्रा की छोटी-मोटी चीज़ों से ऊपर उठकर कुछ ऐसे गंभीर प्रश्नों की ओर उन्मुख हो जाता है, जो उस घड़ी के साथ एक क्षीण तंतु से जुड़े हैं।
तीसरा नमूना मुख्यतः अवलोकन आधारित है। सामने की दीवार पर एक घड़ी दिखती है और उसकी ख़ूबसूरती, गति, आवाज़, टँगे होने का अंदाज़ ये सारी चीज़ें लेखक की टिप्पणी का विषय बन जाती हैं। टिप्पणी में स्थिति का बयान करने के साथ-साथ वह अपनी राय भी ज़ाहिर करता है और इनके द्वारा अपने लेखन को सपाट विवरण बनने से बचाता है। कहीं एक-दो वाक्यों में निचोड़ के तौर पर किसी सामान्य सत्य को प्रतिष्ठित करने की पद्धति यहाँ भी अपनाई गई है।
तरीक़े और भी हो सकते हैं। मसलन, किसी ज्वलंत सामाजिक सांस्कृतिक प्रश्न (जातिवाद का ज़हर) पर लिखना हो, तो आप तथ्य और उसका विश्लेषण प्रस्तुत करने की पद्धति अपना सकते हैं। किसी ख़ास जगह के दृश्य (मेरे मुहल्ले का चौराहा) को उकेरना हो, तो आप कल्पना में उस दृश्य को उपस्थित मानकर चल-कैमरे की तरह अनेक ब्योरों को समेट सकते हैं; किसी प्रवृत्ति या चलन पर लिखना हो, तो उसके गुणावगुण पर तर्कपूर्वक विचार कर सकते हैं। ये तरीक़े पिछले तीन नमूनों के लिए अपनाए गए तरीक़ों से जुदा हैं। कहने का मतलब यह कि आप अपनी सुविधा और विषय की माँग के अनुसार अपने तरीक़े का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपके सामने विषय है, ‘जातिवाद का ज़हर’, तो ज़ाहिर है कि आप कल्पना की उड़ान वाली शैली नहीं अपनाएँगे। यह एक ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है, जो आपसे ठोस विश्लेषण और स्पष्ट राय की माँग करता है। तो इस विषय के साथ आपका बरताव शायद कुछ इस तरह हो—
जातिवाद का ज़हर

ज़हर जीवित शरीर को मौत की नींद सुला देता है और अगर शरीर की प्रतिरोध क्षमता के कारण वह ऐसा न कर पाए, तब भी शरीर की व्यवस्था में भयंकर उथल-पुथल मचाकर उसे अशक्त और बीमार तो बना ही देता है। मानव समाज के जीवित शरीर में जातिवाद ने ऐसे ही ज़हर का काम किया है। हमारे जिन पुरखों ने कर्म के आधार पर वर्ण तय किए थे, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कल को यह विचार जन्मना जातिव्यवस्था में परिणत हो जाएगा और इसके चलते गर्भ में शिशु के आते ही उसकी नियति तय हो जाया करेगी। उन्हें इस बात का शायद ही अंदाज़ा रहा हो कि वे जो बीज बो रहे हैं, उससे ऐसा विषवृक्ष निकलेगा, जो आगे हज़ारों सालों तक ग़ैर-बराबरी और शोषण-उत्पीड़न का आधार बन कर समाज की तंदुरुस्ती का क्षय करता रहेगा। आज हम बड़े-बड़े औद्योगिक संयत्रों, तीव्र गतिवाले परिवहन-साधनों, स्वचालित उपकरणों, कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में जी रहे हैं, फिर भी जन्म के आधार पर कुछ लोगों को अपना और कुछ को पराया मानने, कुछ को बड़ा और कुछ को क्षुद्र मानने की सदियों पुरानी परिपाटी क़ायम है। आए दिन अख़बारों में इस तरह की ख़बरें पड़ने को मिलती हैं कि फलाँ गाँव या क़स्बे में किसी प्रेमी युगल को इसलिए मार डाला गया कि उन्होंने अलग-अलग जातियों से आने के बावजूद साथ जीवन बिताने का सपना देखा था। ऐसी ख़बरों का दुहराव होने में भी ज़्यादा अंतराल नहीं आता कि किसी गाँव में एक जातिविशेष के टोले पर दूसरी जाति के लोगों ने हमला कर दिया और महिलाओं-बच्चों समेत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। यह कहना ग़लत न होगा कि जातिवादी तनाव हमारे रोज़मर्रा के जीवन का हिस्सा बन बैठा है, जो गाहे-बगाहे अपना चरम रूप धारण कर लेता है और अपने तांडव में कितनी ही ज़िंदगियों को उजाड़ देता है।
सामान्य रूप से यह माना जाता है कि आधुनिक लोकतंत्र ऐसी मानवविरोधी परिपाटियों के वजूद को मिटा डालता है, पर हमारे यहाँ मंजर ही उलटा है। हमारे लोकतांत्रिक चुनावों ने जातिवादी भावनाओं को और गहरा बनाने का काम किया है; अलग-अलग जातियाँ राजनीतिक दलों के वोट बैंकों में तब्दील हो गई हैं। ऐसे में कोई उम्मीद भी कैसे कर सकता है कि यह लोकतंत्र जातिवाद की जड़ों पर प्रहार कर पाएगा! राजनीति में जब जातिगत आधारों पर गोलबंदियाँ होती हैं, तब स्वाभाविक है कि हमारे गली-मोहल्ले, हमारे काम के स्थान, हमारे शिक्षण संस्थान इत्यादि भी इस तरह की गोलबंदियों से मुक्त नहीं होंगे। जिस तरह शरीर में प्रवेश करनेवाला ज़हर धमनियों में दौड़ते ख़ून की मदद से अंग-प्रत्यंगों तक पहुँच जाता है, वैसे ही जातिवाद का ज़हर समाज के हर अंग को अपनी जकड़ में ले चुका है। पर इस समाज की जिजीविषा अद्भुत है। वह इस ज़हर को परास्त करके ही रहेगा, क्योंकि इसे जीना है और वह भी तंदुरुस्त रहकर, घिसट-घिसट कर नहीं। जातिवाद से फ़ायदा उठानेवाले लोग मुट्ठीभर हैं और उसका नुकसान झेलनेवाले बहुसंख्यक इस बात को समझने के संकेत हिंदुस्तान की जनता देने लगी है। जिस दिन उसकी सोच पर पड़े सारे झोल को चीर कर यह बात साफ़-साफ़ दिखने लगेगी, उसी दिन इस मारक विष का सही उपचार शुरू हो पाएगा।
- पुस्तक : अभिवक्ति और माध्यम (पृष्ठ 155)
- प्रकाशन : एनसीईआरटी
- संस्करण : 2022
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.


