प्रेम की घर वापसी
 शम्पा शाह
07 जनवरी 2026
शम्पा शाह
07 जनवरी 2026
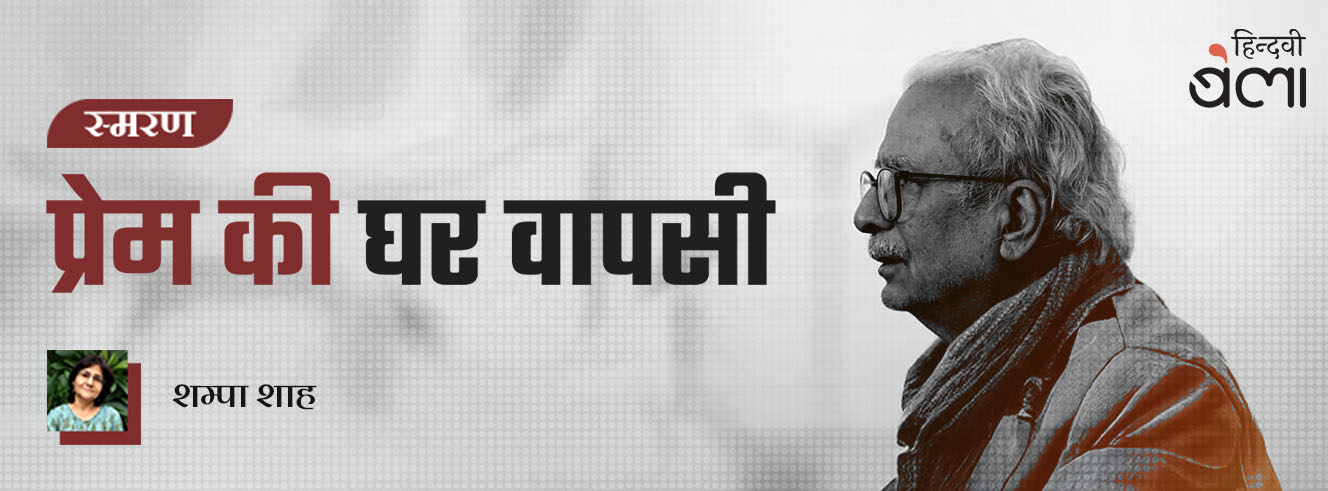
आज, अभी, इस दिन, इस क्षण की लंबान कितनी हो सकती है? इसका एक वाजिब जवाब है—विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास, ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ जितनी! इस उपन्यास को पढ़ते हुए पहली ही बात जो ध्यान खींचती है, वह है इस उपन्यास का विगत की स्मृतियों और भविष्य की आहटों से पूरी तरह मुक्त होना। यह पूरा उपन्यास ‘आज’, ‘अभी’, ‘इस दिन’ के घटित होने में अवस्थित है। या यूँ कहें कि यह पूरा उपन्यास ‘आज’ ‘अभी’, ‘इस दिन’ का विस्तार है। समूचा उपन्यास जैसे ‘आज’ की लंबान को जीवन की लंबान बना पाने की अपार लेखकीय खोज है। इस उपन्यास में यदि सेमल के फाहे-सी उड़ती हुई भारहीनता है, तो इसीलिए कि वह सिर्फ़ वर्तमान का नर्तन है जिस पर भूत और भविष्य सवार नहीं हैं।
मिलान कुंदेरा ‘दी नॉवल एंड यूरोप’ नामक अपने लेख में लिखते हैं—“आप मानें या न मानें पर उपन्यास, दरअस्ल मानव अस्तित्व क्या है और उसमें कविता कहाँ वास करती है—इसकी खोज है।” इस लेख में मिलान कुंदेरा उपन्यास विधा की नितांत सत्ता की बात करते हुए यह भी कहते हैं कि उपन्यासकार के अपने सैद्धांतिक विचार क्या हैं, इससे उपन्यास को कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि एक असल, प्रतिभावान लेखक के भीतर से ‘उपन्यासकार’ नहीं, ‘उपन्यास’ की अपनी ‘विज़्डम’ बोलती है। वह आगे लिखते हैं—“उपन्यास व्यक्ति की कल्पना का स्वर्ग है।”
ये तीनों ही बातें ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण हैं। आज़ादी के बाद हमारा पारंपरिक-सामाजिक परिवेश, जिसमें आस-पड़ोस का मित-भाव भरा दायरा था, छीजता चला गया। वहीं दूसरी ओर, शहर का आकार तेज़ी से बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले गाँवों को लीलता, अपने मोहल्ले में तब्दील करता चला गया। बीसवीं सदी के अंतिम दशकों में जब यह उपन्यास लिखा गया, भारतीय समाज का वह ‘लोक’ स्वरूप जिसमें पारस्परिकता का दायरा मनुष्येतर जगत को सहज ही अपने में समेटे हुए था, विस्मृत और विलुप्त हो रहा था। थोड़ी-सी भी हैसियत के परिवारों के नवयुवक गाँव से शहरों की ओर बड़ी संख्या में प्रस्थान कर रहे थे। और क्योंकि, यह अपने ही देश के गावों-क़स्बों से शहरों की यात्रा थी जो ‘शिक्षा’ और ‘तरक़्क़ी’ के स्वप्न के साथ की जा रही थी, इसलिए इसे ‘विस्थापन’ की तरह न देखा गया, न समझा गया। लेकिन सत्य यह है कि हमारा भारतीय समाज बहुत तेज़ी से देश और काल के लिहाज़ से दो बिल्कुल भिन्न फाँकों में बँट गया— गाँव और शहर, जिनका आपस में जोड़ शिथिल से शिथिलतर होता चला गया है। गाँव-क़स्बे का वह समावेशी परिवेश जिसमें लोगों का आपस में, और अन्य जीवों, पेड़ों, सितारों से घरोपा होता था/है—वह धीरे-धीरे शहरी भारतीय बुद्धिजीवी के लिए केवल कामना का विषय बन के रह गया। उसके ह्रास को लेकर चंद भावनात्मक पंक्तियाँ टाँकने का काम बदस्तूर हिंदी कविता में आज भी चल रहा है। भावुक सदिच्छाओं की कविताई एक बात है, मगर जीवन के उस सूखते आब को पहले तो ठीक-ठीक पहचानना और फिर उसे पुनः आविष्कृत करने का बीड़ा उठाना बिल्कुल अलग बात है।
विनोद कुमार शुक्ल का यह उपन्यास उसी नितांत भारतीय लोक जीवन का आह्वान और रि-इनेक्टमेंट है। लेकिन इस उपन्यास में वह ‘लोक’ जीवन एक विलुप्त प्रायः प्रजाति या जीवाश्म बन कर नहीं आता कि जिसे साहित्य के संग्रहालय में बचा लेने की ज़रूरत है। वह जीवंत, फूलों से लदी लता-सी जिजीविषा लेकर इस उपन्यास में प्रकट होता है, जिसमें मरने-नष्ट होने के लक्षण नहीं हैं। उपन्यासकार लोक में पगी इस भारतीय जीवन शैली को अतीत का अंग न मानकर, वर्तमान में अमल में लाने लायक़ मानता है। लेखक उसे अतीत की स्मृति या नोस्टेलजिया की तरह नहीं देखता। बल्कि अपनी सृजनात्मकता से उसे ऐन हमारी आँखों के आगे सजीव कर दिखाता है—आज, अभी और यहाँ।
यूँ तो विनोद कुमार शुक्ल के तीनों उपन्यासों में, मध्यमवर्गीय परिवार में दाम्पत्य के सुख की खोज और व्याप्ति है। लेकिन ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ में वह मुकम्मल रूप में प्रतिष्ठित हो पाया है। इस सफलता का बड़ा कारण लेखक का रघुवर-सोनसी की ऐसी कथा को बुनने के विचार से मुक्त रहना है, जिसकी शुरूआत कभी बीते हुए अतीत में हुई थी और अंत कहीं भविष्य में होगा। उपन्यास ऐसी कोई कथा नहीं कहता। यह केवल रघुवर-सोनसी और उनके संसार के ‘आज’ को हमारे सम्मुख अभिनीत करता है।
लेकिन इसी कारण, जब से यह उपन्यास पढ़कर समाप्त किया, एक गुत्थी मेरे सम्मुख मुँह बायें खड़ी है—वर्तमान का ऐसा सुघर विस्तार रच पाने के बाद लेखक इस उपन्यास को दीवार में एक खिड़की रहती ‘है’ कहने के बजाय ‘थी’ क्यों कहता है? ‘थी’ कहते ही उपन्यास का अतीत के मोह से ख़ुद को दूर रखने का संकल्प ही कहीं विफल नहीं हो जाता? रघुवर-सोनसी की यह कथा किसी सुदूर अतीत के जीवन की कथा न होकर ‘आज’, ‘अभी’ की है, इसी बात में तो आज के समाज के लिए, प्रेम के लिए संभावना निर्मित हुई है। लेखक के उस वर्तमान में साकार करने से ही तो उसकी अकूत, छलकती ऊर्जा है।
ऐसी स्थिति में उपन्यास के शीर्षक में ‘थी’ की व्याख्या केवल हान्ना एरेंट की इस बात से ही हो सकती है, जिसमें वह कहती हैं कि लेखक जो भी लिखता है, वह इस अर्थ में भूत ही होता है कि वह उसकी कल्पना में पहले (भले क्षण भर पहले) घटित हो चुकता है और तब कहीं वह लिखने की क्रिया में चरितार्थ होता है। यानी, कुछ भी लिखा जाना एक तरह से विगत ही होता है। उपन्यास के शीर्षक के भूतकाल में अवस्थित होने के पीछे यह कारण युक्ति युक्त है। अन्यथा, तो यह पाठक पर कुठाराघात होता कि जिस वर्तमान की कथा को अभी उसने उपन्यास में घटित होते देखा, वह यकायक विगत की कथा हो अतीत के गर्भ में समा जाए।
इस उपन्यास की बुनावट ही कुछ ऐसी है कि यह पूरा का पूरा हमारी आँखों के आगे जैसे मंच पर देह धारण कर साकार होता है। हमें रघुवर प्रसाद और सोनसी के बचपन या विगत जीवन के बारे में बमुश्किल एक-आध पंक्ति उपन्यास में मिलती है और इसी तरह उनके भविष्य की चिंता या स्वप्न की कोई आहट भी उपन्यास में सुनाई नहीं देती। भविष्य को लेकर उपन्यास में बार-बार एकमात्र जो ज़िक्र आता है, वह इतना कि साधु यदि हाथी को छोड़ एक दिन अचानक ग़ायब हो गया तो क्या पालतू हो चुके हाथी को फिर जंगल में छोड़ा जा सकेगा? क्या हाथी अपने को बचा पाएगा? हाथी की सवारी जो अतीत में कभी ऐश्वर्य का प्रतीक थी, आज उस सवारी का उपयोग उपहास और दारिद्रय को इंगित कर सकता है।
तब क्या जीवन की जो रीति एक बार विलुप्त हो गई उसे फिर से ज़िंदा करना असंभव हो जाता है? क्या इसीलिए जो भी बचाने योग्य हो, मसलन—हाथी (प्रकृति) से हमारा नाता, उसे बिना देर किए, विलुप्ति की कग़ार पर पहुँचने के पहले बचाना होगा?
आज उपन्यास के लिखे जाने के इतने वर्षों बाद ये तमाम प्रश्न भी कितने मानीख़ेज हो उठे हैं। पूरे उपन्यास के फ़लक में हाथी का दिखना और न दिखने पर ख़ाली जगह का छूट जाना, विलुप्त हो रही वस्तुओं, प्रजातियों का प्रतीक बन कर उभरता है।
उपन्यास के कथानक में सोनसी-रघुवर प्रसाद की नई-नई गृहस्थी और उनके क़रीब की दुनिया है। पड़ोसी हैं, आस-पड़ोस के ख़ूब सारे बच्चे हैं, रघुवर प्रसाद के माता-पिता-भाई हैं, विद्यार्थी हैं, कथानायक के साथ काम करने वाले विभागाध्यक्ष हैं, हाथी और साधु हैं, कमरे की खिड़की पर आती गाय है, आसमान, हवा, पेड़ है और खिड़की से कूद कर उस पार चले जाओ तो जंगल को जाती गोबर से लीपी हुई पगडंडी है, कमल से भरा ताल, चाय के टपरे वाली बूढ़ी अम्मा हैं, पक्षियों का कलरव और रात के आसमान में चहल-क़दमी करते चाँद-तारों का अप्रतिम सौंदर्य है और दरवाज़े से बाहर जाओ तो एक क़स्बाती गली- मोहल्ला, बस स्टैंड, म्यूनिसिपल अस्पताल आदि है।
इस उपन्यास और इसकी खिड़की से पार के दृश्य और दुनिया की व्याख्या प्रायः ‘जादुई यथार्थ’ की तरह की गई है। लेकिन मेरी दृष्टि में यह पूरा उपन्यास एक टाइम-स्पेस-कंटिनुअम है, जिसमें वास्तविक और अवास्तविक में विभेद ही मिट जाता है। वे दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं और इनमें आपस में अदला-बदली भी चलती रहती है। प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की अपनी पहचान और उपयोगिता है, लेकिन इतनी ठोस और मुकम्मल नहीं कि वह किसी दूसरी पहचान में रूपांतरित न हो पाए। दिन है जो रात से अलग पहचाना जा सकता है। रघुवर प्रसाद का महाविद्यालय, उनके सहकर्मी हैं और उससे बिल्कुल इतर चाय पिलाने वाली बूढ़ी अम्मा है जो खिड़की के उस पार पेड़ों के बीच रहती हैं। लेकिन इन तमाम वस्तुओं, जगहों और समय के अलग-अलग प्रहर, दिन, मौसमों के बीच अनवरत आवाजाही है। जब सोनसी एक दिन रघुवर प्रसाद के लिए खाना लेकर महाविद्यालय पहुँच जाती है, तब वह चट्टान और पेड़ जहाँ बैठ कर वे साथ में खाना खाते हैं, उतने ही स्वप्न-से हो जाते हैं, जितनी खिड़की के पार की दुनिया है। उसी प्रकार, खिड़की के पार की बूढ़ी अम्मा यूँ रघुवर प्रसाद की माँ से कोई ख़ास भिन्न नहीं हैं। रिक्शे में बैठकर अस्पताल जाते हुए सोनसी की नीलकंठ देखने की इच्छा को रघुवर ही नहीं, रिक्शेवाला भी पूरा करना चाहता है। जब वह कहता है—“लखोली गाँव चलूँ, वहाँ बहुत नीलकंठ दिखते हैं?” यानी नीलकंठ देखने की काव्यात्मक इच्छा सिर्फ़ रघुवर-सोनसी की नहीं है, रिक्शेवाला के मन में भी ऐसी इच्छाएँ उठती होंगी, तभी तो वह उस गाँव को जानता है—जहाँ नीलकंठ बहुतायत में हैं। यानी काव्यात्मक दृष्टि, संवेदनशील मन जो नीलकंठ देखने को तड़प उठे, सिर्फ़ कवि- कलाकार की मिल्कियत न होकर प्रकृति से जुड़े समाज में एक सर्व सामान्य बात भी हो सकती है।
हमारे देश की भील और राठवा जनजाति में धरती की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए एक अनुष्ठानिक ‘पिठोरा’ चित्रांकन किया जाता है। इसमें पूर्वज देवता ‘पिठोरा कुँवर’ के ब्याह के अवसर पर समूचा ब्रह्मांड मय आकाशगंगा के उपस्थित रहता है। पर उसके ऐन पड़ोस में सात-खंडी धरती, बाँस का झुरमुट और बसौड़ परिवार भी रहता है। यानी, धरती और आकाश, दैवीय और मानुषी संसार में भेद तो है, पर ऐसा नहीं कि उनके बीच संवाद हो न पाए कि वे एक-दूसरे का ‘पड़ोस’ रच ही न पाएँ।
विनोद कुमार शुक्ल के इस उपन्यास में भी यथार्थ और अति यथार्थ, वास्तविक और अवास्तविक एक-दूसरे का ऐसा ही ‘पड़ोस’ रचते हैं। बल्कि, ऐसे वर्गीकरण से मुक्त होते हुए यह कहना चाहिए कि यह उपन्यास किसी सतही, इकहरे यथार्थ की सपाट बयानी के बरक्स कई स्तरों वाले जीवंत यथार्थ को उद्घाटित करता है।
वह निम्न मध्यवर्गीय एक कमरे का घर ही रघुवर-सोनसी की गृहस्थी की एक मात्र वास्तविकता नहीं हैं। उनके मन की मौज, उनकी कल्पना और हाँ, उनके आदर्श—सब मिल कर वास्तविकता को रचते हैं, जो इस प्रकार बहुआयामी हो जाती है। इसीलिए ऐसी आर्थिक तंगी के माहौल में जहाँ पिता की टूटी चप्पल को बदलने के लिए सब्ज़ी-भाजी की खपत में कटौती करनी होगी, वहाँ सुख-साहचर्य का ऐसा सौंदर्यमय संसार खड़ा होता है, जिसे किसी भी आर्थिक संपन्नता से नहीं ख़रीदा जा सकता। इस उपन्यास में निम्न मध्यमवर्ग को स्थापित करनेवाले सारे स्टीरियो टाइप धरे के धरे रह जाते हैं और फिर भी कहानी इतनी अपनी लगती है कि हर घर की लगती है।
फ़्रेंच क्लासिक ‘दी लिटिल प्रिंस’ का प्रसिद्ध वाक्य है—“केवल हृदय से ही सही देखा जा सकता है; जो नितांत आवश्यक है वह आँखों से ओझल रहता है।” यह जो देखने को उसकी सामान्य जगह से विस्थापित कर, अलग कोण से देखना और ‘कविता’ खोज लेना है, क्या यही साहित्य और कला का मुख्य हासिल नहीं है? वह जीवन के सामान्य से किरदार या घटना को विशिष्ट और अविस्मरणीय बना देता है। यह कोई छोटा-मोटा काम नहीं होता। जब होता है, तब चमत्कार से कम नहीं होता। विनोद कुमार शुक्ल अपने उपन्यासों में हमारे गाँव-क़स्बों के लोक जीवन में ‘कविता’ को दाम्पत्य में खोज निकालते हैं।
साहित्य में ‘प्रेम’ को मान्यता प्रायः विवाह पूर्व अथवा विवाहेतर संबंधों को मिली है। प्रेयसी का पत्नी में बदलना तो फिर भी हुआ है, लेकिन पत्नी का प्रेयसी में रूपांतरण एक विलक्षण घटना है जो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों में घटती है।
ज़रा एक नज़र उस समाज पर डालिए जहाँ यह रूपांतरण घटित हो रहा है—तरह-तरह की वर्जनाओं, मर्यादाओं में क़ैद एक रोमांचविहीन, रूटीन पारंपरिक जीवन जिसमें माँ-पिता, भाई-बहन, पति-पत्नी की सदियों पुरानी, तयशुदा-सी भूमिकाएँ हैं, जिसमें ज़िम्मेदारियों का निर्वाह ही सर्वोपरि और श्रेष्ठ माना जाता रहा है। ऐसी स्थितियाँ जिनमें प्रेम की भावना अव्यक्त, अतृप्त, अदृश्य बने रहने को अभिशप्त जान पड़ती है। तिस पर समाज का जाति, धर्म, लिंग, उम्र आदि के आधार पर सर्वमान्य स्तरीकरण स्थितियों को और जटिल बना देता है। परिवारों का ऐसा पारंपरिक ताना-बाना, जिसमें बचपन से बुढ़ापे तक के आपके सारे क्रियाकलाप बग़ैर आपके चुने, पहले से ही तय होते है। उसमें कोई फाँक, कोई रंध्र ही नहीं दिखता कि जिसमें प्रेम का पौधा लहलहा सके। किंतु, क्या कोई समाज पीढ़ी-दर-पीढ़ी बिना प्रेम के प्राणवान बना रह सकता है?
हमारे यहाँ विवाह अवसर पर फेरों के बाद सखियों द्वारा दुल्हन के कान में ‘राम-सीता सा प्रेम’, ‘राधा-कृष्ण सा’, ‘शिव-पार्वती सा प्रेम’ मिलने की कामना कहने का रिवाज़ है। यानी, समाज के पास प्रेम के पुराने ही सही, मॉडल तो हैं। विनोद कुमार शुक्ल के पात्र समाज के, परिवार के पारंपरिक ढाँचे को उस तरह से प्रश्नांकित नहीं करते, बल्कि वे शिद्दत से उसका हिस्सा होते हैं। यानी, उनके पात्र उस ढाँचे से विद्रोह न करते हुए, उसी के भीतर से नई राह खोजते हैं। इसीलिए उनके पात्र सामाजिक या व्यक्तिगत तौर पर किसी मानसिक उथल-पुथल से नहीं गुज़रते। उनके पात्रों के लिए प्रेम के वे प्राचीन मॉडल अभी भी काम के हैं।
विनोद कुमार शुक्ल पारंपरिक लोक जीवन के छंद को रसहीन, उबाऊ और केवल ज़िम्मेदारियों के निर्वाह की तरह नहीं देखते। वह उसे कुछ इस तरह देखते हैं कि उसमें नवोन्मेश जागता है। वह अपनी काव्य प्रतिभा से हमारे मध्यमवर्गीय परिवारों के पारंपरिक वैवाहिक जीवन को, पुराने मॉडलों से प्रेरणा लेते हुए पुनर्विन्यस्त करते हैं और ऐसा करते हुए, दाम्पत्य में प्रेम का आविष्कार करते हैं। उन्होंने सामान्य भारतीय पारिवारिक जीवन से पूरी तरह ग़ायब रोमांच और रूमानियत को अपने उपन्यासों में संभव बना दिया है—जीवन की दीवार में वह फाँक, वह खिड़की पैदा कर दी है जिसमें एक असमाप्य, निरवधि प्रेम अपनी संपूर्ण मांसलता, ल्हास और सौष्ठव के साथ सजीव हो उठता है।
किंतु, यह आविष्कार मात्र सदिच्छा से नहीं होता। सिर्फ़ कल्पना से ‘जादुई यथार्थ’ रचकर भी संभव नहीं होता। विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास की खिड़की महज़ मन की जादुई खिड़की नहीं है। इसके संभव होने की कम से कम दो मूल शर्तें हैं, जिनकी जड़ें ठोस यथार्थ में हैं।
उपन्यास की शुरूआत ही कमरे की खिड़की के उस पार खड़ी, पड़ोस की एक असल बच्ची से होती है, जो चरितनायक के उठने की राह देख रही है कि वह उठें और आम के बौर तोड़कर उसे दे दें जो उसकी माँ ने पूजा के लिए मँगाए हैं। रघुवर प्रसाद उठ कर, खिड़की के उस पार जाते हैं, बच्ची को बौर तोड़ कर देते हैं और फिर कुछ ईंटें लाकर खिड़की के नीचे अच्छी तरह से जमाते हैं, ताकि बच्चों को कमरे में झाँकने में सुविधा हो।
यहाँ लेखक ने साफ़तौर पर खिड़की के उस पार की दुनिया में सबसे पहले बच्चों को प्रतिष्ठित किया है। वह पूरे उपन्यास में जब देखो तब वहाँ खेलते पाए जाते हैं। नव विवाहित रघुवर प्रसाद के मन में अपनी प्राईवेसी का ख़याल नहीं आता। वह तो बच्चों के कमरे में झाँक पाने के लिए उल्टे इंतज़ाम करते हैं! सोनसी भी जब सुबह उठने पर एक बच्ची को खिड़की पर इंतज़ार करते पाती है तो उठ कर उसके नेल पोलिश, टिकुली लगा देती है। वह बिन कहे ही बच्ची के मन की इच्छा को भाँप लेती है। कुछ देर में पाँच और बच्चियाँ उसी फ़रमाइश के साथ आती हैं, और सोनसी उन सभी को सँवारती है। वह अपने शृंगार रस का एक ओर अपनी सास के साथ और दूसरी ओर बच्चियों के साथ साझा करती है और इस तरह अपने शृंगार रस के आनंद की लंबान को बढ़ा देती है। इसी तरह रघुवर प्रसाद गुड़िया नाम की बच्ची को ‘ब’ में छोटे ‘उ’ की मात्रा बुढ़िया कह कर उससे चुहल करते हुए—एक खुला, ज़िंदादिल माहौल रचते हैं, जिसमें बच्चों से बूढ़ों तक सबकी साझेदारी है।
यह उपन्यास प्रस्तावित ही यह करता है कि दीवार में ऐसी जादुई खिड़की का हर जीवन, हर दाम्पत्य में खुलना संभव है कि यह ‘खिड़की’ अक्सर होते हुए भी उपयोग में नहीं लाई जा पाती क्योंकि हमारा बचपन से (बच्चों से), उस निष्प्रयोजन, निष्कलुष ‘मैं’ से नाता ही नहीं रह जाता जिसमें कोई फाँक नहीं थी। जिसमें शंका का कोई काँटा नहीं उगा था। जिसमें स्वयं को पूरी तरह दिया और अन्य को लिया जा सकता था। बड़े होने के बाद बचपन की उस अवस्थिति को जानने का एक मात्र उपाय बच्चों के सानिध्य, उनसे जुड़ कर ही संभव है। रघुवर प्रसाद इसीलिए सोनसी के घर आने की ख़ुशी में वह खिड़की बंद नहीं करते, बल्कि उसे बच्चों के लिए और सुगम, सुलभ बनाते हैं। वह सोनसी के जीवन में आने के पूर्व भी बच्चों के सखा थे। बल्कि, बाद के कथानक में जब पोखर के पास की जगह में सोनसी-रघुवर को रंगोली बनी मिलती है जो उनके प्रणय का बिछावन बनती है और जो निश्चित ही माहौल को जादुई आभा से भर देती है, तो वह भी बच्चों की बातचीत से पता चलता है कि उन्हीं के द्वारा पत्थर के चूरे से डाली गई थी! यूँ रघुवर-सोनसी के प्रेम के जादुई लोक के तार सीधे बच्चों के कल्पना लोक से जा जुड़ते हैं।
इस तरह प्रेम के संभव होने की पहली शर्त बचपन के निष्कलुष जीवन से नाता होना है। बचपन ही वह समय भी है, जब कल्पना लोक सहज सुलभ होता है। बिना कल्पना के दीवार में खिड़की नहीं खुल सकती। इसलिए, यह उपन्यास प्रस्तावित करता है कि कल्पना को ज़िंदा रखना सिर्फ़ लेखक- कलाकार ही नहीं एक गणित के स्कूल टीचर, हमारे और आपके के लिए भी ज़रूरी है! यह राह बच्चों और बचपन के मार्फ़त खुलती है। लेकिन ध्यान रहे कि ये बच्चे आस-पड़ोस के हैं, उनके अपने नहीं। कथानायक-नायिका के बीच उपन्यास के पूरे वितान में कभी उनकी अपनी संतति को लेकर कोई बात नहीं होती। अपनी संतति से तो सभी प्यार करते हैं, किंतु यह लगभग ख़ुद से प्यार करना ही है।
यहाँ अनायास ही दोस्तोयवस्की की अंतिम कहानी ‘द ड्रीम ऑफ़ अ क्वीयर मैन’ का ख़याल हो आता है, जिसमें आत्महत्या करने की कगार पर कहानी के नायक का हाथ अचानक सड़क में एक आठ साल की बच्ची पकड़, उससे सहायता माँगती है। नायक यह सोच सहायता से इनकार कर देता है कि अब जब वह कुछ घंटे में मरने ही वाला है, तब उसके किसी भी कृत्य की क्या अहमियत होगी। लेकिन अपने कमरे पर लौटकर वह बच्ची का चेहरा भुला नहीं पाता और पूरी स्थिति पर, अपने समूचे जीवन पर नए सिरे से गहन विचार करने को बाध्य होता है—ऐसा करते हुए आत्महत्या करने की वह घड़ी टल जाती है। वह बच्ची जो उससे सहायता माँगने आई थी, स्वयं नायक के जीवन जीने की राह खोजने में सहायक बन जाती है! यह पूरी कहानी ही दरअस्ल स्वप्न में घटित होती है। दोस्तोयवस्की अपने नायक के मार्फ़त कहीं यह इशारा करते हैं कि जीवन की अर्थवत्ता दरअस्ल जीवन में हिस्सेदारी से ही मिलती है और भला एक बच्चे से जीवंत क्या होता है?
‘प्रेम’ के संभव होने की दूसरी शर्त जो इस उपन्यास में निर्दिष्ट है, वह है प्रकृति—आसमान, तारे, सूर्योदय, नीम, आम, पोखर, नदी, पहाड़ से क़रीबी नाता। कमरे की खिड़की को नव-विवाहित दंपति बंद करने की बात इसलिए भी नहीं सोचते क्योंकि खिड़की को बंद करने से वे हवा, आकाश, उजास, पक्षियों के कलरव, नीम-आम-महुआ के फूलने की महक, और हाँ बच्चों की निश्छल दुनिया से भी वंचित रह जाएँगे। इस तरह, यह उपन्यास प्रस्तावित करता है कि जीवन को ताज़ादम जीने और समझने के लिए क़ुदरत का साथ ज़रूरी है। ‘यथार्थ’ सहज ही ‘जादुई’ हो उठता है, यदि नदी-पहाड़- पेड़ों का पड़ोस हो। इस उपन्यास के नायक-नायिका का पड़ोस सिर्फ़ मनुष्य से नहीं, बल्कि नदी- पोखर और उसमें खिलते कमल के फूलों से भी बनता है। उनकी रसोई में यूँ सिर्फ़ रोटी-चटनी है लेकिन उसमें साझा गाय, हाथी, तोते और हाँ अपने पिता से छिपने के लिए पेड़ पर चढ़े रहने वाले बच्चे का भी है। यह उपन्यास शहरी जीवन के बरक्स, क़स्बाती जीवन के रोमांच और रूमानियत का चित्र रचता है, वह भी एक ऐसे समय में जब सबको लग रहा है कि जीवन का असल आनंद और रोमांच तो केवल शहरों में ही संभव है।
एक बेहद ग़ौर करने लायक़ बात यह है कि उपन्यास में सिर्फ़ नव-विवाहित सोनसी-रघुवर प्रसाद ही नहीं, उनके बूढ़े माता-पिता भी खिड़की से उस पार जाकर ताल में नहाते हैं और सोनसी-रघुवर प्रसाद के प्रणय की कथा कहती ताल किनारे छूट गई किन्ही भौतिक वस्तुओं (जिसमें सोनसी के पैरों की पायल भी है) को चुपके से सहेज कर ले आते हैं। इन बुज़ुर्ग़ दम्पति के ताल में नहाकर लौटने का वर्णन सोनसी-रघुवर के स्नान प्रसंग से कोई कम रूमानी नहीं है—“रघुवर की माँ के मन में आया कि वह एक फूल चोटी में खोंस लेती पर नहीं खोंसी। पिता के मन में आया कि रघुवर की माँ की चोटी में वे एक फूल खोंस देते पर नहीं खोंसे। पेड़ के नीचे से जब वे आगे बढ़े तो फूलों की सुगंध इनके साथ हो ली। पहले एक फूल की सुगंध इनके साथ हुई फिर बहुत से फूलों की सुगंध इनके साथ हो गई। वे दोनों चुपचाप (घर) आए थे। आहट नहीं थी पर सबको एक साथ फूलों की सुगंध आई थी। उस सुगंध की कोई आहट हुई हो”
खिड़की के पार के अरण्य में उनके बीच घटा यह संवाद भी देखिए—“यहाँ जीवन इतना अच्छा लग रहा है कि लगता है बहुत जी गए और मृत्यु यहाँ से समीप हो” पिता ने कहा। जवाब में आगे माँ कहती हैं—“बचे जीवन को देख लेने के बाद फ़ुरसत मिलेगी तब। जीवित आँख से मृत्यु नहीं जीवन दिखता है।”
नहाने के बाद, माता-पिता भी बूढ़ी अम्मा की चाय पीते हुए बतियाते हैं। यह पूरा प्रसंग एक तरह से प्रेम और साहचर्य की कामना के उम्र के साथ छीजने का प्रतिकार करता है। इस परस्पर पूर्णता के अहसास में प्रकृति का भी भरपूर योग है, तभी तो माँ कहती हैं कि जीवित आँख से मृत्यु नहीं जीवन दिखता है।
उपन्यास में रघुवर प्रसाद के स्कूल में पढ़ाने वाले विभागाध्यक्ष को भी रघुवर प्रसाद के साथ खिड़की के पार के संसार में जाने का अवसर मिलता है, जहाँ आम बीनती सोनसी, कई बच्चे, पत्ते बुहारती बूढ़ी अम्मा, पोखर और कुहुकते पक्षियों वाले पेड़ उन्हें मिलते हैं। अलबत्ता, वे इस दृश्य को अपने परिवार के साथ तमाम कोशिशों के बावजूद अन्य किसी रास्ते से नहीं खोज पाते हैं। निश्चित ही रघुवर प्रसाद के कमरे की खिड़की में और उसके पार के दृश्य में कुछ ख़ास है। लेकिन ग़ौर से देखने पर ऐसा भी नहीं कि वह बिल्कुल अलभ्य, अपने में कोई अजूबा दुनिया हो। उपन्यासकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ही इस बात में है कि यह खिड़की लगातार एक ठोस दीवार की एक ठोस खिड़की भी बनी रहती है और जादुई खिड़की भी। यह उस अर्थ में ‘सुर्रीयल’ या ‘जादुई यथार्थ’ का उपन्यास नहीं है जैसा कि बार-बार इसके बारे में कहा गया है। उपन्यास में रघुवर प्रसाद और सोनसी खिड़की के पार के जंगल में साधु के हाथी पर बैठकर जाना चाहते हैं, पर अफ़सोस कि खिड़की इतनी बड़ी नहीं है कि उसमें से हाथी को बाहर ले जाया जा सके। यदि वह जादुई यथार्थ की खिड़की होती तो उसमें से निश्चित ही हाथी भी जा पाता। इस उपन्यास के युवा पात्र इतने अधुना भी नहीं कि लिहाज़ की ज़रूरत से ही इनकार कर दें—वे खटिया को खड़ा कर एक झीनी आड़ बनाते हैं। किंतु, इतने भीरू भी नहीं कि माता-पिता के गाँव लौट जाने की राह देखते हुए, मन की मौज को अनसुना कर दें—वे माता-पिता, भाई को सोता छोड़ खिड़की से आधी रात कूदकर बाहर जाने का माद्दा रखते हैं। यदि यह खिड़की से बाहर जाना इतना मन ही मन और जादुई यथार्थ में होता तो माँ को इस पूरे वाक़ये का पता चलना आवश्यक नहीं था। माँ न सिर्फ़ देखती-जानती हैं, बल्कि समझती भी हैं। कोई नैतिक झंडा उठाने की बजाय, वह इशारा भर करती हैं कि मुझे सब पता है और फिर स्वयं भी अपने पति के साथ उसी खिड़की से कूदकर नहाने चली जाती हैं और हाँ, छोटे बेटे को साथ नहीं ले जातीं! माँ यदि चुपके से सोनसी का पोलका ला उसे थमा देती हैं तो सोनसी भी उनको पिताजी के साथ पोखर में नहा आने को प्रेरित करती है।
किराए के उस एक कमरे के मकान से सटे हुए दूसरे पड़ोसी रहते हैं। शुरू में ही यह पता चल जाता है कि रघुवर प्रसाद के घर की एक चाबी पड़ोस में भी रहती है, तभी न विद्यालय से लौटने पर उन्हें घर खुला मिलता है। पड़ोसियों ने पिता के लिए खाट नीम तले लगा दी थी, और स्वयं गौना के गीत गा कर नई नवेली सोनसी का सत्कार कर रहे थे। उपन्यास में खटखटाने पर जब भी दरवाज़ा नहीं खुलता तो पड़ोसी बोलते हैं कि वो खिड़की के उस पार चले गए होंगे। कई मौक़ों पर सोनसी या रघुवर प्रसाद अकेले भी खिड़की के उस पार जाते हैं, यानी उस खिड़की से कूद कर उस पार जाना कोई असाधारण बात नहीं है, शायद पड़ोसी भी जाते हों। यह भी संभव है कि पड़ोसियों के कमरे में भी ऐसी ही कोई खिड़की हो।
इस उपन्यास के अनुकथन में न जाने क्यों विष्णु खरे ने लिखा है कि स्कूल में काम करने वाले विभागाध्यक्ष और रघुवर प्रसाद के माता-पिता को ‘खिड़की’ के पीछे की दुनिया नहीं दिखती। वे लिखते हैं कि माँ-बाप गाँव से क़स्बे की यात्रा, कमाऊ बेटे के कमरे के सामने की सांसारिकता से ही संतुष्ट रहते हैं और विभागाध्यक्ष भी चोरी की साइकिल आदि में उलझे रहते हैं। ऐसी तथ्यात्मक भूल शायद उपन्यास को एक ख़ास ढंग से पढ़ने की हड़बड़ी का नतीज़ा है। वर्ना यह उपन्यास तो दरअस्ल बौद्धिक और ग़ैर बौद्धिक, कला रसिक और सामान्य जन के बीच के नक़ली विभेद को मिटाने का उपक्रम करता है। इस उपन्यास की बड़ी सफलता ‘प्रेम’ और ‘कविता’ के जादुई संसार के जनतांत्रिक रूप से सबके लिए उपलब्ध, संभव और पहुँच में होने को स्थापित करना है। जैसा कि ऊपर रेखांकित किया जा चुका है, रघुवर-सोनसी के घर की खिड़की के उस पार के जादुई संसार में, मोहल्ले के तमाम बच्चों, विभागाध्यक्ष, रघुवर प्रसाद के माता-पिता सबका आना-जाना और क्या ख़ूब आना-जाना है।
उपन्यास के कथानक में यूँ कोई जिरह, कोई संघर्ष नहीं है। लेकिन हमारे पारंपरिक लोक जीवन के बिगड़ते छंद, शिक्षित वर्ग के विशेष रूप से उससे कटते जाने की चिंता, निश्चित ही उपन्यासकार के मन में सर्वोपरि है। समूचे चराचर के साथ पारस्परिकता की नातेदारी को फिर खोजना ही वह संघर्ष है जिससे इस उपन्यास का लेखक जूझ रहा है ताकि प्रेम की घर वापसी हो सके।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
