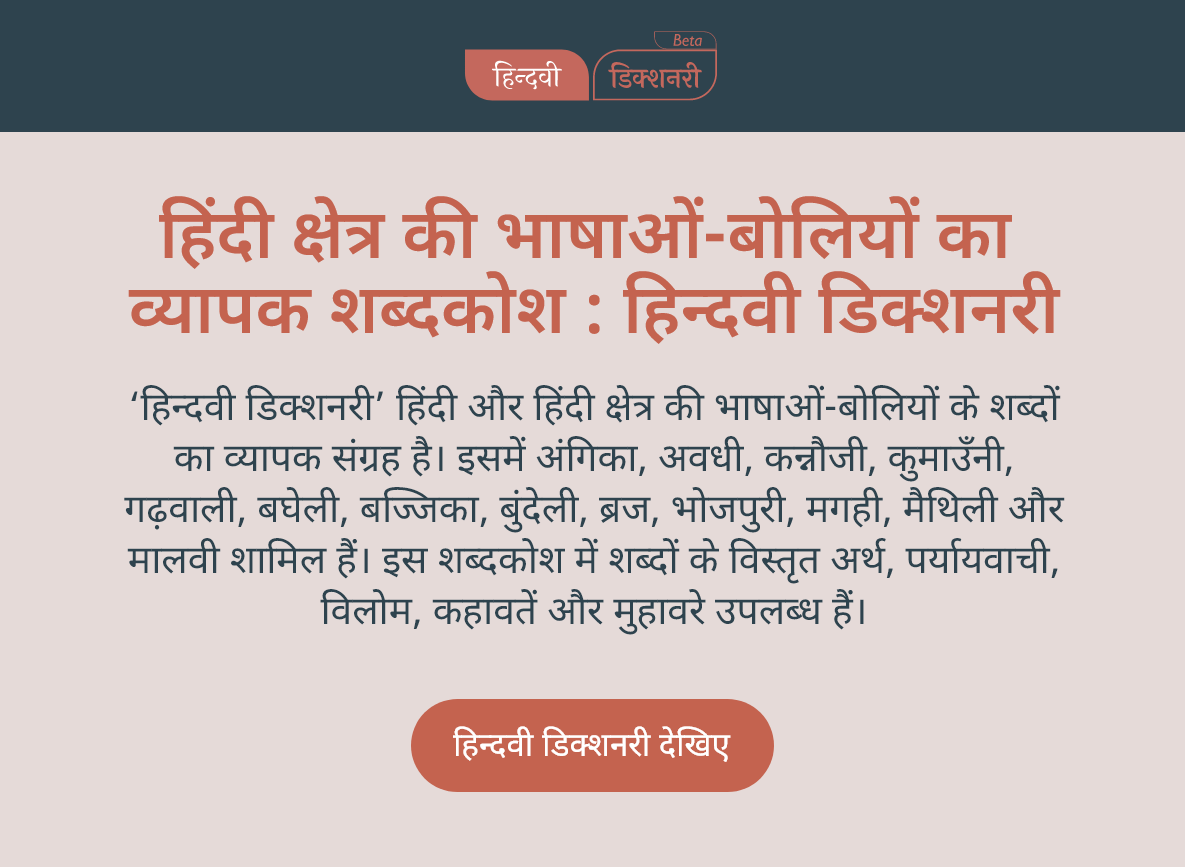भारतेंदु हरिश्चंद्र (बाबू श्यामसुंदर दास)
bhartendu harishchandr
संवत् 1657 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और उसे भारतवर्ष से व्यापार-संबंध स्थापित करने का एकाधिकार दिया गया। बारह वर्ष तक उद्योग में लगे रहने के अनतर संवत् 1666 में इस कंपनी का पहला कारख़ाना सूरत में खुला। इस साधारण घटना से ब्रिटिश जाति और भारतवर्ष के पारस्परिक संबंध का सूत्रपात हुआ। क्रमशः व्यापार की वृद्धि होने लगी। डच और फ़्रांसीसी लोगों ने भी इसी समय के लगभग भारतवर्ष से व्यापारिक संबंध स्थापित किया। इन तीनों यूरोपीय जातियों से पहले तो अपना अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बहुत कुछ स्पर्धा हुई, पर पीछे से जब यूरोप में युद्ध छिड़ गया, तब यहाँ भी उसका परिणाम देख पड़ने लगा और यहाँ भी वे जातियाँ परस्पर छोटा-मोटा युद्ध करने लगीं; यह दशा बहुत वर्षों तक रही। अंत में इस सामरिक तथा व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता में अंग्रेज़ जाति की विजय हुई और वह दृढ़तापूर्वक भारतवर्ष में अपना प्रभुत्व जमाने लगी। संवत् 1814 की पलासी की लड़ाई के उपरांत अंग्रेज़ों के पैर इस देश में दृढ़ता से जमने लगे, परंतु अवस्था अभी तक डाँवाँडोल थी। संवत् 1860 में मुग़ल साम्राज्य का अंत हो गया और मुग़लसम्राट अंग्रेज़ों से पेनशन पाकर अपना जीवन बिताने लगा। अब इस विस्तृत राज्य को भली भाँति शासित करने का उद्योग किया जाने लगा। संवत् 1914 में सिपाही विद्रोह हुआ, जिससे ब्रिटिश शासन की जड़ हिल गई, पर अंग्रेज़ों के सौभाग्य से उन्हें थोड़े ही दिनों में इस विपत्ति से छुटकारा मिल गया और उन्होंने इस विद्रोह का दमन करके अपने शासन की नींव दृढ़ता से जमा ली। इसके उपरांत ब्रिटिश जाति और भारतवर्ष के संबंध की घनिष्ठता दिन पर दिन बढ़ने लगी। एक व्यापारी संस्था ने वाणिज्यव्यापार के लिए इस देश से आकर 250 वर्षों में यहाँ अपना अटल राज्य स्थापित कर लिया।
इस दैवी घटना के कारण इंग्लैंड की अपेक्षाकृत नवीन सभ्यता का भारवर्ष की प्राचीन सभ्यता से संबंध स्थापित हुआ और दोनों में संघर्षण होने लगा। विजय के उत्साह में मग्न होकर अंग्रेज़ अपनी जाति तथा अपने देश के उपकर में दत्तचित्त थे और अत्यंत कुशलतापूर्वक अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्रयत्नवान हो रहे थे। पिछले एक सहस्त्र वर्षों से भारतवर्ष विदेशियों के अधीन होकर तथा उनकी सेवावृत्ति करके अपना जीवन बिता रहा था। एक में उत्साह, जातिप्रेम और देशाभिमान के भाव भरे हुए थे, दूसरा संकटापन्न होकर अपने दिन कठिनाई से काट रहा था। उसे अपने जीवन तक के लाले पड़ रहे थे, स्वार्थपरता ने उस पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लिया था। ऐसी अवस्था में दो भिन्न-भिन्न सभ्यताओं का संघर्षण सम शक्ति से नहीं वल सकता था।
किसी लेखक का कहना है कि यूरोप के लोग पहले व्यापार का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं। उसके पीछे धर्म का झंडा खड़ा किया जाता है और अंत में सभ्यता का अजेय दुर्ग खड़ा होकर विजितों को अपना अस्तित्व भुलाकर उसी की महत्ता स्वीकृत करने के लिए बाध्य करता है। भारतवर्ष में भी क्रमशः ये ही घटनाएँ हुई। जब अंग्रेज़ों के पैर यहाँ जम गए तब उन्हें अपने शासन को सुचारु रूप से चलाने की चिंता हुई। उन्होंने भारतवर्ष को भारतीय सिपाहियों की सहायता से जीता था। अब शासन भी भारतीयों की सहायता से चलने लगा, पर शासन को ठीक-ठीक चलाने के लिए शासक और शासित में परस्पर व्यवहार की आवश्यकता होती है और यह व्यवहार केवल भाषा के द्वारा सपन्न हो सकता अतएव यह आवश्यक हुआ कि शासक शासित की भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और शासित शासक की भाषा का। इस पारस्परिक व्यवहारविनिमय के लिए ऐसे विद्यालयों के स्थापन की आवश्यकता हुई जहाँ अंग्रेज़ों को भारतीय भाषाएँ सिखाई जाएँ। साथ ही ऐसा आयोजन भी अनिवार्य था, अनियार्य ही नहीं वरन् परम आवश्यक था, जिससे भारतीयों को अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराया जाए। इस अन्योन्याश्रित व्यापार की आवश्यकता में मात्रा का भेद रहा। शासकों के लिए भारतीय भाषाओं का व्यावहारिक ज्ञान उतना आवश्यक नहीं था जितना शासितों के लिए, क्योंकि शासितों को अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराके वे उनके द्वारा सुगमता से अपना काम चला सकते थे। इस स्थिति में पहले तो फ़ोर्ट विलियम कालेज में ऐसा प्रबंध किया गया कि इंग्लैंड से आए हुए नवयुवक शासकों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा दी जाए, पर पीछे से इसकी तादृश आवश्यकता न समझी गई और यह कालेज बंद कर दिया गया। पहले चाहे जिस भाव से प्रेरित होकर यह कालेज खोला गया और फिर बंद कर दिया गया हो, पर इसने हिंदी साहित्य का रूप ही बदल दिया। अंग्रेज़ों का यह नियम है कि वे पहले यह निश्चय कर लेते हैं कि कौन-कौन सी बातें हमारे लिए आवश्यक और उपयोगी हैं और तब वे उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नवान हो जाते हैं! हमारी हिंदी भाषा का साहित्य अब तक प्रायः पद्यमय था, गद्य तो उसमें नाममात्र को था। पद्य के द्वारा पारस्परिक व्यवहार कभी चल नहीं सकता। यद्यपि सब देशों के साहित्य में पहले पद्य का ही आविर्भाव होता है, पर साथ ही परस्पर भावविनिमय के लिए गद्य का भी प्रयोग होता है। हिंदी में भी साहित्य का आरंभ पद्यरचना से हुआ है और इसके लिए ब्रजभाषा का ही विशेष प्रयोग हुआ है, पर भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और प्राचीन समय में देश के भिन्न-भिन्न भागों के रहने वालों के आने जाने तथा मिलने-जुलने के साधन सुगम न होने के कारण भावविनिमय के लिए अनेक प्रांतीय भाषाओं तथा उपभाषाओं का खंडराज्य था। इस अवस्था में जब अंग्रेज़ों को शासकों और शासितों के बीच परस्पर व्यवहार स्थापित करने की आवश्यकता हुई, तब वे इस काम के लिए भिन्न-भिन्न उपभाषाओं तथा बोलियों में से किसी एक को नहीं चुन सकते थे। इस काम के लिए उन्होंने मुख्य-मुख्य प्रांतीय भाषाओं को चुना जिसमें हिंदी भी एक थी। पर हिंदी में गद्यग्रंथ तो थे ही नहीं, इसलिए वे इन ग्रंथों के निर्माण की ओर दत्तचित्त हुए। इस प्रकार फ़ोर्ट विलियम कालेज में लल्लूजीलाल, सदल आदि पंडितों को यह काम सौंपा गया और उन्होंने सफलतापूर्वक इसे संपन्न किया। इन घटनाओं के वशवर्ती होकर हिंदी गद्य की नीव दृढ़तापूर्वक रखी गई।
अब इस बात का विचार आरंभ हुआ कि भारतवासियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाए और वह भी किस भाषा के द्वारा। बहुत वाद-विवाद तथा सोच-विचार के अनंतर अंग्रेज़ी भाषा द्वारा पाश्चात्य विद्याओं की शिक्षा देना निश्चित हुआ और उसके अनुसार भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में इसका प्रबंध होने लगा। इस कार्य को इँग्लैंडवासी कितना आवश्यक और उपयोगी समझते थे, इसका अनुमान इसी बात से कर लेना चाहिए कि संवत् 1614 में, जब कि सिपाही-विद्रोह भयानक रूप धारण किए हुए था, पहला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया। तब से लेकर आज तक शिक्षा का कार्य बराबर चला आ रहा है। पाश्चात्य शास्त्रों की शिक्षा देने और अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने में बड़ा अंतर है। एक से ज्ञान की वृद्धि हो सकती है, पर दूसरे से एक विदेशीय जाति के परस्पर व्यवहार की भाषा से परिचय होता है। भाषा द्वारा जो विजय प्राप्त होती है, वह चिरस्थायिनी और अधिक व्यापक होती है। अपनी निज की भाषा, अपने प्राचीन साहित्य तथा अपने प्राचीन इतिहास के ज्ञान से शून्य रहकर जब मनुष्य किसी विदेशीय भाषा, विदेशीय साहित्य और विदेशीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त करता है और उनकी महत्ता पर मुग्ध हो जाता है, तब वह धीरे-धीरे अपने आप को भूलने लगता है और अंत में विदेशीय रंग में ऐसा रंग जाता है कि उसे अपने देश की सब बातों से विराग उत्पन्न होने लगता है, उसे अपनी भाषा गँवारू और व्यंजक-शक्तिरहित जान पड़ने लगती है, अपना साहित्य हीन और अपूर्ण देख पड़ने लगता है और अपने इतिहास में पारस्परिक ईर्ष्याद्वेष के झगड़ों को छोड़कर और कुछ मिलता ही नहीं; सारांश यह कि वह अपने आपको एक अशिक्षित, असभ्य और गुणहीन जाति का मनुष्य समझने लगता है। अँग्रेज़ी शिक्षा ने बहुत दिनों तक शिक्षित भारतीयों के हृदयों पर ऐसा ही प्रभाव डालना आरंभ कर दिया था। वे सब बातों में शासकों ही को सर्वश्रेष्ठ और अपना आदर्श मानने लगे थे; उनका अनुकरण करने में ही अपना महत्व समझते थे। रहन-सहन, कपड़ेलत्ते, चाल-ढाल, बातचीत आदि सब बातों में अंग्रेज़ उनके आर्दश हो रहे थे। यदि यह अवस्था और कुछ काल तक बनी रहती, तो भारतवर्ष का रूप ही कुछ का कुछ हो जाता। उसमें अपने पूर्व गौरव का कोई चिह्न वर्तमान न रह जाता। वह अंग्रेज़ी रंग में ऐसा रंग जाता कि उसे क्रिस्तान होने, अंग्रेज़ी भाषा बोलने और अंग्रेज़ी आचार-विचार तथा व्यवहार को अंगीकार करने में ही अपने जीवन का सफल जान पड़ने लगता। पर ईश्वर को यह स्वीकृत न था। उसकी तो यह इच्छा थी कि पूर्व और पश्चिम के सम्मेलन से वृद्ध भारत फिर से जाग उठे, उसमें नई शक्ति का संचार हो जाए, वह नए भावों से पूर्ण हो संसार की उन्नत जातियों में पुनः अपना महत्व स्थापित करे। संसार में जब-जब ऐसे महत्व के परिवर्तन होने को होते हैं, तब-तब उनको सिद्ध करने के लिए विशेष शक्तिसंपन्न आत्माओं का आविर्भाव होता है। ब्रह्मसमाज ने बंगाल को क्रिस्तान होने से बचा लिया। उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म और समाजसुधार की ऐसी बलवती धारा प्रवाहित की कि देश का यह भाग अपने पूर्व गौरव को समझ और अपने प्राचीन आचार-विचार से अभिज्ञ होकर क्रिस्तान होने से बच गया। वैसे ही भारतेंदु हरिश्चद्र ने हिंदी भाषा में नई संजीवनी शक्ति का संचार कर उसे इस योंग्य बना दिया कि वह जातीय विकास की सहायक होकर भारतवासियों की मातृभाषा के उपयुक्त गौरव को प्राप्त करने में समर्थ हुई। पहले कहा जा चुका है कि सभ्यता की विजय राजनीतिक विजय से अधिक महत्वपूर्ण और स्थाई होती है। संयोग से जब राजनीतिक विजय के साथ सभ्यता की विजय की सहयोगिता और सहकारिता हो जाती है तब वह राजनीतिक विजय चिरस्थायिनी होकर किसी विजित देश को सदासर्वदा के लिए अपना बना लेती है। एक दूरदर्शी लेखक का कथन है कि यदि किसी देश को निरंतर दासत्व की शृंखला में बाँधे रखना हो, तो पहले उसका इतिहास नष्ट कर देना चाहिए। इसका सबसे सुगम उपाय उस देश के वासियों में अपनी मातृभाषा से अरुचि उत्पन्न करके विजेता की भाषा के प्रति विशेष अनुराग और गाढ़ी ममता उत्पन्न कर देना है। भारतवर्ष में यही उद्योग किया गया था, पर ‘मेरे मन कछु और थी कर्ता के मन और’। ईश्वर ने भारतेंदु हरिश्चंद्र को इस लोक में भेजकर इस प्रवाह को उल्टा बहा दिया। मातृभाषा हिंदी के प्रति विराग के स्थान पर अनुराग उत्पन्न हो गया। पाश्चात्य शिक्षाप्राप्त लोगों की रुचि बदल गई और उनमें अपने साहित्य-भंडार को सुंदर-सुंदर रत्नों से भरने की उत्कट कामना उत्पन्न हो गई।
भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हिंदी-साहित्य का नया युग प्रारंभ होता है। इन्होंने जिस अवस्था में हिंदी को नया पाया वह विलक्षण थी। पद्य में जायसी, सूर, तुलसी आदि के आख्यानकाव्यों का समय एक प्रकार से बीत चुका था। केशव के चलाए हुए नायिकाभेद, रस, अलंकार आदि को लक्ष्य करती हुई स्फुट कविताओं के छींटे उड़ रहे थे। गद्य प्रेमसागर, सिंहासनबत्तीसी और वैतालपचीसी से ही संतोष किए बैठा था।
यद्यपि देश में नए-नए भावों का संचार हो गया था, पर हिंदी भाषा उनसे दूर थी। लोगों की अभिरुचि बदल चली थी, पर हमारे साहित्य पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा था। शिक्षित लोगों के विचारों और व्यापारों ने दूसरा मार्ग तो पकड़ लिया था, पर उनका साहित्य उसी पुराने मार्ग पर था। ये लोग समय के साथ स्वयं तो कुछ आगे बढ़ पाए थे, पर जल्दी में अपने साहित्य को साथ न ले सके। उसका साथ छूट गया और वह उनके कार्यक्षेत्र से अलग पड़ गया। प्रायः सभी सभ्य जातियों का साहित्य विचारों और व्यापारों से लगा हुआ चलता है। यह नहीं कि उनकी चिंताओं और कार्यों का प्रवाह तो एक ओर हो और उनके साहित्य का प्रवाह दूसरी ओर। फिर यह विचित्र घटना यहाँ कैसे हुई? बात यह है कि जिन लोगों के हृदय में नई शिक्षा के प्रभाव से नए विचार उत्पन्न हो चले थे, जो अपनी आँखों से देशकाल का परिवर्तन देख रहे थे, उनमें अधिकांश तो ऐसे थे जिनका कई कारणों से हिंदी साहित्य से लगाव छूट सा गया था, और शेष ऐसे थे जिन्हे हिंदी-साहित्य का मंडल बहुत ही बद्ध और परिमित दिखाई देता था तथा जिन्हें नए विचारों को सन्निविष्ट करने के लिए स्थान ही नहीं सूझता था। उस समय एक ऐसे साहसी और प्रतिभासंपन्न पुरुष की आवश्यकता थी जो कौशल से इन बढ़ते हुए विचारों का मेल देश के परंपरागत साहित्य से करा देता। बाबू हरिश्चंद्र का प्रादुर्भाव ठीक ऐसे ही समय में हुआ और वे यह कार्य करने में समर्थ हुए।”
भारतेंदुजी की साहित्यसेवारूपी सरिता अनेक धाराओं में प्रवाहित हुई थी। नाटक, आख्यान, काव्य, स्तोत्र, परिहास, इतिहास, माहात्म्य इत्यादि भिन्न-भिन्न विषयों पर इनकी लेखनी परिचालित हुई थी। साधारणतः हम इनकी रचनाओं का दो मुख्य भागों में विभक्त कर सकते हैं—पद्यात्मक रचनाएँ और गद्यात्मक रचनाएँ। इन दोनों प्रकार की रचनाओं में हम समान रूप से एक व्यापक भाव पाते हैं। चाहे जैसा अवसर हो और चाहे जिस प्रकार की रचना की आवश्यकता हो, भारतेंदुजी अपने देश को नहीं भूलते, घूम-फिरकर इन्हें उसके पूर्व गौरव, वर्तमान हीन अवस्था और भविष्य का ध्यान आ ही जाता है और वे तत्सबंधी अपने हृदयोद्गारों को रोक नहीं सकते। जिस समय भारतीय सेना के मिस्र में विजय प्राप्त करने का समाचार इस देश में पहुँचा, काशी में इस उपलक्ष में बड़ा आनंद मनाया गया। भारतेंदुजी ने उस अवसर पर “विजयिनी विजय वैजयंती” शीर्षक कविता लिखकर अपना आनंद प्रकट किया था। बुद्ध की घटना का इस प्रकार साधारण वर्णन करते हुए—
तड़ित तार के द्वार मिल्यो सुभ समाचार वह-
भारतसैना कियों ओर संग्राम मिअ महँ॥
जेनरल मकफरसन आदिक जे सेनापतियन।
तिन लै भारतसैन कियों भारी अति ही रन॥
घोलि भारती सैन दई आवसु उठि घाओ।
अभियानी अरबी वेगहि वेगहि पाहि लाओ॥
सुनि कै सबहि परम वीरता आज दिखाई।
सत्रुगनन सों सन्मुख भारी करी लराई॥
छिन में सत्रु भगाइ यस्लो अरबी पासा कहूँ।
तीन सहस रनबीर करे बँधुआ सगर महँ॥
आरजगन को नाम आजु सबही रख लीनो।
पुनि भारत को लील जगत महँ उन्नत कीनो॥
जहाँ भारतवर्ष का नाम, भाषा, से अपने को संभाल नहीं सके और अपने प्यारे देश के विषय से इस प्रकार कह चले—
कित अर्जुन कित भीम कित्त, करने नकुल सहदेव।
कित्त विराट अभिमन्यु कित, द्रुपद सख्य नरदेव॥
प्राचीन गौरव का स्मरण करते ही उन्हें वर्तमान दीन अवस्था का भी स्मरण हो आता है।
हाय वहै भारत भुव भारी, सबही विधि ते भई दुखारी।
यह कहा जा सकता है कि यह विषय ही ऐसा था कि कवि की लेखनी इस प्रकार चंचल हो उठी। पर यही प्रवृत्ति उनके नाटकों में भी देख पड़ती है। भारत-दुर्दशा, नीलदेवी, अँधेरनगरी आदि रचनाओं में देशहितैषिता के भाव कूट-कूटकर भरे हैं। भारत-दुर्दशा के आरंभ में ही वे लिखते हैं—
रोंबहु सब मिलिकै आवहु भारत भाई।
हा हा! भारतदुर्दशा न देखी जाई॥
सबके पहिले जेहि ईश्वर धन बल दीनो।
सबके पहिले जेहि सभ्य विधाता कीनो॥
सबके पहिले जो रूप रंग रस भीनो।
सबके पहिले विद्याफल जिन गहि लीनों॥
अब सबके पीछे सोई परत लखाई।
हा हा! भारतदुर्दशा न देखी जाई॥
जहँ भए शाक्य हरिचदर नहुष ययाती।
जहँ राम युधिष्ठिर बासुदेव सर्याती॥
जहँ भीम करन अर्जुन की छटा दिखाती।
तह रही मूढ़ता कलह अविद्या राती॥
इसी नाटक के छठे अंक के आरंभ में भारतभाग्य से कहलाते हैं—
सोबत निसि बैस गंवाई, जागो जागो रे भाई।
निसि की कौन कहै दिन बीत्यो कालराति चलि आई॥
देख परत नहिं हित अनहित कछु परे बैंरि बस जाई।
निज उद्धार पंथ नहि सूझत सोस धुनत पछताई॥
अबहुँ चेति पकरि राख्यो किन जो कछु बची घड़ाई।
फिरि पछिताए कछु नहिं है है रहि जैहो मुँह बाई॥
इसके आगे भारत के प्राचीन गौरव का ऐसा सुंदर चित्र खींचा गया है जिसे पढ़ते ही रोमांच हो आता है और हृदय देशाभिमान से पूर्ण हो जाता है, पर अंत में अपनी वर्तमान अवस्था देख कर कवि का यह कहना सोई भारत की आज यह भई दुरदशा हाय उसके क्षोभ, उसकी निराशा और उसकी उद्विग्नता सूचित करता है। इसी प्रकार नील देवी के सातवें अंक में सब भाँति देव प्रतिकूल होइ एहि नासा आदि पंक्तियों में उन्होंने भारतवर्ष की वर्तमान और भावी अवस्था का कैसा सच्चा पर साथ ही कितना हृदयविदारक चित्र अंकित किया है जिसे पढ़कर भारतमाता का कौन ऐसा पुत्र होगा जिसका हृदय विचलित न हो उठे और जिसके मुँह से अनायास आह न निकल पड़े? जब मनुष्य सब ओर से हार जाता है तब उसका ध्यान दीन-दुखियों के एकमात्र आश्रय परमेश्वर की ओर जाता है और वह उसकी शरण में जाकर अपने प्राण की प्रार्थना करता है। नीलदेवी के आठवें अंक में यह विनय कितनी हृदयस्पर्शी और द्रावक है—
कहाँ करनानिधि केसब सोए!
जागत नेक न यदपि बहुत विधि भारतवासी रोए।
इक दिन वह हो जब तुम छिन नहिं भारतहित बिसराए॥
प्रलयकालसम साग सम का बहुत बनाई।
उत के पसु गज को आरत लखि आतुर प्यादे वाए॥
इक दिन दीन हीन नर के हित तुम दुख सुनि अकुलाई।
अपनी संपत्ति जानि इनहि तुम रहो तुरंतहि वाई॥
प्रलबकाल सम जौन सुंदरसन असुर-प्रान-संहारी।
ताकी घार भई अब कुंतित हमरी वेर मुरारी॥
दुष्ट जवन बरबर तुव संतति घास साग सम काटैं।
एक एक दिन सहस सहस नर सीस काटि भुव पाटैं॥
है अनाथ भारत कुलविधवा बिलपहिं दीन दुखारी।
बल करि दासी तिनहिं बनावहिं तुम नहिं लजत खरारी॥
कहाँ गए सब शास्त्र कहा जिन भारी महिमा गाई।
भक्तबछल करुनानिधि तुम कहँ गायों बहुत बनाई॥
हाय सुनत नहिं निठुर भए क्यों परम दयाल कहाई।
सब विधि बूड़त लखि निज देसहिं लेहु न अबहुँ बचाई॥
इस नाटक के संबंध में भी वही आपत्ति खड़ी की जा सकती है जो 'विजयिनी विजय वैजयंती' में हो सकती है, पर शृंगार-रस-पूर्ण कर्पूरमंजरी” के प्रशस्तिवाक्य को देखिए—
उन्नत चित ह्र आर्य परस्पर प्रीति बढ़ावै।
कपट नेह तजि सहज सत्य व्यौहार चलावै॥
जबन ससरमजात दोपगन इनसों छूटें।
सबै मुपथ पथ चल नितहि सुख सपति लूटे॥
तजि विविध देवरति कर्ममति एक मक्ति पथ सब गहैं।
हिय भोगवती सम गुप्त हरि प्रेम धार नितही बहे॥
इसी प्रकार 'सत्य हरिश्चत' का प्रशस्ति वाक्य है, जिसका उपयोग 'कविवचन सुधा' के सिद्धांत वाक्य में किया गया है। ऐसे ही और भी अनेक उदाहरण उपस्थित किए जा सकते हैं और तो और, प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान को जगाने के लिए जागो मणलरूप सफल बजन रखवारे कहते हुए भी उन्हें भारतभूमि का स्मरण हो आता है और वे यहाँ के प्राचीन गौरव की बात कहते-कहते भगवान से वह प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकते—
जागो हौं बलि गई विलब न तनिक लगावहु।
चक्र सुदर्सन हाथ धारि रिपु मारि गिरावहु॥
थामहु थिर, करि राज छत्र खिर अटल फिराबहु।
सूरखता दीनता कृषा करि बेग नसावहु॥
गुन विद्या धन बल मान बहु सबैं प्रजा सिलिकै लहै।
जय राज राज महराज की आनंद सो सब ही कहै॥
सब देसन की कला सिमिटिकै इतनी आषै।
कर राजा नहिं लेह प्रजन पै हेत बढ़ावै॥
गाय दूध बहु देहिं तिनहि फोऊ न नसावै।
द्विजगन आस्तिक होहिं मेंघ सुभ जल बरसावे॥
तजि छुद्र बासना नर सबै निज उछाह उन्नति करहिं।
कहि कृष्ण राधिकानाथ जय हमहूँ जिय आनंद भरहिं॥
सारांश यह कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के हृदय में सब अवसरों, सब अवस्थानों और सब फालों पर अपने देश की स्मृती जाग्रत हो उठती थी और वे उसी की भलाई की कामना निरंतर करते रहते थे। इसी देशभक्ति के भाव से प्रेरित होकर वे सब कार्यों में प्रवृत्त होते थे। यह उनका जीवनव्यापी भाव और व्येय था। हमारी समझ में भारतेंदुजी की इतनी महत्ता इसलिए नहीं मानी जानी चाहिए कि वे उच्च कोटि के कवि, हिंदी को नया जीवन तथा स्वरूप देने वाले आदरणीय गद्यलेखक, अथवा नाट्यसाहित्य की नींव रखने वाले नाट्यकार थे, जितनी इस बात के लिए मानी जानी चाहिए कि वे भारतभूमि की हितचिंता में निरत रहकर उसके अभ्युदय की सदा कामना करने वाले, अपने सब कामों में उसी आदर्श को सामने रखकर कार्यक्षेत्र में अवतीर्ण होने वाले और उसकी सिद्धि के लिए अपने आपको तथा अपना सर्वस्व उसके लिए निछावर कर देने वाले थे। देशहितैषिता ही उनका मुख्य प्रेरक भाव था, और सब बातें गौण तथा उसी मुख्य भाव की पुष्टि के लिए थीं।
भारतेंदजी ने 38 वर्ष और 4 महीने की आयु पाई और 16 वर्ष की आयु में उनके सार्वजनिक जीवन का आरंभ हुआ। इस हिसाब से के लगभग 18 वर्ष तक अपने देश की सेवा तथा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर सके। इस अल्पकाल ही में उन्होंने जो कुछ कर दिखाया वह उनकी स्मृति की सदा बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक है। उत्तर भारत पाश्चात्य सभ्यता और पाश्चात्य शिक्षा के प्रवाह में बह चला था, उसमें यह इतना निमझ हो चला था कि उसे आपने वास्तविक रूप का ज्ञान ही न रह गया था। इस प्रवाह में उसका पुराना साहित्य पीछे छूट गया था और एक प्रकार से देश की साधारण स्थिति से उत्तका संपर्क कम होता जाता था तथा उसकी भाषा नए-नए भावों और विचारों को प्रकट करने में असमर्थ हो रही थी। ऐसी स्थिति से साहित्य के प्रवाह को देशकाल के अनुकूल बहाकर तय भाषा को नया रूप देकर अपने देश की अपने साहित्य की और अपनी भाषा की उन्होंने रक्षा कर ली। यद्यपि भारतेंदुजी की साहित्यिक सेवा अमूल्य थी पर उनका महत्व उसके कारण इतना नहीं है जितना हिंदी भाषा को संजीवनी शक्ति देकर उसे देशकाल के अनुकूल सामर्थ्ययुक्त बनाने और देशहितैषिता के भावों को अपने देशवासियों के हृदयों में उत्पन्न करने में था। लल्लूजी लाल ने जिस भाषा को नया रूप दिया, लक्ष्मणसिंह से जिसे सुधारा, उसको परिमार्जित और सुंदर साँचे में ढालने का श्रेय भारतेंदुजी को प्राप्त है। उनके समय में भी इस बात का झगड़ा चल रहा था कि हिंदी उर्दू-मिश्रित हो या नहीं। राजा शिवप्रसादजी उर्दू-मिश्रत भाषा के पक्षपाती और उर्दू शैली के पृष्ठपोषक थे। भारतेंदुजी ने इसके विरुद्ध शुद्ध हिंदी का पक्ष लिया और उसको नए साँचे में ढालकर एक नवीन शैली की स्थापना की। उनकी भाषा में माधुर्य गुण की प्रचुरता है तथा वह प्रौढ़ता और परिमार्जितता से संपन्न है। उन्होंने स्वयं लिखा है कि 'हरिश्चंद्र मैगजीन' के उदय के साथ संवत् 1930 में हिंदी नए साँचे में ढली।
भारतेंदुजी के जीवन का उद्देश्य अपने देश की उन्नति के मार्ग को साफ़-सुथरा और लंबा-चौड़ा बनाना था। उन्होंने इसके काँटों और कंकड़ों को दूर किया, उसके दोनों ओर सुंदर-सुंदर क्यारियाँ बनाकर उनमें मनोरम फलफूलों के वृक्ष लगाए। इस प्रकार उसे ऐसा सुरम्य बना दिया कि भारतवासी उस पर आनंदपूर्वक चल कर अपनी उन्नति के इष्ट स्थान पर पहुँच सके। यद्यपि भारतेंदुजी अपने लगाए हुए, वृक्षों को फल फूलों से लदा न देख सके, फिर भी हमको यह कहने में किसी प्रकार का संकोच नहीं होता कि वे अपने जीवन के उद्देश्य में पूर्णतया सफल हुए। हिंदी भाषा और साहित्य की जो उन्नति आज देख पड़ रही है उसके मूल कारण भारतेंदुजी हैं और उन्हें ही इस उन्नति के बीज को आरोपित करने का श्रेय प्राप्त है। यदि वे उसकी भावी उन्नति का मार्ग परिष्कृत न करते, उसे सुरम्य न बनाते, तो अब तक उसका अस्तित्व ही लुप्त हो जाता और साथ ही देश के रूपरंग में ऐसा परिवर्तन हो जाता कि वह कठिनता से पहचाना जा सकता। उन्होंने अपने अव्यवसाय से, अपने स्वार्थत्याग से, अपनी प्रतिभा से, अपनी देशहितैषिता से, अपने सर्वस्व को आहुति देकर उसे स्थाई रूप दे दिया और उसे अंधकूप में गिरने से बचा लिया। इस भारतीय प्रकाश के चंद्रमा को अस्त हुए आज 42 वर्ष हो चुके पर उसकी यशच द्रिका ज्यों की त्यों चारों ओर अब तक छिटक रही है और जब तक इस भारतभूमि में हिंदीभाषा, हिंदीसाहित्य और हिंदीभाषाभाषियों का नाम रहेगा तब तक यह चंद्रिका भी नित्य नई उज्ज्वलता से छिटककर भारतीय इतिहास को उज्वल और हिंदी-साहित्यसेवियों के मार्ग को प्रकाशित कर उन्हे उत्साहित करती रहेगी—
जब लौ भारतभूमि मध्य प्रारजकुल बासा।
जब लौं पारजधर्म माहिं प्रारज विश्वासा॥
जब लौ गुन आगरी नागरी आरज बानी।
जब लौं आरजबानी के प्रारज अभिमानी॥
तब लौ यह तुम्हरों नाम थिर चिरजीवी रहिहै अटल।
नित च द सूर सम सुमिरिहैं, हरिच दहु सज्जन सकल॥
[श्रीधर पाठक]
- पुस्तक : हिंदी निबंधमाला (दूसरा भाग ) (पृष्ठ 103)
- संपादक : श्यामसुंदर दास
- रचनाकार : श्यामसुंदर दास
- प्रकाशन : नागरी प्रचारिणी सभा
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.