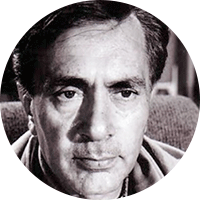पृथ्वीराज सन् 1926 के लगभग अभिनय की भूख मिटाने के लिए अपने प्यारे शहर पेशावर को छोड़कर बंबई आए थे। यह वह ज़माना था जब पंजाब का मध्यम वर्ग अपनी भाषा, अपने रहन-सहन और साहित्य के प्रति विरक्त था। उस समय आज की तरह पंजाबी भाषा में अच्छे नाटक और उपन्यास नहीं लिखे जा रहे थे। आज भी पंजाबियों की बहुत बड़ी संख्या अपने नए और पुराने साहित्य से अनभिज्ञ है, लेकिन बँटवारे के ज़ख़्म की पीड़ा ने दोनों तरफ़ के लोगों को उस साझे ख़ज़ाने का एहसास ज़रूर करा दिया है, जो हर पंजाबी के ख़ून में दबा पड़ा है और जो कभी बाँटा नहीं जा सकता। वारिस शाह, फ़रीद, नानक, बुल्लेशाह, दमोदर इत्यादि इस ख़ज़ाने के अनमोल मोती हैं, और इनकी फ़रमाइश आज फिर से नए रन पैदा कर रही है। लेकिन वह वक़्त और था। उस वक़्त पंजाबी भद्र लोग नाटक और फ़िल्म को विशेष तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। बुज़ुर्ग कहते थे कि ऐसे काम शरीफ़ लड़कों के लिए नहीं हैं। और उस ज़माने के नाटकों का हाल भी बुरा ही था। धंधेदार कंपनियों के पेश किए हुए नाटकों का सांस्कृतिक स्तर उतना ही गिरा हुआ था जितना कि बद-क़िस्मती से कुछ वर्षों से हमारी फ़िल्मों का गिर चुका है। उनका मक़सद कलात्मक नहीं, सिर्फ़ पैसा कमाना था। उनके भाव और उनका ढंग दोनों घटिया थे। उनके लिखने वालों को पैसे की मजबूरी ने साहित्यिक वेश्या बना दिया था। शृंगार रस को छोड़कर अपने बुज़ुर्गों के बताए हुए बाक़ी सारे रस भूल चुके थे।
आख़िर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में आशा की एक नई किरण फूट पड़ी। शेक्सपियर की यथार्थवादी परंपरा में सदियों से पले हुए यूरोपियन नाटक का असर हमारे नौजवानों पर पड़ने लगा। कॉलेजों की ड्रामा सोसाइटियाँ शेक्सपियर, बर्नार्ड शॉ, इब्सन, गॉल्सवर्दी इत्यादि के नाटक या तो सीधे अंग्रेज़ी में या फिर उर्दू में अनुवाद करके खेलने लगीं। खेलने वालों की ना-तजुर्बेकारी की वजह से ये नाटक बहुत ज़ियादा सफल नहीं होते थे, और न ही आम जनता पर इनका कोई असर पड़ता था। लेकिन निस्संदेह इनके द्वारा नाटक-प्रेमी युवकों में एक नर्इ 'स्पिरिट' पैदा हो गई थी। अहमदशाह बुख़ारी, गुरुदत्त सोंधी, ईश्वरचंद्र नंदा, के. एल. सहगल, दीवान शरर, ज़ुल्फ़िकार बुख़ारी, इम्तियाज अली ताज, रफ़ी पीर, पृथ्वीराज कपूर इत्यादि इस ‘स्पिरिट’ की पैदावार थे और इनमें से अधिकांश अपनी रुचि के अनुकूल वातावरण की तलाश में पंजाब से बाहर चले गए थे। कलाकार पृथ्वीराज और उनके थिएटर को परखने के लिए यह देखना आवश्यक है कि वह नई 'स्पिरिट' क्या थी।
शेक्सपियर से पहले यूरोप का नाटक भी हमारे प्राचीन नाटकों की तरह देवी-देवताओं या राजा-महाराजाओं की स्तुति का साधन हुआ करता था। रोज़मर्रा के जीवन से उसका बहुत ही कम संबंध था। उस नाटक की भाषा कविता थी, वह भी ऐसी जिसमें सच्ची मानुषिक भावनाएँ कम, शब्द-क्रीड़ा और अतिशयोक्ति ज़ियादा थी। उनका उद्देश्य शाही दरबार की चापलूसी और शासकों का मनोरंजन था। साधारण पात्रों को अव्वल तो स्टेज पर लाया ही नहीं जाता था, और अगर कभी लाया भी जाता तो प्रहसन मात्र के लिए। कालिदास एक अमर और महान नाट्यकार हैं, इसमें कदापि संदेह नहीं है। लेकिन विचार और टेकनीक की दृष्टि से उनके नाटक एक अंश तक उपर्युक्त प्राचीन स्पिरिट से प्रभावित मालूम पड़ते हैं जो उनका युग देखते हुए स्वाभाविक है।
लेकिन शेक्सपियर ने नाटक की दुनिया में एक ज़बरदस्त इंक़लाब पैदा कर दिया और एक नए युग का आरंभ हुआ।
जिस ज़माने में शेक्सपीयर पैदा हुआ, इंगलिस्तान की सामाजिक व्यवस्था एक क्रांति के दौर में से गुज़र रही थी। व्यापारी और कारख़ानेदार ऊपर आ रहे थे, ख़ानदानी मुफ़्तख़ोर ज़मींदार और जागीरदार नीचे जा रहे थे। व्यापारियों के जहाज़ देश-देशांतर के तटों से टकरा रहे थे, नए स्थलों की खोज कर रहे थे। उनका उद्यम विज्ञान को तरक़्क़ी दे रहा था। अनपढ़ देहातियों के लिए ज़मींदारों के ज़ुल्म से भागने के लिए नर्इ राहें और नए उपनिवेश खुल रहे थे। सरमायादारों की अगुवाई में एक नया क़ौमी भाव पैदा हो रहा था कि जागीरदारी ख़त्म हो, सारे देश का एक ही बादशाह हो, और देश एक पार्लियामेंट का विधान स्वीकार करे। इस इंक़लाबी वक़्त में, जिसे साहित्य में 'रेनेसाँ' कहा जाता है, इंसान यह अनुभव करने लग गया था कि वह सिर्फ़ क़िस्मत के हाथ का खिलौना नहीं, बल्कि ज्ञान में वृद्धि करके प्रकृति पर भी क़ाबू पा सकता है। अपनी श्रेष्ठता वह अनुभव करने लगा था।
शेक्सपियर ने नाटक द्वारा इस नए अनुभव, इस नई स्पिरिट का एलान किया। देवी-देवताओं को त्यागकर उसने मनुष्य का अध्ययन करना शुरु किया चाहे वह राजा हो या रंक। मानवीय हृदय की भावनाओं को यथार्थ भाषा में पेश करने का उसने बीड़ा उठाया चाहे वह प्रेम की भावना हो, ईर्ष्या की, वैराग्य की, या देशभक्ति की।
उसने नाटक में गद्य का प्रयोग करना शुरू किया और पद्य को भी ठोस और स्पष्ट बनाया।
उसने जनता के 'एक देश, एक बादशाह और एक पार्लियामेंट' के नारे से प्रेरित होकर दर्जनों ऐतिहासिक नाटक लिखे, जिनके द्वारा देशभक्ति की भावनाओं को विकसित किया। शेक्सपियर ने नाटक के इतिहास में पहली बार स्त्री को इंसान का दर्जा दिया, पात्रों को भी सजीव और यथार्थ ढंग से पेश किया। इससे पहले स्त्री का दर्जा नाटकों में सिर्फ़ यही था कि वह पुरुष की संपत्ति है।
संक्षेप में, शेक्सपियर ने ज़िंदगी से भागने की परंपरा को ख़त्म करके ज़िंदगी ही को स्टेज पर लाने की परंपरा शुरु की। उसने प्रगतिशील विचारों को अपनाया और पुराने मृत विचारों का त्याग किया। उसने नाटक की एक नई परिभाषा क़ायम की, और वह परिभाषा आज तक पुरानी नहीं हुई है। उसके यथार्थ विचारों ने यथार्थवादी टेकनीक को भी जन्म दिया। टेकनीक के क्षेत्र में भी शेक्सपियर की क़ायम की हुई क़द्रें आज तक पुरानी नहीं हुई है। आज भी हैमलेट के मुँह से अभिनेताओं को दिलवाई हुई नसीहत अभिनय का सही और सच्चा मार्ग दिखाती है, जो प्रत्येक अभिनेता के लिए शिरोधार्य है। उसका एक उद्धरण यहाँ देना अप्रासंगिक न होगा :
हैमलेट (एक अभिनेता से)- ठीक उसी ढंग से अपना पार्ट अदा करना, जैसा मैंने कहा है। अपनी पंक्तियाँ ऐसे बोलो, जैसे वह तुम्हारी ज़बान पर नृत्य कर रही हों। अगर तुम्हें चिंघाड़ना है, तो पहले से बता दो, मैं तुम्हारा पार्ट शहर के ढिंढोरची को दे दूँगा। और देखो, अपने हाथ-रूपी कुल्हाड़े से लगातार हवा को मत चीरते रहना। अभिनेता को संयम रखना चाहिए। चाहे दिल के भीतर भावनाओं के ज्वालामुखी फूट रहे हों, फिर भी यह संयम अभ्यास से आता है और इससे अभिनय में सच्चाई पैदा होती है। तुम्हारी क़सम, मेरी आत्मा जल जाती है, जब मैं किसी भूतनाथ को स्टेज पर इधर से उधर भागते, गला फाड़ते और सच्ची भावनाओं की धज्जियाँ उड़ाते हुए देखता हूँ। ऐसे अभिनेताओं को जूतों से पीटना चाहिए, जो कि 'हैरड' का पार्ट करते समय हैरड से भी बढ़कर ‘हैरडपना’ दिखाते हैं। इस इल्लत से बाज़ आना।
अभिनेता- मैं वादा करता हूँ, हुज़ूर।
हैमलेट- और देखो, 'अंडरऐक्ट' करना भी ठीक नहीं। समझ गए न? जो बात अपने दिल और दिमाग़ को सच्ची और ठीक जँचे, वही करना। इशारे शब्दों के और शब्द इशारों के अनुकूल हों। नक़लीपन कहीं न आए। अगर कहीं नक़लीपन आ गया, तो समझो कि नाटक का उददेश्य ही ख़त्म हो गया, क्योंकि नाटक का उददेश्य सिर्फ़ एक है, और वह यह कि जीवन को नाटक के आइने में प्रतिबिंबित करना अच्छाई को, बुराई को, नफ़रत को, प्यार को उनका असली रूप दिखाना है।
अभिनेता- हमने काफ़ी सुधार कर लिया है, जनाब।
हैमलेट- काफ़ी सुधार से कुछ न होगा, पूरा सुधार कर डालो। और अपने अभिनेताओं को, विशेषतः मसख़रों को हिदायत कर दो कि जो कुछ लेखक ने उनके लिए लिखा है, सिर्फ़ वही बोलें। दर्शकों को हंसाने के लिए अपनी तरफ़ से कुछ न जोड़ें। यह बहुत बुरी आदत है। ऐसा करके यही लोग कई बार दर्शकों का ध्यान नाटक के किसी ज़रूरी अंग से हटा देते हैं। यह उनका ओछापन है, यानी अपनी नुमाइश के लिए वे नाटक का सत्यानाश करते हैं। जाओ, अब तैयार हो जाओ।’’
यथार्थवाद का सबसे बड़ा मार्गदर्शक शेक्सपियर और केवल शेक्सपियर ही है। उसके नाटकों में अनेक स्थल आते हैं, जहाँ वह ज़िंदगी से भागने वाले नाटकों की निंदा करता है। स्वाभाविक ही था कि इस शिक्षा का हमारे शिक्षित वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ता और वे महसूस करते कि अपने देश की नाट्य-परंपरा को उन्हें किसी दूसरे मार्ग पर लाना है। नाटक वास्तव में चरित्र को बनाने वाली चीज़ है, बिगाड़ने वाली चीज़ नहीं, बशर्ते कि वह यथार्थवादी हो।
बंबई आने से पहले पृथ्वीराज केवल न पुरानी परंपरा का तजुर्बा हासिल कर चुके थे, बल्कि नाटक की इस नई परिभाषा को भी दिल में बैठा चुके थे। पृथ्वीराज का परिवार उनसे एक कामयाब डॉक्टर, वकील या बड़ा अफ़सर बनने की आशा रखता था। केवल सतरह वर्ष की आयु में उनका ब्याह हो गया था और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ सिर पर आ पड़ी थी। जिस दिन अपनी क़ानूनी किताबों को अंतिम श्रद्धांजलि भेंट करके पृथ्वीराज ने अभिनेता बनने का फ़ैसला किया, घर में तूफ़ान-सा मच गया। घर का प्रत्येक व्यक्ति स्तंभित हो उठा, जब पृथ्वीराज ने बताया कि वह अपनी सामाजिक ज़िम्मेदारियों से भागने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए अभिनेता बनने जा रहे हैं, और यह कि नाटक उनकी नज़रों में बड़ी ऊँची चीज़ है। पृथ्वीराज के दृढ़ और निर्मल चरित्र पर बुज़ुर्गों को पूरा भरोसा था, और इसीलिए उन्हें आशीर्वाद दिया और फिर एक दिन वह भी आया जब पृथ्वीराज ने अपना वचन पूरा करके दिखा दिया। अभिनय का पेशा अपनाने से पहले के जीवन में पृथ्वीराज पर दो व्यक्तियों का विशेष असर पड़ा था। पहला असर उनके दादा का था। पृथ्वीराज की माता उन्हें दो-ढाई वर्ष का छोड़कर चल बसी थीं। बचपन का ज़माना दादा की छत्रछाया में बीता था। यह बुज़ुर्ग हद से ज़ियादा उदार, मिलनसार और सर्वप्रिय थे। वह न केवल अपने निकट संबंधियों का, बल्कि शहर भर का सुख-दुःख बाँटा करते थे। वह अपने धार्मिक विचारों में भी बड़े उदार थे। हिंदू धार्मिक पुस्तकों के अलावा बाइबल, क़ुरआन शरीफ़ इत्यादि का भी बाक़ायदा अध्ययन करते थे। उनके इस गुण को पृथ्वीराज ने भी पल्ले बाँधा और निभाया है। उनकी 'पृथ्वी थिएटर्स' एक संस्था भी है, और एक परिवार भी। उसकी इमारत उनकी उदार, प्यार-भरी, दुःख-सुख बाँटने वाली शख़्सियत की बुनियाद पर ही खड़ी है। सच तो यह है कि इस परिवार से बाहर के विशाल मानव समाज की माँगों को भी पृथ्वीराज ने कभी नहीं ठुकराया। अपनी इस ख़ूबी के लिए उनके दोस्त और दुश्मन दोनों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। यही मानवीय भावना पृथ्वीराज द्वारा पेश किए गए नाटकों की मूल प्रेरणा भी मालूम पड़ती है।
पृथ्वीराज को बचपन से ही नाटकों का शौक़ हुआ था, जो कि उनके दादा की उदार मनोवृत्ति का ही लक्षण है। पाँच वर्ष की अवस्था में पृथ्वीराज ने 'हरिश्चन्द्र नाटक' में 'गनपत' का पार्ट किया था। उसके बाद शहर की रामलीला खेलने वाली मंडली उन्हें लक्ष्मण का पार्ट दिया करती थी। एक बार उन्होंने लक्ष्मण-मूर्छा का दृश्य इस कामयाबी से अदा किया कि स्टेज पर लेटे ही लेटे सो गए और दर्शकों को चिंतित कर दिया।
इस ज़माने की एक घटना उल्लेखनीय है। पेशावर में 'हरिश्चंद्र' नाटक खेला जा रहा था। उस ज़माने के मशहूर अभिनेता मुहम्मद हयात, तारामती का पार्ट अदा कर रहे थे। नन्हा-सा पृथ्वीराज भी दर्शकों में मौजूद था। नाटक के अंतिम दृश्य में तारामती अपने पुत्र रोहित की लाश को हाथों में उठाए श्मशान भूमि में दाख़िल हुई तो दर्शकों में से एक आवाज़ उठी, ‘पख़्तून! (ग़ज़ल सुनाओ)।’ इस आवाज़ के उठते ही मंडल में हर तरफ़ 'पख़्तून' का शोर होने लगा। चुनाँचे तारामती ने रोहित की लाश को रख दिया और आगे बढ़कर पश्तो भाषा की एक इश्क़िया ग़ज़ल सुनाने लगी। नाटक का यह अपमान देखकर नन्हे पृथ्वीराज का मन विद्रोह से भर गया और यह घटना उसकी स्मृति में हमेशा के लिए अंकित हो गईए। पिछले साल जब शिमला में अपना अत्यंत सुंदर नाटक 'पठान' खेल रहे थे तो अकस्मात यही आवाज़ 'पख़्तून' फिर उनके कानों में पड़ी। उन्होंने फ़ौरन पर्दा गिरवा दिया और सख़्त दुःखी हुए। अंत में उन्होंने दर्शकों को समझाया कि उन्हें अपने दिमाग़ से नाटक की पुरानी परिभाषा निकालनी पड़ेगी, नाटक केवल तमाशा नहीं है।
दूसरा असर पृथ्वीराज पर प्रोफ़ेसर जयदयाल साहब का हुआ था, जो उन्हें कॉलेज में पढ़ाया करते थे। प्रोफ़ेसर जयदयाल ने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक एक आशीर्वाद भी है और श्रद्धांजलि भी। इससे बड़ी ख़ुशी एक उस्ताद के लिए क्या हो सकती है कि जो अंकुर उसने अपने शागिर्द में फूटते देखे थे और जिनकी अपने हाथों परिवरिश की थी, वे फूलें-फलें, परवान चढ़ें। पुस्तक डायरी की शक्ल में है और पृथ्वीराज के विद्यार्थी जीवन की कई यादें उसमें अंकित है। प्रोफ़ेसर साहब ने पृथ्वी थिएटर्स के नाटकों और नाट्यकला के बारे में विस्तार और गंभीरता से नहीं लिखा है। भावुकता का प्रवेश ज़रूरत से ज़ियादा है जो कि पुस्तक की कमज़ोरी है। फिर भी, यह साफ़ मालूम होता है कि पश्चिमी नाट्यकला के पहले सबक़ पृथ्वीराज को प्रोफ़ेसर साहब से मिले थे। उनकी देख-रेख में उन्होंने बहुत से अंग्रेज़ी एकांकी नाटकों में भाग लिया और शेक्सपियर का भी अध्ययन किया था।
इस विषय में एक और बात का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जहाँ यूरोपियन साहित्य के यथार्थवाद की अच्छी शिक्षा कॉलेजों में प्राप्त होती थी, वहाँ बुरी शिक्षा भी बहुत मिलती थी। हमारी शिक्षा प्रणाली विदेशी शासकों के लिए बनाई गई थी न कि जनता के फ़ायदें के लिए। शासकों का बुनियादी उद्देश्य था विद्यार्थियों को अपने देशीय साहित्य और संस्कृति से विमुख करना, उनके अंदर दास मनोवृति पैदा करना। यह शिक्षा नौजवानों को उनकी सामाजिक ज़िम्मेदारियों की तरफ़ से लापरवाह करती थी, उनके अंदर साधारण जनता के प्रति घृणा और अहंकार की विकृत भावनाएँ पैदा करती थी, उनके दिमाग़ में यह ख़याल कूट-कूटकर भर देती थी कि पैसा कमाना और कामयाब होना ही ज़िंदगी का सबसे बड़ा आदर्श है।
यह नामुमकिन था कि इन बुरे प्रभावों की छूत से पृथ्वीराज बिल्कुल ही बचे रहते। यह सोचना ग़लत होगा कि अपने देश के नाटक और फ़िल्म को यथार्थवाद की ओर ले जाने के उद्देश्य से ही पृथ्वीराज ने अभिनेता बनने का फ़ैसला किया था। मेरे ख़याल में उन्होंने यह फ़ैसला इसलिए भी किया होगा कि क़ुदरत ने उसको भरपूर शारीरिक सौंदर्य दिया था। फ़िल्मी दुनिया के फ़ैशनों को देखते हुए यह अजीब बात नहीं है, अगर पृथ्वीराज ने यह सोचा हो कि इस क्षेत्र में उनमें कामयाबी हासिल करने की बहुत बड़ी संभावना है। उनमें अहंभाव काफ़ी है, और अपने देश तथा अपनी भाषा के साहित्य का अध्ययन भी उनका आज तक अधूरा है। लेकिन उनको श्रेय इस बात का है कि समाज-विरोध के बावजूद उन्होंने अभिनय का पेशा इख़्तियार किया, जबकि इस काम की इज़्ज़त नहीं की जाती थी। वह क़ामयाब हुए और ख़ूब क़ामयाब हुए, मगर क़ामयाबी ने उन्हें कई दूसरे अभिनेताओं की तरह दंभी और स्वार्थी नहीं बनाया। उनका हिंदुस्तानी साहित्य का अध्ययन अधूरा सही, पर वह पश्चिमी साहित्य और कला के ऐसे ग़ुलाम नहीं बने, जैसे कि हमारे कई अन्य विद्वान और कलाकार बन गए हैं। कमज़ोरियाँ हर इंसान में होती है, मगर पृथ्वीराज को श्रेय इस बात का है कि अपनी कमज़ोरियों से लड़ने की ताक़त उनमें पहले भी थी, और अब भी है। अगर ऐसा न होता, तो वह उतने महान कलाकार न बन पाते, जितने कि निःसंदेह वह इस वक़्त हैं। नाट्यकला के जिस शिखर पर पृथ्वीराज जा चढ़े हैं, वहाँ तक पहुँचने की हमारे देश के कम अभिनेताओं ने हिम्मत की है।
पृथ्वीराज का फ़िल्मों में प्रवेश और शुरू-शुरू की उलझनें एक दिलचस्प दास्तान हैं। परंतु मेरा विषय नाटक है। यहाँ इतना कह देना काफ़ी है कि फ़िल्मों में कामयाबी का मुँह देखने में पृथ्वीराज को देर न लगी। परंतु साथ ही एक ऐसी घटना भी हुई कि फिर एक बार वह नाटक की धुन में बह गए। यह घटना थी बंबई में एंडर्सन नामक एक अंग्रेज़ अभिनेता द्वारा नाटक-मंडली का खुलना।
कहते हैं कि देवता स्वयं इतने बड़े नहीं होते, जितने पुजारी उन्हें बना देते हैं। इंग्लैंड में नाटक की दुनिया काफ़ी विशाल है, और उसमें एंडर्सन कोई प्रसिद्ध नाम नहीं है। मुम्किन है कि वह काफ़ी ऊँचा कलाकार हो। इस बात के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता। पर इसमें कोई शक नही कि पृथ्वीराज पर उसके व्यक्तित्व का ज़बरदस्त और चिरस्थाई असर पड़ा। 'रॉयल ऑपेरा हाउस' बंबई की एक मशहूर नाट्यशाला है। 'पृथ्वी थिएटर्स' के नाटक यहीं खेले जाते रहे हैं और 'रॉयल ऑपेरा हाउस' ही में पृथ्वीराज के गुरु एंडर्सन ने आज से लगभग बीस वर्ष पहले अपनी नाटक-मंडली बनाई थी। इसी 'रॉयल ऑपेरा हाउस' में पृथ्वीराज जहाँ दुष्यंत, कुंवर, रामकृष्ण आदि के पार्ट करते रहे हैं, वहीं एडर्सन की छाया में 'हैमलेट', 'जूलियस सीज़र', 'मर्चेंट ऑफ वेनिस', 'ट्वेल्थ नाइट' आदि शेक्सपियर के नाटकों और 'स्कूल फ़ॉर स्कैंडल', 'चित्रा', 'पोर्ट्रेट ऑफ़ अ मैन विद रेड हेयर' आदि दूसरे अंग्रेज़ी नाटकों में मुख्य पार्ट खेलते रहे हैं।
एंडर्सन की नाटक-मंडली लगभग एक साल तक क़ायम रही। पृथ्वीराज के अलावा रफ़ी पीर, मुबारक आदि और भी कई नामी कलाकार उसमें शरीक हुए थे और इन लोगों ने मंडली को ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन क़ुर्बानी दी थी। पृथ्वीराज तो अपने फ़िल्मों के काम को तिलांजलि देकर अपनी नाटकी सनक पूरी करने के लिए इसमें कूद पड़े थे। लेकिन अफ़सोस, यह सारी मेहनत निष्फल हुई। अंग्रेज़ी नाटकों में जनता की रुचि न होने के कारण इस मंडली को आर्थिक कठिनाइयों की छुरी के नीचे शहीद होना पड़ा। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि इस एक वर्ष का तजुर्बा पृथ्वीराज के लिए अमूल्य था। नाटक की सनक अब इश्क़ की सूरत इख़्तियार कर चुकी थी।
यूरोप की नाटक-मंडलियों की सबसे बड़ी ख़ूबी उनकी व्यवस्था होती है। यूरोप वालों ने मशीनें ईजाद की हैं, और कई सदियों से अपनी ज़िंदगी को भी मशीनी-डिसिप्लिन में ढाला है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों मनुष्य किस तरह से एक होकर किसी मक़सद के लिए इकट्ठे काम कर सकते हैं, यह ख़ूबी अभी तक हम में, विशेषकर हमारे मध्यम वर्ग में, बहुत कम पैदा हुई है। यह एक अंग्रेज़ की ही हिम्मत थी कि वह एक पराए देश में आकर नाटक-मंडली स्थापित कर सका और उसे लेकर देश के सभी बड़े-बड़े शहरों में घूम गया। पृथ्वीराज ने बताया है कि एंडर्सन एक महीने के अंदर दो-दो नाटकों की रिहर्सलें पूरी कर लिया करता था और उसकी शख़्सियत का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि वह अपनी टोली से हँसी-ख़ुशी रोज़ बारह-बारह चौदह-चौदह घंटे काम करवा लिया करता था।
इस बात में कोई संदेह नहीं कि इस एक वर्ष की सचेष्ट ट्रेनिंग और लगातार दर्शकों के सम्मुख आने से पृथ्वीराज नाटक के दक्ष कलाकार बन गए। एंडर्सन की कंपनी के साथ उन्होंने हिंदुस्तान भर का दौरा किया था। यही नहीं, प्रबंध का भी बहुत-सा बोझ उन्होंने अपने कंधों पर उठाया था। आज जब 'पृथ्वी थिएटर्स' साल में कई बार बंबई से बाहर चला जाता है, तो हम सोचते है कि इसी ट्रेनिंग ने पृथ्वीराज को बाहर जाकर सफल होने की शिक्षा दी होगी। हम जानते हैं कि 'पृथ्वी थिएटर्स' के दौरे कितने सफल होते हैं। आजकल के ज़माने में नब्बे के लगभग कलाकारों को लेकर, जिनमें लड़के-लड़कियाँ, बच्चे-बूढ़े, हर जाति, हर धर्म के, अच्छे-बुरे, शिक्षित तथा अशिक्षित सब शामिल हैं, नगर-नगर घूमना कोई सहज काम नहीं है। 'पृथ्वी थिएटर्स' की सफलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले साल पंजाब के एक दौरे में सारा ख़र्च निकालकर थिएटर को सवा लाख रुपये का लाभ हुआ था। केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, हर दृष्टि से दौरे सफल रहे हैं। 'पृथ्वी थिएटर्स' का हर मेम्बर इन दौरों के मीठे अनुभवों की कहानियाँ मज़े ले-लेकर सुनाता है। इन कहानियों को सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है। उनके 'पृथ्वी थिएटर्स' के जीवन की सुंदर झलकें मिलती हैं और साथ ही पृथ्वीराज के शानदार चरित्र पर प्रकाश पड़ता है। दौरों के दौरान पृथ्वीराज अपनी संस्था से बिल्कुल घुल-मिलकर रहते हैं। जो सब कलाकार खाते हैं, वही वे खाते हैं, और इनका दुःख-सुख बाँटते हैं। मेरे विचार से हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक किसी नाटक-मंडली ने इतनी ख़ूबी से दौरे नहीं किए होंगे, जितनी ख़ूबी से 'पृथ्वी थिएटर्स' करता है। दौरों ने कई शानदार कंपनियों की कमर तोड़ दी है, मगर 'पृथ्वी थिएटर्स' दौरे करने से और मज़बूत होता जाता है।
एंडर्सन की कंपनी कलकत्ता जाकर टूट गई थी और पृथ्वीराज ने मजबूर होकर फिर फ़िल्मों में काम करना शुरू किया था। सौभाग्य से उन्हें 'न्यू थिएटर्स' जैसी अच्छी फ़िल्म कंपनी में काम मिला। विश्व युद्ध छिड़ने तक वह कलकत्ता में रहे और फिर बंबई लौट आए। उन्हें लाखों की आमदनी, जिसके बारे में बहुधा चर्चा सुनी जाती है, बंबई आने के बाद ही हुई, जबकि युद्ध-काल में 'स्टारों' की भी चाँदी हो गई, और सेठों को पहली बार मजबूर होकर अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को अपनी लूट का भागीदार बनाना पड़ा, जिनको वे आज तक केवल चूसना ही जानते थे। परंतु युद्ध का अंत होते ही पृथ्वीराज ने 'पृथ्वी थिएटर्स' का आरंभ कर दिया और फ़िल्मों की ओर से ध्यान हटा लिया। अब भी वह कभी-कभी फ़िल्मों में काम करते हैं, क्योंकि थियेटर का लगभग बीस हज़ार का माहवारी ख़र्च उनके सिर पर है, और यह बोझ कभी-कभी असह्य हो जाता है।
जहाँ मैंने एंडर्सन कंपनी के प्रभाव का उल्लेख किया है, वहीं कुछ ऐसे पहलुओं का ज़िक्र भी ज़रूरी है, जो मेरी अपनी राय में लाभदायक नहीं थे। शेक्सपियर को स्टेज पर खेलने की परंपरा इंगलिस्तान में समय-समय पर बदलती रही है। पिछले बीस वर्षों में जॉन गिलगुड, लेज़ली हॉवर्ड, लॉरेन्स ओलीवियर आदि सुविख्यात अभिनेताओं के नेतृत्व में इस टेकनीक में बुनियादी तब्दीलियाँ हुई है। अभिनेता सामाजिक नाटकों में तो नाटकीय ढंग को पहले ही छोड़ चुके थे, परंतु शेक्सपियर के नाटकों को क़ुदरती ढंग से निभाना बड़ा कठिन समझा जाता था। जॉन गिलगुड ने आगे बढ़कर यह काम करके दिखा दिया। गिलगुड से पहले भी इंग्लैंड में बड़े-बड़े शेक्सपिरियन अभिनेता हो चुके हैं, परंतु जितना भाव-प्रधान अभिनय गिलगुड ने कर दिखाया, वह सचमुच एक नई चीज़ थी।
मेरी राय में एंडर्सन या तो इस नई परंपरा से वाक़िफ़ नहीं था, या उसका इससे मतभेद था। उसकी शेक्सपिरियन अभिनय-कला जॉन वैरीमोर से ज़ियादा संबंधित मालूम होती है, जिसमें कि शरीर की तरफ़ अधिक ध्यान दिया जाता था, और अभिनय की आत्मा की ओर कम। इस लिहाज़ से देखा जाए तो एंडर्सन की शिक्षा से पृथ्वीराज को नुक़सान भी काफ़ी हुआ। एक तो उनके लिए फ़िल्मों में, जहाँ कि बिल्कुल स्वाभाविक और भावना-प्रधान अभिनय की आवश्यकता होती है, अपने को संभालना कठिन हो गया, दूसरा उनका शेक्सपिरियन अध्ययन उतना गंभीर नहीं हो सका, जितना कि मेरी राय में उन-जैसे महान कलाकार के पास होना चाहिए था। एक बार एक लेखक ने पृथ्वीराज से पूछा था, ‘आप शेक्सपियर के किसी नाटक का हिंदी अनुवाद करवाकर क्यों नहीं खेलते?’, उन्होंने जवाब दिया था, ‘मुझ पर अपने इस देश की धरती और उसकी समस्याओं का बहुत गहरा असर छा गया है।’ यह बड़ा ईमानदार जवाब था। परंतु फिर भी लेखक को तृप्ति नहीं हुई। शेक्सपियर मनुष्य की आत्मा का सम्राट है, वह केवल अंग्रेज़ों का नहीं, बल्कि सारी दुनिया के इंसानों का साझा ख़ज़ाना है। सदियों से न केवल यूरोप के बल्कि दुनिया भर के साहित्य और नाटक पर शेक्सपियर की अमिट छाप है। प्रत्येक सभ्य देश की भाषा में शेक्सपियर का अनुवाद हो चुका है, और सभी देशों के कलाकार उसके नाटकों को बड़ी श्रद्धा और प्यार से खेलते हैं। और दर्शकों की भूख भी दिन-ब-दिन कम होने के बजाए बढ़ती ही जाती है। हिंदुस्तानी भाषाओं में शेक्सपियर का अच्छा अनुवाद न होना बड़ी भारी कमी है, जिसे दूर किए बिना न तो हमारे देश के नाटक और न ही फ़िल्में सच्चे यथार्थ के मार्ग पर अग्रसर हो सकती हैं। और यह काम पृथ्वीराज से बेहतर कौन कर सकता है, जबकि वह स्वयं शेक्सपिरियन नाटक का इतना अनुभव रखते हैं ! अगर उन्हें अपने इस फ़र्ज़ का पूरी तरह एहसास नहीं हुआ, तो इसका मतलब यह है कि एंडर्सन उनके अंदर शेक्सपिरियन जुनून पैदा नहीं कर सका। यह दोष गुरु के हिस्से आता है, इससे पृथ्वीराज की महानता कम नहीं होती।
ब्रिटिश-इंडिया, अकाल-पीड़ित बंगाल, आई०एन०ए० का मुक़दमा, जहाज़ियों का विद्रोह, पोस्टमैनों की कुल-हिंद हड़ताल, शिमला कांफ़्रेंस आदि अख़बारों की सुर्ख़ियों के वातावरण में 'पृथ्वी थिएटर्स' का जन्म हुआ था। पृथ्वीराज की गिनती उन कलाकारों में नहीं है, जो कला को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। जनता के आंदोलन कलाकार को प्रभावित करते हैं, और कलाकार अपने विचारों से जनता को प्रभावित करता है, इस सत्य को वह मानते हैं। उनके मिज़ाज में छुई-मुईपना नहीं है। जुलूसों-जलसों में, क्रिकेट और फुटबॉल के मैदान में भीड़ से कंधा भिड़ाना, गरजना, बरसना पृथ्वीराज को पसंद आता है। उस ज़माने के जन-आंदोलनों ने नाटक के दूसरे भी कई सोये हुए शेरों को जगा दिया था। जन-नाट्य-संघ (इप्टा) का आंदोलन देखते देखते देश भर में फैल गया था। इस बंबई शहर में नेशनल थिएटर, रंगमंच ग्रुप-थिएटर और बीसियों दूसरी नाटक-मंडलियाँ बहार की कोंपलों की तरह फूट पड़ी थीं। इनमें 'पृथ्वी थिएटर्स' ही एक ऐसी संस्था थी, जिसने स्टेज पर काम करने वालों के लिए दाना-पानी का प्रबंध भी किया।
सन पैंतालीस, छियालीस और सैंतालीस के वे दिन सचमुच पागलपन के दिन थे। बंबई में बोली जाने वाली हर भाषा के प्रमुख लेखक नाटकों पर क़लम चला रहे थे। खेलने वालों का उत्साह भी अपूर्व था। चौपाटी और कामगार मैदान के राजनीतिक जुलूसों में भी ये लोग खुली हवा को पर्दा और सीनरी बनाकर नाटक खेल आते थे। लेखकों और अभिनेताओं के जुलूस भी निकले, जिन में हज़ारों नहीं, लाखों आदमी शरीक हुए थे। कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट हर ख़याल के लोग नाटक द्वारा अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को व्यक्त करते थे, बहसें होती थीं, झगड़े भी होते थे, और वातावरण और भी स्फूर्तिदायक हो जाता था। इन हंगामों में 'पृथ्वी थिएटर्स' किसी से पीछे नहीं था। अगर आज अमर शेख़ के गीतों को सुनने के लिए शिवाजी पार्क में भीड़ लगी है, तो कल 'दीवार' की टिकटों के लिए ऑपेरा हाउस से लेकर चर्नी रोड स्टेशन तक क्यू लगा हुआ है।
संकीर्ण दृष्टि से देखने वालों की नज़रों में (जिनमें थोड़े समय के लिए यह लेखक भी शरीक था) 'पृथ्वी थिएटर्स' पेशेवर होने के कारण ऐमेच्योर मंडलियों से भिन्न था। किंतु पृथ्वीराज ने ऐसी संकीर्णता के जवाब में ख़ुद कभी संकीर्णता नहीं दिखाई। 'पृथ्वी थिएटर्स' ने हर संस्था को सहयोग दिया। उसने नाटकों के माध्यम से यह प्रमाणित करने की कोशिश की कि यह संस्था पेशेवर कंपनियों की तरह पैसा बटोरने के ख़याल से नहीं बनाई गई है। अगर इन नाटकों द्वारा कुछ कलाकारों को रोज़ी मिलती है, तो इसमें नाटक को लाभ पहुँचता है, पृथ्वीराज को नहीं।
'पृथ्वी थिएटर्स' का पहला नाटक था 'शुकंतला'। यह नाटक सामाजिक वातावरण को देखते हुए बेमौक़ा था। इसके अलावा, बाद में पेश किए गए नाटकों से भी उसका जाति-भेद था। शायद यही कारण था कि बंबई में वह ज़ियादा लोकप्रिय नहीं हुआ, हालाँकि बंबई से बाहर उसे भी काफ़ी पसंद किया गया।
यदि गंभीरता से देखा जाए तो कालिदास की यह अमर कृति किसी समय भी बेमौक़ा नहीं कही जा सकती। मुझे अगर कोई शिकायत है तो यह कि 'पृथ्वी थिएटर्स' के इस प्रोडक्शन में कालिदास की 'स्पिरिट' प्रायः ग़ायब थी। मुझे याद है कि इंग्लैंड से लौटने पर, जहाज़ से उतरते ही मैं बड़े शौक़ से शांताराम रचित 'शकुंतला' देखने गया था। मगर देखने के बाद तबीअत कई दिनों तक उचाट रही थी। दिल्ली पहुँचकर अपने एक मित्र की अलमारी में 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' पड़ी देखी थी। मेरे मित्र को संस्कृत साहित्य से बहुत प्रेम था। हम दोनों इस पुस्तक को लेकर बैठ गए थे और सारी शाम कालिदास की अद्वितीय पंक्तियों का रसास्वादन करते रहे थे। तब जाकर फ़िल्म का असर कुछ कम हुआ था। यदि मैं 'पृथ्वी थिएटर्स' से शेक्सपियर खेलने का अनुरोध कर सकता हूँ तो मुझे उसके 'शकुंतला' खेलने पर कभी आपत्ति नहीं हो सकती। मगर प्राचीन नाटकों को खेलते वक़्त निर्माता का कर्तव्य होगा है कि दर्शकों के मनोरंजन की ख़ातिर मूल नाटक की ऐतिहासिक और कलात्मक सच्चाइयों को क़ुर्बान न करे।
'कालिदास' को खेलते समय यह आवश्यक है कि उसके नाटकों का मनगढ़ंत रूपांतरण नहीं, बल्कि प्रामाणिक और सुंदर अनुवाद किया जाए। खेलने की टेकनीक ऐसी हो कि तत्कालीन ऐतिहासिक वातावरण, वेश-भूषा आदि सजीव होकर सामने आ जाएँ। ऐसा उद्योग सराहनीय और प्रगतिशील होगा। पर अफ़सोस कि यह उद्योग न शांताराम ने किया, और न पृथ्वीराज ने।
'पृथ्वी थिएटर्स' की 'शकुंतला' के लेखक ने कालिदास से सिर्फ़ प्लॉट ही लिया, और उसके आधार पर एक ऐसा नाटक लिख डाला, जो कालिदास का हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। यह कालिदास के साथ अन्याय था, उसी प्रकार का अन्याय जो हमारे देश की फ़िल्में ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों से आए दिन करती आई हैं।
हिंदी-उर्दू का संस्कृत से माँ-बेटी का रिश्ता है, इसलिए यह कहना कि कालिदास को प्रामाणिकता से खेलना असंभव है, या जनता को यह रुचिकर नहीं है, सर्वथा ग़लत है। संस्कृत नाटक पूरी प्रामाणिकता से यूरोप की भाषाओं में अनुवादित हुए और खेले भी गए हैं। यदि विदेशी जनता उन्हें पसंद कर सकती है, तो अपने देश की जनता क्यों न करेगी?
सच्चाई कला की सबसे बड़ी ख़ूबी है। मुझे विश्वास है कि अगर पृथ्वीराज ने 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' का अध्ययन मूल संस्कृत में स्वयं किया होता, तो वह इस दिशा में पुरानी रीतियों को त्याग एक नई और स्वस्थ परंपरा क़ायम करते।
'पृथ्वी थिएटर्स' का दूसरा नाटक 'दीवार' था। इस नाटक को जो शानदार सफलता प्राप्त हुई, वह बयान से बाहर है। आज तक हज़ार बार से ज़ियादा यह नाटक स्टेज पर आ चुका है, और आज भी दर्शक उसे चाव से देखते हैं। 'दीवार' और उसके बाद के तीन नाटक 'गद्दार', 'पठान' और 'आहुति' देश में पैदा हुई एक विकट परिस्थिति को सामने रखकर लिखे गए हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने आज से तीस वर्ष पहले दो कठोर सत्य जनता के आगे रखे थे। पहला कि आज़ादी लड़कर ही हासिल की जा सकती है, अर्ज़ियों, दरख़्वास्तों से नहीं। दूसरा यह कि इस लड़ाई में विजय तभी हो सकती है, जबकि देश की दो बड़ी धार्मिक जमातें—हिंदू और मुस्लिम, जिन्हें आपस में लड़ा-लड़ाकर अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्य को मज़बूत किया, संगठित हो जाएँ।
ये दोनों कठोर सत्य आज भी उतने ही सच्चे और कठोर हैं, जितने कि तीस बरस पहले थे।
गाँधीजी ने किस तरह सदियों से कुचली हुई और निःशस्त्र जनता को संसार के सबसे मज़बूत और निर्दयी साम्राज्य से टक्कर लेने के क़ाबिल बना दिया, यह बीसवीं सदी का एक अचंभा है। गाँधीजी के अहिंसा के सिद्धांत की बुनियाद में यह ऐतिहासिक तथ्य शामिल था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताक़त जनता के संगठन की ताक़त है। जनता अगर अपने अधिकारों के लिए संगठित हो जाए, तो उसे बंदूक़ें, तोपें और एटम बम भी नहीं हरा सकते। इस बात का सबूत न केवल हमें अपने राष्ट्रीय आंदोलन से मिलता है, बल्कि आज कोरिया और वियतनाम में भी हम यही देख रहे हैं कि साम्राज्यवादियों को जनता के अमन और शांति के लिए किए गए दस्तख़तों से भी डर लगता है। गाँधीजी का 'अहिंसा' का अर्थ कायरता हरगिज़ नहीं था। उन्होंने बार-बार कहा है कायरता से हिंसा कहीं अच्छी है। इसी तरह हिंदू-मुस्लिम संगठन के सिद्धांत की बुनियाद में भी एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक तथ्य है- क़ौमों और जातियों का आत्मनिर्णय। गाँधीजी ने बताया कि राष्ट्रीय धर्म का जात-पात और छुआछूत से कोई संबंध नहीं है। राष्ट्रीय भावना इन पक्षपातों से आज़ाद होकर ही पैदा हो सकती है। गाँधीजी ने चाहा कि पठान अपनी राष्ट्रीयता को समझें, पंजाबी अपनी पंजाबियत को समझें, बंगाली अपनी बंगालियत की क़द्र करें, और सब मिलकर अपने महान राष्ट्र हिंदुस्तान का सिर ऊँचा करें—एक-दूसरे से बराबरी और इंसाफ़ का रिश्ता पैदा करके।
गाँधीजी की इस शिक्षा से हिंदुस्तान के करोड़ों आदमी प्रेरित हुए। 'पृथ्वी थिएटर्स' के उपर्युक्त नाटकों में भी इन्हीं सिद्धांतों की प्रेरणा है। 'दीवार' के अंत में दोनों भाई एक होकर नक़ली बँटवारे के भ्रम से जागकर साम्राज्य को ललकारते हैं और उसे अपने घर से निकालकर बाहर करते हैं। 'पठान' में दिखाया जाता है कि पठान चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, वह पठान है, जिस तरह कश्मीरी कश्मीरी है और पंजाबी पंजाबी है। पर अफ़सोस कि गाँधीजी राजनीतिक नेता से अधिक संत-महात्मा थे और पंजाबी पृथ्वीराज राजनीतिक बुद्धिवादी कम और कलाकार ज़ियादा थे। यदि गाँधीजी ठीक समय पर देख लेते कि किस प्रकार देश और विदेश की प्रतिक्रियावादी ताक़तें समझौते की आड़ में उनके सिद्धांतों का ख़ून कर रही हैं, और न केवल उनको बल्कि सारे देश में स्वतंत्रता आंदोलन को मौत की तरफ़ घसीट रही हैं, तो शायद हमारे इतिहास के वर्तमान पन्नों को दूसरे शब्दों में लिखा जाता। पर वक़्त हाथ से निकल गया। जो हाथ आज़ादी के लिए उठे थे, वे अपनी माँ-बहन की छातियाँ काटने में जुट गए। स्वार्थी लीडरों ने अहिंसा को कायरता में तब्दील करवा दिया। कायरता की ऐसी मिसालें दुनिया में कहाँ मिलेंगी, जो आज़ादी के स्वागत में इस देश में प्रकट हुईं?
'दीवार' पेश करते समय कलाकार पृथ्वीराज से भी एक भारी भूल हो गई। उन्होंने परिस्थिति का गंभीरता से विश्लेषण नहीं किया। उन्होंने यह नहीं पूछा कि वह हिंदू-मुस्लिम जनता, जो कल एक होकर 'शहीद-दिन' मना रही थी और जहाज़ी विद्रोह के अवसर पर कंधे से कंधा मिलाए ख़ून बहा रही थी, आज एकाएक उसे क्या हो गया कि वह एक-दूसरे पर टूट पड़ी? क्या यह सारा दोष जनता ही का है या जनता के लीडरों का भी?
पृथ्वीराज कलाकार थे, वह भावों की लहरों में बह जाने की ग़लती भी कर बैठे। उन्होंने यह न देखा कि इस समय कांग्रेस और लीगी दोनों ही लीडर अंग्रेज़ के हाथ का खिलौना बने हुए हैं। नतीजा यह हुआ कि कांग्रेस के असर में आई हुई हिंदू जनता ने 'दीवार' को बेहद पसंद किया और लीग की भड़काई हुई मुस्लिम जनता ने उसे सख़्त नापसंद किया। एक ईमानदार कलाकार की हैसियत से पृथ्वीराज को उस समय सबसे बड़ा आघात इसी बात का हुआ। उनका मक़सद मुस्लिम जनता को आकर्षित करना था, नाराज़ करना नहीं। और सच तो यह है कि आज 'दीवार' को हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक नई दृष्टि से देखते हैं और सच्चे कलाकार की भविष्यवाणी को आदर के साथ सुनते हैं। पर 'अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।'
ऐसा ही अंतर्विरोध हमें 'पठान' में भी मिलता है। पठानों की राष्ट्रीयता के प्रश्नों को भी पृथ्वीराज ने ठोस प्रामाणिकता से पेश करने के बजाय भावुक ढंग से पेश किया है, इसलिए दर्शकों की प्यास नहीं बुझती। उदाहरण के लिए नाटक के दौरान पठान हीरो जगह-जगह पर पंजाबी मुसलमानों की निंदा करता है। दर्शक हैरान होता है कि पृथ्वीराज जैसा बेदार आदमी, जिसका आदर्श ही धार्मिक संकुचितता का खंडन करना है, कैसे पंजाबी क़ौम के एक भाग को धर्म की कसौटी पर एक पात्र के मुँह से बुरा कहलवा सकता है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि इस तरह की भावुक भूलें केवल 'पृथ्वी थिएटर्स' में ही नहीं हुई। ठीक इसी तरह की भूलें लोकनाट्य-संघ के कलाकारों से भी हुई। जिस तरह पृथ्वीराज ने एक विशेष राजनीतिक पक्ष की नीति को शिरोधार्य कर लिया, उसी तरह लोक-नाट्य संघ ने एक दूसरे राजनीतिक पक्ष के नारों पर नाटक का निर्माण करना शुरू किया। दोनों संस्थाएँ स्वयं इस बात का विवेचन करने में असफल रहीं कि कौन-सी नीति किस हद तक सही है, और किस हद तक ग़लत।
आज देश की सामाजिक अथवा राजनीतिक हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। वे पहले के तूफ़ान ख़त्म हो चुके हैं। हर तरफ़ निराशा और किंकर्तव्यविमूढ़ता नज़र आती है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की तमाम बुनियादी कमज़ोरियाँ सामने आ रही हैं। इस निराशा और किंकर्तव्यविमूढ़ता का असर कला-संसार पर भी पड़ा है। बंबई का रंगमंच आजकल प्रायः फ़िल्म-स्टारों की नुमाइश के लिए ही इस्तेमाल होता है।
'पृथ्वी थिएटर्स' के हर नाटक की अलग-अलग समालोचना करना, गुण-अवगुण का विश्लेषण करना न तो इस लेख में संभव है, और न इसकी कोई आवश्यकता है। इन नाटकों को आज तक जनता लाखों की संख्या में देख चुकी है और मुक्त कंठ से प्रशंसा कर चुकी है। न केवल विचारशील और आदर्शवादी होने के कारण, बल्कि टेकनीक की दृष्टि से भी यथार्थवादी और अत्यंत सुंदर होने के कारण ये नाटक लोकप्रिय हुए हैं। पृथ्वीराज ने निर्माता-निर्देशक की हैसियत से अपनी प्रचुर ट्रेनिंग का, जिसका ज़िक्र मैं पहले विस्तार से कर चुका हूँ, पूरा लाभ उठाया है और बार-बार पर्दा गिराकर तीस-तीस, चालीस-चालीस दृश्य दिखाने की परंपरा ख़त्म कर दी है। अभिनय का स्तर भी पूरी तरह यथार्थवादी है। इस दिशा में 'पृथ्वी थिएटर्स' की इससे बड़ी तारीफ़ और क्या हो सकती है कि उसने इस थोड़े से समय में राज कपूर, ज़ोहरा, अज़रा, प्रेमनाथ, सज्जन जैसे कलाकार पैदा किए हैं। इन नाटकों में लाइटिंग, संगीत आदि को बड़े सहज भाव और संजीदगी से इस्तेमाल किया गया है। स्वयं पृथ्वीराज के अभिनय की प्रशंसा करना सूरज को चिराग़ दिखाना है। फिर भी लेखक के अपने अनुभव की एक-दो बातें उल्लेखनीय हैं।
पाठक जानते हैं कि 'आहुति' नाटक के पहले अंक का घटना-स्थल रावलपिंडी है। रावलपिंडी मेरा अपना शहर है और वहाँ के लोगों की बातचीत के ख़ास अंदाज़ और इशारों से मैं बख़ूबी परिचित हूँ। उनमें से एक अंदाज़ यह है कि कोई बोलने वाला अगर कोई पते की कह दे, तो श्रोता के मुँह से 'आय-हाय' ज़रूर निकलेगी और यह 'आय-हाय' अंधे रामकृष्ण का पार्ट करते वक़्त पृथ्वीराज के मुँह से बराबर निकलती है। जिस दिन 'ऑपेरा हाउस' में मैंने पहली बार यह नाटक देखा, मेरे साथ वाली सीट पर रावलपिंडी के एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे। मैंने देखा कि जिस क्षण पृथ्वीराज के मुँह से 'आय-हाय' निकलती, ठीक उसी क्षण उस बुज़ुर्ग के मुँह से भी निकलती और वह झूम-झूम जाता और ठंडी साँसें भरता। ऐसा मालूम होता था कि किसी बिजली के तार से इन दोनों व्यक्तियों का संबंध जोड़ दिया गया है। बताइए भला अभिनय की इससे ऊँची मर्यादा भी कोई हो सकती है?
एक दिन जब मैं पृथ्वीराज से मिलने गया तो मालूम हुआ कि आज थिएटर का सारा सामान—पर्दे, पोशाकें, सीनरी वग़ैरा किसी बैंक के पास गिरवी रखा गया है, ताकि उसके बदले में कुछ क़र्ज़ लेकर काम चलाया जा सके। मैं ऊपर कह चुका हूँ कि ऐसे मौक़े अक्सर आते थे, क्योंकि 'पृथ्वी थिएटर्स' का माहवार ख़र्च बीस हज़ार के लगभग है। बंबई में हर माह इतनी आमदनी होना दुश्वार है, क्योंकि आवश्यकतानुसार थिएटर न मिलने के कारण 'पृथ्वी थिएटर्स' को शाम के बजाए सुबह शो करने पड़ते हैं, और वह भी हफ़्ते में केवल तीन या चार।
सुनकर मुझे दुःख हुआ और मेरी हैरानी की भी हद न रही जब मैंने देखा कि पृथ्वीराज के चेहरे पर कोई मलाल नहीं, बल्कि हमेशा से ज़ियादा ख़ुश नज़र आ रहे थे।
घंटों इधर-उधर की बातें होती रहीं, जिनका थिएटर से कोई संबंध न था। विदा होते वक़्त मैं पूछ ही बैठा कि आख़िर इस ख़ुशी का कारण क्या है? उस वक़्त हम दोनों 'ऑपेरा हाउस' की अंधेर घुप्प सीढ़ियों पर खड़े थे। पृथ्वीराज ने कहा, बलराज, आज जब मैं स्टेज पर पार्ट कर रहा था तो मैंने देखा मेरी शलवार का इज़ार-बंद लटक रहा है। उसे ठीक करने के लिए मैं हाथ बढ़ाने ही वाला था कि मुझे ख़याल आया कि मैं तो अंधे आदमी का पार्ट कर रहा हूँ। उसे कैसे मालूम हो सकता है कि उसका इज़ार-बंद लोगों को दिखाई दे रहा है? सो, मैं रुक गया। बस सुबह से यह घटना बार-बार याद आती है और मैं हँस पड़ता हूँ। है न फ़िज़ूल-सी बात?
पृथ्वीराज का उदाहरण सामने रखते हुए महसूस होता है कि कलाकार के लिए तीन गुण बड़े ज़रूरी हैं-
1. व्यक्तिगत ईमानदारी और सच्चाई।
2. अपने हुनर में निपुण बनने की तीव्र इच्छा और अथक परिश्रम करने की हिम्मत।
3. सामाजिक जीवन का अनुभव, सामाजिक आंदोलनों तथा घटनाओं को वैज्ञानिक तरीक़े से समझना और अपना राष्ट्रीय दृष्टिकोण भी वैज्ञानिक बनाना।
जिस कलाकार में ये तीनों गुण मौजूद हों, वह सच्चा कलाकार है। वही जनता का सच्चा मनोरंजन भी कर सकता है, और मार्गदर्शन भी।
अगर इन तीनों में से एक गुण भी ग़ायब हो जाए तो कलाकार और उसकी कला दोनों घटिया दर्जे के हो जाते हैं।
नाटक खेलना एक सामूहिक काम है, सिर्फ़ एक कलाकार का नहीं, बहुत से कलाकारों का संयुक्त काम है। गोया ये तीन गुण न केवल कलाकार के लिए अनिवार्य हैं, बल्कि हर नाटक-संस्था के लिए भी ज़रूरी हैं। लेकिन अफ़सोस कि नाटक-संबंधी बहसों में इन तीनों में से एक न एक को अक्सर दृष्टि से परे कर दिया जाता है। कई विद्वान टेकनीक से एकदम लापरवाही करना चाहते हैं। उनका कहना है कि विचार अच्छे हों, इरादे ठीक हों तो नाटक ज़रूर कामयाब होगा। यह बात उतनी ही ग़लत है जितना यह कहना कि सुई, तागा, कपड़ा, कैंची हाथ में हो तो पतलून अपने आप बन जाएगी। वे यह नहीं समझते कि नाटक का हुनर सदियों पुराना और बेहद सूक्ष्म है। इसको सीखने के लिए न केवल अपने देश का, बल्कि अपने देश की परंपराओं का सक्रिय अध्ययन करना पड़ता है, चाहे उन देशों का समाज सामंतवादी हो, पूँजीवादी हो या समाजवादी हो। अगर हमारे सर्वश्रेष्ठ, प्रगतिशील लेखक भी उतने कामयाब नाटक नहीं लिख पाते, जितने कि यूरोप के घटिया-से-घटिया लेखक लिख डालते हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा तक बेच डाली है, तो इसका कारण यही है कि उन्होंने इस हुनर को सीखने में पर्याप्त परिश्रम नहीं किया है।
दूसरी ओर कई विद्वान हर वक़्त टेकनीक ही की रट लगाए रखते हैं। वे भूल जाते हैं कि टेकनीक आर्ट का साधनमात्र है, उसका उद्देश्य नहीं। नाटक का उद्देश्य है जनता का मार्गदर्शन। ऐसे समय में जबकि हमारे देश में भूख, ग़रीबी और शोषण का हाहाकार मचा हुआ है, किसी भी कलाकार को टेकनीक के रेशमी खोल में बंद हो जाने का अधिकार नहीं है। ऐसा करके वह अपनी कला का अपमान करता है।
इसी तरह ऐसे विद्वान भी मिलेंगे, जो कलाकार के व्यक्तिगत जीवन को उसकी कला से अलग रखना चाहते हैं। वे भूल जाते हैं कि युगों से हमारे देश के महान कलाकारों ने व्यक्तिगत जीवन के उच्चतम स्तर क़ायम किए हैं और दूसरी बात है कि नाटक जैसे सामूहिक काम में हर आदमी को कड़े अनुशासन में रहना पड़ता है। अगर किसी संस्था में उच्छृंखल, स्वार्थी और अपने आपको महत्ता देने वाले लोगों को खुली छुट्टी दे दी जाए तो वह संस्था कभी भी सफल नहीं हो सकती। ईमानदारी और संयम का अनुशासन बड़े-से-बड़े और छोटे-से-छोटे कलाकार के लिए आवश्यक है।
यदि मैं पृथ्वीराज को सच्चा कलाकार मानता हूँ तो इसलिए कि उनमें ये तीनों गुण मौजूद हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पृथ्वीराज को सर्वांगपूर्ण कलाकार मानता हूँ। गुण-अवगुण सब में होते हैं और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि पृथ्वीराज को भी इन तीनों दिशाओं में और भी कड़ी तपस्या की ज़रूरत है। मुझे विश्वास है कि यह तपस्या वह करेंगे। इसलिए मैं यह कहने का साहस करता हूँ कि जिस देश में पृथ्वीराज जैसे कलाकार मौजूद हों, उस देश में नाट्यकला का भविष्य उज्ज्वल है।
- पुस्तक : बलराज साहनी- संतोष साहनी समग्र
- संपादक : बलदेवराज गुप्त
- रचनाकार : बलराज साहनी
- प्रकाशन : हिंदी प्रचारक संस्थान
- संस्करण : 1994
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.