उदय प्रकाश : समय, स्मृति और यथार्थ के अद्वितीय रचनाकार
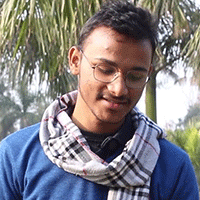 उज्ज्वल शुक्ल
25 जुलाई 2025
उज्ज्वल शुक्ल
25 जुलाई 2025

“कोई भी रचनाकार-कथाकार समय, इतिहास स्मृति के स्तर पर, ख़ासकर टाइम एंड मेमोरी के स्तर पर लिखता है। …मेरा मानना है कि किसी भी रचनाकार को अपनी संवेदना लगातार बचा कर रखनी चाहिए। अपने आस-पास के परिवर्तन के प्रति ग्रहणशीलता लगातार बनी रहनी चाहिए। जिस मोमेंट आप उसे खो देते हैं, आपकी संवेदनशीलता ख़त्म हो जाती है। फिर आपके पास सिर्फ़ नॉस्टेल्जिया या स्मृतियाँ बचती हैं।” (उदय प्रकाश अपने एक साक्षात्कार में)
जब वर्तमान में सामूहिक स्मृतियों का ध्वंस और उसके नवनिर्माण की प्रक्रिया निरंतर चल रही हो और दूसरा यह कि स्मृतियाँ एक विष बुझे तीर के तर्ज़ पर निरंतर निर्माणाधीन हों तो ऐसे वक़्त में मनुष्य अपनी आस्था की आश्वस्ति के लिए अपनी संस्कृति, अपने मिथक, इतिहास एवं साहित्य के पास बार-बार जाता है। वह निरंतर थकान का शिकार हो सकता है। वह किसी रूढ़िवादी ‘तिरिछ’ का काटा, प्यासा मारा भी जा सकता है अथवा वह गड्ड-मड्ड व्यवस्था में ‘मोहनदास’ की भाँति अपने अस्तित्व पर बार-बार सवाल कर सकता है। इन सबके बाद भी वह ‘पाछू मत देख... मत देख पाछू, अगाड़ी देख...! पाछू कुच्छ नहीं...’ बार-बार सुनना चाहता है। वह अपनी आस्था बनाए रखना चाहता है।
उदय प्रकाश का साहित्य इस अगाड़ी देखने की प्रक्रिया में रचा और बुना गया साहित्य है। वह पाछू देखते भी हैं तो वहाँ से उतना ही सामान लेते हैं, जितने की आवश्यकता होती है। उनकी लंबी कहानी ‘मोहन दास’ में इसकी बानगी देखने को मिलती है। इस कहानी का मुख्य किरदार मोहन दास अपने नाम और संबंधों में हर जगह गांधी से मिलता है, फिर भी वह निरंतर सरकारी फ़ाइलों से ग़ायब होता रहता है अथवा बुरे रूप में प्रस्तुत किया जाने लगता है। आने वाले समय की पदचाप को इससे बेहतर क्या सुना जा सकता है, जिसे उदय प्रकाश ने अपनी इस कहानी में दर्ज किया है। जिस समय में एक ऐसे व्यक्ति (गांधी) की ज़रूरत हो, जहाँ वह विकास की तमाम अंधी दौड़ को धता बताते हुए, मानवीय मूल्यों और उसके विकास की संधारणीय धारणा का पक्षधर हों, उस समय में वह मोहनदास की स्थिति का शिकार हो जाते हैं।
उदय प्रकाश का कथाकार इस एक कहानी में जिस तरह अपने समकालीन मुद्दों को दर्ज करता है; युगीन परिस्थितियों को प्रकाश में ले आता है, वह कथा-साहित्य की दुनिया में दुर्लभ है। उन्होंने अपने कथ्य और भाषा में जो समकालीनता बरती है, वह इस समय के गद्य में एक निकष की तरह है।
अपनी कहानी ‘टेपचू’ के अंत में वह घोषित करते हैं कि सामान्य मनुष्य यूँ ही नहीं मरने वाला। वह हर संघर्ष में घास हो जाता है और बार-बार व्यवस्था में शामिल होने की अर्ज़ी देता है। इस संदर्भ में उदय प्रकाश की ही कविता ‘अर्ज़ी’ की कुछ पंक्तियाँ यहाँ ध्यातव्य है :
मैं तो यों ही आपके शहर से गुज़रता
उन्नीसवीं सदी के उपन्यास का कोई पात्र हूँ
मेरी आँखें देखती हैं जिस तरह के दृश्य, बेफ़िक्र रहें
वे इस यथार्थ में नामुमकिन हैं
इस तरह उदय प्रकाश की कई कविताएँ, कहानियों की पूरक लगती हैं। सामान्य जन की आँखों में जो दृश्य हैं, वे उनकी कविताओं का हिस्सा बनते हैं और उनका यथार्थ उनकी कहानियों में आता है। वह स्वप्न की शैली में लिखते हुए भी स्वप्न नहीं लिखते। किसी यथार्थ को उसके होने की हर प्रायिकता में तलाशते हैं। ‘टेपचू’, ‘जज साहब’, ‘राम सजीवन’ या ‘हीरालाल’ कोई भी हो, ये इसी व्यवस्था के जीव हैं जो अपनी दिनचर्या और व्यवस्था के मारे हैं; और संघर्ष की प्रक्रिया में उनका जीवन—क्या होता है और क्या हो सकता है के बीच—उनकी कहानियाँ झूलती हैं। इन परिस्थितियों में जो कहानियाँ बुनी गई हैं, उनमें यह स्पष्ट होता है कि व्यवस्था की मार हर बार अलग ढंग से पड़ सकती है। सत्ता का चरित्र कभी शासन-प्रशासन वाला तो कभी सामंती होगा। यहाँ तक कि वह विश्वविद्यालय में ‘पीली छतरी वाली लड़की’ की कथा की तरह भी हो सकता है।
अपनी कविता ‘तानाशाह की खोज’ में वह कहते हैं :
अब तो वह आएगा तो उसे पहचानना भी मुश्किल होगा
हो सकता है, वह कहता हुआ आए कि मैं इस
शताब्दी का सबसे ज़्यादा छला गया व्यक्ति हूँ
उदय प्रकाश अपने कथा-साहित्य में सिर्फ़ शिल्प और भाषा के स्तर पर ही नहीं बल्कि कथ्य के स्तर पर भी अपनी पूर्वपीठिका से नयापन तलाश कर रख देते हैं। यह नयापन लाने की लालसा उनके सामने पात्रों के बचपन के द्वार खोलती है। अपनी कई कहानियों में वह अपने पात्रों के बचपन की कोई घटना ज़रूर बताते हैं, जिससे यह बात रेखांकित हो जाती है कि यह पात्र किस प्रकार से विकसित होगा। सात-आठ वर्ष का ‘टेपचू’ अपने प्रति हो सकने वाले व्यवहार से परिचित है :
काका, मुखिया से मत खोलना यह बात; नहीं तो मार-मार कर भुरता बना देगा हमें।
यही वो ‘टेपचू’ है जो मार खाने और मरने का डर भूल जाता है, जो कई किलोमीटर घिसटने के बाद, छिली पीठ लिए पुलिसवालों से चाय माँगता है। इसकी निर्मिति उसके बालमन से ही होती दीखती है। उनकी कहानी ‘नेलकटर’ और ‘अरेबा-परेबा’ भी महत्त्वपूर्ण हैं। दोनों कहानियाँ सहज ही पाठकों को बचपने की ओर जाने को उकसाती हैं।
बचपन का कोरा एकाधिकार और युवावस्था की परिणति में अनुभवजनीन सत्य ‘नींव की ईंट हो तुम दीदी’ में दिखलाई पड़ता है :
ढिबरी थीं दीदी तुम
हमारे बचपन के
अचार का तलछट तेल
अपनी कपास की बाती में सोखकर
जलती रहीं
हमने सीखे थे पहले-पहल अक्षर
और अनुभवों से भरे क़िस्से
तुम्हारी उजली साँस के स्पर्श में
उदय प्रकाश की कहानियों में जीवन का एक महत्त्वपूर्ण स्वरूप दाम्पत्य, पूर्णतः उपस्थित रहा है। ‘हीरालाल का भूत’ और ‘मोहन दास’ कहानियों में पत्नियाँ बाढ़ के दुर्दिनों में मजबूत खंभे-सा साथ निभाती रहीं। कहानी ‘दिल्ली के दीवार’ में भी पत्नी अपने पति से कोई सवाल करती नहीं दिखती है, जबकि वह पति के विवाहेतर संबंध के विषय में जानती है। इन सभी स्त्रियों पर पड़ती दोहरी मार को भी वह चित्रित करते हैं, लेकिन भारतीयता में बसे संघर्ष के स्वरूप को वह छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसीलिए वे स्त्रियाँ हँसिया उठाकर मारने भी दौड़ सकती हैं और जीवन के उत्स के प्रति उल्लसित, नदी में स्वच्छंद प्रेम भी करती हैं।
उनकी कविताओं में आई हुई स्त्रियाँ; अपने छीले हुए यथार्थ के साथ उनके यहाँ आई जान पड़ती हैं, न कि हेतु रूप से लाई हुई।
एक और औरत बालकनी में आधी रात खड़ी हुई इंतज़ार करती है
अपनी जैसी ही असुरक्षित और बेबस किसी दूसरी औरत के घर से लौटने वाले
अपने शराबी पति का
संदेह, असुरक्षा और डर से घिरी एक औरत अपने पिटने से पहले
बहुत महीन आवाज़ में पूछती है पति से—
कहाँ ख़र्च हो गए आपके पर्स में से तनख़्वाह के आधे से
ज़्यादा रुपये?
[औरतें]
उदय प्रकाश जिस इतिहासबोध के साथ अपनी कहानियों में जाते हैं, उन्हें बचाए रखने की माँग वह कविताओं में भी करते हैं। जहाँ इतिहास के बड़े तस्वीरों को दिन-प्रतिदिन नष्ट किया जा रहा हो और ‘ऑर्वेलियन मॉडल’ में ‘वर्तमान अतीत को नियंत्रित कर रहा हो’ ऐसे में इतिहास, कला और स्मृतियों से मिटने की साज़िश कवि-कथाकार के रूप में वह अपनी कविता ‘तीली’ में खड़े होते हैं।
एक तीली
अब तक पढ़ी न जा सकी, लुप्त सभ्यताओं की
अज्ञात लिपियों को राख
किसी मिथक-नायक के शौर्य और शोक को राख
किसी समाज के स्मृतिकोष, किसी समुदाय के प्राक्-बिंबों को राख
किसी समुदाय की अस्मिता
किसी ग़रीब का घर
किसी स्त्री की जवान देह को राख
उनका कथा साहित्य भी इसी जद्दोजहद में लगा हुआ दिखता है। हालाँकि उदय प्रकाश अपनी कथाओं में जिस रूप में प्रयोगशील रहे हैं, वह उनकी कविताओं में नहीं मिलता। उनकी कविताओं में संवेदना किसी बाँध से छोड़ी और रोकी जाती नदी-सी प्रवाहित होती है, जबकि उनकी कहानियों में वह यथार्थ के घाटों को भी काटती है और अपना मार्ग प्रशस्त करती है। भाषा की मजबूत पकड़, परंपरा का ज्ञान, शिल्प पर अधिकार और राजनीतिक चेतना उनकी कविताओं में दिखती है। उनकी कविता ‘मरना’ इस समय में बहुउद्धृत कविताओं में से एक है, जो लगभग एक नारे का स्वरूप इख़्तियार कर चुकी है। ‘अबूतर-कबूतर’ और ‘अम्बर में अबाबील’ संग्रह की उनकी कविताएँ उनकी काव्य-प्रतिभा की परिचायक हैं। उनकी कविताओं में से उनका कहानीकार, उनका इतिहासचेता इंसान बार-बार झाँकता रहता है। वह भारतीय मिथकों में भी लौट-लौटकर आते हैं, वह लोकगीतों से बात आगे बढ़ाते हैं। ‘मोहन दास’ कहानी में मैना का अंडा देना, मरना, फिर अंडा देना प्रतीकात्मक रूप से चलता रहता है।
वह अपनी कहानियों में ‘कहते हैं’ की शैली अक्सर अपनाते हुए दिखते हैं। ऐसे में यथार्थवाद का आग्रह छूट जाता है और वह कथाकार को वह बात करने की स्वतंत्रता देता है, जिस उद्देश्य से वह कहानी लिख रहा है। इन कहानियों में सच्चाई का प्रतिशत मापना—उद्देश्य से भटकना होगा। वह इन कहानियों में ‘कहते है’ या ‘ऐसा सुना जाता है’ अथवा ‘लोग बताते हैं’ की मुद्रा धारण करते हुए अपनी बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। अपनी कहानियों में वह प्रायः महत्त्वपूर्ण को रेखांकित नहीं करते हैं, बल्कि उसे सामान्य माने जाने के आग्रह में बात को आगे बढ़ाते हैं। उनकी शैली में जादुई यथार्थवाद की संभावना भी तलाशी जाती है, जबकि वह मार्केस की शैली से अधिक बोर्हेस के पास ठहरते हैं। उनकी छोटी-सी कहानी ‘डिबिया’ में काजल की डिबिया में क़ैद प्रकाश को लेकर एक बालमन के विचार उसी के क़रीब ले जाते हैं। ‘तिरिछ’ कहानी पर भी कहीं-कहीं वह प्रभाव दिखाई देता है। परंतु ध्यातव्य यह है कि उदय प्रकाश आयातित शैली की भाँति उसका प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि अपने कथ्य से उस शैली की आवश्यकता को पुष्ट करते हैं। ‘हीरालाल का भूत’ कहानी को हम विदेशी जादुई यथार्थवाद कैसे कह सकते हैं, जबकि ऐसी कहानियाँ लोक में बहुत पहले से व्याप्त हैं। वह समय की चक्रीय गति को अपनी कहानियों में बार-बार दिखाते हैं; इतिहास बार-बार लौटता है, नए रूप और किरदार लेकर लेकिन शोषण की कहानियाँ एक-सी होती हैं। वह इसीलिए अपने इतिहास, मिथक और लोक के पास से कहानियाँ बुनते हैं, जो नितांत भारतीय हों। कहानी ‘जज साहब’ में मार्केस की कहानी का वह राष्ट्रपति ज़रूर याद आ जाता है, यद्यपि दोनों बहुत भिन्न कहानियाँ हैं।
हालाँकि यह अतिशयोक्ति न माना जाए तो कहना ही होगा कि उदय प्रकाश वर्तमान समय के बड़े कहानीकारों में से एक हैं। उन्होंने अपनी कहानियों में मध्यवर्गीय और निम्नवर्गीय जीवन की त्रासदियों का चित्रण जिस प्रकार से किया है, वह उनकी कथा को श्रेष्ठता प्रदान करती है। उनके यहाँ त्रासदी है, लेकिन सिर्फ़ बयानबाजी नहीं। उनके यहाँ संवाद हैं, लेकिन अधिक नाटकीय नहीं। उन्हें विवरण में जाते हुए पता रहता है कि कहाँ निकल जाना है। वह ख़बरें भी कहानियों में डालते हैं, लेकिन अख़बार की शैली नहीं इख़्तियार करते। इस प्रकार वह जर्नलिस्ट की तरह कहानियाँ नहीं कहते। अपनी कविताओं में वह कुछ स्थानों पर अपनी संवेदना से पाठक की संवेदना को रेजोनेट करते हैं। उनमें कहीं वैचारिकी का चमत्कार है। राजनीतिक व्यंग्य उनकी कविताओं में जितना आता उतना ही परिवार और प्रकृति भी। इसी के साथ अंत में जो उनकी न्याय के प्रति नैसर्गिक आस्था है, वह व्यवस्था पर भरोसा न करने के बावजूद अडिग दिखती है और संघर्षरत रहती है—“न्याय की आकांक्षा कालातीत है।”
साथियो, यह एक लुटेरा अपराधी समय है
जो जितना लुटेरा है, वह उतना ही चमक रहा है और गूँज रहा है
हमारे पास सिर्फ़ अपनी आत्मा की आँच है और थोड़ा-सा नागरिक अंधकार
कुछ शब्द हैं जो अभी तक जीवन का विश्वास दिलाते हैं...
हम इन्हीं शब्दों से फिर शुरू करेंगे अपनी नई यात्रा...
[चंकी पांडे मुकर गया है]
~~~
समादृत कवि-कथाकार उदय प्रकाश इस बार के ‘हिन्दवी उत्सव’ में कविता-पाठ के लिए आमंत्रित हैं। ‘हिन्दवी उत्सव’ से जुड़ी जानकारियों के लिए यहाँ देखिए : हिन्दवी उत्सव-2025
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
