शिक्षक-शिक्षा-शिक्षण
 हिन्दवी डेस्क
04 सितम्बर 2024
हिन्दवी डेस्क
04 सितम्बर 2024
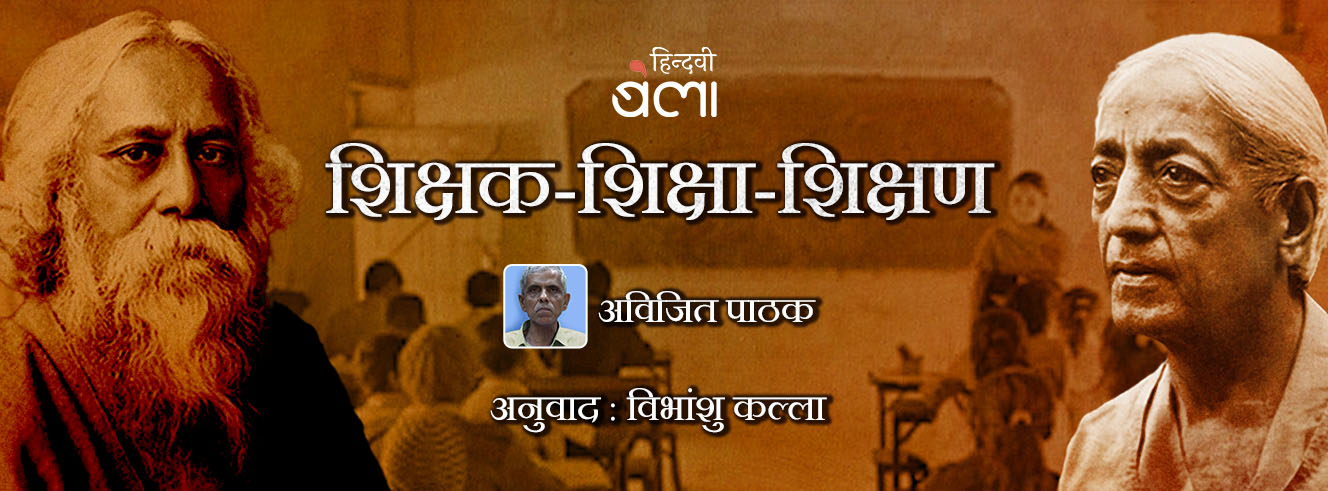
क्या क्रूर सत्ता, उग्र राष्ट्रवाद और बाज़ार प्रेरित तार्किकता से ग्रस्त समाज के लिए शिक्षण के पेशे में निहित गहरी दृष्टि और रचनात्मकता की सराहना और उसका परिपोषण करना संभव है? क्या वह समाज, जो अपनी शिक्षा को महज़ भौतिक सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष तरह के ‘सूचनाओं के कैप्सूल’ की तरह देखने का आदि हो चुका है, इस बात को स्वीकार करेगा कि शिक्षक का कार्य शिक्षा को एक ‘उत्पाद’ की तरह बेचने का नहीं है?
जब हमारे बच्चों और उनके चिंता ग्रस्त अभिभावकों के मानसिक परिदृश्य पर कोचिंग संस्थानों के ‘गुरुओं’ का क़ब्ज़ा हो चुका है और पूरे देश में कैंसर की तरह उग आई लोकलुभानी शिक्षा की दुकानें एक भौंडे बाज़ार-उपयोगी शैक्षणिक चिंतन को बढ़ावा देने में लगी हैं, ऐसे समय में क्या शिक्षकों को रोगहारी (रोग हरने वाला) संवाद करने वाले एक सतत यात्री तरह देखा जा सकता है?
भले ही शिक्षक दिवस जैसे विशेष मौक़ों पर हम शिक्षण के पेशे के बारे बहुत अच्छी और पवित्र बातें करते हैं, और सरकार द्वारा कुछ शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाता है, लेकिन सत्य यह है कि एक समाज के तौर पर हमने शिक्षकों को एक बंधनों से मुक्ति दिलाने वाले शैक्षिक दूत की तरह गंभीरता से नहीं देखा है।
शुरुआत भर के लिए एक बार हम ‘अव्यावहारिक’ होने का जोखिम उठाते हैं और कल्पना करते हैं कि शिक्षण का पेशा कैसा होना चाहिए। हम पाएँगे कि हमारे अंतर्मन में प्रचलित रूप से एक आदर्श शिक्षक की भूमिका एक ‘ज्ञानी’ और विशेषज्ञ व्यक्ति की है। लेकिन शिक्षक महज़ एक विषय विशेषज्ञ नहीं है। वह सिर्फ़ क्वांटम फ़िज़िक्स या मध्यकालीन इतिहास नहीं पढ़ाता, वह उससे कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य भी करता है।
एक शिक्षक अपने छात्रों के साथ एक सहयात्री की तरह चलता है, वह उनकी अंतरआत्मा को छूता है और एक उत्प्रेरक की तरह अपने युवा छात्रों को अपनी विशिष्टताओं और अंतर्निहित संभावनाओं को समझने में सहयोग प्रदान करता है।
वह एक मशीन की तरह नहीं है, जो औपचारिक पाठ्यक्रम का पठन और दोहराव करवाए, न ही वो निगरानी रखने वाला व्यक्ति है जो—अनुशासन बनाए, सज़ा दे, परीक्षा और परिणाम की रस्मों के सहारे अपने छात्रों को श्रेणीबद्ध और सामान्यीकृत करे।
बजाय इसके उसे एक रचनात्मक व्यक्ति की तरह कार्य करना चाहिए, जो अपनी महीन जोड़ने की कला से विद्यार्थी का उसकी विशिष्टता पर भरोसा क़ायम करे और याद दिलाए कि उसे किसी भी दूसरे की तरह होने की आवश्यकता नहीं। और उसे अपने आंतरिक प्रस्फुटन की प्रक्रिया पर ध्यान देने को कहे और मानव रचित सफलता और असफलता के द्वन्द्व को समाप्त करे।
एक और महत्त्वपूर्ण बात जिस पर शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। उसे इस बात को महसूस करना चाहिए कि शिक्षण और उपदेश देने की अपनी सीमाएँ है, और उससे यह अपेक्षा नहीं कि जाती कि वह विद्यार्थी के दिमाग़ को भारी किताबी ज्ञान से भरे। बजाय इसके, उसका प्राथमिक काम विद्यार्थी की अवलोकन की शक्ति, सोचने और विचारने की क्षमता, सौंदर्यता की समझ और इन सबसे पहले अनंत विस्तार की झलकियों को अनुभव करने की आध्यात्मिक प्रेरणा को तीक्ष्ण करने में मदद करे।
दूसरे शब्दों में, एक बार जब ये शक्तियाँ विकसित हो जाएँ तो कोई भी औपचारिक डिग्रियों और डिप्लोमाओं से परे आजीवन के लिए विद्यार्थी हो सकता है। ज़ाहिर तौर पर, शिक्षक एक समन्वय की क्रिया के रूप में और विद्यार्जन शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक विकास की योजना के रूप में बंधन-मुक्त, आज़ाद तालीम की नींव तैयार कर सकती है। आज़ाद तालीम केवल मात्र ‘कौशल विकास’ का कार्य नहीं है, न ही वो सिर्फ़ बौद्धिक और अकादमिक विशेषज्ञता से संबंधित है।
मूलतः आज़ाद तालीम सार्थक, रचनात्मक और सुखद जीवन जीने की चाह है। यह विभिन्न प्रकार की दूसरों पर हावी होने वाली और बहकाने वाली विचारधारओं को पहचान कर ख़त्म करने की योग्यता उत्पन्न करने वाली होनी चाहिए।
आज जब लोकतंत्र के विचार को कुछ आत्ममुग्ध लोगों ने ‘चुनावी प्रक्रिया’ द्वारा अपने मालिक चुनने तक सीमित कर दिया है, सैन्य राष्ट्रवाद के विचार ने लोगों की मानसिकता में डर और नफ़रत को भर दिया है और नवउदारवाद ने ‘स्मार्ट’ होने का मतलब एक ऐसे अतिप्रतियोगी—जो कैशलेस पेमेंट करके तुरंत संतुष्टि प्राप्त करने वाले—उपभोगवादी के रूप स्थापित कर दिया है। तब एक शिक्षक की ज़िम्मेदारी है कि वह बंधन-मुक्त शिक्षा के ज़रिए छात्रों को लिंगभेद, नस्लवाद, जातिवाद, प्रकृति का नाश करने वाले विकास, खोखले उपभोगवाद और मौत की हद तक ले जाने वाली ‘उत्पादकता’ के विचार जिसने मनुष्य को एक रचनात्मक जीव के बजाय ‘संसाधन’ माना है को सवाल करना सिखाए।
लेकिन विडंबना यह है कि अभी तक हमारे मन में आज़ाद तालीम को बढ़ावा देने वाले और शिक्षण के सच्चे अर्थ को पोषित करने वाले पर्यावरण की चाह नहीं पैदा हो सकी है। भारत के किसी भी औसत विद्यालय की तरफ़ ध्यान देने पर आप पाओगे कि यह रट्टामार पढ़ाई, बहुत ही ख़राब शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, दयनीय इन्फ़्रास्टक्चर, अव्यवस्थित कक्षाएँ और थके हुए शिक्षकों का घर बन चुकी है।
ऐसे में बौद्धिक उत्तेजना और न्यायप्रियता स्थापित करने वाली शिक्षा की थोड़ी-सी भी संभावना नहीं है। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम एक समाज के तौर पर एक अच्छे शिक्षक के मूल्य को नहीं पहचान पाए है।
साथ ही परिवारवाद, भ्रष्टाचार और बीएड डिग्री को छोटा आँकने के कारण शिक्षण के पेशे में भारी गिरावट आई है। वैसे ही हमारे कुंठित शासक वर्ग ने देश के कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों को भयंकर क्षति पहुँचाने का कार्य किया है। इसके अलावा हमारे प्रचलित टेक्निकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई करवाने वाले संस्थान प्राथमिक तौर पर अपनी भूमिका टेक्नो-कॉरपोरेट को प्रशिक्षित मज़दूर देने तक ही समझते हैं।
इन सब कारणों से शिक्षक केवल एक ‘सेवा प्रदाता’ और सत्ता की हाँ-में-हाँ मिलाने वाले पेशे की तरह सीमित हो गया है। हमारा पूरा समाज नौकरशाही द्वारा मिलने वाली शक्ति, टेक्नो-मैनेजर की नौकरी और चकाचौंध वाले सेलेब्रिटीज़ पर सम्मोहित है। तब हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि समाज के तौर पर हमने अपने शिक्षकों मृत प्रायः करके छोड़ दिया है।
फिर भी, उन लोगों को उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए जो अब भी शिक्षण के पेशे से प्यार करते हैं और इसमें अत्यधिक संभावना देखते हैं। आख़िर में हम वह समाज हैं जिसने गिजुभाई बोधका, रवींद्रनाथ टैगोर और जिद्दु कृष्णमूर्ति जैसे शिक्षकों को देखा है। जो हमें अनवरत यह विश्वास करने की प्रेरणा देते हैं कि एक शिक्षक नौकरशाही की मशीन के पुर्ज़े से कहीं अधिक है। जो अपने छात्रों के साथ सत्य का प्रकाश लिए साधक और सहयात्री की तरह चलता है और जिस संसार में हम रह रहे हैं उसकी समझ पैदा करता है, और अपने विद्यार्थियों को निम्नताओं से आज़ाद करता है। आज हमें इस प्रकार के आशा भरे शिक्षाशास्त्र का उत्सव मनाना चाहिए और इसमें अत्यधिक संभावना देखते हैं।
आख़िर में हम वह समाज हैं जिसने गिजुभाई बोधका, रवींद्रनाथ टैगोर और जिद्दु कृष्णमुर्ति जैसे शिक्षकों को देखा है। जो हमें अनवर यह विश्वास करने की प्रेरणा देते हैं कि एक शिक्षक नौकरशाही की मशीन के पुर्ज़े से कहीं अधिक है। जो अपने छात्रों के साथ सत्य का प्रकाश लिए साधक और सहयात्री की तरह चलता है और जिस संसार में हम रह रहे हैं उसकी समझ पैदा करता है और अपने विद्यार्थियों को निम्नताओं से आज़ाद करता है। आज हमें इस प्रकार के आशा भरे शिक्षाशास्त्र का उत्सव मनाना चाहिए।
~~~
मूल आलेख यहाँ पढ़िए : The Idea of a Teacher
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
