ओ रोमियो : क्राइम-रोमांस का थका हुआ प्रयोग
 तापस
21 फरवरी 2026
तापस
21 फरवरी 2026
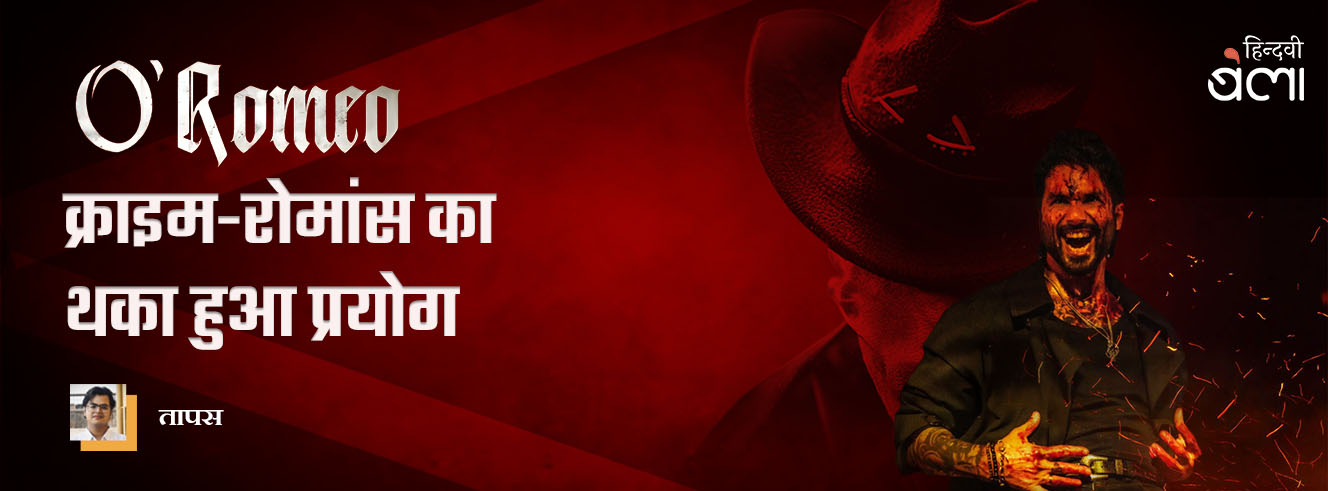
O Romeo, Romeo! wherefore art thou Romeo?—ओ रोमियो, रोमियो! तुम रोमियो क्यों हो?
शुरुआत के पाँच मिनट उलझन में नहीं बीते। बहुत सीधा-सादा कथानक आदित्य धर या सिद्धार्थ आनंद सरीखे डायरेक्टरों की फ़िल्मों का फ़र्स्ट हॉफ़ याद आता रहा। लेकिन अचानक उलझन का कहानी में प्रवेश होता है—फ़रीदा जलाल। वह प्रोटोगोनिस्ट को आदेश वाले लहजे में कुछ कहती हैं। यह बताना फ़िल्म की कहानी सुना देने जैसा होगा और यह सब बहुत-से लोग किया करते हैं।
कल से आज में भीषण संक्रमण हो गया है। खाँसने और हँसने पर सीने में भयानक दर्द हो रहा है। बुख़ार भी भीतर कहीं बना हुआ है। तिस पर विशाल भारद्वाज को देखने की ज़िद—‘ओ रोमियो’ कहीं ‘रोमियो जूलियट’ का रूपांतरण तो नहीं। नहीं रूपांतरण नहीं। वैसे यह सब इतनी आसनी से कहना मुश्किल है। विशाल भारद्वाज के यहाँ बहुत फ़्लो है और उस फ़्लो में बहुत-सी ख़ामियाँ भी अनुस्यूत हैं।
सिनेमाघर शानदार था इसलिए शरीर तकलीफ़ में भी फ़िल्म में बना हुआ था। बल्कि फ़िल्म देखने से बदन और टूटने लगा। इंटरमिशन के दस मिनट पहले से ही पेशाब के बहाने पर ख़ुद को दिलासा देते हुए कि सारी वजह तबीयत ही है और अब भाग जाना चाहिए। मन फ़ोन पर बात कर लेने या फ़ोन चला लेने की ओर हचकचा के फिसलता रहा।
जबकि ऐसा कुछ था और कुछ नहीं था। विशाल भारद्वाज अपनी विधा से या तो चिढ़ गए हैं या अब उनसे फ़िल्म बन नहीं पा रही है। दोनों वजह हो भी सकती है और नहीं भी।
उस्तरा यह फ़िल्म में प्रोटोगोनिस्ट का नाम है जो पेशे से कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जिस एक्शन की दरकार फ़िल्म में शुरूआती पाँच मिनट में आई थी, वो मेरे देखने तक बनी रही। (एक्शन में हॉलीवुड के एक्शन पैरामीटर के समकक्ष या उससे कुछ कम फ़िल्म में मारपीट और मर्डर की तारतम्यता थी। भूल-भटक और उस्तरा के मारने का तरीक़ा कुछ-कुछ ‘अमेरिकन साइको’ के पैट्रिक बैटमेन जैसा था। पर वो मुझ जैसों को आसानी से नहीं भाता। इंट्रोवर्ट क़िस्म की यह फ़िल्म बिल्कुल भी डेरोगेट्री नहीं। रक्तचाप नहीं बढ़ता। हॉल से बार-बार बाहर जाने और भीतर आने का मन करने लगा।
प्रमुख सहयोगी कलाकार की भूमिका नाना पाटेकर कर रहे हैं और वह कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। वही ‘अब तक छप्पन’, ‘शागिर्द’ और ‘क्रांतिवीर’ वाले नाना की आत्मा ही भटक रही थी, पूरी फ़िल्म में लेकिन यह कहते हुए मुझे बेहद अफ़सोस भी हो रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड का काम भी न हो पाया फ़िल्म में नाना से। विधु विनोद की फ़िल्म ‘परिंदा’ में नाना ख़लनायक हैं, स्टाइलशिट तो उनकी वैसी ही है मगर त्वचा के सारे छिद्रों में हवा घुसती रहती है। उस फ़िल्म और हत्या के दृश्यों में उन्हें देख रोमांच होता था। यह सब कल हुआ और नहीं भी हुआ।
यह जो होने और अनहोने के बीच फाँसी का फंदा है, वहाँ जाकर मेरा मन लटक जा रहा था। तृप्ति डिमरी ने पूरी फ़िल्म में शबाना और स्मिता की छाया रहने दी है। शाहिद कपूर ने अपनी एनर्जी से यह साबित किया है कि उनके यहाँ बहुत-से रंग हैं—अभी ही देवा आई थी। दरअस्ल दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज का म्यूज़िकल एप्रोच भी ढीला पड़ गया। गाने और डांस बेवजह जैसे बॉलीवुड फ़िल्मों में आ जाया करते हैं, कई बार आते रहे।
यह सब नहीं होना था। कुल मिलाकर डिज़ास्टर से भी नीचे कहीं।
वेश्यावृत्ति दिखाना सिनेमा में आसान नहीं। दिशा पाटनी अच्छी नहीं लग रही थी। कोई और वाईबरेंट अभिनेत्री होती—मिसाल के लिए आलिया भट्ट। वैलेंटाइन डे में बिगाड़ नहीं पैदा कर पाए विशाल भारद्वाज। 8:40 के शो में जगह थी PVR: Promenade, Vasant Kunj हॉल नंबर 7। हॉल में कुल लोग 14 जो जाते रहे, मुझ समेत बचे 7। मैं भी इंटरमिशन के बाद असुविधाजनक परिस्थिति में था। क्या करें, क्या न करें, ये कैसी मुश्किल हाय!
अफ़्शाँ के लिए ज़रिया है उस्तरा मर्डरर अफ़्शाँ ही है बुनियादी रूप से। प्यार है जो ये सब होने-हवाने दे रहा है। हमारी तो मुहब्बत भी महँगी है तूने तो रंजिश ख़रीद ली बहन... जलाल और उसकी विक्षिप्त पत्नी का दृश्य थोड़ा जमा। पर हिचकी आती रही और जाती रही। यानी तमन्ना भाटिया से और अभिनय करवा सकते थे। विक्षिप्तता सस्टेन कर सकती थी। राहुल देशपांडे ने कमाल किया है। उनके गायक होने और उनकी गायकी का पूरा-पूरा इस्तेमाल हुआ है। पर राहुल देशपांडे का एप्रोच इरिटेट करता रहा। गायकी भी चुभती रही। दरअस्ल यहाँ पर विशाल भारद्वाज ने छंद पकड़ लिया था कि शास्त्रीय संगीत कितना उबाऊ और इरिटेट करने लगता है, जब वह ज़रूरत से ज़्यादा हो जाय। इंस्पेक्टर पठारे का उनकी गायकी को लेकर जो रुख़ रहा पूरी फ़िल्म में उसका दूसरे चरित्रों द्वारा मज़ाक़ बनता रहा। उसके मर जाने से बड़ी तसल्ली मिलती है। IMDB पर बड़ी लंबी कास्ट दी हुई है। उतने लोग सिनेमा में है नहीं। फ़िल्म के आख़िरी हिस्से में जलाल और उस्तरा का फ़ाइट सीक्वेंस भी रोचक है। लेकिन मेरे लिए फ़िल्म लोकल ट्रेन में ही ख़त्म हो गई थी। ख़ान और उस्तरा को गोली लगने के बाद फ़िल्म है नहीं, उसके बाद जो कुछ है—वह बहुत-सी फ़िल्मों में होता रहा है। पिता व्योमेश शुक्ल को जब यह सब कारिस्तानी सुनाई तो वह कहने लगे—अधिकांश लोकप्रिय भारतीय सिनेमा ऐसी ही है।
मैंने एकबार देखी है कम-से-कम तीन बार और देखनी ही है। विशाल भारद्वाज, इरफ़ान की जगह नहीं भर पाए। उनके दरवाज़े की चाभी ग़ुम गई है, जिसे वह खोज भी रहे हैं।
कुछ हुआ तो है लेकिन क्या...?
यह उलझना ज़्यादा समझना कम है। इन भीषण क्रूरताओं में फ़िल्म भी और क्रुएल हो उठती है। क्राइम, ड्रामा और रोमांस बहुत आसान विधा हो गई। अब आईफ़ोन के नए सबसे हाई एंड वर्ज़न के फ़ोन से ऐसी विधा की बहुत-सी घटिया फ़िल्में बनाई जा सकती हैं।
इस रोमियो का दिल सोचकर कुछ और गया था, हो कुछ और गया।
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
