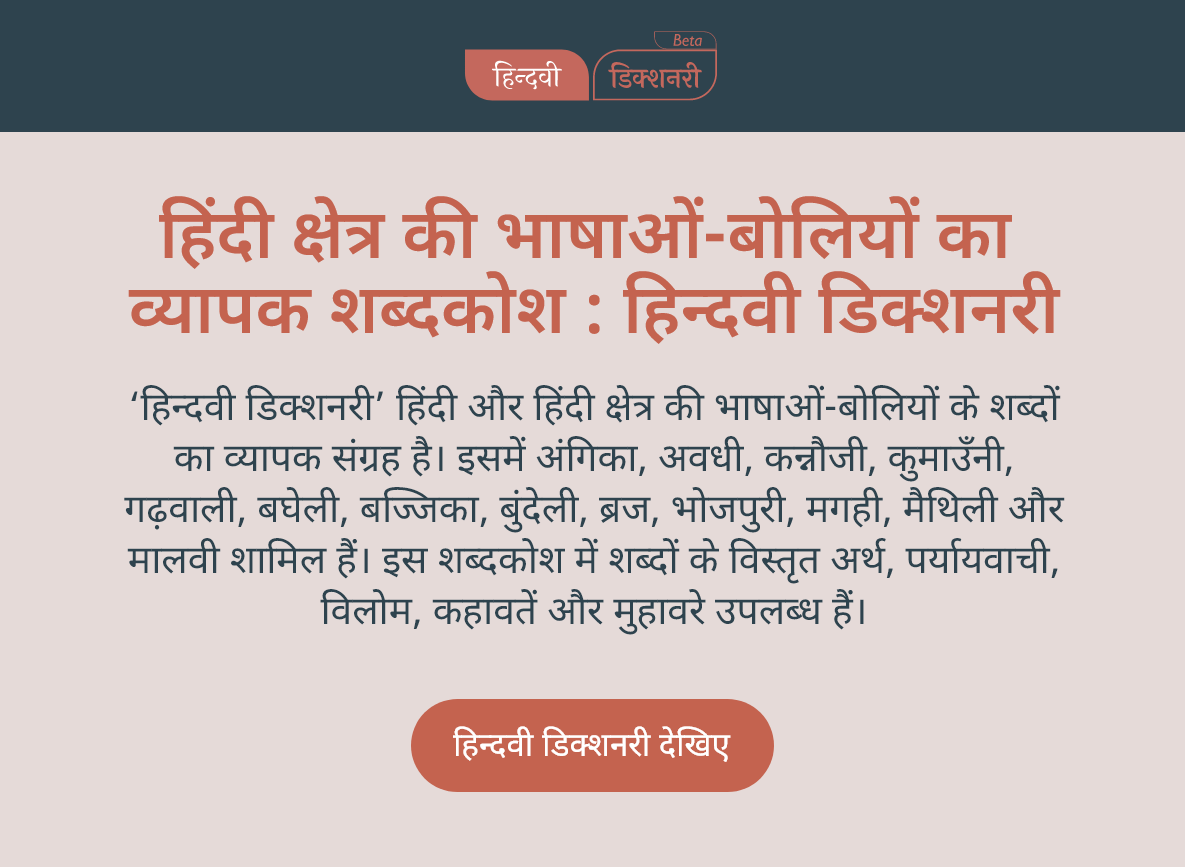प्रयोगवादी रचनाएँ
prayogavadi rachnayen
पिछले कुछ समय से हिंदी काव्य-क्षेत्र में कुछ ऐसी रचनाएँ हो रही हैं, जिन्हें किसी सुलभ शब्द के अभाव में, प्रयोगवादी रचना कहा जा सकता है। इन रचनाओं को यह नाम स्वयं इनके रचयिताओं ने दिया है, अतएव इनके लिए किसी दूसरे नाम की खोज करना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। इन रचनाओं पर, इनके प्रयोगवादी नाम और गुणों पर, इनके रचयिताओं को बहुत काफ़ी गर्व है, और वे समय-समय पर अपने इन प्रयोगों के पक्ष में अनेक तर्क और दलीलें देते रहते हैं। जहाँ तक नाम का संबंध है, ‘प्रयोगवाद’ नाम पर वे जितना चाहें गर्व कर सकते हैं (कोई भी किसी नाम पर गर्व कर सकता है)। इस संबंध में हमें उनसे कुछ नहीं कहना। किंतु प्रयोगवादी काव्य के स्वरूप पर, कविता में प्रयोगों की स्थिति, आवश्यकता और उपयोगिता पर हम प्रयोगवादियों के तर्कों को अवश्य समझना चाहेंगे। साथ ही प्रयोगवादी रचनाओं के कुछ नमूने लेकर हम यह भी देखना चाहेंगे कि उन रचनाओं में और उनके लिए दी गई दलीलों में किस सीमा तक समता या समकक्षता है। और अंत में हम हिंदी कविता पर पड़ने वाले प्रयोगवादियों और उनकी रचनाओं के प्रभाव और परिणाम की भी जाँच करेंगे, जिससे प्रयोगवादी काव्य-सृष्टि और उससे होने वाली लाभ-हानि का पूरी तरह आकलन हो सके।
यहाँ आरंभ में यह कह देना भी आवश्यक है कि हिंदी काव्य-परंपरा में प्रयोगवादी शैली कभी भी अधिक सम्मान सूचक नहीं रही। प्रयोग शब्द से प्रायः नए अभ्यास, नवीन प्रयास या नई निर्माण चेष्टा का अर्थ लिया जाता है। प्रयोगवादी साहित्यिक से साधारणतः उस व्यक्ति का बोध होता है जिसकी रचना में कोई तात्त्विक अनुभूति, कोई स्वाभाविक क्रमविकास या कोई सुनिश्चित व्यक्तित्व न हो। वास्तविक सृजन और कांतदर्शिता के बदले सामान्य मनोरंजन और शैली प्रसाधन ही उसकी विशेषता होती है। अधिकार और उत्तरदायित्व की अपेक्षा अनिश्चय और उद्देश्यहीनता की भावना ही वह उत्पन्न करता है। स्रष्टा और संदेश वाहक न होकर वह प्रणेता और प्रवक्ता-मात्र होता है।
सच्चे साहित्यकार और प्रयोगी साहित्यिक के इस अंतर को आज के प्रयोगवादी या तो जानते ही नहीं, या जानकर भी उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं! तभी तो अपने प्रयोगों के पक्ष में वे जायज़-नाजायज़ हर तरह के विज्ञापन करते रहते हैं। यह भी नहीं कि इन प्रयोगों को वे अपने आगामी काव्य-विकास का साधन मात्र मानते हों—ऐसी सीढ़ी जिस पर चढ़कर वे कहीं आगे जाएँगे। वे तो इन प्रयोगों में ही पूरी तरह रम गए हैं और उन्हें ही काव्य का चरम लक्ष्य मानने लगे हैं। उनकी इस रुचि और प्रवृत्ति का परिचय 'तारसप्तक' नामक संग्रह पुस्तक में दिए गए वक्तव्यों से प्राप्त होता है। 'तारसप्तक' नए प्रयोगवादियों की प्रतिनिधि कृति कही जा सकती है, जिसमें उनकी रचनाएँ और उनके वक्तव्य सुविधा के लिए 'तारसप्तक' पुस्तक को ही प्रयोगवादी रचनाओं के विवेचन का मुख्य आधार मान कर चलेंगे।
एक
'तारसप्तक' के संग्रहकर्ता श्री 'अज्ञेय' पुस्तक की 'विवृत्ति' में लिखते हैं :—'उनके तो एकत्र होने का कारण ही यही है कि वे किसी एक स्कूल के नहीं हैं, किसी मंज़िल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, अभी राही है—राही नहीं, राहों के अन्वेषी।' वे आगे लिखते हैं, 'काव्य के प्रति एक अन्वेषी का दृष्टिकोण उन्हें समानता के सूत्र में बाँधता है।' 'दावा केवल इतना है कि वे सातों अन्वेषी हैं।' कहीं यह भ्रम न हो जाए कि ऊपर की पंक्तियों में किसी स्कूल के कुछ राह भूले हुए विद्यार्थियों का ज़िक्र किया गया है, यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यहाँ अज्ञेय जी राह भूले हुए विद्यार्थियों की नहीं, विशुद्ध प्रयोगवादी कवियों की चर्चा कर रहे हैं!
ये प्रयोगवादी कवि किसी मंज़िल पर पहुँचे हुए नहीं हैं, राही या राह पर चलने वाले भी नहीं, ये हैं केवल राहों के अन्वेषी! अब तक हमने 'पहुँचे हुए' कवियों का नाम सुना था, 'लीक छोड़ कर चलने वाले शायरों और सपूतों' की चर्चा सुनी थी पर अब अज्ञेय जी से ऐसे कवियों का हाल भी सुनने को मिला जो न तो पहुँचे हुए हैं (अर्थात् जो राह पार कर चुके हैं) और न राही हैं (अर्थात् जो राह बेराह किसी ओर चलो ही नहीं) परंतु जो एकाग्र होकर राहों का अन्वेषण करते हैं। (अर्थात् जो चलने के अर्थ में बिल्कुल ठप हैं)। फिर अन्वेषण के लिए इनके पास अन्वेषी की दृष्टि भी नहीं, केवल 'दृष्टिकोण' है। कदाचित् कहीं न चलने के कारण ही ये 'प्रगतिशील' कहे जाते हैं, और दृष्टि के बदले 'दृष्टिकोण' रखने के कारण ही अन्वेषी या प्रयोगवादी कहलाते हैं!
इस नई कवि-श्रेणी का स्वरूप-परिचय कराने के लिए हम अज्ञेय जी के कृतज्ञ हैं, पर हम और अधिक आभारी हैं अज्ञेय जी की आगे की व्याख्याओं और विवरणों के लिए। प्रयोगवादी कवियों की प्रकृति प्रवृत्ति का परिचय देते हुए वे लिखते हैं:—'उनमें मतैक्य नहीं है, सभी महत्वपूर्ण विषयों में उनकी राय अलग-अलग है—जीवन के विषय में, समाज और धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य-वस्तु और शैली के, छंद और तुक के, कवि के दायित्वों के—प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। यहाँ तक कि हमारे जगत के ऐसे सर्वमान्य और स्वयंसिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे स्वीकार नहीं करते, जैसे लोकतंत्र की आवश्यकता, उद्योगों का सामाजीकरण, यांत्रिक युद्ध की उपयोगिता, वनस्पति घी की बुराई अथवा काननबाला और सहगल के गानों की उत्कृष्टता, इत्यादि। वे सब एक दूसरे की रुचियों-कृतियों और आशाओं-विश्वासों पर एक दूसरे की जीवन-परिपाटी पर और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हँसते हैं।'
अपने युग की दुनिया से नितांत भिन्न और स्वतंत्र दृष्टि रखने वाले विक्टर ह्यूगो या बर्नार्ड शा जैसे व्यक्ति कभी-कभी विश्व के साहित्यिक रंगमंच पर आते हैं, उनके आने पर संसार में विचारों की नई परंपरा स्थापित होती है। ऐसे व्यक्ति अपनी अदम्य प्रतिभा के बल पर युग को नए चिंतन का मार्ग सुझाते हैं, फिर भी युग चेतना ऐसे व्यक्तियों का पूरी तरह अनुगमन नहीं कर पाती, और वे व्यक्ति अपनी लंबी छाया ही विचारों की रंगभूमि पर छोड़ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रायः विचारक ही होते हैं, कवि नहीं होते, जैसे शा या गांधी या मार्क्स। कवियों की दुनिया में इतनी बड़ी इतनी निस्संग और कदाचित् इतनी निष्ठुर व्यक्तिवादिता पनप नहीं सकती। कवि की भावना और कल्पना उसे मनुष्यों की सामान्य अनुभूति के अधिक समीप बना रहने देती है। युग-चेतना के नियामक और प्रतिनिधि कवि जनसमाज के लिए इतने दुरूह नहीं होते, जितने वे विचारक हुआ करते हैं। महान विचारकों और महान कवियों में यह नैसर्गिक अंतर आरंभ से ही चला आ रहा है।
पर कल्पना कीजिए आपके सामने सात ऐसे महामानव लाकर खड़े कर दिए जाते हैं जो एक से एक बढ़कर कृतविद्य विचारक भी हैं और बड़े लासानी कवि भी। विचारक वे ऐसे हैं कि 'सभी महत्वपूर्ण विषयों में उनकी राय अलग अलग है।' 'हमारे जगत के सर्वमान्य और स्वयंसिद्ध मौलिक सत्यों को भी वे स्वीकार नहीं करते।' और कवि इतने स्वाधीन हैं कि 'काव्य-वस्तु और शैली, छंद और तुक, कवि के दायित्व—प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है'। कवि और विचारक दोनों का संगम हो जाने पर वे सातों एक दूसरे की रुचियों, कृतियों, आशाओं, विश्वासों...और यहाँ तक कि एक दूसरे के मित्रों और कुत्तों पर भी हँसते हैं! ऐसी स्थिति में आप उन्हें क्या कहेंगे (कवि बड़ा, या विचारक बड़ा, या दोनों) यह तो आप जानें, पर अज्ञेय जी उन्हीं को 'प्रयोगवादी कवि' कहते हैं!
ऊपर यह ज़िक्र किया जा चुका है कि प्रयोगवादी कवि अन्वेषी होता है, या अन्वेषी होने के कारण ही वह प्रयोगवादी होता है; परंतु अब तक यह नहीं बताया जा सका कि वह अन्वेषी किस वस्तु का होता है? अज्ञेय जी की 'विवृत्ति' में इस विषय की विवृति नहीं मिलती, पर आगे चलकर (तारसप्तक पृष्ठ 74-75 में) जब वे काव्य-संबंधी अपने व्यक्तिगत अनुभव लिखते हैं, तब इस विषय पर पूरा प्रकाश डालते हैं। उनके हिसाब से 'प्रयोग (या अन्वेषण) सभी कालों के कवियों ने किया है।...किंतु कवि क्रमशः अनुभव करता आया है कि जिन क्षेत्रों में प्रयोग हुए हैं, उनसे आगे बढ़ कर अब उन क्षेत्रों का अन्वेषण करना चाहिए जिन्हें अभी नहीं छुआ गया या जिनको अभेद्य मान लिया गया है।'
इससे इतना तो स्पष्ट हुआ कि कवि नित्य नए 'अन्वेषण' किया करता है और इस सिलसिले में प्रायः अछूते और अभेद्य क्षेत्रों में भी पहुँच जाता है, पर यह बात फिर भी जानी न जा सकी कि आजकल वह किस अभेद्य क्षेत्र में काम कर रहा है! इस प्रश्न पर अज्ञेय जी किसी प्रकार की शंका के लिए स्थान नहीं रखते—आजकल भाषा के क्षेत्र में विशेष रूप से 'अन्वेषण' का काम हो रहा है। वे लिखते हैं, 'भाषा को अपर्याप्त पाकर विराम संकेतों से, अंकों और सीधी-तिरछी लकीरों से, छोटे-बड़े टाइप से सीधे या उलटे अक्षरों से, लोगों और स्थानों के नामों से, अधूरे वाक्यों से सभी प्रकार के इतर साधनों से कवि उद्योग करन लगा कि अपनी उलझी हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अक्षुण्ण पहुँचा सके।'
यहाँ थोड़ी सी उलझन हमें भी पैदा होती है। एक ओर तो अज्ञेय जी कहते हैं कि सभी कालों के कवियों ने प्रयोग या अन्वेषण किए हैं, अन्वेषण करता हुआ आज-कल और वह स्वभावतः नए और अभेद्य क्षेत्रों में कल 'सीधी-तिरछी लकीरों' और 'सीधे या उलटे अक्षरों' के क्षेत्र में आ गया है! पर दूसरी ओर वे यह भी संकेत करते हैं कि 'अपनी उलझी हुई संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अक्षुण्ण पहुँचाने की नीयत से वह ये प्रयोग करता है। उलझन यह है कि दोनों में कौन सी वस्तु उन प्रयोगों की प्रेरक है—अभेद्य क्षेत्रों में जाने की स्वाभाविक आकांक्षा या उलझी हुई संवेदना को पाठकों तक पहुँचाने की उद्विग्नता? यह भी समझ में नहीं आया कि 'उलझी हुई' संवेदना क्या वस्तु है? क्या कवियों की संवेदना उलझी हुई भी होती है?
पर यह उलझन केवल हमारे लिए है, अज्ञेय जी के लिए नहीं। प्रयोग करने या अन्वेषी होने की प्रेरणा स्वभावसिद्ध है या उलझी संवेदना को सुलझाने के फलस्वरूप है—इस प्रश्न का महत्व अज्ञेय जी के लिए तब तक नहीं है जब तक प्रयोग या अन्वेषण का काम चलता रहे। प्रयोग किस उद्देश्य से किए जा रहे हैं, इस संबंध में आसान उत्तर यही है कि लक्ष्य तो प्रयोग ही है। उसके प्रयोजन की खोज व्यर्थ है।
किंतु उलझी या सुलभी संवेदना के प्रश्न को अज्ञेय जी आसानी से टाल नहीं सके हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि आज के कवि की संवेदना उलझी हुई है। इस उलझी संवेदना के दो कारण हैं—आंतरिक-संघर्ष और बाह्य संघर्ष। आंतरिक संघर्ष के फलस्वरूप 'आज के मानव का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा हुआ है, और वे कल्पनाएँ सब दमित और कुंठित हैं। उसकी सौंदर्य-चेतना भी इससे आक्रांत है। उसके उपमान सब यौन प्रतीकार्थ रखते हैं।...'और इस आंतरिक संघर्ष के ऊपर जैसे काठी कस कर एक बाह्य-संघर्ष भी बैठा है, जो व्यक्ति और व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति समूह का, वर्गों और श्रेणियों का संघर्ष है। व्यक्तिगत चेतना के ऊपर एक वर्गगत चेतना भी लदी हुई है और उचितानुचित की भावनाओं का अनुशासन करती है, जिससे एक दूसरे कार की वर्जनाओं का पुंज खड़ा होता है।'
कदाचित् इस उलझी हुई संवेदना के परिणामस्वरूप ही कवि 'स्वांतः सुखाय' नहीं लिखता वह अनुभूति की उस भूमि पर पहुँच नहीं पाता जो वास्तविक कविता की भूमि है और जिस पर पहुँच कर ही स्वांतः सुखाय लिखा जा सकता है। अज्ञेय जी लिखते हैं कि वे स्वांतः सुखाय नहीं लिखते। उनकी दृष्टि में कोई भी कवि केवल स्वांतः सुखाय नहीं लिखता। उनका कहना है कि 'आत्माभिव्यक्ति अपने आप में संपूर्ण नहीं है। अपनी अभिव्यक्ति, किंतु किस पर अभिव्यक्ति?' यहाँ आकर अज्ञेय जी ने न केवल तुलसीदास जी के 'स्वांतः सुखाय' लिखने पर शंका प्रकट की है, उन्होंने काव्यशास्त्र संबंधी पूरे आधुनिक विवेचन पर—कोलरिज से लेकर कोचे तक की सारी निष्पत्तियों पर एक प्रश्नचिह्न लगा दिया है। विशेषकर आत्माभिव्यक्ति को ही काव्य मानने वाले 'सब्जेक्टिव आइडियलिस्ट' (व्यक्ति- तत्त्ववादी) विचारकों के सामने एक समस्या खड़ी कर दी है।
यहाँ पहला प्रश्न यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने 'स्वांतः सुखाय' राम की गाथा लिखने की बात क्या झूठ कही है? वैसा कहने में उनका प्रयोजन क्या हो सकता है? यह मानने का कोई कारण नहीं दीखता कि गोस्वामी जी ने स्वांतः सुखाय नहीं लिखा अथवा आत्माभिव्यक्ति को काव्य मानने वालों का पक्ष ग़लत है। फिर अज्ञेय जी के इस कथन में क्या तथ्य है कि कोई भी कवि केवल स्वांतः सुखाय नहीं लिखता?' मेरे विचार से 'उलझी हुई संवेदना' ही उनके इस वक्तव्य के मूल में है। उनका यह कथन सार्थक अवश्य है कि 'अभिव्यक्ति' में एक ग्राहक या पाठक या श्रोता अनिवार्य होता है। पर श्रोता के अनिवार्य होने और स्वांतः सुखाय या आत्माभिव्यक्ति के लिए काव्य लिखने में कोई मौलिक विरोध नहीं है। उलझी हुई संवेदना की भूमि को पार कर काव्य के स्तर पर कवि जो भी रचना करता है, वह आत्माभिव्यक्ति ही होती है। आत्माभिव्यक्ति होने पर ही वह काव्य कही जाती है और तभी वह श्रोता या ग्राहक को सुलभ-सुखद होती है।
किंतु 'उलझी हुई संवेदना' के कारण प्रयोगवादी कवि बुद्धि और भावना के ऐसे संघर्षों में पड़ा रहता है कि वह अपने और श्रोता के बीच के द्वंद्व को मिटा ही नहीं पाता। इस बौद्धिक और शंकालु प्रवृत्ति के कारण प्रयोगवादी कवि अन्वेषी हो जाता है और वास्तविक काव्यभूमि पर कभी पहुँचता ही नहीं। ऐसे कवि व्यक्तियों की जीवन-संबधी धारणाएँ इतनी 'बुद्धिग्रस्त' हो जाती हैं कि कभी-कभी तो उनका अर्थ समझना भी आसान नहीं होता। उदाहरण के लिए 'तारसप्तक' में की गई अज्ञेय जी की 'प्रेम' की यह व्याख्या—'निराशा और कुंठा से धैर्यपूर्वक लड़ता हुआ, किंतु विश्वास की निष्कम्प अवस्था से कुछ नीचे—आज के प्रेम का सर्वोत्तम संभव रूप यही है' (पृष्ठ 76)। 'आज के प्रेम के सर्वोत्तम संभव रूप का निरूपण! कितना उलझा हुआ बुद्धि-विभ्रांत प्रयास! एक अन्य स्थान पर ‘व्यक्ति-सत्य’ (कवि की अनुभूति) और 'व्यापक सत्य' (सार्वजनिक अनुभूति) के अंतर को प्रदर्शित करते हुए ऐसी ही बुद्धिविजड़ित व्याख्या अज्ञेय जी ने की है, “यदि हम यह मान लेते हैं (यह कि व्यक्तिबद्ध सत्य जितना ही व्यापक होगा उतना ही काव्योत्कर्ष-कारी) तब हम 'व्यक्ति सत्य' और 'व्यापक सत्य' की दो पराकाष्ठाओं के बीच में उसके कई स्तरों की उद्भावना करते हैं, और कवि इन स्तरों में से किसी एक पर भी हो सकता है।” यहाँ स्पष्ट है कि 'व्यक्ति सत्य' और 'व्यापक सत्य' की भूमियों को कोरी बौद्धिक दृष्टि से देखा गया है, तभी उसमें अनंत स्तरों और भेदों की संभावना पाई गई है। अज्ञेय जी 'उलझी हुई संवेदना' की भूमि से ही यह सारी नाप-जोख करते हैं, अन्यथा प्रेम और सत्य (व्यक्तिगत या समूहगत) के संबंध में किसी कवि को इतनी परेशानी उठाने की आवश्यकता ही क्या पड़ती! 'प्रेम' और 'सत्य'—कवियों की अपनी वस्तुएँ, उनका चिरकालिक उत्तराधिकार!
परंतु अज्ञेय जी के इस प्रयास से (वह कितना ही थका देने वाला क्यों न हो) यह लाभ तो हुआ हो कि आधुनिक हिंदी कविता में 'प्रयोगवाद' की स्थिति और स्वरूप का हमें कुछ आभास और परिचय मिल सका और अब हम उन व्याख्याओं की सहायता से प्रयोगवादी काव्य की एक सामान्य परिभाषा करने की स्थिति में आ गए हैं। वह परिभाषा कुछ इस प्रकार होगी—'उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति के लिए अथवा अभेद्य क्षेत्रों में जाने की स्वाभाविक प्रेरणावश सीधी-तिरछी लकीरों, सीधे या उलटे अक्षरों आदि का उपयोग करते हुए कभी किसी विषय पर सहमत न होने वाले अन्वेषियों की रचना।' इनमें से एक-एक वाक्यखंड को लेकर उसकी थोड़ी सी छान-बीन करते ही हम प्रयोगवादी कविता के संबंध में नीचे लिखे निष्कर्षों पर पहुँचते हैं:—
'उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति' से यह ज़ाहिर है कि कवि पर एक अतिरिक्त बुद्धिवादिता का शासन है। वह अनिश्चित मानसिक स्थिति का व्यक्ति है और काव्य की वास्तविक भावभूमि पर पहुँचने में अक्षम है। हम यह मान लेते हैं कि आज कवि पर अनेक प्रकार के मानसिक दबाव और दुश्चिंताएँ रहती हैं। उसका व्यक्तित्व किसी हद तक जटिल मानसिक उपकरणों से बना होता है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह अपनी संवेदनाओं को—वे जैसी भी हैं—सुलझा न सके और उनकी काव्यात्मक (या भावात्मक) अभिव्यक्ति न कर सके। 'उलझी हुई संवेदना की अभिव्यक्ति से तो मूलवर्ती कविकर्म के ही अभाव की सूचना मिलती है—ऐसी कमी जो कवित्व की सत्ता पर ही आघात करती है।
एक उदाहरण लेकर यह बात और स्पष्ट की जा सकती है। हिंदी में कवि 'बच्चन' की रचनाएँ मनोवैज्ञानिक कुंठा या दबाव का परिणाम कही जाती हैं, परंतु उनमें उलझी संवेदना की अभिव्यक्ति नहीं है। उनकी रचनाओं में आप विक्षत, आह्त या पराजित अनुभूति पाएँ यह संभव है, और यह भी संभव है कि आप उनके काव्य को कुंठापूर्णं या हासोन्मुख काव्य कहें, पर वह काव्य अवश्य है। उसे आप उलझी संवेदना की अभिव्यक्ति का बौद्धिक या असाहित्यिक प्रयास नहीं कह सकते। काव्य संबंधी उत्तरदायित्व बच्चन जी ने पूरा किया है, और अपनी व्यक्तिगत अनुभूतियों के प्रति न्याय किया है। भले ही वह उत्तरदायित्व सामाजिक जीवन-विकास के अनुकूल न हो। पर प्रयोगवादी रचनाकारों में क्या यह मूलवर्ती साहित्यिक उत्तरदायित्व भी है?
अब दूसरा वाक्यांश 'अभेद्य क्षेत्रों में जाने की स्वाभाविक प्रेरणा' लेकर देखिए। यही वह वैचित्र्यवाद है जिसके मूल में कोई गंभीर भावना काम करती नहीं जान पड़ती। पुराने कवियों में यह प्रवृत्ति केशवदास में थी जो अलंकारों के क्षेत्र में नए अन्वेषण करने के आदी थे और इसीलिए जिनके अलंकार कृत्रिम और अकाव्योपयोगी हुए हैं। वे केवल चमत्कार की सृष्टि करते हैं।यही स्थिति नए प्रयोगवादियों की है जिन्होंने वैचित्र्य के लिए सीधी-टेढ़ी लकीरों और सीधे या उलटे अक्षरों को चुना है। यह तो बिना कहे ही ज़ाहिर है कि इस प्रकार की काव्य-प्रवृत्ति कलाहीन और असाहित्यिक है, यद्यपि अज्ञेय जी की यह धारणा है कि इस प्रकार का अन्वेषण भाषा-संबंधी किसी आवश्यक अभाव की पूर्ति में सहायक होता है। अधिक से अधिक ऐसे प्रयासों को हम नवीनता का अनोखा तक़ाज़ा कह सकते हैं।
कभी-कभी प्रयोगवादी प्रवृत्ति काव्य के विषयों और वर्णनों में भी नवीनता का संचार करती देखी जाती है। उदाहरण के लिए आज के कवि और लेखक मनोविज्ञान, जीवविज्ञान, समाजविज्ञान तथा अन्य विषयों की पुस्तकों को पढ़ कर उसमें पाए जाने वाले नवीन तथ्यों का उपयोग अपनी साहित्यिक रचनाओं में करते हैं। जहाँ तक इनसे लेखक की बहुज्ञता का परिचय मिलता है, यह उपक्रम प्रशंसनीय है। कभी किसी चरित्र-विश्लेषण या स्वभाव वर्णन के प्रसंग में ये प्रयोग और दृष्टांत अत्यंत सजीव और आकर्षक भी बन जाते हैं जिससे रचना का महत्त्व बढ़ता है। परंतु किसी भी अवस्था में यह प्रयोगों का बाहुल्य वास्तविक साहित्य-सृजन का स्थान नहीं ले सकता।
प्रयोग में और काव्यात्मक निर्माण या सृजन में जो मौलिक अंतर हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विशेष कर काव्य का क्षेत्र प्रयोगों की दुनिया से बहुत दूर हैं। कवि सब से पहले अपनी अनुभूतियों के प्रति उत्तरदायी है। वह उनके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसका दूसरा उत्तरदायित्व काव्य परंपरा और काव्यात्मक अभिव्यक्ति के प्रति है। वह किसी भी अवस्था में ऐसे प्रयोगों का पल्ला नहीं पकड़ सकता जिनका उस काव्य के भावगत और भाषागत संस्कारों से तथा उन दोनों के स्वाभाविक विकास क्रम से सहज संबंध नहीं है। हमारे कवि हमारे काव्य-क्षेत्र में अजनबी बन कर आएँ और रहें यह उनके लिए ही नहीं हमारे लिए भी एक ओछी बात होगी। हम अपने काव्योद्यान में ऐसे फूल लगाना नहीं चाहेंगे जो हमारी धरती से रस खींचना अस्वीकार करें और जिन्हें प्रयोगों का इंजेक्शन देकर ही जिलाया जा सके।
तीसरे वाक्यांश 'कभी किसी विषय में सहमत न होने वाले अन्वेषियों' का अर्थ भी स्पष्ट ही है। मित्रों और कुत्तों पर हँसने में एक साधारण विनोद-वृत्ति भले ही लक्षित होती हो, पर 'समाज के सर्वमान्य मौलिक सत्यों को अस्वीकार' करने में व्यंग्य और विद्रोह की भावना व्यंजित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे व्यक्ति व्यापक समाज के प्रति गहन आत्मीय संबंध से बँधे हुए नहीं हैं, केवल उसको तार्किक भूमियों में विचरण करना ही जानते हैं। विद्वानों का आपस में मतभेद रखना और बात-बात में एक दूसरे से असहमत होना उन विद्वानों के लिए भी ख़तरे का काम है! सक्रिय सामाजिक सहयोग के बदले एक सर्वदिक् उपेक्षा-वृत्ति का प्रदर्शन समाज के लिए आशा का नहीं अनिष्ट का ही परिचायक है।
और इन व्याख्याओं और निर्देशों को जब हम अज्ञेय जी के मुख्य वक्तव्य में कही गई इस बात के साथ जोड़ कर देखते हैं कि ये प्रयोगवादी कवि मंज़िल पर पहुँचे हुए नहीं है, राही भी नहीं हैं, केवल राहों का अन्वेषण कर रहे हैं तब प्रयोगवाद के स्वरूप और स्थिति के संबंध में हमारे ये निष्कर्ष और भी सहज अनुमेय हो जाते हैं। संक्षेप में हम अपने निष्कर्षों को इस प्रकार रख सकते हैं:—
1. प्रयोगवादी रचनाएँ पूरी तरह काव्य की चौहद्दी में नहीं आतीं। वे अतिरिक्त बुद्धिवाद से ग्रस्त हैं।
2. प्रयोगवादी रचनाएँ वैचित्रय-प्रिय हैं, वृत्ति का सहज अभिनिवेश उनमें नहीं।
3. प्रयोगवादी रचनाएँ वैयक्तिक अनुभूति के प्रति ईमानदार नहीं हैं और सामाजिक उत्तरदायित्व को भी पूरा नहीं करतीं।
ऊपर हमने देखा कि कवि का उत्तरदायित्व मुख्यतः तीन वस्तुओं के प्रति होता है—, 1 व्यक्तिगत अनुभूति के प्रति, 2 काव्य सत्ता के प्रति और 3 सामाजिक जीवन के प्रति। हमारे प्रयोगवादी कवियों में उनमें से एक भी पक्ष परिपुष्ट नहीं है।
दो
ऐसी अवस्था में प्रश्न यह होता है कि हिंदी काव्य में प्रयोगवादी रचनाओं की आवश्यकता या उपयोगिता ही क्या है?
इस प्रश्न का उत्तर 'तारसप्तक' में संग्रहीत कुछ अन्य कवियों ने देने की चेष्टा की हैं। श्री० प्रभाकर माचवे इसको उपयोगिता छायावाद और प्रगतिवाद के दोनों छोरों को मिलाने की दृष्टि से मानते हैं। वे लिखते हैं—छायावाद हिस्टीरिया की भाँति हिंदी कविता का एक मानसिक रोग है। दोनों में स्मृतियों की प्रच्छन्न और अज्ञात पुनरावृत्ति तथा तज्जन्य अहेतुक त्रास दिखाई देते हैं।' ...'पेंडुलम प्रतिक्रिया से जिस प्रकार दूसरा छोर पकड़ लेता है, ऐतिहासिक जड़वाद के अध्ययन से और भारतीय राजनैतिक क्षितिज के धूम-संकुल हो जाने से नए कवियों ने छायावाद तज प्रगतिवाद को अपनाया। अपनी प्रारंभिक अवस्था में यह अभी अपरिपक्व और नाम का ही प्रगतिवाद है।'
और इसी कारण माचवे जो यह समझते हैं कि हिंदी में 'प्रयोगशील अभिव्यंजना' (या प्रयोगवादी कविता) के मध्यमार्ग पर चलने की आवश्यकता और गुंजाइश है। आप लिखते हैं कि हिंदी कविता में विषयों की विविधता, व्यंग्य का तीक्ष्ण और सुरुचिपूर्ण प्रयोग, प्रकृति के संबंध में अधिक वैज्ञानिक दृष्टि, आदि का विकास होना चाहिए। उनकी राय में 'हमारी कविता में पाए जाने वाले अधिकांश कल्पना-चित्र या बिंब बच्चों के से निरे शाब्दिक, सहस्मृत या परंपरागत होते हैं। इनके बजाए हमें राग और ज्ञान से पूरित ऐंद्रयिक, आवेगाश्रित और अभिजात मूर्त-विधान करना है।'
यह सब तो ठीक है पर हमारा कहना यह है कि जब छायावाद ‘हिस्टीरिया’ है और प्रगतिवाद 'दमित इच्छाओं से निर्मित होने वाला औद्धत्य की सीमा पर पहुँचा हुआ परपीड़न-प्रेम है' तब इन दोनों के संयोग से उत्पन्न हुई प्रयोगवादी संतति सर्वगुण संपन्न होगी कैसे? इस प्रकार की बेमेल और संकर सृष्टि पर हमारा विश्वास नहीं है। हिंदी में समन्वय-भावना या समझौते के मार्ग का विज्ञापन करने वाले यदि यह जान लेते तो अच्छा होता कि समझौता सदैव एक हार या पराजय का भी परिचायक होता है। विचारों और विश्वासों की निर्बलता प्रायः समस्त समझौतों के मूल में रहा करती है।
इसलिए यदि इन नवीन प्रयोगों को समन्वयात्मक प्रयास न कह कर परिवर्तन की एक चेष्टा कहा जाए और यदि यह मान लिया जाए कि प्रयोगवाद कोई काव्यपद्धति नहीं है, वरन् वह पिछले खेवे के छायावादी साहित्य और विशेष कर महादेवी जी की गहन ऐकांतिकता और बच्चन की उच्छवासपूर्ण नराश्य-भावना की प्रतिक्रिया में किया गया व्यंग्य-विनोद पूर्ण हल्का काव्य प्रयत्न है, तो हम कदाचित् प्रयोगवाद की ऐतिहासिक वस्तुस्थिति के अधिक समीप कहे जाएँगे। पर यहाँ भी यह प्रश्न रह जाता है कि क्या प्रयोगवादी कविता में भी उन्हीं भावनाओं का संचार नहीं होने लगा है जिनके निषेध का श्रेय हम उसे दे रहे हैं। क्या इन नवीन प्रयोगों में भी निराशा और विषाद का प्रभाव व्याप्त नहीं है? और इतना होते हुए भी क्या काव्यदृष्टि से ये उन मूल रचनाओं की बराबरी पर रखे जा सकते हैं?
हमें मानना पड़ेगा कि प्रयोगवाद की किसी सुनिश्चित आवश्यकता या वैशिष्ट्य पर हम आग्रहपूर्वक कुछ नहीं कह सकते, सिवा इसके कि युग और समाज की स्थितियों और प्रवृत्तियों ने इसे भी जन्म दिया है और हिंदी के विशाल कव्योद्यान में प्रयोगवादियों के लिए भी स्थान मिल गया है। एक दूसरे अर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि काव्य-समृद्धि आधुनिक साहित्य के युगों में ही कोई साहित्य ऐसे प्रयोगों के लिए अवकाश पा सकता है और हिंदी में इतनी पर्याप्त समृद्धि है कि वह इन संशयालु और संस्कार शिथिल कवियों के अनगढ़ प्रयोगों की कुरूपता को भी सहन कर लेती है।
तीन
अब प्रयोगवादी रचनाओं के कुछ नमूने लेकर देखना चाहिए। पर इसके पहले यह आरंभिक निवेदन कर देना आवश्यक है कि भाषा, पद-प्रयोग, छंद, तुक आदि के संबंध में प्रयोगवादियों ने जिन नई खोजों का दावा अपनी व्याख्याओं और विवेचनों में किया है, उनसे संभ्रम में पड़ कर यह न समझ लेना चाहिए कि उन समस्त खोजों या उनमें से अधिकांश का भी उपयोग वास्तविक रचनाओं में किया गया है। एक तो शैली और रचना-संबंधी इस ऊहापोह या आडंबर से ही यह प्रतीत होता है कि प्रयोक्ताओं ने काव्य-कामिनी का सौंदर्य उसके ऊपरी संभार और प्रसाधनों में ही समझ लिया है—एक ऐसी अभिरुचि जिसका सामाजिक प्रतिरूप आजकल के सौंदर्य-द्रव्यों की बाढ़ में देखा जाता है। यह अभिरुचि आधुनिक भले ही हो, अभिनंदनीय नहीं है—स्वस्थ सौंदर्य-दृष्टि की परिचायक नहीं है। रुग्ण नारी को वेश-भूषा से सज्जित करने का सा प्रयास है। फिर, जिन सौंदर्य-चमत्कारों की खोज का वे विज्ञापन करते हैं, उनका व्यवहार वे अपनी कृतियों में कर सके हैं या नहीं, यह भी देखना होगा। शैली-संबंधी वे सौंदर्य प्रयोग हमारी भाषा की प्रकृति और हमारी रचनात्मक परंपरा के मेल में हैं या नहीं यह भी जानना होगा, क्योंकि निरे विदेशी सौंदर्योपचारों को आँख मूँद कर अपनाने में हम कोई विशेषता नहीं देखते।
एक छोटी-सी पृष्ठभूमि बनाकर और उसमें खड़ी-बोली कविता के क्रम-विकास की एक हल्की झाँकी दिखाते हुए इस वस्तु को प्रस्तुत करना अधिक उपयोगी होगा। नई खड़ी-बोली कविता की शैशवावस्था में (आज से 40-50 वर्ष पूर्व) एक नई सामाजिक जागृति के साथ एक संयत आदर्शवादी विचारधारा का पहला आलोक फैलने लगा था। उस प्रातःकालीन वातावरण में एक सरल सुंदर दीप्ति थी। मन पर किसी प्रकार के अन्यथा आवरण न थे। आशा का हल्का उत्साह था, विश्वास की प्रचंड गरिमा न थी। इस काल के कवियों की भावना में एक सरल सौम्यता खेल रही थी। कल्पना की आकाशीय उड़ानों का नाम न था। कवियों ने अधिकतर पुराने आख्यान लेकर उन्हें अपट्टी नई भावना से सज्जित किया। चित्रित चरित्रों और वर्णन किए गए विषयों में कोई बड़ी व्यापकता या प्रसार न था। मनोवैज्ञानिक संघषों की भरमार न थी। अभिव्यंजना में भी सरलता थी, सजावट न थी। अलंकारों और अप्रस्तुतों की योजाना चकाचौंध करने वाली नहीं थी! भाषा का आच्छद कलात्मक न था (रचना में भाषा को पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया गया था) किंतु क्लिष्टता और बेढंगापन भी उसमें नहीं था। इन समस्त विशेषताओं का सूचक एक उदाहरण देखा जा सकता है—
प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है?
दुःख-जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है?
लख मुख जिसका मैं आज लौं जी सकी हूँ
वह हृदय हमारा चैन-तारा कहाँ है? (हरिऔध)
यद्यपि कविता में खड़ी बोली का व्यवस्थित प्रयोग इसी समय से आरंभ होता है, पर स्मरण रखना चाहिए कि व्रजभाषा की एक मँजी हुई और शिष्ट परंपरा उस समय भी कार्य कर रही थी। श्रीधर पाठक और 'रत्नाकर' जैसे कवि उसकी साजसज्जा में लगे हुए थे। कदाचित् इस पार्श्ववर्ती प्रगति के कारण ही खड़ी-बोली कविता में भी कहीं-कहीं भाषा को सजाने की प्रवृत्ति दिखाई देती हैं। ब्रजभाषा कवियों के लिए स्थिति नई नहीं थी। ब्रजभाषा का विशाल काव्य-भंडार उनके पास था। खड़ी-बोली के कवियों के लिए वह वस्तु नए प्रयोग के रूप में ही आई। उन्हें (खड़ी बोली के कवियों को) संस्कृत शब्दावली के अनभ्यस्त चयन का नया कार्य करना पड़ा। परंतु इस प्रकार के प्रयोगों का बाहुल्य कभी नहीं हो पाया और न वे हिंदी की प्रतिनिधि काव्य-शैली के रूप में परिगणित हो सके। ऐसे उदाहरणों में नीचे की पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध है:—
रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय कलिका राकेंदु बिश्वानना,
तन्वंगी कल-हासिनी सुरसिका क्रीड़ा कला पुत्तली,
शोभा-वारिधि की अमूल्य मणि सी लावण्य लीला मयी
श्री राधा मृदुभाषिणी मृगदृगी माधूर्य सन्मूर्ति थीं। (हरिऔध)
इसी युग के दूसरे प्रतिनिधि कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त हैं जिनकी रचनाएँ प्रायः पचास वर्षों के लंबे समय तक फैली होने के कारण कई नए प्रभावों को भी ग्रहण करती गई हैं। विशेषकर 'द्वापर' के मनोवैज्ञानिक चित्रणों और 'साकेत', 'कुणाल गीत' और 'झंकार' की गीतात्मक रचनाओं में गुप्त जी के एक नए काव्य-स्वरूप का आभास पाया जाता है। यह ठीक है कि गुप्त जी के लंबे काव्य-विकास में किसी एक युग की अकेली छाप नहीं रही, पर उनके मुख्य और मूलवर्ती काव्याधार को परख सकना फिर भी कठिन काम नहीं है। अपने भाषा प्रयोग में (शब्द संगीत और शब्द-शक्तियों के उपयोग में) पीछे आने वाली छायावादी काव्यधारा से अपनी दूरी की सूचना वे पुकार कर देते हैं। छायावादी कल्पना-प्रवणता और सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रणों से भी वे अधिक संबंध नहीं रखते। 'अज्ञात की अभिलाषा' और अन्य स्वच्छंद प्रवृत्तियाँ भी उनमें नहीं हैं। गुप्त जी को प्रतिनिधि रचनाओं के दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:—
जो कोकिला नंदन-विपिन में हर्ष से गाती रही।
दावाग्नि दग्धारण्य में रोने चली है अब वही। (भारत भारती)
मुझे फूल मत मारो।
मैं अबला बाला वियोगिनी कुछ तो दया विचारो।
रूप दर्प कंदर्प तुम्हें यदि मेरे पति पर वारो।
लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। (साकेत)
स्पष्ट है कि ये रचनाएँ अपने भाषा परिधान में किसी ऊँची कलात्मकता, चयन या सौष्ठव का दावा नहीं करतीं और न इनके भाव या रूप-चित्रण में किसी प्रकार का असाधारण उत्कर्ष या मनोवैज्ञानिक बारीकी है। न ये रचनाएँ कल्पना के प्रचुर और अबाध सामर्थ्य की परिचायक हैं। इन विशेषताओं से संपन्न साहित्य का आगमन कुछ समय पश्चात् छायावादी काव्ययुग में हुआ।
छायावादी काव्ययुग हिंदी कविता के नवीन विकास का स्वर्णयुग रहा है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं, जिनकी समता का कवि पाकर कोई भी साहित्य गौरवांवित हो सकता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काव्ययुग भी अपने समय पर विकसित होते हैं और उस समय के बीत जाने पर नई काव्य-शैलियाँ प्रवर्तित होती हैं। इसलिए यह कहने का कोई अर्थ नहीं होता कि छायावाद काव्यधारा इतना शीघ्र समाप्त क्यों हो गई। कुछ लोगों ने छायावाद के पतन का कारण भी बताना चाहा है, पर वह ऐसा ही है जैसे कोई वसंत ऋतु के पतन (!) का कारण बताने बैठे। कुछ अन्य लोगों ने मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता के नाम पर छायावादी काव्य-सृष्टियों को रुग्ण और अस्वस्थ बताने की चेष्टा की है पर वह चेष्टा 'अँगूर खट्टे हैं' वाली कहावत का ही पूरा निदर्शन बनी है। कतिपय मतप्रवर्तकों ने यह भी कहा है कि छायावादी काव्य व्यक्तिवादी और अंतर्मुख है और वह सामाजिक भूमि का व्यापक स्पर्श नहीं करता। पर जिन कवियों को वे व्यक्तिवादी बताते हैं उन्हीं पर (उन्हीं के कवित्व रहित वाग्जाल पर) उनके प्रगतिवादी मतवाद की नैया अपना सहारा ढूँढ़ती है। निराला और पंत (और विशेषकर पंत, क्योंकि उनकी रचनाओं की कील जल्दी-जल्दी घूम जाती है) आज भी इस नवीन काव्यवाद के नेता या उन्नायक माने जाते हैं। उनके और हमारे विचारों में अंतर यह है कि हम निराला और पंत की सन् 35 के पीछे की रचनाओं को उस काव्यस्तर पर नहीं पाते जिस स्तर पर इस समय के पूर्व की रचनाओं को पाते हैं। और इसके विपरीत प्रगतिवाद के हिमायती पिछली रचनाओं को ही अधिक श्रेष्ठता और महत्त्व देते हैं। उदाहरण के लिए प्रगतिवाद के समर्थ सहायक श्री राहुल जी पंत का काव्यविकास दिखाते हुए 'पल्लव' 'वीणा' या 'गुंजन' की रचनाओं को, पंत जी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, रुग्णावस्था की रचना बतलाते हैं और सबसे बड़ा आश्चर्य तो यह है कि स्वयं पंत जी अपने को सन् 30 के पहले अस्वस्थ शरीर और अस्वस्थ मनोवृत्ति का स्वीकार करने लगे हैं। पर उन लोगों को क्या कहा जाए जिन्होंने सन् 30 के पहले के पंत जी के सौम्य, सुंदर और स्वस्थ चित्र देखे हैं या स्वयं जीते-जागते पंत जी को ही देखा है! इस प्रकार के बयान और विवरण साहित्य-समीक्षा के वास्तविक निर्माण में सहायक नहीं हो सकते। यदि हम यह मान भी लें कि सन् 30 के आसपास पंत जी कुछ दिन अस्वस्थ रहे थे तो भी शरीर की अस्वस्थता सदैव मन की अस्वस्थता नहीं हुआ करती, और थोड़ी देर के लिए हम यह भी मान लें कि पंत जी वास्तव में सन् 30 के पहले या आसपास शरीर और मन दोनों से अस्वस्थ थे तो भी यह कौन साबित कर सकेगा कि उस समय की पंत जी की सुंदरतम रचनाएँ शारीरिक और मानसिक अस्वास्थ्य का परिणाम हैं! प्रश्न और समस्या बिल्कुल साफ़ और दोटूक है। हमारे सामने पंत जी की सन् 30 तक की रचनाएँ हैं और फिर उनके 34-35 से आरंभ होने वाले मतवादी उद्गार हैं। देखना यह है कि साहित्यिक दृष्टि से (और साहित्यिक दृष्टि के अंतर्गत, मेरे विचार से वे समस्त दृष्टियाँ समन्वित हो जाती हैं जिनका काव्य के उत्कर्ष-अपकर्ष संबंधी निर्णय से कुछ भी संबंध हो सकता है) इन दोनों में से किस वर्ग की रचनाएँ श्रेष्ठतर हैं। यह एक विशुद्ध साहित्यिक समस्या है अतएव इसके निर्णय के लिए हम समस्त साहित्यिकों को आमंत्रित कर सकते हैं।
सन् 30 के पूर्व की पंतजी को दो रचनाओं के उदाहरणय हैं:—
1. आज बचपन का कोमल गात
ज़रा का पीला पात!
चार दिन सुखद चाँदनी रात
और फिर अंधकार अज्ञात।
*** *** ***
अभी तो मुकुट बँधा था माथ,
हुए कल ही हलदी के हाथ;
बना सिंदूर अँगार!
वातहत लतिका वह सुकुमार
पड़ी छिन्नाधार। (परिवर्तन)
2. अये, एक रोमांच तुम्हारा दिग्भूकंपन,
गिर-गिर पड़ते भोत पक्षिपोतों से उडुगन :
आलोडित अंबुधि फेनोन्नत कर शत शत फन
मुग्ध भुजंगम सा इंगित पर करता नर्तन!
दिक पिंजर में बद्ध गजाधिप सा विनतानन
वाताहत हो गगन
आर्त करता गुरु गर्जन! (परिवर्तन)
यहाँ जान बूझकर मैंने एक ही रचना से ऐसे दो स्थल चुने हैं जो दोनों ही निराशावादी उद्गार कह कर रुग्ण और अस्वस्थ असामाजिक और अप्रगतिशील (और न जाने क्या क्या) घोषित किए जाते हैं। साथ ही ये दोनों पद्य दो पृथक् पद-रचना के उदाहरण हैं। दोनों ही पद्म कल्पना की मूर्तिमत्ता से पूर्णतः सज्जित हैं। पहले पद्य में 'बचपन का कोमल गात' अपनी वर्णध्वनि में बचपन की कोमलता का आभास लिए हुए है। जरावस्था 'पीला पात' द्वारा प्रत्यक्ष की गई है। 'चार दिन सुखद चाँदनी रात' में एक लोक-प्रचलित उक्ति (चार दिन की चाँदनी फिर अँधियाली रात) को परिष्कृत रूप में अपनाया गया है। पाँचवीं और छठी पंक्तियों में 'माथे पर मुकुट बाँधा जाना' और 'हल्दी के हाथ' होना, इतने प्रसिद्ध लोकाचार से जुड़े हुए हैं और साथ ही इतना अनायास मांगलिक भावों का द्योतन करते हैं कि पाठक की स्मृति इन उपमानों का सहज ही साथ देती है और उसके सामने विवाह का पूरा चित्र जाग उठता है। सातवीं पंक्ति वैषम्य का झटका देने के लिए लाई गई है—छंद में भी वह ऊपर की पंक्तियों से भिन्न है। आठवीं और नवीं पंक्तियाँ फिर एक नई उपमा—और अत्यंत प्राकृतिक उपमा—'वायु से उखाड़ी सुकुमार लता' को हमारी आँखों के सामने लाती हैं। कोई भी पंक्ति ऐसी नहीं है जिसमें कोई रूप-योजना न हो—दृश्य को साकार करने का सामर्थ्य न हो।
दूसरा उदाहरण और भी संश्लिष्ट कल्पना योजना से संपन्न है। प्रलय के समय होने वाला विराट् परिवर्तन चित्रित किया गया है—उसी के अनुरूप समस्त रुपयोजना में विराट उपमानों का संग्रह है—दिशाओं और पृथिवी का काँप उठना, पक्षियों के बच्चों की भाँति आकाश के तारों का टूट गिरना, समुद्र की ऊँची लहरों का फण उठा कर साँप की भाँति प्रलय के इशारे पर नाचना। दिशाओं के पिंजड़े में बद्ध आकाश रूपी हाथी का, वायु के कोड़े खाकर, नतमस्तक और आर्त भाव से कराहना—सभी चित्र प्रलय की भयंकरता लिए हुए हैं और समस्त पद्य की भाषा अपने असाधारण उत्कर्ष में प्रस्तुत किए गए भाव का पूरा साथ देती है। पहले पद्य की शैली सरल और मुहावरेदार है, दूसरे पद्य में संग्रथित और धारावाही शब्द चयन किया गया है।
काव्य की दृष्टि से दोनों पद्य ऊपर उद्धृत हरिऔध जी और मैथिलीशरण जी के पद्यों की अपेक्षा स्पष्ट ही अधिक समुन्नत काव्य वैभव लिए हुए हैं। शब्दों की संगीतात्मकता, भावानुरूपता और अर्थप्रवणता में ऊपर के दोनों कवियों की अपेक्षा पंत जी का रचना-संभार अधिक समृद्ध हैं। रूपों (उपमानों या अप्रस्तुतों) की योजना में पंत जी की कल्पना कहीं अधिक शक्तिमती है। प्रस्तुत किया जाने वाला भाव भी इस सशक्त और समृद्ध रूपयोजना के कारण पूरी तरह खिल उठा है। काव्य-दृष्टि से किसी ऐसी वस्तु का अभाव या कमी नहीं है जिसके कारण रचना को काव्य की सर्वोच्च श्रेणी में न रखा जा सके।
परंतु जिन महानुभावों को काव्य-साहित्य की अपनी विशिष्ट परंपरा से संबंध नहीं है, जो रचना के निर्माणात्मक गुणों को परखने के अभ्यस्त नहीं हैं—या परखना चाहते ही नहीं, वे इन कृतियों पर क्या-क्या आरोप नहीं लगाया करते! ऐसे समीक्षकों की विशेषता यह है कि उनके ये आरोप कभी कुछ और कभी कुछ—प्रायः परस्पर विरोधी हुआ करते हैं, जिनके कारण वे अपने ही तकों को अपने ही तर्कों से काट कर बराबर कर देते हैं। पर कठिनाई यह है कि इस काटा-कूटी में वास्तविक तथ्य भी घायल हो जाता है और काव्य-सत्य की ओर हमारा ध्यान नहीं जा पाता।
इस साहित्यिक अनाचार को रोकने का कार्य सच्चे साहित्यिकों का ही है—वे साधक जो जीवन की प्रगति के साथ काव्यप्रगति का संबंध देख सकें और साथ ही जो काव्य की अपनी सत्ता को किसी काव्येतर या असाहित्यिकवाद की धीगाधींगी में पड़ने से बचा सकें। जैसे किसी बच्चे के हाथ में तेज़ धार की छूरी नहीं दी जा सकती या किन्हीं हिलते हाथों को ऑपरेशन का काम नहीं सौंपा जा सकता वैसे ही किन्हीं नौसिखिए वाद-विज्ञानियों या किन्हीं स्थविर शास्त्राचारियों को भी आधुनिक काव्य-समीक्षा का कार्य नहीं सौंपा जा सकता।
पर इस प्रासंगिक चर्चा में पड़ कर हम अपने मुख्य विषय से अधिक दूर नहीं जाना चाहते। अतएव हमें अपने विचार प्रवाह का संवरण कर छायावाद युग के कुछ अन्य प्रतिनिधि कवियों की रचनाओं के स्फुट उदाहरण देखने होंगे। प्रसाद जी, जो इस युग के प्रवर्तक और प्रधान संदेशवाहक हैं, जिनके दार्शनिक और सांस्कृतिक अध्ययन और मनन पर विरोधियों को भी श्रद्धा है, अपने काव्यनिर्माण में छायावाद युग की प्रमुख विशेषताओं को प्रतिफलित करते हैं। 'चिंता' और 'लज्जा' जैसी सूक्ष्म और अशरीरी वस्तुओं का चित्रण करने में उनकी लेखनी का चमत्कार देखा जा सकता है। केवल कुछ ही पंक्तियाँ दी जा सकती हैं:—
हे अभाव की चाल बालिके
री ललाट की खल लेखा।
हरी-भरी सी दौड़-धूप, ओ
जल-माया की चल रेखा!
इस ग्रह-कक्षा की हलचल, री
तरल-गरल की लघु लहरी।
जरा अमर जीवन की, और न
कुछ सुनने वाली बहरी। (चिंता : 'कामायनी' से)
*** *** ***
मंजुल स्वप्नों की विस्मृति में
मन का उन्माद निखरता ज्यों।
सुरभित लहरों की छाया में
बुल्ले का विभव विखरता ज्यों।
नीरव निशीथ में लतिका सी
तुम कौन आ रही हो बढ़ती;
कोमल बाहें फैलाए सी
आलिंगन का जादू पढ़ती। (लज्जा: 'कामायनी' से)
और 'निराला' जी, जिन्होंने नवीन कविता-कामिनी को मुक्त छंद का नया परिधान पहनाकर नीचे को पंक्तियों में उसका स्मरणीय स्वागत किया था। कौन जानता था कि उनको इस नई भेंट का कितना दुरुपयोग न होगा। भाषा की गति-लय से अपरिचित व्यक्ति मुक्त-छंद का सहारा लेकर कितने अनर्गल और काव्यहीन प्रयाग न करेंगे। निराला जी का मुक्त छंद काव्य को नया आच्छद देने की अभिरुचि का परिचायक है, उसे अशोभन या भोंड़े रूप में उपस्थित करने की प्रेरणा का परिणाम नहीं है, यह उनकी मुक्त-छंद को इस आरंभिक कृति से ही स्पष्ट हो जाता है:—
आज नहीं है मुझे और कुछ चाह।
अर्धविकच इस हृदय-कमल में आ तू, प्रिये,
छोड़कर बंधनमय छंदों की छोटी राह।
गजगामिनि, वह पथ तेरा संकीर्ण, कंटकाकीणे;
कैसे होगी उससे पार!
काँटों में तेरा चीर उलझ जाएगा,
और निकल जाएँगे उसके तार—
जिसे अभी-अभी पहनाया,
किंतु नज़र भर देख न पाया,
कैसा सुंदर आया!
इन पंक्तियों में कवि के कलापूर्ण साधन-प्रेम की झलक तो है ही, उसके भाषा संबंधी अधिकार और कुशल गतियोजना का भी यथेष्ट आभास है और इन सबके ऊपर उसका अदम्य आत्मविश्वास तथा प्रवाहमयी कल्पना या रुपयोजना का सामर्थ्य भी स्पष्ट होता है। छायावादी काव्य को भाषा-संबंधी प्रौढ़ प्रयोग और नए शब्द चयन के साथ नवीन सामासिक योजना के सबसे अधिक उपहार निराला जी के काव्य से ही मिले हैं। भावचित्रण में अज्ञात की आकांक्षा का सुन्दर स्वरूप उनकी रचनाओं में व्यंजित हुआ है: —
लख ये काले काले बादल,
नील सिंधु में खुले कमल-दल;
हरित ज्योति चपला अति चंचल
सौरभ के, रस के—
अलि, घिर आए घन पावस के।
इन पंक्तियों में काले बादलों का घिरना देखकर नील-सिंधु में (श्वेत) कमलदलों का खिल पड़ता और उन पर पड़कर विद्युत की चंचल ज्योति का हरित वर्ण की झलक मारता, जहाँ एक ओर रंगों का समारोह सामने लाता है, वहीं दूसरी पंक्ति में 'नील सिंधु' में कमलदलों के खिलने की सूचना कवि की अज्ञात सौंदर्य-लालसा की परिचायक है।
इन सुंदरतम काव्य-प्रयोगों के मूल में एक अभिनव रहस्य-भावना, एक विश्वजनीन दार्शनिकता और एक परिष्कृत सौंदर्य-चेतना काम कर रही थी। विना उस मूलवर्ती आधार के रचनाओं में यह चमत्कार और ये कलात्मक विशेषताएँ न आ सकतीं, यह स्वीकार करने के लिए यदि हमारा सामान्य बोध (Common Sense) पर्याप्त नहीं है, तो कदाचित् इस छोटे दायरे में दिए गए निदर्शन भी पर्याप्त न होंगे। इसलिए हम रचना-संबंधी दृष्टांतों का सहारा छोड़ कर स्वयं एक रचयिता (या रचयित्री) का साकार दृष्टांत लेते हैं—वह दृष्टांत है महादेवी वर्मा का। छायावाद काव्ययुग के अंतिम और विलंबित प्रतीक के रूप में महादेवी जी इस बात की सूचना तो देती ही हैं कि आधुनिक छायावाद या रहस्यवाद एक स्वतंत्र जीवन-दृष्टि से ही नहीं कदाचित् एक गंभीर साधना-प्रणाली से भी संबद्ध है।
महादेवी जी के काव्य को हमें सदैव आदर की दृष्टि से देखते आए हैं, पर यह स्वीकार करने में हमने कोई आपत्ति नहीं देखी कि महादेवी जो की रचनाओं में छायावादी काव्य को आरंभिक स्फूर्ति और स्वाभाविक (कहीं-कहीं उद्दाम) कल्पना-प्रवाह के बदले एक सुसंयत गति, एक सुचिंतित आभरणप्रियता और साथ ही एक सुनिर्दिष्ट प्रतीक योजना का भी क्रमशः सघन योग होता गया है। इन विशेषताओं के मनोवैज्ञानिक या अन्य प्रेरणा-सूत्रों पर बिना गए हुए भी हम दो बातें संशयरहित होकर कह सकते हैं। प्रथम यह कि छायावादी काव्यधारा की मूलवर्ती आध्यात्मिक भावना ही परिपुष्ट होकर महादेवी जी के काव्य में व्यक्त हुई है और दूसरी यह कि महादेवी जी की दुःखवादी दार्शनिकता कोरा दुःखवाद न होकर उसी आध्यात्मिक प्रेरणा से अनुरंजित है, जो छायावाद का मुख्य आधार है। काव्य-दृष्टि से महादेवी जी की रचनाएँ उज्वल किंतु मंथर रहस्यात्मक भाव सृष्टि से समन्वित हैं। आज उनकी कविता रहस्य-'वाद' से शृंखलित और सीमाबद्ध हो गई है, अतएव सभी 'वादी' रचनाओं की भाँति उसमें भी वह स्वातंत्र्य और प्रवेग नहीं है जो छायावाद के आरंभिक कवियों में प्रचुर मात्रा में रहा है। दो उदाहरण नीचे दिए जाते हैं:—
1. दूसरी होगी कहानी
शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में खोई निशानी।
आज जिस पर प्रलय विस्मित,
मैं लगाती चल रही नित,
मोतियों की हाट औ' चिनगारियों का एक मेला।
2. भरे सुमन बिखरे अक्षत सित,
धूप अर्घ्य नैवेद्य अपरिमित,
तम में सब होंगे अंतर्हित,
सब की अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो।
यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो।
हिंदी साहित्य के सांस्कृतिक काव्योत्थान (छायावादी युग) के समाप्त होते-होते प्रथम श्रेणी के दो अन्य कवि—बच्चन और दिनकर—इसे अपने नवीन काव्य-सौरभ से सुरक्षित करने लगे थे। कई दृष्टियों से इन दोनों कवियों में बहुत बड़ा विभेद भी हैं। कुछ समीक्षकों ने इनमें से एक दूसरे के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, और तब उन्हें उक्त दोनों में से एक तोहीन करना भी आवश्यक जान पड़ा है। पर मुझे इन दोनों के काव्यों में उतना बड़ा भेद नहीं दिखाई देता कि उनकी चर्चा दो विरोधी शिविरों में रखकर की जाएँ। जहाँ तक काव्य और अभिव्यंजना का संबंध है छायावादी कवियों की समता का परिष्कार और कलात्मकता कदाचित् इन दोनों में नहीं है। ये दोनों ही प्रतिवर्तन या उतार के कवि हैं। बच्चन की रचनाओं में वैयक्तिक वेदना का अधिक-प्रबल उभार दिखाई देता है। दिनकर जी की कृतियों में उसी भावावेश को सामाजिक परिधान दे दिया गया है किंतु स्पष्ट दार्शनिकता और जीवन-लक्ष्य के संबंध में दोनों एक से ही अनिर्णीत हैं—या यह कहें कि दोनों किसी विशिष्ट जीवन-साधना के अभाव में एक से ही परिक्लांत हैं। दोनों की रचनाओं का एक उदाहरण दिया जाता है—
जीवन-मरघट पर अपने सब
अरमानों की कर होली
चला राह में रोदन करता
चिता-राख से भर झोली।
शीश हिला कर दुनिया बोली,
पृथ्वी पर हा चुका बहुत यह
इतने मत संतप्त बनो (बच्चन : ‘आकुल अंतर’)
हाय रे मानव, नियति का दास!
हाय रे मनुपुत्र, अपना आप ही उपहास।
प्रकृति की प्रच्छन्नता को जीत,
सिंधु से आकाश तक सब को किए भयभीत।
सृष्टि को निज बुद्ध से करता हुआ परिमेय,
चीरता परमाणु की सत्ता असीम, अजेय!
बुद्धि के पवमान में उड़ता हुआ असहाय,
जा रहा तू किस दिशा की ओर हो निरुपाय। (दिनकर : 'कुरुक्षेत्र')
इन्हीं भावात्मक रचनाओं के सिर पर जब हम नए प्रयोगवादियों के प्रयोगों को देखते हैं तब सहसा प्रश्न होता है कि हिंदी कविता अपनी रचनात्मक दिशा का इतनी शीघ्रता से परित्याग कर दिग्भ्रांत क्यों होती जा रही है। प्रयोक्ताओं को क्या पड़ी है कि वे हिंद की इस नवनिर्मित परंपरा का मूलोच्छेद कर एकदम एक नया वैशिष्ट्य प्राप्त कर लेना चाहते हैं। नए प्रयोगवादी अपने को अन्वेषक कहते हैं, पर नई हिंदी में अभी इस अबाध अन्वेषण के लिए—इस बेतहशा दौड़ के लिए—स्थिति और अवसर ही कहाँ हैं? नवीन कविता समृद्धि की उस सीमा पर नहीं पहुँची है जहाँ से विघटन का कार्य आरंभ हो के। इसलिए अच्छा तो यह होता कि हमारे प्रयोगवादी हिंदी भाषा और उसकी काव्य परंपरा को परिपुष्ट करते—उसे और आगे बढ़ने का अवसर देते। यदि अन्वेषण ही करना है तो अन्वेषण के लिए भी स्थान है—नई विचारधाराओं और नए जीवन-दर्शन का अन्वेषण ही नहीं उनको जीवन में उतारने के प्रयोग पर ऐसा दिखाई देता है कि प्रयोगवादी अभी से ऊब उठे हैं, समाज साहित्य और उनको समस्त सांस्कृतिक आधारों से। तभी तो इतनी उतावली के साथ सब की भर्त्सना और सब का परिहास करने की शून्यगामी योजना उन्होंने अपना ली है। संभव है मध्यवर्ग का सांकृतिक सत्ता के समाप्त होने-नए निर्माण में उस सत्ता को रंच मात्र भी उपयोगिता न रह जाने का इज़हार किया जा रहा हो। पर प्रश्न यह है कि शून्य का स्तवन करने वाली काव्य सृष्टि, किस वर्ग का कल्याण करने का उद्देश्य रखती है?
प्रयोगवादी रचनाओं के कुछ उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। पहली कविता आर्थिक साम्य या वैषम्य से संबंध रखती है:—
इतने प्राण, इतने हाथ, इतनी बुद्धि!
इतना ज्ञान, संस्कृति और अन्तः शुद्धि!
इतना दिव्य, इतना भव्य, इतनी शक्ति
यह सौंदर्य, वह वैचित्र्य, ईश्वरभक्ति।
इतना काव्य, इतने शब्द, इतने छंद
जितना ढोंग जितना भोग है निबंध,
इतना गूढ़, इतना गाढ़, सुंदर जाल।
केवल एक जलता सत्य देते टाल। (तारसप्तक, पृष्ठ 16)
'पहली पंक्ति में 'प्राण' और 'बुद्धि' के बीच में 'हाथ' किस बारीकी से बैठा है! 'ज्ञान', 'संस्कृति' और 'अंतः शुद्धि' जैसे शब्द दूसरी पंक्ति में आए हैं, जिनमें से एक-एक का अर्थ जान लेने में ही एक पूरे जीवन को आवश्यकता है! जब तक अर्थ ग्रहण नहीं कर लेते तब तक भाव का अनुभव ही क्या करेंगे (इसलिए अभी से अर्थ-सिद्धि में लग जाना चाहिए)। तीसरी पंक्ति में 'दिव्य' और 'भव्य' जैसे विशेषण किस विशेष्य के लिए हैं—भव्य और दिव्य कौन सी वस्तुएँ हैं, इसका पता नहीं बताया गया। शायद 'इतना' ही दिव्य और भव्य है। चौथी पंक्ति में 'सौंदर्य', 'वैचित्र्य और 'ईश्वरभक्ति' का समन्वय किया गया है, मानो एक ही पिता के ये दो पुत्र और एक कन्या हो! पाँचवीं और छठी पंक्तियाँ एक दूसरे की अनुलोम या प्रतिलोम हैं क्योंकि एक में 'इतना' 'इतना' और दूसरी में 'जितना' 'जितना' आया है। जान पड़ता है कि कवि अपने 'काव्य', 'शब्द' और 'छंद' को ही ढोंग और भोग की उपाधि दे रहा है। कवि की इस अंतः-शुद्धि का कारण क्या है—'ईश्वरभक्ति' या कुछ और? सातवीं पंक्ति में कोई जाल है—गूढ़, गाढ़ और सुंदर। कोई जाल-विशेषज्ञ ही बता सकता है कि सब से सुंदर जाल क्या ऐसा ही हुआ करता है और क्या वह सुंदर जाल किसी जलते (या उबलते) सत्य को टालने के काम भी आ सकता है? प्रश्न यह भी हैं कि इन पंक्तियों का आर्थिक साम्य या वैषम्य से क्या संबंध है? इसका एक ही उत्तर ढूँढ़कर निकाला जा सका है। वह यह कि जो कोई इन पंक्तियों को पढ़ेगा वही साम्यवादी होगा और बिना पढ़े वैषम्य का शिकार रहेगा— पूँजीवादी कहलाएगा!
एक कविता, कविता के संबंध में भी लिखी गई है:—
कविता क्या है? कहते हैं जीवन का दर्शन है आलोचन।
वह कूड़ा जो ढँक लेता है, बचे-खुचे पत्रों में के स्थल।
कविता क्या है? स्वप्न-श्वास है उन्मन, कोमल।
जो न समझ में आता कवि के भी ऐसा है। वह मूर्खपन।
कविता क्या है? आदिम कवि की दृग झारी से बरसा वारी।
वे पक्तियाँ जो कि गद्य हैं कहला सकती नहीं बिचारी। ('तारसप्तक', पृष्ठ 57)
कविता के संबंध में यह धारणा एक प्रयोगवादी कवि को क्यों हुई? माना कि उसके आसपास ऐसी रचनाओं का भी ढेर लगा है, जो कूड़ा-करकट कही जा सकती हैं, जिनका अर्थ समझना उनके रचयिताओं के लिए भी आसान नहीं है, और साथ ही जो, प्रयत्न करने पर भी, किसी प्रकार गद्य नहीं कहला सकतीं (क्योंकि वे पद्य में लिखी गई हैं) पर प्रश्न यह है कि क्या इस कविता में आत्माभिव्यंजना का तत्व बिल्कुल नहीं है—आत्मानुभूति का नितांत अभाव है? क्या लेखक के मस्तिष्क के किसी अज्ञात कोने में अपनी रचनाओं का संस्कार नहीं रहा है? इस प्रश्न का उत्तर भी कोई मनः विशेषज्ञ ही दे सकता है!
और अंत में हम स्वयं अज्ञेय जी की 'जनाह वान' कविता लेते हैं (तारसप्तक, पृष्ठ 77) जिसमें वीर-भाव को जगाने की चेष्टा की गई है:—
ठहर ठहर आततायी, ज़रा सुन ले,
मेरे क्रुद्ध वीर्य की पुकार आज सुन जा,
रागातीत, दर्पस्फीत, अतल, अतुलनीय,
मेरी अवहेलना की टक्कर सहार ले,
क्षण भर स्थिर खड़ा रह ले—
मेरे दृढ़ पौरुष की एक चोट सह ले,
नूतन प्रचंडतर स्वर से
आततायी आज तुझ को पुकार रहा मैं।
रणोद्यत दुर्निवार ललकार रहा मैं।
कौन हूँ मैं?
तेरा दीन दुःखी पददलित पराजित
आज जो कि क्रुद्ध सर्प से अतीत को जगा
'मैं' से 'हम' हो गया।
'आततायी' शायद कुछ दूर है, और क्रमशः दूर होता जा रहा है! वह दूसरी दिशा में जा रहा है। कोई व्यक्ति उसे रोकता है, रुकने को कहता है। वह उसे अपने दिल का गुबार सुनाना चाहता है। पहली पंक्ति में वह आततायी को ठहराता है। और ठहरा कर कहता है 'ज़रा सुन लो।' यहाँ 'ज़रा' शब्द का प्रयोजन क्या है? क्या आततायी से 'दो मिनट' 'एक बात’ सुनने की प्रार्थना की जा रही है? क्या सामूहिक आह्वान या ललकार ऐसी ही होती है? और दूसरी पंक्ति 'मेरे क्रुद्ध वीर्य की पुकार आज सुन जा' में 'आज' और 'सुन जा' की विशेषता क्या है? क्या यहाँ भी कोई मिन्नत है कि कृपा कर 'आज पुकार सुनकर चले जाना?' तीसरी और चौथी पंक्तियों में टक्कर संभालने की अपेक्षा 'अवहेलना' का मनोवैज्ञानिक स्वरूप स्पष्ट करने में अधिक समय ले लिया गया है—रागातीत, दर्पस्फीत, अतल, अतुलनीय अवहेलना'—इसके बाद टक्कर संभालने को कुछ रह नहीं जाता! 'अवहेलना' का 'टक्कर' भी एक अद्भुत पदार्थ है। 'अवहेलना' स्वयं ही टक्कर बचाती है, फिर उसकी टक्कर संभालने में कौन सी बहादुरी होगी? पाँचवीं और छठी पंक्तियों में पहली और दूरी पंक्तियों का पुनरावृत्ति सी है 'क्रुद्ध वीर्य' और 'दृढ़ पौरुष' में केवल शाब्दिक अंतर है।
सातवीं, आठवीं और नवीं पंक्ति काफ़ी ज़ोरदार हैं परंतु जो कुछ भी उनका ज़ोर था, उसे नीचे की चार पंक्तियों ने समाप्त कर दिया है। किसी व्यक्ति को ललकार कर फिर उसी से अपनी दीनता का वर्णन करना अपने को 'तेरा दीन दुःखो पददलित, पराजित' कहना मनोविश्लेषणात्मक तथ्य हो सकता है, परंतु भावात्मक सत्य नहीं। 'उलझी संवेदना' का यह कविता एक अच्छा उदाहरण है (उलझी संवेदना, जिसकी चर्चा अज्ञेय जी ने प्रयोगवादी कविता की व्याख्या करते हुए की है)।
मैं यह नहीं कहता कि इन प्रयोगवादी रचनाओं का कोई मूल्य ही नहीं है; संभव है ये रचनाएँ किसी नए और श्रेष्ठतर कवि के आगमन का हेतु बनें, परंतु वर्तमान रूप में वे जैसी हैं, उनमें साहित्यिक परिष्कार की बड़ी आवश्यकता है।
प्रयोगवादी 'शृंगार’ का एक उदाहरण देकर यह प्रसंग समाप्त करूँगा।
मैं वैसा का वैसा ही रह गया सोचता
पिछली बातें;
दूज-कोर-से उस टुकड़े पर
तिरने लगीं तुम्हारी सब लज्जित तसवीरें!
सेज सुनहली,
कसे हुए बंधन में चूड़ी का झर जाना।
निकल गईं सपने जैसी वे रातें
याद दिलाने रहा सुहाग-भरा यह टुकड़ा। ('चूड़ी का टुकड़ा' तारसप्तक, पृष्ठ 42)
महाराज अज का 'सुलोचना' के लिए विलाप कवि कालिदास ने कराया था। परंतु उनको भी दृष्टि इतनी महीन चीज़ों की ओर नहीं गई—'कसे हुए बंधन में चूड़ी का झर जाना।’ कदाचित् कालिदास में थोड़ी सी लोक-मर्यादा बच रही थी। इसी से वे प्रयोगवादी कवियों की बराबरी पर नहीं रखे जा सकते। प्रयोगवादी इस विषय में उनसे बाज़ी मार ले गए हैं!
अधिक उदाहरणों की आवश्यकता नहीं। इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि हिंदी काव्य की ऊपर दिखाई परंपरा से टूट कर अलग होने का प्रयोगवादियों का प्रयत्न न तो उनके लिए और न हिंदी कविता के लिए श्रेयस्कर है। नवीनता लाइए पर अपनी विरासत से मुँह न मोड़िए। उत्तराधिकार न छोड़िए। अन्वेषण के लिए—अन्वेषण ही नहीं जीवन संबंधी धारणा और साधनों के लिए, प्रचुर स्थान है, उस ओर आगे बढ़िए। अपने प्रति (अपनी अनुभूतियों के प्रति) काव्य के प्रति और समय और समाज के प्रति उत्तरदायित्व को भूल कर प्रयोग नहीं किए जा सकते। उन प्रयोगों का अर्थ होगा शून्य पर दीवाल खड़ी करना।
प्रयोगवादी काव्य की इस अंधाधुंध में सब से बड़ी बुराई यह हुई कि काव्य और कला संबंधी स्थिर पैमानों पर किसी का विश्वास नहीं रहा और सुमित्रानंदन पंत जैसे निसर्ग-सिद्ध कवि भी कविता का पल्ला छोड़कर वादों का राग अलापने लगे। पंत जी का काव्यक्षेत्र छोड़कर वादी क्षेत्रों में चला जाना कदाचित् हिंदी साहित्य के इस युग की सबसे बड़ो दुर्घटना है। परंतु उससे भी अधिक खेदजनक बात यह हुई कि समीक्षा के क्षेत्र में काव्य-संबंधी विचार परंपरा सुरक्षित न रह सकी, काव्य और वाद को एक ही श्रेणी में मिला दिया गया। इसलिए आज की समीक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व यह है कि इन दोनों का पृथक्करण करके काव्य की अपनी सत्ता की पूर्ण प्रतिष्ठा को जाए। यह कार्य अभी तो असंभव सा दीखता है, परंतु आशा खोने के पक्ष में हम नहीं हैं। हिंदी के समस्त कलाकार—और प्रयोगवादी कलाकार भी उनमें सम्मलित हैं—यदि सब कुछ छोड़कर केवल एक बात में एकमत हो जाएँ, यदि वे केवल इतना मान लें कि वे हिंदी साहित्य के कवि और कलाकार हैं और उनका कार्य हिंदी की काव्य-सृष्टि की रक्षा और विकास करना है, तो दूसरे समस्त प्रश्न आसानी से हल हो जाएँगे और तब हिंदी कविता—और प्रयोगवादी कविता भी—अपने अस्तित्व के लिए परमुखापेक्षिणी न रहेगी, वह अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी।
- पुस्तक : आधुनिक साहित्य (पृष्ठ 15)
- रचनाकार : नंददुलारे वाजपेयी
- प्रकाशन : भारती भंडार लीडर प्रेस
- संस्करण : 2007
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.