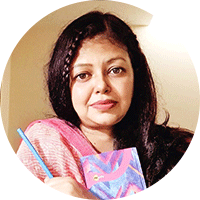तो वह एक सुखी परिवार था, हर लिहाज़ से सुखी। सुदामा प्रसाद, एम.ए.बी.एल. अपने ज़माने के मुँहफट वकील। इस ज़माने तक ज़बान सही-सलामत आबाद थी। हालाँकि धार कुंध हो चली थी...वक़्त की मार। बहरहाल वे बासठ की उम्र में हटे-कट्ठे थे। पंजा लड़ाने में आज की तारीख़ में, वे एक तरफ़...और दोनों बेटे और तीन पोते एक तरफ़ हों, तब भी उनका पंजा ही ऊपर रहे, ऐसा हौसला। वैसे ये कोई ख़ास हैरत-अँग्रेज़ बात न हुई। आजकल के बेटों-पोतों में ताक़त होती ही कितनी है। नए चलन में ताक़त का केंद्र शरीर की जगह दिमाग़ हुआ करता है। दिमाग़ मज़बूत और शरीर पिलपिला। सुदामा प्रसाद अपने ओरिजिनल दाँतों से ईख की मोटी लग्गी सटाक से छीलते और पोतों को छोटी-छोटी गुल्लियाँ बनाकर देते, ताकि रस चूसने में सहूलियत हो। उनकी इस जवाँमर्दी से पोते किलकते और बेटों के मसूरों में टीस उठती। ठहाके वग़ैरह लगाने में वे परहेज़ नहीं करते और जितनी हसरत से क्रिकेट मैच देखा करते, दूरदर्शन धारावाहिकों के साथ भी वही सलूक होता। शहर में जब केबल के कनेक्शन का फ़ैशन आरंभावस्था में था, तभी उन्होंने एक पतला सफ़ेद तार अपने घर में खिंचवा लिया था। और 'स्टारप्लस' उनका पसंदीदा चैनल था। सारतः वे स्वस्थ थे, मस्त थे और जीवन को चुस्कियों में पीते हुए भरपूर मज़े से जी रहे थे।
दीवानबाई क़िस्से की तरह चंचल थी। छलिया सुपारी की शौक़ीन। उसके होंठ के पोर ताज़े पान की लाली से सिले मिलते और आँखों के नीचे-ऊपर काजल होता था। एड़ियों में आलते की लाली और पल्लू के आख़िरी छोर में चाभियों का काल्पनिक गुच्छा! दीवानबाई के हाथों में आज भी घर की दीवानी मौजूद थी।
दीवानबाई कहानी की तरह गंभीर थी। उसकी भौंहों के बीचों-बीच चवन्नी बराबर लाल सिंदूर की बिंदी रहती थी जो दिन ढलते-ढलते थोड़ा ऊपर की तरफ़ तिरछी लिप जाया करती थी। अपनी भौंहों के उठान-गिरान की तरह ही वह घर के पैबंद और मख़मल वाले दोनों दिनों की साक्षी थी। सुदामा प्रसाद के साथ जब उसकी भाँवरें पड़ीं, तब दीवानबाई बमुश्किल सतरह-अठारह की रही होगी। हालाँकि उस ज़माने में वर या वधू की रज़ा या नामर्ज़ी जैसे सवालों का कोई रिवाज नहीं हुआ करता था। फिर भी देखें तो दीवानबाई की नामर्ज़ी की घोर उपेक्षा करके उनका कन्यादान किया गया था। और इधर सुदामा प्रसाद के घर की लचर हालत चरमावस्था पर थी। सुदामा प्रसाद क़ानून की दाँवपेंच से भरी ख़र्चीली पढ़ाई पढ़ रहे थे और उनके स्वर्गीय पिता की धरी-छोड़ी पूँजी से उनकी पढ़ाई का ख़र्च चल रहा था—लोग ऐसा जानते थे। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। सुदामा प्रसाद अपने माँ-बाप के बुढ़ापे की इकलौती संतान थे। उनके पिता मरे थे ज़रूर, पर बिना कुछ छोड़े। उस ज़माने में शरीफ़ जाति की औरतें दिन-दहाड़े बाहरी काम नहीं किया करती थीं। तो उनकी उम्र-दराज़ कुलीन माँ रात के अँधेरे में मुँह ढाँपकर रेलगाड़ियों में मूँगफली, भूँजा आदि-आदि बेचा करती थीं और दिन के उजाले में बचे-खुचे गहने और धराऊँ बरतन। इन दुबले-पतले पैसों से उनकी गाड़ी खिंचती थी। निम्न मध्यमवर्ग की हक़ीक़तें कभी-कभी बड़ी चौंकाऊ हुआ करती हैं। दीवानबाई ब्याह के बाद जब इस हक़ीक़त से रू-ब-रू हुई तो उसकी चेतना सुन्न रह गई। पर जल्दी ही वह इस सदमे से उबर गई क्योंकि इससे बड़ा सदमा सामने था। एक रात, इसी तरह गाड़ियों से चढ़ने-उतरने वाले खेल में ट्रेन से उतरते वक़्त सुदामा प्रसाद की माँ के कुलीन अभ्यस्त पैर साड़ियों में उलझ गए और गाड़ी एक सिसकी लेती हुई खच...खच...खचाक से रुकी और दो मिनट बाद फिर चल पड़ी। बिनबिकी मूँगफली, जो प्लेटफ़ॉर्म और पटरियों पर छितर गई थीं उनसे उस रात कुत्तों का अच्छा भोज हुआ, पर तेरह दिन बाद सगे-संबंधियों और ब्राह्मणों को जिमाने के लिए एक छोटे भोज का प्रबंध अच्छा न हो सका। माँ की दुआ, वक़्त का फेर, दीवानबाई की क़िस्मत...जो कहें घटना के तुरंत बाद सुदामा प्रसाद को एक राशन-पानी की दुकान पर छोटी-मोटी नौकरी मिल गई। दीवानबाई ने ख़ुशहाल, बचपन और सुस्त जवानी के कौमार्यावस्था वाले दिनों के अपने सीखे हुनरों को चमकाया और कुछ सादे कपड़े उसके घर आने लगे और उस घर से जाते वक़्त उन कपड़ों पर क़िस्म-क़िस्म के फूल पत्ते-डालियाँ कढ़े होते। क़शीदे के पैसों से दाल-नमक का जुगाड़ हुआ और बनियागिरी के पैसों से पढ़ाई पूरी हुई। फिर शुरू हुई वकालत और दिन पलट गए।
अब तक की कहानी से एक सवाल बनता है। ब्याह में दीवानबाई की नामर्ज़ी थी, ऐसा क्यों? इसके बारे में थोड़ा ठहरकर। अभी सुदामा प्रसाद और दीवानबाई के कुल में उत्पन्न दोनों बेटों की बात। मूँगफली वाली बुढ़िया की तर्ज़ पर ही दीवानबाई को भी अपेक्षाकृत अधिक उम्र में मातृत्व सुख मिला। हालाँकि इन दो औरतों के इस संयोग की पृष्ठभूमि निहायत अलग थी। पहली जहाँ इच्छा, आवश्यकता और प्रयास तीनों की उपस्थिति में भी उम्र ढलने पर माँ बन पाई थी, वहीं दीवानबाई के मामले में इच्छा तत्त्व का घोर अभाव था। फिर भी वह सास जितनी विलंब का शिकार होने से बच गई और ब्याह के दस साल बाद उसकी गोद में पहला बेटा आया। फिर दूसरा। दोनों बेटे ज़माने के लिहाज़ से अपेक्षाकृत सपूत निकाले। बहुओं के स्वभाव में चंचलता, स्वतंत्रता और उग्रता का हलका पुट था ज़रूर पर घर इस तरह सुदामा प्रसाद और दीवानबाई के शिकंजे में जकड़ा था कि उन्होंने अपनी इन भावनाओं को फ़िलहाल सुप्तावस्था में रहने देना ही श्रेयस्कर मान लिया था। बड़े बेटे के एक लड़का था और छोटे के दो। सुदामा प्रसाद इस बेदाग़ पुत्रों की नस्ल से गदगद थे और संतुष्टि थी कि अपने ख़ानदान को कन्या के ग्रहण से अभी तक साबुत बचा लाए थे वे। बेटे पढ़ने-लिखने में कोई ख़ास करिश्मा करते नहीं नज़र आए थे तो उन्होंने अपने आरंभिक पेशे की ओर रुख़ किया। अब बड़े बेटे का एक काम-चलाऊ जनरल स्टोर था और छोटे का एस.टी.डी. बूथ कम फ़ैक्स-ज़िरॉक्स सेंटर। पोते अभी दूध चावल के दाँत के बीच की उम्र में थे।
समय अपनी सम गति से चल रहा था, जब अचानक ये घटना घटी। इस घटना के प्रभाव के सूत्र को समझने के लिए बीच में छूट गए उस प्रश्न का उत्तर आवश्यक है। सन् उन्नीस सौ तिरसठ-बासठ। वह ज़माना, जब दीवानबाई उलटी पल्ला साड़ी पहने और रिबन से कसकर बाँधी गई दो मुड़ी-मुड़ी चोटियों को कानों पर लटकाते, शहर के इकलौते वीमेंस कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। तीन मकान छोड़कर चौथे मकान के लगभग हमउम्र पर संपन्न विजातीय लड़के से उनका प्रेम हुआ। तत्कालीन अर्थों वाला प्रेम, और प्रेम होने की स्थिति और उसे करने का तरीक़ा भी वही, जो उस ज़माने में ख़ूब चला हुआ था। पहले छत से देखा-देखी, फिर गली में कभी आते-कभी जाते नज़रों का टकराना, या फिर मेले में, या फिर कॉलेज के बाहर...आदि-आदि। संवाद अदायगी के नाम पर एक रोज़ कॉलेज के बाहर बस नाम वग़ैरह का आदान-प्रदान हुआ था। बाक़ी समय बस मूक संदेशों का ही सहारा था। लेकिन ऐन वक़्त पर दीवानबाई के पिता खलनायक के गेट-अप में मंच पर नमूदार हुए। वे पेशे से वकील थे लिहाज़ा लॉ-कॉलेज में भी पढ़ते थे। और वहीं से उन्होंने एक ज़हीन पर आर्थिक मोर्चे पर पस्त हाल जवाँई ढूँढ़ा अपने लिए। फ़ायदा दोहरा। वर के सुयोग्य निकलने की गारंटी थी और कमज़ोर हैसियत के पितृहीन वर को अपनी हैसियत की धाक दिखाकर मुक्त में कन्यादान निबटाए जा सकने का मौक़ा भी था। दीवानबाई से न मर्ज़ी पूछी गई ना उसने बताई। बस ज़िबह होने के लिए अपनी गरदन आगे बढ़ा दी। दूल्हा प्रसन्न, प्रेमी अवाक।
दीवानबाई अग्नि के फेरे लेने के बाद सरद गई। ठंडी सिल पर गृहस्थी की शुरुआत हुई। आरंभ के दिन तो ताज़े-ताज़े बहूपने को सँभालने में गुज़र गए और ट्रेन वाले हादसे में सुदामा प्रसाद की माँ के गुज़रते ही दीवानबाई एकदम से सख़्तजान बन गई। वह दिन-भर खटने लगी और अपने आपको काम में लसेड़े रही। पर किसके लिए? किसी और के लिए नहीं। शायद अपने लिए। ताकि यादों से और उन अँधेरों के सपनों से पीछा छुड़ाया जा सके। लेकिन अगर ऐसा संभव हुआ होता तो दुनिया की शायद हर प्रेम कहानी अधूरी रह जाती। कशीदा काढ़ते काढ़ते उसी उँगलियों में सूई चुभ जाती कभी, तो आह उस तीन घर छोड़कर चौथे घर वाले के नाम की ही निकलती थी। जब कपड़े देने वाले, वापस उन्हें ले जाने लगते और दीवानबाई की मुट्ठी सिक्के और ख़ुदरा रुपयों से भरी होती, तब अनायास उसका दिल चहकता—इन पैसों से उस मंगल मूरत, साँवली सूरत के लिए क्या ख़रीदा जाए। पर उसी तेज़ी से उसका दिल बैठ भी जाता और उसके होंठ सूख जाते वर्तमान के ताप से। लोगों ने कहा दीवानबाई की मेहनत रंग लाई...उसका पति वकील बन गया। दीवानबाई ने सुना उसका प्रेमी दिन-रात मेहनत कर रहा है...बाप के बाद उसका कारोबार बख़ूबी सँभाल लिया है उसने। तो दोनों अपने प्रेम की धार छिपाने के लिए और क़िस्मत की मार को भुलाने के लिए ताबड़-तोड़ मेहनत किए जा रहे थे! दीवानबाई जब पंद्रह-बीस मिनट रिक्शे की सवारी कर अपने मायके पहुँचती तो शाम के लुकझुके में उसकी आँखें तीन घर पार वाली छत से चिपक जातीं। कहीं...कुछ...दिखे। शक्ल न...आकृति सही। एक बार दीवानबाई का बहुत टूट-फूटकर अम्मा-पापा-मामा बोलनेवाला डेढ़ साल का बेटा जब उस घर से दिन-दहाड़े कुछ फूल चुरा लाया था, तब दीवानबाई ने जमकर उसे पीटा था। फूल चुराने के लिए नहीं...बल्कि इसलिए कि दीवानबाई के लाख माँगने पर भी बच्चा उसे वे फूल देने को तैयार न था। बच्चे ने मार खा ली, पर मुट्ठी नहीं खोली। उसके सो चुकने पर दीवानबाई ने ढीली पड़ चुकी मुट्ठी की उँगलियाँ सीधी की और पसीने से नहाई बेली की तीन कलियाँ वहाँ से निकालीं। उन तीन मुरझाई कलियों को अपनी हथेली पर खिलाया, आँसुओं से धो-धोकर। दीवानबाई जब उन कलियों को भरपूर प्यार कर चुकने के बाद अपने आँचल में बाँध, सहेज लेने चली, तब बेली की एक नन्हीं पंखुड़ी उसके निचले होंठ के पोर से चिपकी रह गई। दीवानबाई की जवान आँखों के सामने उसके प्रेमी का घर बसा। उसकी बाल-बच्चेदार, लँदी-फँदी आँखों के सामने उसके प्रेमी के घर किलकारियाँ गूँजी। उसके चलनी के उस पार से चाँद और सुदामा प्रसाद को बारी-बारी से देखती आँखों के सामने उसका प्रेमी विधुर हुआ। उसके दूर की चीज़ें धुँधली दिखाई पड़ने वाली आँखों के सामने उसके प्रेमी के बाल सफ़ेद हुए और अब...थोड़ा भी ज़ोर देकर या लगातार कुछ देखने पर पनिया जाने वाली आँखों के सामने उसके प्रेमी के दोनों बच्चे अपने परिवार समेत, कार-दुर्घटना में मारे गए।
छोटा शहर था। क़स्बा कहें, बात सीझते गोश्त की ख़ुश्बू की तरह फैलती थी। शहर का एक इज़्ज़तदार भला आदमी और ऐसी विपदा! श्याम! श्याम! स्त्रियों की आँखें भर आई थीं और पुरुषों ने लंबी आँहें लीं। सुदामा प्रसाद शाम की तफ़री से घर को लौटे और उनके बदहवास होंठों पर ये ख़बर थी। घर में टी.वी. पर अंताक्षरी देखने की तैयारी थी। सब अपना-अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। बस उनकी ही प्रतीक्षा थी। दीवानबाई चश्मा चढ़ाकर जल्दी-जल्दी सुबह के पाले के चावल बीन रही थी। यही दृश्य था जब मंच पर सुदामा प्रसाद ने आँहें भरते हुए वो नाटकीय संवाद प्रेषित किया। सभी लोग थोड़ा-थोड़ा होंठ खोलकर हक्के-बक्के रह गए। पर सबसे गहरा भाव दीवानबाई के चेहरे पर उभरा। बारीक़ नज़रों से जायज़ा लें तो उसके चेहरे पर रेशमी डोरे जैसी महीन कई छोटी-छोटी रेखाएँ उभरी थीं। दीवानबाई के आगे के सारे कंकड़ और चावल एक रंग के हो गए। ये तो भेद के मिटने की शुरुआत थी। इसके आगे अपना-पराया, जायज़-नाजायज़, उचित-अनुचित, सही-ग़लत...सबके भेद एक-एक कर मिटने लगे उसके आगे से। वह चुपचाप उठकर अपने बिस्तर तक गई। छप्पन साल की उम्र में दो जवान बेटों की माँ दीवानबाई चित्त लेटी थीं। उसकी पलकें पथराई-सी अँधेरे में टँगी थीं। उन पर एक नवजात माँ के तुतले दूध की बूँदें फैल रही थीं। ये वे बूदें थीं, जिन्हें उसकी युवावस्था ने सँभालकर रखा था अपने पहले प्रेमी से उत्पन्न संतानों के स्वागत के लिए और जिन्हें वह वृद्धावस्था की दहलीज़ पर लुटा रही थी उन संतानों को आख़िरी विदाई देने के लिए। उसके गले से एक बेसुध चीत्कार निकली और हिचकी और आँसू गड्डमड्ड पड़ गए। परिवार उसका, इस ख़बर के बाद धीमी आवाज़ में टी.वी. देख रहा था। लिहाज़ा दीवानबाई का विलाप उन्हें उसके कमरे तक खींच लाया। बड़े बेटे ने दीवानबाई को कसकर थामा... दीवानबाई तो भेद मिटाने की मुहिम पर थी... उचित-अनुचित, सही-ग़लत। ऐसी रुलाई, ऐसी चीख़...कौन कहेगा कि जो बच्चे मरे, वे बिना माँ के थे। दीवानबाई के माथे पर बहुओं ने ठंडा तेल चपोड़ा। तलुवों की मालिश की। पानी पिलाया और उसे अच्छी तरह ढंक-दाब कर सुलाया...दीवानबाई अर्धचेतना में रातभर चौंकती रही।
सूरज चैतन्य कर गया। आगे रात की आधी-अधूरी कड़ियों वाली कहानी थी। गड्डमड्ड-सी स्मृतियाँ थीं। उसने चिहुँककर अपनी साड़ी का अगला हिस्सा टटोला...कलेजे पर वाला। भीतर के कपड़ों का सूखापन परखा। वहाँ बूँदों की सिम-सिम स्मृति पसरी थी। मतलब? रात भर!
घर गंभीर था। लोग विचलित से थे और तीनों बच्चे आतंकित थे...दीवानबाई से। उसने दरवाज़े की ओट से अपने कमरे में झाँकते सबसे छोटे पोते को इशारे से अपने पास बुलाया और आँचल में दुबका लिया। बच्चे ने अपनी नन्हीं उँगली उसकी नाभि में फँसा दी और दीवानबाई ने आँखें बंद कर लीं। उसकी आँखों से फिर हाहाकार करते आँसू टपकते थे। उसने बच्चे को कसकर चिपकाया अपने से और आँसू पोंछकर अपने आपको मज़बूत बनाया और वापस अपनी दिनचर्या में डूबने की कोशिश की।
रात हुई। सब सो चुके थे। दीवानबाई आँखें खोले लेटी थी। सुदामा प्रसाद ने उसकी ओर करवट फेरी तो नाइट बल्ब की शांत नीली रौशनी में उसे ऐसे जागता हुआ देखकर हड़बड़ा गए। वे धड़फड़ी में उठे और दीवानबाई के ठंडे माथे पर तलहथी रखी अपनी। दीवानबाई ने पुतलियाँ उनकी ओर फेरी, उसने नीले धुँधलके में उस इंसान को देखने की कोशिश की जो उसका सबकुछ था... जो उसका कुछ नहीं था। कहाँ कमी रही गई इस रिश्ते में—दीवानबाई के भीतर तेज़ी से यह सवाल उठा...कहाँ तीव्र आकर्षण था उस रिश्ते में?... उसी जगह से पहले सवाल के जवाब में दूसरा सवाल उठा। सुदामा प्रसाद ने उसे खींचकर अपनी बाँहों में समेट लिया। दीवानबाई के ऊपर एक ठंडी परत चढ़ गई और ठीक उसी वक़्त उसने महसूस किया कि उसके भीतर नादानी वाली उम्र की वही तपिश अभी तक बाक़ी थी, जिसे मायके की दहलीज़ पर चुनवा आई थी वह बरसों पहले... कभी।
पर दीवानबाई और सुदामा प्रसाद की गृहस्थी की नींव ऐसी कच्ची थोड़े न थी! माना कि आधार उनके संबंधों का सीली हुई ज़मीन पर रखा गया था। पर ज़मीन सीली हुई थी, दरकी हुई तो नहीं! दीवानबाई फिर घर-संसार के छोटे-छोटे कामों में उलझ-पुलझ गई थी। सुदामा प्रसाद और बेटों को चाँक से नीम का उबला पानी पिलवाना, पोतों की उँगलियाँ पकड़कर सड़क पार करवाना, बहुओं के लिए फेरीवाले से मोल-तोल पर चूड़ियाँ ख़रीदना, सूखे धनिया के स्वस्थ मोटे-गोटे को सिल पर दररना, चावल और कंकड़ को एक-दूसरे से अलग करना... दीवानाई वक़्त की रफ़्तार से क़दम साधकर चलना चाहती थी, पर अपने साथ छल करने के जुनून में कभी वक़्त से आगे निकल जाती। कभी वक़्त को पीछे छोड़ देता। और एक रोज़ वक़्त उसके साथ छल कर गया...घटना के लगभग महीने भर बाद दीवानबाई छोटे पोते को साथ लिए मायके गई। मायके में सुख-दुख, हारी-बीमारी, हर तरह के हिस्सों की गाँठें खुल गईं। गप्प की बुनावट जब महीन और तराशी हुई सधने लगी, तभी किसी का ध्यान उचटा। और उस 'किसी' को यह ध्यान आया कि नन्हा मेहमान नदारद है। पल में गप्प-गोष्ठी बिखर गई और खोज मच गई। अब उसे क्या कहें कि दीवानबाई के आँचल में बेली के कलियों की तीन आत्माएँ सुगबुगाईं और उसके नथुने ताज़ी सुगंध से भर गए। सुध-बुध खोई पोते की तलाश में वह सीधे जाकर वहीं खड़ी हो गई, जहाँ पोता मौजूद था। इस बार पौधे बेली के नहीं थे...हरसिंगार की छतनार छाँह थी। अल-सुबह के चू गए हरसिंगार के फूल थे ज़मीन पर, जिन्हें नन्हा देवदूत मस्ती से बैठा चुने जा रहा था और उसे देखती दो मुग्ध आँखें थीं...जहाँ-तहाँ बेदर्दी से सफ़ेद हो चुके केरा थे, एक दुबली काया थी, लहराती उज्ज्वल धोती की फहक थी, बेदाग़ सफ़ेद कुर्ता था...और नफ़ासत भरी कोल्हापुर की चप्पल थी। दीवानबाई को धड़कनों का होश न था। उसका जूड़ा ढलक चुका और आँचल छितरा पड़ा था। सीना साँसों को लिए-लिए ऊपर जाता और फिर पछाड़ खाकर ख़ुद को समेट लेता था। उसके खुले पाषाण चक्षुओं ने महसूसा किसी के अपनी ओर तल्लीनता से देखकर बढ़ते आते क़दमों की आहट को। इतनी नज़दीकी थी कि अगर सामने वाले की आँखों से कोई आँसू चूता तो दीवानबाई झटके से चेहरा आगे बढ़ाकर उन आँसुओं को अपनी जिह्वा पर ले सकती थी, उसकी आँखों में कोई कुछ खोज रहा था। किसी ने तो नहीं किया आज तक ऐसा! बाहर-बाहर जिसे जितना मिला... उसके आस-पास के लोग उतने से ही तो मतलब रखते आए थे आज तक। ऐसे भीतर जाकर कुछ खोज निकालना! उसकी इच्छा हुई कि सामने वाले की आँखों को जिस चीज़ की तलाश थी उसमें, वह उसे और भीतर छुपा ले अपने, ताकि उस चीज़ की खोज में वे आँखें उसके भीतर तक उतर सकें। आँखों से भी भीतर और भीतर...लेकिन तभी...बीच में ही सामनेवाला चेहरा पीछे मुड़ गया और धीरे-धीरे उससे दूर होता गया। वह मंत्रबिद्ध-सी सूत के माहे में फँसी-फँसी उसके पीछे बढ़ने लगी। घर के चबूतरे तक जाकर आगे वाले पैर थम गए और उसने पीछे मुड़कर दीवानबाई को बैठने का इशारा दिया। दीवानबाई बैठ चुकी। उसके बग़ल की जगह भी भर गई। उनके ठीक सामने हरसिंगार की वो छाँह थी, जिसके नीचे दो नन्हीं हथेलियाँ लगातार फूल चुने जा रही थी। बच्चा दीवानबाई की मौजूदगी से बेख़बर था। दीवानबाई अपने आपकी मौजूदगी से बेख़बर थी। सुख से पगे कुछ पल। बरामदे पर बैठे दो लोगों के घुटने के बीच बित्ते भर से भी कम का फ़ासला था। दोनों की नज़रें उस फ़ासले पर ही टिकी थीं। तभी बच्चा उठा। उसे सामने दीवानबाई दिख गई। उसकी फूलों से भरी दोनों मुट्ठियाँ खुल गई और हरसिंगार झहड़ कर वापस नीचे बिखर गए। दीवानबाई की बग़ल से कोई तेज़ी से उठा और पलक झपकते में वह लंबी-सी परछाई बच्चे के पास थी। बच्चा तलहथी छितराए हतप्रभ-सा खड़ा था। परछाईं झुककर वापस उन फूलों को चुनने लगी। जो काम बच्चा इतने परिश्रम और इत्मीनान से लंबे-लंबे मिनटों में कर पाया था, वही काम यहाँ क्षणों में संपादित कर दिया गया था, बच्चे की हथेलियाँ वापस फूलों से भर गईं, बच्चा प्रसन्न कम, विस्मित अधिक था। बच्चे के पास जो परछाई आई थी, वह उलटे पाँव लौट गई। इस बार धीमे क़दम और अब वही परछाईं दीवानबाई पर पड़ती थी। दीवानबाई ने गरदन उठाकर आँखें मिलाईं और वह उठने का प्रयास करने लगी। पर घुटने अकड़े पड़े थे। वह उठ नहीं पाई। उसने पास की दीवार पकड़नी चाही कि तभी एक खुली हथेली उसके सामने बढ़ी, जिस पर हरसिंगार का एक सूखा फूल चिपका था। दीवानबाई के हाथ बग़ैर सोचे-समझे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ गए, उस हथेली में अपना भार सौंप देने को। दीवानबाई उठ खड़ी हुई। उसने अपनी और सामने वाले की हथेलियों के बीच हरसिंगार की उपस्थिति महसूस की और तीसरे किसी की मौजूदगी से उसे लज्जा हुई। उसने अपनी हथेली वापस खींच ली। एक हथेली सामने बढ़ी ही रह गई जिस पर हरसिंगार... दीवानबाई का कलेजा धौंकने लगा। वह हड़बड़ाकर बच्चे के पास आई और उसे कंधे से पकड़कर खींचती हुई बाहर ले जाने लगी। बच्चा मुड़कर पीछे देखता रहा अपने शुभचिंतक को, पर वो जो थी दीवानबाई—मुड़ी नहीं वापस।
दीवानबाई ने आइने में सबसे छिप-छिपाकर अपने-आपको देखा। हैरत, ग़ुस्सा। ठीक माँग के पास से सफ़ेद हो आए केश, आँखों के नीचे...बीच गाल पर काली झाइयाँ, पसीना, चिपचिपाहट, चेहरे पर सूजन। इतने दिनों बाद दिखी भी तो ऐसा रूप लेकर! इस ख़याल पर घिन-सी आ गई उसे अपने ऊपर। ऐसे वक़्त में जब वो शख़्स अपने बच्चों की मौत का दर्द झेल रहा था, क्या उसका ध्यान दीवानबाई की शक्ल, रंग-ढंग पर गया होगा! पता नहीं उसने उसमें दीवानबाई को देखा भी होगा या उसके मन की दशा ऐसी होगी कि उसे उसमें एक साधारण औरत नज़र आई होगी। कोई भी हो सकने वाली औरत। परिचित-अपरिचित। कैसी भी। नन्हें हरसिंगार चुनते शिशु को निहारती उसकी वात्सल्य भरी दृष्टि किसे ढूँढ़ रही होगी? यह सोचते दीवानबाई का सीना भर आया। उसके मन में अपने प्रेमी के लिए पहली बार वात्सल्य जागा...
दीवानबाई मायके से अपने पुराने दिन के सपने वापस लाई थी। अब उसका चौतन्य उसे ज़बरदस्ती आइने के सामने से अलग करता। हल्का रंग अब अपनी उम्र के मुताबिक नहीं लग रहा था...चटक रंगों की जीवन में वापसी थी। चेहरा सौंदर्य के तमाम घरेलू नुस्ख़ों की पृष्ठभूमि बना पड़ा था और मन! मन तो मक्खन-सा छताकर पानी के ऊपर-ऊपर तैर रहा था। एड़ियों को झाँवा पत्थर से रगड़ते-रगड़ते दीवानबाई सोचती...अब तक अपने को साफ़-सुथरा रखने का...सँवारने का ख़याल किए बग़ैर ज़िंदगी कैसे गुज़र गई! और अभी भी जब उसमें सामने वाले को एक साधारण औरत ही दिखाई दी थी, तब ये सब फिर किसके लिए! नहीं...वो दीवानबाई को देखकर ठिठकना, उसकी ओर बढ़ता चला आना, वो हाथों का सहारा और वो मौन की भाषा...वो सब सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी के लिए थे। दीवानबाई के लिए।
अपने पोतों के पीछे थाली लेकर...कौर बनाकर घूमते हुए...उनसे खा लेने की मनुहार करते हुए। उनका मुँह अपने आँचल में पोंछते हुए...अक्सर वह भटकने लगी। आगे-आगे दौड़कर उसे छकाता बच्चा कब कनपटियों पर सफ़ेद बाल वाला रूप धर लेता, कुछ होश ही न रह पा रहा था। कौन रखता होगा उसके खान-पान का ध्यान! रात को सोए में अचानक खाँसी का दौरा आ जाता होगा तो कौन एक गिलास पानी तक लाकर देता होगा! कुर्ते मैले पड़ रहे हैं या चप्पल घिस रही है या वज़न कम हो रहा है...कौन दिलाता होगा इसका ध्यान! दीवानबाई सोई रातों को उँगलियों से टटोल-टटोल कर बिस्तर पर कुछ ढूँढ़ती। उसका प्रेमी एक नवजात शिशु में सिमट आता...पूरी तरह से बस उस पर आश्रित। उसका खाना, सोना, पीना, नहाना सब दीवानबाई पर निर्भर। वह भूखा होता तो उसके होंठ दीवानबाई को तलाशते...उसे नींद आ रही होती तो उसकी आँखें दीवानबाई को ढूँढ़ती...दीवानबाई ने अपने सीने को दोनों बाँहों की गिरफ़्त में कसकर जकड़ लिया...ये कैसा प्रेम था जो मातृत्व में, वात्सल्य में घुल-मिल जाता था!...क्या औरत एक उम्र के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ रह जाती है? क्या औरत हर उम्र में सिर्फ़ और सिर्फ़ माँ होती है? नहीं?
रंगमहल से सफ़ेद जड़ी के क़शीदे वाला हल्का नीला परदा, उठा। रंगमहल की दीवारें धुले शंख की बनी थी। छोटे-बड़े, सफ़ेद नीले, चितकबरे शंख। कक्ष की बाईं तरफ़ हाथी दाँत का बना एक नक़्क़ाशीदार खांभा था। उससे लिपटा सोनजूही के लतरों का एक जोड़ा अपने में डूबा हुआ-सा साँसें ले रहा था। दूसरी तरफ़ चंदन की महीन लकड़ियों से बना एक पिंज़रा था, जिसमें चटख उन्नावी पंखों वाले पक्षियों का एक जोड़ा कोलाहल भरे उत्सव में लीन था। रंगमहल शमादानों की लौ से रौशन था। हवा के महीन झोंके से कक्ष के श्वेत ज़हीन परदे इस कोने से उस कोने तक लहराते थे। रंगमहल के रंगोली सजे फ़र्श पर राधा के एक जोड़ी तलवों की छाया पड़ी और कक्ष के शमादानों की शमा फ़क से बुझ गई। अब वहाँ शेष रह गई...कक्ष के बीचोंबीच छत से लटकते फ़ानूस की मद्धिम रौशनी। राधा के दाएँ तलवे से फ़र्श पर एक थाप पड़ी और रंगोली के गुलाबी अबीर का धुआँ कक्ष में तैर उठा। पक्षियों का कलरव थम गया और मृदंग की थाप कक्ष में गूँज उठी। मृदंग की थाप और पंजे-एड़ी की लय...रंगमलह अबीरमय हो उठा और एक-एक करके दीवारों के सारे शंख गुलाबी होने लगे। राधा का महीन पारदर्शी कपड़े के चुन्नटों से पटा लहँगा पूरे निखार पर आ गया और कमर की उठान तक उठते-गिरते लहरों से गुलाबी लहँगे के स्पर्श से एक-एक कर शमादान की लौ प्रज्ज्वलित होने लगी। कक्ष की दीवारों के परदे राधा के नृत्यरत शरीर में लिपटने लगे और रंगमहल में कुछ भी न बचा...सिवाय प्रेम और आनंद के एक गुलाबी आवरण के...
दीवानबाई की आँखें झटके खुली, सुदामा प्रसाद उसे कंधे से पकड़कर बुरी तरह हिला रहे थे—'अविनाश की माँ...'
दीवानबाई ने विस्फारित नेत्रों से उन्हें देखा। उसकी साँसें तेज़-तेज़ चल रही थीं। जूड़ा बिखर चुका था और आँचल अपनी जगह से हट गया था। अविनाश की माँ—इस आवाज़ से मृदंग की थाप पर विजय पा ली थी। 'सपना देख रही हो?' सुदामा प्रसाद ने पूछा। दीवानबाई कोई उत्तर न दे सकी। वह बस देखती रही अपने पति की आँखों में। फिर उसने अचानक सुदामा प्रसाद को अपने-आप में समेट लिया। बाँहें कसकर उसके गिर्द बाँध दीं। उम्र के इस मोड़ पर ये कैसा भटकाव था। जब उम्र थी, इच्छाएँ भूख थी, तब जो सब नहीं कर पाई, उन चीज़ों की ओर अब...इतने सालों बाद! ये तो जीवन का अंत क़रीब आ रहा था। अब फिर से एक नया जीवन जीने की चाह! वह भी इतने दायित्वों में बँधी होने पर...समाज, घर, परिवार, रिश्तेदार...एक औरत होने के बावजूद! नहीं। उसे अपनी पुरानी दुनिया में ही रहना होगा। उसी में रमा देना होगा अपने मन को। उसने सुदामा प्रसाद की पीठ को सहलाया अपनी तर्जनी से। उसे मालूम था कि उसके स्पर्श मात्र से सुदामा प्रसाद के मन में हसरतें जाग उठेगी और फिर...वह हमेशा के लिए अपने को अपनी गृहस्थी में डुबो देगी। लेकिन ये क्या? कोई हरकत नहीं हुई, सुदामा प्रसाद में। उसने अपनी बाँहों का बंधन धीरे-धीरे श्लथ किया। उसके कानों में सुदामा प्रसाद के ख़र्राटे की महीन आवाज़ आई। उसने सावधानी से पूरी तरह अपने आपको सुदामा प्रसाद से अलग कर लिया। दीवानबाई ने नीले बल्ब की रौशनी में ग़ौर से अपने पति का चेहरा पढ़ा। उसपर साफ़-साफ़ लिखा था कि सुदामा प्रसाद ये बाज़ी हमेशा के लिए हार चुके थे। दीवानबाई ने करवट फेर ली और तकिए में अपना मुँह छुपा लिया। हर औरत के मन के एक कोने में कोई रंगमहल होता है और हर औरत के मन में एक राधा होती है। दीवानबाई ने आँखें कसकर मूँद लीं।
दीवानबाई ने अपने आपको सजाया और अपने प्रेमी के दरवाज़े की घंटी बजा दी। दरवाज़ा खुला। उसका दुबला और थका हुआ मेज़बान चौंक गया। दीवानबाई ने उसके कुछ कहने की प्रतीक्षा नहीं की और भीतर घुसकर अंदर तक चलती हुई सोफ़े पर बैठ गई। अतिथि के पीछे उसका मेज़बान। दीवानबाई ने उसके चेहरे पर नज़रें जमाईं। वह सिर नीचा किए बैठा था। क्षणभर पहले का विस्मय धुल चुका था और अब विषाद की छाया वहाँ निखरकर पसरी थी।
'आप अपना ख़याल नहीं रखते ना...' दीवानबाई ने प्रश्न करना चाहा था। लेकिन वाक्य के पूरा होते-होते उसमें से प्रश्नसूचक पुट मिट चुका था और वह एक साधारण, सर्वमान्य उक्ति की तरह सामने था। दीवानबाई ने बिना लाग-लपेट के फिर कहा—'अगर मैं अपका ध्यान रखूँ तो?' सामने वाले ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वह चुपचाप वैसे ही बैठा रहा। कुछ पल गुज़रस गए।
'चलती हूँ' दीवानबाई उठ खड़ी हुई।
घर में एक बार फिर से, पुराने तरीक़े से शाम ढली थी। बच्चे स्कूल से आने के बाद भाग-दौड़ पकड़ा-पकड़ी में मशग़ूल थे। बहुएँ जल्दी-जल्दी नाश्ता तैयार कर रही थीं। बेटे अपनी-अपनी दुकान पर थे। सुदामा प्रसाद शाम की सैर की तैयारी कर रहे थे। दीवानबाई ने संध्या जलाई और प्रसाद देने के लिए पोतों को आवाज़ दी। बच्चे उसे घेरकर खड़े हो गए तो उसने मँझले पोते के सिर पर हाथ रखकर पूछा—'दादी न रहे तो प्रसाद कौन देगा?'
छह साल के बच्चे ने अचरज से उसे देखा। उसका छोटा भाई चिल्लाया—'दादी नहीं रहेगी तो हम पूजा करेंगे और प्रसाद किसी और को नहीं देंगे।' दीवानबाई ने मुस्कुराकर उसके सिर को हलके छुआ, प्यार से। बच्चा किलककर भाग गया। दीवानबाई देहरी पर बैठ गई। कितना छोटा और सधा हुआ जवाब था। उसके सारे अंतर्द्वंद्व, ऊहा-पोह, भीतरी उठा-पटक का जवाब इस नन्हें से बच्चे ने कैसे पलक झपकते दे दिया। कितना सही। कितना नपा-तुला। वह नहीं रहेगी, तब भी दुनिया उसी रफ़्तार से चलेगी। कोई और ले लेगा उसका स्थान। उसने अपने आप को लोप कर मंच का ज़ायक़ा लिया। अगर उसकी अचानक मौत हो जाए, असमय तो...? शाम ऐसे ही ढलेगी। बहुएँ चूल्हें में व्यस्त रहेंगी, बच्चे धमा-चौकड़ी मचाते रहेंगे, बेटे अपनी-अपनी दुकान पर और सुदामा प्रसाद टहलने जाने की तैयारी में, सुदामा प्रसाद के पास आकर भी दीवानबाई की सूई अटकी नहीं, सुदामा प्रसाद की दिनचर्या में उसकी क्या जगह थी? सुबह पाँच बजे जागना, सुबह की सैर, अख़बार, दाढ़ी बनाना, स्नान, नाश्ता, फिर घर के बग़ल में बने अपने छोटे से दफ़्तर में क़ानूनी दाँव-पेंच, दुपहर का भोजन, शाम की बाग़वानी, टहलना, फिर टी.वी. चैनल घुमा-घुमाकर कोई भावनात्मक फ़िल्म तलाशना, उसे देखना। न मिले तो गाने जिन चैनलों पर आते हों हमेशा, उन्हें चाव से देखना। नए ज़माने के कपड़े उघाड़ गाने भी वे उसी आनंद से देखते जैसे सुरैया और सहगल के ज़माने के गाने। दीवानबाई को न तो टी.वी. के चैनलों की जानकारी हो सकी आजतक, न कार्यक्रमों की। और सुदामा प्रसाद! बेटे और बहुएँ तक उनकी जानकारी के मोहताज हैं। टी.वी. देखते-देखते भोजन और फिर पक्की नींद, दीवानबाई कहाँ थी? कहीं नहीं। न वो; न उसकी परछाईं, छोटी बहू ने भीतर से उसे आवाज़ लगाई। दीवानबाई ने उठने की कोशिश की। पर घुटने जवाब दे गए। उनका दाहिना हाथ सामने बढ़ गया। पर उसे थामने के लिए हरसिंगार की कली चिपकी कोई हथेली वहाँ नहीं थी...
रात ढल चुकी थी। सुदामा प्रसाद सोने की तैयारी में थे। दीवानबाई की साँसें तेज़ी से उठ-गिर रही थीं। उसका सिर खिड़की से टिका था और हवाओं के झोंके में आगे के बाल जूड़े से निकलकर चेहरे पर फहरा रहे थे।
बत्ती बुझा देना। आज बारिश होगी। क्या सोच रही हो भई? सुदमा प्रसाद ने उसे टोका।
दीवानबाई ने वैसे ही खिड़की से लगे-लगे, थोड़ा रुककर कहा “सोचती हूँ अगर मैं ना रहूँ तो क्या होगा?
हँस पड़े सुदामा प्रसाद अरे भई, तुम बड़ी भाग्यशाली कहलाओगी। अपने पीछे इतना सुखी घर छोड़ जाओगी। मैं तुम्हें मुक्ति दूँगा। और क्या चाहिए? इसमें इतना सोचने का क्या है?'' दीवानबाई चुप रही वैसे ही, तो सुदामा प्रसाद आगे बढ़े।
“मज़ाक़ कर रहा था भई। तुम भला अभी जाओगी कहाँ? ये सब क्या सोच रही हो आज अचानक? उन्होंने दीवानबाई का कंधा पकड़कर उसे अपनी ओर मोड़ दिया।
“अचानक नहीं... दीवानबाई की आँखों में कुछ था, जिसे देखकर सुदामा प्रसाद ठगे रह गए। वह बोलती गई “अचानक नहीं...अगर मैं कहूँ कि मैं संन्यास लेना चाहती हूँ तो?”
संन्यास...'' इस बार हँस नहीं पाए सुदामा प्रसाद, हालाँकि बात हँसने की थी सरासर। पर दीवानबाई की आँखों ने उन्हें हँसने नहीं दिया।
आप हमें जाने देंगे?
“क्या हो गया है तुम्हें? कुछ ठिठककर सुदामा प्रसाद बोले “मैं सोता हूँ।'
“नहीं। जो बात मुझे आपको पहली रात बतानी चाहिए थी, उसे आख़िरी रात तो बता लेने दीजिए।
सुदामा प्रसाद ने आँखें छोटी कर उसे देखा और उसके माथे पर अपनी तलहथी रखी।
“ताप नहीं है मुझे। मैं ठीक हूँ। शादी से पहले किसी और के साथ मेरे संबंध थे और मैं उसके पास जाना चाहती हूँ।'' दीवानबाई ने मुट्ठी में आँचल को दबाया और पैर का अँगूठा ज़मीन में फँसाया।
“कैसे संबंध? ये हथौड़े की गहरी आवाज़ थी।
मन के संबंध
सुदामा प्रसाद ने दोनों हाथरों से उसका चेहरा पकड़ा, उसके बालों को भरपूर खींचा और उत्तेजित होकर उसे धकेल दिया बिछावन पर। वे काँप रहे थे बेतरह।
मैं उसके पास लौटना चाहती हूँ। इस घर के सारे कर्त्तव्य पूरे कर दिए मैंने। अभी आपने कहा कि अपने पीछे मैं एक सुखी घर छोड़ जाऊँगी। आपने कहा था आप मुक्ति देंगे मुझे। मुझे मुक्ति चाहिए। दीवानबाई बिस्तर पर हाँफ़ रही थी। सुदामा प्रसाद झपटकर उस तक पहुँचे।
“मुक्ति तुम्हें मैं देता हूँ उन्होंने दीवानबाई का गला पकड़ लिया और पूरी ताक़त से उसे दबाने लगे। दीवानबाई जूझ रही थी। माथे से, नाख़ून से। उसे मुक्ति चाहिए थी। लेकिन मरकर नहीं। उसे जीना था। उसने अपने दाँत गड़ा दिए अपना गला दबाते हाथ में, कलाई से थोड़ा ऊपर। बंधन श्लथ हुआ और वह झपटकर अलग हुई। दोनों योद्धा की साँसें फूल रही थीं। सुदामा प्रसाद जल्दी सँभले। उन्होंने ताबड़-तोड़ मारना शुरू किया दीवानबाई को। उन्होंने दीवानबाई को मार-मारकर चूड़ डाला। आख़िर वे पति थे उसके! इतना तो हक़ बनता था। दीवानबाई ने उठना चाहा, पर वह भुरभुराकर बिस्तर पर बिखर गई।
दुनिया जानती थी कि सुदामा प्रसाद की पढ़ाई का ख़र्च उनके पिता की रख छोड़ी संपत्ति से चल रहा है जबकि दिनभर इज़्ज़त से कुलवधू बनकर गुज़ार देने वाली उनकी ग़रीब माँ अँधेरा होते झोला, तराज़ू, बटखरा, काग़ज़ का ठोंगा...लेकर चल पड़ती थी। इन्हीं दो ज़िंदगियों के बीच तालमेल बिठाने के फेर में उसके पैर रेलगाड़ी और प्लेटफ़ॉर्म के बीच लय न साध पाए। क्या दो समानांतर ज़िंदगियों के बीच सम साधने वाली औरत की हमेशा ऐसी ही नियति होती है...! दीवानबाई में हरकत हुई। उस रूह ने, जिसके पैर रात के अँधेरे में ठीक-ठीक प्लेटफ़ॉर्म की थाह नहीं ले पाए थे, दीवानबाई के जिस्म पर हाथ फेरा...सर से पैर तक। दीवानबाई उठ खड़ी हुई। उसने घर के मुख्य दरवाज़े की साँकल हटाई। बाहर घुप्प अँधेरा। बारिश तेज़ हवा, वह नीम बेहोशी में चल रही थी। पता सीधा-साधा, मायके के तीन घर बाद। दीवानबाई ने अपनी नई मंज़िल के दर पर सर झुका दिया। वह एक बंद दरवाज़े के आगे निढाल हो गई। रूह का सफ़र पूरा हो गया। उसने एक बार फिर दीवानबाई के जिस्म पर हाथ फेरा और वह वहाँ से चली गई। चुपचाप, जहाँ उसकी मंज़िल थी, उधर।
आसपास में और भी बहुत बारिश के आसार थे। रातभर बारिश होगी तय था। सुबह क्या होगा? बारिश शायद थम जाए। पर बंद दरवाज़े पर रखे इस सवाल का क्या होगा! हो सकता है कल का सवेरा किसी इंद्रधनुष का साक्षी बने! और अगर...नई मंज़िल ने इस सवाल से मुँह फेर लिया तो! फ़ैसला चाहे जो भी हो, जिसके भी हक़ में हो, इतना क्या कम है कि सुदामा प्रसाद की माँ की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी थी।
- पुस्तक : श्रेष्ठ हिंदी कहानियाँ (2000-2010) (पृष्ठ 102)
- संपादक : कमला प्रसाद
- रचनाकार : नीलाक्षी सिंह
- प्रकाशन : पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस प्रा. लिमिटेड
Additional information available
Click on the INTERESTING button to view additional information associated with this sher.
About this sher
rare Unpublished content
This ghazal contains ashaar not published in the public domain. These are marked by a red line on the left.