शहर नक़्शे से नहीं, यात्राओं से पहचाने जाते हैं
 राशि पांडेय
22 दिसम्बर 2025
राशि पांडेय
22 दिसम्बर 2025
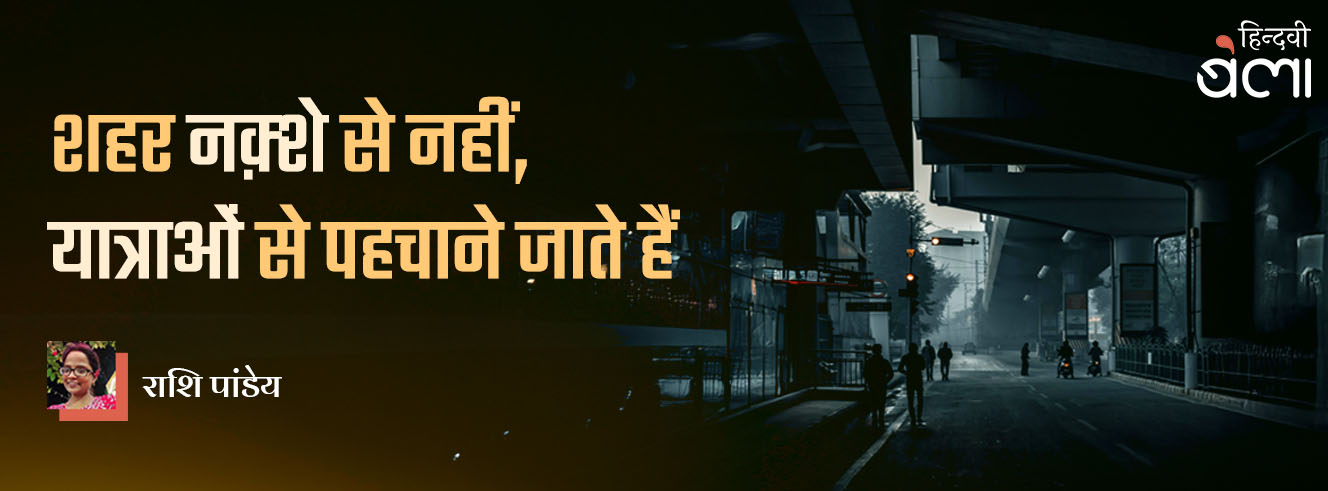
जाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा था। घर में ही एक कोना दे दिया गया, जैसे किसी मुट्ठीभर उम्मीद को दरकिनार कर दिया गया हो। सोफ़ा बिस्तर बन गया, जो कमरा कभी साझा हँसी और कहानियों से भरा होता था, वह अब एक अस्थायी निर्वासन का प्रतीक बन गया। बात करने की तमाम कोशिशें एक कोने में पड़ी टूटी-फूटी टूक-टूक में सिमट गई थीं। वही ड्रम वाला खिलौना, जो कभी मेरी हँसी का साथी था, अब मौन में मेरा अकेलापन बुन रहा था। हफ़्ते भर आधे दिन की भूख हड़ताल और आधे घर निकाले के बाद भी तय कर लिया कि “जाना है, तो जाना है”।
अगली सुबह गंगा-गोमती एक्सप्रेस पर बैठा दिया गया—जैसे कोई बटुआ या थैला रख दिया जाता है, जिसे बाद में उठाना है। माँ ने सख़्त हिदायत दी थी, “सीट मत छोड़ना। ट्रेन में किसी से बात मत करना। उस यात्रा में मैं अकेली थी, फिर भी आधिकारिक रूप से मेरा छोटा भाई भी मेरे साथ था। जिसे दरअस्ल मौसी के घर जाना था और घूमना था। मेरे साथ कोई नहीं था, सिवाय उन अनकहे शब्दों के जो मेरे मन में चुपचाप बैठकर मेरी अगली मंज़िल की ओर इशारा कर रहे थे।
और मंज़िल? कोई शहर या घर नहीं थी, बल्कि एक मुलाक़ात थी—एक लेखक से। नहीं, सिर्फ़ लेखक नहीं—एक अभिनेता, नाटककार, फ़िल्म निर्देशक और मंच निर्देशक भी। और शायद सबसे अहम बात, वह एक ऐसे जादूगर थे जो अपने शब्दों और अभिनय से दिलों-दिमाग़ पर छाए हुए थे। मेरे लिए वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे; वह मेरे भीतर के उस हिस्से से जुड़े थे—जो आज़ाद होना चाहता था, जो बोलना चाहता था, जो महसूस करना चाहता था। उस मुलाक़ात के उन जादुई पलों को जो सचमुच में घटित होने वाले थे।
मैं ट्रेन में बैठी उस अजनबी शहर की ओर जा रही थी, जहाँ मुझे उनसे मिलना था। रास्ते भर मैं अपनी हथेलियों में टूक-टूक की आवाज़ें समेटे हुए थी। जैसे वो मेरी हिम्मत की ताल थी। माँ की हिदायतें, पापा की चुप्पी, घर का संघर्ष—सब मेरे भीतर एक यात्रा का हिस्सा बन गए थे, जो केवल भौगोलिक नहीं थी, बल्कि आत्मिक भी थी।
पहली बार था जब मैं अपने लिए, सिर्फ़ अपने लिए किसी से मिलने जा रही थी। कोई पाठ्यक्रम, कोई परीक्षा, या औपचारिकता नहीं थी—सिर्फ़ मेरी इच्छा थी। और उस इच्छा के पीछे था संघर्ष, संकोच और एक गहरा विश्वास कि यह मुलाक़ात मुझे कुछ ऐसा देगी, जो जीवन भर साथ रहेगा।
शायद यही वह क्षण था जब मैंने जाना कि स्वतंत्रता सिर्फ़ बाहर की दीवारों को लाँघना नहीं, बल्कि भीतर की चुप्पियों से बाहर आना भी है।
दुपहर तक किसी तरह मौसी के घर पहुँची थी। वह घर, जो मेरे लिए बस एक ठिकाना भर था, न कि वह जगह जहाँ लौटकर राहत महसूस होती हो। तीन बार टैक्सी बदलनी पड़ी थी, और दो बार ओला ऑटो कैंसिल हुई। लखनऊ में तब मेट्रो नहीं थी और ये ऑटो ही एकमात्र किफ़ायती विकल्प थे। पर शहर के ट्रैफ़िक में, जहाँ वक़्त ख़ुद से टकरा जाता है, वहाँ कुछ भी किफ़ायती कहाँ होता है—ना पैसे, ना धैर्य, ना उम्मीद।
बीच रास्ते में छुट्टे पैसे ना होने के कारण बीस रुपये ज़्यादा देने पड़े। वही बीस रुपये जिनसे मुझे एक डेरी मिल्क ख़रीदनी थी। शायद कोई कहेगा, “बस एक चॉकलेट ही तो है” पर उस एक चॉकलेट में मेरे लिए बहुत कुछ था—ग्लूकोज से मिलोने वाली एनर्जी या बिना थके चलते रहने की एक उम्मीद, एक सहारा, जब आप अकेले हों, किसी अनजान शहर में, ठंडी हवाएँ आपके कानों में फुसफुसा रही हों कि ‘नवंबर आ गया है’, लेकिन सूर्य देवता ऐसे चिपके हैं जैसे जुलाई का पसीना अभी भी बहता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसे में ‘डेरी मिल्क’ शायद एकमात्र दोस्त बन सकती थी, पर वह भी हाथ नहीं लगी।
घर में घुसते ही किसी ने हाल नहीं पूछा। मौसा जी ने सीधे DF 41 निकाली और सवाल दागने शुरू कर दिए, “क्यों जाना है? कौन है? हम तो नहीं जानते। अमिताभ बच्चन जैसा कोई हो तो जाओ भी। आजकल जाने कहाँ-कहाँ से शौक़ पाल लेते हैं बच्चे। नाम न पहचान, बिन-बुलाए कविमान।” (हाँ, उन्होंने यही कहा था “कविमान”) मैं इस प्रहार के लिए तैयार थी, अपने अंदरूनी कवच के साथ। पर यह हमला जल्दी और ज़्यादा तीखा था।
मैंने संयम से जवाब दिया, “बच्चन नहीं, कौल हैं।”
इतना कह देने से लगा कि मैंने ख़ुद को साफ़ कर दिया है, पर नहीं—यह तो शुरुआत भर थी।
17 तारीख़ थी। दुपहर 12 नहीं, बल्कि 12:30 बजे के आस-पास मैं कैफ़े रेपेर्तवह्र (Repertwahr) पहुँची। छोटा-सा कैफ़े, पर किसी गुफ़ा की तरह शांति से भरा हुआ। मौसा जी मेरे साथ थे। और वहाँ पहुँचते ही उन्होंने—पास बैठे लोगों को समझाया कि ये सब फ़िज़ूल कार्यक्रम होते हैं, और आगे कहा कि से इन बेतुके आयोजनों में भागीदारी देने से अच्छा है घर बैठकर नेशनल जियोग्राफी देखो। लोगों ने उन्हें सुना नहीं सुना, क्या फ़र्क़ पड़ता है, ज्ञान का पिटारा खोल सबको अपनी बात सुनाने की उनकी कोशिश सफल हुई।
जाते-जाते कमान का एक आख़िरी तीर भी छोड़ दिया, “आप लोग ऐसे फ़ालतू के लोगों को सुनने आते हैं, इनका महत्त्व बढ़ाते हैं। ये बस अपनी किताबें बेचने आते हैं और बेवक़ूफ़ बनाते हैं।” उस पल, मेरे भीतर एक गहरी चुप्पी उतर आई थी। कोई जवाब नहीं दिया मैंने। क्योंकि उस वाक्य के पीछे जो चुप्पी थी, उसमें मैं अपनी हज़ार इच्छाओं की मौत महसूस कर रही थी—पर साथ ही उनमें से किसी एक की फिर से साँस भी।
मैं जानती थी कि वह क्षण मेरे लिए हार का नहीं—बल्कि यह जानने का था कि जिन चीज़ों को दुनिया ‘फ़ालतू’ कहती है, वही मेरे जीवन का अर्थ बनेंगी।
पहला सेशन ख़त्म हुआ। संचालन मशहूर क़िस्सागो कर रहे थे, जिनकी आवाज़ में लखनऊ की मिट्टी की नमी और अवधी की मिठास दोनों घुली हुई थी। उनका घर यहीं, इसी शहर में था, लेकिन जब वह मंच पर थे तो शहर जैसे उनके भीतर ही समा गया था। उन्होंने लेखन की बारीक़ियों से हमें अवगत करवाया। उनकी बातों में सिर्फ़ काग़ज़ और क़लम नहीं, बल्कि ख़ामोशी, धैर्य और आत्मा की परतें भी थीं। वह लिखने के प्रोसेस के बारे में बता रहे थे, लेकिन असल में वह हमें स्वयं को समझने की प्रक्रिया सिखा रहे थे।
दूसरा सेशन शाम 6 बजे शुरू हुआ। तब तक कैफ़े में हलचल थी, लेकिन जगह मिल गई थी। पर जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ा, 7 बजे तक पूरा कैफ़े खचाखच भर चुका था। कुर्सियों के नीचे बैग रखे गए, कॉफ़ी कप अब ठंडे हो चले थे और लोगों की आँखों में वह प्रतीक्षा थी जो केवल एक लंबे इंतज़ार के बाद पनपती है। 7:32 हो चुके थे। दरवाज़े की ओर हर कोई एक अनकहे प्रश्न की नज़रों साथ देख रहा था। जिन लोगों ने सुबह से इंतज़ार किया था, उनके धैर्य में अब बेचैनी घुलने लगी थी। और जो लोग शाम को ही आए थे, वो घड़ी की सुइयों से अपना धैर्य नापने लगे थे। उनके चेहरे पर यह भाव था कि शायद चले जाना चाहिए। किसी के कान में किसी ने कहा, “शायद आए ही ना...” तो किसी ने जवाब दिया, “न्यूज़ शूटिंग चल रही होगी…” लेकिन सब एक-दूसरे की ओर ऐसे देख रहे थे, जैसे आँखों में सवाल ओर जवाब साथ मिले हुए हों। तभी पीछे वाली सीढ़ियों के पास जो दरवाज़ा था—नए ज़माने का, लेकिन उसकी आवाज़ पुराने ज़माने की हवेलियों जैसी थी—वह धीरे से खुला। और उसमें से कोई दाख़िल हुआ। सफ़ेद क़मीज़ और काली, हाँ, काली ही पैंट पहने।
कोई चमक, चकाचौंध, शोर नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई फ़ैन की भीड़ नहीं। वह धीरे-धीरे चलता हुआ सामने मंच तक पहुँचा। और जब तक वह मंच पर नहीं चढ़ा, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह वही शख़्स है जिसके इंतज़ार में सुबह शाम में और शाम रात में बदल गई, यही ‘अशोक’ है—‘तुम्हारी सुलु’ वाला। वही जो स्क्रीन पर दिखता है, जिसकी आवाज़ हमें किसी कविता की तरह छूती है।
लोगों के दिमाग़ में शायद लाइट्स, मीडिया, भीड़ और अफ़रा-तफ़री की तस्वीर थी। शायद मेरे दिमाग़ में भी। पर जो आया, वह बस ‘आया’—जैसे कोई हवा कमरे में दाख़िल हो जाए ओर ठंडक दे जाए। न कोई घमंड, न कोई प्रदर्शन—सिर्फ़ एक उपस्थिति, जो सादगी से भरपूर थी और इसीलिए सबसे ज़्यादा असरदार भी। उस क्षण मुझे समझ आया कि कुछ लोग अपनी ख़ामोशी से भीड़ में सबसे ज़्यादा गूँजते हैं। और कुछ दरवाज़े, चाहे जितने भी नए हों, अगर सही वक़्त पर खुलें तो वह आपकी आत्मा में पुरानी हवेली की तरह गूँजते हैं।
बातें शुरू हुईं उस किताब पर, जो हाल ही में प्रकाशित हुई थी। पर जल्दी ही बातचीत किताब से आगे बढ़कर मुड़ गई—जीवन और यात्रा की ओर। मंच पर बैठे लेखक ने जब ‘यात्रा’ पर बोलना शुरू किया, तो उनकी आवाज़ में एक ठहराव था, जैसे वो शब्दों को नहीं, अपनी साँसों को भी माप रहे हों। उन्होंने पूछा, “यात्रा क्या होती है? कितने तरह की होती है?” और फिर मुस्कुराकर इशारा किया सामने बैठे कुछ लोगों की ओर—“आपकी, मेरी, इन जनाब की जो दाएँ बैठे हैं, और इन मोहतरमा की जो बाएँ हैं—हम सबकी यात्राएँ अलग हैं। कोई अपने बचपन से भाग रहा है, कोई उसी की ओर लौटने की कोशिश में है।” फिर उन्होंने अपनी किताब की ओर इशारा किया और कहा, “मैं यहाँ आया हूँ, अपनी किताब पर बात करने के लिए, आप सबसे मिलने, आपसे बात करने के लिए—ये मेरी बाहरी यात्रा है। पर भीतर, मैं अभी भी यात्रा पर हूँ। और यह यात्रा रुकी नहीं है।” न रुकेगी। और शायद वहीं, पहली बार, कमरे की दीवारें थोड़ी-सी और पीछे सरक गईं। कोई टेबल, कोई कैफ़े कप नहीं रहा। बस हम थे, वह थे और शब्द थे, जो किसी नदी की तरह बह रहे थे। फिर अकेले यात्रा करने की बात आई। वह बोले, “ट्रैवल इज़ नॉट ईज़ी।” और न जाने क्यों, ये बात सीधा भीतर उतर गई। जैसे किसी ने तुम्हारे अकेलेपन की पीठ पर धीरे से हाथ रख दिया हो।
“यात्रा में आप ख़ुद को खोजते हो,” उन्होंने आगे कहा। “सुबह आपकी होती है, शाम आपकी होती है। जिस रिक्शे की पिछली सीट पर आप बैठे हैं, वह भी आपकी होती है। चाय का वह कप ओर कॉफ़ी की वह प्याली भी जो गिनती में चौथी या पाँचवी होगी।”
इन वाक्यों में न कोई शोर था, न कोई दावा। लेकिन जैसे हर शब्द मेरी ही कहानी कह रहा था, हर चीज़ अपनी कहानी कह रहा था—जैसे वह रिक्शा, जिसमें मैं अकेले लखनऊ की गलियों से गुज़र रही थी; या वह डेरी मिल्क, जो मैं ख़रीद नहीं सकी; या वह इंतज़ार, जो 7:32 बजे तक कैफ़े की कुर्सी पर बैठा था—ये सब उस वक़्त मेरे साथ बैठे थे।
उनकी आवाज़ में, जैसे किसी पुराने दोस्त की चिट्ठी थी। सादगी से लिपटी हुई, लेकिन हर अक्षर में एक स्पर्श। मुझे नहीं पता वह बाक़ी लोगों के लिए क्या थे, पर उस वक़्त, वह मेरे लिए एक संकेत थे—कि मेरी यात्रा कोई भटकाव नहीं, बल्कि एक रास्ता है।
इतनी सारी बातों के बाद, एक छोटे-से विराम के साथ, उन्होंने अपनी किताब ‘बहुत दूर, कितना दूर होता हैं’ के कुछ अंश पढ़ने शुरू किए। कमरे में हल्की-सी ख़ामोशी उतर आई थी। कुछ लोग सिर झुकाए सुन रहे थे, कुछ ने अपनी आँखें बंद कर ली थीं—जैसे शब्दों को केवल सुनना नहीं, महसूस करना छह रहे थे।
हर वाक्य जैसे किसी पुराने खत से निकलकर हमारे सामने आ रहा था। उनके शब्दों में एक थकान भी थी और एक दूरी भी—जैसे वह सचमुच किसी बहुत दूर की यात्रा से लौटे हों। और फिर उन्होंने एक जगह रुककर कहा : “जब मैं पैरिस में था, वहाँ था, लेकिन वह मैं पैरिस में नहीं था। मेरी आँखों से देखा हुआ पैरिस था, पर मन की आँखों से नहीं। वह दूसरों का दिखाया हुआ था।” कमरे में जैसे कुछ ठहर-सा गया। यह वाक्य बाहर जितना सीधा लगता है, भीतर उतने गहरे से काट रहा था। हम सबके पास ऐसे ‘पैरिस’ होते हैं—जगहें जहाँ हम गए, पर अपनी नहीं लगी। अनुभव जो हमने किए, पर हमारे नहीं थे। शहर, रिश्ते, घटनाएँ—जो हमारी आँखों से तो देखी गईं, लेकिन हमारे भीतर नहीं उतरीं। वो सब जैसे किसी और के फ़्रेम में रखे गए चित्र थे, जिन्हें हम बस पकड़े रहे। उस क्षण मुझे लगा जैसे वह न केवल अपनी किताब पढ़ रहे थे, बल्कि मेरे अंदर किसी अधूरी यात्रा को भी शब्द दे रहे थे। जैसे कह रहे हों : “देखो, यह दूरी सिर्फ़ भौगोलिक नहीं होती—यह भीतर की भी होती है।” इस एक वाक्य में जैसे वह पूरा जज़्बा सिमट गया था, जो किसी संवेदनशील लेखक को एक भीड़ से अलग करता है। वह पैरिस, जो टूर गाइड में नहीं था। वह अकेलापन, जो सेल्फ़ी में नहीं आता। और वह सवाल, जो वापसी की टिकट से भी ज़्यादा भारी होता है—“क्या यह मेरी यात्रा थी, या किसी और की लिखी हुई पटकथा?” उस पल उनके कहे हुए शब्द मुझमें कुछ ऐसा खोल गए, जो मैंने शायद लंबे समय से बंद कर रखा था। वह एहसास कि ‘दूरी’ सिर्फ़ किलोमीटरों में नहीं होती। कभी-कभी वो हमारी ही आँखों और मन के बीच होती है।
जब हम किसी शहर में दाख़िल होते हैं, तो दरअस्ल किसी ज़मीन पर नहीं, एक रिश्ते पर क़दम रखते हैं। शहर सिर्फ़ इमारतों से नहीं बने होते, वह स्मृति होते हैं, संवेग होते हैं और कभी-कभी वह आईना भी बन जाते हैं जिसमें हम ख़ुद को ढूँढ़ने लगते हैं। शहर को देखकर उसका नक़्शा नहीं, उसकी आत्मा समझ में आती है। उसके पुराने हिस्सों में चलना, जैसे किसी बुज़ुर्ग की दैनंदिनी पढ़ना हो—जहाँ हर गली एक अधूरा ख़त है और हर इमारत एक अधूरी दुआ। पुराने मकानों की खिड़कियों से झाँकते रंग और जालीदार नक़्क़ाशी मानो कह रही हो : हमने बहुत कुछ देखा है, और अब तुम्हें देख रहे हैं।
मैं लखनऊ में थी। जिसे लोग तहज़ीब का शहर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो एक अजनबी शहर था, जिसे केवल सफ़र के दौरान थोड़े बहुत हाल के साथ जाना था।
गोमती नगर की चौड़ी सड़कों, लखनऊ सेंट्रल मॉल की रोशनी और अंबेडकर पार्क की संगमरमरी ख़ामोशी में मैं मौसी के साथ घूमी। वो सब देखा जो शहर ने दिखाने के लिए सजाया था। पर जो छुपा रखा था, वहाँ मेरा दिल अटका रहा।
मुझे रूमी दरवाज़ा देखना था, क्योंकि वह किसी जिंजर प्रोफ़ाइल की तरह नहीं, किसी पुराने रिश्ते की तरह खुलता है।
मुझे चौक जाना था, जहाँ हर मोड़ पर कोई अजीब-सी पुरानी याद खड़ी मिलती है।
मुझे घंटा घर के पास खड़े होकर वो वक़्त सुनना था जो किसी घड़ी में नहीं, बस हवा में बजता है।
मुझे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, और भूतनाथ मार्केट देखना था। जहाँ सामान नहीं, कारीगरी बिकती है। वह जो देखा गया, शहर का मुखौटा था। और जो छूट गया, वह उसकी रूह थी।
आज हम सब शहरों को गूगल रिव्यू में पढ़ते हैं, लेकिन जो किसी गली के मोड़ पर अकेले चलने से समझ आता है। वह किसी पोस्ट में नहीं मिलता। जुड़ाव, कभी मॉल्स में नहीं, अक्सर धूलभरी गलियों में मिलता है। जहाँ वाई-फ़ाई नहीं चलता, पर एहसासों का नेटवर्क फ़ुल रहता है।
तस्वीरें भी खिंच गई थीं।
स्टोरीज़ भी डाल दी थीं।
भीतर एक ख़ाली कोना रह गया, जैसे कुछ छूट गया हो, जो वापस जाकर भी नहीं मिलेगा।
मेरा उदेश्य पूरा पर ‘यात्रा अधूरी’ थी।
संबंधित विषय
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
