सामान्य जीवन-प्रसंगों का कहानीकार
 मधुरेश
25 दिसम्बर 2025
मधुरेश
25 दिसम्बर 2025
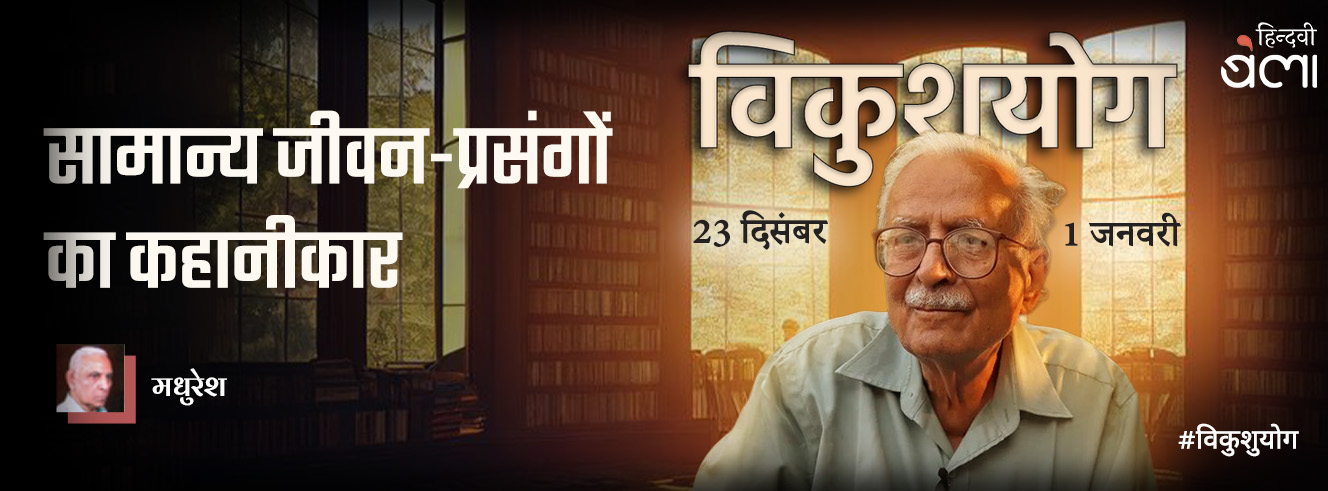
विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यासों वाली अपेक्षाओं के साथ उनकी कहानियाँ पढ़ने पर किसी को भी कुछ निराशा हो सकती है। कहानियाँ वैसे भी उन्होंने अधिक नहीं लिखी हैं। जो लिखी हैं, उनमें न तो मध्यवर्गीय विडंबनाओं का कोई बेधक और मार्मिक अंकन हैं—’नौकर की क़मीज़’ की तरह, और न ही ‘दीवार में एक खिड़की रहती थी’ की तरह वह किसी जादुई संसार में आवाजाही करते हैं। इधर अर्से से उन्होंने कहानियाँ नहीं लिखीं। अतः यह कह पाना भी मुश्किल है कि ‘खिलेगा तो देखेंगे’।
ग्यारह कहानियों के उनके इकलौते संग्रह ‘महाविद्यालय’ में जो कहानियाँ संकलित हैं, वे अधिकतर निम्नमध्यवर्गीय समाज और परिवेश की हैं। अपनी इन कहानियों में वह प्रायः ही उस अमूर्तन से बचते हैं जो कवियों द्वारा लिखित कहानियों की एक विशिष्ट पहचान मानी जाती है। ये कहानियाँ बहुत छोटे-छोटे घटना-प्रसंगों के इर्द-गिर्द बुनी गई हैं, जिनमें छोटे-छोटे संघर्षों के बीच, नौकरी और परिवार के बीच जीते लोगों की छवियाँ अंकित हैं। ये अधिकतर प्रथम पुरुष में लिखी गई कहानियाँ हैं, जिनमें बचपन की स्मृतियों की एक विशिष्ट भूमिका है।
इन कहानियों में निम्न मध्यवर्गीय युवाओं के लिए कठिन परिश्रम से कमाए गए रुपयों का क्या मूल्य होता है, इसे समझने के लिए ‘रुपए’ और ‘बोझ’ जैसी कहानियों का उल्लेख ख़ास तौर से किया जा सकता है। ‘रुपये’ में नब्बे रुपये मासिक की नौकरी करता एक युवक है, जो आठ रुपये मासिक किराये वाले एक कमरे में रहता है। घर साझा है जो बच्चे वाले परिवारों के कारण हरदम गंदा रहता है। अपनी तनख़्वाह के बीस रुपये खो जाना उसके लिए एक बड़ा सदमा है। उसकी पारिवारिक हालात बहुत अच्छी नहीं है। मैट्रिक करते ही उसे यह नौकरी करनी पड़ी है। घर से यह दूरी पैंतालीस मील है। मितव्ययता और सादगी उसके जीवन-मूल्य हैं। वेतन में से पचास रुपए उसे पिता को भेजने होते हैं, क्योंकि उससे छोटे तीन भाई हैं जो पढ़ते हैं। पिता प्राइमरी स्कूल में हेड मास्टर हैं। उसकी सबसे बड़ी चिंता यही है कि खोए हुए बीस रुपये कैसे पूरे किए जाएँ? कतरब्यौंत करके वह हिसाब लगाता है—पिता को चालीस भेजेगा, उनकी नाराज़गी की आशंका के बावजूद। इस महीने सिनेमा नहीं देखेगा। इतवार को भी नहीं खाएगा। न ही चाय पिएगा। अपने इरादे पर अमल करते हुए, शाम को घूमने निकलने पर, कुल्फ़ी की इच्छा होने पर भी वह खाता नहीं है।
रुपये खो जाने का जितना गहरा सदमा उसे होता है, उनका मिल जाना भी उसे वैसी ही गहरी ख़ुशी से भर देता है। होटल को देने वाले बीस रुपये पेटी में रखकर वह भूल गया था। रुपये मिल जाने पर वह पिता को दस रुपये अलग से भेजता है। उसी दिन वह सिनेमा भी जाता है और दस आने का टिकट ब्लैक में एक रुपये में ख़रीदता है। एक मामूली हैसियत के आदमी के लिए रुपये होने और न होने के बीच के अंतर को कहानी बारीकी से अंकित करती है। यह वह जीवन है, जिसमें बीस रुपये पूरे महीने उसे प्रभावित करने की सिफ़त रखते हैं।
ऐसा ही युवक ‘बोझ’ में भी है। वह भी अकेला रहता है और डेढ़ सौ रुपये मासिक की नौकरी करता है। सामान के नाम पर कमरे में सिर्फ़ एक छोटी पेटी और बिस्तर है। होटल के जिस कमरे में वह मासिक किराये के हिसाब से रहता है, उस होटल का लड़का ही रोज़ कमरे में झाड़ू लगाता है। दो दिन पहले मिले वेतन के सारे रुपये वह पेटी में रख देता है। एहतियातन वह रुपयों को रूमाल से ढक देता है—इससे वे ढके भी रहेंगे और कोई चीज़ निकालने पर गिरेंगे भी नहीं। एकबारगी पेटी खोलने पर भी किसी की नज़र नहीं पड़ेगी। दफ़्तर जाते हुए, काफ़ी दूर निकल जाने पर, उसे आशंका होती है कि कमरे का ताला जाते समय उसने लगाया है या नहीं। लौटकर वह उसे देखने आता है। आख़िर पूरे महीने के वेतन का मामला है। पिछले दिन साइकिल से दफ़्तर जाते हुए नीम की एक सूखी पत्ती उड़ती हुई उसकी जेब में आ गिरी थी। उसे तब तक वह बोझ लगती रही, जब तक उसने साइकिल रोककर उसे निकाल नहीं दिया था—उसके टूट जाने के बावजूद। आज भी उसे याद नहीं कि चलते वक़्त उसने ताला बंद किया है या नहीं। लेकिन आज वह लौटता नहीं है। वेतन के रुपयों से महीने की सारी उधारी उसने निपटा दी है। महीने का ज़रूरी सामान वह ख़रीद चुका है। इस बार उसने एहतियातन होटल का एडवांस भी दे दिया है। अब बोझ काहे का?
विनोद कुमार शुक्ल की कहानियाँ मुख्यतः सामान्य लोगों के छोटे-छोटे घटना-प्रसंगों के सहारे विकसित होती हैं। सामान्य लोगों की छोटी-छोटी बातों को भी वह पर्याप्त महत्त्व देते हैं और इस बहाने उनके चरित्र की भीतरी पतों को खोलते हैं। ‘झुंड’ का बूढ़ा व्यक्ति दो बहुओं वाले परिवार के साथ रहता है। दस वर्ष का एक पोता भी है। बूढ़े को तंबाकू इकट्ठी करने का शौक़ है और इसके लिए वह संदूक़ या वैसी ही किसी दूसरी चीज़ के बजाए खूँटी पर टँगे अपने कोट की जेबों का इस्तेमाल करता है। नीली क़मीज़ वाला आदमी, जो थोड़े से अंतराल के बीच दो बार दही लेकर गुड़ाखू लेन में जाता है, अपनी उपस्थिति का कोई तर्क नहीं तलाश पाता। वाचक के पिता मर चुके हैं। वह भैया-भाभी के साथ रहता है, लेकिन भाभी से उसकी पटती नहीं है। लोगों के इस झुंड का होना ही कहानी में घटित होता है। कहानी किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ती। इसी तरह पात्रों और घटना-प्रसंगों के बावजूद ‘टुकड़ा’ भी एक जटिल और दुरुह कहानी है। कहानी में वाचक और उसका मित्र दिनेश है। राह चलते इन लोगों को पाँच-छह तोले का पीली धातु का एक टुकड़ा सड़क पर मिलता है। उठाकर देखने-परखने के बाद वे तय नहीं कर पाते कि वह सोना है या पीतल। इसी संशय की स्थिति में जब वे लोग एक परिचित सुनार के पास जाकर उसे दिखाना चाहते हैं तो उन्हें दरवाज़े पर ताला लटका मिलता है। इसी ऊहापोह के बीच थाने जाकर वे उस टुकड़े को जमा करने जाते हैं, देखने के बाद थानेदार उसे पीतल बताते हुए उनके सामने ही बाहर सड़क पर फेंक देता है। घूमघाम कर लौटने पर जब वे फिर थाने के आगे से गुज़रते हैं, उन्हें लगता है कि सिर्फ़ उन्हें दिखाने के लिए थानेदार ने उसे फेंक दिया होगा, फिर बाद में उठा लिया होगा। लेकिन उनकी आशंका ग़लत साबित होती है। टुकड़ा तब भी वहीं पड़ा होता है, वैसे ही। उस टुकड़े को वहीं पड़ा देख दिनेश ख़ासतौर से उदास हो जाता है। उसने उसे सोना मानकर उससे मिलने वाली अनुमानित राशि के अपने हिस्से से एक मोटे से ख़र्च का हिसाब मन में बैठा लिया था। वह वाचक मित्र के पहने उन्हीं गंदे कपड़ों में अपने घर चला जाता है, जिन्हें बारिश में भीगकर उसने बदला था। उसकी उदासी शायद उसकी अपेक्षा से जुड़ी है। धातु के उस टुकड़े की तरह ग़लत निकलकर अपेक्षाओं का कारण अंततः उदास तो करता ही है।
‘पेड़ पर कमरा’ में पीपल की शाख़ कमरे की खिड़की सटी है। पेड़ पर गिलहरियों की भाग-दौड़ बनी रहती है। कमरे में हलचल को उसने चूहों का उत्पात समझा था। बाद में उसकी समझ में आया कि वे गिलहरियाँ ही थीं। पेड़ से उनकी आवाजाही कमरे में बनी रहती है। कमरा पेड़ से इतना सटा है कि लगता है जैसे वह पेड़ पर ही हो। बाद में दूसरे दो कमरों वाले मकान में रहते हुए वह एक बार फिर कमरे पर गया था। तब कोई बुज़ुर्ग-सा आदमी उसमें रह रहा था। कमरे को देखकर उसे अपने घर की याद आती है। मकान मालिक से मिलकर वह फिर उसी कमरे में रहने की अपनी इच्छा जताता है। वह आश्वासन देता है कि ख़ाली होने पर इसकी सूचना वह उसे देगा। रास्ते में उसे याद आता है कि अपना पता तो उसने छोड़ा ही नहीं है। तभी उसे मकान मालिक का ‘नौकर आदमी’ अपने पीछे आता दिखाई देता है। रास्ता काटकर वह दूसरी ओर मुड़ जाता है। फिर वह उस पीपल वाले कमरे की ओर कभी नहीं जाता। कमरे में साँप आ जाने की कल्पना और उसे काट लेने के बाद अपने परिवार की दशा सोच वह सिहर उठता है। खिड़की को हमेशा तो बंद नहीं रखा जा सकता।
‘झुंड’ की तरह ‘भीड़ का फ़ालतू वक़्त’ में भी बहुत छोटी और मामूली घटनाएँ हैं। नई बनी सड़क कल ही चालू हुई है। कोलतार का ड्रम और सड़क बंद की सूचना वाला लाल झंडा अभी भी वहाँ है। पंडितनुमा आदमी, अधेड़ औरत, गंभीर और चुप-सा लड़का, जूते का काटा आदमी आदि विभिन्न कार्य व्यापार में व्यस्त हैं। जूतों का ज़िक्र चलने पर, अच्छे जूतों के लिए जब वह रामचंदानी या लालाजी की दुकान का नाम लेता है तो लोग उसे उन दुकानों का एजेंट समझ लेते हैं। ये कहानियाँ काफ़ी कुछ रिपोर्ताज की शैली में चीज़ों को बयान करती हैं, लेकिन इससे न तो चरित्रों की कोई विशिष्टता उभरती है, न ही वह कोण सामने आता है, जहाँ से कहानी को देखने समझने का कोई संकेत मिलता हो।
‘गोष्ठी’ साहित्य में आलोचना की तानाशाही पर केंद्रित है। युवा कवियों की गोष्ठी में अकेला अधेड़ आलोचक कवियों को अपने हिसाब से हाँकने की कोशिश करता है। कवियों की निरीहता के आगे आलोचक की तानाशाही की परतें कहानी में धीरे-धीरे खुलती हैं। आलोचक द्वारा प्रतीकों के प्रत्यक्षीकरण के आग्रह पर व्यंग्य की अंतर्धारा कहानी में स्पष्ट है। कविता में प्रयुक्त प्रतीकों को कवि लाकर आलोचक को दिखाते हैं। ऐसे प्रतीकों में रोटी, चाँदी का गिलास, ज़री का दो गज़ का टुकड़ा, टूटी-फूटी चीज़ें, एक पंखुड़ी वाले गुलाब आदि पर ख़ास ज़ोर है। एक पंखुड़ी वाला गुलाब न मिलने पर कवि कमरे में ही रखे फूलदान से गुलाब निकाल, उसकी पंखुड़ियों को नोच सिर्फ़ एक पंखुड़ी छोड़ देता है। कवियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ये प्रतीक आलोचक के गोदाम में बंद रहते हैं। भुतहे वातावरण के बीच, कवियों द्वारा परिश्रमपूर्वक लाए जाने वाले इन प्रतीकों को ही आलोचक की दृष्टि में सफलता की कसौटी माना जाता है। प्रतीकों की प्रत्यक्ष और स्थूल उपस्थिति ही, आलोचक की दृष्टि में कविता की सफलता की कसौटी है। उसे ही आलोचक प्रकारांतर से अपनी सफलता समझता है। कमरे के भुतहे वातावरण में असंख्य अज़ीब-ओ-ग़रीब प्रतीकों को देख एक कवि को लगता है—उसकी कविता का शोषण हुआ है।
‘‘उसने देखा कि एक ही जगह काव्य-प्रतीक के रूप में पेट्रोल का डिब्बा रखा हुआ है। उससे थोड़ी ही दूर पर किसी दूसरी कविता के प्रतीक के रूप में एक माचिस की डिब्बी भी थी। अचानक उसकी आँखें चमक उठीं। चारों तरफ़ पेट्रोल को छिड़कने के बाद उसने माचिस से आग लगा दी। भभककर आग फैल गई। पीछे के दरवाज़े से वह ज़ोरों से भागा, उसे डर था कि वह भी जल जाएगा। आग धीरे-धीरे फैलती जा रही थी। एक भगदड़ मची थी। इतने में दौड़ते-दौड़ते आलोचक आया। उसे याद आया कि दरवाज़े के पास प्रतीक के रूप में आग बुझाने के यंत्र भी हैं। उसी यंत्र से सारी आग तुरंत बुझा दी गई। नुक़सान ज़्यादा नहीं हुआ था। इकट्ठी हुई भीड़ को और बचे हुए कवियों को आलोचक गर्व के साथ प्रतीकों की प्रत्यक्ष उपयोगिता समझा रहा था...’’ आलोचक की यह सफलता ही वस्तुतः कविता की पराजय है। स्थूल प्रतीकों की उपलब्धता की तानाशाही कविता को नष्ट करती है। आग से भले ही ज़्यादा नुक़सान न हुआ हो, कविता इससे ज़रूर झुलसी है।
‘महाविद्यालय’ मूलतः बचपन और युवावस्था की स्मृतियों से बनी रचना है। कहानी का वाचक ‘मैं’ महाविद्यालय में अंतिम वर्ष का छात्र है, अपने दोस्त की ही तरह, जबकि उसका छोटा भाई प्रथम वर्ष में है। बाज़ार की कहानी में एक विशिष्ट भूमिका है। मटरगश्ती करते हुए बाज़ार में घूमना वाचक को प्रिय है। वह बाज़ार में किसी ख़रीददार को चुन उसका पीछा करता है। बाज़ार की सारी क्रूरता के बावजूद उसकी उससे दोस्ती है।
‘महाविद्यालय’ किसी पुराने क़िले को सुधार कर बनाया गया है, जिसके तीन तरफ़ तालाब हैं। वाचक का परिवार एक सनातनी ब्राह्मण परिवार है—विपन्नता की हदों को छूता। हाल पर पिता डेढ़ सौ रुपया महावार पाते हैं। आस-पास कहीं से खाने का निमंत्रण मिलने पर प्रायः वे दोनों लड़कों को साथ ले जाते हैं। ‘मैं’ अर्थात् वाचक से वे इसलिए ख़ुश रहते हैं क्योंकि उसकी ख़ुराक अच्छी है, जाने पर ढंग से खाता है। परिवार की ग़रीबी का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि टट्टी में गिरा और सना पीतल का गिलास जमादारिन से निकलवाकर, आग में डाल, उसी से ‘शुद्ध’ करवाकर फिर इस्तेमाल किया जाने लगा था।
माँगने पर भी उसे जमादारिन को नहीं दिया जाता जिसके कारण मोहल्ले-पड़ोस में उसने ख़ूब बदनामी की थी। परिवार में चलती पीतल की थालियों के नाम पुराने फ़िल्मी गानों पर आधारित है, जैसे पिता की थाली थी ‘घर-घर में भगवान’ जबकि माँ की ‘संत सखूबाई’। बेटों की थालियों के नाम क्रमशः ‘दुनिया न माने’ और ‘झुमरू’ थे। अपनी ग़रीबी के विरुद्ध छोटे भाई का तर्क था—‘‘बीस बिसवा ब्राह्मण हैं, ग़रीब होने पर भी बड़े रहेंगे।’’ जब बड़े बेटे की कुंडली की माँग आने लगती है, पिता ‘संकल्प’ की बात अवश्य पूछते। उनका आशय दहेज से होता। ‘देखवा’ लोगों को वह महाविद्यालय भी ले जाते थे, लड़कों को दिखाने के वास्ते। कहानी में बचपन की स्मृतियाँ भी हैं—वह मैदान भी जिसमें प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय खेलते थे, उड़ती हुई चील की परछाईं में रखे गए काग़ज़ का खेल जिसके बारे में माना जाता था कि चील की परछाई काग़ज़ पर पड़ने से वह रुपया बन जाएगा। मैदान के सामने इमली के पेड़ पर चढ़ना और कुछ लड़कों को पेशाब लगने पर वहीं पेड़ पर से पेशाब करना। घर में माँ-अजिया की काठ की एक छोटी-सी संदूक़ थी। उसमें चिल्हर पैसे, सुपारी, दुर्गा की पोथी और दो बँटी हुई हल्दी लगी सुतली थीं। इनमें से एक में वाचक अर्थात् बड़े बेटे की उम्र जितनी गाँठें थीं, दूसरे में छोटे की। काठ को कंघी से बाल काढ़ते समय टूटे बालों को ही बँटकर माँ ने यह सुतली बनाई थीं। माँ को अफ़ीम खाने का शौक़ था। चीकट अफ़ीम की धनिए जैसी गोलियाँ वह इसी संदूक़ में रखती थीं जिसकी ताली डोरे से बंधी उसकी गर्दन में पड़ी रहती थी।
इस बीच महाविद्यालय में बचत का अर्थशास्त्र समझाने वाले वाणिज्य अर्थशास्त्र के शिक्षक को निकाल दिया गया है। उसकी किशोरावस्था में जो बाज़ार उसका मित्र था, ख़ुद ख़रीदी की स्थिति न होने पर भी जिसमें घूमना-भटकना उसे अच्छा लगता था, वही ‘बाज़ार’ उसका दुश्मन हो गया है। बेईमानी, मुनाफ़ाख़ोरी जैसी चालबाज़ियाँ वह समझने लगा था। चूँकि बाज़ार से ख़रीदी के लिए घर में गुंजाइश कम होती थी, धीरे-धीरे बाज़ार में उसका भटकना बंद-सा हो गया था। बाज़ार में भटकने के बजाय अब शाम को वह ‘भरकापारा वाचनालय’ जाने लगा था। महाविद्यालय सिर्फ़ वही नहीं है जो क़िले को सुधार कर बनाया गया है। बाज़ार की शक्तियों को समझकर, दोस्त से दुश्मन बनने की वह समूची प्रक्रिया ही वस्तुतः उसका महाविद्यालय है। इसकी क्रूरता और अमानवीय व्यवहार का सामना ज्ञान और विवेक से ही संभव है। ‘भरकापारा वाचनालय’ जिसका एक प्रतीक है। यह किस क़दर विस्मित करने वाला तथ्य है कि विनोद कुमार शुक्ल के यहाँ प्रेम पर केंद्रित कहानियाँ एकदम नहीं है। उनके यहाँ स्त्री—पत्नी, माँ, बहन और ऐसे ही दूसरे सामाजिक पारिवारिक संबंधों से बँधी हैं। वह ‘प्रिया’ रूप में इन कहानियों में कहीं नहीं है। ‘महाविद्यालय’ में माँ की कुछ मार्मिक छवियाँ विन्यस्त हैं। स्त्री के प्रसंग में उनकी दो कहानियों—‘आदमी की औरत’ और ‘मछली’ का उल्लेख ख़ासतौर से किया जा सकता है। ‘आदमी की औरत’ में जयनाथ के साथ वाचक भी बग़ीचे में है। लेकिन साथ होकर भी जैसे वह उसके साथ नहीं चल रहा था। संवाद में परस्पर विरोधी-सी लगती अनेक चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ सुनने को मिलती हैं। पार्क से अधिक खंडहर जैसे दिखने वाले उस पार्क में घास पर लेटे जयनाथ के ऊपर एक चील को मँडराते देख, वाचक उसी के पास टहलना शुरू कर देता है ताकि जयनाथ की तरह चील उसे मुर्दा न समझे। जयनाथ की पत्नी है कृष्णाबाई। वाचक ने मित्र की पत्नी को कभी देखा नहीं है। उसके बारे में सारी सूचनाएँ मित्र से ही मिलती रही हैं। यह सूचना भी उसे मित्र से ही मिली है कि पत्नी के दाहिने हाथ पर उसका नाम गुदा है—कृष्णाबाई, जिसे वह मिटवाना चाहता है। पत्नी के हाथ पर गुदा उसका नाम पति को गहरे आक्रोश से भर देता है। मित्र को मनःस्थिति को देखते, बिजली के खंभे पर कटीली हरी बेल को लिपटी देख वाचक जानबूझकर तय करता है कि बेल पर एक ‘कृष्णाबाई’ उगा हुआ है। मित्र जयनाथ आवेश में पत्नी का हाथ काट डालने का इरादा भी व्यक्त कर चुका है। सामने के तीन बेढंगे मकान उसे बिलकुल ‘कृष्णाबाई’ और सूअर बाई की बड़ी ‘ई’ की तरह लगते हैं। वाचक हाथ काटने के बजाए ब्लेड से अक्षरों को खुरचकर मिटाने का सुझाव देता है। घर पहुँचने पर बर्तन माँजती पत्नी से ही पैसे माँगकर वह नया ब्लेड लाया था। डरी-सहमी भागकर दूर जाती पत्नी को तैयार कर लेने के बाद पहले से बैठकर इस काम को करना चाहता है। फिर उसे लगता है कि खड़े होकर ही ठीक रहेगा। अपनी पीठ से उसे दबाकर वह गुदे हुए नाम को खुरचने की कोशिश करता है। कृष्णाबाई का केवल ‘कृ’ खुरचते-खुरचते उसके कपड़े ख़ून के दाग़ से भर जाते हैं। यही कपड़े धुले और साफ़ थे जो वह अब पहने था। घाव पर पेनीसिलिन का मरहम लगाने से अब वह ठीक है। पहले पत्नी ने इसके लिए मना किया था, फिर वह मान गई थी।
वाचक के साथ बैठकर अगली बार गंधक के तेज़ाब से गुदे हुए नाम को जलाने की बात तय होती है... ‘‘गंधक का गाढ़ा तेज़ाब पानी की तरह होता है। कोशिश करें तो आसानी से वह तेज़ाब उसे मिल जाएगा। घाव में दवा लगाने के बहाने वह पत्नी को बैठाएगा। थोड़ा प्यार करेगा। फिर गल्-गल् पूरा तेज़ाब शीशी का हाथ पर उड़ेल देगा। वह चीख़ेगी तो चीख़ने देगा। डरेगा नहीं। ज़्यादा ज़ोर से न चीख़े इसलिए उसका मुँह दबा देगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि उसके ऊपर तेजाब के छीटें न पड़ें।’’
कहानी में पति और वाचक जैसे समूची पुरुष-सत्ता और वर्चस्व का प्रतीक बनकर खड़े हैं। पत्नी कृष्णाबाई के हाथ पर गुदा उसका नाम, स्त्री के रूप में उसकी पहचान, मिटाने को वे सब कुछ करने को तैयार हैं। पति अंततः अपनी ज़िद छोड़ पत्नी के प्रति कुछ सदय होकर उसके सिलाई-कढ़ाई की बात जानने पर, उसे सुई-धागा और रंग-बिरंगे डोरे लाकर देता है। ग़िलाफ़ पर उसका अपना ही नाम काढ़ने के उसके अनुरोध को पहले वह किसी षड्यंत्र का हिस्सा समझ शंका की दृष्टि से देखती है। फिर, जैसा कि उसका स्वभाव है, वह तैयार हो जाती है। उसके कढ़े हुए नाम को देख वाचक की प्रतिक्रिया है : ‘‘ध्यान से देखा कि वाक़ई उसने बहुत साफ़ काढ़ा था। फिर मैं चला आया। मैंने सोचा जयनाथ पशु है। और मैंने, उससे दोस्ती तोड़ दी। मैंने तेज़ाब लाकर जयनाथ को कभी नहीं दिया...’’
जयनाथ उसे इसलिए पशु लगने लगता है, क्योंकि उसने पत्नी के प्रति अपने रवैये और सोच को बदल लिया है। वाचक का दंभ और पुरुष वर्चस्व की धमक अभी भी साँप की तरह फन उठाए खड़ी है। जिस तेज़ाब को न लाने की बात वह कहता है, बदले हुए संदर्भों में वस्तुतः उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं बची है।
पितृ और पुरुष सत्ता के वर्चस्व वाली यही दृष्टि ‘मछली’ में भी मौजूद है। वैष्णव परिवार में घर में गोश्त-मछली आदि बनना माँ को पसंद नहीं है। सिर्फ़ पिता हैं जो यह सब खाते हैं। माँ के प्रभाव में बच्चों की भी इसमें कोई रुचि नहीं है। नौकर ही यह सब काटता, बनाता। बाज़ार से लाई गई तीन मछलियों में से एक छिपाकर वाचक कुएँ में डालकर पालता है। लेकिन पिता के क्रोध का भय दिखाने पर नौकर की डाँट-डपट पर छिपाई गई मछली उसे लौटा देता है। उसे छिपाई गई मछली और कमरे में उदास अपनी दीदी में उसे गहरा साम्य दिखाई देता है : ‘‘मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की-हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही है। धीरे से दरवाज़ा खोलकर में अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी गई साड़ी को सिर तक ओढ़े, करवट लिए, सिसक-सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अँगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया...’’
जब छोटा संतू अँगोछे में छिपाई गई मछली को देने में आनाकानी करता है, घर में घुसते पिता की तेज़ और क्रोध भारी आवाज़ उसे सुनाई देती है। नौकर भग्गू को डाँटते हुए वह घर में घुसने पर नरेन के हाथ-पैर तोड़ देने की हिदायत देते हैं—आगे जो होगा, देख लेने के आश्वासन के साथ। वाचक को लगता है, पिता ने शायद दीदी को पीटा भी है। पूरे नहान घर में मछली की गंध भरी पड़ी है, जो पूरी बाल्टी पानी डालने के बावजूद दूर नहीं होती। मछली के सफ़ेद चमकीले पंख इधर-उधर फैले हैं। संतू के बाल काढ़ते हुए दीदी के सुंदर होने का उल्लेख वाचक ने किया है। लेकिन अपने सारे सौंदर्य और लगाव के बीच वह मछली की तरह लहरते और पितृसत्ता के पत्थर पर काटे जाने को अभिशप्त है। संतू और वाचक अपनी सारी कोशिशों के बावजूद मछली को बचा नहीं पाते। क्या दीदी की नियति भी इससे बहुत भिन्न है? पारंपरिक अर्थों में ‘मछली’ प्रेम कहानी नहीं है। लेकिन पितृसत्ता के वर्चस्व वाले समाज में प्रेम के प्रति किए जाने सुलूक के संकेत उसमें बहुत सघनता से विन्यस्त हैं।
•••
विकुशुयोग के अंतर्गत प्रकाशित अन्य लेख यहाँ पढ़िए : ‘नहीं होने’ में क्या देखते हैं | हिंदी का अपना पहला ‘नेटिव जीनियस’
'बेला' की नई पोस्ट्स पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए
कृपया अधिसूचना से संबंधित जानकारी की जाँच करें
आपके सब्सक्राइब के लिए धन्यवाद
हम आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे
बेला पॉपुलर
सबसे ज़्यादा पढ़े और पसंद किए गए पोस्ट
